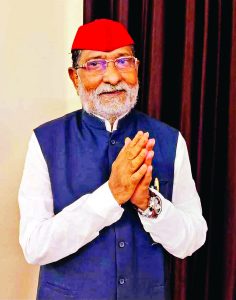चार राज्यों में विपक्ष को बड़ा झटका, पंजाब में चली झाडू
पाँच राज्यों में विधानसभा के चुनाव नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले रहे हैं। कड़े मुक़ाबले की स भावना के विपरीत चार राज्यों में (गोवा में एक सीट कम) भाजपा को और पंजाब में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। यह चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त देने वाले साबित हो सकते हैं, भले सपा सहित विपक्ष के कुछ दलों ने इन चुनावों में धाँधली का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की, तो उत्तराखण्ड में भी भाजपा ने लगातार दो चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद सभी दलों की सफ़ार्इ करते हुए पंजाब में ब पर जीत दर्ज करके नया इतिहास लिख दिया है। इस साल के आख़िर में अब गुजरात और हिमाचल जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ज़ाहिर है हारे हुए विपक्ष के सामने आगे भी चुनौतियाँ होंगी। फ़िलहाल पाँच राज्यों के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? बता रहे हैं विशेष संवाददाता राकेश रॉकी :-
पाँच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव नतीजे 2024 में किसी करिश्मे की उम्मीद कर रहे देश के पूरे विपक्ष के लिए बड़ा झटका हैं। भाजपा अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ताक़त और भरोसे के साथ आगे बढ़ेगी, जबकि खंडित विपक्ष के सामने यह चुनौती होगी कि वह अब करे क्या? हाँ, पंजाब में जीत दर्ज करके विपक्ष की ही एक पार्टी अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जगह लेने का ख़त्म ठोंक दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब तीसरे मोर्चे के लिए ज़्यादा मेहनत से काम करना होगा। यदि आने वाले महीनों में संगठन और नेतृत्व के मसले पर कांग्रेस ने वर्तमान स्थिति पर समझदारी और गहराई से अवलोकन नहीं किया, तो यह नतीजे कांग्रेस को और अँधेरे की तरफ़ ले जाने वाले साबित हो सकते हैं। हार के बाद विपक्ष ने इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धाँधली के आरोप लगाये हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पाँच राज्यों में जीत की इस बढ़त के बूते ही भाजपा की नैया 2024 में पार लगेगी, या वह सिर्फ़ इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है?
उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल से पहले कड़े मुक़ाबले के जो कयास थे, वो सभी ग़लत साबित हुए। भाजपा ने भले सन् 2017 के विधानसभा चुनाव से इस बार कम सीटें जीतीं; लेकिन फिर भी अपने बूते बहुमत हासिल कर उसने विपक्ष को पस्त कर दिया। समाजवादी पार्टी ने सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी तो की; लेकिन इतनी नहीं कि सत्ता के द्वार पर पहुँच सके। अखिलेश यादव के लिए यह चुनाव निश्चित ही बड़ा झटका है। भले सपा में उनके नेतृत्व के लिए कोई चुनौती पैदा न हो; लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी दोबारा परीक्षा होगी। हाँ, उन्हें पार्टी के भीतर यह साबित करना होगा कि उनकी नेतृत्व क्षमता पिता मुलायम सिंह यादव से कमतर नहीं है।
इस चुनाव के बाद भाजपा के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मज़बूत नेता के रूप में उभरे हैं और भविष्य में निश्चित ही वह भाजपा में देश के प्रधानमंत्री पद के मज़बूत दावेदार होंगे, जो कि वह चाहते भी हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के बाद समर्थकों और सोशल मीडिया ने उन्हें इस तरह पेश भी किया है। ‘सैफरॉन मोंक’ और इस तरह के अन्य नाम देकर उनके समर्थकों ने उन्हें भाजपा और संघ के बड़े चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। निश्चित ही आने वाले महीनों में योगी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रोजेक्ट करने की कोशिश होगी। आख़िर प्रदेश में पहली बार उनके नेतृत्व में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इन चुनाव नतीजों को भाजपा के भीतर मोदी-शाह समर्थकों ने ‘मोदी का करिश्मा बरक़रार है’ के रूप में पेश किया है। ज़ाहिर है मोदी समर्थक किसी भी सूरत में अगले चुनाव मोदी के नेतृत्व में ही लडऩा चाहते हैं। इन चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत से उनके लिए उनके लिए ऐसा करना आसान हो गया है। नतीजों से यह साबित हो गया है कि भाजपा में मोदी एक चुनाव जिताने वाले नेता हैं और उनका कोई विकल्प फ़िलहाल नहीं। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान जो भाजपा नेता सम्भावित हार-जीत को मोदी से जोडऩे से परहेज़ कर रहे थे, उन्होंने नतीजे आते ही इसे ‘मोदी की लोकप्रियता की जीत’ करार दिया।
उत्तराखण्ड में भले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार गये, भाजपा ने एकतरफ़ा बहुमत हासिल करके कांग्रेस को करारा झटका दिया है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि उत्तराखण्ड की सत्ता में उसकी वापसी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके मुख्यमंत्री पद के दावेदार दिग्गज नेता हरीश रावत तक अपनी सीट से हार गये, भले उनकी बेटी चुनाव जीत गयीं। उत्तराखण्ड में पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीती है। मुख्यमंत्री धामी के लिए निश्चित ही जीत के बावजूद यह नतीजा अफ़सोस वाला रहा; क्योंकि पार्टी ने उनके नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा था। यह वैसा ही हो गया, जैसा 2017 में हिमाचल के चुनाव में हुआ था, जब पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गये थे।
पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस ही नहीं पंजाब की राजनीति में स्थापित पंथक पार्टी अकाली दल (शिअद) को भी साफ़ करके रिकॉर्ड जीत हासिल की। कांग्रेस फिर भी कुछ सम्मानजनक 18 सीटें जीतने में सफल रही, अकाली दल और भाजपा के साथ-साथ कैप्टेन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और किसानों की नयी-नवेली पार्टी का तो बँटाधार ही हो गया। कॉमेडी के सरताज रहे भगवंत सिंह मान अब पंजाब की राजनीति के नये सरताज हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने खुलकर काम करने दिया, तो मान को ख़ुद को प्रमाणित करने का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर कहीं आम आदमी पार्टी नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली से चलाने की कोशिश की, तो अभी कहना कठिन है कि मान की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आम आदमी पार्टी की जीत से पंजाब में नये राजनीतिक युग की शुरुआत हुई है। अगले लोकसभा चुनाव में भी निश्चित ही इसका असर दिखेगा।
गोवा के नतीजे भी पूर्व अनुमानों के बिलकुल विपरीत रहे। वहाँ कांग्रेस को पक्की उम्मीद थी कि उसकी सरकार बनेगी। लेकिन नतीजों ने उसके उत्साह पर बर्फ़ डाल दी। वहाँ भाजपा बहुमत के क़रीब पहुँच गयी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल थी; लेकिन भाजपा ने जुगाड़ करके अपनी सरकार बना ली थी। गोवा में टीएमसी कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पायी; लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सत्ता हासिल करने का सपना एक बार फिर टूट गया। गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के भाजपा से बाग़ी हुए बेटे भी चुनाव हार गये।
उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट (अफ्सपा) की ज़ोरदार माँग थी और ऐसा लग रहा था कि वहाँ भाजपा को इसका नुक़सान होगा; लेकिन भाजपा ने सत्ता में वापसी की। वहाँ कांग्रेस पहले भाजपा को टक्कर देती दिख रही थी; लेकिन उसे चौथे नंबर से सन्तोष करना पड़ा। पिछले चुनाव में उसने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। मणिपुर में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन तो क्षेत्रीय दलों ने किया, जिनमें एनपीपी शामिल है।
भाजपा का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश में आसान जीत दर्ज करके भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। यदि भाजपा कुछ राज्यों में चुनाव हारती या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उसे बहुमत न मिला होता, तो विपक्ष के पास मुस्कुराने की वजह होती। भाजपा का लक्ष्य निश्चित ही अब 2024 है और इस मिशन के लिए वह पूरी ताक़त से मैदान में जुट जाएगी। भाजपा की चार राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की जनता ने उनकी सरकारों के काम पर मुहर लगायी है। भले विपक्ष इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धाँधली के आरोप लगाये हों; लेकिन मोदी बेफ़िक्र दिखते हैं और उनका कहना है कि हार के बाद जनता की समझदारी पर सवाल उठाना विपक्ष की पुरानी आदत है।
भले उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें पिछली बार से कम हुई हैं; लेकिन इसके बावजूद सरकार बना लेने का लाभ उसे लोकसभा के चुनाव में भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सीटें बढऩे के बाद भी लोकसभा चुनाव तक उसे अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। कारण यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को आज की तारीख़ में कोई बड़ी चुनौती नहीं है।
कांग्रेस किसे अध्यक्ष बनाती है और तीसरे मोर्चे से कौन उन्हें चुनौती देने सामने आता है? यह देखना दिलचस्प होगा। ज़्यादातर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भले आज स्थितियाँ भाजपा के हक़ में हों, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। वह राहुल गाँधी की दावेदारी को भी ख़ारिज़ नहीं करते; क्योंकि उनका कहना है कि वक्त अस्थायी रूप से ख़राब हो सकता है। लेकिन यदि कांग्रेस के दिन फिरे, तो राहुल गाँधी ही प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती के रूप में सामने होंगे।
इन विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की नज़र 2022 में ही होने वाले राष्ट्रपति पर भी थी। वह हर हालत में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जीतना चाहती थी, क्योंकि ऐसा न होने पर उसे राष्ट्रपति चुनाव में दिक़्क़त आ सकती थी। अब शायद ऐसा न हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस साल नवंबर में पूरा हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि भाजपा उन्हें फिर से अपना उम्मीदवार बना दे या किसी नये चेहरे को सामने ले आये।
भाजपा के नेता बार-बार कहते हैं कि पार्टी की सरकार 2040 तक रहेगी। कांग्रेस मुक्त भारत भी भाजपा का नारा है। राज्यों में कांग्रेस को योजनाबद्ध तरीक़े से किनारे करके भाजपा ने निश्चित ही राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए चुनौती कम की है। लेकिन इन दो वर्षों में देश के सामने कई चुनौतियाँ होंगी। महँगाई, अर्थ-व्यवस्था, बेरोज़गारी जिस स्तर पर हैं; उनसे मोदी सरकार को निपटना होगा।
मोदी बनाम योगी
भाजपा में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए अब कोई कशमकश होगी, इसकी फ़िलहाल तो कम ही सम्भावना है। लेकिन इसमें कोई दो-राय नहीं कि लगातार दूसरी जीत के बाद योगी भाजपा में नये शक्ति केंद्र के रूप में उभरे हैं। उनके समर्थकों की भाजपा और भाजपा से बाहर बड़ी फ़ौज है, जो उन्हें हिन्दुत्व के नये और कट्टर चेहरे के रूप में देखती है। मोदी के विपरीत योगी खुले रूप से हिन्दुत्व की बात करते हैं। ऐसे में उनकी लोकप्रियता हिन्दुत्व के समर्थकों में मोदी से कहीं ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की लगातार दूसरी जीत के बाद सोशल मीडिया पर जो सन्देश चलाये गये, उनमें से 80 फ़ीसदी योगी के समर्थन में थे और मोदी के समर्थन में महज़ 20 फ़ीसदी। आरएसएस के लोगों ने बड़ी संख्या में अपने ग्रुप्स में ‘प्रो-योगी’ सन्देशों को फैलाया। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हिन्दुत्व समर्थक राहुल श्रीवास्तव ने इस संवाददाता से बातचीत में कहा- ‘निश्चित ही हिन्दू धर्म की रक्षा पर फोकस करने की ज़रूरत है। योगी से बेहतर यह काम और कोई नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने प्रशासन भी चलाया और हिन्दुत्व की रक्षा का काम भी किया। हमें ऐसा ही नेता चाहिए।’
हालाँकि हिन्दुत्व के एजेंडे को विकास में बाधा मानने वालीं आईटी सेक्टर में काम कर रहीं मालिनी चक्रवर्ती ने कहा- ‘मुझे नहीं मालूम कौन उन्हें (योगी को) बहुत बेहतर प्रशासक मानता है? क्या आप भूल गये कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के समय उत्तर प्रदेश की नदियों में लोगों के शव के तैरते हुए मिले थे। लोगों के पास रोजगार नहीं और यह लोग ख़ामख़्वाह के मुद्दों में जनता को फँसाये हुए हैं।’ भले बहुत-से लोग राहुल की बात से असहमत हों, इसमें कोई दो-राय नहीं कि भाजपा से बाहर आम जनता में भी योगी के समर्थकों की कमी नहीं। यह चर्चा अभी से शुरू हो गयी है कि क्या अगले लोकसभा चुनाव तक योगी भाजपा के भीतर मोदी के लिए चुनौती बनेंगे? देश की राजनीति पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार एसपी शर्मा कहते हैं कि निश्चित ही योगी भाजपा के भीतर हिन्दुत्व का आज सबसे बड़ा चेहरा हैं। मोदी और शाह से भी बड़ा चेहरा। आरएसएस का उन्हें पूरा समर्थन है। ऐसे में आने वाले समय में वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो रहेंगे ही। मोदी दो बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हो सकता है कि आरएसएस उन्हें अब आराम देना चाहे। राजनीतिक गलियारों में यह बहुत चर्चा रही है कि मोदी-शाह की जोड़ी योगी को एक सीमा तक सीमित रखने की कोशिश करती रही है।
पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन कुछ महीने पहले स्थानीय निकाय के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और योगी में तल्खी की ख़बरें सामने आयी थीं। इसमें कोई दो-राय नहीं कि भाजपा में अभी भी मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और चुनाव जिता सकने की उनकी क्षमता का लोहा पार्टी के नेता मानते हैं। लेकिन भाजपा में सब कुछ भाजपा के हिसाब से नहीं चलता। आरएसएस का दख़ल टालने की हिम्मत भाजपा में कोई नहीं दिखा सकता। ऐसे में योगी के सिर पर आरएसएस का हाथ है, तो कुछ भी हो सकता है।
कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी
देश में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए यह विकट संकट की घड़ी है। उसके पास उम्रदराज़ हो रहीं सोनिया गाँधी का नेतृत्व है, और इसी साल के मध्य में उसे नया अध्यक्ष चुनना है। इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कुछ राज्यों में जीत मिली होती, तो राहुल गाँधी के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ़ हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। प्रियंका गाँधी ने निश्चित ही उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की पर कांग्रेस को वहाँ पिछली बार से कम सीटें मिलीं। कांग्रेस के संकट का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नतीजे आने के अगले ही दिन जी23 के नेताओं ने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के निवास पर बैठक करके चुनाव नतीजों को लेकर चिन्ता जतायी। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तो राहुल गाँधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया। ‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में नेताओं ने सचिन पायलट को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की माँग उठायी।
कांग्रेस के भीतर राहुल गाँधी को अध्यक्ष नहीं बनाने का समर्थन करने वाले भी प्रियंका गाँधी को अध्यक्ष बनाने के हक़ में दिखते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजों से उन्हें झटका लगा है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गाँधी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। एक नेता के रूप में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट भी किया। प्रियंका ने कितनी मेहनत की यह इस बात से साबित हो जाता है कि उन्होंने राज्य के कुल 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 370 में प्रचार किया। प्रियंका का यह प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ज़्यादा था। लेकिन कांग्रेस को इसका फल नहीं मिला और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि चुनाव शुरू होते ही यह भाजपा बनाम सपा हो गया था। ऐसे में कांग्रेस के पास यही विकल्प था कि वह उन सीटों पर पूरी ताक़त झोंक दे, जहाँ उसकी स्थिति मज़बूत थी। लेकिन माना जाता है कि प्रियंका गाँधी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव थे ही नहीं और उनकी कोशिश पूरे प्रदेश में पहुँचकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ज़मीन तैयार करना था। नतीजों से ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस के वोट बैंक में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ है। राहुल गाँधी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे। सारा दारोमदार प्रियंका गाँधी और उनकी टीम पर था। लेकिन पिछले दो विधानसभा चुनाव जीतने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू इस बार चुनाव हार गये। निश्चित ही लल्लू ऐसे नेता थे, जो योगी सरकार के पाँच साल के शासन के दौरान सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे थे। उन्हें योगी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते हुए प्रशासन ने कई बार जेल में डाला। कहा जाता है कि इस दौरान उन्हें 100 से ज़्यादा बार जेल में डाला गया। यदि ज़्यादा सीटें न जीतने के बावजूद कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा होता, तो निश्चित ही प्रियंका गाँधी की मेहनत सफल होती।
‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक, इस कमज़ोर प्रदर्शन के बावजूद प्रियंका गाँधी उत्तर प्रदेश में सक्रियता जारी रखने का फ़ैसला कर चुकी हैं। प्रदेश में भविष्य में उनके कार्यक्रम बनाने की तैयारी चुनाव नतीजे आने से पहली हो चुकी थी। इन कार्यक्रमों में उनका लक्ष्य संगठन को मज़बूत करना था। वह उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़ा फेरबदल करना चाहती थीं। अब ऐसा होगा या नहीं, पता नहीं; लेकिन यदि वह सक्रिय रहती हैं और संगठन पर फोकस करती हैं, तो 2024 के चुनाव में पार्टी को बेहतर स्थिति में पहुँचा सकती हैं।
कांग्रेस में एक और बड़ी समस्या हाल के महीनों में दिखी है। आम जनता में अनजाने में यह सन्देश गया है कि राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी के रूप में कांग्रेस के भीतर दो ख़ेमे हैं। सार्वजनिक मंचों पर प्रियंका गाँधी राहुल गाँधी को बतौर अध्यक्ष पूरा सम्मान देती रही हैं। लगता नहीं कि वह पार्टी के भीतर कोई समांनातर शक्ति केंद्र बनना चाहती हैं। राहुल गाँधी ने ही बतौर अध्यक्ष प्रियंका गाँधी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया था। लेकिन यह सम्भव है कि दोनों के साथ जुड़े अलग-अलग नेता राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी को कुछ इस तरह पेश करते हों और इससे यह सन्देश जाता हो मानों दोनों में नेतृत्व का मुक़ाबला है।
पार्टी के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उसे इसी साल नया अध्यक्ष चुनना है। संगठन के चुनाव का कार्यक्रम तय हो चुका है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि नये अध्यक्ष के लिए अब जी-23 समूह के नेता भी आवाज़ बुलंद करेंगे। वे पहले से ही गाँधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुनने की बात दबे अंदाज़ में कहते रहे हैं, भले अभी भी कांग्रेस का बड़ा बहुमत गाँधी परिवार के साथ ही जाना चाहे। इन चुनाव नतीजों से निश्चित ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा फैली है। भले उत्तर प्रदेश और मणिपुर को छोडक़र बाक़ी राज्यों में अभी भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। राहुल गाँधी अध्यक्ष पद फिर सँभालना चाहते हैं या नहीं? इस पर भी अभी सवालिया निशान है। ख़ुद राहुल गाँधी ने पिछले साल मंशा जतायी थी कि गाँधी परिवार से बाहर किसी नेता को अध्यक्ष बनाना चाहिए। निश्चित ही अगस्त या सितंबर में जब भी कांग्रेस नये अध्यक्ष का चुनाव करेगी, यह काफ़ी गहमागहमी वाला होगा। यह तय है कि गाँधी परिवार से बाहर अध्यक्ष बनाना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं होगा। इसका कारण है- किसी एक नेता के नाम पर सहमति बनाना। पार्टी के भीतर आज भी बहुमत गाँधी के साथ है। ऐसे में यही हो सकता है कि राहुल गाँधी के चुनाव में खड़े में होने की स्थिति में विरोधी ख़ेमा अपना उम्मीदवार उतारे। जैसा कि सोनिया गाँधी के सामने 9 नवंबर, 2000 के अध्यक्ष चुनाव में जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए थे। हालाँकि उन्हें हार झेलनी पड़ी थी।
कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए चुनौती का समय है और देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसे इसका सामना करती है? फ़िलहाल तो उसे पाँच राज्यों के चुनाव में हार पर सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाकर इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। पाँच राज्यों में पार्टी की हार के कारण बने दबाव के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 13 मार्च को हुई, तो ख़ुद सोनिया गाँधी के, और राहुल गाँधी व प्रियंका गाँधी वाड्रा के कांग्रेस छोड़ देने की पेशकश ने वहाँ उपस्थित नेताओं को सन्न कर दिया। सोनिया गाँधी की इस पेशकश का विरोध करने के लिए अपनी सीट से जो नेता सबसे पहले उठा, वह और कोई नहीं, गुलाम नबी आज़ाद थे। फ़िलहाल तय है कि कांग्रेस संगठन-चुनाव तक गाँधी परिवार की छत्रछाया में ही रहेगी।
यूपीए, तीसरा मोर्चा और आम आदमी पार्टी
देश के राजनीतिक पटल पर नज़र दौड़ाएँ, तो ज़ाहिर होता है कि हाल के महीनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ग़ैर-कांग्रेस तीसरा मोर्चा बनाने की क़वायद में दिखी हैं। उन्होंने इसे गम्भीरता से लिया है और वह देश के बड़े विपक्षी नेताओं, जिनमें शरद पवार और कुछ क्षेत्रीय क्षत्रप शामिल हैं; से मिली हैं। ममता चाहती हैं कि ग़ैर-कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करके भाजपा का मुक़ाबला किया जाए। अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा ठोस कुछ सामने नहीं आया है: लेकिन इसमें दो-राय नहीं कि देश में कई विपक्षी दल इस तरह के गठबंधन को ज़रूरी मानते हैं।
हालाँकि पाँच विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद पंजाब में बम्पर बहुमत हासिल करने वाली अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, उससे विपक्ष के ख़ेमे में दरार पड़ सकती है। कारण यह है कि पंजाब में जीत के तुरन्त बाद केजरीवाल के सिपहसालारों ने कहा कि पार्टी अब केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ेगी और देश भर में संगठन को फैलाएगी। ज़ाहिर है आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के रूप में किसी और नेता को आगे बढ़ाने का समर्थन क्यों करेंगी? पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को छोडक़र विपक्षी दलों में देश की तीसरी पार्टी बन गयी है, जिसकी एक से ज़्यादा राज्यों में सरकार है।
इन पाँच में से उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और पंजाब में सरकार बनायी। दूसरे राज्यों में भी वह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में सफल रही। ऐसे में ज़ाहिर है आम आदमी पार्टी अब साल के आख़िर में कुछ और विधानसभा चुनावों में अपनी क़िस्मत आजमाएगी। इनमें हिमाचल और गुजरात पर उसकी ख़ास नज़र है। आम आदमी पार्टी की ताक़त और बढ़ी, तो ज़ाहिर है उसका दावा 2024 के लोकसभा चुनाव उसका ग़ैर-कांग्रेस विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का दावा मज़बूत हो जाएगा।
ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी या दूसरे ग़ैर-कांग्रेसी वरिष्ठ नेता केजरीवाल को अपना अगुवा मानने को तैयार होंगे? यह बात ममता बनर्जी के मामले में नहीं कही जा सकती है, जिन्हें शरद पवार सहित अन्य बड़े नेताओं का समर्थन रहा है। हालाँकि उनके ख़ेमे में भी कुछ राजनीतिक दल हैं, जो यह मानते हैं कि कांग्रेस के बिना राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कांग्रेस ख़ुद ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसमें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस के अलावा कोई और हो।
वैसे भी कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए अस्तित्व में है और कुछ राज्यों में उसके सहयोगी दलों की सरकारों भी हैं। इस तरह मिलकर देखा जाए, तो भाजपा गठबंधन के बाद देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सरकारें हैं। हालाँकि भविष्य में भी इन सहयोगी दलों को अपने साथ बनाये रखने के लिए कांग्रेस को निश्चित ही मशक़्क़त करनी होगी। वैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल में संकेत दिये हैं कि वह यूपीए के साथ जा सकते हैं। चूँकि कांग्रेस पूरे देश में आधार रखती है। ऐसे में अगर 2024 तक उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है और वह लोकसभा चुनाव में 100 के पार चली जाती है, तो निश्चित ही उसका दावा मज़बूत हो जाएगा।
ज़ाहिर है पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद विपक्षी गठबंधन के तीन केंद्र बन गये हैं। इनमें से एक कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए है, जिसकी काफ़ी राज्यों में सरकारें हैं। ममता बनर्जी वाला सम्भावित गठबंधन है, जिसका अभी कुछ ख़ास नहीं हुआ है। अगर यह गठबंधन बना, तो ज़ाहिर है कि इस गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी। यह बात टीएमसी के दिग्गज नेता पहले ही साफ़ कर चुके हैं। तीसरा सम्भावित गठबंधन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बन सकता है। हालाँकि फ़िलहाल इसकी कोई चर्चा नहीं है और इस गठबंधन की कल्पना ही की जा सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, जो दो राज्यों में फैल चुकी है और बाक़ी कुछ राज्यों में जमीन तैयार कर रही है। उसका देश के किसी राज्य में किसी अन्य दल से गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी अरविन्द केजरीवाल को केंद्र में रखकर उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरह आगे बढऩा चाहती है। इसके लिए वह ज़्यादा-से-ज़्यादा राज्यों में अपना विस्तार करना चाहती है। ज़ाहिर है जब तीन शक्ति केंद्र विपक्ष में होंगे, तो उनका साथ आना सम्भव कैसे होगा।
कई मंत्री, मुख्यमंत्री धराशायी
उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव कई बड़े नेताओं पर भारी पड़े। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पंजाब के दो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता चुनाव हार गये।

“पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव हार गये। उन्हें आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जीवन ज्योत कौर ने हराया। सिद्धू के राजनीतिक करियर का यह पहला चुनाव है, जिसमें उन्हें हार झेलनी पड़ी।”
नवजोत सिंह सिद्धू

“चरणजीत सिंह चन्नी दो सीटों से लड़े; लेकिन दोनों पर ही हार गये। भदौड़ और चमकौर साहिब से वह मैदान में थे।”
चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री (अब पूर्व)

“पिछले पाँच महीने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बहुत भारी रहे हैं। चुनाव से ऐन पहले पंजाब लोक कांग्रेस बनाने वाले कैप्टन पटियाला सीट से चुनाव में हारे। भाजपा के दोस्ती भी उन्हें नहीं बचा पायी। आम आदमी पार्टी के अजीत पाल सिंह कोहली ने उन्हें क़रीब 19,000 मतों से मात दी।”
कैप्टन अमरिंदर सिंह

“पंजाब के दिग्गज नेता और पाँच बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का अपने मज़बूत गढ़ लम्बी में हार गये। बादल को आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुडिय़ा ने 11,000 वोट से हराया।”
प्रकाश सिंह बादल

“पिता की तरह बेटे को भी हार झेलनी पड़ी। शिअद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को जलालाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी के जगदीप कम्बोज ने 29,024 के बड़े अन्तर से हराया।”
सुखबीर बादल

“उत्तर प्रदेश में चुनाव से ऐन पहले मंत्री पद छोड़ सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्या फ़ाज़िलनगर सीट से हार गये। केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री (अब पूर्व) केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से सपा की पल्लवी पटेल से हार गये।”
स्वामी प्रसाद मौर्य
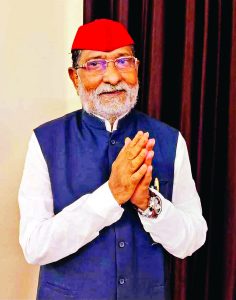
“उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी भी चुनाव हार गये। चौधरी बलिया की बांसडीह सीट से मैदान में थे। उन्हें भाजपा की केतकी सिंह ने हराया।”
रामगोविंद चौधरी

“उत्तराखण्ड में ही कांग्रेस चुनाव अभियान के चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सीट नहीं बचा पाये। रावत लालकुआँ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी थे।”
हरीश रावत

“गोवा में उप मुख्यमंत्री रहे चंद्रकांत कवलेकर हार गये। उन्हें केपे सीट से कांग्रेस के एलटन डी. कोस्ता ने 3,601 वोटों से हराया।”
चंद्रकांत कवलेकर

“उत्तराखण्ड में भाजपा तो अच्छे बहुमत से जीत गयी; लेकिन खटीमा सीट पर पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गये। धामी को कांग्रेस के भुवनचंद्र कापड़ी ने हराया। धामी इस चुनाव में भी भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा थे।”
पुष्कर धामी

“भाजपा को मिली जीत ऐतिहासिक है। यह मतदाताओं की जागरूकता की जीत है। एक दिन ऐसा आएगा, जब देश में जनता परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त करेगी।’’
नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री (नतीजों के बाद)

“पार्टी इन चुनाव परिणामों से सबक़ लेगी और वह देश की जनता के लिए काम करती रहेगी। ये नतीजे हमारी अपेक्षा के विपरीत हैं और पार्टी इसको लेकर अंतर्-मंथन करेगी।’’
राहुल गाँधी
कांग्रेस नेता

“पंजाब में पार्टी की जीत ऐतिहासिक है। यह दिल्ली में केजरीवाल मॉडल सरकार की सफलता है और इसी के आधार जनता ने जनादेश दिया है।’’
राघव चड्ढा
आप नेता