झारखंड:राँची में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखण्ड के राँची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नकदी जब्त की है।सूत्रों के मुताबिक, अभी तक 30 करोड़ रुपये के कैश बरामदगी का अनुमान है।
लोकसभा चुनाव के दौरान झारखण्ड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। केंद्रीय एजेंसी राँची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है।जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम मामले में झारखण्ड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के यहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। नोटो की गड्डियों का ढेर लगा हुआ है, जिसे देखकर अधिकारी भी चकरा गए हैं, जिन्हें गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं।30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी… आज ED की कार्रवाई में कॉंग्रेस विधायक दल के नेता व झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेट्री संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई…संजीव लाल के आवास पर
ईडी के अधिकारियों की ओर से जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में किस तरह से नोटों को रखा गया था। बैग, सूटकेस और पॉलिथीन में भरकर नोटों की गड्डियां रखी गई थीं। अधिकारी घर का कोना-कोना छान रहे हैं।ईडी ने करीब आधा दर्जन ठिकानों पर रेड डाली गई है।ED की ये कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी हो रही है। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखण्ड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था।बीते साल फरवरी में एजेंसी ने वीरेंद्र राम से लंबी पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने 21 फरवरी 2023 को राँची जमशेदपुर और झारखण्ड, बिहार और दिल्ली के कुछ अन्य स्थानों पर सर्च अभियान चलाया था, जिसके बाद उसे पकड़ा था। एजेंसी ने तमाम परिसरों से 30 लाख का कैश, 1.5 करोड़ रुपए के गहने, कई करोड़ की 8 लग्जरी कारें और एसयूवी, मेट्रो और अन्य शहरों में फ्लैट व बंगले जब्त किए थे।
झारखण्ड में मंत्री के पीएस के नौकर के घर से मिला नोटों का अंबार
रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी
*अमेठी ये इनको बनाया उम्मीदवार
नई दिल्ली:नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने अपना पत्ता खोल दिया है।रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे।
कांग्रेस के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति’ की बैठक में लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली से और किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किया गया है।
बताते चलें कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है। कैसरगंज से करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये वहां से वर्तमान सांसद बज्र भूषण सिंह के बेटे हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 17वीं लिस्ट
नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की 17वीं लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बहु प्रतीक्षित रायबरेली सीट और कैसरगंज के उम्मीदवारों के नाम से पत्ते खुल गए हैं। जैसी कि चर्चा थी, उसी के अनुसार कैसरगंज सीट से पार्टी ने बृजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट दी गई है। वहीं पार्टी ने रायबरेली के उम्मीदवार के नाम का भी खुलासा कर दिया है। पार्टी ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है।
बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से मैदान में उतारा है।दरअसल, करण भूषण सिंह (Karan Bhushan Singh) बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। 13 दिसंबर 1990 को जन्मे करण भूषण एक बेटी और एक बेटे के पिता हैं।वह डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, करण भूषण ने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से बीबीए व एलएलबी की डिग्री हासिल की है।साथ ही ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया है।वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। साथ ही सहकारी ग्राम विकास बैंक (नवाबगंज, गोण्डा) के अध्यक्ष भी हैं। यह उनका पहला चुनाव है।मालूम हो कि फरवरी, 2024 में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया था।अब वह लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं, करण भूषण के बड़े भाई प्रतीक भूषण सिंह बीजेपी के विधायक हैं। ब्लॉक प्रमुख की राजनीति से शुरुआत करने वाले दिनेश प्रताप सिंह वर्तमान में योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री हैं। पहली बार 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान परिषद का चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी से चुनाव हार गए. बाद में 2007 में बसपा के प्रत्याशी के तौर पर तिलोई विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वहां भी इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा।उसके बाद दिनेश प्रताप ने कांग्रेस में किस्मत आजमाई।कांग्रेस पार्टी में दिनेश प्रताप को कद, पद और ख्याति, तीनों ही मिले। पहली बार 2010 में एमएलसी बने और 2011 में उनकी भाभी जिला पंचायत अध्यक्ष बनीं। फिर 2016 में दोबारा एमएलसी बने और इनके भाई जिला पंचायत अध्यक्ष बने। उनके एक भाई 2017 में हरचंदपुर से कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। फिर 2019 के आते-आते इनका कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया और ये बीजेपी में शामिल हो गए ।बीजेपी में शामिल होने के बाद इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के सामने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और करीब पौने 4 लाख वोट हासिल किए, लेकिन चुनाव हार गए. सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को 1,67,178 वोटों से हराकर रायबरेली की अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की थी। दिनेश प्रताप सिंह 3,67,740 वोट हासिल करने में कामयाब रहे, वहीं सोनिया गांधी 5,34,918 वोटों के साथ फिर से सीट जीतने में कामयाब रही थीं. इस सीट पर सपा और बसपा ने उनका समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार का जब दूसरा टर्म शुरू हुआ तो इन्हें स्वतंत्र राज्य मंत्री बनाया गया और इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और आज इनका नाम एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया है।
सिमडेगा की सलीमा टेटे बनी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान
नई दिल्ली: एफआईएच प्रो लीग के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा हुई। टीम बेल्जियम और इंग्लैंड चरण में भाग लेगी। टूर्नामेंट में टीम की कमान झारखंड की सिमडेगा की सलीमा टेटे संभालेंगी।सलीमा को हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं टीम की उपकप्तान नवनीत कौर हैं।बता दें कि भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की चार बेटियों का चयन हुआ है।
जिनमें निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमार और दीपिका सोरेंग के नाम शामिल है।बेल्जियम चरण 22 मई को शुरू होकर 26 मई को समाप्त होगा। जबकि इंग्लैंड चरण 1 जून से शुरू होकर 9 जून तक चलेगा।सलीमा टेटे 2017 में बेलारूस के खिलाफ राष्ट्रीय टीम में पदार्पण की थी।2018 के युवा ओलंपिक खेलों में भारत ने सलीमा की कप्तानी में रजत पदक जीता था।2021 में वह भारतीय ओलंपिक टीम का हिस्सा थी।
चुनावों में झूठ का खेल
*पैसे लेकर चुनाव में गलत जानकारियां फैलाते हैं बिचौलिये !
इंट्रो- चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां और उनके उम्मीदवार जीतने की कोशिश में साम, दाम, दंड, भेद के हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और आचार संहिता लागू होने के बावजूद यह खेल चोरी-छिपे खूब चलता है। इसी खेल का हिस्सा है- पैसे लेकर ग़लत सूचनाएँ और अफवाहें फैलाना। ‘तहलका’ एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में चुनावों के दौरान जानबूझकर गलत सूचनाएँ प्रसारित करने से उत्पन्न चुनौतियों का खुलासा किया है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कम्पनियाँ और सक्रिय बिचौलिये पैसे के लिए करते हैं। तहलका एसआईटी की रिपोर्ट :-
‘चुनाव के दौरान गलत सूचना फैलाने का काम करने के लिए हमें किसी तथ्य या सुबूत की आवश्यकता नहीं है। हम गलत सूचना फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाते हैं और उन्हें तुरंत बंद कर देते हैं। भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) इन फर्जी (बॉट) खातों का पता नहीं लगा सकता है। यह हमारी गारंटी है, जो सोशल मीडिया व्यवसाय में हमारे 14 वर्षों के अनुभव की देन है। 2019 के आम चुनाव में भी मैंने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले एक बड़े राजनेता के पक्ष में एक बड़े हिंदी समाचार चैनल को पांच लाख रुपये का भुगतान करके उससे एक ट्वीट पोस्ट कराने में कामयाबी हासिल की।’
ये बातें नकली ग्राहक बने ‘तहलका’ के रिपोर्टर से सीओज डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी, जिसका मुख्यालय द्वारका (नई दिल्ली) में है; के निदेशक गौरव मग्गो ने कहीं। अपने सहयोगी प्रबंधक अक्षय कुमार के साथ गौरव ने उत्तर प्रदेश से 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर स्वतंत्र रूप से लड़ने वाले हमारे (तहलका रिपोर्टर के) काल्पनिक उम्मीदवारों के लिए डिजिटल मार्केटिंग रणनीति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में गौरव से मुलाकात की।
जैसे ही भारतीय चुनाव आयोग ने 2024 के आम चुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की, उसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ‘4एम’- बाहुबल, धन, गलत सूचना और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लगाम कसने की चुनौती पर जोर दिया। पिछले अंक में ‘तहलका’ ने बाहुबल के दुरुपयोग और एमसीसी उल्लंघन को लेकर पड़ताल की थी। इस बार हम अपना ध्यान गलत सूचनाओं के खतरे पर केंद्रित कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारी रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग कम्पनियां सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएँ फैलाकर या दुष्प्रचार करके चुनाव मैदान में उम्मीदवारों की सहायता कर रही हैं और भारत के चुनाव आयोग की आंखों पर पट्टी बांधकर प्रभावी ढंग से पैसे लेकर उम्मीदवारों की मदद करने के लिए तैयार हैं।

‘तहलका’ की पड़ताल तब शुरू हुई, जब हमने चुनाव के दौरान गलत सूचना फैलाने के कारोबार में शामिल डिजिटल मार्केटिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों से संपर्क किया। सबसे पहले हमारा ध्यान दिल्ली में मुख्यालय वाली सीओज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पर गया। उनके संपर्क विवरण के साथ हमने संचार शुरू किया। कंपनी की ओर से आये एक फोन कॉल के कारण ‘तहलका’ रिपोर्टर ने शीघ्रतापूर्वक दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में गौरव मग्गो से मिलकर मुलाकात की। बैठक के दौरान रिपोर्टर की मुलाकात कम्पनी के दो प्रतिनिधियों से हुई- गौरव मग्गो और अक्षय कुमार, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक प्रचार में अनुभवी जोड़ी है।
‘तहलका’ रिपोर्टर ने उन्हें एक काल्पनिक परिदृश्य प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि हमारे (रिपोर्टर के) कई उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से 2024 के लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं और उन्हें डिजिटल प्रचार की आवश्यकता है, जिसमें उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के बारे में गलत सूचना फैलाना भी शामिल है। गौरव ने सोच-समझकर ‘तहलका’ रिपोर्टर को अपनी रणनीति से अवगत कराया। काल्पनिक उम्मीदवार के विरोधियों के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए फर्जी खाते बनाने की बात कही। महत्वपूर्ण रूप से उसने रिपोर्टर को आश्वासन दिया कि वह इन खातों को तुरंत बंद कर देगा। इस प्रकार भारत चुनाव आयोग की सतर्क नजर से उम्मीदवार बच जाएंगे। इसके लिए गौरव ने डिजिटल मार्केटिंग व्यवसाय में अपने 14 वर्षों के व्यापक अनुभव पर जोर देकर रिपोर्टर को निश्चिंत रहने के लिए आश्वस्त किया।
गौरव : अकाउंट बनेगा मिस-इंफॉर्मेशन डालोगे…, और बन्द…?
रिपोर्टर : फिर वही बात है ना! …इमिडेटली बंद हो गया, तो ईसी (चुनाव आयोग) की नजर में आ जाएगा?
गौरव : नहीं; दैट विल बी। (यह हो जाएगा।) …सब चीजें होती हैं। …कैसे बनती है, हम जानते हैं। हम तो ऑलरेडी उसमें हैं। ..हम तो 14 साल से कर ही रहे हैं, वो काम।
रिपोर्टर : 14 साल से हैं आप डिजिटल मीडिया में?
गौरव : हां जी!

जब रिपोर्टर ने गौरव को बताया कि उनके पास अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के बारे में सुबूत या तथ्य नहीं हैं, तो उसने यह कहकर रिपोर्टर को आश्वस्त करने की कोशिश की कि गलत सूचना फैलाने के लिए उन्हें तथ्यों या सुबूतों की आवश्यकता नहीं है। गौरव ने कहा कि इसके लिए ब्लैक कॉलर या फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसने रिपोर्टर को मौजूदा जानकारी का लाभ उठाने और अनिश्चितताओं का फायदा उठाने का सुझाव भी दिया।
रिपोर्टर : नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, …अपोजिशन कैंडिडेट (विपक्षी उम्मीदवार) की मिस-इंफॉर्मेशन जो हम करेंगे, वो कैसे करेंगे?
गौरव : अच्छा, इंफॉर्मेशन? सर! देखो, इंफॉर्मेशन तो आप ही दोगे कि ये चल रहा है, उसको चलाएंगे।
रिपोर्टर : आइडिया तो आप दे सकते हो?
गौरव : आइडिया तो मैं तब दे सकता हूं, जब आपको कुछ भी न पता हो उस आदमी के बारे में, कि उसका कोई मिसलीड (गलत उपयोग) किया है या नहीं भी किया है। या आपको पता है कि इस चीज में वो फंसा था। वो पुराने मुद्दे उठा के लाओ।
रिपोर्टर : मान लीजिए, कोई डाक्यूमेंट्स नहीं मिलता है, एविडेंस नहीं मिलता है, तो?
गौरव : एविडेंस की जरूरत नहीं होती है इसमें; …तभी तो ब्लैक कॉलर होता है। तभी तो उसे ब्लैक कॉलर कहते हैं।
अब रिपोर्टर ने गौरव से पूछा कि वह स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों के बारे में गलत सूचना कैसे फैलाएंगे, जिस पर उन्होंने प्रसार रणनीति और लक्षित सोशल मीडिया अभियानों के लिए बॉट्स का उपयोग करने का उल्लेख किया।
रिपोर्टर : मुझे एक चीज बताइए, क्या मिस-इंफॉर्मेशन का काउंटर मिस-इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता?
गौरव : हो सकता है। मगर यहाँ पे मिस-इंफॉर्मेशन अगर एक बार आ गयी, तो आप एक नेगेटिव इमेज बंदे की नहीं बना सकते। मान लीजिए, मैंने आज आपको बताया कि फलाने ने जाके ऐसा काम किया, तो पहले इंप्रेशन क्या चला गया?- अरे इसने तो रेप कर दिया! एक आदमी पर ऑलरेडी ब्लेम गेम चल रहा है। …तो आप काउंटर कैसे मारोगे? आप अपने आपको क्लीयर करोगे या पहले काउंटर मारोगे? …समझ रहे हो आप? पहली बार आप क्लीयर करोगे। चार दिन बाद काउंटर मार दूंगा मैं। …भाई! पहले अपने को क्लीयर भी तो करोगे, फिर चार दिन बाद काउंटर मार दो।
रिपोर्टर : वो काउंटर क्या होगा? मैं जानना चाह रहा हूं। चार तो आपने कर दिया, पॉजिटिव वीडियो बना के?
गौरव : अब जैसे उन्हें पता है, इस आदमी की यहां पे ये चोरी पकड़ी गयी है…।
रिपोर्टर : कोई नहीं, पकड़ी गयी; मान लो क्लीयर आदमी हैं, …दोनों आदमी चार हैं। …मैंने यही सवाल किया आपसे मिस-इंफॉर्मेशन का?
गौरव : मिस-इंफॉर्मेशन पर मिस-इंफॉर्मेशन मारेंगे।
रिपोर्टर : वो कैसे मारोगे? यही सवाल है मेरा।
गौरव : अकाउंट बनेगा, मिस-इंफॉर्मेशन डालोगे, और बंद।
अब गौरव ने प्रचार के लिए व्हाइट और ब्लैक कॉलर के रूप में वर्गीकृत फर्जी खातों का उपयोग करने का सुझाव दिया। उसने दावा किया कि सभी पार्टियां अभियान के लिए फर्जी अकाउंट बनवाती हैं, यह आश्वासन देते हुए कि वे चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगी। गौरव ने राजनीतिक रणनीतियों में बॉट्स के व्यापक उपयोग पर प्रकाश डालते हुए व्हाइट और ब्लैक कॉलर खातों और अभियानों में उनके उपयोग के बीच अंतर पर चर्चा की। गौरव ने बॉट्स की अस्थायी प्रकृति के बारे में भी बताया और आश्वासन दिया कि वे चुनाव से पहले बन्द हो जाएंगे, साथ ही पता लगाने से बचते हुए प्रभाव को अधिकतम करने के लिए रणनीतिक समय के महत्व पर जोर दिया।
गौरव : अच्छा, इसमें भाई सब दो चीजें होती हैं। एक ब्लैक कॉलर, एक व्हाइट कॉलर। …आपको ब्लैक कॉलर चाहिए या व्हाइट?
रिपोर्टर : दोनों करवा दो। …वैसे डिफरेंस क्या है?
गौरव : डिफरेंस ये होता है कि अकाउंट्स होते हैं। …खुलते हैं, बंद होते हैं। व्हाइट कॉलर ये होता है कि आपके अकाउंट से ही हो रहा है।
रिपोर्टर : जेनुइन (असली) होंगे?
गौरव : जेनुइन होंगे।
रिपोर्टर : ब्लैक वाले फेक होंगे?
गौरव : जी!
रिपोर्टर : तो फेक अकाउंट से करवाना ठीक होगा?
गौरव : वो आप देख लो। लोग तो कराते हैं। एक्चुअली क्या होता, कुछ टाइम के लिए अकाउंट खुलता है, फिर बंद हो जाता है। बॉट्स हो गया, बॉट्स क्या होता है कि प्रमोशन आपके उस अकाउंट से हो रही है, रीच (पहुंच) बढ़ाने के लिए।
रिपोर्टर : हूं, ओके।
गौरव : कि जैसे अब मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं। …बहुत सारे तो मैंने बॉट्स कर दिये। …यूपी के अंदर में जो लोगों को रीच मिल रही है, वो आपको एक अच्छा इंपैक्ट मिल रहा है उसका। …मल्टीपल जो हैं ना, सोसायटीज बनी हुई हैं। फेसबुक के ऊपर ग्रुप बने हैं, उस पर हम लोग रीच बनाते हैं।
रिपोर्टर : ये हो कि फेक अकाउंट पकड़ में न आये?
गौरव : नहीं होगा, वो एक बार होकर बन्द हो जाता है।
रिपोर्टर : देखिए, आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन हैं, …मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आदर्श आचार संहिता)। इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए।
गौरव : वो चीज सर आपने देखनी है। इसमें ये सब चीज होती है। ये xxxxx जी भी करते हैं, ये xxxxx पार्टी भी करती है। ये सब कर रहे हैं।
रिपोर्टर : अच्छा; आप जितने कंडीडेट्स की (बात) कर रहे हो, वो फेक तरीके से कर रहे हैं?
गौरव : कर रहे हैं। …क्यूंकि उनका तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उनका तो मई, 24 के बाद है। …आचार संहिता से पहले कर लोगे, तो अच्छा होगा।
रिपोर्टर : आचार संहिता के बाद बोला था। इलेक्शन अनाउंस होने से पहले।
गौरव : हां, तो आचार संहिता से पहले-पहले कर लो।
रिपोर्टर : अब तो आचार संहिता लगी हुई है?
गौरव : लगी हुई है; लेकिन अकाउंट मिलते हैं ना! …तो उसमें दिक्कत क्या है? उसे प्रमोट करो, उसमें कोई फेक अकाउंट नहीं है। …मेरे हैं पांच लाख सब्सक्राइबर्स। …वो मैं उन्हें अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो कोई बुराई थोड़ी है उसमें!
रिपोर्टर : आप कह रहे हो ना कुछ टाइम के लिए प्रमोशन बंद हो जाते हैं?
गौरव : वो तो इसलिए कह रहा, कभी ईसी ने पूछा कि आपने क्या-क्या प्रमोशन किये? इस वजह से लोग क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। जब इलेक्शन है, उस टाइम पर किया, फिर बंद कर दिया।
रिपोर्टर : अच्छा; बॉट अकाउंट के लिए ये है कि इलेक्शन तक वो ऑपरेट, फिर?
गौरव : बंद हो जाएंगे, हाँ जी! इलेक्शन से दो दिन पहले सब बंद हो जाता है; …48 ऑवर (घंटे) पहले। बट, 48 घंटे पहले सब प्रिंट और ऑनलाइन बंद होता है। कमेंट्रीज बंद होती है; …बट व्हाट्सएप चलता है।
नकली ग्राहक बने ‘तहलका’ के रिपोर्टर की चिंताओं का समाधान करने की कोशिश करते हुए गौरव ने आश्वासन दिया कि हमारे काल्पनिक उम्मीदवारों के लिए बने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। हालांकि गौरव ने उल्लेख किया कि उम्मीदवार मतदान के दिन भी एसएमएस संदेश भेजते हैं। गौरव ने चुनावी उम्मीदवारों को डिजिटल रूप से प्रचारित करने, 2024 के आम चुनाव के लिए आठ दावेदारों को संभालने में अपनी कम्पनी के अनुभव को साझा किया, जिसमें xxxx पार्टी के दिल्ली के xxxx और xxxx भी शामिल हैं।
गौरव : कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन (चुनाव के दिन) भी लोग एसएमएस भेजते हैं।
रिपोर्टर : ये देख लीजिए कि फेक अकाउंट जो है, वो इलेक्शन कमीशन की पकड़ में न आये?
गौरव : वो सब, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। (यह समस्या नहीं है।)
जब गौरव से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के उनके पिछले अनुभव के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि उनकी कम्पनी ने अतीत में कई उम्मीदवारों के डिजिटल प्रचार का काम संभाला है। गौरव ने दावा किया कि वर्तमान में वह 2024 के आम चुनावों में भाग लेने वाले आठ उम्मीदवारों के लिए अभियान का प्रबंधन कर रहा है।
रिपोर्टर : आपको पॉलिटिकल एक्सपीरिएंस है?
गौरव : हम लोगों ने किया है।
रिपोर्टर : हमें ऐसे लोग चाहिए, जो इलेक्शन कैम्पेन कर चुके हों। ..पार्टीज के लिए कंडीडेट्स के लिए मार्केटिंग कर चुके हैं।
गौरव : दिल्ली में ऑलरेडी xxxxx जी हैं। xxxx पार्टी से xxxx जी हैं; …तो इन लोगों का काम कर चुके हैं, और कर भी रहे हैं। xxxxx जी, xxxx हैं xxxx से, उनका ऑलरेडी हम कर रहे हैं।
रिपोर्टर : ये लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं?
गौरव : दे आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। (वे चुनाव लड़ रहे हैं।)
रिपोर्टर : तो उनका क्या-क्या देख रहे हैं आप?
गौरव : सर! उनका सारा सोशल मीडिया हैंडलिंग; …इवन थाउ (चाहे) हमारे पास टीम है, जो ऑलराउंड (पूरी दौर) इन्हीं के साथ रहती है। वो हमें क्लिप भेजते हैं और हम फटाफट उनको अपलोड करते हैं। …तो जितनी भी रिलीज है, सब चीजें हम लोग हैंडल कर रहे हैं।
रिपोर्टर : फिलहाल 2024 में कितने कैंडिडेट्स हैं आपके पास?
गौरव : अभी सर! हमारे पास आठ कंडीडेट्स हैं।
रिपोर्टर : सब दिल्ली के हैं? …किस-किस पार्टी के हैं?
गौरव : एक xxxxx हो गया, xxxx है। एक xxx पार्टी बनी है, उसके 8-10 लोग हैं; वो भी अदर्स में हैं।
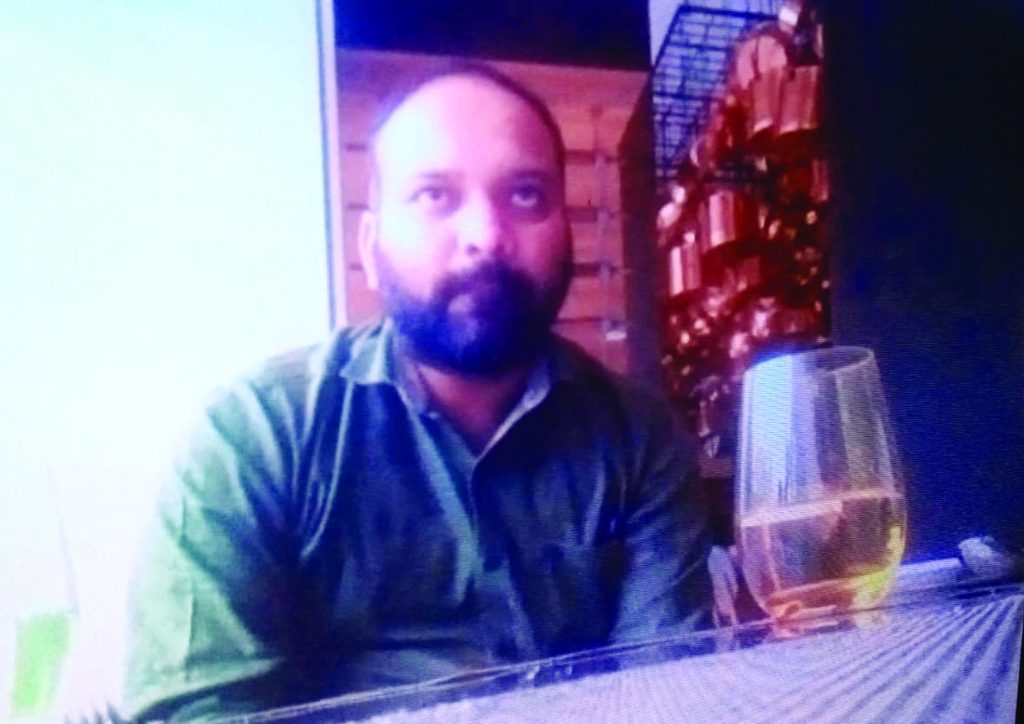
यह पूछे जाने पर कि क्या गौरव हमारे उम्मीदवारों (काल्पनिक) के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अनुकूल ट्वीट की व्यवस्था कर सकते हैं? गौरव ने ऐसे कार्यों के लिए प्रमुख हिंदी समाचार चैनलों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। उसने तीन साल पहले के एक पिछले उदाहरण का हवाला दिया, जहां (बकौल गौरव के) उसने पांच लाख रुपये में एक प्रमुख हिंदी समाचार चैनल के माध्यम से एक वरिष्ठ राजनेता के लिए सकारात्मक ट्वीट की सुविधा प्रदान की थी।
रिपोर्टर : अच्छा; कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई इनके फेवर में ट्वीट कर दे?
गौरव : सर! वो तो चैनल से करवाना पड़ेगा, …न्यूज चैनल से।
रिपोर्टर : न्यूज चैनल से मतलब?
गौरव : जो बड़े-बड़े न्यूज चैनल हैं, xxxx, xxxx एक्सेट्रा (इत्यादि), अगर हम इनको बोलते हैं, तो आपको अच्छा ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी।
रिपोर्टर : लेकिन वो क्यूं ट्वीट करेंगे?
गौरव : वो इसलिए करेंगे, क्यूंकि उनको पे किया जाएगा। (पैसे दिये जाएंगे।)
रिपोर्टर : एक ट्वीट का कितना होगा, अमाउंट?
गौरव : सर! वो मुझे पूछकर पता चलेगा।
रिपोर्टर : आपने पहले भी कराया होगा?
गौरव : सर! मैं जो लास्ट किया था, xxxx से करवाया था; वो मेरे से ऑलरेडी सर्विस लेते हैं एसएमएस की, तो उन्होंने एक पर्सन के लिए किया था। …तो पांच लाख लिया था।
रिपोर्टर : xxxx ने लगाया था?
गौरव : तीन साल पहले xxxx के लिए।
रिपोर्टर : xxxxx के लिए तीन साल पहले?
डिजिटल युग में राजनीतिक अभियानों को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रिटी समर्थन का लाभ उठाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हुए गौरव ने शुल्क के लिए अपने उम्मीदवारों के पक्ष में ट्वीट करने के लिए बॉलीवुड सितारों या प्रभावशाली लोगों को शामिल करने पर भी सहमति व्यक्त की। उसने प्रचार और ट्वीट के लिए बॉलीवुड सितारों और अन्य मशहूर हस्तियों के बीच अंतर पर भी चर्चा की।
रिपोर्टर : सर! मैं ये चाहता हूँ कि कोई सेलिब्रिटी बॉलीवुड का इनके फेवर में ट्वीट कर दे?
गौरव : बोलिए, किससे करवाना है? बोलिए सर! ये तो इंफ्लूएंसर (प्रभावशाली व्यक्ति) का ही काम है।
रिपोर्टर : आप ही बता दो; लेकिन बॉलीवुड स्टार अलग चीज हो गया, सेलिब्रिटी अलग चीज।
गौरव : वैसे दोनों एक ही लेवल का होता है।
रिपोर्टर : बॉलीवुड स्टार की ज़्यादा मास अपील (सामूहिक
निवेदन) है।
गौरव : आपको चाहिए किस लेवल का? वो मैटर करता है।
रिपोर्टर : आप करा दीजिए xxxxx का।
इसके बाद गौरव ने अपनी प्रभावशाली सेवा की पेशकश की, जिसमें उसने सनी आर्य उर्फ तहलका भाई और एल्विश यादव जैसे सेलिब्रिटीज को निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के लिए भी पेशकश की, जिनमें से प्रत्येक ने सात लाख रुपये का शुल्क लिया। रिपोर्टर ने राजनीतिक ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए चुनाव अभियानों पर प्रभावशाली बैठकों के प्रभाव के बारे में पूछताछ की।
गौरव : बाकी हमारा इंफ्लूएंसर (प्रभावशाली व्यक्ति) का भी काम है। …आपको अगर इंफ्लूएंसर चाहिए, तो मिल जाएगा।
रिपोर्टर : इंफ्लूएंसर की अगर हम कोई मीटिंग करवा दें इलेक्शन में, उससे फायदा होगा?
गौरव : जी! आपको ब्रांडिंग चाहिए। …अब मैं एल्विश को कहूं, तू जरूर ब्रांडिंग कर यूपी में, तो क्यूं नहीं करेगा?
रिपोर्टर : एल्विश वो तो फंसा हुआ है केस में?
गौरव : फंसा, अब तो क्लीयर हो गया। …अब तहलका भाई का नाम सुना होगा आपने?
रिपोर्टर : तहलका भाई? हां।
गौरव : सन्नी आर्य। …आप कहोगे, तो मैं अरेंज करवा दूंगा।
रिपोर्टर : उसके चार्जेज क्या होंगे सर?
गौरव : सर! डिपेंड करता है, वो क्या चार्ज करेगा।
रिपोर्टर : मान लीजिए एल्विश है, तहलका है…!
गौरव : सर! एल्विश, तहलका भाई तो बड़े हैं। …7-7 लाख लेते हैं।

अब गौरव ने अपनी वित्तीय योजना के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें गलत सूचना फैलाने, उम्मीदवार के अनुकूल ट्वीट करने, प्रभावशाली लोगों का उपयोग करने और लोकसभा चुनाव के लिए वायरल वीडियो के खर्च शामिल हैं। उसने स्पष्ट किया कि इस काम के लिए वह हमसे (रिपोर्टर से) 10 लाख रुपये लेगा। उसने प्रभावी सोशल मीडिया आउटरीच के लिए कम-से-कम 10 लाख रुपये के बजट की आवश्यकता पर जोर दिया।
गौरव : दिस इज एन एमपी इलेक्शन, …राइट? (यह संसदीय चुनाव है, …ठीक?) …जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। इस वक्त जो एमपी का बजट लेकर सब चल रहे हैं, वो 5-10 लाख रुपीज का है।
रिपोर्टर : सोशल मीडिया का?
गौरव : सब कुछ। …एसएमएस, व्हाट्सऐप, वॉयस; …ये मानकर चलिए, कम-से-कम 10 लाख का बजट। इसके नीचे कोई फायदा ही नहीं। …रीच ही नहीं मिलेगी। आपको हमें न 10 लाख का बजट देना, …उसमें हम आपको कैटेगरीज कर देंगे कि इतना व्हाट्सऐप जाएँगे, इतना एसएमएस, इतनी वॉयस जाएगी। इनता फेसबुक होगा, और इतना इंफ्लूएंसर लेगा।
रिपोर्टर : और इसमें वीडियो वायरल करवाना हो तो, …ट्विटर पे ट्रेंड करवाना हो? री-ट्वीट्स करवाने हों?
गौरव : हो जाएगा, सब हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट करवाना हो, तो अलग लगेगा।
इस चुनावी मौसम में गलत सूचनाओं ने एक नया तरीका अपनाया है, जो भारतीय मतदाताओं के साथ इस तरह से जुड़ रहा है, मानो सच हो। यह सूक्ष्म; लेकिन सम्मोहक है, जिससे इसे पहचानना और विनियमित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। यह कहा जाना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में घृणास्पद भाषण और दुष्प्रचार अभियान करने वाले कोई अजनबी लोग नहीं थे। लेकिन इस पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने वाली तकनीक ने तीव्र गति से इतनी क्रान्ति ला दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भारत के सबसे बड़े चुनाव (लोकसभा चुनाव) को बाधित करने की धमकी देता है।
सन् 2019 के लोकसभा चुनाव को सोशल मीडिया चुनाव करार दिया गया था। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव एआई-संचालित चुनावों के खतरनाक उदय के गवाह बन सकते हैं। आधिकारिक एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि 2024 में औसत भारतीय मतदाता को गलत चुनावी सूचनाओं के सबसे अधिक जोखिम का सामना करना पड़ेगा। एआई-जनित सामग्री के चलते वास्तविकता और गलत सूचनाओं में अन्तर करने में ज्ञान का सहारा ही एक सही माध्यम है। इन फर्जी खबरों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही सोशल मीडिया कम्पनियों के लिए इस चुनावी मौसम में चुनौती और बढ़ गयी है। फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को रोकने के प्रयासों के बावजूद डिजिटल मार्केटिंग कम्पनियाँ पैसे के लिए गलत सूचनाओं का प्रचार करने को तैयार हैं।
‘तहलका’ एसआईटी का यह खुलासा ‘4एम’ में से एक और ‘एम’- गलत सूचना को उजागर करता है; जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के आगे एक कठिन चुनौती बनकर खड़ा है। ‘तहलका’ ने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बारी भारत चुनाव आयोग की है।
मुसलमान को सेकुलर पार्टियों ने ही सियासी मंजर से गायब कर दिया
लेखक-खालिद सलीम
सियासत के महरीन खिलाड़ी हैरान है की 2024 के आते-आते हिंदुस्तानी सियासत से मुसलमान को इस तरह बेदखल कर दिया जाएगा की जैसे हिंदुस्तानी सियासत में उनका कोई रूल ही नहीं रह गया है अजीब बात यह है कि एक वह वक्त भी था जब हिंदुस्तानी सियासत में मुसलमान को सबसे ज्यादा अहमियत का हमिल समझा जाता था और कहा जाता था के मुसलमान हिंदुस्तानी सियासत का एक ऐसा मोहरा है कि वह जिधर भी पलट जाए और जिस सियासी पार्टी के हक में वोट कर दें हिंदुस्तान में इस पार्टी की हुकूमत होगी यह बात गलत भी नहीं है आजादी के 60 साल तक हिंदुस्तानी मुसलमान ने बादशाह ग र का रुल अदा किया है और कांग्रेस पार्टी को मुसलमान नेऔर दूसरी सेकुलर पार्टियों को हिंदुस्तान में हुकूमत करने के मौके दिए हैं लेकिन पिछले 20 सालों से हिंदुस्तानी सियासत से मुसलमान को ऐसे बाहर कर दिया गया है कि जैसे हिंदुस्तान में उनका कोई वजूद ही नहीं रह गया है और बीजेपी की 10 साल की हुकूमत में तो मुसलमान को स्टेट और सेंट्रल से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है हैरत की बात यह है कि भाजपा ने तो अपने सियासी फायदा के लिए और अपने सियासी नजरियात के तहत मुसलमान को ना पार्लियामेंट के टिकट दिया ना किसी असेंबली का टिकट दिया लेकिन अफसोस तो उन सियासी सेकुलर पार्टियों पर है जो मुसलमानो के वोट से विधानसभाओं और सेंट्रल में अपनी हुकूमतें बनती आई है उन्होंने भी पिछले 10 सालों के इलेक्शन में मुसलमान को विधानसभाऔ में लोकसभा में राज्यसभा में बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है और अब2024 के सिलेक्शन में अगर सरसरी नजर भी डाली जाए तो साफ नजर आ जाएगा की तमाम सेकुलर पार्टियों चाहे वह कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो और बिहार में तेजस्वी यादव या सेकुलरिज्म का दम भरने वाले और अब बीजेपी के साथी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हो इन सब ने मुसलमानो को टिकट देने में आनाकानी की है अजीब बात यह है कि महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अखाडी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है वहां दलितों के मशहूर लीडर प्रकाश आंबेडकर जो के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते हैं उन्होंने विंचित बहुजन अखाडी इलजाम लगाया है कि वह मुसलमानौ को टिकट देने से इसलिए डर रही है की कहीं हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए बताया जाता है की महाराष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरों से मिलने के लिए आई और उन्होंने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी मुसलमान को टिकट न दिया जाए और कांग्रेस की लीडरशिप ने उनकी यह बात मान ली है पिछली लोकसभा में मुसलमान पार्लियामेंट की तादाद सिर्फ 23 थी और आजादी के बाद यह तादाद सबसे कम थी हमें लग रहा है कि इस मर्तबा मुसलमान पार्लियामेंट मे 23 की तादाद को भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर ऐसा होगा तो यह हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और यहां के सेकुलरिज्म पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाएगा हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस मर्तबा बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है और वह हुकूमत बना लेती है तो आइंदा हिंदुस्तान में इलेक्शन जम्हूरियत डेमोक्रेसी एक पुराना किस्सा बन जाएगा अगर ऐसा है तो इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार अगर कोई होगा तो वह हिंदुस्तान की नाम निहाद सेकुलर पार्टियों होगी जिन्होंने यहां की अलपसंकयक को नजरअंदाज किया है खासतौर से मुसलमान को जिनके वह वोट से कामयाब होती आई है और सता के मजे लूटती रही है कांग्रेस ने अपनी गलतियों से अभी भी सबक हासिल नहीं किया है वह बीजेपी और आरएसएस के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है उसे जिधर बीजेपी और आरएसएस ने धकेल ना चाहा कांग्रेस इस तरफ बढ़ती चली गई उसे अंदाजा भी नहीं हुआ है कि उसके साथ क्या हो रहा है कांग्रेस के नौजवान लीडर राहुल गांधी की ईमानदार शख्स है और उन्होंने मेहनत भी बहुत की है लेकिन वही मिसाल दी जा सकती है कि एक चना क्या भाड़ झुकेगा कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और जो कुछ बच्चे खींचे हैं उनसे भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह कब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दें सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी उस इज्जत को कैसे वापस लाईगी जो नेहरू गांधी मौलाना आजाद सरदार पटेल जी जैसे बड़े मा पुरुषों ने कांग्रेस की इज्जत को चार चांद लगा दिए थे मुसलमान और दूसरे अल्पसंख्यक ग्रुप कांग्रेस से बहुत ही मायूस है और उम्मीद करते हैं कि वह डटकर फिर का प्रस्तावों का मुकाबला करेगी हां एक उम्मीद यहां कि अल्पसंख्यकों को बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से है फिरका परस ताकतों से लड़ रही है और उनकी सियासत ढकी छुपी नहीं है वह जो करती हैं खुल्लम-खुल्ला करती हैं और जो बोलते हैं साफ बोलते हैं उन्हीं से बहुत सी उम्मीद है कि वह हिंदुस्तान की सियासत को उन ताकतों से आजाद कराएंगी जो हिंदुस्तान को तोड़ने और बिखरने पर आमादा है
लवली की जगह देवेंद्र यादव के हाथों में कमान, बने दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष
नई दिल्ली: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली कांग्रेस को अंतरिम अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे बाद पार्टी ने नए नाम पर मुहर लगा दी है। देवेंद्र यादव को दिल्ली कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व चांदनी चौक क्षेत्र से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने सोमवार को इलाके के आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त बैठक की। इस मौके पर उन्होंने लवली के बयान की चर्चा किए बिना कहा कि आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के बीच हुए समझौते में कोई दरार नहीं है।
उधर, उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने होर्डिंग्स व बैनरों, पोस्टरों व झंडों पर राहुल गांधी के फोटो के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का भी फोटो लगाया है। उन्होंने मतदाताओं को लुभाने के लिए आप की उपलब्धियों का भी बखान करना शुरू किया है। लिहाजा उन्होंने अपना प्रचार अभियान पूरी तरह इंडिया गठबंधन को समर्पित कर दिया है।
प्रदेश कांग्रेस में पूरा दिन छाया रहा सन्नाटा
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को सन्नाटा पसरा रहा। पार्टी कार्यालय में एक भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यालय में कोई बैठक नहीं हुई। प्रदेश कार्यालय में सोमवार को केवल वॉर रूम में ही चहल-पहल दिखी। यहां सोशल मीडिया टीम के सदस्य चुनाव प्रचार करने की रणनीति के संबंध में चर्चा करते दिखे। इसके अलावा कार्यालय परिसर से लेकर तभी सभागारों व कक्षों में सन्नाटा छाया था।
अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की वजह
अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस आलाकमान को भेजे त्यागपत्र में 10 कारण गिनाए थे। इनमें उन्होंने सबसे अधिक प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर निशाना साधा था। उनके व्यवहार को ही उन्होंने त्यागपत्र देने का मुख्य कारण बताया था। ये हैं कारण 1. प्रदेश प्रभारी बाबरिया ने प्रदेश स्तर के साथ-साथ ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की अनुमति नहीं दी। दिल्ली में 150 से ज्यादा ब्लॉकों में कोई अध्यक्ष नहीं है। 2. प्रदेश इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी। इसके बावजूद पार्टी ने आप के साथ गठबंधन किया।
- गठबंधन के तहत सात सीटों में कांग्रेस को सिर्फ तीन सीटों चुनाव लड़ने के लिए आवंटित की गईं। 4. तीनों सीटों पर प्रदेश के नेताओं को टिकट नहीं दिए गए। 5. उत्तर-पश्चिम दिल्ली और उत्तर-पूर्व दिल्ली सीट पर पार्टी की नीतियों के लिए पूरी तरह से अजनबी नेताओं को टिकट दिए गए। 6. उदित राज और कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाने के संबंध में औपचारिक रूप से पहले प्रदेश इकाई को सूचित भी नहीं किया गया। 7. उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्व दिल्ली के उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और उनके खिलाफ उन्होंने प्रदेश कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 8. प्रदेश प्रभारी ने पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार और अन्य को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रभारी ने स्थिति को शांत करने की जगह सार्वजनिक बैठकों में भी पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, राजकुमार चौहान, पूर्व विधायक भीष्म शर्मा व सुरेंद्र कुमार के साथ कई बार तीखी नोकझोंक की। 9. उत्तर-पश्चिम दिल्ली के उम्मीदवार ने अपमानजनक और पार्टी विरोधी बयान देकर स्थिति को खराब किया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया और उन्हें कई लिखित संदेश भेजे हैं, जिसमें विभिन्न स्थानीय नेताओं को निलंबित करने के लिए कहा गया है। 10. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार पार्टी लाइन और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं की मान्यताओं का उल्लंघन कर रहे हैं।
बिहार में सड़क हादसा ; 6 बारातियों की मौत,3 घायल
बिहार : भागलपुर-कहलगांव मुख्य मार्ग एनएच-80 पर घोघा के आमापुर के पास सोमवार की देर रात भीषण दुर्घटना हो गई। एक बारात गाड़ी पर गिट्टी लदा हाईवा पलट गया, जिसमें दबकर स्कॉर्पियो में सवार छह बाराती की मौके पर मौत हो गई।तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना रात करीब 11.30 बजे की है। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल, भागलपुर भेजा गया है।पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।घटना की सूचना मिलने के बाद घोघा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एनएच-80 का निर्माण कर रही एजेंसी की जेसीबी और अन्य संसाधनों से मलबा हटाने का काम शुरू कराया।
मलबे में से निकाले गए लोगों में तीन घायल थे, शेष छह लोगों की मौत हो चुकी थी।मौके पर आसपास के लोगों की काफी भीड़ जमा हो गयी।घायलों ने स्थानीय लोगों को जो सूचना दी, उसके अनुसार बारात मुंगेर के हवेली खड़गपुर के गोवड्डा से पीरपैंती के खिदमतपुर जा रही थी।तीन स्कॉर्पियो से बाराती एनएच-80 पर भागलपुर से कहलगांव की ओर जा रहे थे। विपरीत दिशा से यानी कहलगांव की ओर गिट्टी लदा हाईवा आ रहा था। इसी दौरान हाईवा अनियंत्रित हो गया और स्कॉर्पियो पर पलट गया।
बीच में चल रही स्कॉर्पियो पूरी तरह से हाईवा की जद में आ गई। हाईवा में जितनी गिट्टी भरी थी, वह स्कॉर्पियो पर आ गई और उसमें दबकर बारातियों की मौत हो गई। मृतक में दो बच्चे भी शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो के आगे-पीछे चल रही दो अन्य स्कॉर्पियों किसी तरह हाईवा से बच निकली। वरना और भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। बताया गया कि घटनास्थल पर सड़क निर्माण कार्यचल रहा था। सड़क एक ओर से करीब तीन से चार फीट तक ऊंची थी, जिस पर ट्रक गुजरने के कारण वह अनियंत्रित होकर बाराती वाहन पर पलट गया।घोघा में बारात गाड़ी की दुर्घटना में घायल 60 वर्षीय कैलाश दास सहित अन्य घायलों को सोमवार रात लगभग 1.30 बजे मायागंज अस्पताल लाया गया।सबकी स्थिति गंभीर बतायी जा रही है। घायल कैलाश ने बताया कि लगभग एक घंटे तक वे लोग मलबे में दबे रहे।सांसें अटकी रहीं।गाड़ी में बैठे अन्य लोगों के साथ वह भी अपना होश खो बैठे थे, लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें यह अहसास हुआ कि कोई हमें निकाले। अंदर दम घुट रहा था। साथी बाराती की क्या स्थिति थी, कौन जिंदा रहा और कौन नहीं, यह भी पता नहीं चल पा रहा था।
गति और तकनीकी विकास में सूचनाओं का महत्व

कल्पना मनोरमा
सावधान! सूचनाओं में शांति, धर्म, अहिंसा, सन्मार्ग, आनंद और ऐश्वर्य तलाशती दुनिया को मालूम होना चाहिए कि सूचना मात्र जानकारी, इत्तिला, नोटिस, विज्ञापन, प्रतिवेदन भर है। स्थाई समाधान नहीं। स्थायित्व की चाहना रखने वालों को सूचनाओं के इतर सोचना, देखना और समझना होगा।
‘रोटी कपड़ा और मकान’ आदमी की मूलभूत ज़रूरतें हैं। इन्हीं तीन के फेर में चकरघिन्नी बने आदमी को हमेशा दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती रही हैं। इस में कोई दो राय नहीं। कम से कम भारतीय नागरिकों के सामने रोटी के जुटान में पेंचीदगी का आलम हमेशा बना ही रहा है। आज भी आय के न्यूनतम साधनों में जीवन यापन करने वालों की भारत में कोई कमी नहीं। जिन्हें अपने और अपनों का जीवन उगने और फलने-फूलने लायक बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बावजूद इसके आधुनिक विकसित काल में इन तीन ज़रूरी तथ्यात्मक साधनों को जुटाने में जटिलता कम नहीं हुई बल्कि अब कठिनाइयों का ग्राफ इंसान के कद से ऊँचा उठ गया है।
आज इंसान के सामने सूचनाओं के अंबार में से अपने लायक उपयुक्त सूचना तलाश लेने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलत सूचनाओं के फेर में पड़ जाए तो वह अपने जीवन की यात्रा वैसे ही बना लेता है, जैसे- फ्लाई ऑवर पर एक गलत टर्न लेने से मिनटों की यात्रा घंटों में परिवर्तित कर मुसाफ़िर सही मुकाम पर पहुँचने से चूककर चुक जाता है।
‘सूचना’ शब्द तब भी शायद इतना महत्वपूर्ण न बन पड़ा होगा जब इसे खोजा गया होगा। कहा जाता है कि यह आकस्मिक व सामान्य ‘सूचना’ शब्द 20वीं सदी की शुरुआत में लैटिन मूल इन्फोर्मेम “रूपरेखा या विचार” से गढ़ा गया था और आज मायाजाल की तरह नहीं, अमरबेल की तरह इंसानों के ऊपर पसर चुका है।
समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजीकरण (Socialization) के लिए सूचना का महत्व उतना ही जरूरी है जितना अन्य क्रियान्वयन…। क्योंकि सुन्दर समाज बनाने की प्रक्रिया जटिल है। इसके गठन में किसी एक प्रकार की भूमिका या विधि से काम नहीं चल सकता। सामाजीकरण की प्रक्रिया में मनुष्य के व्यवहार व्यवस्था में स्थिरता और पूर्वानुमेयता पैदा करने के लिए सामाजिक नियंत्रण शामिल है, और इन प्रक्रियाओं में सूचनाओं का महत्व अपनी तरह काम करता है। समाज अपनी सुगंध और संस्कृति को बनाये और बचाए रखने के लिए सूचनाओं को तरजीह देता है। सामाजिक प्रविधियों के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों और सामाजिक कौशल को सीखने की चल रही प्रक्रिया को सीखा जा सकता है। सूचनाओं के माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति-रिवाज़, गतिविधियाँ इत्यादि को एक से दूसरे तक पहुँचाता रहा है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजीकरण के माध्यम से ही होता है। और सूचना सामाजीकरण में सहयोगी साबित होती आ रही है।
धर्म के चार स्तंभ सत्य, तप, पवित्रता एवं दान बताए गए हैं। इन्हीं पर इंसानी जीवन की छत टिकी होती है लेकिन आज सूचना का महत्व जीवन से ज्यादा दिख रहा है। दिन-रात इंसान के कान से लग कर कोई न कोई बोलता जा रहा है। पहले भी लोग हाथों में अखबार और कान से रेडियो लगाए फिरते रहते थे लेकिन तब सूचनाओं में सत्य की प्रामाणिकता कौतुहल से ज्यादा होती थी। दाल में नमक भर कौतुहल मिलाकर उसे रोचक बनाया जाता था।ताकि पाठक को आनंद आये और वह मुद्दे की बात तक पहुँच सके। लेकिन अब सूचनाओं में सब उलट चुका है। अब दाल में नमक भर सत्यता मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जबकि सूचना ज्ञान, संचार और मूल्य व गुणवत्ता निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस माध्यम से व्यक्तियों और समाज के प्रति अवगत कराकर निर्णय लेने में मदद करता है। वर्तमान समय में सूचनाओं में सत्य की कसौटी बिना जाँचे अगर फेर में पड़ गए तो हालत क्या होती है….सब जानते और समझते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं।
सूचना के समानधर्मी शब्द डेटा, तथ्य, बुद्धिमत्ता, सलाह को माना जाता है। क्या आज की सूचनाओं में इन सभी का समावेश दिखता है? कभी-कभी लगता है कि इंसान को सूचना की जरूरत पड़ी ही क्यों? लेकिन फिर लगता है कि सूचना जनता का अधिकार है और यह इंसान को सूचित कर आगाह करने, जानकारी देने की एक कामयाब विधि है। कहा जाता है कि सूचना के मद्देनज़र भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया, जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कभी भी और कोई भी जानकारी ले सकता है। शर्त बस इतनी कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। क्या इस बात को माना जा रहा है?
आज धरती से लेकर आसमान तक बस खबरें ही ख़बरें सुनाई-दिखाई पड़ रही हैं। प्रचारित खबरों में न गुणवत्ता की परवाह है, न तथ्यों की कसौटियाँ, न गोपनीयता और न अखंडता के प्रति प्रतिबद्धताएँ । न ही जनमानस के आगे परोसी जा रही सूचनाओं में किसी भी प्रकार के सिद्धान्ताकी की कोई गुंजाइश समझ आती। जबकि सूचना सुरक्षा के मूल सिद्धांत गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता है। गोपनीयता के सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्तिगत जानकारी को उजागर न करते हुए किसी की निजता को निजी रखना होता है। यह सिद्धांत ये सुनिश्चित करना है कि दी जा रही सूचना केवल उन व्यक्तियों के लिए दृश्यमान होगी जिन्हें संगठनात्मक कार्यों को करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।
वर्तमान समय में सूचना सुरक्षा खतरों की सैकड़ों श्रेणियाँ और लाखों ज्ञात खतरे हैं। आज सिर्फ राजनीति ही नहीं, उद्यम, सुरक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, मनोरंजन, शादी-ब्याह आदि के प्रति आधी-अधूरी सूचनाएँ खतरे के निशान के ऊपर उपलब्ध हैं। गति और तकनीकी विकास के महान दौर में सुरक्षा उपायों में हर व्यक्ति यानी शहरी, ग्रामीण, व्यवसायी, नौकरीपेशा, किसान, मेहनतकश यहाँ तक भिक्षा के माध्यम से जीवन-यापन करने वालों को भी कम-ज्यादा समझौते करने पड़ रहे हैं। कौन कब ठगी के जाल में फँस जाए,किसी को नहीं पता।
तुलसीदास ने मन की तुलना पीपल के पत्तों से की है। मन को इसी तरह से होना भी चाहिए। मन का स्थूल होना जीवन को कीचड़ के समान बना देता है। जिस तरह पुरवा, पछुआ, दक्खिनी, उत्तरायणी माने तनिक सी भी हवा के सिहरन से पीपल के पत्ते डोल उठते हैं, हमारे मन को भी इसी तरह संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन पीपल के सादगी भरे लेन-देन उच्छृंखल नहीं, सुगठित होते हैं। सूचनाओं के इस महान समय में क्या हम इस बात को ठीक से समझ पा रहे हैं?
क्या हम अपने आस-पास दुष्प्रचार फैलाने से कम से कम अपने को रोक पा रहे हैं? या दुष्प्रचार के इस अमानवीय समय में अपनों को समझा पा रहे हैं कि हर एक सूचना को सत्य, तप, पवित्रता एवं दान की कसौटी पर देखने के बाद, सबसे बड़ा धर्म मानवता पर कस कर देखने के वे पक्षधर बने रहें ? आख़िर हम चाहते क्या हैं? क्या कभी इस प्रश्न को सोचते हैं?
अंत में बस इतना ही कि सूचनाओं का यह महान दौर जो भड़भूजे की तरह हमें भून देने पर आमादा है, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? और कितनी होनी चाहिए? क्योंकि सही सूचनाओं से ही कुछ उपयोगी विमश हो सकता है, अन्यथा समय की बर्बादी पर लगाम लगानी होगी। इंसान को समझना होगा कि वर्तमान में परोसी जा रहीं सूचनाएँ, उसके लिए कितनी उपयोगी और कितनी अनुपयोगी हैं। किन-किन सूचनाओं का स्वागत करना चाहिए और किन का बहिष्कार। विकास के मोह में फँसा जीवन अब हंस-विवेक की माँग कर रहा है।
(लेखिका साहित्यकार, विचारक एवं सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं।)
कांग्रेस को तगड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति
मध्यप्रदेश : गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और झटका लगा है।इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है।यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अक्षय बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है।
कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है।
बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे।नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल दिन आखिरी दिन था। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ‘ऑपरेशन’ को अंजाम दे दिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होगा और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी।
मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने बीते 24 अप्रैल को ही अपना नामांकन दाखिल किया था। हलफनामे में बम ने अपनी कुल प्रॉपर्टी 57 करोड़ रुपए बताई। खास बात यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार के कोई कार नहीं है। वह 14 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं। पिछले दिनों गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार निलेश कुम्भानी का नामांकन एक दिन पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था।उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया था।कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापिस ले ली थी।ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए थे।चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया।











