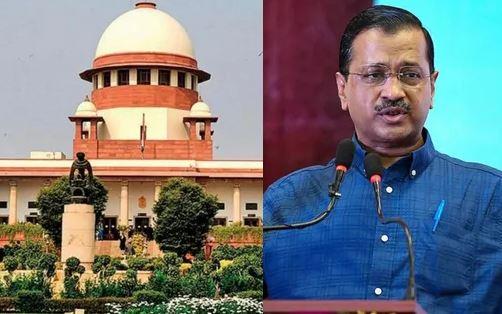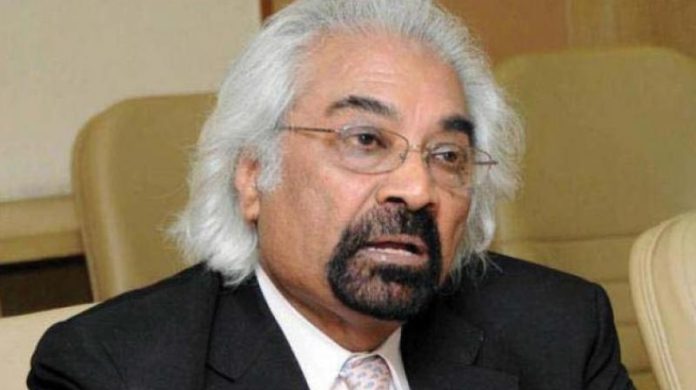उत्तराखंड: जंगलों में लगी भीषण आग बेकाबू होते जा रही है।गढ़वाल हो या कुमाऊं। यहां कई जगहों पर जंगलों में आग की लपटें नजर आ रही हैं।एक जगह अगर आग पर काबू पाया जाता है तो फिर दूसरी जगह से खबर आती है कि वहां जंगलों में भीषण आग भड़क गई है।सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन कई जगहों पर नाकाफी साबित हो रहे हैं।
इस बीच पौड़ी जिले के डीएम ने जंगल की आग बुझाने के लिए वायुसेना से मदद मांगी है और एक पत्र लिखा है। इसके बाद भारतीय वायुसेना का विमान पौडी के लिए रवाना हो गया है।सबसे भीषण आग उन वनक्षेत्रों में लगी है जहां चीड़ के पेड़ हैं।गर्मी का मौसम होने की वजह से कई जंगलों में लीसा निकाला जा रहा है और यहां आग और तेजी से भड़क रही है। उत्तराखंड वन विभाग के मुताबिक, कुमाऊं मंडल में आग लगने के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, वहीं गढ़वाल मंडल में भी आग लगने की काफी घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
आग लगने से राज्य की अमूल्य वन संपदा खाक हो रही है।कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में सबसे अधिक आग लगने की घटनाएं सामने आई थी जहां फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं।इसके अलावा अल्मोड़ा। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जैसे जिलों के कई जंगली क्षेत्र भी आग की चपेट में आए थे जिनमें से बागेश्वर और चंपावत के अधिकांश इलाको में आग पर काबू पा लिया गया है।
वहीं गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहां नरेंद्र नगर, उत्तरकाशी, मसूरी, कोटद्वार, टिहरी गढ़वाल, गोपेश्वर, रूद्रप्रयाग जैसे कई वन्यक्षेत्र आग की चपेट में आ चुके हैं।इनमें से कुछ जगहों पर आग पर काबू पा लिया गया है जबकि कुछ जगहों पर अभी भी आग धधक रही है।उत्तराखंड वन विभाग के मुताबिक, आग लगने से 749.6375 रिजर्व फॉरेस्ट एरिया (हेक्टेयर) प्रभावित हुआ है।
उत्तराखंड के वनाग्नि नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने आजतक से बात करते हुए बताया कि कुमाऊं मंडल में आग लगने से सबसे अधिक प्रभावित अल्मोड़ा जिला हुआ है जबकि गढ़वाल मंडल में पौड़ी जिला सबसे अधिक प्रभावित है।निशांत वर्मा के मुताबिक, आग लगने के जो भी मामले सामने आए हैं उनमें से अधिकांश मामले सरफेस फायर के हैं, जिसमें घास, पत्ती, पिरूल पर आग लगती है और इससे नुकसान कम होता है, वहीं ग्राउंड फायर में सर्वाधिक नुकसान होता है जिसके मामले कम दर्ज किए हैं।निशांत वर्मा के मुताबिक, ‘कुमाऊं मंडल में अभी भी बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल के कुछ वन्य क्षेत्रों में आग लगी हुई है जबकि चंपावत और पिथौरागढ़ के अधिकांश इलाकों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है।वहीं गढ़वाल मंडल में भी जिन जगहों पर आग लगी थी वहां भी काबू लिया गया है और फिलहाल पौड़ी जिले में आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं।’
रविवार को पौड़ी तहसील में एक 65 वर्षीय एक महिला जंगल में आग बुझाने की कोशिश के दौरान झुलस गई थी जिसे एम्स ऋषिकेश में लाया गया था जहां उसकी मौत हो गई। वहीं अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में भी दो लीसा श्रमिकों की मौत हो गई है। जंगलों में आग बुझने का एकमात्र सहारा बारिश ही नजर आ रही है। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य में 8 मई तक बारिश होने की संभावना है, जो 11 मई से तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा, इससे जंगल की आग बुझाने में मदद मिल सकती है।सिंह ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में 7 मई से और गढ़वाल क्षेत्र में 8 मई से बारिश शुरू हो जाएगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह का नोटिस देकर जंगल की आग की नियमित निगरानी के निर्देश जारी करने को कहा। इस दौरान सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह के लिए सभी प्रकार के चारे को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश देने को भी कहा।
इसके अलावा, शहरी निकायों को जंगलों में या उसके आसपास अपने ठोस कचरे को जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कहा गया है।धामी ने शनिवार को राज्य में हो रही जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आपस में समन्वय स्थापित कर एक ऐसा तंत्र बनाएं जिससे जंगल की आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंडवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, ”वन संपदा हमारी विरासत है, जिसे हमें हर कीमत पर सुरक्षित रखना है।’