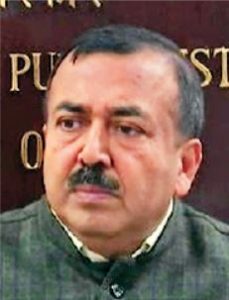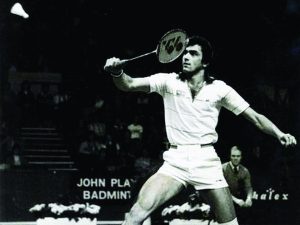बाल श्रम एक बड़ी सामाजिक समस्या है। इसी पर रोक के लिए पूरी दुनिया में हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक 20 साल पहले अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने बाल श्रम ख़त्म करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्रवाई लिए वर्ष 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की थी। बता दें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा काम कराये जाने को बाल श्रम में रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य ऐसे बच्चों को शिक्षा दिलाना और उन्हें जागरूक करना है।
बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने और उनके अधिकार के लिए लडऩे वालों को दुनिया का श्रेष्ठ सम्मान नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल-श्रम के विरुद्ध पक्षधर कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन अफ़सोस कि हिन्दुस्तान में बाल श्रम को ख़त्म नहीं किया जा सका। न ही नोबेल पुरस्कार पाने के बाद कैलाश सत्यार्थी का बाल श्रम से बच्चों को बचाने का पहले जैसा अभियान देश में देखने को मिला। हिन्दुस्तान में बाल श्रम का यह हाल है कि हर ढाबे, चाय की दुकान और अनेक फैक्ट्रियों में एक-दो बच्चे काम करते मिल जाएँगे। भले ही ये बच्चे मजबूरी में पढ़ाई की जगह नौकरी करते हैं; लेकिन इनकी परेशानी को लोग अमूमन नहीं समझते और न ही केंद्र सरकार व राज्य सरकारें इस ओर कोई खास ध्यान देती हैं। हालाँकि इस ओर केवल सरकारों को ही नहीं, बल्कि श्रम संगठनों, बाल संरक्षक संस्थाओं, नागरिकों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, समाज, समाज सुधारकों, नेताओं, अभिनेताओं, धर्म गुरुओं, माँ-बाप और नियोक्ताओं, सबको ही ध्यान देने की ज़रूरत हैं। देश में 5 से 14 साल तक के 15 फ़ीसदी बच्चे मजबूरी में बाल श्रम का शिकार हैं।
बाल श्रम निषेध दिवस की थीम-2022

बाल श्रम निषेध की हर साल थीम तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2019 में इसकी थीम ‘बच्चों को खेतों में काम नहीं, बल्कि सपनों पर काम करना चाहिए’ थी। इसी तरह वर्ष 2020 में इसकी थीम ‘बच्चों को कोरोना महामारी’ रखी गयी। वर्ष 2021 की थीम ‘कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना’ रखी गयी थी। इस बार यानि 2022 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम ‘बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण’ है। सवाल यह है कि क्या हर साल एक नयी थीम बनाने भर से बाल श्रम रुकेगा? क्योंकि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वाले दिन बच्चों को बचाने की मुहिम पर भाषण देने भर से यह समस्या ख़त्म नहीं होने वाली।
बाल श्रम के नुक़सान
बाल श्रम के नुक़सान केवल श्रम के चंगुल में फँसे बच्चों को ही नहीं होते, बल्कि समाज और देश को भी होते हैं। बच्चों के बाल श्रम में फँसने से उनकी ज़िन्दगी बुरी तरह या कुछ हद तक बर्बाद ज़रूर होती है। बाल श्रम के पीछे भयावह और दिल दहला देने वाली घटनाएँ भी सामने आती रहती हैं, जिनमें बच्चों के यौन शोषण से लेकर उनसे अवैध कार्य कराने तक के मामले सामने आते रहते हैं। इन सबके चलते श्रम करने वाले बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं होता है और न ही वे जीवन में तरक़्क़ी कर पाते हैं। दरअसल बाल श्रम के पीछे निर्दयी और सामंतवादी विचारधारा का बड़ा हाथ है। कितने ही बच्चे बहुत मजबूरी में बचपन से ही नौकरी करने लगते हैं। अगर बच्चों से श्रम करवाने वाले लोग निर्दयी और सामंतवादी सोच के न हों, तो बाल श्रम को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। हमारे देश में आज भी व्यापक स्तर पर बच्चों अधिकारों का हनन कुछ लोग बाल श्रम के लालच में करते हैं। यही वजह है कि एगमार्क जैसे बाल श्रम के मानक अस्तित्व में आये।
जागरूकता के अभाव में लोग बाल श्रम को अनदेखा करते हैं और बच्चों से काम कराने वालों से कुछ नहीं कहते। सवाल यह है कि क़ानूनी तौर पर बालक कौन है? दुकान एवं स्थापना अधिनियम (फैक्ट्री अधिनियम)-1948 की धारा-2(2) में कहा गया है कि 15 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे से श्रम करवाना बाल श्रम है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि मां-बाप भी अपने बच्चों से कोई काम नहीं करा सकते। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद-45 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बाल यानि बालक माना गया है। हालाँकि गार्डन वर्कर एक्ट-1951 12 वर्ष से कम, खनन अधिनियम-1952 16 वर्ष से कम, महिलाओं एवं बालिकाओं में अनैतिक तस्करी के प्रतिषेध अधिनियम-1956 में 21 वर्ष से कम, बीड़ी और सिगरेट श्रमिक अधिनियम (रोज़गार दशाएँ) 1966 में 14 वर्ष से कम, किशोर न्याय (बालक के संरक्षण व ध्यान) अधिनियम-1986 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बालक माना गया है।
वर्ष 1989 में अपनाये गये बच्चों के अधिकारों पर अभिसमय-का अनुच्छेद-28, अनुच्छेद-32 और अनुच्छेद-34 में क्रमश: बच्चों को शिक्षा के अधिकार की लड़ाई, यौन शोषण और प्रताडऩा से संरक्षण की और श्रम के लिए मजबूर बच्चों को प्रशय देने की व्यवस्थाओं को सरकारों की ज़िम्मेदारी बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय-138 व 182 में भी बाल अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम-2006 में भारतीय दण्ड संहिता धारा 82 के तहत प्रावधान है कि 7 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चों को किसी भी अपराध में दण्डित करना वर्जित है। दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 125 में प्रावधान है कि संतान चाहे वैध हो या अवैध, वह भरण-पोषण व भत्ते की अधिकारी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अनुसार बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम-2001 में जोड़े गये नये अनुच्छेद-21 में कहा गया है कि राज्यों को 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना होगा। अनुच्छेद-24 कहता है कि 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों से कारख़ाने, खान, परिसंकटमय गतिविधियों, निर्माण, रेलवे आदि में काम कराना निषिद्ध है। संविधान के अनुच्छेद-39 (ई) कहता है कि राज्यों का कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और उन्हें आर्थिक तंगी के चलते विवश होकर ऐसे श्रम के लिए न जाना पड़े, जो उनकी आयु एवं शक्ति के अनुकूल न हो। अनुच्छेद-39 (एफ) कहता है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ एवं शैशव से लेकर किशोर अवस्था तक शोषण से, नैतिक और आर्थिक परित्याग से उनका संरक्षण हो।
इसी प्रकार 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम-2001 में मूल कर्तव्यों के अध्याय में एक अन्य खण्ड 51 (के) जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना उनके माता-पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है।
बाल श्रम कराने पर सज़ा कितनी?
बाल श्रम कराना क़ानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके बहुत-से लोग, जो किसी-न-किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, बच्चों से काम कराते हैं। इन लोगों का तर्क होता है कि उन बच्चों की मजबूरी पर तरस खाकर ये उन्हें काम देते हैं, लेकिन सच यह भी है कि कम पैसे में ज़्यादा काम के लालच में कई लोग बच्चों को काम पर रखते हैं। हालाँकि इसमें यह भी कारण है कि कई बच्चों के कंधों पर अपने घर की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इनमें कई बच्चे अनाथ होते हैं, तो कई के घर में कोई बड़ा कमाने वाला नहीं होता या कमाने योग्य नहीं होता। ऐसे में सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वे ऐसे बच्चों को चिह्नित करके उनके रहने, खाने और पढ़ाने की व्यवस्था करें। आज भारत में लाखों बच्चे बाल श्रम की भट्ठी में तप रहे हैं, जिन्हें वहाँ से निकालकर उनका भविष्य बनाने की महती ज़रूरत है। बच्चों से श्रम कराने वालों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा करने पर उन्हें एक साल की जेल से लेकर कम-से-कम 10,000 रुपये के ज़ुर्माने का प्रावधान है। धारा 14 के तहत ज़ुर्माने की राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये भी किया जा सकता है।
आयोग व समितियाँ
हमारे देश में बाल श्रम तथा श्रम पर अब तक कई आयोगों और समितियों का गठन हो चुका है; लेकिन बाल श्रम को ख़त्म नहीं किया जा सका है। बाल श्रम सम्बन्धी समिति की संस्तुति पर केंद्र सरकार ने श्रम मंत्रालय के अंतर्गत बाल श्रम पर विशेष केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जिसका काम बाल श्रम की समीक्षा करना और सलाह देना है। श्रम पर राष्ट्रीय आयोग 1969 व बाल श्रम पर समिति 1981 की रिपोर्टों में हिन्दुस्तान में बाल श्रम के कारणों व परिणामों की जाँच की गयी है।
इसके अलावा सन् 1974 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, 1975 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव पारित करने के साथ राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन किया, 1987 में बच्चों पर राष्ट्रीय नीति बनी, जिसमें कहा गया कि बच्चे देश की सबसे महत्त्वपूर्ण और क़ीमती सम्पत्ति हैं। इसके अलावा बाल श्रम पर राज्यों ने भी समितियों और आयोगों का गठन किया हुआ है। लेकिन बाल श्रम पर प्रतिबंध आज तक नहीं लग सका। कोरोना महामारी में रोज़गार के अभाव और घर में किसी कमाने वाले की मृत्यु के बाद बाल श्रम में बढ़ोतरी होना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए सरकार को देश भर में बाल श्रमिकों की संख्या जानने के लिए सर्वे कराना चाहिए, ताकि बाल श्रमिकों को एक बेहतर जीवन दिया जा सके।
हिन्दुस्तान में बाल श्रम अधिनियम
बाल श्रम के निराकरण के लिए कई वैधानिक प्रावधान किये गये। इनमें से कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं :-
कारख़ाना अधिनियम-1948
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948
गार्डन वर्कर अधिनियम-1951
अपरेंटिसशिप अधिनियम-1961
मोटर वाहन अधिनियम-1961
खनन अधिनियम-1952
दुकान एवं स्थापन अधिनियम-1961
शिशु अधिनियम-1961 (यथासंशोधित, 1978)
बीड़ी व सिगरेट श्रमिक अधिनियम-1966
बँधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम-1976
बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम-1986
किशोर न्यायालय अधिनियम-1986
किशोर न्याय (बच्चों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2000