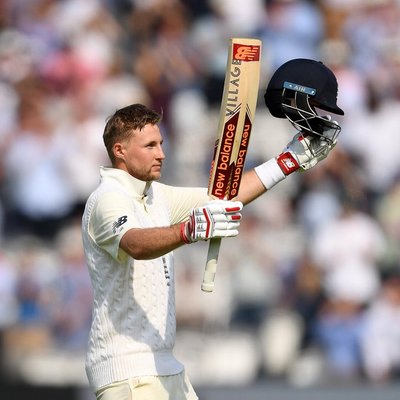प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्य सभा में विपक्षी दलों से आग्रह किया कि किसानों को समझाएं कि यह क़ानून उनके हित में हैं लिहाजा उन्हें आंदोलन ख़त्म करना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने जबाव में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कानूनों में वहीं सब लाई है जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते रहे हैं। मोदी ने तंज की भाषा में कहा कि देश को ‘आंदोलन जीवी’ लोगों से बचने की जरूरत है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर अपने जवाब में मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है और ज्यादा से ज्यादा समय जो बात बताई गईं वो आंदोलन के संबंध में बताई गयी हैं। यह कोई नहीं बता रहा कि किस बात को लेकर आंदोलन है? उस पर सब मौन रहे हैं। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उस पर भी चर्चा होती। उन्होंने कहा – ‘किसान आंदोलन पर राजनीति हावी हो रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर अचानक से यू-टर्न ले लिया है। विपक्ष को किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात करनी चाहिए।’
अब जबकि किसान आंदोलन एक नए तेवर के साथ सामने आया है, पीएम ने इसपर कहा कि खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ कहां है। मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी की बात बताना चाहता हूं। वो छोटे किसानों की दयनीय स्थिति पर हमेशा चिंता करते थे। कृषि सुधारों की बात करने वाले अचानक से पीछे हट गए।
मोदी ने कहा कि 86 फीसदी किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। पहले छोटे किसानों को कर्जमाफी का फायदा नहीं मिलता था। मोदी ने कहा – ‘हमारी हर किसान को क्रेडिट कार्ड देने की योजान है। अब तक पौने दो करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया। हमनें फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ परिवारों को लाभ हुआ। हमने उनके खाते में सीधे पैसे डाले हैं।’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सदन में हाजिर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तरफ देखते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने जो कहा था हमने वही कृषि सुधार किया है। इसके लिए कांग्रेस को गर्व करना चाहिए। हर सरकारों ने कृषि सुधारों की वकालत की है। सुधारों की बात करे विपक्ष ने यू-टर्न ले लिया। आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे बढ़ाना होगा।’
पीएम ने मनमोहन सिंह का कथन भी पढ़ा – ‘हमारी सोच है कि बड़ी मार्केट को लाने में जो अड़चने हैं, हमारी कोशिश है कि किसान को उपज बेचने की इजाजत हो। जो मनमोहन सिंह ने कहा वो मोदी को करना पड़ रहा है, आप गर्व कीजिए।’
आंदोलन का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा – ‘खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां हैं, मैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण के भाषण का जिक्र करना चाहूंगा। किसानों का सेंसेस लिया गया, तो 33 फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 18 फीसदी जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2-4 बीघे जमीन है। ये कितनी भी मेहनत कर ले, अपनी जमीन पर इनकी गुजर नहीं हो सकती है।’
मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वक्त में जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है, वो 68 फीसदी किसान हैं। 86 फीसदी किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। हमें अपनी योजनाओं के केंद्र में 12 करोड़ किसानों को रखना होगा।’
प्रधानमंत्री ने कहा कि शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात की है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया, हमें जो अच्छा लगा वो किया आगे भी सुधार करते रहेंगे। आज विपक्ष यू-टर्न कर रहा है, क्योंकि राजनीति हावी है।