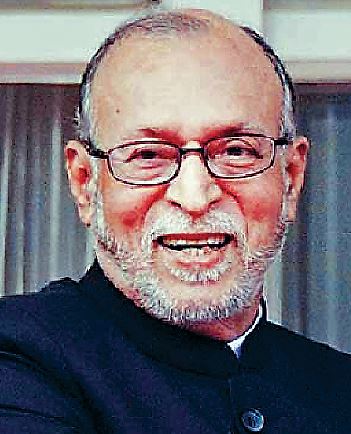केंद्र सरकार ने दिल्ली में उप राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से ज्यादा ताकतवर बनाया
केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पारित दिल्ली के राजकाज से जुड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक-2021 पर होली से एक दिन पहले 28 मार्च (रविवार) को राष्ट्रपति ने मुहर लगाकर इसे कानून की शक्ल दे दी। केंद्र में क़ाबिज़ भाजपा पर पहले से ही राज्यपालों के दुरुपयोग से राज्य सरकारों को कमज़ोर करने, उन्हें गिराने के आरोप लग रहे हैं। इस घटना से उस पर पिछले दरवाजे़ से सत्ता हथियाने के आरोपों को और मबूती मिली है; साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धों पर और विपरीत असर पड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने केंद्र सरकार के इस नये क़ानून को काला क़ानून करार देते हुए इसका विरोध किया है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी इस विरोध में दिल्ली सरकार के साथ हैं। तमाम पहलुओं पर विशेष संवाददाता राकेश रॉकी की रिपोर्ट :-
 केंद्र सरकार के दिल्ली में उप राज्यपाल की शक्तियाँ बढ़ाने सम्बन्धी संशोधन क़ानून ने देश की राजनीति में फिर गर्माहट ला दी है। इस क़ानून में उप राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियाँ और तरजीह दी गयी है। विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद इसके इसे बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के छोटी होली के दिन 28 मार्च (रविवार) को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी देने के साथ अब ये क़ानून बन गया है। क़ानून बनने के साथ ही अब दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल है।
केंद्र सरकार के दिल्ली में उप राज्यपाल की शक्तियाँ बढ़ाने सम्बन्धी संशोधन क़ानून ने देश की राजनीति में फिर गर्माहट ला दी है। इस क़ानून में उप राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियाँ और तरजीह दी गयी है। विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद इसके इसे बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के छोटी होली के दिन 28 मार्च (रविवार) को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी देने के साथ अब ये क़ानून बन गया है। क़ानून बनने के साथ ही अब दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल है।
केंद्र सरकार पर पहले ही गै़र-भाजपा राज्यों से भेदभाव के आरोप लगा रहे विपक्ष ने इस $कानून पर सख़्त प्रतिक्रिया देते हुए इसे राज्यों के अधिकारों में घुसने जैसा क़रार दिया है। दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक-2021 पेश होने के तुरन्त बाद ही इसे काला क़ानून क़रार दिया और इसके खिल़ाफ आवाज उठाने के साथ-साथ प्रदर्शन भी किये। विपक्ष का आरोप है कि हाल के वर्षों में केंद्र-राज्यों के सम्बन्धों में इसलिए भी खटास आ चुकी है; क्योंकि केंद्र राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में दख़ल कर रहा है। जीएसटी के बाद अब इस तरह के दूसरों के अधिकारों पर प्रहार करने वाले अन्य क़ानूनों के बाद केंद्र और राज्यों के बीच की खाई बढऩे की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। अब दिल्ली में केंद्र के हस्तक्षेप का दायरा और बढ़ जाएगा।
वैसे मोदी सरकार का यह क़ानून सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के भी विपरीत है, जिसमें 4 जुलाई, 2018 को ऐतिहासिक आदेश में उसकी संवैधानिक पीठ ने कहा था- ‘दिल्ली में चुनी हुई सरकार को जमीन, पुलिस और क़ानून व्यवस्था के अलावा सभी मामलों पर फै़सला लेने का अधिकार है। मंत्रिमंडल जो फै़सला लेगा, उसकी सूचना उप राज्यपाल को देनी होगी। मंत्रीमंडल का हर मंत्री अपने मंत्रालय के लिए ज़िम्मेदार है। हर राज्य की विधानसभा के दायरे में आने वाले मुद्दों पर केंद्र सरकार जबरन दख़लअंदाज़ी न करे। संविधान ने इसके लिए पूरी स्वतंत्रता दी है। इसलिए दिल्ली के असली बॉस मुख्यमंत्री ही हैं।
क़ानून का दिल्ली सरकार ने कड़ा विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा- ‘मोदी सरकार अब पिछले दरवाज़े से दिल्ली पर शासन करना चाहती है। जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती कि हम काम करें। हम इस क़ानून का ज़ोरदार विरोध करते हैं। लेकिन इससे दिल्ली की जनता के कल्याण की हमारी प्रतिबद्धता बिल्कुल कम नहीं होगी। जनता को हमारा काम पसन्द है।
आम आदमी पार्टी के राजनीतिक स्तर पर विरोध के बावजूद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस क़ानून का विरोध कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और क़ानून के जानकार सिब्बल ने कहा- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) क़ानून, 2021 गै़र-संवैधानिक है। यह संघीय ढाँचे के खिलाफ़ है। निर्वाचित सरकार पर अंकुश लगाने वाला है। विधायकों को पिंजड़े में जकड़ा प्रतिनिधित्व बना देता है। यह क़ानून इस सरकार (मोदी सरकार) में पैदा हो चुकी सत्ता के अहंकार की भावना का एक बड़ा उदाहरण है।
क्या है क़ानून में
दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके लिए पहले से ही एक अधिनियम है, जिसमें प्रदेश सरकार भी जनता द्वारा चुनी जाती है और उसकी अपनी शक्तियाँ तय हैं। अब मोदी सरकार इसमें संशोधन करके अपनी तर$फ से वर्तमान अधिनियम की धारा-44 में संशोधन करके अपनी ओर से एक प्रावधान जोडऩा चाहती है, जिसके बाद उप राज्यपाल की शक्तियाँ चुनी हुई सरकार से भी ज़्यादा हो जाएँगी और चुनी हुई सरकार अपनी इच्छा से जनहित में कोई क़दम नहीं उठा सकेगी, जब तक कि उप राज्यपाल इसकी अनुमति न दें। बता दें कि दिल्ली सरकार पहले भी उप राज्यपाल द्वारा विकास कार्यों में अड़चन डालने का आरोप लगाती रही है। इस व्यवधान को रोकने के लिए उसे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ा था, जहाँ उसे राहत मिली थी। केंद्र के प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, दिल्ली में लागू किसी भी क़ानून के तहत चुनी हुई दिल्ली सरकार, प्रशासक या मुख्य आयुक्त या किसी अन्य के फै़सले को लागू करने से पहले संविधान के अनुच्छेद-239(एए) की उप धारा (क्लॉज)-4 के तहत उप राज्यपाल की राय और अनुमति लेनी होगी। यह विषय उप राज्यपाल एक सामान्य या विशेष आदेश के ज़रिये स्पष्ट कर सकते हैं। अनुच्छेद-239(एए) में दिल्ली से जुड़े विशेष प्रावधानों का ज़िक्र है।
विरोध का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह प्रावधान लागू होने के बाद अपने प्रस्तावों को उप राज्यपाल से हरी झंडी मिले बिना दिल्ली सरकार कोई फै़सला नहीं कर सकेगी। एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र ने यह भी कहा है कि उप राज्यपाल विधानसभा से पारित किसी ऐसे क़ानून को मंजूरी नहीं देंगे, जो विधायिका के शक्ति-क्षेत्र से बाहर हैं। वह इसे राष्ट्रपति के विचार करने के लिए रिजर्व रख सकते हैं।
संशोधन क़ानून के अनुसार, विधानसभा का कामकाज लोकसभा के नियमों के हिसाब से चलेगा। यानी विधानसभा में जो व्यक्ति मौजूद नहीं है या उसका सदस्य नहीं है, उसकी आलोचना नहीं हो सकेगी। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि कई मौको पर विधानसभा में केंद्रीय मंत्रियों या प्रधानमंत्री का नाम लेकर किसी विषय पर उनकी आलोचना की गयी है। इसके अलावा इन प्रावधानों के लागू होने के बाद विधानसभा खु़द या उसकी कोई समिति ऐसा नियम नहीं बना सकेगी, जो उसे दैनिक प्रशासन की गतिविधियों पर विचार करने या किसी प्रशासनिक फै़सले की जाँच करने का अधिकार देता हो। यह उन अधिकारियों की ढाल बनेगा, जिन्हें अक्सर विधानसभा या उसकी समितियों द्वारा तलब किये जाने का डर होता है। ज़ाहिर है ये प्रावधान किसी भी राज्य सरकार को पच नहीं सकते; क्योंकि इससे उसका अस्तित्व नाममात्र का ही रह जाएगा। $कानून और संविधान के जानकार कहते हैं कि अगर इस क़ानून को देखा जाए, तो वास्तविक तौर पर दिल्ली के मुखिया उप राज्यपाल ही होंगे। निर्वाचित सरकार सिर्फ़ कहने के लिए होगी। जबकि यह ग़लत है। क्योंकि हर महत्त्वपूर्ण फै़सले में उप राज्यपाल का दख़ल होगा। यदि उप राज्यपाल को कोई क़ानून पसन्द नहीं आएगा, तो उसे दिल्ली सरकार किसी भी क़ीमत पर लागू नहीं कर पाएगी, भले उसके पास कितना ही बड़ा बहुमत क्यों न हो। भले ही वह कितना भी जनहित में हो, दिल्ली के विकास का मामला क्यों न हो। यानी दिल्ली सरकार एक तरह से बिना शक्तियों वाली सरकार या कहें कि केवल रबर स्टैंप बनकर रह जाएगी।
विरोध और समर्थन
इस मामले में क़ानून के जानकारों की राय जाननी भी ज़रूरी है। क़ानून के खिलाफ बोलने वालों का कहना है कि यह क़ानून 4 जुलाई, 2018 के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की संविधान पीठ के फै़सले के खिलाफ़ है। ज़ाहिर है इस क़ानून से दिल्ली सरकार को छोटी-छोटी चीज़ो के लिए उप राज्यपाल के दरवार में हाजि़र होना पड़ेगा, जो चुनी हुई सरकार की बेइज्जती है। चुनी सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन संशोधन क़ानून उन पर लगाम लगा देगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि दिल्ली सरकार काम न कर पाए।
इसके विपरीत क़ानून के समर्थक क़ानूनी जानकार कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के फै़सले का ही हवाला दिया जा रहा है, जबकि 2019 के एक फै़सले में उप राज्यपाल की अधिकतर शक्तियों को मान्यता दी गयी थी, इसे दूर करने और दिल्ली के लोगों को सुच्चा प्रशासन देने के लिए केंद्र संसद के ज़रिये क़ानून लायी है।
राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता केंद्र के का़नून के खि़लाफ बोल चुके हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति ने संसद में पेश क़ानून के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन किया। हालाँकि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी का यह भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा आपस में मिले हुए हैं। चौधरी ने कहा- ‘दिल्ली की चुनी सरकार की ताक़तों को कम करने वाले क़ानून को करीब दो महीने पहले मंत्रिमंडल ने इसे पास कर दिया था। केजरीवाल दो महीने क्यों ख़ामोश रहे? उन्होंने केंद्र सरकार से यह मुद्दा उठाकर इसे रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं की? दिल्ली ही नहीं देश भर में चुनी हुई सरकारों की ता$कत कम करने की कोशिशें चल रही हैं। अफ़सोस है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसमें सहयोग कर रहे हैं।
दिल्ली में आप सरकार और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल इस क़ानून को लेकर बहुत नाराज़ हैं। मोदी सरकार के संसद में प्रस्तुत किये गये क़ानून के विरोध में आप नेताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और मंत्रिमंडल मंत्री गोपाल राय ने इसका आयोजन किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी, पार्टी सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक सुर से मोदी सरकार के कानून का विरोध किया।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सा$फ कहा कि की पार्टी किसी भी ऐसे क़ानून या कोशिश के खिलाफ़ है जिससे राज्यों की शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने के मार्ग में काँटे बिछाये जाते हों। सिसोदिया ने कहा- ‘अगर केंद्र सरकार को तानाशाही करनी है, तो दिल्ली में चुनाव कराने का क्या मतलब है? केंद्र दिल्ली सरकार पर अपनी तानाशाही कर रही है। संसद में जो क़ानून लाया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य दिल्ली सरकार को काम न करने देने का है, जबकि क़ानून का अनुच्छेद-239(एए) सा$फ कहता है कि दिल्ली की अपनी विधानसभा होगी। उसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और ज़मीन को छोड़कर सभी मामलों में फै़सला लेने का अधिकार है। यही बात सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भी कही है।
उधर अधिकारों को लेकर छिड़ी इस जंग के बीच दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन क़ानून, 2021 का हम समर्थन करते हैं। इस संशोधन के बाद दिल्ली में विकास की गति बढ़ेगी और दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच अधिकार को लेकर मतभेद दूर होंगे। दोनों के काम निर्धारित हो जाएँगे, लिहाज़ा हम इसके समर्थन में हैं। एक और कारण यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को बहुत दिनों तक दिल्ली सरकार ने रोके रखा, जबकि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लागू ही नहीं किया। क़ानून में संशोधन से दिल्ली सरकार को जनहित के काम करने पड़ेंगे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर अपना काम करना चाहिए।
बढ़ेगी तकरार
दिल्ली के असली बॉस को लेकर जंग पुरानी है। याद करें सन् 2018 में भी इस मामले पर राजनीति गर्मायी थी। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। संघीय ढाँचों में राज्यों को भी स्वतंत्रता मिली है और हर मामले में उप राज्यपाल की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि क़ानून, ज़मीन और पुलिस को छोड़ दिल्ली सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर फै़सला ले सकती है। बस संविधान का पालन होना चाहिए। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और लोकतांत्रिक मूल्य ही सर्वोपरि हैं और ऐसे में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
यह तय है कि आने वाले समय में केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव नया मोड़ ले सकता है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को किसी भी सूरत में यह मंजूर नहीं है कि राज्य मंत्रिमंडल या सरकार के किसी फैसले को लागू करने से पहले उप राज्यपाल की राय लेनी जरूरी बनायी जाए। उनका कहना है कि इससे तो चुनी सरकार होने के कोई मायने ही नहीं रह जाएँगे। इसके अलावा विधानसभा या उसकी कोई समिति प्रशासनिक फै़सलों की जाँच नहीं कर सकेगी और उल्लंघन में बने सभी नियम रद्द हो जाएँगे।
वैसे पिछले दो साल से आप सरकार और उप राज्यपाल के बीच तनाव कुछ कम हुआ था। लेकिन इस क़ानून के क़ानून बनने के बाद जब ज़मीनी स्तर पर केजरीवाल सरकार को अपने फै़सलों को लेकर उप राज्यपाल के पास जाना पड़ेगा और उप राज्यपाल उन पर रोक लगाएँगे, तो सरकार का उनसे टकराव बढ़ेगा।
सरकार अभी से कह रही है कि यह क़ानून उसको अपंग बनाने के लिए लाया गया है और उसे मंजूर नहीं है। केंद्र निश्चित ही संसद में अपने बहुमत के बूते इसे पास करवा लेगी। आप नेता संजय सिंह राज्य सभा में अब विपक्ष को इस मामले में अपने साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहाँ क़ानून पास न हो। हो सकता है राज्यसभा में कुछ दिक़्क़ते आये, लेकिन पहले भी सरकार विपक्ष के विरोध के बावजूद क़ानून पास करवाती रही है।
यह बहुत दिलचस्प बात है कि जब इस क़ानून पर आम आदमी पार्टी की सरकार विरोध के स्वर ऊँचे कर रही थी, तभी केंद्र ने एक और फै़सले में केजरीवाल सरकार की महत्त्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित घर-घर राशन वितरण योजना पर रोक लगा दी और मंजूरी देने से साफ़ मना कर दिया। केजरीवाल सरकार ने इस पर कहा कि केंद्र सरकार का यह दिल्ली सरकार पर एक और प्रहार है।
इसे संयोग कहे या केंद्र या भाजपा की सोची समझी रणनीति कि जब उसने दिल्ली सरकार की हर-घर राशन वितरण योजना पर रोक लगायी उसी समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी का विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर रही थीं। ममता बनर्जी ने भी दिल्ली सरकार जैसी घर-घर राशन योजना की घोषणा करते हुए इसे द्वारे सरकार योजना का नाम दिया। ममता ने 17 मार्च को अपनी पार्टी का घोषणा-पत्र जारी किया और उधर केंद्र ने दिल्ली सरकार की वैसी ही योजना पर रोक लगा दी। यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता में दोबारा लौटने पर यदि ममता इस योजना को लागू करती हैं, तो क्या केंद्र सरकार इस पर भी रोक लगाएगी?
केजरीवाल के लिए केंद्र की रोक इस लिहाज़ा से भी बदतर रही कि उसने तो योजना को अधिसूचित तक कर दिया था और 25 मार्च से इसे लागू किया जाना था। याद रहे केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में गणतंत्र दिवस भाषण में इस योजना का ऐलान किया था। पूरी तैयारी के बाद उनकी सरकार ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिये थे। जैसे ही केंद्र ने योजना रोकने के आदेश जारी किये आम आदमी पार्टी ने इक ट्वीट में मोदी सरकार पर हमला बोल दिया।
पार्टी ने ट्वीट में कहा- ‘केंद्र सरकार ने घर-घर राशन पहुँचाने की योजना को रोक दिया है। केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना 25 मार्च को शुरू की जाने वाली थी। आखि़र मोदी सरकार राशन माफिया के ख़ात्मे के खि़लाफ क्यों है?
दरअसल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव एस. जगन्नाथन ने दिल्ली सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव सह आयुक्त को एक पत्र लिखकर कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के अनाज के वितरण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा योजना के नये नाम को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।
वैसे केंद्र ने साफ़ किया कि यदि प्रदेश सरकार एनएफएसए के अनाजों की मिक्सिंग किये बगै़र अलग से कोई योजना बनाती है, तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। केंद्र ने कहा कि एनएफएसए के तहत सब्सिडी वाला अनाज किसी भी राज्य-विशेष की योजना के लिए नये नाम से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
केंद्र के ब्रेक लगाने के बाद केजरीवाल सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना के नाम पर आपत्ति थी। अगर यही आपत्ति है, तो हमने योजना का नाम हटाने का फै़सला करते हैं। क्योंकि हमें कोई श्रेय (क्रेडिट) नहीं चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने कहा कि योजना का म$कसद लोगों को कष्ट से बचाना है। उनके मुताबिक, हम बोरी में पैक करके लोगों का जितना राशन बनता है, उतना सीधे उनके घर पहुँचा देते हैं, तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। इसी मक़सद से मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना लायी गयी थी। अब इस योजना का कोई नाम नहीं होगा, हमें श्रेय नहीं चाहिए।
केजरीवाल ने कहा कि योजना पर रोक केंद्र ने इस आधार पर लगायी क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि आप इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं रख सकते। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम यह योजना अपना नाम चमकाने या श्रेय के लिए नहीं कर रहे हैं। मैंने अफसरों से योजना का नाम हटाने को कहा और अब इसका कोई नाम नहीं होगा। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था और दुकानों के ज़रिये बाँटा जाता था, अब यह घर-घर पहुँचाया जाएगा। मुझे लगता है कि इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार की आपत्तियाँ दूर हो गयी होंगी और अब वह इस पर रोक नहीं लगाएगी।
चतुर राजनीतिज्ञ केजरीवाल

कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा अरविंद केजरीवाल को भी निपटाना चाहती है। हाल के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी है, उससे भाजपा के रणनीतिकार चौकन्ने हुए हैं। उन्हें लगता है कि यदि केजरीवाल को अभी से राजनीतिक रूप से कमज़ोर नहीं किया गया, तो वह उसके लिए आने वाले समय में उनके राजनीतिक करियर के लिए ख़तरा बन सकते हैं। केजरीवाल जनता को अपने पक्ष में करने में माहिर माने जाते हैं साथ ही वो बहुत चतुर भी हैं। इसकी झलक शाहीन बाग़ में सीएए विरोधी आन्दोलन के दौरान मिली थी, जब भाजपा के बहुत उकसाने के बावजूद केजरीवाल एक समय तक तटस्थ बने रहे थे।
पिछले विधानसभा चुनाव में उनका हनुमान चालीसा पढऩा और बाद में अपनी जीत का श्रेय हनुमान जी को देना भी एक राजनीतिक पैंतरा था। भाजपा के लिए सबसे बड़ी दिक़़्कते यह है कि वह बहुत कोशिश करके भी केजरीवाल की हिन्दू विरोधी छवि गढऩे में पूरी तरह नाकाम रही है। ऐसा कांग्रेस के बारे में नहीं कहा जा सकता। इसका एक कारण कांग्रेस और उसके बड़े नेताओं का मुद्दों पर खुले रूप से निर्णय लेना भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या राहुल गाँधी सच में हिन्दू विरोधी है। कांग्रेस और राहुल गाँधी के विपरीत केजरीवाल बहुत सँभलकर बोलते हैं। इसका कारण देश भर में भाजपा का हिन्दू उभार लाना या धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना है। केजरीवाल जानते हैं कि भाजपा के जाल में फँसने का मतलब होगा- भाजपा को दिल्ली में अपने हिसाब से मुद्दे चलाने का रास्ता दे देना।
केजरीवाल भाजपा के बड़े नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह सार्वजनिक धार्मिक उत्सवों में हिस्सा लेते हैं। दीवाली हो या अन्य हिन्दू त्यौहार, केजरीवाल खुलकर दीपमाला करते और जनता को अपना सन्देश देते हैं। देशभक्ति दिखाने के मौके़ भी वह नहीं चूकते। एक तरह से केजरीवाल भाजपा की तरह की ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह भाजपा से अलग दिखते हैं। भाजपा के विपरीत उनकी मुस्लिमों और अन्य समुदायों में बेहतर पैठ है। यहीं केजरीवाल के सामने भाजपा मजबूर है।
यह केजरीवाल की राजनीतिक चतुराई ही है कि जब भाजपा मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसे घाघ नेताओं के होते हुए भी या पुडुचेरी में ऐन चुनाव के समय कांग्रेस सरकारें गिरा लेती है, या मनमर्ज़ी से उसके दिग्गज नेताओं को अपने पाले में कर लेती है, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद वह केजरीवाल के आगे पस्त नज़र आती है। अब भाजपा अपनी केंद्र सरकार के ज़रिये इस मोर्चे पर हारकर केजरीवाल के अधिकार सीमित करने का दाँव आजमा रही है। उसकी कोशिश केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सामने राजनीतिक अस्तित्व का संकट पैदा करना है।
दिल्ली में अब अगले साल स्थानीय नगर निगम के चुनाव होने हैं। हाल में पाँच सीटों पर हुए उप चुनाव में से चार सीटें जीतकर केजरीवाल की पार्टी भाजपा के लिए ख़तरे का घंटी बजा चुकी है, जिसे एक भी सीट नहीं मिली। जबकि कांग्रेस एक सीट जीतने में सफल रही। केजरीवाल बहुत खू़बसूरती से अपने खिल़ाफ अन्याय वाला कार्ड खेलते हैं और अब फिर वह ऐसा ही करेंगे। वह बार-बार कहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही। जनता में वह कमज़ोर न दिखें, इसके लिए वह हार हाल में जनता की लड़ाई मज़बूती से लडऩे की बात भी साथ ही कह देते हैं। केजरीवाल का मशहूर डायलॉग है- ‘वे (केंद्र में बैठे लोग) हमें परेशान कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आप (जनता) हमारे साथ हैं।’ इस तरह केजरीवाल केंद्र के ख़िलाफ अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई बना देते हैं। दिल्ली की अधिकतर जनता भी उनके काम से काफी खु़श है और उनके समर्थन में दिखती है। जब एक बड़े टीवी चैनल, जिसे लोग गोदी मीडिया की लिस्ट में शामिल करते रहे हैं; ने ‘दिल्ली का बॉस कौन? नाम से एक वोटिंग कैंपेन चलाया, तो 90 फीसदी मत केजरीवाल के पक्ष में पड़े, जबकि केवल 10 फ़ीसदी मत ही उप राज्यपाल के पक्ष में पड़े। इससे केजरीवाल की शोहरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यह पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री के लिए लोग ‘आई लव’ लिखने लगे हैं।
याद कीजिए किसान आन्दोलन के शुरुआती दिनों में केजरीवाल पूरे मंत्रिमंडल के साथ सिंघु बार्डर पहुँच गये थे। उन्हें पता है कि किसानों का आन्दोलन पंजाब और उत्तर प्रदेश में उन्हें लाभ दे सकता है। यह भी याद रखें कि बाराणसी में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री मोदी के खिलाफ़ चुनाव लड़ गये थे। केजरीवाल मोदी के गुजरात पर नज़ारें गढ़ाये हैं। निकाय चुनाव में उनकी पार्टी ने गुजरात में जब 42 सीटें जीती, तो केजरीवाल खु़द जनता का आभार जताने वहाँ पहुँच गये।
अब शक्तियों वाले क़ानून को लेकर केजरीवाल फिर भाजपा और केंद्र के खिल़ाफ निशाना साध चुके हैं। इस मुद्दे पर वह राजनीतिक स्तर पर केंद्र और भाजपा पर हमले कर रहे हैं। यही उनकी रणनीति है। घर-घर राशन की योजना के लिए जब केंद्र ने इसमें मुख्यमंत्री शब्द जोडऩे पर ऐतराज जताया, तो वह तुरन्त यह शब्द हटाने के लिए मान गये। उन्हें पता है कि हर-घर राशन पहुँचाकर राजनीतिक $फायदा तो उन्हें ही मिलेगा। लेकिन उप राज्यपाल को सरकार से ज्यादा शक्तियाँ देने का क़ानून चूँकि राजनीतिक रूप से उन्हें कमज़ोर करता है, वो इसके खिलाफ़ मज़बूती से खड़े हो गये हैं।
इस विधेयक (क़ानून) से केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच तालमेल बिठाना आसान हो जाएगा। इस संशोधित क़ानून का उद्देश्य उप राज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करना है। सर्वोच्च न्यायालय के फै़सले के अनुरूप उप राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच मेल-मिलाप के सम्बन्ध सुनिश्चित करने के लिए क़ानून में संशोधन किया गया है।
केंद्र सरकार (क़ानून बनने से पहले विधेयक पर बयान)
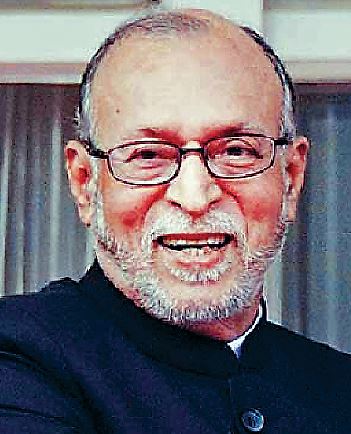
केंद्र और राज्यों में
टकराव के बिंदु
आठ राज्यों पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखण्ड, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ने अपने-अपने राज्य में मामलों की जाँच के सम्बन्ध में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच सम्बन्धी अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली। यह क़दम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकारी संघवाद के मंत्र के दावे के विपरीत केंद्र-राज्य सम्बन्धों में टकराव का संकेत है।
कोविड-19 से लडऩे के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तय कड़े नियमों को राज्यों ने मानने से इन्कार कर दिया।
जीएसटी मुआवजे़ के अपने हिस्से की माँग तक गै़र-भाजपा राज्य केंद्र के साथ टकराव की मुद्रा में। केंद्र पर शक्तियों के दुरुपयोग की कोशिश का आरोप लग रहा है।
जीएसटी में अपने हिस्से को लेकर राज्य केंद्र के खिलाफ़ लामबंद।
सीएए क़ानूनों को लेकर गै़र-भाजपा सरकारें केंद्र के खिलाफ़ हैं।
केंद्र के तीन कृषि क़ानून को गै़र-भाजपा राज्यों ने नहीं माना और कांग्रेस सरकारें तो अपने संशोधित विधेयक विधानसभाओं में लेकर आयी हैं।
उप राज्यपाल को सरकार से ज़्यादा शक्तियों वाले विधेयक के खिलाफ़ है दिल्ली सरकार और दूसरे विपक्षी दल।
पहले भी हुआ है टकराव
दिल्ली में उप राज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच पिछले क़रीब छ: साल में कई बार टकराव हुआ है। शुरुआत तब हुई, जब पहली अप्रैल, 2015 को एक आदेश जारी करके तत्कालीन उप राज्यपाल नजीब जंग ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री केजरीवाल का वह आदेश नहीं मानने का फ़रमान जारी कर दिया, जिसमें पुलिस, सार्वजनिक आदेश और ज़मीन से जुड़े सभी मामलों की फाइलें उनके माध्यम से उप राज्यपाल को भेजने का निर्देश था। हालाँकि कुछ दिन चली तकरार के बाद 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अधिकारियों को सभी फाइलें उप राज्यपाल के पास भेजने से मना कर दिया। एक महीने बाद ही 15 मई को केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन को केंद्र की तरफ़ से कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाये जाने का विरोध किया। इसके पाँच दिन बाद ही 20 मई को उप राज्यपाल जंग ने यह कहकर कि यह उनका अधिकार है, दिल्ली सरकार की तमाम नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इसके एक दिन बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके सा$फ किया कि दिल्ली में सभी स्थानांतरण और नियुक्तियों का अधिकार सिर्फ़ उप राज्यपाल को है। यही नहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्रांच (एसीबी) को केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने के अधिकार से बाहर कर दिया गया। आप सरकार ने 28 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) में चुनौती दी। उसी दिन केंद्र सरकार अधिसूचना को लेकर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के खिलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय चली गयी। क़रीब 14 दिन बाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना रद्द कर दी। 4 अगस्त, 2016 को जब उच्च न्यायालय ने उप राज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक मुखिया बताया, तो 31 अगस्त को इस आदेश को आप सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सन् 2016 में ही दिल्ली के उप राज्यपाल ने केजरीवाल की तर$फ से डीआईआरसी चेयरमैन पद पर नियुक्त कृष्णा सैनी की नियुक्ति रद्द कर दी थी। 15 फरवरी, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजनिवास और दिल्ली सरकार के बीच चल रही रस्साकशी को संवैधानिक पीठ को भेज दिया। 20 फरवरी, 2018 को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आप विधायकों और मुख्यमंत्री पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय पीठ ने उप राज्यपाल को चुनी हुई सरकार की सलाह मानने को कहा। आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर 2018 की गर्मियों में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्रियों के साथ उप राज्यपाल के घर पर ही धरना दे दिया था। 14 फरवरी, 2019 को दो सदस्यीय संविधान पीठ ने शक्तियों के विभाजन का निर्णय दिया, लेकिन इस निर्णय को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया और यह मामला वहाँ लम्बित है। इसके आलावा दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने को लेकर भी केंद्र से केजरीवाल का विवाद हुआ। क्योंकि केजरीवाल किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। गेस्ट टीचर की नौकरी पक्की करने पर भी उप राज्यपाल से केजरीवाल की तनातनी बढ़ी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शिक्षकों से जुड़ी फाइल दबा ली गयी है। दिल्ली में सीलिंग विवाद में भी केजरीवाल और उप राज्यपाल आमने सामने आये।
जब कोरोना हुआ, तो केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में पहले दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, तो उप राज्यपाल ने इस फै़सले को बदल दिया कि दिल्ली में सबका इलाज होगा। दिल्ली सरकार ने जब पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवज़े का ऐलान किया, तो उप राज्यपाल ने वो फाइल ही सरकार को वापस भेज दी। ऐसा ही नौ सलाहकार नियुक्त करने के सरकार के फै़सले में हुआ।
दिल्ली में उप राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सलाह से काम करेंगे। उप राज्यपाल स्वतंत्र तौर पर काम नहीं करेंगे, अगर कोई अपवाद है, तो वह मामले को राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर सकते हैं और जो फै़सला राष्ट्रपति लेंगे उस पर अमल करेंगे। अनुच्छेद-239(एए) के तहत मंत्रीपरिषद् के पास कार्यकारी शक्तियाँ हैं। मंत्रिपरिषद् राज्य और समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं, उसमें तीन अपवाद को छोड़कर बाकी मामले में स्वतंत्र होकर काम कर सकेगी। सार्वजनिक आदेश, पुलिस और •ामीन को छोड़कर राज्य सूची में जो भी विषय हैं, उसमें राज्य सरकार $कानून बना सकती है। जो भी फै़सला सरकार लेगी उसके बारे में वह उप राज्यपाल को अवगत कराएगी; लेकिन उप राज्यपाल की सहमति ज़रूरी नहीं है। अपवाद के तौर पर उप राज्यपाल किसी मामले को राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ हर मामला नहीं है। उप राज्यपाल फै़सले में दिये गये सिद्धांत को ध्यान में रखकर मामले को उप राज्यपाल समझौता कर सकते हैं। दिल्ली में उप राज्यपाल की स्थिति दूसरे राज्यों के राज्यपालों जैसी नहीं है। वह एक प्रशासक हैं। इसमें निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है। संतुलित संघीय व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र तमाम अधिकार अपने पास न रखे, बल्कि राज्य अपनी परिधि में बिना द$खल के काम करें। अनुच्छेद-239(एए) में जो व्याख्या है, उसमें उप राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् की सलाह मानना अनिवार्य है। यह अनिवार्यता तब तक होगी, जब तक कि वह क्लॉज-4 के तहत मामले को राष्ट्रपति को हस्तांतरित न कर दें। उप राज्यपाल को $खुद स्वतंत्र तौर पर फै़सला नहीं लेना है।
(न्यायाधीश दीपक ठाकुर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का 4 जुलाई, 2018 का आदेश।)