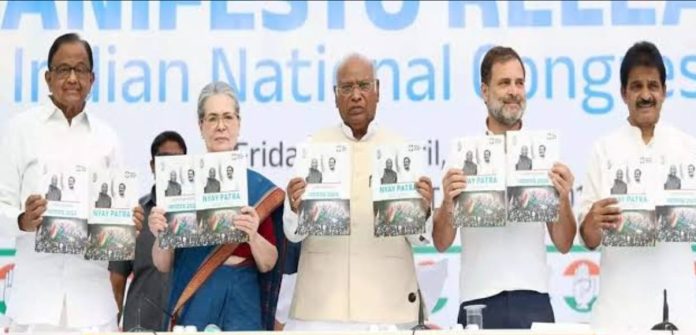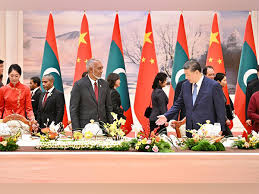क्या बूथ लूटने वालों के सहारे आज भी जीते जाते हैं चुनाव ?
इंट्रो-
2024 के आम चुनाव होने में केवल कुछ ही ह$फ्ते बचे हैं। सभी पार्टियाँ चुनाव जीतने के लिए हर सम्भव कोशिश में लगी हैं। भाजपा की अगुआई में एनडीए और दूसरी तरफ़ कांग्रेस की अगुआई में इंडिया गठबंधन का मुक़ाबला होना है। इसलिए यह चुनाव दिलचस्प होने के साथ-साथ दोनों तरफ़ नाक का सवाल भी बन गये हैं। ऐसे समय में ‘तहलका’ एसआईटी ने जम्मू-कश्मीर में बूथ कैप्चरिंग और अन्य चुनावी कदाचार की परेशान करने वाली वास्तविकता को उजागर किया है। तहलका एसआईटी की रिपोर्ट :-
——–
‘पैसे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने पिछले चुनावों में बूथ कैप्चरिंग की थी। ऐसे ऑपरेशन्स की लागत हर बूथ पर अलग-अलग होती है। बूथ के आकार के आधार पर यह एक लाख से दो लाख तक हो सकता है, या पाँच लाख और 10 लाख तक भी बढ़ सकता है। कश्मीर में जब उम्मीदवारों को पता चलता है कि वे चुनाव हार रहे हैं, तो वे पत्थरबाज़ी का सहारा लेते हैं। वे युवाओं को पत्थर फेंकने के लिए नियुक्त करते हैं, जिसके बाद उनके समर्थक बूथों पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं।‘
यह बातें बूथ कैप्चरिंग सहित चुनाव प्रबंधन में माहिर एक कश्मीरी सामाजिक कार्यकर्ता और एजेंट एजाज़ अहमद डार ने कहीं, जो उम्मीदवारों को गारंटी से जीत दिलाने का वादा करता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा 2024 के आम चुनाव की तारीख़ों की घोषणा करने से बहुत पहले एजाज़ कश्मीर से दिल्ली पहुँचा और ‘तहलका’ एसआईटी के ख़ुफ़िया कैमरे पर क़ुबूल किया कि उसने अतीत में कई चुनावों में परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया था। उल्लेखनीय है कि चुनाव में बाहुबल के दुरुपयोग पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दौरान व्यापक चर्चा की थी। राजीव कुमार ने ‘4एम’ (बाहुबल, धनबल, ग़लत सूचना और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन) पर प्रकाश डाला था, जो इस गर्मी के आम चुनाव के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग इनमें से प्रत्येक मुद्दे के समाधान के लिए रणनीतिक रूप से योजना तैयार कर रहा है। कुमार ने टिप्पणी की थी- ‘जिस तरह कुछ राज्यों में ताक़त के इस्तेमाल की संभावना अधिक होती है, उसी तरह अन्य राज्य वित्तीय दुरुपयोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।‘
जम्मू-कश्मीर की पाँच लोकसभा सीटों के लिए मतदान पाँच चरणों में होगा, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई को समाप्त होगा। इसके अलावा निकटवर्ती लद्दाख़ क्षेत्र की एकमात्र लोकसभा सीट पर भी उसी दिन मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश, जो अनुच्छेद-370 और 35-ए के निरस्त होने के बाद अपनी पहली महत्त्वपूर्ण चुनावी लड़ाई का गवाह बनने के लिए तैयार है; में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। सन् 2017 में श्रीनगर लोकसभा उप चुनाव में सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान आठ लोगों की जान चली गयी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 7.14 फ़ीसदी निराशाजनक मतदान दर्ज किया गया। सन् 2019 में जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) ने मतदान के दौरान देवर लोलाब इलाक़े में पीडीपी नेता अब्दुल हक़ ख़ान के समर्थकों द्वारा कथित बूथ कैप्चरिंग का ज़ोरदार विरोध किया गया। जेकेपीसीसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ज़िला निर्वाचन अधिकारी, कुपवाड़ा से पीडीपी कार्यकर्ताओं और मतदान कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इसके अलावा सन् 2020 में जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जे एंड के एनसी) के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने बूथ कैप्चरिंग और अन्य अनियमितताओं के कथित उदाहरणों का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में गरूरा ज़िला विकास परिषद् (डीडीसी) निर्वाचन क्षेत्र में फिर से मतदान की माँग की। इसी वर्ष ज़िला विकास परिषद् (डीडीसी) चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग के ऐसे ही आरोपों के कारण जम्मू क्षेत्र के पुंछ ज़िले में कम-से-कम छ: सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था।
अब कुछ सप्ताह बाद होने जा रहे आम चुनाव को देखते हुए जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में चुनाव कराना भारत निर्वाचन आयोग के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक होने जा रहा है। सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव न कराने का फ़ैसला किया है, और आम चुनाव के तुरन्त बाद विधानसभा चुनाव निर्धारित करने का विकल्प चुना है। चुनाव आयोग का दावा है कि उसने 4एम पर नकेल कसने की योजना तैयार कर ली है। 2024 के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ‘तहलका’ ने 4एम पर एक खोजी शृंखला भी शुरू की है, जिसकी शुरुआत इस संस्करण में बाहुबल पर केंद्रित है।

अपनी जाँच के हिस्से के रूप में ‘तहलका’ रिपोर्टर ने एजाज़ अहमद डार से बात की, जो ‘तहलका’ के अंडरकवर रिपोर्टर से मिलने के लिए कश्मीर से दिल्ली आया था। ‘तहलका’ रिपोर्टर ने ख़ुद को एक ग्राहक के रूप में पेश करते हुए जम्मू-कश्मीर में कथित तौर पर चुनाव लड़ रहे एक काल्पनिक उम्मीदवार के लिए चुनाव अभियान का प्रबंधन करने के लिए एजाज़ के साथ एक (काल्पनिक) सौदा किया। एजाज़ ने रिपोर्टर को उनके (काल्पनिक) उम्मीदवार की सफलता का भरोसा दिलाया। उसने इस मामले में एक रहस्य भी उजागर किया कि, ‘कश्मीर में यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि वह हार रहा है, तो वह समर्थकों को निर्देश देगा कि वे सुरक्षाबलों का ध्यान भटकाने के लिए पत्थर फेंकना शुरू कर दें, जिससे संभावित बूथ पर क़ब्ज़ा हो सके।
रिपोर्टर : कितना पैसा ख़र्च हो जाएगा उसमें?
एजाज़ : उसमें तो काफ़ी पैसा लगेगा और कश्मीर की अगर बात करें, …वहाँ पर एक मसला ये भी होता है कि आराम से अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर हम नहीं जीत पाएँगे, तो वहाँ पर पत्थर, …स्टोन पेल्टिंग (पत्थरबाज़ी) करवाके…।
रिपोर्टर : जी! क्या कह रहे हैं आप?
एजाज़ : वहाँ स्टोन पेल्टिंग करवा के बूथ कैप्चरिंग…।
रिपोर्टर : स्टोन पेल्टिंग करवा के बूथ कैप्चरिंग? …लेकिन मुझे गारंटी दो, काम हो जाएगा?
एजाज़ : हाँ; हो जाएगा। …आराम से हो जाएगा।
अब एजाज़ ने कश्मीर की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी का नाम लिया, जिसके लिए उन्होंने 2014 के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग आयोजित करने का दावा किया था। इस संदिग्ध कृत्य को वित्तपोषित करने के लिए पार्टी को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ीं और लाखों रुपये ख़र्च करने पड़े। हालाँकि एजाज़ के अनुसार, कश्मीर इस घटना से अछूता नहीं है; क्योंकि राज्य में अब तक हुए लगभग हर चुनाव की यह विशेषता रही है।
रिपोर्टर : खुल के बताओ ना! बात करो, किस पार्टी के लिए?
एजाज़ : xxxx के लिए।
रिपोर्टर : स्टोन पेल्टिंग (पत्थरबाज़ी) करवाके?
एजाज़ : हाँ; ये सब तो चलता है वहाँ पर। …ऐसा कुछ नहीं है।
रिपोर्टर : ये कब करवाया आपने xxxx के लिए?
एजाज़ : 14 के बाद।
रिपोर्टर : 2014 में? …कितना पैसा लगा उसमें?
एजाज़ : उसमें बहुत सारा पैसा लगा; …लाखों में उसमें पैसे लगे हैं, एक-एक जगह के।
रिपोर्टर : देता कौन है आपको? पैसा मिल जाता है?
एजाज़ : हाँ…।
जब पूछा गया कि बूथ कैप्चरिंग के लिए उसे कितना पैसा मिलता है? तो एजाज़ ने ‘तहलका’ के रिपोर्टर को बताया कि यह स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें शामिल जोखिमों पर चर्चा करते हुए एजाज़ ने कहा कि वह सम्बन्धित राजनीतिक दल से एक आश्वासन पर बातचीत करता है कि बूथ कैप्चरिंग के प्रयास के बाद गिरफ़्तार होने की स्थिति में वह जेल से लड़कों की रिहाई सुनिश्चित करेगी। जब उससे पूछा गया कि हमारे चुनाव प्रबंधन में वह क्या ज़िम्मेदारियाँ उठा सकता हैं? तो एजाज़ ने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया कि पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है।
रिपोर्टर : लेकिन बूथ आप कैप्चर करवाओगे, उसमें आप पर कोई एक्शन नहीं होगा? पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी?
एजाज़ : वो है ना! लड़के बन्द हो जाते हैं; …वो पैसों के लिए होते हैं। …उनको पता होता है।
रिपोर्टर : जो पत्थर फेंकते हैं?
एजाज़ : उनको पता है, …बिलकुल।
रिपोर्टर : उनको पैसा मिल जाता है? …कितना-कितना मिल जाता है?
एजाज़ : वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन पर।
रिपोर्टर : फिर भी कम-से-कम कितना?
एजाज़ : एक तो उनको छुड़वाने के पैसे, …उनको जो लगते हैं। …गारंटी लेनी पड़ती है वहाँ पे; …छुड़वाने के लिए पैसा जितना लगेगा, वो हम देंगे।
रिपोर्टर : उसकी गारंटी कौन लेता है?
एजाज़ : उसके लिए बंदे रखे होते हैं।
रिपोर्टर : जो पॉलिटिशियन हैं, जिनके लिए वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं; वो ही गारंटी लेते हैं?
एजाज़ : हाँ।
रिपोर्टर : आप ज़िम्मेदारी किस चीज़ की ले सकते हैं? ये बताएँ।
एजाज़ : देखिए भाई! मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, …जहाँ पर पैसे होंगे, वहाँ पर मेरे को कुछ भी बोलो, …मैं करूँगा।
फिर रिपोर्टर ने एजाज़ से पूछा कि उसने योजना को अंजाम देने की योजना कैसे बनायी? जबकि घाटी से अब पत्थरबाज़ी की घटनाएँ रिपोर्ट नहीं की जा रही हैं। इसके जवाब में एजाज़ ने हँसते हुए कहा कि यह एक ग़लत धारणा है कि पत्थरबाज़ी की घटनाएँ बन्द हो गयी हैं। उसने बताया कि ऐसी घटनाओं में कमी धन की कमी के कारण आयी है। उन्होंने आगे कहा कि सही मात्रा में धन के साथ कोई भी कश्मीर में पत्थरबाज़ी के लिए भीड़ को उकसा सकता है। उसने दावा किया कि वह ऐसे लड़कों को जानता है, जो अनुरोध पर पत्थरबाज़ी करने को तैयार हैं।
रिपोर्टर : लेकिन अब स्टोन पेल्टिंग वग़ैरह तो बन्द हो गयी सब, …कश्मीर में?
एजाज़ : बन्द हो गयी? …हा..हा…हा (हँसते हुए)। …फिर से करानी है, तो बोल दीजिए।
रिपोर्टर : हैं…!
एजाज़ : इसमें क्या? …पैसे लगते हैं। पैसे दे दो, फिर स्टार्ट। …पैसे आने बन्द हो गये…।
रिपोर्टर : लड़के भी तो बन्द हैं फेंकने वाले?
एजाज़ : कहाँ बन्द हैं? …किसने कहा बन्द हैं?
एजाज़ ने रिपोर्टर को उन लड़कों के बारे में जानकारी दी, जो बूथ कैप्चरिंग के लिए पत्थरबाज़ी में शामिल होते हैं। उसके अनुसार, ये लड़के आमतौर पर नौ महीने जेल में बिताते हैं और उसके बाद तीन महीने आज़ादी में बिताते हैं। हालाँकि उन तीन महीनों के दौरान वे पूरे साल भर के लिए पर्याप्त कमायी कर लेते हैं। पत्थरबाज़ी उनकी आय का नियमित स्रोत लगती है। अगर उन्हें जेल नहीं होती, तो वे पैसा नहीं कमाते।
एजाज़ : लड़के तो हैं साथ में, उनको तो आदत ही है। …साल में वो नौ महीने तो जेल में रहते; …तीन महीने बाहर। …वो तीन महीने काम करेंगे, एक साल के बराबर…।
रिपोर्टर : किस चीज़ से कमाते हैं वो?
एजाज़ : पैसे लेकर स्टोन पेल्टिंग वग़ैरह। …साल भर बैठो, तीन महीने कमाओ। …ये तो काम है ना उनका, …उनका रोज़ का है। अगर वो जेल नहीं जाएँगे, तो पैसे कहाँ से आएँगे?
रिपोर्टर : जेल से पैसे कैसे आते हैं?
एजाज़ : पहले से ही लेकर रखते हैं, उनको पता है छ: मंथ्स के लिए जाना है या नौ मंथ्स…। एक साल के लिए जाना है, दो साल का कमा लिया; …चले जाएँ जेल आराम से।
जब एजाज़ से पूछा गया कि उन्होंने अतीत में बूथ कैप्चरिंग के लिए कितना पैसा लिया था? तो उसने कहा कि यह कई स्थितियों के अलावा बूथ के आकार पर निर्भर करता है। उसने कहा कि प्रति बूथ एक से दो लाख रुपये या पाँच से 10 लाख रुपये तक की राशि मिलती है। चुनाव में वह हमारे लिए कितने बूथों पर क़ब्ज़ा कर सकता है? इस पर एजाज़ ने कहा कि वह पूरे दक्षिण कश्मीर को सँभाल सकता है। क्योंकि वह इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उनके एनजीओ का भी वहाँ गढ़ है।
रिपोर्टर : कितना ख़र्चा आ जाएगा एक बूथ का?
एजाज़ : ये अब देखना पड़ेगा; …बूथ कैसा होगा?
रिपोर्टर : अभी तक जो आपने किया है, उसमें कितना ख़र्चा आया है?
एजाज़ : एक-एक लाख, …दो-दो लाख।
रिपोर्टर : एक बूथ का?
एजाज़ : हाँ; कहीं-कहीं पाँच लाख, 10 लाख भी होगा। …डिपेंड करता है, बूथ कितना बड़ा है?
रिपोर्टर : अच्छा; कितने बूथ असेंबली इलेक्शंस में आप कैप्चर करवा सकते हैं, …हमारे लिये?
एजाज़ : मैं साउथ की बात करूँ?
रिपोर्टर : साउथ कश्मीर?
एजाज़ : जी! …जहाँ-जहाँ आप टार्गेट देंगे, वहाँ कर देंगे।
रिपोर्टर : नंबर ऑफ बूथ (बूथों की संख्या) बताएँ?
एजाज़ : मुझे लगता है, वहाँ कोई भी ऐसा बूथ नहीं होगा, जहाँ पर हमारा कंट्रोल न हो।
रिपोर्टर : साउथ कश्मीर के आप एक्सपर्ट हैं?
एजाज़ : हाँ।
रिपोर्टर : बूथ कैप्चर हो जाएँगे सही से?
एजाज़ : हमारे एनजीओ हैं ना! वहाँ से लड़के आते हैं।
रिपोर्टर : एनजीओ से? …मतलब, समझा नहीं?
एजाज़ : मतलब, जो हमसे जुड़े हैं। …जिनको हम हेल्प देते हैं। …काफ़ी मेहनत लगती है बूथ कैप्चर करने में।
रिपोर्टर : वो आपकी एनजीओ से जुड़े हैं?
एजाज़ : हाँ।

अब एजाज़ ने बूथ कैप्चरिंग के तरीक़े का ख़ुलासा किया। उसके अनुसार, जब किसी उम्मीदवार को पता चलता है कि वह किसी विशेष बूथ पर हार रहा है, तो वह अनियंत्रित स्थिति पैदा करने के लिए अपने समर्थकों को पत्थरबाज़ी करने का आदेश देता है। जैसे ही पत्थरबाज़ी शुरू होता है, बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी वक़्त बूथ कैप्चरिंग होती है।
रिपोर्टर : किस चीज़ पर ख़र्चा आता है ये?
एजाज़ : वहाँ पर पहले आता है कि वोटर कितने हैं? …मान लो 100 वोटर हैं। अब एक अंदाज़ा होता है अपना कि 10 में से हमारे कितने वोटर्स हैं? …अगर इसमें हमें लगे कि हमारे कम वोटर्स हैं; …क्या हम उनको ख़रीद सकते हैं फिर? अगर ख़रीद नहीं पाये, तो वहाँ पर हम क्या करें, ताकि वो वोटर वहाँ पर न जा पाएँ।
रिपोर्टर : उसके लिये क्या करते हैं आप?
एजाज़ : उसके लिये स्टार्ट होती है स्टोन पेल्टिंग। …स्टोन पेल्टिंग; दो-तीन लड़के हायर किये, उन पर ख़र्चा आता है- लाख, 1.5 लाख, दो लाख।
रिपोर्टर : दो-तीन लड़कों पर?
एजाज़ : हाँ; ज़्यादा भी आ जाता है। मान लो कोई लड़का एक लाख लेगा, और बोलेगा हालात ख़राब हो जाएँगे; …मैं जेल जाऊँगा। दूसरा मुझे छुड़ाना है। कम-से-कम छ: महीने तो उनके लगने हैं अंदर। …और उन छ: महीनों के लिए मुझको एक लाख, 1.5 लाख चाहिए; …जो मुझे मिलना चाहिए। फिर वो भी हो जाता है; …शाम को वोटिंग बन्द। वो भी सामने आ जाता है।
एजाज़ के मुताबिक, बूथ कैप्चरिंग जहाँ उसकी ख़ासियत है। वहीं वह प्रलोभन के ज़रिये लोगों को वफ़ादारी बदलने के लिए भी राज़ी कर सकता है। उसने चुनाव अभियान आयोजित करने और मतदाताओं को पैसे की पेशकश करके वोट ख़रीदने की अपनी क्षमता का उल्लेख किया। हालाँकि उसने आगाह किया कि ये सभी कार्रवाइयाँ शामिल पक्षों के लिए ज़्यादा ख़र्च लेकर आती हैं।
रिपोर्टर : तो आपका जो काम है, जिसमें आप स्ट्राँग हो; वो है बूथ कैप्चरिंग?
एजाज़ : बूथ कैप्चरिंग, लोगों को ख़रीदना। …वो भी हम कर सकते हैं। …आराम से कर चुके हैं हम।
रिपोर्टर : अब आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, आप इलेक्शन में क्या-क्या करते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं?
एजाज़ : इलेक्शन में आप कैंपेनिंग करवा सकते हैं। …लोगों को जुड़वा सकते हैं। वोट को इधर-उधर करवा सकते हैं।
रिपोर्टर : वोट को इधर-उधर कैसे करवाओगे?
एजाज़ : पैसे देकर लोगों को। …पैसे या कोई लालच; या व्हाट एवर (जो कुछ भी), …जो नीड (माँग) हो, वो सब करके।
रिपोर्टर : कितना पैसा ख़र्च हो जाएगा उसमें?
एजाज़ : अगर कहीं पे जब भी करना पड़ेगा स्ट्राइक (धरना) वग़ैरह। …कोई अपना होता है नेता, बन्द हो जाता है; …या एक्शन लिया जाता है तब, उसको छुड़वाने के लिए प्रोटेस्ट; …वो भी करवा सकते हैं।

चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के अलावा एजाज़ ने ‘तहलका’ रिपोर्टर को यह भी बताया कि अगर किसी राजनीतिक नेता को सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ़्तार किया जाता है, तो वह उसके लिए विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने में मदद कर सकता है। एजाज़ ने क़ुबूल किया कि जिस उम्मीदवार के लिए वह काम कर रहा था, उसके पक्ष में वोट सुरक्षित करने के लिए उसने मतदाताओं को 1,000 से 2,000 रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कश्मीर में लोगों को शराब से नहीं, बल्कि अन्य तरीक़ों, जैसे- ड्रग्स, ब्राउन शुगर आदि से लुभाया जाता है।
रिपोर्टर : लीकर (शराब) वग़ैरह, पैसे बाँटना?
एजाज़ : हाँ; पैसे तो बाँटे हैं।
रिपोर्टर : कितना-कितना?
एजाज़ : एक हज़ार, दो-दो हज़ार दिये हैं।
रिपोर्टर : शराब?
एजाज़ : शराब नहीं चलती वहाँ।
रिपोर्टर : वहाँ ड्रग्स वग़ैरह चलती है क्या?
एजाज़ : चलती है। …बहुत ब्राउन शुगर है वहाँ पर।
रिपोर्टर : कश्मीर में?
एजाज़ : हाँ; बहुत।
जब एजाज़ से पूछा गया कि वह किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? तो उसने ने जवाब दिया कि वह उन पार्टियों से जुड़ा हैं, जो उसे पैसे देती हैं। उसने कहा कि वह विचारधारा के आधार पर ख़ुद को किसी विशेष पार्टी के साथ नहीं जोड़ता है, बल्कि उसके लिए पैसा ही प्राथमिकता है। इसलिए एजाज़ की वफ़ादारी सबसे ऊँची बोली लगाने वाले के साथ है, जो एक अनुस्मारक (द्योतक) है कि विचारधारा कभी-कभी राजनीतिक खेल में पीछे रह सकती है।
रिपोर्टर : अभी आप किसके साथ जुड़े हो?
एजाज़ : हर किसी के साथ जुड़ा हूँ; …सच में।
रिपोर्टर : मतलब, जो पैसा दे-दे, उसके साथ?
एजाज़ : हाँ; हमारा क्या है…?

संक्षेप में ‘तहलका’ एसआईटी की जाँच ने बूथ कैप्चरिंग की परेशान करने वाली वास्तविकता को उजागर किया है, जो चुनावी धोखाधड़ी का एक स्पष्ट रूप है और लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। इस अनैतिक प्रथा को बूथ लूट के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें किसी विशिष्ट उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के वफ़ादारों या भाड़े के अपराधियों द्वारा मतदान केंद्रों पर हेर-फेर का खेल शामिल है। यह न केवल वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करता है, बल्कि यह मतदाता दमन का एक गम्भीर रूप भी है। जैसा कि चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले 4एम के बारे में चेतावनी जारी की है, ‘तहलका’ के रहस्योद्घाटन ने पहले एम यानी बाहुबल पर ध्यान केंद्रित किया है। यह महत्त्वपूर्ण है कि सत्ता के द्वारा ऐसे दुरुपयोग से निपटने और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखण्डता की रक्षा के लिए कड़े क़दम उठाये जाएँ।
बूथ कैप्चरिंग के मूल कारणों को संबोधित करके और कड़े नियमों को लागू करके हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं। केवल सामूहिक प्रयासों से ही हम लोकतंत्र के सिद्धांतों को क़ायम रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में प्रत्येक वोट मायने रखता है।