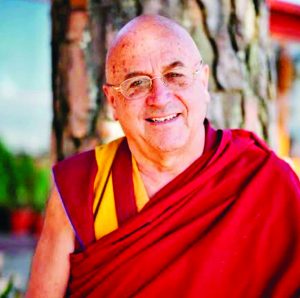महेंद्र सिंह राठौड़
अवैज्ञानिक खनन और सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाना मौत को न्यौता देने जैसा है। हरियाणा के ज़िला भिवानी में पत्थर की डाडम खान में यही सब कुछ हो रहा था। सरकारी विभागों की अनदेखी का नतीजा यह रहा कि खनन कम्पनी गोवर्धन माइंस ऐंड मिनरल्स कम्पनी मनमाने तरीक़े से काम कर रही थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की टीम ने अपनी जाँच रिपोर्ट में कम्पनी पर अवैज्ञानिक तरीक़े से खनन, बल्कि अरावली वन क्षेत्र में घुसपैठ जैसे गम्भीर आरोप दर्ज किये थे।
अब तो जाँच में बहुत-सी गम्भीर ख़ामियाँ सामने आ रही हैं। पर्यावरण से लेकर तय अनुमति से ज़्यादा गहराई में खनन करने जैसी बात सामने आ रही है। यह कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, बल्कि अक्टूबर वर्ष 2021 में एनजीटी टीम की औचक जाँच में गम्भीर ख़ामियाँ मिलीं।
सवाल यह कि कम्पनी को काम करने की अनुमति किस आधार पर दी गयी। खान में दिहाड़ी पर काम करने वाले कामगारों की राय में खान मौत के कुएँ जैसी थी। कभी भी हादसा होने का ख़तरा हरदम बना रहता था। बावजूद इसके पेट के लिए काम करने को मजबूरी थी। दिहाड़ीदारों की तो मजबूरी हो सकती है, लेकिन सरकारी विभागों की मजबूरी समझ से बाहर है, जिन्होंने गम्भीर आरोपों के बावजूद कम्पनी को फिर से काम करने की अनुमति दी।
नये साल की शुरुआत में डाडम की पत्थर खान ने पाँच लोगों को लील लिया। हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन काफ़ी समय तक रुका काम कुछ समय पहले ही शुरू हुआ था, लिहाज़ा कामगारों की संख्या कम थी।
भिवानी ज़िले में तौशाम पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर की कई खानें हैं। खानक, रिवासा, निगाना, दुल्हेड़ी, धारण और खरकड़ी मखवा में भी डाडम हादसे के बाद सरकार को अहतियाती क़दम उठा लेने चाहिए, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। वरना हादसे के बाद जाँच, मृतकों को मुआवज़ा, कम्पनी पर कार्रवाई जैसी औपचारिकताएँ होती रहेंगी। डाडम खनन क्षेत्र अरावली की पहाडिय़ों वाला है, यहाँ वन क्षेत्र है, जहाँ किसी तरह का निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है।
कहा जाए तो यह खनन प्रतिबन्धित इलाक़ा होता है। लेकिन औचक जाँच में जाँच ऐसे क्षेत्र में खनन में काम आने वाली मशीनें और औज़ार आदि मिले। अरावली क्षेत्र में पर्यावरण से छेड़छाड़ के मद्देनज़र सर्वोच्च न्यायालय के कड़े आदेश हैं, जिनकी अनदेखी कई बार होती दिखी है। जबकि पिछले वर्ष राज्य के फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गाँव में अरावली क्षेत्र में दशकों से बने सैकड़ों घर तोड़ दिये गये थे। पूरे क्षेत्र में अवैध निर्माण गिराने से एक लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जबकि वहाँ रहने वालों के बिजली और पानी के कनेक्शन तक थे। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन डाडम में अवैज्ञानिक और अवैध खनन के आरोपों पर काम करने वाली कम्पनी पर कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। शुरुआती जाँच में पाया गया है कि डाडम खान में बैच बनाकर खनन नहीं हो रहा था। बैच एक तरह से पहाड़ों के बीच रास्ते बनाकर खनन क्षेत्र तक पहुँचने का सुरक्षित माध्यम होता है। अगर पहाड़़ दरकता है, तो उसका ज़्यादा हिस्सा उस रास्ते (बैच) पर गिरता है, जिससे जन हानि बच सके। जाँच में पाया गया है कि खनन क्षेत्र के कुछ पहाड़ों में दरारें आयी हुई हैं। बारूद के विस्फोट से दरार वाले इन पहाड़ों के दरकने का ख़तरा बना हुआ है। इस हादसे की वजह भी दरार वाले पहाड़ का गिरना ही रहा, जिसमें वहाँ काम करने वाले लोग दब गये। खनन के काम में जुटी बड़ी मशीनें ट्रैक्टर आदि उससे बुरी तरह से पिचक गये।
राहत कार्य के बाद बचे लोग ख़ुशक़िस्मत ही कहे जाएँगे। खनन के काम में अवैध और अवैज्ञानिक जैसी बातें नयी नहीं है। लेकिन गहराई में ये बातें जानलेवा साबित होती हैं। जाँच टीम ने पाया कि डाडम खान में 109 मीटर तक की गहराई हो गयी है, जबकि सरकारी अनुमति 78 मीटर तक की है। तय सीमा से ज़्यादा गहराई में खनन क्यों हो रहा था। 31 मीटर ज़्यादा गहराई कोई एक-दो महीने में तो नहीं हो गयी थी।
यह राज्य सरकार की अनदेखी का एक उदाहरण है। खनन करोड़ों का कारोबार है और लाख्रों रुपये की भेंट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिना इसके करोड़ों का काम चल ही नहीं सकता। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है। सन् 2013 में खनन और भूभर्ग विभाग ने डाडम खान की नीलामी की तो इसके लिए कर्मजीत सिंह ऐंड कम्पनी (केजेएसएल) और सुन्दर मार्केटिंग एसोसिएट (एसएमए) को सबसे ज़्यादा बोली देने पर योग्य पाया गया।
सन् 2015 में कर्मजीत सिंह ऐंड कम्पनी ने सरकार से आग्रह किया कि वह डाडम खान ठेके पर आगे काम नही करना चाहती। मई, 2015 में कर्मजीत सिंह ऐंड कम्पनी के 51 फ़ीसदी शेयर (हिस्सा) सुन्दर मार्केटिंग एसोसिएट को दे दिये गये। यह सब कुछ हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि सुन्दर मार्केटिंग एसोसएशन नामक कम्पनी के पास खनन का पर्याप्त अनुभव नहीं है। एक तरह से वह डाडम खान में खनन काम के लिए सक्षम नहीं है। बिना पर्याप्त अनुभव के उसे कर्मजीत सिंह ऐंड कम्पनी के साथ सयुक्त रुप से ठेका किस आधार पर दिया गया?
सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया और सुन्दर एसोसिएट नामक कम्पनी का ठेका रद्द कर दिया और खान क्षेत्र हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआईडीसी) के सुपर्द कर दिया। काफ़ी महीनों तक खान बन्द रही। मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुँचा। आख़िर नवंबर, 2017 में डाडम खान का ठेका गोवर्धन माइंस ऐंड मिनरल्स कम्पनी को मिला, जो अब तक उसी के पास है। काम मिलने के बाद कम्पनी विवादों में घिरी रही है। खनन के लिए विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और पर्यावरण के दूषित होने जैसे आरोप बराबर लगते रहे हैं। सन् 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की छ: सदस्यीय टीम ने शिकायतों के बाद खान क्षेत्र का औचक दौरा किया, तो वहाँ बहुत-सी ख़ामियाँ पायी गयीं। इन्हें गम्भीरता से लिया गया होता और ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया गया होता, तो डाडम हादसा नहीं होता। खनन के ठेकेदार जहाँ आर्थिक रूप से मज़बूत होते हैं। वहीं राजनीतिक तौर पर भी बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राजनीतिक संरक्षण के आरोपों को ख़ारिज़ करते हुए कहा है कि हादसे की विस्तृत जाँच होगी और दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के आदेश पर अतिरिक्त ज़िला उपायुक्त (एडीसी) राहुल नरवाल की अध्यक्षता में समिति गठित कर हादसे की विस्तृत जाँच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। डाडम खान पर्यावरण के लिए क्षेत्र में एक ख़तरनाक संकेत है। सरकार के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर मोटी कमायी करने वाले ठेकेदारों को शायद पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों से जैसे कोई सरोकार नहीं होता।
मामले की गम्भीरता को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आठ सदस्यीय समिति गठित कर दी है। इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र से जुड़े कई विभागों के उच्चाधिकारियों को शामिल कर आठ सदस्यीय समिति गठित की गयी है। इस समिति की जाँच रिपोर्ट काफ़ी महत्त्वपूर्ण साबित होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि तय समय में जाँच रिपोर्ट आये और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की जाए, वरना डाडम जैसे हादसे होते रहेंगे। कम्पनियाँ और मालिक बदलते रहेंगे और पहले की तरह सरकारी नियमों की अवहेलना होती रहेगी। यह सिलसिला रुकना चाहिए वरना कामगार केवल 500 रुपये की दिहाड़ी पर जान हथेली पर लेकर जाते रहेंगे।
हादसे में बचे एक कामगार के मुताबिक, डाडम खान में काम पर जाते समय मौत की आशंका बनी रहती है। यहाँ के कई पहाड़ों में दरारें आयी हुई हैं, जो विस्फोट के बाद भरभराकर गिर सकते हैं। मजबूरी यह कि हम लोग खनन के काम शुरू से कर रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। यह हमारी रोज़ी-रोटी है। लेकिन इसके बदले मौत मिलती है, तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। मौत के कुएँ में आख़िर कब तक उतरते रहेंगे। किसी दिन उसी में समा जाएँगे। सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सरकारों की होती है। ठेकेदार या उसके लोग तो ज़्यादा-से-ज़्यादा खनन करने में लगे रहते हैं। ये खाने उनके लिए सोना उगलती हैं। लेकिन हमारे पास तो पेट भरने लायक पर्याप्त पैसा ही नहीं मिल पाता है।
शिकायतें आती रही हैं
डाडम खान क्षेत्र भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह हैं। सन् 2014 से लगातार दूसरी बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके मुताबिक, शिकायतों के बाद वह सम्बन्धित विभागों और सरकार को यहाँ होने वाले बेक़ायदा काम के बारे में बताते रहे हैं। डाडम खान क्षेत्र के चार स्थानों पर खनन के सरकारी दिशा-निर्देशों की उल्लंघना हो रही है, यह उनकी जानकारी में है और इसके बार में स्पष्ट तौर पर बताया जा चुका है। यही वजह है कि बार-बार जाँच और मामला उच्च न्यायालय में जाता रहा है। हादसे को दुर्भाग्यशाली बताते हुए उन्होंने जाँच में दोषी पाये जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है।