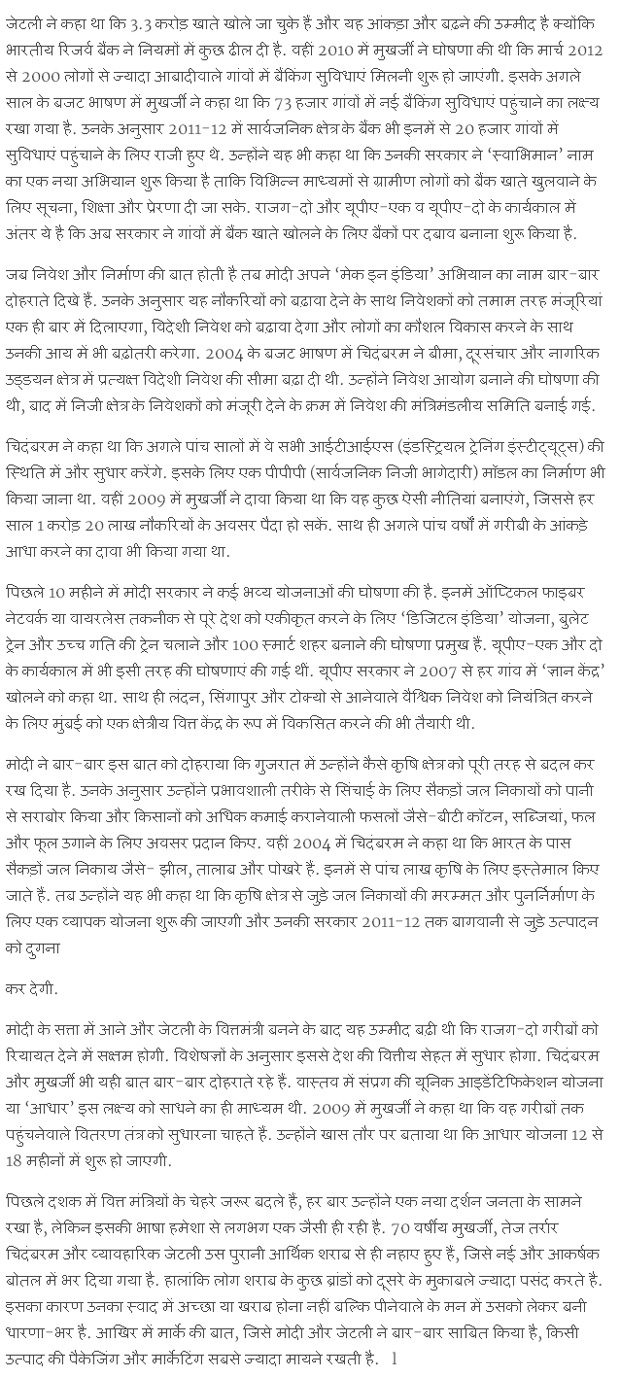देश में दलितों की स्थिति में क्या कोई सुधार आया है?
दलितों से छुआछूत का मामला हो या मंदिर में प्रवेश को लेकर टकराहट या उनसे व्यभिचार की घटनाएं- लगभग हर रोज देश के किसी न किसी कोने से देखने-सुनने को मिल जाती हैं. मंदिर में प्रवेश के मसले पर दलितों की हत्या तक कर दी जाती है. थोड़ी पुरानी बात है. उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के आने के बाद बरेली के पास ही एक गांव में मंदिर में दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था. अखबार और टेलीविजन चैनलों ने इस घटना को छापा-दिखाया. पुजारी मंदिर में ताला लगाकर गांव छोड़कर भाग गया लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकारी तंत्र में इसे लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी.
देश में इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत सख्त कानून मौजूद हैं. ‘दलित एक्ट’ के तहत सजा के कठोर प्रावधान किए गए हैं. दलित उत्पीड़न के संदर्भ में उन्हें उचित ढंग से लागू किया जाए तो उसके भय से ही बहुत हद तक ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा. दलित, सवर्णों के रास्ते से गुजर कर न जाएं इसलिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बहुत ऊंची-ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गईं. अफ्रीका में ‘रंगभेद’ की बातें जब थीं तब वहां काले लोगों के लिए चलने के लिए सड़कों पर अलग लेन होती थीं. उनके लिए दुकानें अलग होती थीं. वे गोरों की दुकानों से अपनी जरूरत का समान नहीं खरीद सकते थे. वे रेलगाडि़यों के सामान्य डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकते थे. उनके लिए ट्रेनों में अलग डिब्बे होते थे. पर भारत में यह सब तो आज भी घट रहा है. ‘रंगभेद’ व्यवस्था के खिलाफ पूरी दुनिया एक हो गई थी. भारत भी ‘रंगभेद’ के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था. उस जमाने में अफ्रीका के लिए ‘वीजा’ नहीं मिलता था. मुझे याद है कि उन दिनों मुझे भारत सरकार ने 1980 के आसपास किसी साल में पासपोर्ट जारी किया तो उसपर साफ-साफ लिखा था कि आप दो देशों (अफ्रीका और इजरायल) की यात्रा नहीं कर सकते थे. लेकिन यह सोचकर भी शर्म आती है कि आज 21वीं सदी के भारत में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं! ‘रंगभेद’ के खिलाफ जो माहौल पूरी दुनिया में बना वैसा भारत में ‘जाति-व्यवस्था’ के खिलाफ कभी बन नहीं पाया. ‘रंगभेद’ की जो विशेषताएं थीं, वे सब इस जाति व्यवस्था में पाई जाती हैं. यहां जाति-व्यवस्था के बने रहने की मूल वजह ‘हिन्दू धर्म’ है. धार्मिक व्यवस्था में बदलाव लाए बगैर आप सिर्फ कानून के सहारे सामाजिक या धार्मिक स्तर पर दलित उत्पीड़न खत्म नहीं कर सकते. चाहे इस देश में लेनिन ही क्यों न पैदा हाे लें.
मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं कि जाति-व्यवस्था या दलित उत्पीड़न को खत्म करने के प्रयास अपने देश में ईमानदारी से नहीं हुए?
मैं आपको थोड़ा पीछे स्वतंत्रता संग्राम में ले जाना चाहूंगा. 1929-30 के आसपास गांधी जी की बाबा साहब अांबेडकर की पहली मुलाकात हुई थी तब उन्होंने अांबेडकर से कहा कि मैंने देश की आजादी का आंदोलन छेड़ रखा है. अांबेडकर ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया, ‘मैं सारे देश की आजादी की लड़ाई के साथ उन एक चौथाई जनता के लिए भी लड़ना चाहता हूं जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हैै. आजादी की लड़ाई में सारा देश एक है और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, वह सारे देश के खिलाफ है. मेरी लड़ाई बहुत कठिन है.’ औपनिवेशिक सत्ता (अंग्रेजों) के खिलाफ तो सारा देश खड़ा था इसलिए उनका जाना तय था लेकिन देश के लोग अपने ही लोगों के साथ जो भेदभाव बरत रहे हैं तो मेरी लड़ाई तो उनसे भी है. दलितों, पिछड़ों को न तो जमीन रखने का अधिकार था, न ही उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार था. वे सदियों से जमींदारों और सामंतों के खेतों और कारखानों में मजदूरी करते चले आ रहे थे. हिंदू धर्म, वर्ण व्यवस्था और जातिगत व्यवस्था की खुलकर वकालत करते हैं. डॉ. अांबेडकर ने सोचा कि यहां जातिगत व्यवस्था का मूल आधार धार्मिक व्यवस्था से ही लड़ना पड़ेगा. संकेत के तौर पर 1927 में डॉ. अांबेडकर ने ‘मनुस्मृति’ को जलाया. यह यहां दोहराने की जरूरत नहीं है कि इस हिंदू धर्म-ग्रंथ में शूद्रों के बारे में क्या-क्या लिखा गया है. मनुस्मृति के जलाए जाने से हिंदू घबरा उठे.
धार्मिक व्यवस्था में बदलाव लाए बगैर आप सिर्फ कानून के सहारे सामाजिक या धार्मिक स्तर पर दलित उत्पीड़न खत्म नहीं कर सकते. चाहे इस देश में लेनिन ही क्यों न पैदा होे लें
एक उदाहरण और देना चाहूंगा. अपने देश में दलितों को कुएं और तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता था. महाराष्ट्र में इस भेदभाव से लड़ने के लिए बाबा साहब ने ‘महाड़’ आंदोलन चलाया. जलगांव में एक तालाब के किनारे लाखों की संख्या में दलित जुटे और उन्होंने प्रकृति के पानी पर अपना हक जताया था. बाद में कोंकणी ब्राह्मणों ने उस तालाब के शुद्धिकरण के लिए मंत्रोच्चारण और पूजा-पाठ आयोजित करवाया. इसके विरोध में अांबेडकर ने 12 दलितों का चयन किया और कहा कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो. देश में सनसनी फैल गई. तत्काल ब्राह्मणों ने दलितों के लिए गांव के दो कुएं पानी लेने के लिए खोल दिए. ब्राह्मणों ने इस दबाव में कुएं का पानी लेने की आजादी दलितों को दे दी क्योंकि उन्हें लगा कि उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा. अांबेडकर ने पूना-पैक्ट के समय यह बयान दिया कि वे बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो तुरंत पैक्ट पर समझौता हो गया. पूना पैक्ट की वजह से दलितों काे बहुत लाभ हुआ. उनका सबलीकरण इस पैक्ट की वजह से ही संभव हो पाया. इसी पैक्ट की वजह से दलितों को आरक्षण आधा-अधूरा ही सही मिल पाया. इसी पैक्ट के नतीजे के चलते दलित समुदाय के लोग मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी बन पाए. इसी पैक्ट की वजह से लाखों की संख्या में दलितों के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले. इस बारे में प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ का एक लेख है ‘कछुआ धर्म’. वे पंडित थे. हर रोज पूजा-अर्चना करते थे. टीका लगाते थे. उन्होंने अपने लेख में हिंदू धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या की थी. उन्होंने लिखा है, ‘हिंदू धर्म को जब अपने ऊपर खतरा नजर आता है तब वह कछुए की तरह अपनी गर्दन और मुंह अंदर समेट कर मृत के समान निष्क्रिय होने का प्रदर्शन करता है लेकिन जब कोई संकट नहीं दिखता है तब वह गर्दन उठाकर आक्रामक मुद्रा में ऐसे चलता है मानो पूरी दुनिया जीतने निकला हो.’
प्राचीन काल से एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा. गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा और उपदेशों के बल पर जाति-व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा लिया और धर्म-परिवर्तन किया. बड़ी संख्या में ब्राह्मण ही बौद्धभिक्षु बने. कई राजाओं ने भिक्षुओं के खिलाफ अभियान चलाया. पुष्यमित्र आदि राजाओं ने छोटे-मोटे अभियान चलाए. सबसे जोरदार अभियान बौद्ध-धर्म के खिलाफ 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य के समर्थकों ने चलाए. शंकराचार्य और उसके समर्थकों को हिंदू राजाओं का समर्थन था, उन्हें किसी का डर नहीं था तो वे बौद्ध मठों को तोड़ने और भिक्षुओं पर हमले करने लगे. दरअसल, बुद्ध वर्ण व्यवस्था पर चोट कर रहे थे. वे मानव-मानव के बीच वर्ण के आधार पर भेद करने की बात को झुठला रहे थे. वर्ण व्यवस्था की रक्षा और शंकराचार्य का समर्थन पाकर तीसरी सदी में व्यापक स्तर पर हिंदू धर्म-ग्रंथ रचे गए. उससे पूर्व सिर्फ वेदों की रचनाएं ही हुई थीं, जिनका जिक्र बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है. बौद्ध-ग्रंथों में रामायण और महाभारत की चर्चा नहीं मिलती है. बुद्ध के आसपास ही चार्वाक भी हुए जिन्होंने तीन वेद होने की ही बात की है. मतलब साफ है कि सिर्फ तीन वेद ही बुद्ध-चार्वाक के समय तक रचे गए थे. आप गौर करें तो पाएंगे, शंकराचार्य के बाद जिस भी धर्म ग्रंथ की रचना की गई, उनमें वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है.
आप पूना पैक्ट के जरिए दलितों के जीवन में बदलाव आने की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर यह सुनने को मिलता है किसी भी सरकार ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है. उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपका जबाव चाहूंगा?
हां, सरकारों द्वारा दलितों के विकास के लिए उठाए गए कदम संतोषजनक नहीं कहे जा सकते हैं लेकिन यह कहना कि दलितों के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है, एक उग्रवादी किस्म की सोच है. उत्तर प्रदेश हिंदुत्ववादियों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारी धार्मिक नदियां उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं इसलिए इस प्रदेश का सबसे ज्यादा सांप्रदायीकरण हुआ है. गंगा का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है. कुंभ का आयोजन इलाहाबाद में होता है. ज्योतिर्लिंग बनारस में है. मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश हिंदुत्व को उर्वर भूमि प्रदान करने का काम करती रही है. यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी घटित होता है तो उसका असर दूसरे राज्यों पर जरूर पड़ता है. इसलिए मेरा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में जाति-व्यवस्था को कमजोर कर दिया जाए तो उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा.
मायावती या कोई दलित हजार बार भी मुख्यमंत्री बन जाए, उससे दलितों के जीवन में परिवर्तन नहीं आनेवाला. परिवर्तन सामाजिक आंदोलन के दबाव के फलस्वरूप ही आ पाएगा
कांशीराम -मायावती का आंदोलन और खासकर मायावती का उत्तर प्रदेश की सत्ता में आसीन होने का असर दलितों की जिंदगी बदलने में कितना हो पाया है?
जाति-व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक आंदोलन चलाए गए थे. वह बुद्ध, ज्योतिबा फुले से लेकर आंबेडकर तक चलता चला आ रहा है. आंबेडकर के बाद जो भी दलित आंदोलन हुए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि सभी दलित नेतृत्व अपनी-अपनी अलग-अलग डफली पीटते चले गए. खुद आंबेडकर द्वारा खड़ी की गई रिपब्लिकन पार्टी भी बाद के दिनों में चार भागों में बंट गई. उसका एक भाग रामदास अठावले के नेतृत्व में पहले शिवसेना और बाद में भाजपा में शामिल हो चुका है. आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल हो गए. एक भाग में योगेंद्र कबाड़े थे, वे अब भाजपा में हैं. रिपब्लिकन पार्टी के एक भाग के नेता आरएस गंवई थे जो कांग्रेस में शामिल हो गए. कुछ दिनों तक वे केरल के राज्यपाल भी रहे. आंबेडकर के बाद उनकी पार्टी विखंिडत हुई और उसका अधिकांश हिस्सा दक्षिणपंथी पार्टियों में शामिल होता चला गया. निश्चित तौर पर इससे सामाजिक न्याय की लड़ाई कमजोर हुई. दलित राजनीति में निर्वात-सा बन गया. उसका फायदा निश्चित तौर पर कांशीराम को मिला.
कांशीराम ने शुरू में यह तय किया कि दलितों को सबसे पहले सामाजिक तौर पर चेतना संपन्न किया जाए. 1960-80 तक उन्होंने चुनाव लड़ने की बात नहीं की थी. इस दलित राजनीति का मूलाधार बामसेफ पार्टी रही. कांशीराम ने सामाजिक जागृति के लिए बहुत मेहनत की. वे गली-गली साइकिल पर घूमते थे. उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का असर बहुत पड़ा. उन्होंने दलितों को अपने आंदोलन से बड़ी संख्या में जोड़ा. दलितों को संगठित करने के बाद उन्होंने राजनीति में उतरने की बात की जिसके चलते बामसेफ भी कई भागों में बंट गया. कांशीराम से अलग हुए दूसरे दल सामाजिक जागृति फलाने की बात पर जोर देने की बात कर रहे थे. आंबेडकर ने सामाजिक बदलाव कोई मंत्री पद पर रहते हुए नहीं किया था. सामाजिक आंदोलनों के जरिए जो परिवर्तन समाज में आता है, वह स्थायी भाववाला होता है.
मतलब आप यह कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन की बात मायावती तक आते-आते पीछे छूट गई?
सामाजिक परिवर्तन पीछे ही नहीं छूटा बल्कि उलटी दिशा में चल पड़ा. कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी और राजनीति में पूरी तरह उतर गए. सामाजिक आंदोलन से जो दबाव समाज में बनता था, वह दबाव बनना खत्म हो गया और जिसके चलते दलित उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ, इसे साफ-साफ महसूस किया जा सकता है. गांधी और आंबेडकर की जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने साफ-साफ कहा था कि सामाजिक आंदोलनों का राजनीतिक आंदोलनों पर वर्चस्व होना चाहिए. राजनीतिक आंदोलन के चलते सत्ता तो मिल जाएगी लेकिन समाज में बदलाव नहीं आ पाएगा इसलिए यदि समाज बदलना है तो सामाजिक आंदोलन बहुत जरूरी हैं.
क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि कांशीराम और मायावती द्वारा सामाजिक आंदोलन को अचानक बंद करके राजनीति शुरू कर देने से समाज में बदलाव की दिशा में निर्वात की स्थिति बन गई?
जी हां, बहुत बड़ा निर्वात बन गया और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज दलितों की स्थिति कई गुणा ज्यादा बेहतर होती. मैं यह कतई नहीं कह रहा हूं कि दलितों को राजनीति में नहीं आना चाहिए. मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सामाजिक आंदोलन से मानस में बदलाव आता है और इसका असर दलित ही नहीं बल्कि गैर-दलितों पर भी देखा जा सकता है. कांशीराम के राजनीति में आने के फैसले से दलितों की सामाजिक स्थिति में जो सुधार दर्ज किया जा रहा था, वह उलटी दिशा में चल पड़ा.
क्या इस परिस्थिति से जो सामाजिक दबाव बनने लगा था वह अब नहीं बन पा रहा है. क्या इसकी वजह से भी दलितों के उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है?
देखिए, कांशीराम-मायावती ने जब तक सामाजिक आंदोलन छेड़े रखा था तब तक हर राजनीतिक पार्टी इस दबाव में काम करती थी कि बिना दलित को साथ लिए चुनाव जीतना मुश्किल होगा. लेकिन मायावती के राजनीति में आते ही ब्राह्मण सत्ता के केंद्र में आ गए. ब्राह्मणों के बारे में यह गुणगान होने लगा कि वे हाशिये पर चले गए हैं. उनकी स्थिति खराब हो गई है. मैं यहां किसी खास व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. ब्राह्मण का मतलब व्यवस्था से मानता हूं. कांशीराम पहले ‘तिलक, तराजू और तलवार…’ का नारा लगाते थे लेकिन राजनीति में आते ही वे ‘हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है’ के नारे लगाने लगे. ब्रह्मा, विष्णु और महेश के खिलाफ अांबेडकर पूरा जीवन लड़ते रहे. कांशीराम और मायावती ने इसे उलट दिया.
कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के निर्माण के बाद एक और खतरनाक कदम उठाया था. उन्होंने कहा कि अपनी-अपनी जातियों को मजबूत करो और इसी से कल्याण होगा. इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलितों की अलग-अलग जातियों के सम्मेलन होने लगे. लेकिन कांशीराम और मायावती भूल गए कि जातियों के मजबूत होने से जाति-व्यवस्था कैसे टूटेगी? इससे हरेक जाति का गौरव भड़क उठा और सामाजिक बदलाव और जाति-व्यवस्था के खिलाफ चल रहे आंदोलन को जोरदार झटका लगा. राजनीति में जातीय धुव्रीकरण बड़े पैमाने पर होने लगा. जातियों के नाम पर अलग-अलग जाति के गुंडे ध्रुवीकरण की वजह से जीतकर नगरपालिका से लेकर विधानसभा और संसद तक में पहुंचने लगे. आज राजनीति का चेहरा जातीय ध्रुवीकरण की वजह से ज्यादा विद्रूप हो गया है. इसकी वजह से देश में लोकतंत्र नहीं जातियां फल-फूल रही हैं. अब पार्टियां नहीं जातियां सत्ता में आने लगी हैं. कांशीराम-मायावती ने सभी जातियों के लोगों से मंत्री पद देने का वायदा किया. सत्ता में आने के बाद मायावती ने ऐसा किया भी लेकिन सभी सुख-सुविधा पाने के बाद भी उन जातियों के लोगों ने पांच साल के भीतर ही इन्हें लात मारकर किनारा कर लिया. मतलब यह है कि आप जाति-व्यवस्था खत्म करने की लड़ाई को मजबूत नहीं करेंगे और जातियों को मजबूत करने की बात करेंगे तो इससे दलित विरोधी शक्तियां ही मजबूत होंगी. बसपा के शासनकाल में तमाम जातियां दलित विरोधी शक्तियों के रूप में खड़ी हो गईं.
कांशीराम पहले ‘तिलक, तराजू और तलवार…’ का नारा लगाते थे लेकिन राजनीति में आते ही वे ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश है’ के नारे लगाने लगे
यह अक्सर आरोप लगाया जाता है कि दलित चिंतक, दलित नेतृत्व ही दलित महिलाओं की उपेक्षा करते हैं. वे ही उन्हें आगे नहीं आने देना चाहते हैं.
जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बाबा साहेब ने अपने आंदोलन के जरिए यह कोशिश की थी कि दलित महिलाएं आगे आएं. वे दलित महिलाओं के साथ हिंदू महिलाओं को भी आगे लाने की बात कर रहे थे. इसलिए 1951 में वह हिंदू कोड बिल लेकर आए. हिंदू कोड बिल, सवर्ण महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार देने और दहेज प्रथा आदि जैसी कुरीतियों के खिलाफ लाया गया. लेकिन उस समय बनारस, इलाहाबाद और देश के दूसरे हिस्सों के साधू-संन्यासी गोलबंद होकर बिल के विरोध में उठ खड़े हो गए. बिल को स्वीकृति नहीं मिल पाई. दलित पुरुष नेता तो कई उभरे लेकिन महिला नेतृत्व नहीं उभर पाया. बाबा साहब की मृत्यु आजादी के चंद वर्षों बाद ही हो गई. उसके बाद जगजीवन राम आए तो उन्होंने भी दलित महिलाओं को नेतृत्व दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया. उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी मीरा कुमार राजनीति में आईं जरूर लेकिन उन्हें यह विरासत में मिली. उन्हें राजनीति संघर्ष के रास्ते से नहीं मिली है. रिपब्लिकन पार्टी के चारों धड़े जिसका मैंने पहले जिक्र किया उसमें से कोई महिला नेतृत्व सामने नहीं आया. मायावती ने तो हद ही कर दी. उसके नेतृत्व में कोई दलित पुरुष तो छोडि़ए, कोई दलित महिला भी आगे नहीं आ पाई. दलित राजनीति में मायावती को छोड़कर कोई दूसरी महिला नजर नहीं आती हैं. मायावती खुद चार बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं लेकिन किसी दूसरी दलित महिला को उन्होंने आगे नहीं आने दिया. मायावती की सामंती सोच देखिए कि उन्होंने पांच-छह वर्ष पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की बात की थी. उन्होंने यह भी कहा था, ‘मैं अपने उत्तराधिकारी का नाम एक लिफाफे में बंद करके जाऊंगी. मेरे मरने के बाद लिफाफा खोला जाएगा.’ मैं इस बात का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आनेवाली पीढ़ी दलित राजनीति में महिलाओं की स्थिति को समझ सके और उसे दुरुस्त करने की कवायद में लगे. दलित राजनीति में सफल पुरुष ने अपनी पत्नी को गृहणी बनाकर रखना पसंद किया. यह स्त्रीविरोधी मानसिकता है और यह भी उसी धर्म व्यवस्था की देन है. इसकी शिकार दूसरी पार्टियां भी रही हैं. महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का मामला दसियों साल से लटका पड़ा है. स्त्री विरोधी मानसिकता को मीडिया और सिनेमा भी बढ़ावा दे रहे हैं. पतियों की पूजा कीजिए और यह इच्छा कीजिए कि वह आपको बराबरी का दर्जा देगा, परस्पर विरोधी बातें हैं. कर्मकांडी व्यवस्था को खत्म किए बगैर स्त्रियों का कभी भी भला नहीं हो सकता है.







 आपके उपन्यास का शीर्षक ‘हिंदू : जीने का समृद्ध कबाड़’ में ‘जीने का…’ के पीछे क्या दर्शन है?
आपके उपन्यास का शीर्षक ‘हिंदू : जीने का समृद्ध कबाड़’ में ‘जीने का…’ के पीछे क्या दर्शन है?