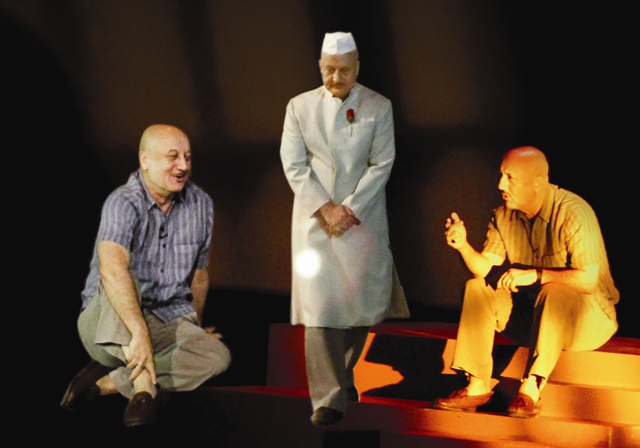जिस तरह सर्दी के मौसम में पुरानी चोट या जख्म की टीस ताजा हो जाती है, उसी तरह दिल्ली में सर्दी की दस्तक 16 दिसंबर 2012 की वीभत्स घटना का दर्द साथ ले आती है. निर्भया के साथ हुए हादसे ने महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के प्रति जागरूकता जगाई और हजारों संवेदनशील लोग उनकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए. उनका उद्देश्य था कि सरकार इस मुद्दे पर उनकी नाराजगी पर तुरंत संज्ञान ले और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे.
हालांकि दिल्ली की सड़कें अब भी सुरक्षित नहीं हो पाईं अलबत्ता अब घरों के आंगन भी सुरक्षित नहीं रहे. दरिंदों के वहशीपन की सारी हदें तब पार हो गईं जब चार साल की नेहा (परिवर्तित नाम) के साथ उसके घर से कुछ ही दूरी पर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया.
इस दरिंदगी के बाद कूड़े के ढेर पर बुरी तरह से घायल पड़ी वह बच्ची अपने पिता को ही बुला पाने में असमर्थ थी तो अपने साथ हुई उस दर्दनाक घटना के बारे में कैसे बता पाती! इस हादसे के बारे में बच्ची के दादा किशन ने अपना दर्द बयां किया, ‘ब्लेड से यहां काटा (गाल पर), होंठ पर भी ब्लेड मारा. सिर पर पत्थर मार दिया और गला घोंटा.’ सिसकी रोकते हुए कहते हैं, ‘मेरी बच्ची से बलात्कार भी किया.’
ये अक्टूबर की शाम थी और वह बच्ची दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है. ये वही अस्पताल है जिसने निर्भया के जख्म भी देखे थे, जहां वो अपने जख्मों से लड़ते-लड़ते जिंदगी की जंग हार गई थी. सूत्रों ने ‘तहलका’ को बताया कि नेहा के गुप्तांग के जख्म बहुत गंभीर थे और डॉक्टरों को वहां क्षत-विक्षत त्वचा जोड़ने में दो घंटे का समय लगा. चोटें इतनी गंभीर थीं कि पेशाब और मलत्याग के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया. डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची के शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक होने में करीब तीन महीने का वक्त लगेगा.
इस पीड़ित बच्ची का परिवार उत्तर-पश्चिम दिल्ली के केशवपुरम में रेल की पटरियों से सटी झुग्गियों में रहता है. उस बच्ची के घर पहुंचने में सीवेज से भरी और पानी के पाइपों की भूलभुलैया सरीखी गलियों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है. एटीएम के गलियारे के जैसे एक कमरे में नेहा की बड़ी बहन (पांच साल) गुमसुम सी बैठी हुई है और उसका आठ महीने का भाई खेल रहा है. फूट-फूटकर रोते हुए नेहा की दादी रामश्री बताती हैं, ‘यहां जगह कहां है! इधर ही ट्रैक के पास बैठे रहते थे सब शाम में. उ (नेहा) यहीं धुरा-मिट्टी में खेलती रहती थी.’ घटना को याद कर वह बताती हैं कि खून से लथपथ अपनी पोती को पहचानना उनके लिए कितना मुश्किल था, जिसे उस रात बस्ती की एक औरत कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी. नेहा की दादी के अनुसार, ‘हमारे हाथ लग जाता तो यहीं बोटी-बोटी कर के गाड़ देते.’
सरकारें अपनी उपलब्धियों के बखान के लिए विज्ञापनों पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च रही हैं लेकिन यौन अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रमों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है
इतने सब के बाद राहत की बात केवल इतनी है कि जब पुलिस द्वारा आरोपी को अस्पताल में चार और लोगों के साथ लाइन में खड़ा किया तब नेहा ने तुरंत उसे पहचान लिया, ‘राहुल भइया ने चोट लगाई मुझे.’ जिस व्यक्ति को वह मासूमियत से भइया कहकर पुकार रही थी, उसी ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया था. हालांकि उसकी प्यारी गुड़िया अब भी कमरे में टंगी हुई है लेकिन उसके दिहाड़ी मजदूर पिता मनोज, उसके लिए अस्पताल में नए खिलौने लेकर आते हैं.
बच्ची के दादा किशन ने ‘तहलका’ को बताया कि आरोपी ने बलात्कार की जगह से ब्लेड लाकर दिया है और उस दिन पहने हुए खून से सने कपड़े अपने घर से लाया है. शराब पीने के लिए इस इलाके में रोज आने वाले राहुल ने अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उस दिन बच्ची को चाऊमीन खिलाने और 10 रुपये देने का लालच दिया था.
किशन बताते हैं, ‘इस मामले की जांच जारी है और मुझे इस घिनौने काम में कुछ और लोगों के शामिल होने का पूरा यकीन है.’ वे आगे कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि नेहा को उस भयानक पल के बारे में कुछ भी याद रहे. वे फरियाद करते हैं, ‘हम बस उसका बेहतर भविष्य चाहते हैं. मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से यही चाहता हूं कि उसकी आगे की पढ़ाई और बेहतर इलाज का प्रबंध करा दें बस.’
बहरहाल, लोग अभी अखबार में छपी इस घटना की सुर्खियां भूले नहीं थे कि पश्चिमी दिल्ली के निलौठी में एक ढाई साल की नौनिहाल के साथ भी ऐसी ही घटना घट गई. वह बच्ची अपने घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी. कुछ ही दूर रामलीला चल रही थी. बच्ची की दादी जगवती बताती हैं, ‘रामलीला में उस वक्त गाना चल रहा था. गुडिया (बदला हुआ नाम) पीले कपड़े पहने हुए मेरे धोरे (पास) ही खेल रही थी. मेरा (घर के अंदर) दूध की बोतल धरना है कि इतने में गुड़िया गायब हाे चुकी थी.’
बच्ची की खोज रात में 11:30 बजे शुरू हुई. दुर्भाग्यवश जब तीन घंटे के बाद पुलिस और परिवार को बच्ची एक किलोमीटर दूर स्थित कर्मभूमि पार्क में मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. खून से लथपथ गुड़िया बेहोश पड़ी हुई थी. गुड़िया के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी उन्हीं लोगों ने किया था, जिन्हें वह भइया कहती थी. इस मामले में दो नाबालिगों लूची (16) और सनोज (17) को पकड़ा गया है.
दोनों किशोर अपने परिवार के साथ किराये के घर में रहते हैं. नौवीं कक्षा में पढ़ने वाला लूची गुड़िया के घर से पचास मीटर की दूरी पर रहता है और गुड़िया का चचेरा भाई उसे जानता था. दूसरा आरोपी सनोज गुड़िया के घर के पीछे बने नौ छोटे कमरों में से एक में अपनी मां और तीन भाइयों के साथ रहता है. वह कुछ साल पहले ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुका है.
घटना की श्रृंखलाओं को जोड़ते हुए पुलिस कहती है कि दोनों नाबालिगों ने बच्ची का अपहरण बिजली कटने के दौरान किया. एक पड़ोसी ने ‘तहलका’ को बताया, ‘बिजली जाने के दौरान लूची अपनी मां का इंतजार कर रहा था. इसके बाद वो हमारे साथ वापस रामलीला आ गया था.’ इसका मतलब है कि लूची ने बच्ची का अपहरण कर सनोज को सौंप दिया था और वापस रामलीला में आ गया. फिर वह अपनी मां को घर छोड़ने के बाद सनोज के पास पहुंचा होगा.
चौंकाने वाली बात ये है कि दोनों नाबालिग उस रात उन लोगों के साथ थे जो गुड़िया को ढूंढ़ रहे थे. अगले दिन लूची रोज की तरह स्कूल गया और सनोज आस-पड़ोस में ही घूमता रहा. लूची के एक सहपाठी ने बताया कि वह पढ़ाई में कमजोर था और कक्षा 9 में दो बार फेल हो चुका है. जिस पार्क में बच्ची का रेप हुआ उस पार्क में लूची देर रात तक बीड़ी पीता रहता था और सनोज ही उसका इकलौता साथी था.
घटना के कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने शक के आधार पर 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया. देर रात छापे के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया. पुलिस ने बताया कि कड़ी पूछताछ के दौरान दोनों टूट गए और इस वहशियाना हरकत को करना स्वीकार कर लिया. लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि दबाव में किए गए कबूलनामे को अदालत स्वीकार नहीं करती. अदालत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अपराध में उनकी संलिप्तता मानेगी.
एक हफ्ते के अंदर घटी ये दोनों घटनाएं भी जैसे कम थी क्योंकि फिर राजधानी के दूसरे इलाके से ऐसी ही घटना की खबर आई. पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पांच साल की मासूम के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. आरोपी उस बच्ची को उसी के घर की दूसरी मंजिल पर ले गया. वहां तीन लोगों ने कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. यहां भी वही मामला था. पीड़िता बहुत कम उम्र की थी, अपना दुख भी सही तरह से बयान नहीं कर सकती थी. उन क्रूर अपराधियों ने सोच-समझकर एक आसान शिकार को पकड़ा था. यहां तसल्ली देने वाली बात ये हो सकती है कि दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है. लेकिन कहानी क्या यहीं खत्म हो जाती है?
बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की ऐसी स्थिति में अब इस बात का अंदाजा लगाना बेहद जरूरी है कि देश की राजधानी और पूरा देश किस तरफ बढ़ रहा हैं! ऐसी घटनाओं का बार-बार होना गहरी निराशा से भर देता है. दिल्ली में जिम्मेदार अधिकारियों और चौकन्नी मीडिया की वजह से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट तत्परता से हो जाती है पर देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी जघन्य घटनाएं लगातार हो रही हैं लेकिन शर्म, बेबसी और समाज में लांछन लगने के डर से परदे में छुपी रह जाती हैं.
16 दिसंबर 2012 को घटा निर्भया कांड हमेशा एक संदर्भ के तौर पर रहेगा. जब मामला सामने आया तो लोगों में घटना को लेकर सामूहिक क्रोध था. त्वरित न्याय की मांग लिए लोग सड़कों पर उतरे थे. दिल्ली पुलिस पर सुस्त और संवेदनहीन होने के आरोप लगे. तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की ये कहने पर खिंचाई की गई कि ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता.
आज तीन साल बाद हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारे पास सख्त कानून के साधन हैं. जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर विधायिका ने सख्त कानून पास किए और सरकारी मशीनरी ने उनको लागू करना शुरू किया. न्यायपालिका ने ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया. लेकिन क्या स्थिति में कोई बदलाव आया है?
नेहा, गुड़िया और न जानें कितनी पीड़ित बच्चियां इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाने की गुहार लगा रही हैं. दिल्ली में घटीं बलात्कार की हालिया घटनाओं पर सवाल किया गया तो सीनियर स्पेशल कमीश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) दीपक मिश्रा का जवाब था, ‘अमेरिका हो या लंदन, बलात्कार की घटनाएं सभी जगह होती हैं.’ लेकिन जब आप सरकार ने उनके बयान की निंदा की, तब उन्होंने जवाब दिया कि मामले को राजनीतिक रंग देना बंद होना चाहिए.
नेहा के दादा और मां का मानना है कि एक समाज के बतौर हम असफल हो चुके हैं. ये समाज चरमरा गया है, सब खत्म हो गया है. कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं
तकनीकी रूप से दिल्ली की कानून-व्यवस्था संभालने वाली केंद्र सरकार भी महिला तो छोड़िए बच्चियों को बचाने के लिए भी राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करती नहीं दिख रही. दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सीधे-सीधे प्रधानमंत्री मोदी और उप-राज्यपाल नजीब जंग पर आरोप लगाना गैर-जरूरी था. सतीश उपाध्याय ने कहा, ‘पहले केजरीवाल अपने घर को संभाले और बाद में पुलिस और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करें. उनके सभी बयान राजनीतिक जुगलबंदी के अलावा और कुछ नहीं हैं.’
ऐसे में आश्चर्य होता है कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार की इसी तरह की प्रतिक्रिया पर तब हमला क्यों बोला था. यहां जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव के वक्त तो ऐसा लग रहा था कि नई सरकार शायद इन मामलों पर संवेदनशीलता दिखाएगी. चुनाव के वक्त भाजपा का एक नारा था, ‘बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अबकी बार मोदी सरकार.’ भाजपा सरकार इस मामले में देश तो दूर, दिल्ली जैसे छोटे क्षेत्र में भी असफल रही है.
एक पीड़ित बच्ची की चाची का प्रधानमंत्री से सवाल है, ‘आप कहते हैं बेटी बचाओ, मगर किसलिए, उन्हें घर में बिठाने के लिए? या लोगों द्वारा छेड़ने, बलात्कार और हत्या किए जाने के लिए.’
पिछले नौ महीनों में प्रतिदिन औसतन बलात्कार के छह और छेड़खानी के 14 मामले दिल्ली पुलिस के सामने आए हैं. आश्चर्यजनक रूप से जून 2012 में लागू हुए पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट के प्रभावी होने के बाद राजधानी में 1,492 मामले में सामने आए. इस कानून के वजूद में आने के बाद 244 केस दर्ज किए गए, जिनमें से सिर्फ 20 प्रतिशत मामलों में ही सजा हो पाई है.
इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में पिछले दो सालों में बलात्कार के मामले 200 प्रतिशत बढ़ गए हैं.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है, ‘हमें अपराधियों में डर पैदा करने की जरूरत है. पिछले साल महिलाओं के विरूद्ध अपराध के 38,000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से केवल 11,000 मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो पाए. इतना ही नहीं, 2014 में केवल 9 मामलों में दोषियों को सजा हुई थी.’ स्वाति का मानना है कि दिल्ली पुलिस को मामले की जांच, सबूत इकट्ठा करने और आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है. वे कहती हैं, ‘जब तक कोई मामला सुनवाई की स्थिति में पहुंचता है, तब तक पीड़ित पक्ष न्याय व्यवस्था में भरोसा खो चुका होता है. ऐसे में मामले कमजोर हो जाते हैं और आरोपी छूट जाते हैं.’
दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो किसी समय दिल्ली में हर बलात्कार के बाद शीला दीक्षित के घर के बाहर यह कहते हुए प्रदर्शन करते थे, ‘हमें मजबूर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए’, का लहजा बदल चुका है. खुद को जिम्मेदारी से अलग करते हुए वे अब कहते हैं, ‘मैं शीला दीक्षित नहीं हूं, अगर बलात्कार नहीं रुकते हैं, तो मैं प्रधानमंत्री को चैन से सोने नहीं दूंगा.’
सरकारें अपनी उपलब्धियों के बखान के लिए विज्ञापनों पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च रही हैं लेकिन लगातार बढ़ते यौन अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रमों पर बल देने कोई प्रयास नहीं किया जा रहा.
अलबत्ता जब मीडिया में इस तरह की घटनाओं पर जोर-शोर से बात होने लगती है तो कुछ फौरी किस्म के सुझाव जरूर उछाले जाते हैं. उदाहरण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग के बाद घोषित किया कि उनकी सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है कि 15 साल तक के बलात्कारियों को वयस्क माना जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है, ‘हां, ये सही है कि नाबालिगों की अपराधों में भागीदारी बढ़ी है पर उतनी भी नहीं जितनी बताई जा रही है. उन्हें अदालत में बालिग मानने की बजाय उनको सुधारने की दिशा में कदम उठाना ज्यादा जरूरी है.’ दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने बलात्कार के सभी लंबित मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाए जाने की संभावना पर भी विचार किया है. एक के बाद एक हो रहे ऐसे जघन्य अपराधों से परेशान आप सरकार ने दिल्ली में ‘जीरो डार्क एरिया इन सिटी’ यानी पूरे शहर में रौशनी के सुनिश्चित इंतजाम करने के लिए स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे जल्द से जल्द लगाए जाने को प्राथमिकता दी है. पर ये सब सुरक्षा के सतही इंतजाम हैं. लिंग आधारित भेदभाव के विरूद्ध तथा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में अभी सरकार को सोचना बाकी है. मोहल्ला सभाओं में इस विषय पर चर्चा शुरू कराने के बारे में आप सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है. दिलचस्प है कि सरकार में आने से पहले आप ने महंगाई, सरकार की नाकामियों जैसे मुद्दों को उठाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का इस्तेमाल सफलतापूर्वक किया था पर इस मुद्दे पर नुक्कड़ नाटकों से जागरूकता फैलाने का कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया है.
निर्भया कांड के बाद पूरी दिल्ली ऐसे विज्ञापनों और होर्डिंग्स से पट गई थी, जिनमें न केवल महिलाओं के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर और कानूनी कदमों के बारे में जानकारी दी गई थी बल्कि जन जागरूकता फैलाने का भी प्रयास किया गया था. वैसे विज्ञापन और पोस्टर अब दिल्ली की सड़कों से गायब हैं. वृंदा ग्रोवर ये बताती हैं कि अपराधों में लिप्त ज्यादातर किशोर स्कूल ड्रॉपआउट (पढ़ाई छोड़ चुके) हैं और ऐसे किशोरों की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है. ‘15 साल के नाबालिग को बालिग माना जाए, किस्म के फौरी इलाज सुझाकर सरकार केवल अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है. इस तरह के सुझाव देकर केजरीवाल साफ कर देते हैं कि उन्हें यौन अपराधों के कारणों की कोई समझ नहीं है. इसके बजाय उन्हें ये देखना चाहिए कि उन्होंने किशोर गृहों की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं. इस तरह प्रतिक्रियात्मक तौर पर लागू किए गए कानून इस समस्या का समाधान नहीं हैं.’
अखबारों की खबरें और टीवी चैनल एक ओर दिल्ली को ‘रेप सिटी’ घोषित करते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सारा देश जैसे ‘रेप हिस्टीरिया’ से ग्रस्त हो गया है. पिछले दो सालों में हर दिन 96 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से 95 प्रतिशत मामलों में पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किए हैं. बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली आते हैं. अगर आप गूगल पर खोजें तो और मलिन तस्वीर उभरती है. अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ दिल्ली में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है तो आप गलत हैं! सितंबर-अक्टूबर में ऐसी ही बर्बरता की खबरें कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी आई हैं. इसी साल अगस्त में झारखंड उच्च न्यायालय ने एक खबर पर संज्ञान लिया जिसके अनुसार एक पिता बलात्कार की शिकार अपनी बेटी को इलाज के लिए रोज चार किलोमीटर दूर ले जाता था. उच्च न्यायालय ने उस पिता को राज्य द्वारा एक लाख रुपये का अनुदान देने तथा बच्ची का बेहतर इलाज करवाने का निर्देश दिया. आंकड़ों का कम या ज्यादा होना इस तरह के अपराधों की भयावहता को कम नहीं करता.
वहीं समाज के दूसरे सिरे पर खाप पंचायतें ‘गैंगरेप’ के आदेश देने के लिए जानी जाती हैं. इसके अलावा वहां पीड़िता को बलात्कारी से शादी करने के लिए भी कहा जाता है और अक्सर पीड़िताओं को ही उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए दोषी ठहराया जाता है. जहां इस तरह का सामाजिक दृष्टिकोण है, वहां यौन अपराधों के मामलों का बढ़ना स्वाभाविक है. जब एक नाबालिग बच्ची को दुराचार का शिकार बनाया जाता है तो इस तरह की सोच ही तह में होती है. दो बार पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी पत्रकार निकोलस क्रिस्टॉफ ने एक ऐसा ही मामला उठाया जो इस बात की ओर संकेत करता है कि किस तरह हमारा समाज जाति और धर्म के आधार पर बलात्कारियों को संरक्षण प्रदान करता है. ‘बिटिया’ नाम की 13 साल की दलित लड़की का न केवल उच्च जातियों के पुरुषों द्वारा गैंगरेप किया गया बल्कि उसकी वीडियो क्लिप भी तैयार की गई. अपराधियों ने बाद में उसकी इस वीडियो क्लिप को सार्वजनिक करने और पीड़िता को मार डालने की धमकी. कुछ दिनों बाद ही उसके पिता अवाक रह गए, जब उन्होंने गांव के एक लड़के को वह वीडियो क्लिप देखते पाया. वह वीडियो क्लिप एक स्थानीय दुकान को बेच दी गई थी. पुलिस ने तो कोई कदम नहीं उठाया लेकिन गांव के बुजुर्गों ने जरूर एक ‘कड़ा’ कदम उठाया और लड़की के स्कूल जाने पर रोक लगा दी. निकोलस तब चौंक गए जब एक गांव वाले ने उनसे कहा, ‘अगर उसने (लड़के ने) लड़की का बलात्कार किया है, तो जरूर वह लड़की को पसंद करता होगा.’ इस तरह जो हल निकाला गया वह यह है कि लड़की को बलात्कारी के साथ शादी कर लेनी चाहिए. सोचने वाली बात है कि इस तरह की मानसिकता से मासूमों पर हो रहे इन जुल्मों से मुक्ति कैसे संभव है!
एक स्पष्ट सवाल सामने आता है कि इस माहौल में लैंगिक संवेदनशीलता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कानून के संबंध में देखा जाए तो देश खासा मजबूत हुआ है, बात चाहे बलात्कार संबंधी कड़े कानून की हो, किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन की या सरकार में बदलाव की. इसके बावजूद लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध जागरूकता दूर की कौड़ी है. दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से स्कूलों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देने के लिए कहते हैं. यहां स्वाति मालीवाल का सुझाव है कि यौन शिक्षा शुरू करने के साथ बड़े पैमाने पर लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध जागरूकता फैलाने की जरूरत है. इतनी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा. पुलिस, कानून निर्माता और समाज को एक साथ आकर योजना की रूपरेखा बनानी होगी और हफ्ते दर हफ्ते इसे लागू करने की जरूरत है.
ऐसे अपराधों की मानसिकता बनने में कहीं न कहीं समाज भी जिम्मेदार है. भारतीय समाज में सेक्स या उससे जुड़े किसी भी पहलू पर खुलकर बात करना वर्जित है. यहीं से एक खास उम्र में जन्मी यौन भावनाएं दमित होती हैं और कई बार हिंसक या आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देती हैं. ‘क्राई’ संस्था के ‘हक- सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स’ में अपराध में लिप्त बच्चों की काउंसलिंग के दौरान मिले ऐसे ही कुछ तथ्यों को एक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है. ये रिपोर्ट कहती है, ‘ज्यादातर परिवारों में यौन जरूरतों या सेक्सुअलिटी पर बात करना वर्जित है, जिससे बच्चे में प्राकृतिक रूप से मौजूद यौन भावनाएं दमित होती हैं. उनके पास इस मुद्दे पर बात करने या अपनी यौनेच्छा जाहिर करने का कोई रास्ता नहीं होता.’ इस तरह की इच्छाओं का लगातार दमन कई बार हिंसा और अपराध की शक्ल में प्रकट होता है.
बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की ऐसी स्थिति में अब इस बात का अंदाजा लगाना बेहद जरूरी है कि देश की राजधानी दिल्ली और पूरा देश किस तरफ बढ़ रहा है
दूसरी ओर हर खौफनाक मामले के सामने आने पर अपराधी को नपुंसक बनाने या उसे भीड़ के हवाले कर देने जैसी मांगें जोर-शोर से उठने लगती हैं. हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चों के साथ यौन हिंसा करने वाले दोषियों को रासायनिक तरीके अथवा सर्जरी द्वारा नपुंसक बनाए जाने का सुझाव सामने रखा है. न्यायमूर्ति एन. किरूबकरण ने सख्त शब्दों में कहा है, ‘वर्तमान कानून ऐसे अपराधियों से निपटने में नाकाम हैं. ऐसे में न्याय-व्यवस्था हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकती, खासतौर पर तब, जब पूरे देश में बच्चों के साथ गैंगरेप की घटनाएं बढ़ रही हैं. नपुंसक बनाने का सुझाव बर्बरतापूर्ण लग सकता है लेकिन बर्बर अपराधियों को बर्बर सजाओं से ही रोका जा सकता है. सजा ऐसी हो कि अपराधी अपराध करते हुए डरे.’ इससे पहले दिल्ली में एडिशनल सेशन जज कुमारी कामिनी लाउ भी ऐसा ही सुझाव दे चुकी हैं. 20 वर्ष पहले एडिशनल सेशन जज एसएम अग्रवाल ने एक मामले में दोषी को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि वह अपनी इच्छा से नपुंसक बनाए जाने की हामी भरे तो उसकी सजा कम की जा सकती है. एडिशनल सेशन जज के इस फैसले को पूरी तरह गैरकानूनी कहते हुए उच्च न्यायालय ने पलट दिया.
भारत में भले ही इस तरह के प्रस्ताव से बहुत से लोग चौंके हों, लेकिन जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, पौलेंड और अमेरिका के कुछ देशों सहित रूस में भी बच्चों के यौन अपराधियों को सजा देने के लिए रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाए जाने के तरीके को अपनाया जाता है. हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन जैसी संस्थाएं इस सजा के खिलाफ हैं और इसे अप्राकृतिक और अमानवीय मानती हैं. दूसरी ओर एक पहलू ये भी है कि यदि इस तरह सर्जरी द्वारा नपुंसक बनाए जाने के बावजूद अपराधी की बुनियादी मानसिकता में बदलाव नहीं आता है तो अपराध तब भी जारी रह सकता है.
मनोविशेषज्ञ डॉ. अरुणा ब्रूटा का कहना है, ‘नपुंसक बनाए जाने की सजा इस तरह के अपराधों को रोक पाने में कितनी कारगर हो पाती है, इस पर अभी एक संजीदा अध्ययन की जरूरत है. प्रतिक्रिया स्वरूप भावुक होकर सोचने से काम नहीं चलेगा. असल में ये ‘तेजी से बढ़ते मामले’ नहीं बल्कि ‘तेजी से सामने आते मामले’ हैं जो अब मीडिया की सक्रियता से चर्चा में आ रहे हैं. मीडिया की सक्रियता से जागरूकता आ रही है और शिकार बच्चों के अभिभावकों और खुद बच्चों में भी हौसला बढ़ रहा है और वे शिकायत या कम से कम विरोध करने के लिए ही सही, सामने तो आ रहे हैं.
मासूमों से बलात्कार की घटनाओं के बाद अक्सर समाज के एक तबके की ओर से आवाज उठती है, ‘सऊदी अरब जैसा सख्त कानून लाओ! काट डालो अपराधियों को!’ लेकिन इस तरह के कदमों से भविष्य में होने वाले बलात्कार शायद ही रुक पाएं. नेहा के दादा और मां का मानना है कि एक समाज के बतौर हम असफल हो चुके हैं. वे हमारे लिए एक सवाल छोड़ देते हैं, ‘ये समाज चरमरा गया है, सब खत्म हो गया है. कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं.’
(निकिता लांबा और रजनी के सहयोग से)