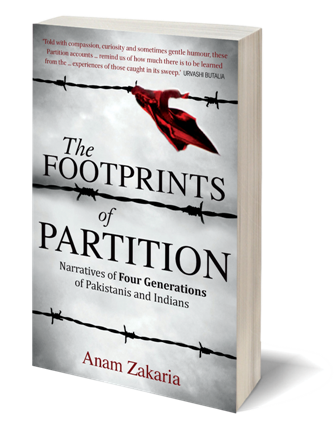रमाशंकर आर्य पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. वे दलित मसलों के जानकार हैं. बिहार के चुनाव परिणाम से खुश दिखते हैं. उनकी खुशी का राज भाजपा की हार में छिपा है. कहते हैं, ‘चलिए यह अच्छा हुआ कि रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी की हार हुई. यह उनके लिए जरूरी था. इस चुनाव परिणाम ने हम सबको खुशी तो दी है. इसकी वजह भी है. लालू प्रसाद दलितों को वोट दिलवाने की स्थिति में लाए, वरना बिहार में दलित वोट के अधिकार से ही वंचित रहते थे. उनके बाद नीतीश ने दलितों को नई शक्ति दी. आज पंचायत और निकाय में 16 प्रतिशत दलित हैं तो यह नीतीश कुमार की ही देन है. अब मंत्रिमंडल में भी करीब 18 प्रतिशत दलितों को जगह मिल गई है.’
हालांकि प्रो. आर्य समेत बिहार से ताल्लुक रखने वाले दूसरे दलित चिंतकों को एक विश्वसनीय दलित नेता की कमी भी खलती है. उनका कहना है कि बिहार में कोई दलित नेता स्वतंत्र रूप से, विश्वसनीयता के साथ, दलितों के बीच में अपनी साख बनाते हुए क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा. प्रो. आर्य कहते हैं, ‘एक सर्वमान्य और बड़ी सोच वाले दलित नेता का उभार नहीं हो पाना चिंता का विषय है. इस पर चर्चा के लिए जल्द ही पटना में दलित रिसर्च स्कॉलरों का जमावड़ा होने वाला है.’ मंडल के 25 साल गुजर जाने और कथित तौर पर मंडल पार्ट टू की शुरुआत होने के बाद भी अपनी जमात से एक मजबूत व विश्वसनीय नेतृत्व को विकसित नहीं कर पाने की दलितों की चिंता राजनीतिक तौर पर वाजिब भी है. साथ ही पड़ोस के उत्तर प्रदेश की तरह पिछड़ों के राज से अलग दलित राज की संभावना न बन पाने की कसमसाहट भी कइयों में है.
दो दलित दिग्गजों की चिंता
ऐसा नहीं है कि इस बार के बिहार चुनाव परिणाम को लेकर दलित राजनीति या दलित वोट बैंक के नजरिये से चिंता में कोई एक नेता या राजनीतिक खेमा है. सभी खेमों में एक जैसी बेचैनी है. हालांकि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव इससे बाहर हैं. कांग्रेस इसलिए बेचैन नहीं है, क्योंकि इस बार के बिहार चुनाव में उसके पास खोने को कुछ नहीं था और जो पाने को था, उसे उससे बहुत ज्यादा हासिल हो गया. लालू प्रसाद के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए नहीं हैं, क्योंकि वे फिर से अपने बिखरते वोटों को सहेजने में सफल हो गए हैं. साथ ही सही समय पर अपनी सत्ता और राजनीति भी अपने उत्तराधिकारियों को सौंप चुके हैं. वह बहुत चतुराई से नीतीश कुमार की बिछाई बिसात अतिपिछड़ा, महादलित, पसमांदा आदि को भी खत्म करने की राह पर बढ़ चुके हैं.
दलित चिंतकों को एक विश्वसनीय दलित नेता की कमी भी खलती है. उनका कहना है कि बिहार में कोई दलित नेता अपनी साख बनाते हुए क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा
दलित वोटों को लेकर सबसे बड़ी चिंता में रामविलास पासवान हैं. उनका एक मशहूर जुमला रहा है. ‘हम हालात बदलने पर किसी के साथ नहीं जाते बल्कि हम जिधर जाते हैं, उधर अच्छे दिन आ जाते हैं, हालात बदल जाते हैं.’ यह जुमला इस बार कारगर तो नहीं ही हुआ साथ ही उनकी पूरी राजनीति का मिथ भी इस बार करवट लेते दिखा. उनकी पार्टी को 4.8 प्रतिशत वोट और दो सीटें मिलीं. उनके तमाम रिश्तेदार हार गए. पहली बार ऐसा हुआ जब उन्हें अपनी जाति का भी वोट नहीं मिला और न ही ये वोट वे राजग को ट्रांसफर करवा पाए. रामविलास पासवान को पार्टी बनाने के बाद 29 सीटें मिली थीं, फिर धीरे-धीरे वह इकलौते विधायक वाली राष्ट्रीय पार्टी के नेता भर बनकर रह गए. पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ होने के चलते उन्हें संजीवनी मिल गई. अब सवाल ये है कि जिस भाजपा के साथ वे पुनर्जीवन पाकर बड़ा उभार पाने में सफल हुए थे, उसी के साथ रहने पर पहली बार उनकी जाति के वोटरों ने भी उनका साथ क्यों छोड़ दिया? अपने गढ़ और सुरक्षित सीटों पर दलितों ने भी उन्हें क्यों नकार दिया? उनका वोट बैंक पहली बार क्यों खिसक गया?
बिहार की राजनीति में तेजी से उभरकर दलित राजनीति की आकांक्षा और उम्मीदों के स्वर बने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं. इमामगंज सीट पर दिग्गज दलित नेता व राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश कुमार के प्रिय उदयनारायण चौधरी को हराने का सुख तो उन्हें है लेकिन अपनी अलग पार्टी बनाने, भाजपा से सहयोग लेने के बावजूद इकलौती सीट पर जीत दर्ज करा पाने की कसक उनके मन में है. उन्हें 2.3 प्रतिशत वोट और एक सीट मिली. सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ?
रामविलास पासवान की बात करें तो जानकार बताते हैं कि उन्होंने परिवारवाद को इतनी तरजीह दी है कि उनकी जाति के लोग ही उनसे बिदक रहे हैं. यह शायद पासवान की पार्टी के हार का कारण बताने में जल्दबाजी जैसा है, क्योंकि उन्होंने पहली बार परिवारवाद नहीं किया. वे इसके लिए जाने जाते रहे हैं और अपने दोनों भाइयों, बेटों को पहले ही राजनीति में सेट कर चुके हैं. इस बार वे अपने दामाद और भतीजे को लेकर आए थे, जो नहीं चल सके. कुछ जानकार बताते हैं कि रामविलास पासवान को पिछली बार तक ऊर्जा इसलिए मिली थी क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें खत्म हो जाने के बाद फिर से बढ़ जाने का एक मौका उपलब्ध करा दिया था. नीतीश कुमार ने 18 जातियों को लेकर जब महादलित नाम से दलितों की एक अलग श्रेणी बनाई थी तो उसमें पासवान को छोड़ दिया गया था. तब रामविलास पासवान के समर्थकों ने पासवानों के बीच यह बात फैला दी थी कि पासवानों को इसलिए नीतीश कुमार ने अलग-थलग छोड़ दिया है, क्योंकि वे रामविलास पासवान को वोट देते हैं. पूरे पासवान रामविलास के पीछे गोलबंद हो गए थे और अगड़ी जातियों के साथ गोलबंदी कर लोजपा के लिए जीत की राह को आसान बना दिया था. लेकिन इस बार ऐसा नहीं था. हो सकता है कि दोनों कारण सही हों. इस बार पासवान ने परिवारवाद को लेकर थोड़ा अलग किस्म का वातावरण बनाया भी था. बोचहा जैसी सीट से पहले उन्होंने एक महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया. फिर अपने नाराज दामाद अनिल साधु को मनाने के लिए महिला प्रत्याशी को हटाकर दामाद को मैदान में उतार दिया था. हालांकि जीत उसी महिला प्रत्याशी की हुई. हो सकता है कि महादलित का मसला इस बार चुनावी मैदान में नहीं रहने के कारण भी पासवान वोटों का बंटवारा हो गया हो.
पासवान की तरह ही जीतन राम मांझी की हार की कहानी भी अलग है. उन्होंने नीतीश कुमार से अलग होकर नेतृत्व को चुनौती दी. कुछ लोगों ने मांझी को अवसरवादी कहा लेकिन मांझी को साहसी कहने वाले भी बहुतेरे रहे. अब सवाल उठ रहा है कि आगे मांझी क्या करेंगे? क्या वे फिर से दलितों में विश्वास जगा पाएंगे? मांझी को जानने वाले कहते हैं कि वे कभी बहुत मुश्किल और चुनौती की राजनीति नहीं करते. अभी उनके पास तीन विकल्प हैं. पहला, वह अगले चुनाव तक दलितों की राजनीति को मजबूत करें और जो 2.3 प्रतिशत वोट उन्हें मिला है, उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करें. दूसरा, वह राजग के साथ बने रहें. केंद्र में राजग की सरकार है तो उन्हें कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए. तीसरा, वह महागठबंधन में वापसी कर जाएं, क्योंकि महागठबंधन में अभी जो तीन दल हैं, उनके साथ मांझी रह चुके हैं और सबके बुरे दिन के संकेत मिलने पर साथ छोड़ते गए हैं. मांझी इस मसले पर बात नहीं करते हैं. उनके करीबी बताते हैं कि अभी वे चिंतन कर रहे हैं और हार की समीक्षा के बाद ही कुछ तय करेंगे.
प्रो. आर्य कहते हैं, ‘मांझीजी को जब सत्ता मिली थी तो पूरे बिहार में दलितों के बीच उम्मीद जगी और अगर वे अलग लड़ते तो बिना संदेह आज बहुत अच्छी स्थिति में होते और पूरे बिहार से दलितों का समर्थन उन्हें मिलता.’ राजनीतिक कार्यकर्ता और बामसेफ से जुड़े मनीष रंजन कहते हैं, ‘मांझी फैक्टर का जो असर बिहार के चुनाव में होना था वह हुआ है. भाजपा की दो भूल, एक तो टिकट वितरण में अगड़ों का वर्चस्व और दूसरा आरक्षण वाला विवादित बयान, अगर नहीं आया होता तो मांझी भाजपा की नैया बहुत मजबूती से पार करवा देते, क्योंकि उनकी बात दलितों तक पहुंच चुकी थी.’ ये बातें सही हैं, लेकिन मांझी के वोट बिखराव और पूरे दलित समुदाय पर पकड़ नहीं बन पाने की एक वजह उनके और पासवान के बीच का टकराव भी रही. पासवान ने मांझी को छोटा नेता कहा तो मांझी ने जवाब में उन्हें परिवार का नेता कहा. दोनों नेताओं की आपसी जंग की वजह से भी दलित वोट एक समूह की तरह नहीं बन सका.
महागठबंधन के नेताओं की चिंता गैरवाजिब नहीं है, क्योंकि चुनाव परिणाम ने ये साफ कर दिया कि भाजपा ने दलितों-अतिपिछड़ों में अपना आधार बढ़ा लिया है
इसके अलावा चुनाव परिणाम ने नीतीश-लालू को भारी जीत दिलाने के बावजूद दलित राजनीति के नजरिये से कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दिया है. यह अलग बात है कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 40 सीटों में से 35 पर महागठबंधन का ही कब्जा हुआ. फिर भी चुनाव परिणाम कुछ अलग संकेत देते हैं. मनीष कहते हैं, ‘भाजपा नेता सुशील मोदी जो लगातार कह रहे थे कि मंडल और कमंडल, दोनों उनके पास हैं, इससे भाजपा ने संकेत दे दिए हैं कि कमंडल के साथ मंडल पर भी उसने डोरे डाले हैं और इस बार किसी कारण गड़बड़ी हो गई लेकिन भविष्य में वह दूसरी राह भी अपना सकती है.’ इन बातों की पड़ताल करें तो यह संकेत मिलते भी हैं.
गणित के संकेत
चुनाव परिणाम ने सिर्फ दलित वोट या राजनीति के नजरिये से पासवान और मांझी को ही चिंतित नहीं किया है बल्कि दूसरे और कई दल भी परेशान हैं. बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार दलित आबादी करीब 16 प्रतिशत है. हालांकि मांझी जैसे नेता इसे 23 प्रतिशत मानते रहे हैं और कई विश्लेषक भी इसे 20 प्रतिशत से कम नहीं मानते. इनका मानना है कि दलित आबादी में एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो इधर से उधर पलायन करता रहता है, इसलिए वह जनगणना में शामिल नहीं हो पाता. यह बात सही भी है. खैर अगर उस पक्ष को छोड़ भी दें तो दलितों की बड़ी आबादी बिहार में है. नीतीश कुमार ने इसी दलित वोट को अपने पाले में और लालू से अलग करने के लिए एक समय में महादलित कार्ड खेला था. उसका लाभ भी उन्हें मिला था. इस बार के चुनाव में भाजपा ने भी दो दिग्गज दलित नेताओं को अपने पाले में इसी वोट को साधने के लिए किया था. हालांकि वह कुछ करिश्मा नहीं कर सके. लेकिन इन सबके बाद भारी जीत हासिल करने वाले नीतीश-लालू की जोड़ी को भी दलित राजनीति के नजरिये से चुनाव परिणाम ने कोई कम चिंतित नहीं किया है. विजयी होने के बावजूद चिंतित होने की वजहें भी ठोस हैं. इस बार के चुनाव में भाजपा को 24 प्रतिशत वोट मिले हैं और अगर उसके सहयोगियों को मिला दें तो राजग को कुल करीब 34.1 प्रतिशत वोट मिले हैं. महागठबंधन के नेताओं की चिंता यह है कि वोटों की प्रतिशतता के बावजूद भाजपा का खेल गड़बड़ा गया या िफर मोहन भागवत के आरक्षण वाले विवादित बयान के बाद दलित और पिछड़े उससे नाराज हो गए. इसके इतर चिंता ये भी है कि वह कौन सा समूह है, जिसने भाजपा के वोट प्रतिशत को इस बार बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर दिया. पिछली बार नीतीश के साथ रहने और उनके जरिये महादलित-अतिपिछड़ों का भी वोट पाने के बावजूद 17-18 प्रतिशत के बीच ही रह गया था. हालांकि एक तर्क यह दिया जा रहा है कि भाजपा अधिक सीटों पर लड़ी इसलिए उसका वोट प्रतिशत ज्यादा है, पर महागठबंधन के नेताओं की यह चिंता गैरवाजिब नहीं है. क्योंकि भाजपा इस बार भले ही पिछड़ गई लेकिन चुनाव परिणाम ने यह साफ कर दिया कि उसने दलितों और अतिपिछड़ों में अपने आधार का विस्तार कर लिया है. यह आनेवाले दिनों में चुनौती की तरह ही होगा.
इस बात की पुष्टि सिर्फ मतदान में मिले कुल प्रतिशत वाले वोट ही नहीं करते बल्कि चुनाव के बाद सीएसडीएस जैसी संस्था ने भी अपनी अध्ययन रिपोर्ट के जरिए यह साफ किया कि इस बार चुनाव परिणाम में अतिपिछड़ों ने 35 प्रतिशत वोट महागठबंधन को किया तो 43 प्रतिशत वोट राजग को. पासवानों में 19 प्रतिशत वोट महागठबंधन को गया तो 54 प्रतिशत राजग को और महादलितों में 25 प्रतिशत वोट महागठबंधन को गया तो 30 प्रतिशत राजग को. राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं, ‘ये आंकड़े भविष्य की राजनीति के संकेत दे रहे हैं. संकेत साफ हैं कि भाजपा ने इस बार अतिपिछड़े और दलितों में सेंधमारी की है क्योंकि उसके सहयोगियों के वोटों को अलग कर दें तो वह अलग 10 प्रतिशत होता है और भाजपा का अपना 24 प्रतिशत है. वोटों के प्रतिशत और सीटों के बीच संख्या के अनुपात में अचानक ही उतार-चढ़ाव होता है. लालू जब अपने सबसे अच्छे दिनों में थे तो 29 प्रतिशत वोट पाकर ही 164 विधायकों के साथ सरकार बना ली थी.
इस बार के चुनाव में भाकपा माले सिर्फ डेढ़ प्रतिशत वोट पाकर ही तीन सीटें अपने पाले में करने में सफल रही है. इस लिहाज से राजग का 34 प्रतिशत वोट और उसमें दलितों व अतिपिछड़े वोटों का भी ठीक ठाक सामंजस्य हो जाना आगे के लिए चुनौती है. यह चुनौती लालू के लिए कम और नीतीश के लिए ज्यादा है. लालू ने अपने पुराने समीकरण का फिर से रिवाइवल कर लिया है लेकिन इस चुनाव में वे सारे कोर वोट बैंक समूह, जिसे नीतीश कुमार ने अपने लिए या अपनी राजनीति के लिए खड़ा किया था, एक हो गए हैं. बिहार के अब सारे दलित महादलित हो चुके हैं. लालू प्रसाद ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि बिहार के सारे दलित अब महादलित की सुविधा लेंगे. सिर्फ दलित-महादलित ही नहीं, अतिपिछड़ा और पिछड़ा मिलकर एक हो गए हैं और राजनीति मंडल की ओर मुखातिब हो गई है. मुसलमानों में नीतीश ने पसमांदा और अशराफ मुसलमानों का बंटवारा किया था, वे दोनों भी एक होकर मुसलमान वोट बैंक जैसे हो गए हैं.’ सवाल यह उठता है कि अगर किसी राजनीतिक कारण से लालू और नीतीश का अलगाव होता है तो क्या अपने बने बनाए सारे वोट बैंक को खत्म कर नीतीश, लालू का मुकाबला कर पाएंगे?
प्रो. आर्य कहते हैं, ‘नीतीश कुमार ने पंचायत चुनाव में दलितों को आरक्षण दिया, उसका असर रहा है और रहेगा. यह सही है लेकिन उसका विस्तारित सवाल यह है कि जब 16 प्रतिशत दलित आज पंचायती व्यवस्था में प्रधान सरपंच, पार्षद आदि बनकर सक्रिय राजनीति में दखल दे चुके हैं तो फिर आने वाले दिनों में वे अपने लिए भी रास्ता तलाशेंगे और वह रास्ता उस ओर जाएगा, जिधर दलित राजनीति की गुंजाइश होगी.’ ये बात भी सही लगती है कि नीतीश कुमार ने दलितों को पंचायत में आरक्षण देकर एक बड़ा काम किया है, जिसका असर रहेगा लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद और इस बार के विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में विधान परिषद चुनाव भी हुआ था. उसमें वोट डालने वाले निर्वाचित निकाय प्रतिनिधि ही थे. अधिकांश दलित और अतिपिछड़े प्रतिनिधियों ने इसमें भी भाजपा का साथ ज्यादा दे दिया था. यानी कुल मिलाकर संकेत यह मिल रहे हैं कि दलित और अतिपिछड़े, जो बिहार की राजनीति में एक समूह की तरह बनाए गए थे, अब भी हिचकोले खा रहे हैं और एक ठोस नेतृत्व की तलाश में कभी भाजपा की ओर तो कभी लालू-नीतीश की ओर तो कभी रामविलास पासवान-जीतन राम मांझी की ओर आ-जा रहे हैं.
‘इस बार के बिहार के चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि जो भी एक ठोस एजेंडे के साथ दलितों को साधकर काम करेगा, वह भविष्य में चैंपियन होगा’
[box]
‘दलित नेता ही दलितों का आत्मबल मारते हैं,
इसलिए कोई विश्वसनीय दलित नेतृत्व उभर नहीं पाया’
इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तीन अशोक की खूब चर्चा हुई. एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनकी जाति का निर्धारण चुनाव के पहले जोर-शोर से हुआ और भाजपा ने उनका स्वरूप बदला. दूसरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी थे. कांग्रेस की जीत चाहे जिन वजहों से हुई, जैसे हुई हो लेकिन अशोक कुमार चौधरी का नाम चमका, अब वे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं. तीसरे अशोक का नाम भी अशोक कुमार चौधरी है. इन्होंने नया इतिहास रचा. अशोक ने मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है. कांटी बिहार में थर्मल पावर प्लांट के लिए ख्यात है. यह विधानसभा क्षेत्र सामान्य श्रेणी का है. अशोक चौधरी, जो दलित जाति से आते हैं, उन्होंने इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया और अजीत कुमार जैसे पुराने नेता को परास्त किया. यहां राजद तीसरे नंबर पर चली गई. अजीत कुमार, जीतन राम मांझी की पार्टी ‘हम’ से उम्मीदवार थे. वे पहले नीतीश कुमार के साथ थे. बाद में मांझी के साथ हो गए थे. कांटी में सामान्य सीट पर एक दलित का जीतना बिहार में यूं ही बड़ी परिघटना के तौर पर माना जा सकता था और उसमें भी निर्दलीय का जीत जाना ऐतिहासिक है. इसके पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास सामान्य सीट से जीतते रहे थे लेकिन अशोक चौधरी का निर्दलीय जीतना एक बड़ी राजनीतिक संभावना की ओर भी संकेत है. कांटी से जीत हासिल करने वाले अशोक चौधरी ने दलित राजनीति पर निराला से बातचीत की
 आपने तो इस लहर में मिथक ही बदल दिया. दलित जाति से होकर सामान्य सीट से लड़ने का साहस जुटाया और निर्दलीय जीत भी गए. ये सब कैसे हुआ?
आपने तो इस लहर में मिथक ही बदल दिया. दलित जाति से होकर सामान्य सीट से लड़ने का साहस जुटाया और निर्दलीय जीत भी गए. ये सब कैसे हुआ?
आप डंड़ेरा जानते हैं. खेत में बांधा जाता है. आरी जैसा. उसका काम होता है कि वह पानी की धार को रोके रहे. पानी इधर से उधर न जाए. मैंने बस एक ही फॉर्मूला रखा था. वह यह कि हमारी जाति या समूह के लोग अगर आजादी के बाद से दूसरों को विजयी बनाते रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बनाएंगे. इसी आधार पर मिथक बदल गया.
जब आप इतने संभावनाशील नेता थे तो आपको टिकट देने के लिए किसी पार्टी ने आपसे या आपने किसी पार्टी से संपर्क क्यों नहीं किया?
कौन देता टिकट और क्यों देता. चुनाव के किसी समीकरण में मैं फिट नहीं बैठ रहा था. आजादी के बाद से इस सीट पर एक जाति समूह का वर्चस्व था. लालू प्रसाद यादव ने इस पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को खड़ा कर उस वर्चस्व को तोड़ा लेकिन यहां दलितों को लेकर कभी किसी ने संभावना की तलाश ही नहीं की. फिर भला हमें क्यों कोई दल टिकट देता. तब मैंने तय किया कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और अपने लोगों के साथ ही दूसरे समूह के लोगों से अपने पक्ष में अपील करूंगा. इसका असर भी हुआ. इस फॉर्मूले ने डंड़ेरा की तरह काम किया. दलित एकतरफ एकजुट हो गए और आप यकीन कीजिए कि यह समूह जहां, जिसके पक्ष में हो जाए, वहां किसी लहर और प्रचार का असर नहीं होना है. आजादी के बाद से पहली बार इस सीट को आजादी मिली और समीकरण बदल गया.
रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दो दलित नेता भी तो थे भाजपा के साथ. बिहार में दोनों अपने लोगों को क्यों नहीं बांध पाए, जबकि वे तो सामर्थ्यवान नेता भी रहे हैं?
मैं एक बात बताऊं. पूरे बिहार का नहीं जानता लेकिन जितना जानता हूं उसके आधार पर कह सकता हूं कि दलितों या वंचितों के समूह में साहस या प्रतिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन जो लोग उनकी रहनुमाई करते हैं वे उनके नाम पर तो सामने आते हैं लेकिन बाद में अपने परिवार और परिजनों के अलावा ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते, इसलिए बड़े से बड़े नाम के नाम पर भी दलित समूह एकजुट नहीं रह पाता, बिखर जाता है.
दलितों की आबादी इतनी बड़ी है, फिर भी एक मुकम्मल दलित नेतृत्व न उभर पाने की राह में आप किस तरह की बाधा देखते हैं? बिहार में दलित राजनीति के सामने चुनौती क्या है?
दलित नेता ही यहां के दलितों का आत्मबल मार देते हैं. और जो बड़े क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल हैं, वे बस किसी एक नेता को आगे बढ़ाकर अपने को दलित हितैषी बताने लगते हैं. ऐसे में दलितों में से एक नेता का उभार हो जाता है और बाकी 99 फीसदी दलित परिवार किस हाल में रह रहे हैं, उसकी खबर नहीं ली जाती. और जो एक नेता बनाया जाता है, वह भी 99 फीसदी की रोजी-रोटी की चिंता की बजाय अपने कुनबे के विस्तार में लग जाता है. यही बिहार में होता रहा है और उसका असर यह रहा है कि बिहार में दलित वोट बैंक या तो किसी दल के राजनीतिक हित साधने का औजार है या फिर किसी नेता के कुनबे के विस्तार का माध्यम. और दलित नेता इस्तेमाल होते रहे हैं.
तो क्या आपसे उम्मीद की जाए कि आप जब इस लहर में एक अलग पहचान के साथ उभरे हैं तो आप पूरे बिहार में अलग किस्म की दलित राजनीति के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे?
अभी पूरे बिहार का क्या कहूं. मैं तो कांटी से जीता हूं. कांटी की ही जनता ने इतना भरोसा कर आजादी के बाद से नया इतिहास रचा है. पुराने मिथक को तोड़ा है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि कांटी को ही अपना पूरा समय दूं. कांटी में बदलाव की बुनियाद रखू. अभी तो इतना ही सोचता हूं.
[/box]
बिहार के समाजवादी नेता धनिकलाल मंडल के बेटे भरत मंडल कहते हैं, ‘इस बार के चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि जो भी एक ठोस एजेंडे के साथ दलितों को साधकर काम करेगा, वह भविष्य में चैंपियन होगा. दलित वोट बैंक छटपटाहट में है, बिखराव की स्थिति में है, उसे सहेजने वाला एक नेता चाहिए.’ लेकिन क्या वाकई बिहार की राजनीति में कोई ऐसा दलित नेता गोलबंदी करने की स्थिति में आता हुआ दिखता है. अब तक का इतिहास बताता है कि बिहार में जो भी दलित नेता रहे हैं, चाहे वे जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री, रमई राम, रामसुंदर दास, रामविलास पासवान या जीतन राम मांझी रहे हों, सब एक बड़े नेता के तौर पर तो दिखे लेकिन कोई भी अपने ही समुदाय को एक समूह की तरह विकसित नहीं कर सका. तब सवाल यह उठता है कि बिहार में दलित राजनीति अब क्या करवट लेगी? और दूसरा सवाल उठता है कि आखिर क्यों बिहार में दलित राजनीति अब भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पिछड़ी राजनीति से अलग पहचान बनाने की स्थिति में नहीं आ सकी, अपना एक मजबूत नेता नहीं बना सकी, एक मजबूत नेतृत्व को जन्म नहीं दे सकी, जबकि उनकी आबादी भी कम नहीं है.
बाधाएं और संभावनाएं
आखिर क्यों बिहार की दलित राजनीति में तनी छटपटाहट दिखने के बावजूद उत्तर प्रदेश की तरह दलित अपना मजबूत नेतृत्व नहीं बना पा रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं, ‘किसी भी समूह से सत्ता में स्वतंत्र व मजबूत नेतृत्व के उभार के लिए आबादी में बड़े स्तर पर मध्यवर्ग का होना जरूरी होता है. बिहार में दलितों की आबादी तो बड़ी है लेकिन इसमें मध्यवर्ग की कमी है, इसलिए अभी यह संभव नहीं दिखता.’ प्रो. आर्य इस बारे में कहते हैं, ‘1998 में दलित हिस्ट्री कांग्रेस हुआ था. उसमें कांशीराम शामिल हुए थे. मैं भी गया था. कांशीराम जी ने तब कहा था, अभी से ही लगना होगा. कम से कम 40-50 अपने लोग संसद में होने चाहिए. तब बाबा साहब की जयंती मनाने का मतलब होगा. उसके बाद वे इस काम में लग गए थे.’ प्रो. आर्य कहते हैं, ‘इतनी बड़ी योजना और फिर धैर्यपूर्वक उस योजना पर काम करने वाला बिहार में कोई दिखता ही नहीं, तो यह संभव होगा, ऐसा नहीं लगता.’
राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार मणि कहते हैं, ‘इसके पीछे कई कारण हैं कि बिहार की दलित राजनीति उत्तर प्रदेश की तरह अभी आगे नहीं बढ़ सकी है. इसके लिए आपको अभी का समय नहीं देखना होगा. पिछड़ों की गोलबंदी 30 के दशक में त्रिवेणी संघ के जरिए ही शुरू हो गई थी. आजादी के बाद कांग्रेस का राज आया. दलित कांग्रेस के साथ चले गए. बीच में लोहिया ने ‘पिछड़ा पावे सौ में साठ’ का नारा चलाया. पिछड़े लोहिया के इस नारे के साथ हो गए, दलित समाजवादी आंदोलन से नहीं जुड़े. वे कांग्रेस के साथ ही रह गए. लालू का उभार हुआ तब दलितों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा. इसलिए दलितों में बेचैनी और अपना एक अलग ठांव तलाशने के बावजूद वह नेतृत्व नहीं मिल पा रहा, जिस तरह से पिछड़ों को बिहार में मिल रहा है. लेकिन इस बार के चुनाव ने ये संकेत दिए हैं कि तमाम लहर वगैरह के बावजूद दलितों ने भाजपा का साथ दिया. यह एक किस्म की बेचैनी ही है कि इतने आंधी-तूफान के बावजूद दलित वोट इधर-उधर हुआ. पासवान-मांझी को मिलाकर तकरीबन 7.5 प्रतिशत वोट मिले हैं. ये कम नहीं है. बस, देखना यह होगा कि मांझी कहीं फिर से लालू-नीतीश के साथ न चले जाएं. अगर ऐसा नहीं होता है और मांझी कोई दीर्घकालिक राजनीति का रास्ता अपनाते हैं तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलेगा.’
ये बात सही भी लगती है. ऐसे कई कारण रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार में दलित राजनीति स्वतंत्र रूप से परवान नहीं चढ़ सकी. उत्तर प्रदेश में इसकी बढ़त का एक दूसरा कारण यह भी रहा कि वहां वाम दलों का कभी प्रभाव नहीं रहा जबकि बिहार में वाम दल शुरू से ही सक्रिय रहे और दलितों के बीच उनकी पकड़ भी रही. यह भी सही है कि लालू पहले भी चाहते थे, अब भी चाहेंगे कि मांझी उनके खेमे में आएं. लालू को भी पता है कि इस बार के चुनाव में दलितों ने या अतिपिछड़ों ने गोलबंदी कर एक तरीके से उस पुराने ऋण को भी चुकाया है, जो लालू का एक तरीके से बकाया-सा भी था. लेकिन दलितों या अतिपिछड़ों ने तब यह ऋण चुकाया है, जब लालू प्रसाद सबसे मुश्किल दिनों में राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे. बिहार की राजनीति अनिश्चित है. ऐसे में यहां की दलित राजनीति किसी करवट बैठेगी और क्या इस समुदाय से कोई बड़ा नेता उभरेगा? इसके जवाब में अब भी कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है.
‘जय हो फिल्म के बाद कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं मिल रहा था. अगर अच्छा प्रस्ताव मिलता तो हेट स्टोरी-3 जैसी इरोटिक थ्रिलर नहीं करती’