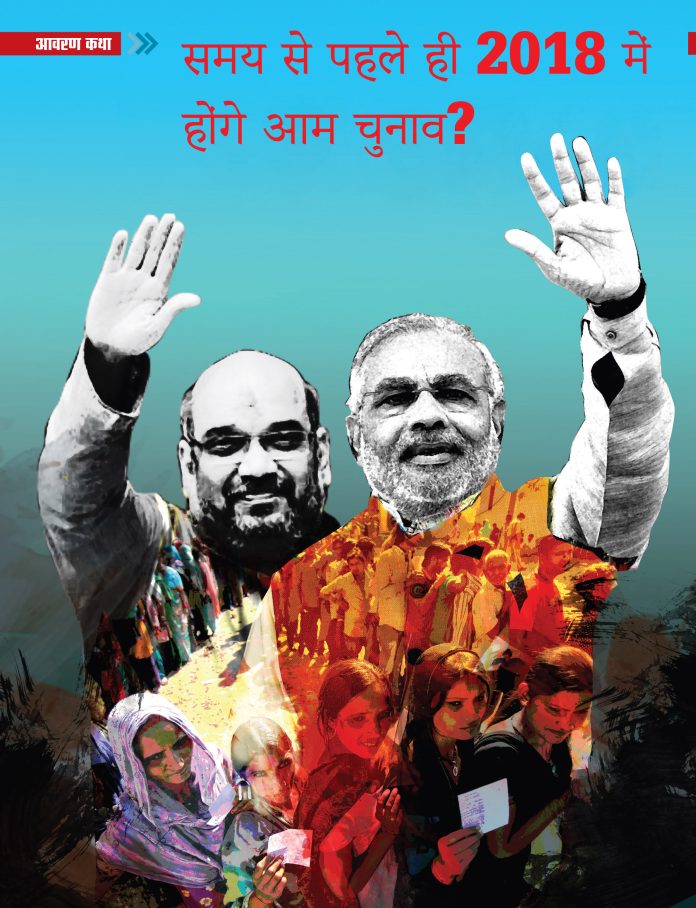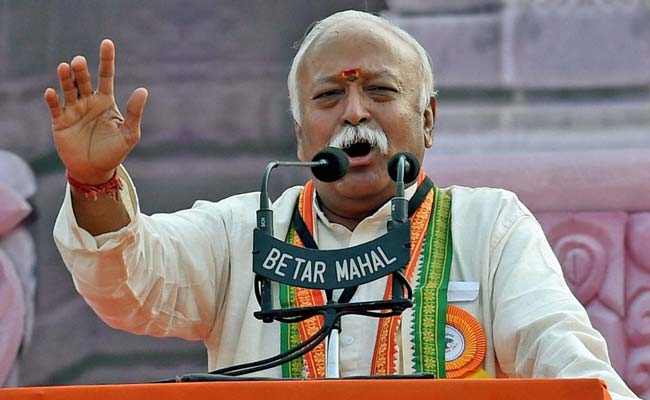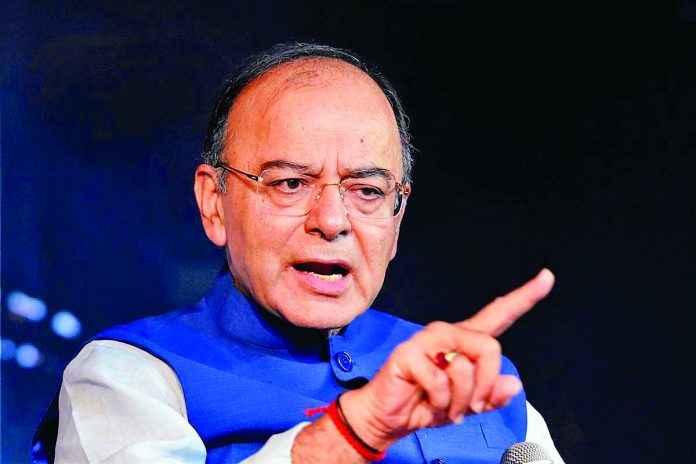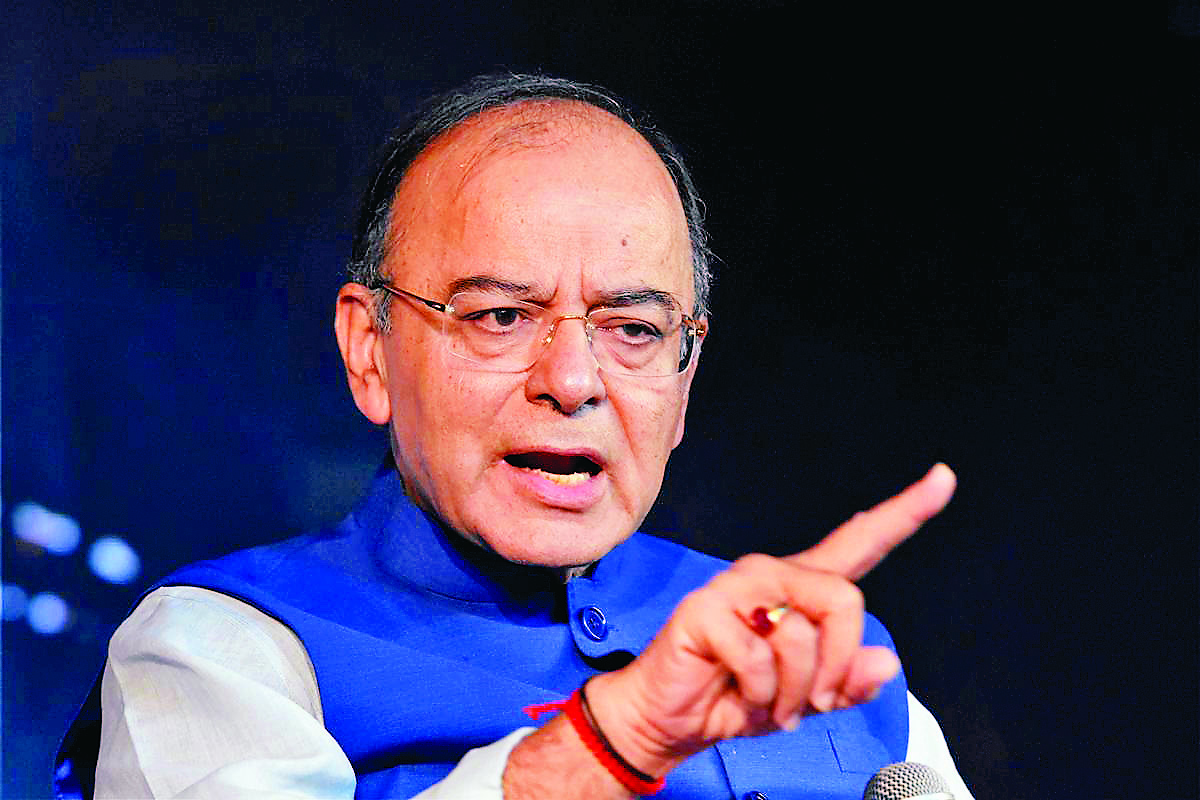प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह इस हुनर में माहिर हैं कि हमेशा वे विपक्ष को नींद से जगाते रहे हैं। ऐसी संभावना है कि लोकसभा चुनाव जो 2019 मेेेें होने हैं उन्हें 2018 समाप्त होने के पहले ही कराने का संदेश ये दोनों महारथी दे दें। इसी की गहरी छानबीन कर रहे हंै चरणजीत आहुजा और रिद्धिमा मल्होत्रा।
सत्ता के गलियारों में यह फुसफुसाहट अब तेज हो गई है कि भाजपा लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा ले। पार्टी को फिर विधानसभा चुनावों में और ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। पार्टी के नेताओं की राय है कि यदि विधानसभा और आम सभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो राज्य के मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों का दबाव पड़ेगा और पार्टी चुनावों में अच्छे नतीजे ला सकेगी। लोगों पर यह नज़रिया प्रभावी पड़ रहा है कि इससे एंटी-इन्कंबैंसी पर भी असर पड़ेगा जो कई राज्यों में दिख भी रहा है। भाजपा के लिए यह सबसे अच्छी बात है कि विपक्ष के पास कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है जिसके चलते यह भाजपा पर हावी हो सके। मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभाओं में चुनाव नवंबर-दिसंबर 2018 में होने भी हैं और ये राज्य आम चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश कर सकते हैं। यदि आम चुनाव समय से पूर्व यानी 2018 में करने पर सहमति बन जाती है।
मुख्यमंत्री मिले मोदी और शाह से
भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा शासित राज्यों के तेरह मुख्यमंत्री और छह उप-मुख्यमंत्रियों ने अभी हाल में मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बैठक में यह बात ज़रूर निर्विवाद तौर पर साफ हुई कि मोदी के मुकाबले में पार्टी में कोई नेता नहीं है और उनकी लोकप्रियता बदस्तूर कायम है। दूसरा नज़रिया जो इस बैठक में साफ हुआ कि पार्टी को निर्धारित तारीख तक यानी 2019 तक दस-बारह महीनों तक बने रहने का मोह त्यागना चाहिए और पांच साल के नए दौर को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी संदर्भ में यह भी देखा जा रहा है कि अमित शाह पार्टी को ज़मीनी स्तर पर जोडऩे में जुटे दिखाई दे रहे हैं। इससे भी यह साफ होता है कि आम चुनाव जल्दी ही होंगे।
आयकर शून्य
राजनीतिक टिप्पणीकार यह मानते है कि उत्तरप्रदेश में भाजपा के जीतने की वजह विमुद्रीकरण है। इस नीति को पार्टी ने बड़ी खूबी से पूरे राज्य में फैलाया जिसके चलते राज्य में पार्टी को जीत हासिल हुई। पार्टी को अस्सी में से 73 सीटें मिली। इस बार पार्टी को उम्मीद है कि विपक्ष को और ज़्यादा झटका लगेगा। सूत्रों का मानना है कि भाजपा इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है कि आयकर खत्म कर दिया जाए। उसकी बजाए बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स (बीटीटी) लगाया जाए।
भले ही लोगों को यह आश्चर्यजनक लगे लेकिन यह सच है कि ऐसे कई देश इस दुनिया में हैं जहां आयकर नहीं लगता। इन देशों में हैं युनाइटेड अरब अमीरात, कतर, ओमान, कुवैत, के मैन द्वीप समूह, बाहरेन, बरमुडा, बहामा, ब्रुनेई दारस्सलम आदि। यही नहीं, इन देशों की संख्या 114 की है। इनमें से कई देशों में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी है। इन देशों में कई ने तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके सरकारी खर्च अदा करने की व्यवस्था की है।
आयकर का शून्य होना भले ही चमत्कृत करे लेकिन इससे भाजपा को चुनाव में गजब की कामयाबी मिल सकती है। यह वैसी ही कामयाबी है जो उत्तरप्रदेश में पार्टी को विमुद्रीकरण के चलते हासिल हुई। इसकी बजाए सरकार खपत कर या खर्चकर लगा सकती है। यह भी आयकर जैसा ही होगा। अंतर सिर्फ यही होगा कि टैक्स तो खर्च पर लगता है आमदनी पर नहीं। इस पर नज़रिया यह है कि इससे खपत बढ़ती है।
हमारे देश में आयकर वह टैक्स है जो खर्च पर लगता है आमदनी पर नहीं। इसका नजरिया है कि इससे खपत को बढ़ावा मिलता है। फिर यह मध्यम वर्ग के वेतन पर लगता है। गरीब लोग तो आय कर देते ही नहीं। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि महज 42,800 लोगों ने ही अपनी सालाना आमदनी यानी रुपए एक करोड़ मात्र से ज़्यादा मानी। यह बात इसलिए अचंभे में डालती है कि देश की कुल आबादी तो 120 करोड़ लोगों की है लेकिन आयकर देने वालों की संख्या बहुत कम है। इसी कारण देश की अफसरशाही और पार्टी के नेताओं को यह एक मजबूत मामला बनता नज़र आ रहा है जिससे आयकर से निजात देशवासियों को दिलाई जा सकती है। आखिर कुछ ही लोगों को आयकर देने के लिए क्यों दबाव डाला जाए? भाजपा के नीति-निर्माताओं का भी यही मानना है और पार्टी इस प्रस्ताव पर गंभीरता से सोच रही है।
यूबीआई से आएगा बदलाव
चुनाव घोषित होने के पहले ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) वास्तविकता हो सकती है। इसकी वजह यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में यह नहीं माना जा सकता कि एक व्यक्ति अपनी निजी ज़रूरतों को इसलिए पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। इस योजना के तहत गरीबी और असमानता पर हल्ला बोला जाएगा। एक बेसिक आय जो गरीबी से जूझने के लिए पर्याप्त हो वह समय पर गरीब के खाते में भेजी जाती रहे। इससे एक बारगी 37 करोड़ पचास लाख गरीब भारतीयों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया जा सकेगा। यूबीआई से होने वाले लाभ अनेक हैं और यह भ्रष्टाचार से निपटने की सरकारी घोषणा से मेल भी खाते हैं और न्यूनतम सरकार और सबसे ज़्यादा सुशासन के उपयुक्त भी हैं। इस मुद्दे पर काफी बहस- मुबाहिसा होता रहा है और किस तरह सरकार इस योजना पर पैसा लगा सकती है।
गरीब के लिए ढेरों योजनाएं
मध्यम वर्ग, किसानों, गरीबों और समाज के बेहद गरीब लोगों के लिए भाजपा नई योजनाएं ला रही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) 27 वस्तुओं पर जीएसटी करों में कटौती इसलिए भी की गई जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को खामोश किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को मसविदा भेजने को कह रखा है जिससे गरीबों के लिए समाज-कल्याण की योजनाएं अमल में लाई जा सकें। तकरीबन रुपए सोलह हज़ार करोड़ की ‘सौभाग्यÓ योजना पूरे देश के लोगों के लिए है जो इस योजना के तहत सब को मिलेगी। इसके तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री के तहत ‘सहज बिजली- हर घर योजनाÓ में देश के हर गरीब घर को बिजली का एक कनेक्शन मिलेगा। इस कनेक्शन के लिए गरीब से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर को की थी। उन्होंने कहा कि सरकार रुपए 16हजार करोड़ मात्र के खर्च से देश के चार करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन देकर उजाला करेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख जताया कि ‘इन घरों में बिजली आज भी नहीं है। इन्होंने बिजली का जलता हुआ बल्ब तक नहीं देखा है। मशहूर वैज्ञानिक टॉमस अल्वा एडीसन ने बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने ने कहा था,’ हम बिजली इतनी सस्ती बनाएंगे कि सिर्फ रईस ही जलाया करेंगे मोमबत्तियां।Ó प्रधानमंत्री ने तकलीफ के साथ कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई घरों में आज भी लालटेन, ढिबरी और मोमबत्तियां ही जलती दिखती हैं। आप सुविधा की बात छोडि़ए। महिलाओं को आज भी अंधेरे में ही भोजन बनाना पड़ता है और वे कोशिश करती हैं कि सूरज डूबने के पहले ही वे रसोई का काम पूरा कर लें। प्रधानमंत्री मोदी दीन दयाल ऊर्जा भवन का उद्घाटन करते हुए यह कह रहे थे। यह नया हरित भवन है जिसे सार्वजनिक तेल कंपनी ओएनजीसी ने देश की राजधानी में बनाया है।
कुछ ही लोगों ने यह सोचा होगा कि सरकार तीस करोड़ गरीब लोगों को बैंक खाते प्रदान करेगी। नब्बे पैसे प्रतिदिन के हिसाब से पंद्रह करोड़ लोगों का बीमा कराएगी। स्टेंट ओर नी-रिप्लेसमंट की कीमतें कम करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘गरीबों का सपना, सरकार का अपना सपना है।Ó क्या कभी किसी ने सोचा था कि सरकार रसोईघर में धुंए-धक्कड़ में खाना पका रही महिला को उससे आज़ादी देगी। क्या वे सोच सकते हैं कि सरकार उन लोगों को एअरोप्लेन(हवाई जहाज) में चढऩे की सुविधा देगी जो हवाई चप्पल पहनते हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि गरीब रोज-ब-रोज जो समस्याएं झेलते हैं उन्हें कम करने में पूरा सहयोग करे।
प्रधानमंत्री की बातों पर सहमति जताते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सरकार के प्रयास से उन्हें भी मदद मिल सकी जिन्हें मिलती नहीं थी। पौने आठ करोड़ व्यवसाइयों को 3.17 लाख करोड़ के बंैक कजऱ् दिए गए। इनमें 70 फीसद महिलाओं को लाभ मिला। मुद्रा योजना के तहत रुपए 50 हजार मात्र तक का कजऱ् ‘शिशु Ó योजना के तहत दिया जाता है। इसी तरह रुपए 50 हजार मात्र से रुपए पांच लाख तक की राशि ‘किशोरÓ को और पांच लाख से दस लाख तक की राशि ‘तरूणÓ को दी जाती है। बैंकों ने 22 हजार आवेदन पत्रों पर रुपए चार हजार छह सौ निन्यानवे करोड़ रुपए ‘स्टैंड अप इंडियाÓ में दिए हैं
चुनाव आयोग तैयार है
चुनाव आयोग ने पिछले ही सप्ताह कहा था कि यह राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में सितंबर 2018 तक एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने यह बात तब कही जब वे ईआरओ नेट साफ्टवेयर के जारी होने के समारोह में भोपाल गए हुए थे। इस साफ्टवेयर की खूबी है कि मतदाताओं की सूची में से गलतियों और दुहराव को यह फौरन छांट देता है। चुनाव आयोग ने सरकार को यह सूचित किया है कि रुपए 3,400 करोड़ और रुपए 12 हजार करोड़ मात्र की ज़रूरत होगी आवश्यक ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को खरीदने में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने बताया कि दो सरकारी उपक्रमों को संबंधित आदेश दे दिए गए हंै और मशीनों का आना भी शुरू हो गया है। यह उम्मीद है कि सितंबर 2018 तक ये मशीनें आ जाएंगी उसके बाद ही चुनाव आयोग विधानसभाओं और लोकसभाओं में चुनाव करा सकेगा।
एक साथ चुनाव की संभावना
भाजपा जब से तीन साल पहले सत्ता में आई है यह राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं की बात करती रही है। पार्टी का तर्क है कि इससे देश के संसाधनों का विनाश रोका जा सकेगा। साथ ही साथ चुनाव कराने पर पहली बार जोर दिया था पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने। अब वे पार्टी के ‘मार्ग दर्शक मंडलÓ में हैं। नीति आयोग में भी अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संभावना पर जोर दिया था । उन्होंने यह भी कहा था कि 2024 तक देश में राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ होने लगेंगे। यह देश के ‘राष्ट्रीय हितÓ में हैं। इससे देश के संसाधनों का नुकसान थमेगा। इस बात का उपराष्ट्रपति वेंकैयानायडू ने भी समर्थन किया है।
यह सही है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का भीषण खर्च देश पर पड़ेगा। लगभग तमाम पार्टियां चुनाव में जो खर्च करती हैं उसमें काफी कुछ सच्चाई नहीं नज़र आती। उधर सत्ता में रही पार्टियां ऐसे जनोपयोगी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं करती हैं जिससे भावी चुनाव में उनकी विजय तय ही हो। एक बार जब चुनावी आचार संहिता जारी हो जाती है तो तमाम अर्थव्यवस्था ठहर सी जाती है। इतना ही नहीं, चुनाव करने-कराने में बड़ी तादाद में सुरक्षा दस्तों और चुनाव अधिकारियों की ज़रूरत होगी।