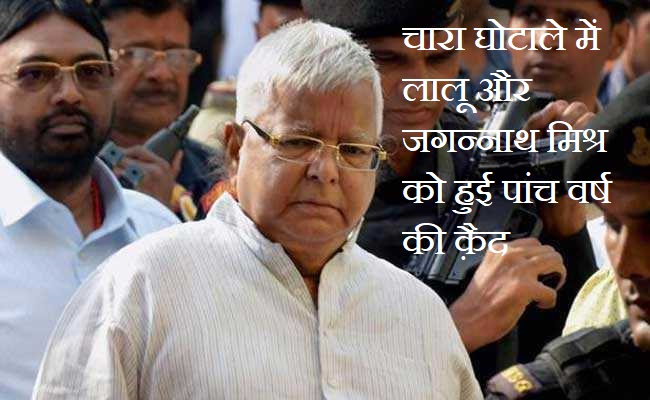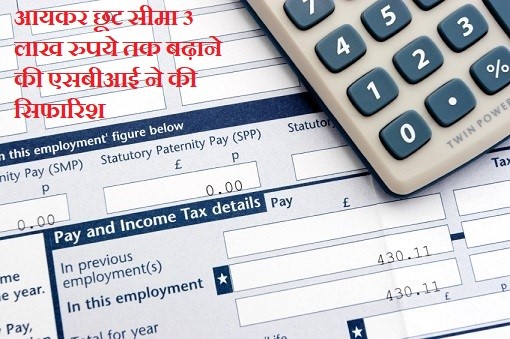वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7-7.5% की वृद्धि हो सकती है।
सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि कृषि सहायता, एयर इंडिया का निजीकरण और बैंक पुनर्पूंजीकरण खत्म करना अगले साल के लिए नीतिगत एजेंडा होगा।
आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ अन्य मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं:
- वित्त वर्ष 2017-18 में 6.75% जीडीपी वृद्धि होने का अनुमान है
- पॉलिसी सतर्कता की ज़रुरत होगी अगर तेल की कीमतों में और बढ़ौतरी होती है या शेयर की कीमतें तेजी से सही होती हैं
- जीएसटी डेटा अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50% वृद्धि दर्शाता है
- राज्यों द्वारा कर संग्रह, स्थानीय सरकारें अन्य संघीय देशों में काफी कम हैं
- विमुद्रीकरण ने वित्तीय बचत को प्रोत्साहित किया है
- दिवालियापन कोड एनपीए संकट को हल करने के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है
- खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 2017-18 में 3.3% था, पिछले 6 वर्षों में सबसे कम
- भारत को अपील और न्यायिक क्षेत्र में लंबितता, देरी और बैकलॉग को संबोधित करने की जरूरत है
- शहरी प्रवास ने कृषि क्षेत्र के नारीकरण की ओर अग्रसर किया
- चालू वित्त वर्ष में किसानों के लिए ब्याज अनुदान के लिए 20,33 9 करोड़ रुपये का मंजूरी
- सुधार की वजह से 2017-18 में सेवा क्षेत्र में एफडीआई 15% बढ़ी है
- वित्तीय संतुलन, कम संतुलन जाल से बचने में मदद करने के लिए जवाबदेही
- वैश्विक व्यापार में संभावित सुधार से भारत को मज़बूती मिल सकती है
- श्रम कानूनों के बेहतर प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए
- स्वच्छ भारत पहल की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में 2014 में 39% से बढ़कर जनवरी 2018 में 76% की वृद्धि हुई
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे की प्राथमिकता
- केंद्र, राज्यों को गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने चाहिए
- लिंग मुद्दों को उजागर करने के लिए गुलाबी रंग में 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया