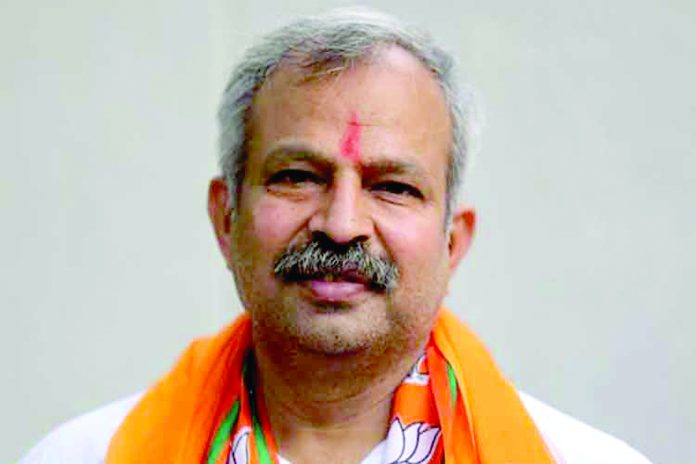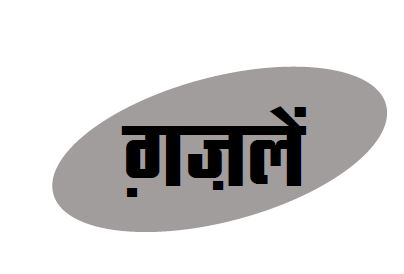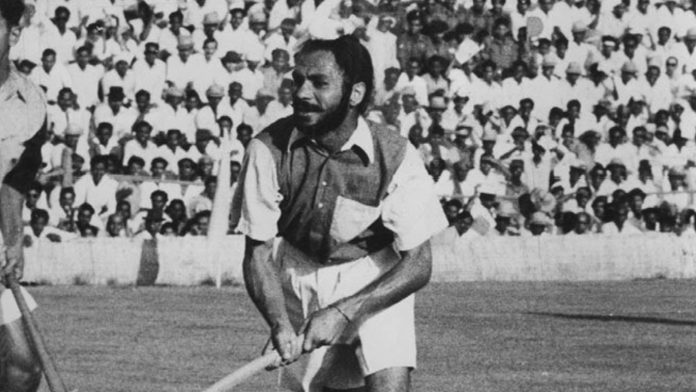1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तब यहाँ आज के आधुनिक युग की कल्पना भी नहीं की गयी थी। हाँ, कुछेक आधुनिक बदलाव की हवा ज़रूर चल रही थी। पर भारत की अधिकतर अर्थ-व्यवस्था बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, रब्बा और पालकी पर ही सवार थी। हालाँकि इन दिनों तक अनेक रईस घरानों की शान कार पर सवार होकर अलग दिखती थी, रेलगाड़ी भी लोगों के लिए तेज़ गति से चलने वाली एक अजूबा ही थी। लेकिन भारत की अर्थ-व्यवस्था की गाड़ी साइकिल पर सवार होकर ही आगे बढ़ी थी और इसे तब और मज़बूती मिली, जब भारत में साइकिल बनाने का कारखाना खुला।
आज आज़ादी के जब 73 साल पूरे होने को हैं, तब प्रगतिशील आत्मनिर्भर भारत की अर्थ-व्यवस्था का छोटा पहिया बन चुकी इसी साइकिल का एक अध्याय इतिहास का हिस्सा बनने के कगार पर है। यह अध्याय है- एटलस साइकिल का; जिसके सभी प्लांटों का बन्द होना इसकी बानगी है। भारत की एक मज़बूत और विदेशी साइकिल कम्पनियों को भारत में न घुसने देने वाली साइकिल निर्माता कम्पनी एटलस ने विश्व साइकिल दिवस यानी 3 जून, 2020 को साहिबाबाद में अपना अंतिम कारखाना बन्द कर दिया। लगभग 69 साल पहले 1951 हरियाणा के सोनीपत में जब एटलस साइकिल का कारखाना शुरू हुआ था, तब किसी के पास साइकिल होना बड़ी बात होती थी। बचपन में जब हम दादा-दादी, नाना-नानी के िकस्सों में कहीं-कहीं जब साइकिल का ज़िक्र सुनते थे, तो साइकिल किसी हवाई जहाज़ से कम नहीं लगती थी। उन दिनों मन में एक सपना होता था कि हम भी बड़े होकर साइकिल चलाएँगे। किस कम्पनी की? यह दिमाग में आते ही एटलस का नाम अनायास मन-मस्तिष्क पर उभर आता था। लेकिन स्टॉकहोम के नोबेल म्यूजियम की दीवारों पर चमकने वाली एटलस साइकिल अब इतिहास बन चुकी है। करोड़ों भारतीयों के ज़िन्दगी और करियर का अहम हिस्सा रही एटलस साइकिल की अहमियत वही लोग बता सकते हैं, जिनके क्षेत्र में आज भी साइकिल ही सफर का सबसे बेहतरीन संसाधन है। म्यूजियम क्यूरेटर की दीवार पर टंगी एक काले रंग की साइकिल आज भी लोग बड़े गौर से देखते हैं। यह साइकिल एटलस कम्पनी की ही है और भारत के जाने-माने अर्थशास्त्री तथा सन् 1998 में नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेन की है। दरअसल इस साइकिल को अमत्र्य सेन के नोबेल पुरस्कार की अहम साथी कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में इसी साइकिल पर सवार होकर उन्होंने काफी समय तक गरीबी, असमानता और पिछड़ेपन पर अध्ययन किया। ऐसी ही कितनी सफलता की कहानियाँ हैं, जिनका सफर साइकिल से ही तय हुआ है।
क्यों बन्द हुआ साहिबाबाद कारखाना?
एटलस साइकिल के साहिबाबाद स्थित तीसरे और आिखरी कारखाने पर जब ताला लगा, तो पूरे देश में इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ होने लगीं। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान देने की ज़हमत नहीं उठायी। वह भी तब, जब उद्योगों को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ के आॢथक पैकेज की घोषणा सरकार कर चुकी है। यह बात यहाँ इसलिए भी कहना ज़रूरी है। क्योंकि एटलस कम्पनी के मालिक कम्पनी के आॢथक तंगी से गुज़रने का हवाला दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा कारखाने के गेट पर एक नोटिस भी लगाया है, जिस पर लिखा गया है- ‘हमें अपने हर दिन के संचालन के लिए फंड जुटाने में परेशानी हो रही है। हम कच्चा माल खरीदने में भी असमर्थ हैं। मौज़ूदा संकट में प्रबन्धन फैक्ट्री चलाने की स्थिति में नहीं है।’
बजट आने पर होगा उत्पादन
एटलस के साहिबाबाद कारखाने के बन्द होने से हुए हंगामे के बीच कम्पनी की प्रबन्ध समिति ने इसे दोबारा शुरू करने की बात कहनी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में श्रम विभाग के उपायुक्त राजेश मिश्रा कम्पनी के प्रबन्धकों और श्रमिकों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। इस बैठक में कम्पनी प्रबन्धकों ने आश्वासन दिया कि सोनीपत में बन्द हो चुके एटलस कारखाने की ज़मीन बेचकर धन जुटाने के बाद साहिबाबाद स्थित कारखाने को दोबारा चालू किया जा सकेगा। कब तक एटलस कारखाने की सोनीपत वाली ज़मीन बिकेगी और कब यह कारखाना शुरू होगा? इस बात की पुष्टि तो अभी नहीं की गयी है; लेकिन ज़मीन बेचने की प्रक्रिया जून में ही शुरू की जाने की उम्मीद है। वहीं कम्पनी को श्रमिकों का पूरा वेतन घर बैठे देना पड़ेगा। कब तक? अभी यह भी तय नहीं है। क्योंकि इस सिलसिले में उप आयुक्त के साथ कम्पनी प्रबन्धकों और श्रमिकों की अगली बैठक इसी 23 जून को होगी, जिसमें कई मामलों पर स्पष्टीकरण की उम्मीद है। इस मामले को ज़िला प्रशासन ने भी अपने संज्ञान में लिया है और एडीएम प्रशासन ने कम्पनी की बैलेंस शीट माँगी है। कम्पनी प्रबन्धकों का कहना है कि फिलहाल सिर्फ कारखाने में उत्पादन का काम रोका गया है; उसे बन्द नहीं किया गया है।
कब बिक सकती है ज़मीन?
किसी कम्पनी की ज़मीन बेचने के लिए उस कम्पनी को सभी साझेदारों, निवेशकों और राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से अनुमति की आवश्यकता होती है। एटलस के सीईओ एनपी सिंह ने कहा है कि एटलस कम्पनी का उत्पादन ले-ऑफ प्रक्रिया के तहत को रोका गया है, जो कि सही है। क्योंकि यह आॢथक तंगी की वजह से करना पड़ा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सोनीपत वाली कम्पनी से उनका कोई मतलब नहीं है। वहाँ जो उनकी ज़मीन है, उसे बेचने के लिए एनसीएलटी से अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। इस पर जून में ही स्पष्टीकरण की उम्मीद है। अगर इस ज़मीन को बेचने की एनसीएलटी ने अनुमति दी, तो कम्पनी ऐसा करेगी। बिना अनुमति के कुछ भी नहीं किया जा सकता।
एटलस की कामयाबी का इतिहास
जानकी दास कपूर ने 1951 में एटलस नाम से साइकिल बनाने के एक कारखाने की शुरुआत एक टिन शेड में की थी। यह वह दौर था, जब साइकिल किसी के लिए भी आवाजाही का सुलभ, सस्ता और बेहतरीन माध्यम होती थी। हालाँकि गरीबों की पहुँच से तब साइकिल बहुत दूर हुआ करती थी। फिर भी पहले साल ही इस कारखाने में बनी एटलस की 12,000 साइकिल भारत में बिकी थीं। यही वजह रही कि टिन शेड से शुरू हुआ यह कारखाना एक साल के अंदर ही 25 एकड़ ज़मीन में फैल गया। इसके बाद एटलस साइकिल पर सवार इस कारखाने ने देखते-ही-देखते दुनिया भर में अपना नाम कमा लिया और सन् 1958 में एटलस कम्पनी ने साइकिलों की पहली खेप विदेश को निर्यात की। आज जब यह कम्पनी में सामान्य साइकिल से अत्याधुनिक साइकिलों का निर्माण कर रही थी, तब इसका बन्द होना भारत के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है, क्योंकि यह एक पूर्णतया स्वदेशी कम्पनी है। अगर इसका इतिहास खंगाले, तो एटलस कम्पनी पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन संक्षेप में कुछ बिन्दुओं को देखने पर पता चलता है कि सन् 1978 में एटलस कम्पनी ने भारत की पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की। यही नहीं सन् 1982 में दिल्ली एशियन गेम्स में यह कम्पनी साइकिल की आधिकारिक सप्लायर थी। सन् 2003-4 से एटलस कम्पनी पर संकट के बादल मँडराने शुरू हुए। इसके तकरीबन 10 साल बाद कम्पनी ने अपना 2014 में मध्य प्रदेश के मलनपुर स्थित एक कारखाना बन्द कर दिया। इसके बाद 2018 में सोनीपत स्थित कारखाने को बन्द किया गया। और अब कम्पनी के साहिबाबाद स्थित आिखरी कारखाने को कम्पनी ने बन्द कर दिया। एटलस साइकिल का यह कारखाना ऐसे समय में बन्द हुआ है, जब दुनिया के कई देशों में एटलस साइकिल का निर्यात होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि एटलस साइकिल ने अभी तक किसी विदेशी साइकिल कम्पनी का भारत में दाँत नहीं गढऩे दिया है।
कई कम्पनियों पर पड़ेगा प्रभाव
एटलस साइकिल के कारखाने के बन्द होने से उन कई कम्पनियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो साइकिल के पार्ट बनाकर एटलस को सप्लाई करती हैं। इसमें टायर-ट्यूब उद्योग, बैङ्क्षरग उद्योग के अलावा साइकिल में उपयोग किये जाने वाले अन्य कई उद्योग हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हर साल एक करोड़ से अधिक साइकिल बनाने वाली एटलस कम्पनी करोड़ों के साइकिल पार्ट आयात भी करती होगी।
उत्पादन में आयी लगातार बढ़ोतरी
कोरोना वायरस के चलते इन दिनों भले ही साइकिल की बिक्री में कुछ कमी आयी हो, लेकिन तमाम इंजन वाहनों की संख्या बेतादाद बढऩे के बावजूद साइकिल के उत्पादन और बिक्री में कमी नहीं आयी। इसका कारण यह भी है कि एटलस कम्पनी साइकिल की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम है। बहुत कम साइकिल बनाने से शुरू किये गये एटलस साइकिल के कारखाने में साल दर साल उत्पादन बढऩे का एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सन् 2010-11 में तकरीबन डेढ़ करोड़ साइकिल हर साल यहाँ से बनकर निकलती थीं। साइकिलों की बिक्री बढऩे का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब कई विदेशी कार कम्पनियाँ तक साइकिल बनाने लगी हैं।
पर्यावरण की दोस्त और मुसीबत की साथी
भारत में लॉकडाउन होने पर कितने ही मज़दूरों की साथी बनी साइकिल की कीमत तो कोई उन्हीं से पूछे कि इस मुसीबत की घड़ी में उन्हें साइकिल मिलना कितने हर्ष की बात रही होगी। साइकिल का महत्त्व हरियाणा से बिहार करीब 1400 किलोमीटर अपने पिता को ले जाने वाली 15 साल की ज्योति बता सकती है, जिसके पिता ने 500 रुपये उधार लेकर एक पुरानी साइकिल खरीदी। साइकिल का महत्त्व एक विकलांग बेटे का वह मजबूर बाप बता सकता है, जिसे बड़ी शॄमदगी के साथ बेटे की खातिर साइकिल चुरानी पड़ी। या फिर वे अनगिनत परिवार बता सकते हैं, जिन्हें छोटे-छोटे बच्चों के साथ पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। आज जब पूरी दुनिया के पर्यावरणविद् कह रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को कम करने के लिए जितना मुमकिन हो साइकिल से सफर कीजिए। आज जब डॉक्टर सलाह देते हैं कि साइकिल चलाना सेहत के लिए लाभदायक है। आज जब पूरी दुनिया में अनेक अमीर भी साइकिल चलाने लगे हैं। दुनिया भर में अनेक लोग साइकिल से कार्यालय तक जाने लगे हैं, तब भारत में एटलस साइकिल के कारखाने का बन्द होना काफी दु:खद है।
साइकिल का आविष्कार
आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि साइकिल का आविष्कार सन् 1839 में स्कॉटलैंड में एक लुहार के हाथों हुआ था। इस लुहार का नाम था- किर्कपैट्रिक मैकमिलन। वैसे यूरोपीय देशों में 18वीं शताब्दी के उतराद्र्ध में साइकिल का विचार पनपने लगा था, जिसका अविकसित मूर्तरूप सन् 1816 में लकड़ी की साइकिल के रूप में पेरिस के एक कारीगर के द्वारा अस्तित्व में सामने आया, जिसे हॉबी हॉर्स कहा गया। इससे पहले साइकिल का एक अधूरा या कहें कि अपूर्ण रूप चलन में था और उसे बच्चों की बेङ्क्षरग गाड़ी की तरह पाँवों की तरह दोनों पाँवों से खिसकाना पड़ता था; जिसके चलते साइकिल का यह आविष्कार न तो चर्चा में था और न ही इसका उपयोग बहुत लोग करते थे। इसके बाद पैडल का आविष्कार सन् 1865 में पैरिस निवासी लालेमे ने किया। उन दिनों पैडल को क्रैंको कहा जाता था और इस यंत्र को वेलॉसिपीड। तब इसे चलाने वाले को बेहद थकावट हो जाती थी। इसलिए बहुत-से लोग इसे बोन शेकर यानी हाड़तोड़ कहते थे। कुछ भी हो साइकिल का आविष्कारक किर्कपैट्रिक मेकमिलन को ही माना जाता है। जब मैकमिलन ने इसे पैरों से चला सकने लायक बनाया, तो इसका उपयोग बढऩे लगा और साइकिल चर्चा में आने लगी। मैकमिलन ने पहले इसका नाम वेलोसिपीड रखा। उसके बाद इसे बायसडक़ल या बाइसिकिल कहा जाने लगा।
ऐसा माना जाता है कि साइकिल के शुरुआती स्वरूप की रूपरेखा सन् 1817 में जर्मनी के बैरन फॉन ड्रेविस ने तैयार की थी। तब यह लकड़ी से बनायी गयी थी और इसका नाम ड्रेसियेन रखा गया था। बताया जाता है कि यह साइकिल एक तेज़ चाल से चलने वाले पैदल व्यक्ति की तरह ही चल पाती थी, जिसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। शायद इसीलिए इसका उपयोग कम ही लोग करते थे। कुछ प्रमाण यह भी कहते हैं कि सन् 1763 में ही फ्रांस के पियरे लैलमेंट ने पैरों से घसीटे जाने वाले एक साधन की खोज की थी, बाद में इसी का रूप सुधरता गया और साइकिल हमारे अस्तित्व में आयी। इसके बाद इसकी माँग बढ़ती गयी और इंग्लैंड, फ्रांस तथा अमेरिका ने इसे यात्रा के सुलभ साधन के रूप में विकसित कर दिया। साइकिल की पहला सही रूप सन् 1872 में में सामने आया, जिसे चलाने बहुत मुश्किल या बोझिल नहीं रह गया था। इसमें लोहे की पतली पट्टी के तानयुक्त दो पहिये लगाये गये थे। इसमें आगे का पहिया 30 इंच से 64 इंच तक के व्यास का और पिछला पहिया 12 इंच के व्यास का होता था। इसमें क्रैंकों के अतिरिक्त गोली के बैङ्क्षरग और ब्रेक भी लगाये गये थे, जिससे इसे चलाना बहुत मुश्किल नहीं था। भारत के आॢथक पहियों में साइकिल के पहिया भी एक अहम पहिया था। आज़ादी के बाद से अगले कई दशक तक यहाँ की यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा साइकिल ही रही है। जब मोटरसाइकिल का चलन बढ़ा, तो साइकिल का चलन कम होता दिखा; लेकिन फिर भी आज भी लाखों लोगों के पास साइकिल ही वाहन का एक मात्र निजी साधन है।
आॢथक मंदी की वजह से उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध एटलस साइकिल कम्पनी में उत्पादन बन्दी की खबर बेहद चिन्ताजनक है। इससे हज़ारों मज़दूरों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। बेरोज़गारी के इस दौर में ये गरीब अब कहाँ जाएँगे? भाजपा की गलत नीतियों की वजह से अब एक और बन्दी शुरू।
अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष
विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल कम्पनी एटलस की गाज़ियाबाद फैक्ट्री बन्द हो गयी है। सरकार के प्रचार में तो सुन लिया कि इतने पैकेज, इतने एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग), इतने रोज़गार। लेकिन असल में तो रोज़गार खत्म हो रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बन्द हो रही हैं।
प्रियंका गाँधी, कांग्रेस महासचिव
ऐसे समय में जबकि लॉकडाउन के कारण बन्द पड़े उद्योगों को खोलने के लिए आॢथक पैकेज आदि सरकारी मदद देने की बात की जा रही है, तब यूपी के गाज़ियाबाद स्थित एटलस जैसी प्रमुख साइकिल फैक्ट्री के धन अभाव में बन्द होने की खबर चिन्ताओं को बढ़ाने वाली है। सरकार तुरन्त ध्यान दे, तो बेहतर है।
मायावती, बसपा प्रमुख