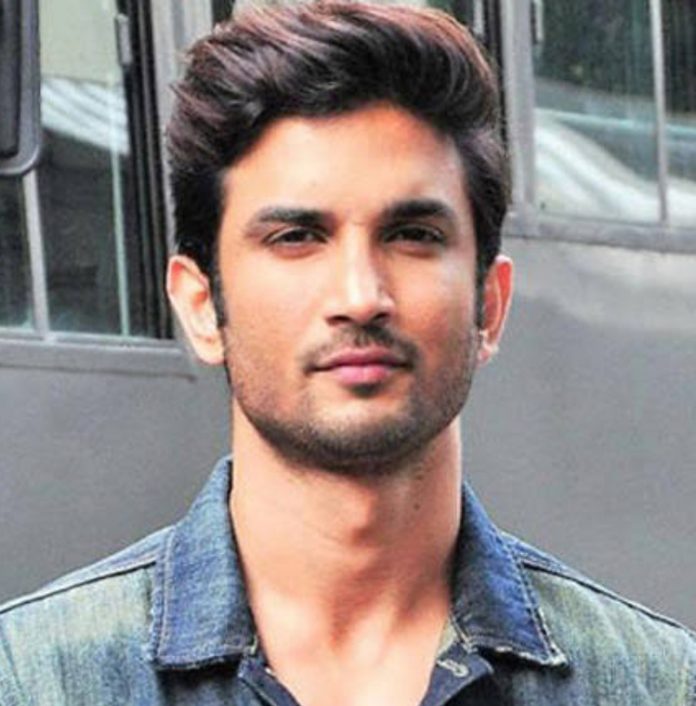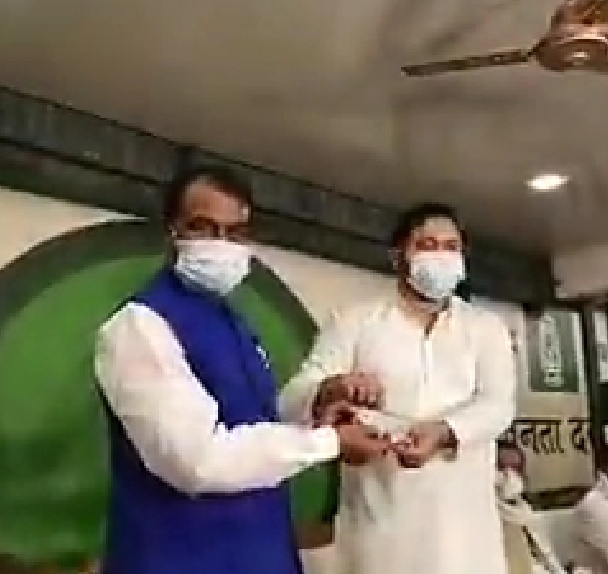कोरोना की शुरुआत के समय 28 मार्च को मोदी सरकार की तरफ से बनाए गए प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन असिस्टेंस ऐंड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशंस (पीएम केयर्स फंड ) को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड का पैसा ट्रांसफर करने को लेकर आज हुई सुनवाई में कहा कि एनडीआरएफ में पैसा ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। न ही किसी नई आपदा राहत योजना की अभी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर दायर दायर याचिका आज खारिज कर दी गई। एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) यह याचिका दायर कर मांग की थी कि पीएम केयर फंड में जमा रकम को कोरोना महामारी के मद्देनजर एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने इसके लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एनडीआरएफ में योगदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति और कॉरपोरेट के लिए कोई वैधानिक बाधा नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार पीएम केयर्स फंड की राशि को उचित जगह ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि ये दोनों फंड अलग हैं।
इससे पहले इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका में पीएम केयर फंड में जमा हुई राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच के सामने कहा था कि पीएम केयर फंड स्वैच्छिक फंड है जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंड बजट आवंटन के दायरे में हैं।
उधर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से दलील पेश करते हुए कहा था कि हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे है लेकिन पीएम केयर फंड का गठन नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट के प्रावधान के विपरीत है। दवे ने कहा था कि एनडीआरएफ का ऑडिट सीएजी करता है लेकिन सरकार कह रही है कि पीएम केयर फंड का ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर से कराया जाएगा।
पीएम केयर फंड के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर पीएम केयर फंड का बचाव किया था। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय और राज्यों के आपदा में राहत कार्यों के लिए पीएम केयर फंड दूसरे किसी फंड पर रोक नहीं लगाता है। इन फंड में लोग स्वेच्छा से डोनेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि एनडीआरएफ जैसी वैधानिक फंड होने के बावजूद ऐसे कोष यानी पीएम केयर फंड के गठन पर कोई रोक नहीं है।
वैसे पीएम केअर्स फंड पर विपक्ष का मोदी सरकार पर लगातार हमला रहा है। कांग्रेस इसके ऑडिट की मांग कर चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस फंड के पैसे आवंटित करने की जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक 31 मई तक कोरोना से लड़ाई के लिए 3100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इनमें 2000 करोड़ रुपये स्वदेशी वेंटिलेटर पर, 1000 करोड़ रुपये प्रवासी मजदूरों की देखभाल और 100 करोड़ रुपये वैक्सीन की रिसर्च पर खर्च किये गए हैं या हो रहे हैं।