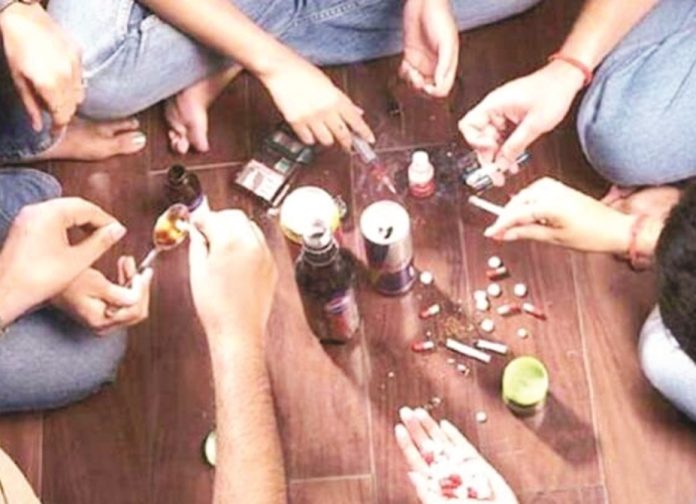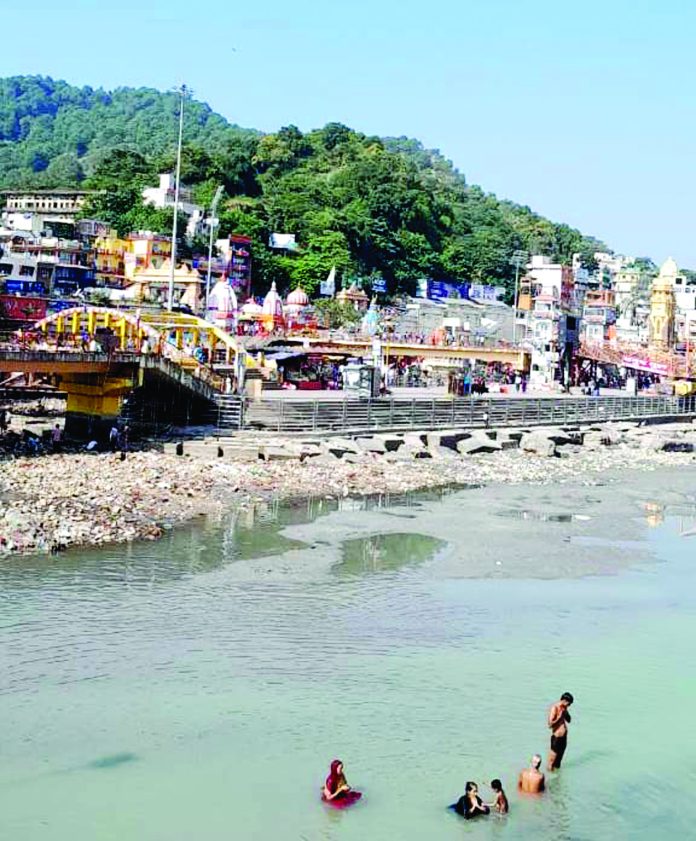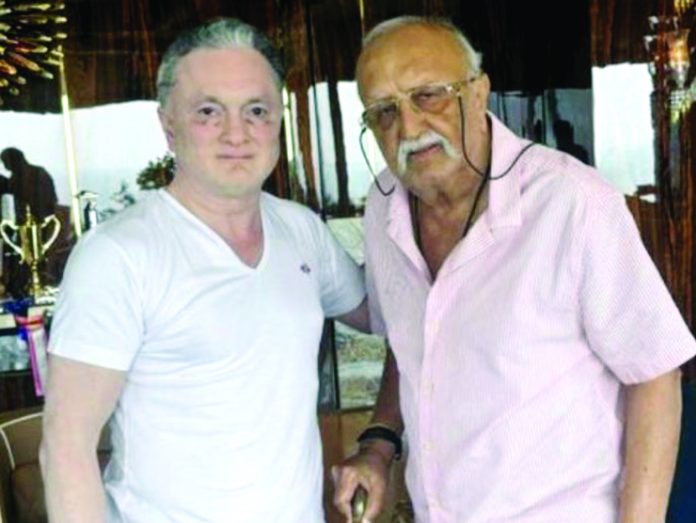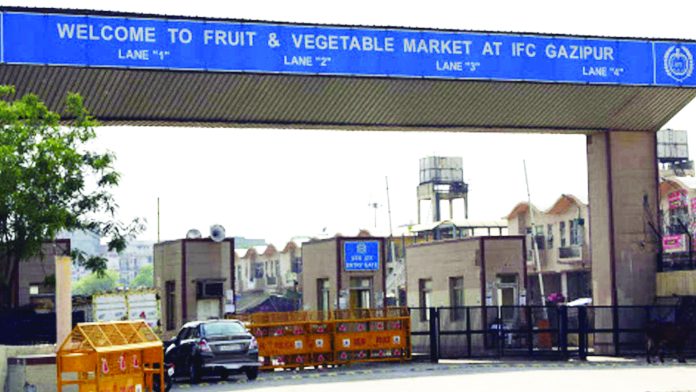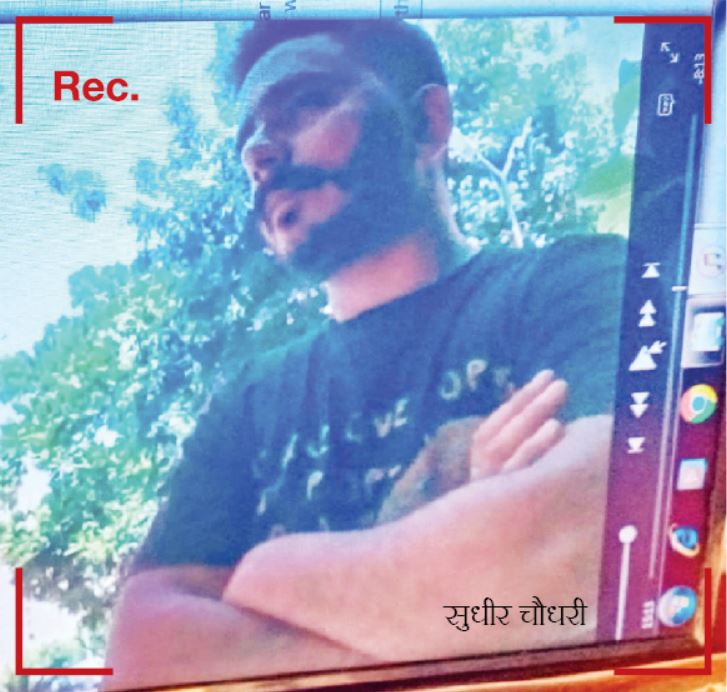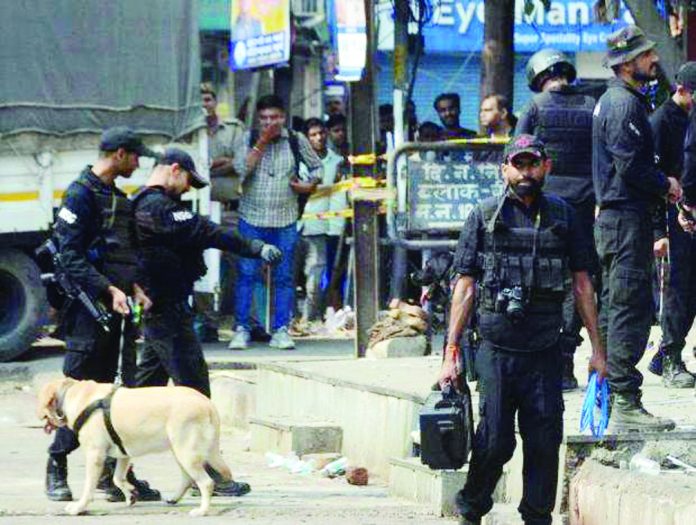यह बहुत दिलचस्प बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को देश के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसे समय में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के नये मुखिया के रूप में स्थापित करने में जुटा हुआ है, जब भारत और कनाडा के द्विपक्षीय सम्बन्ध बहुत ख़राब स्थिति में पहुँच चुके हैं। दोनों देश हाल में एक-दूसरे के छ: राजनयिकों को निष्कासित कर चुके हैं। और यह तब हुआ, जब ओटावा ने यह आरोप दोहराया कि 2023 में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साज़िश भारत सरकार ने रची थी। दिलचस्प यह है कि कनाडा की राजधानी ओटावा में भारत के वरिष्ठ राजनयिकों के ख़िलाफ़ इस मामले में जब साज़िश जैसे गंभीर आरोप लगाये गये, तब कनाडाई अधिकारियों ने चौंकाने वाला यह आरोप भी लगाया कि राजनयिक मिशन को भारत की एजेंसी रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) के इशारे पर कुख्यात अपराधी सरगना लॉरेंस बिश्नोई से मदद मिली।
ज़ाहिर है भारत ने इन सब आरोपों का खंडन किया है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई के इतने ताक़तवर अपराधी हो जाने को लेकर सवाल उठना लाज़िमी है। लॉरेंस विश्नोई पिछले 10 साल, अर्थात् 2014 से गुजरात की जेल में बंद है। इसके बावजूद वह अपने गैंग के संपर्क में रहता है और अपने गुर्गों को जेल से ही दिशा-निर्देश देता है। आख़िर जेल में भी उसे इतनी ढील मिलने के पीछे कौन-सी ताक़त है? पुलिस चाहे, तो किसी क़ैदी के पास पंछी भी पर नहीं मार सकता, उसे मोबाइल फोन मिलना तो दूर की बात है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को ये सब सुविधाएँ जेल के भीतर भी मिल रही हैं। यह इसलिए भी हैरानी की बात है कि देश की सरकार में दो सबसे ताक़तवर नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह गुजरात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में वहाँ सुरक्षा में इतनी चूक कैसे की जा सकती है कि एक अपराधी धड़ल्ले से जेल के भीतर से भी गैंग चलाता रहे और उसके पास मोबाइल फोन और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हों?
हाल में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीक़ी की हत्या की ज़िम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ही ली है। यह वही देश है, जहाँ कथित रूप से पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश के आरोप में दज़र्नों एनकाउंटर किये गये, जिसमें कई आरोपी-अपराधी मारे गये हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद इतना गदर मचाये हुए है कि उसे दाऊद इब्राहिम के बाद अब मुंबई के ख़तरनाक अंडरवर्ल्ड का नया सरगना कहा जाने लगा है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला से लेकर जो भी तमाम अपराध लॉरेंस बिश्नोई के नाम दर्ज हैं, वो यह साबित करते हैं कि निश्चित ही लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में अथाह ताक़त हासिल कर ली है। लेकिन यहाँ यह गंभीर सवाल भी उठ रहा है कि क्या सचमुच लॉरेंस इतना ख़तरनाक अपराधी हो गया है कि यह सब अपने बूते कर रहा है? या उसके पीछे कोई राजनीतिक ताक़त भी है? उसके 14 देशों में अपने संपर्क होने की जानकारी छनकर बाहर आ रही है और यह भी दावा किया जा रहा है कि उसके पास आज की तारीख़ में 700 शूटर्स का गैंग है, जो उसके एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम करने की क्षमता रखता है। और ये शूटर सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों में फैले हुए हैं। सलमान ख़ान जैसे बॉलीवुड के दिग्गज और ताक़तवर अभिनेता को अपनी धमकियों से डराना और उसके घर के बाहर गोलियाँ चलाने की हिम्मत करना आसान बात नहीं है। वह भी तब, जब सलमान ख़ान को तगड़ी पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन लॉरेंस के गुर्गे यह सब कर चुके हैं। फिरौती और हत्या जैसे कई मामलों में लॉरेंस आरोपी है। वह अपनी मज़ीर् से जब भी चाहे अपने गुर्गों के ज़रिये किसी से भी फिरौती लेता है या उसकी हत्या करवा देता है। बाबा सिद्दीक़ी की हत्या जब उसके गुर्गों ने की, तो इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए बिश्नोई के गैंग ने कहा कि चूँकि सिद्दीक़ी उनके सबसे बड़े दुश्मन सलमान ख़ान के दोस्त थे, इसलिए उन्हें मारा गया।
बलकरन बराड़ से लॉरेंस बिश्नोई बन जाने की कथा सचमुच अविश्वसनीय है क्योंकि यह आम धारणा है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के कोई भी अपराधी इतना ताक़तवर नहीं हो सकता कि किसी अन्य देश के बड़े अधिकारी उनके यहाँ हुई हत्या में उसका नाम जोड़ें। हाल में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक हैरानी भरा सच सामने आया था, जब उसके चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने चौंकाने वाला ख़ुलासा किया कि जेल में बंद लॉरेंस पर उसका परिवार साल भर में 35-40 लाख रुपये ख़र्च करता है। हालाँकि इतना पैसा लॉरेंस का परिवार किसलिए ख़र्च करता है और किस चीज़ पर ख़र्च करता है? यह तो उस जेल की पुलिस ही जाने। लेकिन निश्चित ही यह ख़ुलासा कई सवाल खड़े करता है।
यह माना जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के शुरुआती दिनों में कभी भी यह नहीं लगता था कि बलकरन भविष्य में इतना ख़तरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बन जाएगा। अब तो उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी है। हालाँकि यह अलग बात है कि उसके परिवार के लोग इसे ग़लत मानते हैं। रमेश बिश्नोई का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। रमेश के मुताबिक, लॉरेंस को फँसाने की साज़िश हो रही है। रमेश का कहना है कि लॉरेंस तो देशभक्त परिवार का बच्चा है। कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं पास करने वाला लॉरेंस जब कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गया, तो एक साल बाद हुए छात्र संघ के चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। माना जाता है कि इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनीं कि वह अपराध के रास्ते की तरफ़ चल पड़ा। उसे महँगे कपड़े और जूते पहनने अच्छे लगते थे। खेती के लिए अच्छी-ख़ासी ज़मीन थी, इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर ही थी। अब लॉरेंस का नाम अन्य मामलों के अलावा तीन हाई प्रोफाइल मर्डर से जुड़ा हुआ है। इनमें 2022 में पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, कनाडा में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में नाम सामने आने के अलावा बाबा सिद्दीक़ी की हत्या की ज़िम्मेदारी लेना शामिल है।
कनाडा की रॉयल माउंट पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यह दावा किया कि भारतीय एजेंट संगठित अपराध समूह बिश्नोई गैंग की मदद से कनाडा में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों, ख़ासकर खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद निश्चित ही लॉरेंस ज़्यादा सुर्ख़ियों में आ गया और भारत में टीवी चैनल उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड का नया डॉन बताने लगे। उसका देश के 16 राज्यों में दबदबा है और अब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपराध की दुनिया में कुख्यात हो गया है। मुंबई में बाबा सिद्दीक़ी की हत्या के बाद जब मुंबई पुलिस ने पूछताछ करने के लिए गुजरात पुलिस से लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड की माँग की, तो उसे बताया गया कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के एक आदेश के कारण लॉरेंस को रिमांड पर नहीं लिया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक, गुजरात तट से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क चलाने के आरोप में गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश और सीआरपीसी की धारा-268 के तहत अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर ले जाने पर एक साल की रोक है। यह रोक 2023 तक थी; लेकिन उपरोक्त धारा के तहत लगी रोक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-303 के तहत और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
सलमान ख़ान के घर गोलीबारी के मामले में पिछले साल जून में मुंबई पुलिस ने लॉरेंस को हिरासत में लेने के मक़सद से कोर्ट में एक से ज़्यादा बार अर्जी दी; लेकिन मुंबई पुलिस को हिरासत नहीं मिली। साबरमती की जेल हाई सिक्योरिटी जेल है। लेकिन क़रीब 32 साल का लॉरेंस उस जेल से धड़ल्ले से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। पूरे गैंग को जेल से चलाता है। यह सब तब है, जब उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड का अगला डॉन माना जा रहा है। हत्या, हत्या के प्रयास, वसूली और धमकाने के दज़र्नों मुक़दमे उस पर दर्ज हैं। निश्चित ही लॉरेंस बिश्नोई एक ख़तरनाक अपराधी है और प्रतिष्ठित लोगों के साथ-साथ समाज को भी उससे ख़तरा है। लेकिन जिस तरह से वह गैंग चला रहा है, उससे लगता ही नहीं कि वह जेल में बंद है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के वहाँ लगभग निष्क्रिय हो जाने के बाद लॉरेंस यह जगह भरने की फ़िराक़ में है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ़ लॉरेंस की ही कोशिश है या इसके पीछे कोई और भी ताक़त है? जो मुंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री को अपने हिसाब से चलाना चाहती है।
यह देखना होगा कि जेल में बंद होने के बावजूद अपनी आपराधिक गतिविधियों को चलाये रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई का भारत में उसके बिश्नोई गैंग की तरफ़ से किये जा रहे अपराधों के शिकार लोगों और कनाडा में निज्जर हत्याकांड में उसके तार जुड़े होने के कनाडा के अधिकारियों के आरोपों के बीच कोई कड़ी है? बेशक भारत कनाडा के आरोपों को ग़लत बता चुका है; लेकिन ये आरोप इतने छोटे नहीं हैं कि इन पर सवाल न उठें। सवाल इसलिए भी उठने लाज़िम हैं, क्योंकि बड़े-बड़े अपराध करने-कराने के आरोप के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई न होना और यह कहा जाना कि उसके ख़िलाफ़ कोई ठोस सुबूत नहीं है; देश में गुंडागर्दी और आतंकवाद को ख़त्म के दावों पर तमाचा है। हालाँकि लॉरेंस पर आरोप महज़ भारत को बदनाम करने की साज़िश है या इसके पीछे कोई ठोस आधार है? यह अभी नहीं कहा जा सकता। बाबा सिद्दीक़ी की हत्या के बाद मोबाइल से ईयर फोन के ज़रिये रिकॉर्ड लॉरेंस की आवाज़ में देश भक्ति से लबरेज गीत ‘सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।’ वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो साबरमती जेल की बैरक में हाल ही में रिकॉर्ड किया गया है। हालाँकि कई जानकार यह वीडियो आठ साल पुराना बता रहे हैं। निश्चित ही लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी से ज़्यादा एक रहस्य भी बन गया है, जिससे पर्दा उठना ज़रूरी है।