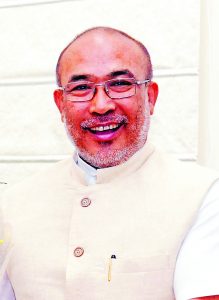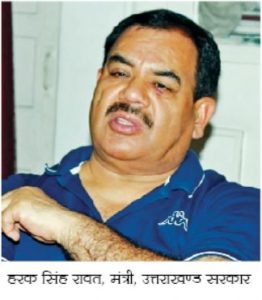लोकसभा के 2024 के चुनाव से पहले पाँच राज्यों के यह चुनाव दो बड़े राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के साथ कुछ क्षेत्रीय दलों का बड़ा इम्तिहान है। भाजपा के सामने उन चार राज्यों को बचाने की चुनौती है, जहाँ वह सत्ता में है; जबकि कांग्रेस उस एक राज्य पंजाब से ज़्यादा राज्यों में जीतना चाहती है, जहाँ वह इस समय सत्ता में है। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल के अलावा कुछ क्षेत्रीय क्षत्रपों की राजनीति का भविष्य भी तय होगा। चुनावों की घोषणा और बढ़ते कोरोना मामलों से उपजी चुनौतियों को लेकर बता रहे हैं विशेष संवाददाता राकेश रॉकी :-
दर्ज़नों चुनौतियों के बीच पाँच राज्यों के चुनाव आ गये। इनमें एक चुनौती कोरोना है, तो महँगाई, बेरोज़गारी और देश में समुदायों के बीच अविश्वास के बढ़ते ख़तरे की बड़ी चुनौती भी है। यह सिर्फ़ पाँच विधानसभाओं के चुनाव भर नहीं हैं।
यह चुनाव जनता के उस सम्भावित निर्णय का संकेत देंगे, जो भविष्य में वह कर सकती है। इन चुनावों के नतीजे देश के नेतृत्व के लिहाज़ से भी बहुत महत्त्वपूर्ण होंगे; क्योंकि कांग्रेस के राहुल गाँधी, टीएमसी की ममता बनर्जी और भाजपा के ही भीतर योगी आदित्यनाथ जाने-अनजाने प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के रूप में सामने रहेंगे। यही नहीं भाजपा के एक बड़े वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता पर अटूट विश्वास भी इन चुनावों में दाँव पर रहेगा। यह चुनाव वोटर की भी परीक्षा हैं; क्योंकि इनमें तय होगा कि वह अपने मुद्दों और भाजपा के हिन्दुत्व के एजेंडे में से किसे चुनता है। भाजपा के लिए यह चुनाव इसलिए भी चुनौती वाले हैं। क्योंकि जिन पाँच राज्यों में मतदान होगा, उनमें से चार पर भाजपा सत्ता में है, जबकि एक पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। सात चरणों के इस चुनाव में देश की राजनीति की भविष्य की दिशा काफ़ी हद तक तय हो जाएगी, यह तय है, भले यह चुनाव प्रदेशों के लिए हैं।
निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों की लिए तारीख़ों का ऐलान ऐसे मौक़े पर किया है जब जनता के मन में ढेरों सवाल हैं। उसके सामने महँगाई से लेकर बेरोज़गारी के मुद्दे दिन प्रतिदिन विकराल होते जा रहे हैं। समुदायों के बीच नफ़रतों की दीवार ऊँची होती जा रही है, जिससे सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न होने को है।
इससे लोगों में अपनी समस्यायों के हल होने की उम्मीद कम होती जा रही है; क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सत्ता में बैठे लोगों की उनकी दिक़्क़तें हल करने में कोई रुचि नहीं। यह चीज़ें जनता में गहरी निराशा इसलिए भी रही हैं; क्योंकि कोरोना से पनपी बेरोज़गारी और अपनों को खोने का गहरा दर्द उन्हें निराशा की तरफ़ धकेल रहा है। वे महसूस करने लगे हैं कि यदि वह अपने असली मुद्दों और समस्यायों (बेरोज़गारी, महँगाई आदि) की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो उन्हें और उनकी नयी पीढ़ी को बहुत कठिनाई भरे दिन देखने होंगे।
मोदी सरकार को सत्ता में आये अब आठ साल होने को हैं। यह वह समय होता है, जब जनता किसी सरकार के वादों, उसके काम और अपनी समस्याओं के हल होने का लेखा-जोखा करने लगती है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय भी यही हुआ था। 10 साल के उसके शासन के दौरान यही समय था, जब जनता उसे लेकर अपनी सोच साफ़ करने लग पड़ी थी। विपक्ष यूपीए सरकार पर गम्भीर रूप से हमलावर होने लगा था और तब क़रीब आठ साल से सत्ता से बाहर भाजपा अचानक बहुत सक्रिय होने लगी थी। तब में और आज में यह अन्तर ज़रूर है कि कोरोना महामारी के कारण कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जनता के बीच आज उस स्तर पर नहीं पहुँच पा रहे, जैसा 2012-13 के आसपास भाजपा कर पा रही थी। दूसरे विपक्ष के बीच आज बिखराव है, भले कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए एकजुट है। ज़ाहिर है एक तरह से यह क्रमश: भाजपा और कांग्रेस के एनडीए और यूपीए के अलावा तीसरे मोर्चे (आप, टीएमसी, वामपंथी दल आदि) की जंग है, जो कमोबेश हर चुनाव में रही ही है।
राज्यों के यह चुनाव ऐसे मौक़े पर होने जा रहे हैं, जब देश में विचारधारा के स्तर पर बड़ा बिखराव हो चुका है और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जनता को धार्मिक आधार पर विचारधाराओं के खुले टकराव की तरफ़ जाने के लिए उकसा रहे हैं, ताकि अपनी राजनीति की फ़सल को पकाया जा सके। यह चुनाव तय करेंगे कि क्या जनता इस मक़सद को समझ रही है या वह उनके राजनीतिक मक़सदों के लिए इस्तेमाल होने को तैयार है, भले इससे उन्हें अपने असली हितों की बलि देनी पड़ जाए।
मोदी सरकार के वादों के बाद किसान आन्दोलन स्थगित हो गया है; लेकिन किसानों और केंद्र सरकार के बीच अविश्वास जस-का-तस है। किसानों की कोई माँग अभी पूरी नहीं हुई है और चुनाव आचार संहिता के बाद इसकी कोई सम्भावना नहीं कि केंद्र सरकार इस दिशा में कुछ करेगी। किसान अब शिद्दत से यह महसूस कर रहे हैं केंद्र सरकार ने उन्हें छला है। एमएसपी की किसानों की माँग और अन्य मुद्दे अभी भी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखण्ड में बड़े मुद्दे बने हुए हैं, जिससे भाजपा विचलित है। चुनावों में इसके उलटे असर का डर उसे सता रहा है। भाजपा के बड़े नेताओं के भाषण इसका संकेत देते हैं।

देश में बुल्ली बाई, सुल्ली डील जैसे सोशल मीडिया के आपराधिक कारनामे और कट्टर विचारों को पोसने वाले धर्म संसद जैसे आयोजन और ऐसे ही अन्य उदाहरण ज़ाहिर करते हैं कि देश में नफ़रतों का बाज़ार किस स्तर पर सज रहा है। धर्म संसद में नफ़रत फैलाने का मसला तो ऐसा था, जिसमें पाँच पूर्व सेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इस पर गहरी चिन्ता जतायी और इस तरह के आयोजनों पर रोक लगाने की माँग की। जनता को धार्मिक आधार पर उलझाने की कोशिश जैसी आज हो रही है, वैसी कभी नहीं हुई।
आश्चर्य यह कि यह काम कोई धार्मिक हिन्दूवादी संगठन नहीं, बल्कि भाजपा जैसा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कर रहा है; और वह भी खुले रूप से। भाजपा ने साफ़ कर दिया है कि हिन्दुत्व उसका मुख्य एजेंडा है और उसे इसपर चुनाव लडऩे में कोई परहेज़ नहीं। ज़ाहिर है इसने देश की आबादी को पूरी तरह बाँटकर रख दिया है। भाजपा को अपने मक़सद में सफल होने का भरोसा है; लेकिन समाज के बीच बँटवारा हो रहा है।
आने वाले पाँच राज्यों के चुनाव में कम-से-कम उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब में भाजपा इसी लाइन पर काम करती दिख रही है, जो चुनाव पास आते आते और तेज़ हो जाएगा।
कांग्रेस, जिन पाँच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन सभी में अपनी उपस्थिति रखती है। उत्तर प्रदेश में भले उसका संगठन कमज़ोर हो, राज्य की जनता उसे उतना ही जानती है, जितना भाजपा, सपा और बसपा को। इसमें कोई दो-राय नहीं कि आज भी भाजपा के मुक़ाबले के लिए जनता के दिमाग़ में कांग्रेस का ही नाम आता है। लेकिन कांग्रेस लगातार दो लोकसभा चुनावों में मिली हार की धूल झाड़कर वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो पा रही।
सन् 2018 के आख़िर में जब उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल करके भाजपा को रक्षात्मक कर दिया था, तब लगा था कांग्रेस अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी; लेकिन लगता है संगठन के भीतर तालमेल की कमी से वह पंगु-सी हो गयी है।
सही मायने में देखा जाए, तो इन पाँच राज्यों के चुनाव जनता के चुनाव होने चाहिए थे। लेकिन साफ़ दिख रहा है कि साम्प्रदायिक ध्रवीकरण के ज़रिये जनता की सोच हाईजैक करके उसे दिमाग़ में धर्म आधारित ज़हर भरकर जनादेश लेने की कोशिश हो रही है। वरना उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में महँगाई, बेरोज़गारी, कोरोना में सरकार के काम जैसे मुद्दों पर चुनाव लडऩे से भाजपा न घबरा रही होती। उसे वहाँ अपने धार्मिक एजेंडे को ही आगे करना पड़ रहा है। भले चुनावी सर्वे में इंतज़ाम करके जो दिखाया जा रहा हो, उत्तर प्रदेश की ज़मीनी सच्चाई यह है कि योगी सरकार पर कामकाज के नाम पर फेल रहने, कोरोना को बहुत ख़राब तरीक़े से हैंडल करने और रोज़गार के मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम रहने की तोहमत लगायी जा रही है। जनता उनसे काम के मामले में बहुत प्रसन्न नहीं है।
ऊपर से उत्तर प्रदेश के राजपूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक ही जाति विशेष के लोगों को पोसने और संरक्षण देने होने के गम्भीर आरोप लग रहे हैं। ब्राह्मण यूपी में योगी के कारण भाजपा के सख़्त नाराज़ हैं। दूसरे वर्ग भी ख़ुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। मुसलमान तो उसके ख़िलाफ़ हैं ही। योगी शासन के दौरान अपराध इतने हुए हैं कि गिनना मुश्किल। ऊपर से तुर्रा यह कि अपराधियों को संरक्षण देने की आरोप हैं।
ऐसे में भाजपा के लिए 2022 के इस विधानसभा चुनाव में बड़ी दिक़्क़ते हैं। भाजपा ने योगी को लेकर जनता की इस नाराज़गी को समझा है। यह तो उसे पता चल गया है कि सरकार के काम या उसके प्रदर्शन के नाम पर पार्टी को दोबारा सत्ता मिलना मुमकिन नहीं है। लिहाज़ा मन्दिर-मस्जिद, काशी-मथुरा, जिन्ना, हिन्दू-मुस्लिम उसके बड़े नेताओं के भाषणों में मज़बूती से उभर आये हैं।
उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे मज़बूत और कट्टर विरोधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा पर चुनावों को साम्प्रदायिक रूख़ देने के आरोप लगा रहे हैं; लेकिन यूपी जैसे राज्य में उसके लिए भाजपा के ख़िलाफ़ माहौल बनाना आसान नहीं। बस एक ही रास्ता है कि जनता तो चुनाव तक किसी तरह असली मुद्दों के नज़दीक ले जाया जाए, जैसा कि अखिलेश यादव और प्रियंका गाँधी कर रहे हैं। योगी सरकार के प्रति नाराज़गी यदि जनता के सिर पर हावी हुई, तो ही भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं; और इसकी सम्भावना को ख़ारिज़ नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बसपा और उसकी नेता मायावती की बात है, तो जनता में फ़िलहाल उसकी छवि भाजपा की बी टीम और गुमसुम बैठी पार्टी वाली स्थापित हो गयी है।
उत्तर पूर्व के राज्य माणिपुर में भी चुनाव के अपने गम्भीर मुद्दे हैं। वहाँ जनता में सुरक्षा बलों की कथित ज़्यादतियों को लेकर नाराज़गी और व्यवस्था के प्रति गहरी निराशा है। लोगों का आरोप है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में सुरक्षा बलों को अफ्सपा क़ानून (एएफएसपीए क़ानून) के तहत मिले विशेष अधिकारों का दुरुपयोग जनता के दमन के लिए किया जाता है। हर किसी को शक की निगाह से देखा जाता है और किसी को भी पकड़कर उसे विद्रोही बताकर गोली से उड़ा दिया जाता है या उस पर ज़ुल्म किया जाता है।
ऐसे में लोगों के बीच बहुत ज़्यादा ग़ुस्सा है। हाल में उत्तर पूर्व के राज्य नागालैंड में 15 लोगों को सुरक्षा बलों ने महज़ इस आधार पर गोली से उड़ा दिया था; क्योंकि उन्हें इन लोगों पर शक था। बाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह को संसद में इसे लेकर सफ़ार्इ देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि ग़लत पहचान के कारण सुरक्षा बलों ने गोली चलायी, जिससे इन लोगों की जान गयी।
मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होने हैं और भाजपा वहाँ इस समय सत्ता में है। वहाँ जनता बहुत ताक़त से राज्य में अफ्सपा क़ानून को लागू नहीं (ख़त्म) करने की माँग कर रही है। लेकिन भाजपा इसके सख़्त ख़िलाफ़ है और चाहती है यह लागू रहे, जबकि एक सच्चाई यह भी है कि उत्तर पूर्व राज्यों के दो मुख्यमंत्री खुले रूप से इस क़ानून के ख़िलाफ़ बोल चुके हैं और हटाने की माँग कर चुके हैं। कांग्रेस वादा कर चुकी है कि सत्ता में आते ही अफस्पा को हटा देगी, ताकि मानवाधिकारों का हनन न हो। चीन की सीमा पर संवेदनशील राज्यों में जनता को मुख्यधारा में बनाये रखने के लिए केंद्र की सरकार को इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए था; लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
पंजाब में भी स्थिति को साम्प्रदायिक करने की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं। किसान आन्दोलन के बाद पंजाब के बहुसंख्यक वर्ग के प्रति एक अलग तरह का अभियान सोशल मीडिया के ज़रिये शुरू हो चुका है, जिसमें उन्हें देश के ख़िलाफ़ दिखाने की गहरी साज़िश हो रही है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब की चुनाव यात्रा के दौरान उनके एक पुल पर फँसने तक को सोशल मीडिया में एक अलग और साम्प्रदायिक तरीक़े से दिखाने की साज़िश हुई है।
यहाँ तक आरोप हैं कि चूँकि पंजाब चुनाव में भाजपा के लिए कोई गुंजाइश नहीं, यूपी चुनाव में लाभ लेने के लिए इस घटना को एक अलग ही तरह का रूप देने की कोशिश हो रही है। ज़ाहिर है ऐसा करके पाकिस्तान से सटे राज्य के एक समुदाय विशेष को निशाने पर रखने की कोशिश भविष्य में बहुत ख़राब नतीजे देने वाली साबित हो सकती है। पंजाब पहले ही दशक तक लम्बे खिंचे आतंकवाद से ग्रस्त रहा है और देश विरोधी शक्तियाँ ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती हैं। ज़ाहिर है, असली मुद्दों की जगह साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है ताकि चुनाव जीते जा सकें। जनता से जुड़े मुद्दों को इसलिए परदे के पीछे सरकाया जा रहा है, क्योंकि यह सत्ता में बैठे लोगों के लिए कलंक बनकर उभरता है। यह उनकी नाकामी और चुनाव जीतने के लिए किये वादों को पूरा न कर पाने की कमज़ोरी को उजागर करता है। ये मुद्दे सामने रहे, तो उन्हें हार का डर सताता है; लिहाज़ा अप्रासंगिक मुद्दे सामने हैं। ये मुद्दे निश्चित ही साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश के लिए हैं। भाजपा को लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे पुलवामा के बाद देश में उठी देशभक्ति की लहर उसके लिए वोटों की खान बन गयी थी, वैसा ही अब भी हो सकता है।
महामारी और चुनाव
चुनाव आयोग की चुनौती इस बार बड़ी है; क्योंकि जिस दिन (8 जनवरी की शाम) उसने चुनाव की घोषणा की, देश में उस सुबह तक कोरोना के 1,41,986 नये मामले सामने आये थे और 24 घंटे में 285 लोगों की जान गयी थी। लोगों में कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर दहशत भर रही थी; लेकिन फिर भी चुनाव की घोषणा हुई।
हाँ, चुनाव आयोग ने पिछले एक महीने से लाखों की भीड़ वाली चुनाव जनसभाओं से बचने के लिए 15 फरवरी तक इन पर और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगते हुए सिर्फ़ वर्चुअल (आभासी) चुनाव सभाएँ करने की मंज़ूरी दी।
यह एक अच्छा फ़ैसला था। यह देश के चुनावी इतिहास का भी पहला ऐसा फ़ैसला है, जिसकी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रशंसा की।
लेकिन सवाल यह है कि इस दौरान जब महामारी के मामले बढ़ेंगे, चुनाव में उलझीं पाँच राज्यों की सरकारें या राजनीतिक दल महामारी पर ध्यान कहाँ दे पाएँगे? चुनाव अपने आप में सरकारी तंत्र के एक बड़े हिस्से को व्यस्त कर देते हैं। चुनाव निपटाने की ज़िम्मेदारियों सरकारी कर्मचारियों पर होती हैं, जिससे निश्चित ही कोरोना से बचाव की तैयारियाँ प्रभावित होंगी। अफ़सरों का एक बड़ा तबक़ा चुनाव में उलझा रहेगा। यही कारण है कि काफ़ी लोग ऐसे संकट के समय में चुनाव करवाने के फ़ैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं।
सत्ता में बैठे लोगों को यह लगता है कि चूँकि देश में बड़े पैमाने पर कोरोना बचाव का टीकाकरण हो चुका है, यहाँ अब महामारी से जानी नुक़सान का कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, बेशक कोरोना मामलों में तेज़ी भी आ जाए। लेकिन यह उतना सच नहीं। आँकड़े ज़ाहिर करते हैं कि देश में ऐसे हज़ारों लोग अब फिर कोरोना संक्रमित हुए हैं, जो पहले ही कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके हैं।
कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने से संक्रमित हो सकता है। लिहाज़ा चुनाव में इसका ख़तरा सबसे ज़्यादा रहेगा, भले चुनाव सभाएँ न भी हों, क्योंकि राजनीतिक दलों के छोटे समूह मतदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क किये बिना रह नहीं पाएँगे। वैसे भी यह पाबंदी 15 जनवरी तक है और उसके बाद इस पर स्थिति को देखकर फ़ैसला होना है।
देश में 2021 के मध्य में कोरोना की दूसरी लहर के बाद यह पहले बड़े चुनाव हैं। भले पश्चिम बंगाल के चुनाव भी हुए थे। लेकिन यह अप्रैल में हुए थे, जब दूसरी लहर उफान पर थी। भाजपा को उस चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या जनता ने देश में उस समय ऑक्सीजन की गम्भीर क़िल्लत और इससे बड़े पैमाने पर हुई मौतों के ख़िलाफ़ जनादेश दिया था! लोगों के ज़हन से वो दौर अभी निकला नहीं है और कोरोना की इस तीसरी लहर के ख़ौफ़ ने उन लम्हों और अपनों को गँवाने वाले लोगों के ज़ख़्मों को फिर हरा कर दिया है। लिहाज़ा इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जनता वोट डालते समय इसे याद रखे।
दिसंबर के आख़िर तक के दूसरी लहर के बाद के पिछले कुछ महीनों में जब कोरोना के कम मामले देश में हुए थे, छोटे धन्धे धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगे थे। हालाँकि मार्च, 2020 के अनियोजित लॉकडाउन के बाद जो करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए उनमें से कुछ फ़ीसदी ही दोबारा रोज़गार में वापस लौट पाये हैं। कई छोटे धन्धे हमेशा के लिए बन्द हो गये हैं, और लोगों की जेब में पैसा नहीं है। रोज़गार आज की तारीख़ में एक बड़ा मुद्दा है ऊपर से महँगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है। उधर देश की अर्थ-व्यवस्था का जो बँटाधार इन दो वर्षों में हुआ है, आज तक उसके बेहतर होने के कोई ठोस संकेत नहीं दिखायी दियी हैं।
लोगों में अभी भी बहुत निराशा है और उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार इस मोर्चे पर बहुत नाकाम साबित हुई है। कोरोना की नयी लहर के ख़तरे से यह निराशा और गहरा रही है, जिसका चुनाव में वोट देने के ट्रेंड पर असर पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो भाजपा को इसका नुक़सान उठाना पड़ेगा। ज़ाहिर है, इस चुनाव के ज़रिये इन पाँच राज्यों की जनता यह मत भी देगी कि क्या वह केंद्र की मोदी सरकार कोरोना लहरों के समय किये इंतज़ामों से सन्तुष्ट रही है, या नहीं?
राजनीतिक दलों की जंग
पाँच राज्यों के यह चुनाव भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, जो अगले लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों को जीतकर अपना सिंहासन बचाये रखना चाहती है। भाजपा के नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता को अभी भी भरोसा है कि पार्टी अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूते येपाँच चुनाव ही नहीं अगले लोकसभा चुनाव भी फिर से जीतेगी। उन्हें इस बात से कोई लेना-देना नहीं कि केंद्र सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरी है? वो सिर्फ़ यह मानते हैं कि आज भी मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है।
मोदी के यह समर्थक यह भी मानते हैं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस, ख़ासकर गाँधी परिवार की छवि जनता के बीच ध्वस्त कर चुका है। वो यह गर्व से कहते हैं कि इसमें ग़लत क्या है? दिल्ली में भाजपा के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर इस संवाददाता से कहा- ‘राजनीति में हर हथकंडा अपनाया जाता है। भाजपा नेतृत्व को कांग्रेस पर हर तरह से आक्रमण करने का अधिकार है। जनता ने हमारे नेताओं की बात पर भरोसा किया न? फिर? बात ख़त्म।‘
लेकिन जो भाजपा ने किया क्या वह सच में स्थायी रूप से जनता के मन में बस गया है? अर्थात् कांग्रेस, ख़ासकर गाँधी परिवार को, बदनाम करने की उसकी मुहिम का जनता पर अभी भी असर है? क्या इस चुनाव में जनता बताएगी कि उसने भाजपा नेताओं के आरोपों पर आँख मूँदकर भरोसा नहीं किया। यह तो चुनाव नतीजों से ही ज़ाहिर होगा।
यदि जनता अब भी कांग्रेस को वोट करती है और कुछ जगह उसे सत्ता में ले आती है, तो यही माना जाएगा कि भाजपा नेतृत्व के उन आरोपों या वर्षों चलायी मुहिम का असर धुलने लगा है। ऐसे में यह तथ्य भाजपा के लिए आने वाले वर्षों में चिन्ता का सबब रहेगा। और यदि कांग्रेस को एक भी राज्य में सत्ता नहीं मिलती, तो यही माना जाएगा कि भाजपा नेतृत्व (या पार्टी रणनीतिकारों) ने देश को कांग्रेस मुक्त करने की, जो मुहिम वर्षों चलाये रखी, उसका असर अभी तक जनता पर है।
राजनीति के जानकार मानते हैं कि भाजपा के नेता चाहे जितना कांग्रेस को कोसें या उसे कमज़ोर बताएँ, वो जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि उसके लिए कोई पार्टी ख़तरा बन सकती है, तो वह कांग्रेस ही है। हाल में टीएमसी नेता ममता बनर्जी की तीसरा मोर्चा जमाने की मुहिम इसलिए ज़ोर नहीं पकड़ पायी; क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को इससे बाहर रखने की कोशिश की।
देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं का साफ़ कहना था कि बिना कांग्रेस के मज़बूत विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती।
भाजपा इन चुनावों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। पंजाब में उसका तुक्का तीर बन जाए, तो पता नहीं। ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि पंजाब में भाजपा बहुत ख़राब स्थिति में है। उसके साथ जाने का नुक़सान पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह को भी झेलना पड़ सकता है। अकाली दल किसान आन्दोलन के समय हुए अपने नुक़सान की भरपाई की कोशिश में अन्यथा लगता यही है कि मुख्य मुक़ाबला कांग्रेस और आप में होगा।
मणिपुर में कांग्रेस उससे सत्ता छीनने की कोशिश में है, जबकि गोवा में स्थिति बिखरी-सी है। इस तरह भाजपा का सबसे बड़ा दाँव उत्तर प्रदेश पर ही है।
यह चुनाव कांग्रेस के लिए बतौर एक पार्टी और बतौर उसके नेतृत्व बहुत-ही ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। यह चुनाव बताएँगे कि आने वाले महीनों में उसके फिर से खड़ा होने की कितनी गुंजाइश है। उसके लिए कम-से-कम एक या दो राज्य जीतने और उत्तर प्रदेश में उसे पहले से बेहतर प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है।
उसके पास उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में सत्ता में लौटने का समान रूप से अवसर है। उसके चुनाव प्रचार पर निर्भर करेगा कि वह कैसे जनता तक मज़बूती से पहुँच पाती है। उत्तर प्रदेश में पार्टी महासचिव प्रियंका गाँधी ने बहुत ज़ोर लगा रखा है।
इस समय मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रियंका गाँधी की यूपी में मेहनत की तारीफ़ कर चुके हैं। भाजपा से नाराज़ चल रहे वरुण गाँधी भी चर्चा में हैं। क्या यह दोनों कांग्रेस से जुड़कर उत्तर प्रदेश की राजनीति की धारा को अचानक बदल सकते हैं? अभी कहना मुश्किल है। मालिक किसानों ने हक़ में लगातार बोल रहे हैं। उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना $कद है।
वरुण गाँधी को लेकर कहा जाता है कि वह प्रियंका गाँधी का काफ़ी सम्मान करते हैं और कभी-कभार दोनों में बात भी होती है। वरुण क्या कांग्रेस में आ सकते हैं? यह भी वक़्त ही बताएगा। यदि सत्यपाल मलिक और वरुण गाँधी आये तो कांग्रेस अचानक बड़ी चर्चा में आ जाएगी। ऐसे में मुस्लिम वोट भी कांग्रेस की झोली में टपक सकता है। लेकिन सब चर्चाएँ हैं, होगा क्या यह आने वाले एक पखबाड़े में ही साफ़ होगा? टीएमसी गोवा में दाँव आजमा रही है और मणिपुर में भी। अन्य राज्यों में उसका कोई नाम लेवा नहीं। आप पंजाब में मज़बूत है और उत्तराखण्ड, गोवा में भी कुछ सीटें जीतने की उसकी मंशा है। गोवा और मणिपुर में क्षेत्रीय क्षत्रप भी हैं।
उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री : योगी आदित्यनाथ (भाजपा)

उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव शायद हाल के वर्षों की सबसे महत्त्वपूर्ण चुनावी लड़ाइयों में से एक है। राज्य के चुनाव नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव पर गहरा प्रभाव डालेंगे। सन् 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 325 सीटों के साथ तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया था। उस समय पाँच बार के सांसद योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने। हिन्दुत्व की राजनीति के मज़बूत पैरोकार योगी को आज भाजपा में उनके समर्थक भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। चुनाव में भाजपा के अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा प्रमुख दावेदार हैं।
पंजाब
मुख्यमंत्री : चरणजीत सिंह चन्नी (कांग्रेस)

पंजाब की राजनीति के पिछले कुछ महीने बहुत उथल-पुथल भरे रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस अभी भी भीतरी उठापटक से पीडि़त है। लेकिन इसके बावजूद सत्ता की दौड़ में वह मज़बूत दिख रही है। उसका मुख्य मुक़ाबला फ़िलहाल आम आदमी पार्टी (आप) से दिख रहा है, जबकि कई बार सत्ता में रहा अकाली दल, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और भाजपा भी मैदान में डटे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मतभेदों की बातें सामने आती रहती हैं; लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस को हारने के लिए आप सहित अन्य दलों को काफ़ी मेहनत करनी होगी। सन् 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जबकि आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। अकाली दल को 15, जबकि भाजपा को सिर्फ़ तीन सीटें मिली थीं।
उत्तराखण्ड
मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी (भाजपा)

सन् 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा; लेकिन ख़ुद रावत और कांग्रेस चुनाव हार गये। हालाँकि हाल के महीनों में भाजपा ने जिस तरह मुख्यमंत्री बदले हैं, उस से उसकी छवि को धक्का लगा है। उस चुनाव में भाजपा ने 57 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गयी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9 मार्च, 2021 को इस्ती$फा दे दिया। उनके बाद मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत भी थोड़े समय बाद चलते बने। धामी के नेतृत्व में अब भाजपा कांग्रेस की तरफ़ से मिल रही चुनौती को झेल रही है। यहाँ ‘आप’ भी मैदान में है।
मणिपुर
मुख्यमंत्री : एन बीरेन सिंह (भाजपा)
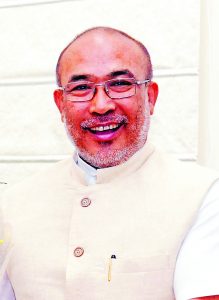
मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में है। वह सत्ता दोहराना चाहती है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी भी मैदान में आ डटी है। कांग्रेस पहले से ही मैदान में है और भाजपा को कड़ी टक्कर देकर सत्ता से बाहर करना चाहती है, पिछली बार वह भाजपा से आगे थी। कुछ स्थानीय दल भी मैदान में हैं।
गोवा
मुख्यमंत्री : प्रमोद सावंत (भाजपा)

गोवा में इस बार चुनावी जंग बड़ी कड़ी दिख रही है। भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी के अलावा स्थानीय दल मैदान में हैं। सन् 2017 में भाजपा ने मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में सरकार बनायी थी। पर्रिकर के मार्च 2019 में निधन के बाद प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने।
चुनाव की तारीख़ें
उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को, दूसरे चरण का 14 फरवरी को, तीसरे चरण का 20 फरवरी को, चौथे चरण का 23 फरवरी को, पाँचवें चरण का 27 फरवरी को, छठे चरण का 3 मार्च को और सातवें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को और दूसरे चरण के लिए 3 मार्च को होगा। उत्तराखण्ड, पंजाब और गोवा में मतदान एक ही चरण में 14 फरवरी को होगा। सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किये जाएँगे।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा और राजनीति

‘अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक ज़िन्दा लौट पाया।‘ यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे, जो उन्होंने 5 जनवरी को बठिंडा हवाई अड्डे पर पंजाब पुलिस अधिकारियों से कहे। उस समय तक उनके हुसैनीवाला के पास लोगों के विरोध के चलते एक पुल (फ्लाईओवर) पर 15 मिनट तक फँसे रहने के मामले को सुरक्षा में लापरवाही ही माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब सरकार के अधिकारियों से ये शब्द कहे, ख़बरों की सुर्ख़ियाँ बन गये, और इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गयी। वैसे अब इस मामले की जाँच के सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त जज इन्दु मल्होत्रा के नेतृत्व में एक जाँच समिति को सौंप दिया है। इसमें राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के डीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की पंजाब यूनिट के एडिशनल डीजी भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी पुल पर तब फँसे, जब उन्होंने फ़िरोज़पुर में भाजपा की चुनाव रैली में अचानक सड़क मार्ग से जाने का फ़ैसला किया, जबकि पहले हवाई यात्रा से जाने की सरकारी स्तर पर जानकारी थी। प्रधानमंत्री की अधिकारियों से कही इस बात के बाद यह मामला पूरी तरह राजनीतिक हो गया। इसमें कोई दो-राय नहीं कि प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा अहम है और इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वैसे पुल पर जहाँ प्रधानमंत्री का क़ाफ़िला रुका, वहाँ से प्रदर्शनकारी काफ़ी दूर थे। लेकिन भाजपा के नेताओं का आरोप था कि प्रधानमंत्री का क़ाफ़िला जानबूझकर रुकवाया गया, ताकि उनकी सुरक्षा ख़तरे में डाली जा सके। एक-दो ने तो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी पर ही आरोप जड़ दिया। कुछ ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पास है, लिहाज़ा ऐसा किसी षड्यंत्र के तहत किया गया।
हालाँकि भाजपा नेताओं बयानों से साफ़ दिखा कि भाजपा इस मसले पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिन्ता कम और राजनीति ज़्यादा कर रही है। जिसे ही मामला सामने आया केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गम्भीर चूक बताते हुए पंजाब सरकार से इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की। मुख्यमंत्री चन्नी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे घटना की पूरी जानकारी ली और एक बयान दिया कि सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी चिन्ता करती है; लेकिन साथ ही यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का सड़क के रास्ते जाने का फ़ैसला अचानक आया। पंजाब सरकार ने भी मामले लिए एक समिति गठित कर दी। लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में दख़ल देते हुए ख़ुद की समिति बनाने का आदेश दिया।
इस सारे मामले को देखा जाए, तो इसमें सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल के गम्भीर क़िस्म के अभाव का पता चलता है। अति विशिष्ट व्यक्ति (वीवीआईपी) सुरक्षा के लिए जो एजेंसियाँ ज़िम्मेदार होती हैं, उनमें बहुत सघन समन्वय की ज़रूरत रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री के एक पुल पर फँसने पर यह समन्वय पूरी छिन्न-भिन्न दिखा।
इसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) ने वायुसेना एयरबेस की ओर लौटने का निर्णय किया। यह बहुत हैरानी की बात है कि देश में ऐसे मामलों में ज़िम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए कोई क़ानूनी प्रावधान नहीं है।
‘तहलका’ की जुटाई जानकारी के मुताबिक, एसपीजी अधिनियम में ऐसी चूक करने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान ही नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा ब्लू बुक (एसपीजी इसी के तहत काम करती है) से निर्धारित होती है। हाँ, यह ज़रूर कि प्रधानमंत्री के दौरों के दौरान सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रधानमंत्री को अचानक सड़क के रास्ते 100 किलोमीटर ले जाने का फ़ैसला ही ग़लत था। उनके सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार एसपीजी को ही ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े लोगों की यह भी बड़ी चूक थी कि दूसरी चूक उस उन्हें उस रास्ते से ले जाने का फ़ैसला किया गया, जिसमें एक ऐसा पुल था; जिसे प्रदर्शनकारियों ने बन्द किया हुआ था। नियमों के मुताबिक, प्रधानमंत्री के दौरों के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा लापरवाही आदि होने की सूरत में केंद्रीय गृह मंत्रालय दोषी / आरोपी कर्मियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सम्बन्धित राज्य (या यूटी) को एक परामर्श भेजता है। इसमें राज्य सरकार से दोषी/आरोपी अधिकारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश होती है। जब एसपीजी कर्मी लापरवाही का ज़िम्मेदार पाया जाता है, उसके ख़िलाफ़ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश के अलावा उसे उसके मूल संगठन में वापस भेजने का प्रावधान है।
सर्वोच्च न्यायालय की समिति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले में जाँच सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार की जाँच समितियों को नकारते हुए सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में समिति का गठन कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने इस समिति में डीजी एनआईए और आईबी के पंजाब के एडीजी शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद समिति के गठन निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान इस मामले में याचिकाकर्ता, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर एडवोकेट) भी हैं; ने रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद जतायी। इस पर प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा कि हमें रात 10 बजे कंप्लायंस (अनुपालन) रिपोर्ट मिली है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि तब हम इस पर परसों बहस कर सकते हैं। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया कि राज्य (पंजाब) के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) कहाँ हैं?
वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. पटवालिया ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल ने इन रिकॉड्र्स को रिकॉर्ड पर रख लिया है। जहाँ तक बात जज के ख़िलाफ़ आरोपों की है, तो सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले में ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है कि कुछ राजनीति हुई है। एसएसपी को सात कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि आख़िर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। मुझे पक्ष रखने का मौक़ा नहीं दिया गया। जब कार्यवाही रोक दी गयी, तो फिर ये कारण बताओ नोटिस कहाँ से आ गये।
मुझे तो केंद्र सरकार की जाँच समिति से न्याय नहीं मिलेगा। मामले की स्वतंत्र जाँच की ज़रूरत है। इस पर सीजेआई ने कहा कि कारण बताओ नोटिस में क्या लिखा है? पढि़ए। याचिकाकर्ता पटवालिया ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव के नाम जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि एसपीजी एक्ट के तहत दी गयी ज़िम्मेदारी का पहली नज़र में पालन होता नहीं दिखा है और बेरोक-टोक वीवीआईपी ट्रेवल की व्यवस्था नहीं की गयी। कारण बताओ नोटिस में हमारे ख़िलाफ़ हर चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि निष्पक्ष सुनवाई होगी। निष्पक्ष जाँच की ज़रूरत है।
केंद्र सरकार की तरफ़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पहले ये नोटिस जारी किये गये थे। हमें आपको वह क़ानून बताना है जिसके अन्दर नोटिस जारी किया गया था। देखिए यहाँ कुछ ग़लत फ़हमियाँ पैदा हुई हैं। कृपया एसपीजी एक्ट के तहत सुरक्षा की परिभाषा को देखिए। इसका मतलब है कि एसपीजी सिर्फ़ नज़दीकी सुरक्षा करेगा। अब बताइए कि डीजी की क्या भूमिका है। प्रोसीजर के लिए एक ब्लू बुक है।‘
एसजी ने कहा कि प्रधानमंत्री का क़ाफ़िला आन्दोलन स्थल से 100 मीटर दूर पहुँचा। ब्लू बुक के मुताबिक, अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वो नियमों का कड़ाई से पालन कराएँ और राज्य सरकार का दायित्व है कि वो अधिकारियों को निर्देश दे, ताकि कम-से-कम असुविधा हो। पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती करके भीड़ को पूरी तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए था।
प्रधानमंत्री के क़ाफ़िले को नहीं बताया गया कि मौक़े पर भीड़ इकट्ठी हो रही है। अगर ख़तरे की आशंका थी, तो प्रधानमंत्री को तुरन्त वहाँ से हटाया जाना चाहिए था। यह पूरी तरह इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला है। कुछ मामलों में डीजी और सीएस प्रधानमंत्री के साथ ट्रेवल करते हैं, ताकि कम्यूनिकेशन सिस्टम में कोई बाधा नहीं आये और सुनिश्चित किया जाता है कि सड़क पूरी तरह साफ़ हो। अगर सड़क कहीं भी जाम हो, तो गाडिय़ाँ 4-5 किमी पहले ही रोक दी जाती हैं। इतना तो तय है कि राज्य जिन मामलों में अपना बचाव कर रही है, वो काफ़ी गम्भीर हैं। केंद्र सरकार की जाँच समिति पता करेगी कि गड़बड़ी कहाँ हुई?
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हेलिकॉप्टर से नहीं, बल्कि गाडिय़ों से जाएँगे, यह फ़ैसला अचानक नहीं किया गया था। एसपीजी ने डीजीपी से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या रास्ता साफ़ है? ये सब बातें राज्य की पुलिस भी स्वीकार कर रही है। सुनवाई तो इस बात की हो रही है कि मामले में क्या अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए? इसके बाद पीठ में शामिल जज आपसे में बात करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत सॉलिसिटर जनरल से कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ़ से जारी कारण बताओ नोटिस अपने आम आदमी पार्टी में विरोधाभासी है। समिति गठित करके आप जाँच करवाना चाहते हैं कि क्या एसपीजी एक्ट का उल्लंघन हुआ है। दूसरी तरफ़ आप चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दोषी भी बता देते हैं। उन्हें किसने दोषी बताया?
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर आप पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो न्यायालय के लिए बचा क्या है? एसजी ने कहा कि इसमें पंजाब फ़ैसला नहीं ले सकता है। समिति के सदस्यों को जाँच करने दीजिए, जो तीन सप्ताह में रिपोर्ट देंगे। सीजेआई ने कहा कि अगर मुख्य मुद्दा किसी-न-किसी पर दोषारोपण करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? कृपया ऐसा दिखावा मत कीजिए, जैसे कि हम इस मामले में गम्भीर नहीं हैं। एसजी ने कहा कि मेरे पास एक सुझाव है। अगर न्यायालय को लगता है कि कारण बताओ नोटिस पूर्वाग्रहों पर आधारित हैं; तो केंद्र सरकार की जाँच समिति इसकी जाँच करेगी और न्यायालय को रिपोर्ट करेगी। तब तक नोटिस के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मुझे लगता है कि यह सही रहेगा। पटियावाला ने कहा कि स्वतंत्र जाँच समिति का गठन किया जाना चाहिए। मुझे केंद्र सरकार की जाँच समिति से कोई उम्मीद नहीं है। हम कौन-सा चेहरा लेकर उस समिति के सामने जाएँगे?
इसके बाद सीजेआई ने पीठ के साथी जजों के साथ बातचीत करने के बाद कहा कि एक सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज जाँच समिति की अगुवाई करेंगे। एनआईए के डीजी और पंजाब के एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका हिस्सा होंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय की बनायी समिति इस मामले की जाँच कर रही है।
चुनाव आयोग की पाबंदियाँ
चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए ये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इनके मुताबिक, 15 जनवरी तक कोई रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली नहीं होगी। कोई फिजिकल रैली नहीं होगी। रात
8:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक कोई पब्लिक मीटिंग या रैली नहीं होगी और ‘कैंपेन कफ्र्यू’ (अभियान निषेध) रहेगा। कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी। विजय रैली नहीं निकाली जाएगी। विजेता के साथ दो से ज़्यादा लोग प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) लेने के लिए निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के पास नहीं जा पाएँगे। सभी राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार वर्चुअल कैंपेन करेंगे। कोरोना दिशा-निर्देश का पालन करके ही मीटिंग कर पाएँगे। एसडीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार ही मीटिंग करनी होगी। इसमें मास्क और सैनिटाइजर का वितरण गेट पर ही करना होगा। घर-घर प्रचार के लिए अधिकतम 5 लोग ही जा पाएँगे। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को सुविधा ऐप पर शपथ पत्र देना होगा कि वे सभी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। कोरोना दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना दिशा-निर्देश का उल्लंघन हुआ, तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की रैलियों को रद्द कर सकता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखण्ड में प्रत्याशी-ख़र्च की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये और मणिपुर और गोवा में 28 लाख रुपये कर दी गयी है।
उत्तर प्रदेशकुल सीटें : 403
कुल मतदाता : 15,02,84,005
पुरुष : 8,04,52,736
महिला : 6,98,22,416
थर्ड जेंडर : 8,853
नये मतदाता : 52,80,882
पुराने नाम हटे : 21.40 लाख
मतदान केंद्र : 1,74,351
पंजाबकुल सीटें : 117
कुल मतदाता : 2,12,75,066
पुरुष : 1,11,87,857
महिलाएँ : 1,00,86,514
मतदाता (अन्य) : 695
80 वर्ष से अधिक : 5,13,229
दिव्यांग : 1,44,667
सेवा मतदाता : 1,10,163
एनआरआई : 1,601
मतदान केंद्र : 24,689
उत्तराखण्डकुल सीटें : 70
कुल मतदाता : 81,43,922
पुरुष : 42,24,288
महिला : 39,19,334
80 प्लस : 1,58,742
दिव्यांग मतदाता : 68,478
सेवा मतदाता : 94,265
मतदान केंद्र : 11,647