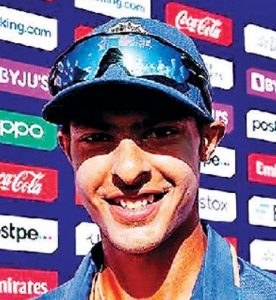लता मंगेशकर पहला गाना मराठी फ़िल्म ‘चिमुकला संसार’ में गाया था- ‘मी म्हणेन तुजला दादा दादुटल्या’। मास्टर विनायक द्वारा निर्मित इस फ़िल्म का निर्देशन वसंत जोगळेकर ने किया था। इस फ़िल्म में लता मंगेशकर ने अभिनेता मास्टर विनायक की छोटी बहन का किरदार भी निभाया था। इसके बाद वसंत जोगळेकर ने ‘किती हसाल’ नामक फ़िल्म में भी लता को मौक़ा दिया। जब वसंत जोगळेकर ने फ़िल्म ‘आप की सेवा में’ बनायी, तो लता को भी पहली मर्तबा हिन्दी फ़िल्म उद्योग में मौक़ा मिला। इससे पहले उन्होंने मंगळागौर, माझं बाळ आणि गजाभाऊ नामक फ़िल्मों में अपनी इच्छा के विरुद्ध अभिनय भी किया। बोनी कपूर की एक फ़िल्म में भी उनके अभिनय की झलक कुछ ही लोगों को पता होगी। लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि एक दिन लता को सरस्वती का अवतार भी कहा जाएगा।
सूरों की सरिता लता मंगेशकर के निधन की ख़बर जैसे ही देश-दुनिया में फैली, लोगों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। फ़िल्म जगत में हलचल-सी मच गयी और बड़े-बड़े सितारों का उनके अन्तिम दर्शन के आना शुरू हो गया। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेशों की सरकारों, महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी का शोक सन्देश मंगेशकर परीवार को दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि लता मंगेशकर का स्मारक अच्छी गुणवत्ता वाला, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुम्बई के ही दादर के शिवाजी पार्क में होना चाहिए। ताकि देश-दुनिया की जनता याद रखे। उनकी अन्तिम यात्रा में न केवल अभिनेत्री-अभिनेता, राजनेता मौज़ूद रहे, बल्कि आम जनमानस ने भी उन्हें एक झलक देख लेने की कोशिश की। लता दीदी को अपनी अन्तिम यात्रा के दौरान भी महाराष्ट्र राज्य की संस्कृति और परम्परा अलविदा कहने में सफल रही।
लता मंगेशकर की आवाज़ का कौन $कायल नहीं रहा, यही वजह है कि उन्हें फ़िल्म के सर्वोच्च पुरस्कारों समेत भारत के तीन सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। एच.एम. व्ही ने महाराष्ट्र के मशहूर मराठी गाने के सम्राट, $कव्वाल स्वर्गीय प्रह्लाद शिंदे को लेकर एल्बम निकालने की सोची। लेकिन प्रह्लाद शिंदे का सादा रहन-सहन देखकर लता मंगेशकर ने एच.एम. व्ही को इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं, जिन बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को हक़ दिलाने वाला हिन्दू कोड बिल नामंजूर किये जाने पर केंद्रीय क़ानून मंत्री पद से इस्तीफ़ा तक दे दिया, उनके ऊपर भी लता मंगेशकर ने गाना गाने से साफ़ इन्कार कर दिया था। जबकि उनसे उस महान् शख़्सियत पर गाना गाने के लिए मुँह माँगे पैसों का ऑफर किया गया और विनती भी की गयी; लेकिन लता फिर भी नहीं मानीं।
महिलाओं को सम्मान के लिए लडऩे वाले और उन्हें कई हक़ दिलाने वाले बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पर एक गाना तो लता मंगेशकर को गाना चाहिए था। यदि बाबा साहेब पर लिखे गाने को स्वर कोकिला ने सुर दिया होता, तो न तो उनका गला ख़राब हो जाता और न ही वह अस्पृश्य हो जातीं। लता मंगेशकर ने ‘काँटा लगा’ से लेकर ‘शाक धुमधुम’ जैसे हज़ारों गाने गाये; लेकिन बाबा साहेब पर लिखा गाना गाने की कभी हामी नहीं भरी। जबकि कहा जाता है कि एक कलाकार की कला के आलावा कोई जाति नहीं होती। इसमें कोई दो-राय नहीं कि हम स्वर साधना की देवी लता मंगेशकर के हमेशा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने देश को एक-से-एक ख़ूबसूरत गाने को अपने स्वरों से नवाज़। लेकिन उनका जीवन कई विवादों से भी घिरा रहा, जिसमें एक विवाद उनकी सोच का मनुवादी होने को लेकर भी था। इसी सोच के चलते उनकी अपने समय के गायकों से भी कुछ अनबन रही। ओ.पी. नैय्यर ने कहा था कि मुझे लगता है कि लता मंगेशकर बहुत अच्छी गायिका हैं। उसकी आवाज़ बहुत पतली है। लेकिन वह मेरे द्वारा रचित गीत भी नहीं गा सकतीं। मेरे प्रतिबन्ध बहुत कठिन हैं, जिससे गायकों का दम घुटता है। और लता ये कठिन टोटके नहीं गा पाएँगी। वह मेरे लेखन की गायिका नहीं हैं।
हम सभी की प्रिय लता दीदी को ईश्वर का बुलावा आया और वह हमारे बीच से चली गयीं। लेकिन उनकी जादुई आवाज़ हमारे कानों में मिठास घोलती रहेगी। हालाँकि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि सामाजिक भेदभावों से पहले संवेदनशीलता की नज़र रखना हम सबका परम् कर्तव्य है। क्योंकि सामाजिक भेदभावों का मैल मन में रखने वाले शाहरूख़ ख़ान की दुआ को भी थूकना साबित करने की कोशिश करते हैं। फिर जिन लोगों का मर्तबा ऊँचा हो और जिन्होंने समाज के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया हो, उनसे भेदभाव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। लता मंगेशकर को मैं पूरे देश की तरफ़ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।