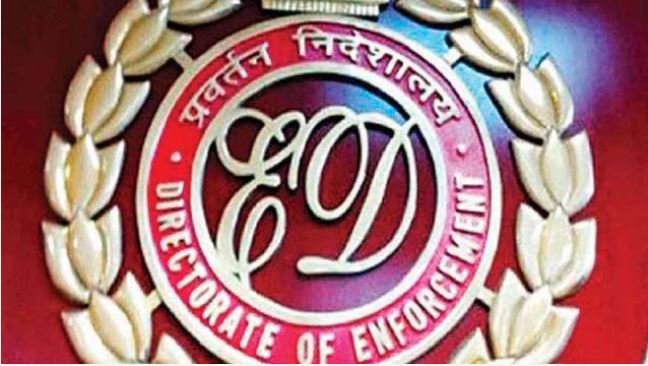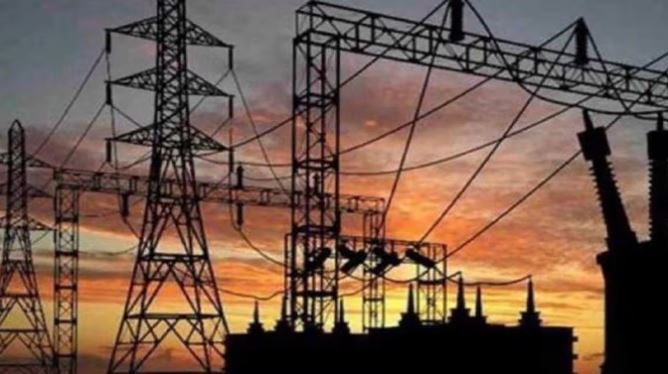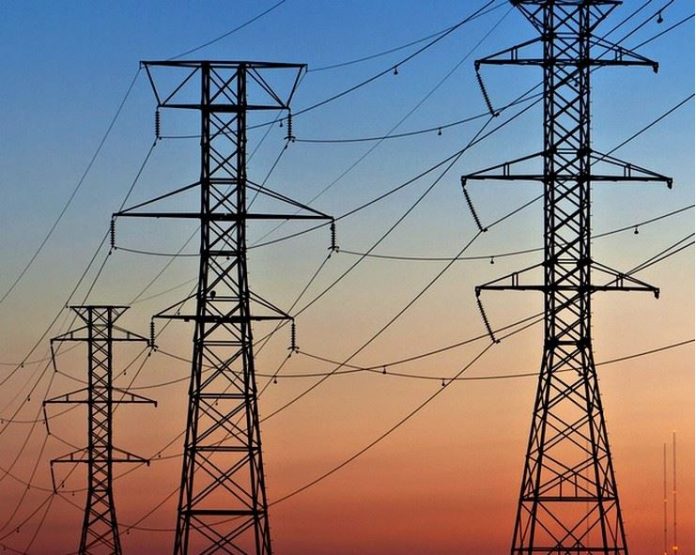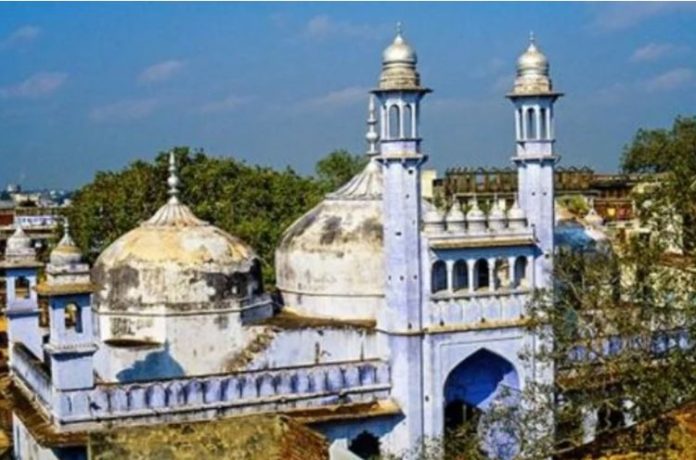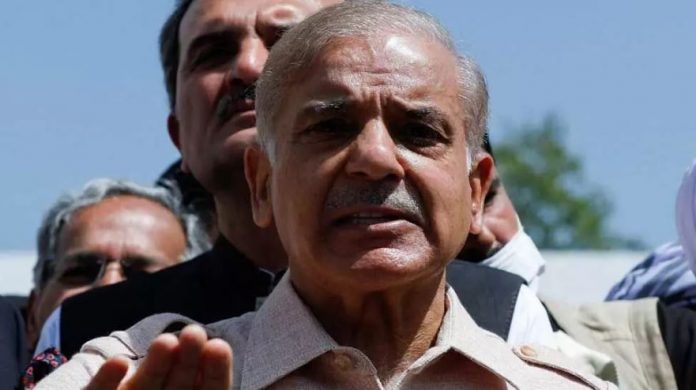प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई में शियोमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5551.27 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ईडी ने यह कार्रवाई फेमा के तहत की है। ईडी ने फरवरी में कंपनी के कथित अवैध लेनदेन को लेकर जांच शुरू की थी।
जानकारी के मुताबिक शियोमी इंडिया चीन स्थित शियोमी ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह राशि कंपनी के बैंक खातों से जब्त की गई है। याद रहे प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी में कंपनी के कथित अवैध लेनदेन को लेकर जांच शुरू की थी।
बता दें शियोमी ने 2014 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया था और 2015 से पैसा भेजना शुरू कर दिया। ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने तीन विदेशी संस्थाओं को 5551.27 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी। इसमें रॉयल्टी की आड़ में एक शियोमी ग्रुप की कंपनी शामिल है। आरोप के मुताबिक रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम उनके चीनी मूल समूह की संस्थाओं के आदेश पर भेजी गई।
अमेरिका की दो संस्थाओं, जो इससे संबंधित ही नहीं थीं, उनको भी पैसा भेजा गया। आरोप है कि शियोमी ग्रुप की संस्थाओं को ही इसका फायदा भी। शियोमी इंडिया एमआई ब्रांड के तहत भारत में मोबाइल फोन कारोबार करती है।