
2011 की एक पंजाबी फिल्म है ‘अन्हे घोड़े दा दान’. गुरदयाल सिंह के लिखे एक उपन्यास पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन गुरविंदर सिंह ने किया था. इस फिल्म में पंजाब के दलित वर्ग की बेबसी को बड़ी ही संजीदगी और धीरज के साथ दिखाया गया है.
तीन साल पहले की इस फिल्म का ज़िक्र यहां इसलिए क्योंकि हरियाणा के भगाणा गांव के दलित परिवारों से बात करते वक्त उस फिल्म के कई सीन आंखों के सामने दौड़ जाते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे वही फिल्म दोबारा देख रहे हैं.
हरियाणा के हिसार जिले से आधे घंटे की दूरी पर भगाणा गांव है. काफी लंबे समय से इस गांव के जाटों ने खाप पंचायत के साथ मिलकर दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर रखा है. पिछले दिनों इस बहिष्कार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा भयानक रूप लिया जिसने गांव के दलित परिवारों की चार लड़कियों को मुंह ढंककर दिल्ली के जंतर-मंतर पर डेरा डालने को मजबूर कर दिया. 13 से 18 साल की उम्र की इन चार मासूम जिंदगियों का साथ गांव के करीब 100 से भी ज्यादा दलित दे रहे हैं. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.
यहां ‘धरना’ शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से इस अलफाज की गंभीरता कम होती जा रही है. शायद इसीलिए भगाणा के इन दलितों की भी कोई सुनवाई नहीं है. चंद अखबारों को छोड़कर ज्यादातर मीडिया ने इनकी तरफ ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा है. शायद उनकी नजर में यह भी जंतर मंतर पर दिया जाने वाला ‘बस-एक-और-धरना’ है. ऊपर से यह चुनाव का मौसम भी है. ‘हर हाथ शक्ति’ और ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ जैसे सुखद नारों के बीच ऐसी किसी बुरी खबर से क्यों जायका बिगाड़ा जाए?
खैर, पूरा मामला यह है कि 23 मार्च की शाम सात बजे, भगाणा गांव के अलग-अलग दलित परिवारों की चार लड़कियां, शौच के लिए घर से बाहर खेतों की तरफ निकली थीं. इन चारों की उम्र 13 से 18 साल के बीच है. जब काफी देर तक लड़कियां घर वापिस नहीं लौटीं तो परिवार वालों ने उन्हें ढूंढना शुरु किया. अगले दिन मदद के लिए सरपंच का दरवाजा खटखटाया गया लेकिन वहां से भी किसी तरह की सहायता न मिलने के बाद ये लोग हताश होकर वापस लौट गए. थोड़ी ही देर बाद सरपंच का संदेश आया कि इन परिवारों की बेटियां मिल गई हैं और वे सभी भंटिडा में हैं.
24 मार्च की शाम को भटिंडा में अपने परिवार से मिलने के बाद इन लड़कियों ने जो जानकारी दी उसने सबको हिला कर रख दिया. लड़कियों ने बताया कि उन्हें एक सफेद गाड़ी में उठा लिया गया था और फिर उनके साथ 12 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया. इन लड़कियों पर सच न बोलने का काफी दबाव था लेकिन मामले को सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगी. जानकारी के मुताबिक डॉक्टरी जांच में दो लड़कियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है लेकिन परिजनों का कहना है कि चारों में से किसी को भी नहीं छोड़ा गया. 25 मार्च को सुबह एफआईआर की गई लेकिन केवल पांच ही लोग गिरफ्तार हुए हैं. पीड़ित लड़कियों के परिजनों का आरोप है कि इस काम में सरपंच की मिलीभगत है और जो सात आरोपी फिलहाल बाहर हैं उनमें सरपंच राकेश और उसका चाचा भी शामिल है. लड़कियों के परिवार वालों का कहना है कि जहां सारी रात दौड़-भाग करने के बाद भी उन्हें अपनी बेटियों का पता नहीं चल पाया, वहीं सरपंच ने थोड़ी ही देर में कैसे लड़कियों के ठिकाने का पता लगा लिया.
यही हमारा घर है
भगाणा के जाटों ने दलितों का हुक्का पानी पहले से ही बंद कर रखा है. इस गांव के 135 दलित और पिछड़े परिवार, पिछले दो सालों से अपने बच्चों, महिलाओं और जानवरों के साथ हिसार के मिनी सचिवालय में खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं. गांव की जिन लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, वो धानक (अनुसूचित जाति ) जाति की हैं. पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स संस्था ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार धानक जाति, दलितों में भी बेहद कमजोर मानी जाती है. दो साल पहले जब जाटों ने गांव में हुए एक विवाद के चलते दलितों का बहिष्कार किया था तब चमार, कुम्हार, खाती जैसी अपेक्षाकृत मजबूत जाति के लोग, हिसार में धरने पर बैठ गए थे. लेकिन धानक जाति के परिवारों ने बहिष्कार के बावूजद गांव में ही रहने का फैसला किया था. इस सामूहिक बलात्कार को धानक जाति के उसी निडर कदम की सजा के रूप में भी कुछ लोग देख रहे हैं.
अब एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत दिखाकर और पांच लोगों को सलाखों के पीछे भेजकर, इन लोगों के लिए गांव में ठहरना अपनी जान को खतरे में डालने से कम नहीं. इसलिए 15 दिनों तक हिसार में डेरा डालने के बाद और हरियाणा सरकार से नाउम्मीदी मिलने के बाद, इन लोगों ने 16 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय की गुहार लगानी शुरु कर दी. लेकिन क्या इंसाफ मिलना इतना आसान है? जब ये सवाल बलात्कार की शिकार कुसुम (नाम बदला हुआ) की मां से पूछा गया तो जवाब था – ‘अगर निर्भया को न्याय मिल सकता है, तो हमारी बच्चियों को क्यों नहीं? फर्क बस इतना है कि वो मर गई और हमारी बच्चियों को तो इन पैसे वालों ने जीते जी मार डाला.’ इस बीच वे चारों लड़कियां मुंह ढककर तंबू के एक तरफ सो रही हैं.
वहीं तंबू के दूसरी और कुछ लोग ताश खेलकर वक्त गुजार रहे हैं. वैसे भी एक-दो दिन की बात हो तो समझ में आता है. यहां तो इंतजार लंबा नहीं बहुत लंबा है. ऐसे में अपने घर से दूर किसी टैंट के नीचे समय बिताना आसान बात नहीं है. हिम्मत कभी भी ‘इंसाफ’ और ‘जंग’ जैसे भारी शब्दों का साथ छोड़कर भाग सकती है.
और हां, एक छोटी सी बच्ची किरण भी है जो हर नए आने वाले के साथ दोस्ती गांठ रही है. जब उससे घर लौटने के बारे में पूछते हैं तो वह कहती है – अब यही हमारा घर है.

फोटोः विजय पांडे
सोनिया गांधी कब आएंगी?
कड़ी धूप में जंतर मंतर पर बजने वाले लाउड स्पीकरों के शोर के बीच उन चार लड़कियों में से एक शशि (नाम बदला हुआ) के पिता विजेंद्र बड़ी मासूमियत से मुझसे एक सवाल पूछते हैं ‘ये सोनिया गांधी कब आने वाली हैं? मैं पूछती हूं, ‘कहां?’ ‘अरे वो बाहर गई हुई हैं ना…वो और राहुल गांधी दिल्ली कब वापिस आएंगे? एक बार बस उनसे मिलना हो जाए.’
उनसे मिलकर क्या कहेंगे पूछने पर विजेंद्र कहते हैं ‘हम बस न्याय चाहते हैं. हमारी बस दो ही मांग हैं. सरपंच और बाकी बचे लोगों को गिरफ्तार करो और हमारे लिए कोई और ठिकाने का इंतजाम कर दो. हम वापिस गांव नहीं लौटना चाहते. क्या मुंह लेकर जाएंगे. इज्जत तो चली ही गई है. वहां लौटेंगे तो जो बची-खुची जान है उसे भी वो लोग ले लेंगे.’
‘लेकिन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद तो गांव लौटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए?’
इस पर विजेंद्र का जवाब आता है, ‘वो लोग पैसे वाले हैं. जेल से छूटना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है. उसके बाद हमारा क्या होगा ? और कितना डर-डर के जिएंगे? हरियाणा की सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है. वो तो जाटों का ही साथ देती आ रही है. इसलिए हम यहां आए हैं. केंद्र सरकार से गुहार लगाने.’
बंदूक से पेट नहीं भरता
इंसाफ की इस लड़ाई में पेट के चूहे साथ नहीं देते. लड़ाई लड़ने के लिए पेट भरा होना जरुरी है. इन लोगों के लिए खाने का प्रबंध सर्वसमाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष और बसपा नेता वेदपाल तंवर ने किया है. विजेंद्र का कहना है कि सर्वसमाज संघर्ष समिति और वेदपाल की बदौलत ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी.
वेदपाल सिर्फ भगाणा ही नहीं, मिर्चपुर गांव के सामाजिक बहिष्कार के शिकार दलित परिवारों का भी साथ दे रहे हैं. 2010 में हिसार जिले के ही मिर्चपुर गांव में एक सत्तर साल के दलित और उसकी एक विकलांग बेटी को जिंदा जला दिया गया था. यही नहीं, यहां के अन्य 18 दलितों के घरों को भी फूंक डाला गया था. इस घटना के बाद करीब 100 से भी ज्यादा दलित परिवार मिर्चुपर छोड़कर भाग गए थे. वे सभी पिछले चार सालों से वेदपाल तंवर के हिसार स्थित फॉर्महाउस में ठहरे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा सरकार ने मिर्चपर के इन दलितों की सुरक्षा में कुछ कदम तो उठाए हैं लेकिन इससे इन खानाबदोशों के पुनर्वास का मसला अभी भी हल नहीं हो पाया है.
भगाणा के दलितों के पुनर्वास की संभावनाओं के बारे में वेदपाल मिर्चपुर मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के उस वक्तव्य का जिक्र करते हैं जिसमें कहा गया था कि पेट, बंदूक से नहीं भरता. पुनर्वास जरूरी है. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की इस डांट पर अमल करने के लिए सबसे जरूरी है इच्छाशक्ति जो मिर्चपुर और भगाणा जैसे मामलों में नदारद दिखती है.
मैं भी दलित हूं
भगाणा के इन दलितों के लिए किसी के पास वक्त नहीं है इसलिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने इनकी बात आगे तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है. ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम (एआईबीएसएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतेंद्र यादव बताते हैं कि सदर हिसार के थाना अध्यक्ष ने एफआईआर में से कुछ लोगों के नाम हटा दिए थे इसलिए इनके फोरम की मांग है कि अनुसूचित जाति आयोग, लड़कियों के बयान लेकर मामले की दोबारा जांच करवाए और बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए. जीतेंद्र का यह भी कहना है कि जिस तरह के सामाजिक बहिष्कार को ये दलित परिवार अपने गांव में झेल रहे हैं- जैसे, कुएं से पानी निकलाने की मनाही, दुकान से सामान खरीदने की मनाही, जाटों के खेत में काम करने की मनाही, यहां तक की उनकी बहन-बेटियां भी वहां सुरक्षित नहीं हैं ऐसे में इनका भगाणा में लौटना कहां की समझदारी होगी.
इस मामले में तहलका ने जब अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ईश्वर सिंह से संपर्क किया तो उनका कहना था कि घटना के अगले दिन ही एसपी और दो डीएसपी को समन भेजकर पूरी रिपोर्ट मंगवाई गई थी. डॉक्टरी जांच में केवल दो लड़कियों के बलात्कार की पुष्टि हुई है जिन्हें एक लाख बीस हजार का कुल मुआवजा भी हाथों-हाथ दे दिया गया था. इसके बाद जंतर-मंतर आने का औचित्य समझ के बाहर है.
ईश्वर सिंह के मुताबिक इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है और पुनर्वास और बलात्कार का मामला दो अलग-अलग मसले हैं. इन्हें जोड़कर न देखा जाए. वहीं एआईबीएसएफ के अध्यक्ष जीतेंद्र यादव ऐसा मानने से इंकार करते हैं. उनका कहना है कि लड़कियों के साथ हुआ बलात्कार, भगाणा के दलितों को गांव से निकाल बाहर करने और उन्हें सबक सिखाने की मंशा से ही किया गया है इसलिए दोनों बातों को अलग-अलग करके देखना, मामले में आयोग की बेरूखी का सबूत है.
27 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, इन चार पीड़ित लड़कियों और उनके परिवार के साथ केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के घर का घेराव करने पहुंचे जहां काफी इंतजार के बाद कुछ लोगों को गृहमंत्री से मिलने का मौका मिला. उन्हें आश्वासन दिया गया कि चिट्ठी लिखकर हरियाणा सरकार से जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की जाएगी. गृहमंत्री ने कहा कि वे खुद भी दलित हैं और इस दर्द को समझते हैं. लेकिन ये मामला राज्य सरकार का है और केंद्र सरकार इसमें ज्यादा दखलअंदाजी नहीं कर सकती. 2012 में केंद्रीय गृहमंत्री का पद हासिल करने के बाद सुशील कुमार शिंदे ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने एक ‘दलित’ को गृहमंत्रालय जैसी गंभीर जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हीं ‘दलित’ गृहमंत्री के टूटे-फूटे आश्वासन के साथ ही भगाणा का यह काफिला वापिस जंतर मंतर के अपने डेरे पर लौट आता है और वे चारों लड़कियां एक बार फिर अपने ढके हुए मुंह को और अच्छे से ढककर सोने की तैयारी करने लगती हैं.
फिलहाल इन परिवारों का वर्तमान और भविष्य अधर में है. अगर नेताओं और आयोग के दिलासे के साथ ये गांव लौट भी जाएं तो इनका हाल क्या होगा किसी से छुपा नहीं है. अगर यह भी मान लिया जाए कि केवल दो लड़कियों के साथ ही बलात्कार हुआ है और दिए गए एक लाख बीस हजार के मुआवजे के साथ इन्हें गांव लौट जाना चाहिए, तब भी इनकी सही-सलामती की गारंटी कौन लेता है? ऐसे में कोई सही राहत नहीं मिलने पर सड़कों पर रहना इनकी मजबूरी हो जाती है.

न्याय दो या प्राण लो
इतिहासविद रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ (गांधी के बाद का भारत) में 1949 की एक घटना का जिक्र किया है जिसमें दिल्ली के आसपास के गांव में बसे दलितों को जाटों ने इसलिए निकाल बाहर कर दिया था क्योंकि कल तक जो उनके जानवरों को चराते थे, आजादी के बाद उनमें बराबर खड़े होकर वोट डालने की हिम्मत आ गई थी. विरोध में गांव के दलितों ने दिल्ली के महात्मा गांधी स्मारक पर भूख हड़ताल की थी और कई गांधीवादी नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था.
लेकिन उस वक्त आजादी नई-नई मिली थी इसलिए जोश भी नया था. यह 2014 है. इस वक्त नेताओं का ध्यान चुनाव में लगा हुआ है. दूसरी तरफ क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ आईपीएल चल रहा है और ये दोनों काफी नहीं थे कि बॉलीवुड के आयफा अवार्ड्स को भी अभी ही शुरु होना था. मीडिया इन सबको कवर करने में मसरूफ है. इतने जरूरी कार्यक्रमों के बीच में इन बेसहारा दलितों की सुनवाई के लिए फुर्सत किसे है.
जंतर मंतर पर शाम का समय है. विजेंद्र टैंट के बाहर लगे एक बोर्ड को बड़ी तन्मयता के साथ ठीक करने में लगे हैं. ऐसे कि जैसे वह बोर्ड अगर थोड़ी देर के लिए भी दिल्ली की नजरों से ओझल हुआ तो उनकी बात नहीं बन पाएगी. बोर्ड पर लिखा है – न्याय दो या प्राण लो.






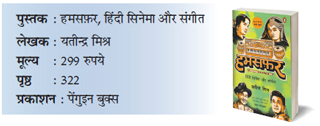 प्रदीप जी एक गाना लिखकर लाए, ‘धीरे-धीरे आ रे बादल, धीरे-धीरे जा/ मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा.’ यह सात मात्रा का गाना था और कहानी की जो सिचुएशन थी उसमें सात मात्रा का गाना अनुकूल नहीं बैठता था. वहां तो एक तरह की लोरी चाहिए थी, साथ ही प्रेम का भाव चाहिए था- यानी दोनों का मिला-जुला रूप और वह तभी हो सकता था, जब गाना आठ मात्रा का हो. मैंने सोचा कि इसमें क्या! किसी एक नोट पर खड़ा हो जाऊंगा, किसी एक सुर पर, तो एक मात्रा मिल जाएगी. इस तरह मैंने सात मात्रा के गाने को आठ मात्रा का बना दिया. प्रदीप जी सुनकर खुद हैरान रह गए थे. प्रदीप जी आखिर कवि थे और साथ ही एक अच्छे गायक भी. इस गाने की कंपोजीशन सुनकर वह मेरे दोस्त बन गए. उनका कहना था कि इस गाने में ऐसा चमत्कार अनिल विश्वास के अलावा और कोई पैदा नहीं कर सकता था. कुछ साल पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, तो वहां उन्होंने स्वीकार किया था, सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी कि अनिल विश्वास को नीचा दिखाने में मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी. मैंने इन्हें सात मात्रा का गाना बनाकर दिया, लेकिन इन्होंने उसे आठ मात्रा का बना दिया. बस, तभी से मैं इनका मुरीद हो गया.
प्रदीप जी एक गाना लिखकर लाए, ‘धीरे-धीरे आ रे बादल, धीरे-धीरे जा/ मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा.’ यह सात मात्रा का गाना था और कहानी की जो सिचुएशन थी उसमें सात मात्रा का गाना अनुकूल नहीं बैठता था. वहां तो एक तरह की लोरी चाहिए थी, साथ ही प्रेम का भाव चाहिए था- यानी दोनों का मिला-जुला रूप और वह तभी हो सकता था, जब गाना आठ मात्रा का हो. मैंने सोचा कि इसमें क्या! किसी एक नोट पर खड़ा हो जाऊंगा, किसी एक सुर पर, तो एक मात्रा मिल जाएगी. इस तरह मैंने सात मात्रा के गाने को आठ मात्रा का बना दिया. प्रदीप जी सुनकर खुद हैरान रह गए थे. प्रदीप जी आखिर कवि थे और साथ ही एक अच्छे गायक भी. इस गाने की कंपोजीशन सुनकर वह मेरे दोस्त बन गए. उनका कहना था कि इस गाने में ऐसा चमत्कार अनिल विश्वास के अलावा और कोई पैदा नहीं कर सकता था. कुछ साल पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, तो वहां उन्होंने स्वीकार किया था, सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी कि अनिल विश्वास को नीचा दिखाने में मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी. मैंने इन्हें सात मात्रा का गाना बनाकर दिया, लेकिन इन्होंने उसे आठ मात्रा का बना दिया. बस, तभी से मैं इनका मुरीद हो गया.








