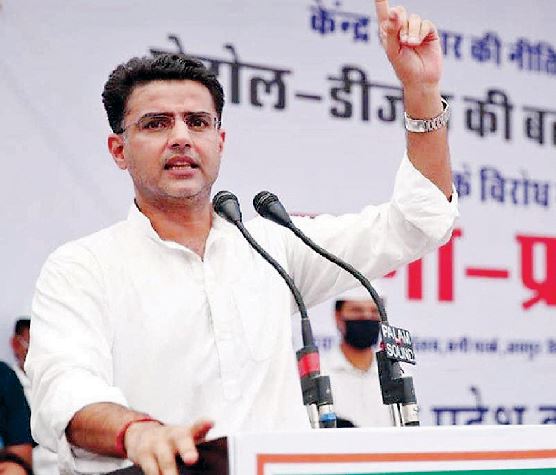पिछले कुछ साल से महँगाई लगातार बढ़ रही है। मुझे याद है, जब नोटबन्दी हुई थी, तो मेरे पास घर के ख़र्चे से बमुश्किल बचाये हुए सात हज़ार रुपये थे, जो कि बड़ी मुश्किल से मैंने और मेरे बेटे ने आधे-आधे बाँटकर बैंक से बदलवाये। तब रसोई गैस का सिलेंडर यही कोई 424-25 रुपये का था, जिसमें कि सब्सिडी भी मिलती थी। अभी वही सिलेंडर लगभग 850 रुपये का हो चुका है, जिसमें एक रुपये की भी सब्सिडी नहीं है। मेरा सरकार से सवाल है कि आख़िर रसोई गैस पर इतनी महँगाई करके पैसा कौन खा रहा है? कौन हम ग़रीबों की सब्सिडी खा रहा है? पिछले पाँच-छ: साल से लगातार बढ़ती महँगाई ने घर-गृहस्थी चलाना मुश्किल कर दिया है। मेरी कमायी घटी है। बीच में नौकरी भी चली गयी थी। मगर ख़र्चे बढ़े हैं। क्या ये मंत्री लोग या ख़ुद प्रधानमंत्री कड़ी मेहनत करके, 12 घण्टे गर्मी में काम करके किराये के मकान में रहकर 10 हज़ार रुपये में दो बच्चों को पालकर गुज़ारा कर सकते हैं? क्यों नहीं समझते नेता और क्यों नहीं समझतीं सरकारें आम आदमी की मजबूरी और परेशानी को? हमने सरकार का क्या बिगाड़ा है? सरकार क्यों हम ग़रीबों को मारना चाहती है? हम लोग मेहनतकश हैं। कोई चोरी नहीं करते। न किसी को लूटते हैं। न झूठ बोलते हैं। न किसी की बेईमानी करते हैं। न मुफ़्त का खाते हैं। एक-एक पैसा कड़ी मेहनत से पेट काटकर जोड़ते हैं, फिर भी हम पर अत्याचार क्यों? क्या सरकार लोगों को महँगाई के ख़िलाफ़ भी सड़कों पर उतारना चाहती है? आलू, प्याज, टमाटर समेत लगभग सभी सब्ज़ियों के दाम आसमान पर चढ़े रहते हैं। रसोई गैस के दाम आसमान पर हैं। दूध और महँगा हो गया। आटा, दाल, मैदा, बेसन, दलिया, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ महँगा होता जा रहा है। कमरे के किराये में आधी कमायी चली जाती है। ऐसे में ग़रीब आदमी क्या करे? क्या हम ग़रीबों को जीने का हक़ नहीं है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या सरकार के पास हम ग़रीबों के बारे में सोचने का वक़्त नहीं है? अगर सरकार आम लोगों की तरफ़ ध्यान नहीं देगी, तो उसे कोरोना महामारी से ज़्यादा महँगाई मार देगी। बच्चों का भविष्य बनाना मुश्किल हो जाएगा, जिसके चलते ज़िन्दगी भी नर्क हो जाएगी।
रुख़साना, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली
सेवा नहीं रही राजनीति
जब कोई नेता यह कहता है कि वह राजनीति में सेवा के लिए आया है या यह कहता है कि वह जनसेवक है, तो मुझे बहुत ग़ुस्सा आता है। आज की राजनीति में 98 फ़ीसदी लोग अपना स्वार्थ साधते हैं, जनता का हक़ मारते हैं और मुफ़्तख़ोरी करते हैं। क्या ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? ऐसे लोगों को हर हाल में जेल में ही होना चाहिए। अब नेताओं में ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं रह गयी है। अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहे भी, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। बिहार में पप्पू यादव की क्या ग़लती थी? यही न कि उन्होंने रुद्र प्रताप सिंह रूढ़ी की एम्बुलेंस छिपाने की पोल खोली थी। मैं बिहार के ऐसे लोगों से तो सवाल पूछ ही सकता हूँ, जिन्होंने पप्पू यूदव से हमेशा मदद ली कि क्या उनकी आत्मा सोयी हुई है, जो सरकार के इस रवैये का विरोध नहीं कर सकते? इसी तरह दिल्ली में सुनने में आता है कि वहाँ एक ईमानदार मुख्यमंत्री को भी तंग किया जाता है। यह कितना ग़लत है कि एक घोटालेबाज़ की इज़्ज़त होती है और ईमानदार नेताओं को परेशान किया जाता है। आज आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को चुनाव ही नहीं लडऩे देना चाहिए।
कमलेश कुमार, पटना, बिहार
हमें बख़्श दो सरकार
बहुत दिनों से मन में एक दर्द-सा उठ रहा है, जिसे अब बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन-सा हो गया है। यह दर्द राष्ट्र और राष्ट्रीयों की बर्बादी का है, जो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरी दुनिया अब हम पर हँस रही है। आर्थिक रूप से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। महामारी पर सरकारी असफलता को ‘धन्यवाद मोदी जी’ के पोस्टरों-बैनरों से उत्सव में बदलने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी कोरोना को हमने ताली-थाली बजाकर उत्सव के रूप में मनाया, बड़े बहुमत से उन्हें सत्ता दी। लेकिन न तो इससे सत्ताधारी पार्टी का पेट भरा, न मंत्रियों का ही भरा है। दोनों ही राष्ट्र और राष्ट्रीयों की बर्बादी और महामारी से लोगों के मरने के दौरान भी हम सबसे ‘वाह, मोदी जी! वाह’ की बुलंद आवाज़ सुनना चाहते हैं। उन्हें यह आवाज़ भी मरी हुई नहीं, बल्कि जोशीली और स्वर्गिक अहसास वाली सुनायी देनी चाहिए। चाहे किसान मरे, चाहे मज़दूर मरे, चाहे कोई और मरे। लेकिन सिर्फ़ वाहवाही होनी चाहिए; उनकी सरकार की और उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री की। आलोचना की, तो जेल होगी; फाँसी होगी। मर तो गये लाखों लोग। अरे अब क्या सबकी जान लोगे? हमें बख़्श दो सरकार!
कुम्भाराम भामी, चूरू, राजस्थान
जबरन बीमा क्यों?
अभी कुछ दिन पहले मेरे खाते से 330 रुपये काट लिये गये। मेरे बैंक अकाउंट में कुल 500 रुपये पड़े थे, जो कि पहले ही बैंक अकाउंट खुलवाने की राशि 2000 से कम थे। पिछले कई महीनों से नौकरी छूट जाने के कारण अब बैंक अकाउंट में मैं पैसा नहीं डाल पाता। इसलिए परेशानी के समय में जब बहुत ज़रूरत पड़ी, तो अकाउंट में रखी जाने वाली न्यूनतम राशि में से भी 1500 रुपये निकालने पड़े। लेकिन अभी हाल में जब मैंने बैंक अकाउंट की जाँच की, तो उसमें 250 रुपये के आसपास ही रुपये थे। जब बैंक में पता किया, तो पता चला कि 330 रुपये एक साल की एलआईसी पॉलिसी के काटे गये हैं। मैंने जब बैंक वालों से कहा कि मैंने तो कोई बीमा नहीं कराया। तो जवाब मिला कि यह तो सरकार की तरफ़ से आदेश है, लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? बीमा जैसी गुज़ारिश की चीज़ भी जबरन क्यों? क्या सरकार जानती है कि परेशानी में ग़रीबों के लिए 330 रुपये कितने होते हैं?
दिनेश, नोएडा, उत्तर प्रदेश