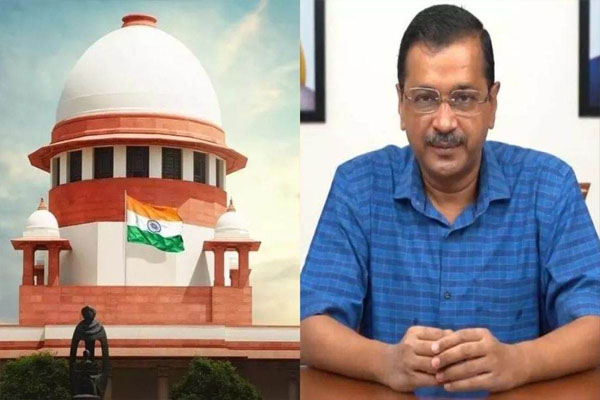सतीश सिंह
प्रसिद्ध शायर दुष्यंत कुमार ने ए के सिंह, जिनका पूरा नाम अवधेश कुमार सिंह के लिये ही कभी लिखा था, “कौन कहता है, आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों”। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अहमदाबाद, गुजरात में पदस्थापित क्षेत्रीय आयुक्त-1, श्री सिंह ने इस कथन को सही मायनों में चरितार्थ किया है।
पूर्व में 50 वर्ष आयु वर्ग और अब 55 वर्ष आयु वर्ग में श्री सिंह मैराथन में देश के उभरते सितारे हैं। मूल रूप से बिहार के पखनपुर, थाना हिलसा, जिला नालंदा के रहने वाले श्री सिंह की पृष्ठभूमि खेल की नहीं रही है। पूर्व में उन्होंने स्कूल या कॉलेज या फिर जीवन के किसी भी कालखंड में कभी भी किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लिया है।
श्री सिंह की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी प्रभावशाली रही है। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में तो वे ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं। कई सरकारी नौकरियाँ कर चुके हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1998 में आयोजित सहायक आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की परीक्षा में श्री सिंह का मेरिट लिस्ट में 22वां स्थान रहा था।
2015 में कोलकाता पदस्थपाना के दौरान श्री सिंह ने मैराथन के बारे में पढ़ा। साथ में यह भी जाना कि जो भी प्रतिभागी दौड़ को पूरा करते हैं उन्हें पदक दिया जाता है। चूंकि, श्री सिंह नियमित रूप से सैर करते थे, इसलिए, उन्हें लगा कि वे भी मैराथन दौड़ सकते हैं और उन्होंने बिना देर किए एयरटेल दिल्ली मैराथन, बड़ौदा अल्ट्रा मैराथन और 25 किलोमीटर के कोलकाता मैराथन के लिए अपना नामांकन करवा लिया।
श्री सिंह ने पहली बार 2015 में 45 वर्ष से अधिक उम्र संवर्ग में बड़ौदा अल्ट्रा हॉफ मैराथन में हिस्सा लिया और 23वां स्थान हासिल किया। पहले प्रयास में सम्मानजनक स्थान हासिल करने से उनके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व इजाफा हुआ। इसके बाद, 2015 में ही श्री सिंह ने दिल्ली और कोलकात्ता हॉफ मैराथन में हिस्सा लिया। कोलकात्ता हॉफ मैराथन में श्री सिंह ने 19वां स्थान हासिल किया तो दिल्ली हॉफ मैराथन में 153वां। तीनों उपलब्धियां, श्री सिंह ने बिना किसी प्रशिक्षण के हासिल की, जिससे उनके हौसले में अभूतपूर्व इजाफा हुआ। उन्हें लगा कि यदि मैराथन का पेशेवर प्रशिक्षण लिया जाये तो आसानी से वे अपने आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं।
संयोग से, नवंबर, 2015 में ही, श्री सिंह का तबादला पंजाब के लुधियाना शहर में हो गया। वे जानते थे कि खेल के मामले में पंजाब देश में अव्वल है। इसलिए, उन्हें यहाँ एक अच्छा कोच मिल सकता है। इस दौरान श्री सिंह ने ओ पी जैयशा के जीवन के बारे में लेख पढ़ा। लेख, जैयशा के जीवन संघर्ष के बारे में था, मसलन, जैयशा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँची। उसी लेख में, श्री सिंह को जैयशा के पति और एथलीट के कोच श्री गुरमीत सिंह जी के बारे में जानकारी मिली।
यह भी पता चला कि जैयशा को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान श्री गुरमीत जी का रहा है। लेख में बताया गया था कि श्री गुरमीत लुधियाना से हैं। श्री सिंह ने श्री गुरमीत जी से उन्हें प्रशिक्षित करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
महज 6 महीनों के पेशेवर प्रशिक्षण के बाद, श्री सिंह ने जुलाई, 2016 में चंडीगढ़ के 21 किलोमीटर हॉफ मैराथन, रन द नाइट ग्लो में हिस्सा लिया और अपने आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में, श्री सिंह को ओवर ऑल 12वां स्थान हासिल हुआ। श्री सिंह ने अगस्त, 2016 में मुंबई में हुए आईडीबीआई हॉफ मैराथन में छठा स्थान प्राप्त किया तो अक्टूबर, 16 में आयोजित बड़ौदा अल्ट्रा हाफ मैराथन में चौथा स्थान। दिसंबर, 2016 को टाटा स्टील द्वारा आयोजित की जाने वाली कोलकात्ता हॉफ मैराथन में श्री सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया।
20 नवंबर, 2016 को दिल्ली में आयोजित एयरटेल डेल्ही हॉफ मैराथन में श्री सिंह ने 19वां स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि उन्होंने चिकनगुनिया से पीड़ित होने के बाद हासिल किया था। श्री सिंह ने इस हॉफ मैराथन को 1 घंटा 38 मिनट में पूरा किया था, जबकि 2015 में इसी दूरी को तय करने में उन्होंने 1 घंटा 55 मिनट का समय लिया था और उनका 153वां स्थान रहा था।
उपलब्धि के दृष्टिकोण से यह एक लंबी छलांग थी। श्री सिंह ने 2016 में हुए आईडीबीआई मुंबई हॉफ मैराथन में छठा स्थान हासिल किया तो 2017 में मुंबई में आयोजित स्टैंडर्ड चार्टर्ड हॉफ मैराथन में चौथा स्थान हासिल किया। 2017 के दिसंबर में पटना में हुए हॉफ मैराथन में श्री सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया।
श्री सिंह के हॉफ मैराथन का कारवां यूं ही आगे बढ़ रहा था। इसी बीच, उन्हें बोस्टन मैराथन के बारे में पता चला। लोगों ने कहा कि बिना बोस्टन मैराथन दौड़े आपके मैराथन दौड़ने का सफर अधूरा है। चूँकि, बोस्टन मैराथन फुल यानी 42 किलोमीटर का होता है। इसलिये, श्री सिंह ने हॉफ मैराथन की जगह फुल मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया।
फिर, 2017 में ही लॉन्गफोर्ड, आयरलैंड में अगस्त महीने में हुए फुल मैराथन में श्री सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। फिर भी, वे बोस्टन मैराथन के लिये पात्रता हासिल नहीं कर सके। पुनश्च: 2017 में हुए आईडीबीआई दिल्ली फुल मैराथन में उन्होंने 13वां स्थान हासिल किया, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक गये। वर्ष 2018 में हुए आईडीबीआई दिल्ली फुल मैराथन में श्री सिंह ने 9वां स्थान हासिल करते हुए बोस्टन मैराथन की पात्रता हासिल कर ली। यह दूरी श्री सिंह ने 3 घंटे 24 मिनट में पूरी की।
श्री सिंह ने 2019 में बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया। यह श्री सिंह के सपने के साकार होने जैसा था, क्योंकि बोस्टन मैराथन को दुनिया भर में मैराथन का मक्का-मदीना माना जाता है। उसके बाद, अप्रैल, 2018 में चंडीगढ़ में आयोजित डेली वर्ल्ड फुल मैराथन को 3 घंटे 32 मिनट में पूरी करते हुए गोल्ड मेडल जीतने का गौरव हासिल किया। श्री सिंह डेली वर्ल्ड मैराथन के ब्रांड एमबेस्डर भी रहे हैं।
श्री सिंह 2017 एवं 2018 में पंजाब मास्टर एथलेटिक्स के 400 व 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। श्री सिंह ने 2019 में गुंटूर में संपन्न हुए राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते 800 मीटर संवर्ग में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। वैसे, श्री सिंह स्वर्ण पदक के हकदार थे, लेकिन फिनिशिंग लाइन से कुछ मीटर पहले गिर जाने की वजह से उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
श्री सिंह 2019 में मलेशिया की राजधानी क्वालालांपुर में आयोजित की गई एशियाई खेल में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 800 मीटर संवर्ग में 2.25 मिनट का समय लेकर 5वां स्थान प्राप्त कर चुके हैं। आम तौर पर मैराथन दौड़ने वाले 400 या 800 मीटर जैसी कम दूरी की स्पर्धाओं में भाग नहीं लेते हैं। यह श्री सिंह की विलक्षण प्रतिभा ही है कि वे मैराथन और छोटी दूरी की स्पर्धाओं में साथ-साथ अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं।
2020 में कोरोना के आक्रमण से दुनिया थम सी गई थी। हर जगह डर और खौफ का माहौल था। ऐसे आपातकाल में श्री सिंह का मैराथन दौड़ना भी बंद हो गया, लेकिन जैसे ही महामारी का प्रकोप कम हुआ, श्री सिंह ने सितंबर 2021 में आयोजित की गई शिवालिक हिल्स हॉफ मैराथन में हिस्सा लिया और बिना अभ्यास के चौथा स्थान हासिल किया।
2022 और 2023 के सितंबर महीने तक पारिवारिक कारणों से श्री सिंह अभ्यास एवं मैराथन दोनों से दूर रहे, लेकिन 15 अक्तूबर को दिल्ली में आयोजित वेदांता हॉफ मैराथन में बिना तैयारी के 26वां स्थान हासिल किया। श्री सिंह ने पुनः 26 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में आयोजित किये गये अडानी फुल मैराथन में 3 घंटे, 55 मिनट और 57 सेकेंड समय के साथ सातवाँ स्थान हासिल किया। फिर, चंडीगढ़ में 18 फरवरी 2024 को आयोजित सीएफएम फुल मैराथन में श्री सिंह ने 3 घंटे 32 मिनट और 1 सेकेंड समय के साथ ओवरऑल 16वां रैंक हासिल किया। साथ ही, बोस्टन एवं शिकागो मैराथन में हिस्सा लेने की पात्रता भी हासिल कर ली। अडानी मैराथन की तुलना में चंडीगढ़ मैराथन में श्री सिंह की टाइमिंग में काफी सुधार आया, जो दर्शाता है कि श्री फिर से ट्रैक पर आ चुके हैं और जल्द ही कुछ और शानदार उपलब्धियां श्री सिंह के खाते में आने वाली हैं।
सतीश सिंह-अहमदाबाद स्थित वरिष्ठ स्तंभकार हैं,विचार व्यक्तिगत हैं