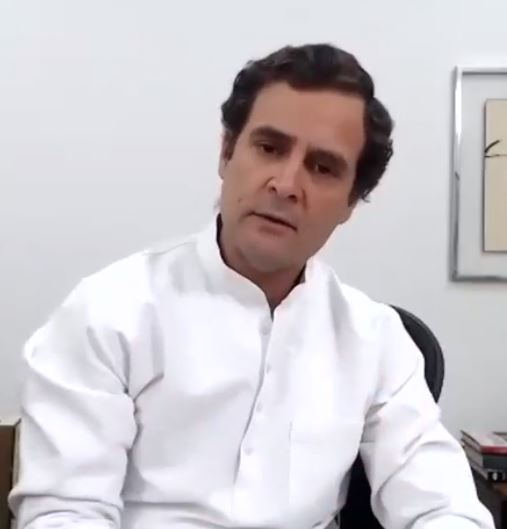महानायक अमिताभ बच्चन और उनके अभिनेता पुत्र अभिषेक बच्चन, जिन्हें शनिवार को कोविड-१९ टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया है, की हालत स्थिर बताई गयी है, और चिंता जैसी कोई बात नहीं है। दोनों इस समय आइसोलेशन वार्ड में हैं। उनके एंटीजेन टेस्ट की रिपोर्ट का अभी इंतजार है, जिससे उनके कोरोना की स्थिति की पूरी जानकारी मिलेगी।
कुछ ही देर पहले उन्होंने अपना एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने नानावटी अस्पताल और देश में डाक्टरों की कोविड-१९ में भूमिका की तारीफ़ की है, साथ ही कहा है कि इन हालातों से बाहर निकलेंगे।
इस बीच खबर है कि अभिनेता अनुपम खेर की मां, भाभी, भतीजी और भाई भी कोविड-१९ पॉजिटिव पाए गए हैं। अनुपम खेर ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। हालांकि, खुद अनुपम की रिपोर्ट नेगेटिव है।
बच्चन परिवार का बंगला ”जलसा” सील कर दिया गया है। इससे पहले उसे सेनेटाइज भी किया गया है। परिवार में अमिताभ की पत्नी जया बच्चन और अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या रॉय और अन्य सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके सारे स्टाफ के टेस्ट भी किये जा रहे हैं। दोनों सीनियर और जूनियर बच्चन के जल्द स्वस्थ होने के किये देश भर में दुआएं की जा रही हैं। वैसे अभिषेक ने कल ही ट्वीट में कहा था कि चिंता की बात नहीं है। रात को दोनों के अस्वस्थ होने की खबर बाहर आते ही देश भर में सोशल मीडिया में दोनों के लिए दुआओं का दौर जारी हो गया। रात होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री के हर छोटे-बड़े कलाकार ने उनकी स्वास्थ्य की कामना की।
ख़बरों के मुताबिक देश में कई जगह बच्चन के फैंस ने मंदिरों में भी पूजा-अर्चना की है। उनके स्वास्थ्य की ख़बरें लगातार ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं। यहाँ यह गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं झेलते रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी एक कार्यक्रम में दी थी कि उन्हें पीठ की बोन में टीवी हुई थी और इलाज के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे।
इसके अलावा अमिताभ लीवर की समस्या आज तक झेल रहे हैं। उनका ७५ फीसदी लीवर खराब है और कोविड-१९ जैसी समस्या होने के कारण उन्हें अतिरिक्त सावधानी की जरूरत रहेगी। वैसे अमिताभ जैसे ”लड़ाके” हैं और जिस तरह जीवन में उन्होंने समस्यायों हो हराया है, उम्मीद है इस बार भी वे स्वस्थ होकर बाहर आएंगे।