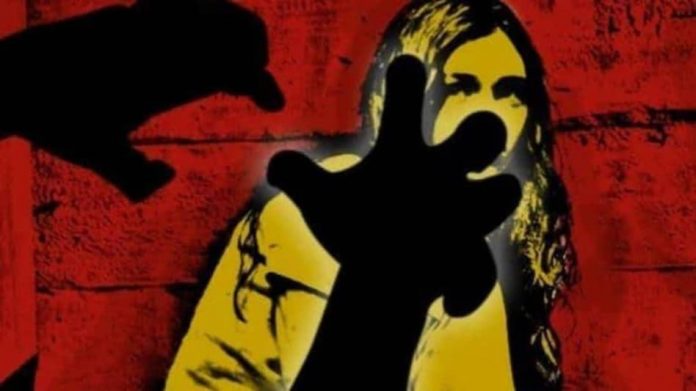स्कूलों को करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन कुछ राज्यों में स्कूल खुलते ही बीमार पड़े बच्चे
बच्चों का भी जल्द होना चाहिए टीकाकरण तीसरी लहर के आने से डरे हुए हैं अभिभावक
बाज़ारों, शराब के ठेकों, मॉलों, सिनेमाघरों के बाद आख़िरकार अधिकतर राज्यों में स्कूल भी खुल ही गये। कोरोना महामारी के चलते क़रीब सवा साल स्कूलों के बन्द रहने के बाद देश के कई राज्यों में इन्हें खोल दिया गया है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूलों को कोरोना आपातकाल (कोविड प्रोटोकॉल) का पालन कराने के सख़्त निर्देश राज्य सरकारों ने दिये हैं। अभी तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में स्कूलों को खोला जा चुका है।
हालाँकि कुछ राज्यों में पूरी तरह से तो कुछ राज्यों में 50 फ़ीसदी छात्र-उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोला गया है। वहीं कुछ में 100 फ़ीसदी उपस्थिति की छूट है। कुछ राज्यों में कॉलेज भी खुल गये हैं। वहीं कुछ राज्यों में स्कूल और कॉलेज दोनों ही नहीं खुले हैं। जम्मू एवं कश्मीर में स्कूल, कॉलेज खुलेंगे और कोचिंग सेंटर फ़िलहाल बन्द रहेंगे; लेकिन केवल बड़ी कक्षाओं के शिक्षण व कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को खोला जा रहा है। इनमें वही अध्यापक और अन्य कर्मचारी जा सकेंगे, जिन्होंने कोरोना-टीका लगवा लिया है।
लेकिन स्कूल और कॉलेज में जाने की अनुमति के मामले में सभी राज्यों ने अपने-अपने क़ायदे-क़ानून बनाये हैं। मसलन पंजाब की सरकार ने निर्देश दिये हैं कि स्कूलों-कॉलेजों में वही अध्यापक और अन्य कर्मचारी प्रवेश कर सकेंगे, जिन्होंने कोरोना-टीके की दोनों ख़ुराकें ले ली हैं। इसके अलावा यदि किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजने की लिखित अनुमति नहीं देंगे, तो वह बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा। वहीं कर्नाटक में वे ही छात्र कॉलेज जा सकेंगे, जिन्होंने कम-से-कम एक बार कोरोना-टीका लगवा लिया है।
कोरोना आपातकाल लागू
स्कूल खोलने वाले तक़रीबन सभी राज्यों ने कोरोना आपातकाल के पालन के निर्देश के साथ शिक्षा विभागों को बच्चों की शिक्षा आगे बढ़ाने के दिशा-निर्देश दिये हैं। इन दिशा-निर्देशों में दो ग़ज की दूरी-मास्क ज़रूरी, अध्यापकों का टीकाकरण और सभी के लिए सेनिटाइजेशन की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना आपातकाल के पालन मात्र से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है? वह भी ऐसे समय में, जब इसकी तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और इस लहर का वायरस बहुत सक्रिय, ताक़तवर, तेज़ी से फैलने वाला बताया जा रहा है। इसमें सन्देह इसलिए भी है; क्योंकि बच्चों से, ख़ासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों से नियमों का पालन कराना कोई आसान काम नहीं होगा। दिन भर जारी रहने वाली बच्चों की अजीब और शरारत भरी गतिविधियाँ, लगातार कई घंटे मास्क को लगाकर रखने की प्रतिबद्धता और उन्हें आपसी दूरी बनाकर रख पाना दूभर काम है। ऐसे में यह पूरे भरोस से तो नहीं कहा जा सकता कि स्कूलों में बच्चे सुरक्षित रह पाएँगे।
दूसरी बात हो सकता है कि राज्य सरकारें शुरू-शुरू में मास्क, सैनिटाइजर और बच्चों के दूर-दूर बैठने की व्यवस्था कर भी दें; लेकिन क्या बहुत दिनों तक यह व्यवस्था किसी राज्य के स्कूलों में रह पाएगी? यह सवाल इसलिए भी, क्योंकि देखा गया है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पहले से ही ढीली-ढाली है। इसकी एक वजह अगर सरकार, शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन की तरफ़ से होने वाली लापरवाही है, तो दूसरी वजह अब तक कई कार्यों में हो चुके घोटाले हैं। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि किसी राज्य में मास्क, सैनिटाइजर और दूसरी चीज़ों पर कोई घोटाला नहीं होगा। कुल मिलाकर बच्चों की सुरक्षा की गारंटी शायद ही कोई दे, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के राबट्र्सगंज ज़िले के एक स्कूल में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन न होने पर वहाँ एक पत्रकार ने पहुँचकर वीडियो बनानी चाही, जिस पर वहाँ मौज़ूद अध्यापकों और छात्रों ने पत्रकार से हाथापाई की और उससे गाली-गलौज की।
फीस न दे सके बच्चों का क्या होगा?
जिन राज्य सरकारों ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है, उन राज्यों में उन बच्चों का क्या होगा, जिनके अभिभावक विद्यालय शुल्क (स्कूल फीस)नहीं भर सके हैं। सरकारी स्कूलों में तो यह दिक़्क़त नहीं है। लेकिन निजी स्कूलों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनके अभिभावक उनकी फीस नहीं भर सके हैं। ऐसे स्कूल पिछले साल बिना पढ़ाई कराये ही बच्चों और अभिभावक पर लगातार फीस भरने का दबाव डाल रहे हैं। फीस न देने पर रिजल्ट और टीसी रोकने, बच्चे का रिकॉर्ड ख़राब करने और जबरन फीस वसूलने की धमकियाँ दे रहे हैं। इसके अलावा एक खेल और भी ये स्कूल कर रहे हैं, वह यह कि नयी कक्षा में प्रवेश के नाम पर पूरे साल की फीस ले रहे हैं और फीस आने पर बच्चों को यह कहकर स्कूल से निकाल रहे हैं कि उन्होंने बीते वर्ष की फीस दी है, चालू वर्ष की फीस उन्हें भरनी होगी, तभी वे आगे पढ़ सकेंगे।
सब बच्चे पहुँच सकेंगे स्कूल?
बड़ा सवाल यह भी है कि जो बच्चे पढ़ाई छोडक़र घर बैठ चुके हैं, क्या उन्हें स्कूल वापस बुला पाएँगे? भारत में आज भी कई गाँव हैं, जो शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। ऐसे गाँवों के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही मिड-डे मील जैसी योजना सरकार ने शुरू की थी, ताकि स्कूलों में ज़्यादा-से-ज्यादा संख्या में बच्चे आ सकें। कोरोना-काल में न तो स्कूल खुले और न ही मिड-डे मील का कार्यक्रम चल सका। ऐसे में बहुत से बच्चे पढ़ाई छोडक़र घर बैठ गये। दूसरे उन बच्चों की पढ़ाई भी छूट गयी है, जिनके अभिभावक दूसरे राज्यों, शहरों में रहते थे और तालाबंदी के बाद अपने गाँव लौट गये। इसके अलावा कुछ बच्चे परिवार की आर्थिक तंगी के चलते कमाने की ओर अग्रसर हो गये। क्या ऐसे बच्चे दोबारा स्कूल जा सकेंगे?
बाहरी बच्चों का क्या होगा?
एक सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकारें नवोदय जैसे बड़े स्कूलों और उन स्कूलों, जिनमें छात्रावास (हॉस्टल) की व्यवस्था होती है; के छात्रावासों को खोलने की अनुमति देंगी? क्योंकि हर राज्य में ऐसे अनेक स्कूल हैं, जिनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास की व्यवस्था होती है। देश में कई स्कूल ऐसे हैं, जो एकल अभिभावक (सिंगल पैरेंट) के बच्चों, अनाथ बच्चों को स्कूल में ही रहने की व्यवस्था देकर पढ़ाते हैं। इसके अलावा कई स्कूल इसी आधार पर बने होते हैं, जो बच्चों को अपने यहाँ रखकर पढ़ाते हैं। अगर इन स्कूलों में बच्चों को रहने की अनुमति नहीं मिलती है, तो वहाँ रहकर अध्ययन करने वाले बच्चों की पढ़ाई सम्भव ही नहीं हो सकेगी।
स्कूल खुलते ही संक्रमित हुए बच्चे
जुलाई में महाराष्ट्र में जैसे ही स्कूल खुले, वहाँ के सोलापुर में एक साथ 613 विद्यार्थी कोरोना की चपेट में आ गये। इससे ज़िला प्रशासन में हडक़ंप मच गया और ज़िले के स्कूलों को बन्द करना पड़ा। हरियाणा स्थित फतेहाबाद के एक स्कूल में भी छ: बच्चे कोरोना संक्रमित मिले। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ स्कूलों में आधा दर्ज़न से ज़्यादा, लुधियाना (पंजाब) में क़रीब 20 और बेंगलूरु (कर्नाटक) के अलग-अलग स्कूलों में सबसे ज़्यादा क़रीब 300 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की ख़बरें हैं।
कुछ अभिभावकों की आपत्ति
राज्य सरकारों ने स्कूल तो खोल दिये, लेकिन बहुत-से बच्चों के अभिभावक उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते। इन अभिभावकों का कहना है कि जब तक सरकार बच्चों के लिए कोरोना-टीका लेकर नहीं आती है और उनकी सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम नहीं करती है, तब तक वे जोखिम नहीं ले सकते। एक नज़रिये से अभिभावकों की बात सही भी है। हालाँकि बच्चों की सुरक्षा की गारंटी तो कोई भी राज्य सरकार नहीं ही देगी। लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर का तांडव हम सब देख ही चुके हैं और तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में माँ-बाप क्यों न बच्चों की चिन्ता करें? वैसे भी बच्चों में कोरोना संक्रमण होने का $खतरा तीसरी लहर में ज़्यादा बताया जा रहा है। कई राज्यों में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की ख़बरें भी सामने आ रही हैं।
तीसरी लहर आ चुकी है : डॉ. मनीष
दिल्ली के द्वारिका स्थित एक निजी अस्पताल में अपनी सेवाएँ देने वाले डॉ. मनीष कहते हैं कि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। डेल्टा वेरिएंट नाम की इस लहर की चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं। हालाँकि भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इससे बचाव की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोरोना-टीका अभी तक नहीं बन सका है। इसके अलावा सभी पात्र लोगों का भी अभी तक टीकाकरण नहीं हो सका है। ऐसे में अगर इस लहर ने दूसरी लहर की तरह तेज़ी पकड़ी, तो एक बार फिर तबाही मच सकती है; जो कि पूरे देश के लिए बहुत परेशानी वाली और दु:खदायी होगी। ऐसे में भारत सरकार को सभी राज्यों से तेज़ी से टीकाकरण करने को कहना चाहिए। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं के लिए भी कोरोना-टीका ईज़ाद करने की दिशा में बेहतर क़दम उठाने चाहिए।