
हममें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रुडयार्ड किपलिंग की लिखी मोगली की कहानी नहीं पढ़ी हो. हां, वही मोगली जिसे भेड़ियों ने पाला था. जाहिर है जब हम रांची से 200 किलोमीटर दूर लातेहार जिले में स्थित देश के एकमात्र भेड़िया अभयारण्य की ओर बढ़े तो हमारे मन में तमाम रोमांचक कल्पनाएं उमड़ती-घुमड़ती रहीं. हम महुआडांड़ स्थित वन विभाग के कार्यालय पहुंचते हैं जहां हमारी मुलाकात रामदेव बड़ाईक से होती है. बड़ाईक वहां के अतिथिगृह की देखभाल करने वाले दिहाड़ी कर्मचारी हैं. हम गौर करते हैं कि देश के इस इकलौते भेड़िया अभयारण्य के कार्यालय में न तो भेड़िये की कोई तस्वीर है न ही कोई अन्य प्रतीक. हमारी जिज्ञासा पर बड़ाईक हमें एक छोटा-सा बोर्ड दिखाते हैं जिस पर लिखा है, ‘महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-18-1 के तहत अधिसूचित, अधिसूचना संख्या- 1062, दिनांक- 23/06/1976.’ इसके आगे कुछ जगहों के नाम लिखे हैं मसलन, चेतमा, सरनाडीह, पुरवा, उरुम्बी आदि. कुल 6,317 हेक्टेयर में फैले भेड़िया अभयारण्य का पूरा ब्योरा वहां दर्ज है. बड़ाईक चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहते हैं, ‘अब यकीन हुआ न कि आप देश के इकलौते भेड़िया अभयारण्य के कार्यालय में हैं.’
बड़ाईक के सिवा वहां कोई नहीं मिलता और घंटे भर बाद जब हम भेड़ियों के आशियाने वाले इलाके में निकलने को होते हैं तो हमारे साथ पथ प्रदर्शक बनकर बड़ाईक ही चलते हैं. 10-15 किलोमीटर उबड़-खाबड़ रास्ता गाड़ी से तय करने के बाद पांच-छह किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है. हम उनसे पूछते हैं, ‘रास्ते में भेड़िये हमला तो नहीं करेंगे न!’ बड़ाईक न हंसते हैं, न कुछ जवाब देते हैं. दुबारा पूछने पर कहते हैं, ‘अभी तो हम लोग तीन-चार की संख्या में हैं, अगर गलती से भेड़िये अकेले इंसान को भी देख लेंगे तो बेचारे अपनी जान बचाकर भागेंगे.’ दुरूह यात्रा के बाद हम सरनाडीह पहुंचते हैं. सरनाडीह यानी देश के इकलौते भेड़िया अभयारण्य का केंद्र स्थल और वर्षों से भेड़ियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना. गांव से थोड़ी दूर पर पत्थरों के विशाल टीले दिखते हैं. बड़ाईक चिल्लाते हैं- मांद नंबर एक दिखने लगी है. मांद नंबर एक के पास पहुंचते ही वे उसके प्रवेश पर लेट जाते हैं. गर्दन घुसाकर गंध लेने की मुद्रा बनाए हुए कहते हैं, ‘आइए ना, गंध सुंघिए.
भेड़िये की गंध आ रही है, सड़े हुए मांस की भी. अंदर होंगे भेड़िये.’ वह काल्पनिक गंध सिर्फ बड़ाईक ही सूंघ पाते हैं. गंध पर हमारे यकीन नहीं करने पर बड़ाईक अपनी टी-शर्ट में सटे एक-दो बाल दिखाते हुए कहते हैं, ‘अच्छा इस बाल को देखिए, अब तो यकीन हो रहा है न कि भेड़िया रहता होगा.’ मांद नंबर दो पहुंचकर भी हमें कुछ नहीं दिखता. बड़ाईक सूखा मल दिखाते हुए कहते हैं, ‘देखिए, भेड़िये का मल है यह. पक्के तौर पर.’ हम समझ नहीं पाए कि वे उसकी पहचान कैसे कर रहे हैं. यहां कई प्राकृतिक मांद हैं, पर कहीं कोई भेड़िया नहीं दिखता, न उसकी कोई ठोस निशानी. बड़ाईक विभाग के वफादार कर्मी की तरह हमें यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि भेड़िये यहां रहते हैं लेकिन वे भी जानते हैं कि देश के इस इकलौते भेड़िया अभयारण्य में भेड़िया दिखा देना अब इतना आसान नहीं है. रास्ते में हमें सरनाडीह अतिथिगृह दिखता है. कभी भेड़िया प्रेमियों का आशियाना अब खंडहर बन चुका है.
गांव में बने वन आरक्षी केंद्र को देखकर भी यही लगता है कि वर्षों से यहां कोई नहीं आया. रास्ते में ही भेड़ियों की प्यास बुझाने के लिए बनाए गए छोटे तालाब भी दिखते हैं. वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है. सरनाडीह गांव में कई लोगों से हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, ‘क्या हाल के दिनों में आपने किसी भेड़िये को देखा है?’ 78 वर्षीया बुजुर्ग मिलियान एक्का बताती हैं, ‘दो-तीन साल पहले भेड़िया मेरी मुर्गी को उठा ले गया था. पहले भेड़िये आते थे लेकिन अब नहीं दिखते.’ इसी गांव में तिनतुसिया कुजूर से बात होती है. वे भी इसी भेड़िया अभयारण्य से सेवानिवृत्त हुए हैं. वे बताते हैं कि पहले अलसुबह और शाम होते ही भेड़ियों की आवाज सुनाई देने लगती थी लेकिन अब नहीं. वे बताते हैं, ‘सरकार ने तो फिर भी 1976 में इसे, देश का इकलौता भेड़िया अभयारण्य घोषित किया लेकिन जिन मांदो को देखकर आप आ रही हैं, आदिवासी समाज के बीच वे पीढ़ियों से ‘हुंड़ार पारिस’ नाम से ही मशहूर रहे हैं.’ हुंड़ार का मतलब भेड़िया और पारिस का आशय है बंगला.
हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और इसी इलाके के बाशिंदे जेरोम जेराल्ड कुजूर भी हैं. वे कहते हैं, ‘हम तो बचपन से ही ‘हुंड़ार पारिस’ जानते हैं और यह भी सुनते रहे हैं कि कभी गांववालों और भेड़ियों में मुठभेड़ नहीं हुई बल्कि गांववाले स्वेच्छा से भेड़ियों के लिए बकरी-सुअर-मुर्गी आदि बाहर छोड़ दिया करते थे ताकि वो आएं तो अपना आहार लेकर लौट जाएं.’ हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों भेड़ियों का आदिवासी समाज से इतना गहरा रिश्ता रहा है और भेड़ियों की मांद के पास गांव बसाने में आदिवासियों को क्यों डर नहीं लगा. इसका जवाब भेड़िया संरक्षण अभियान से जुड़े डेबरा मैकॉन अपनी वेबसाइट ‘सेक्रेड वुल्फ ड्रीम्स स्पिरिट वर्ल्ड’ में लिखते हैं, ‘आदिवासियों और भेड़ियों के बीच गहरा संबंध रहा है और आदिवासी समाज भेड़ियों के साथ बहुत सहज महसूस करते रहे हैं. वे मानते हैं कि भेड़िये खतरनाक जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करेंगे और फिर दोनों की जीवनशैली भी कुछ मायने में एक जैसी है. आदिवासी भी समूह में रहते हैं और भेड़िये भी.’




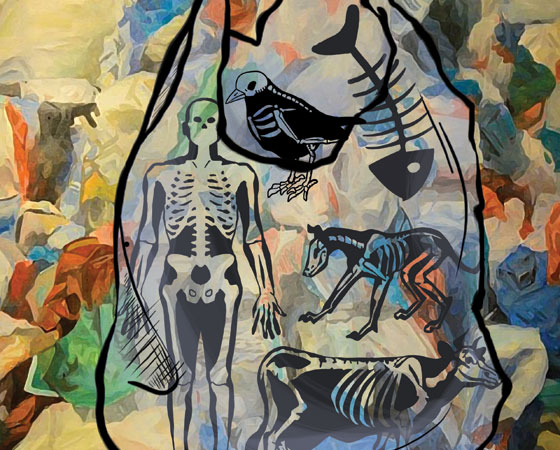












 उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों खुले आम असंतोष अभियान चल रहा है. असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों, मुख्यमंत्री और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों के बीच फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोले जा रहे हैं. इस राजनीतिक ड्रामे की शुरुआत धारचूला के विधायक हरीश धामी के बयान से हुई . नेपाल और चीन सीमा पर बसा धारचूला बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है. पांच जून को धामी ने राजधानी देहरादून में आकर बयान दिया कि उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और अगर 15 दिन के भीतर इस दिशा में सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास नहीं हुए तो वे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे. उन्होंने इस्तीफा देकर धारचूला से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात तो कही ही, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भी अपने खिलाफ मैदान में उतरने की चुनौती दे डाली. उनका कहना था, ‘मुख्यमंत्री बेहद कमजोर हैं और उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है. इन दोनों कारणों से राज्य में नौकरशाही बेलगाम है और भ्रष्टाचार चरम पर है.’
उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों खुले आम असंतोष अभियान चल रहा है. असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों, मुख्यमंत्री और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों के बीच फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोले जा रहे हैं. इस राजनीतिक ड्रामे की शुरुआत धारचूला के विधायक हरीश धामी के बयान से हुई . नेपाल और चीन सीमा पर बसा धारचूला बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है. पांच जून को धामी ने राजधानी देहरादून में आकर बयान दिया कि उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और अगर 15 दिन के भीतर इस दिशा में सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास नहीं हुए तो वे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे. उन्होंने इस्तीफा देकर धारचूला से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात तो कही ही, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भी अपने खिलाफ मैदान में उतरने की चुनौती दे डाली. उनका कहना था, ‘मुख्यमंत्री बेहद कमजोर हैं और उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है. इन दोनों कारणों से राज्य में नौकरशाही बेलगाम है और भ्रष्टाचार चरम पर है.’ भारतीय जनता पार्टी का मीडिया खासकर न्यूज चैनलों से और न्यूज चैनलों का भाजपा से प्यार किसी से छिपा नहीं है. यह स्वाभाविक भी है क्योंकि भाजपा के कई नेताओं की ‘लोकप्रियता’ और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में ‘चमकाने’ में टीवी की बड़ी भूमिका है. कई तो बिना किसी राजनीतिक जमीन के सिर्फ चैनलों के कारण भाजपा की राजनीति में चमकते हुए सितारे हैं. दूसरी ओर, मीडिया और न्यूज चैनल भी भाजपा को इसलिए पसंद करते हैं कि दोनों का दर्शक वर्ग एक है और दोनों तमाशा पसंद करते हैं. न्यूज चैनलों का कारोबार तमाशे से चलता है तो भाजपा की राजनीति तमाशे के बिना कुछ नहीं है.
भारतीय जनता पार्टी का मीडिया खासकर न्यूज चैनलों से और न्यूज चैनलों का भाजपा से प्यार किसी से छिपा नहीं है. यह स्वाभाविक भी है क्योंकि भाजपा के कई नेताओं की ‘लोकप्रियता’ और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में ‘चमकाने’ में टीवी की बड़ी भूमिका है. कई तो बिना किसी राजनीतिक जमीन के सिर्फ चैनलों के कारण भाजपा की राजनीति में चमकते हुए सितारे हैं. दूसरी ओर, मीडिया और न्यूज चैनल भी भाजपा को इसलिए पसंद करते हैं कि दोनों का दर्शक वर्ग एक है और दोनों तमाशा पसंद करते हैं. न्यूज चैनलों का कारोबार तमाशे से चलता है तो भाजपा की राजनीति तमाशे के बिना कुछ नहीं है.