
आंकड़े अक्सर बेहद बोझिल और उबाऊ होते हैं. लेकिन कभी-कभी उनसे कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी उभर जाती हैं. एक आंकड़ा यह है कि हालिया चार विधानसभा के चुनावों में कुल 589 विधानसभा सीटें दांव पर लगी हुई थी. कांग्रेस को इनमें से महज 126 सीटें हाथ लगी हैं. प्रतिशत में यह 22 के आस पास बैठता है. देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी के बारे में यह आंकड़ा क्या कहता है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस देश के उत्तर और मध्य से लगभग विलुप्त हो चुकी है.
जिन चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें राजस्थान को छोड़ दें तो बाकी तीन, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ‘लैंड लॉक्ड’ प्रदेश हैं. न तो इनकी सीमाएं किसी देश से लगती हैं न ही ये समुद्र को छूती हैं. कहने का अर्थ है कि नक्शे के बिल्कुल बीचो-बीच मौजूद ये राज्य देश का हृदयस्थल बनाते हैं. यह भूगोल तो लगभग सबको पता ही है तो फिर इसका यहां जिक्र क्यों? दरअसल इस भूगोल मेंे ही कांग्रेस का इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों चौपट हो गया है. इतिहास इस लिहाज से कि इतनी दुर्गति कांग्रेस को एकाध बार ही देखनी पड़ी है और नागरिक शास्त्र इसलिए कि आज यहां कांग्रेस के पास कहने को अपना कोई भी समर्पित वोटबैंक नहीं बचा है. इन चार राज्यों के अलावा उत्तर भारत (हिंदी हृदय प्रदेश) के दो अन्य महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुए एक अर्सा हो चुका है. 2012 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को अगर संकेत मानें तो यहां 2014 में भी पार्टी के दिन बहुरने नहीं जा रहे. यही बात बिहार के बारे में भी कही जा सकती है. झारखंड में भी कांग्रेस की जोड़-तोड़ वाली सरकार है. यानी उत्तर भारत में पार्टी साफ हो चुकी है.
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. अतीत में दो मौके ऐसे आए हैं जब कांग्रेस हिंदी पट्टी से लगभग लापता हो गई थी. पहला मौका था आपातकाल के बाद सन 77 में हुए लोकसभा चुनाव और दूसरा 1989 के आम चुनाव जब वीपी सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ मशाल लेकर चले थे. हालांकि 1989 में कांग्रेस की असफलता अल्पकालिक और सिर्फ लोकसभा तक सीमित थी और उत्तर के कई राज्यों की सत्ता फिर भी पार्टी के हाथ में थी. लेकिन 1977 और उसके कुछ समय बाद तो वह केंद्र और उत्तर के राज्यों, दोनों में बुरी तरह ढेर हो गई थी. जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल वापस लेकर लोकसभा चुनाव करवाने की घोषणा की तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में कुल मिलाकर कांग्रेस को दो लोकसभा सीटें मिली थीं. इन राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का आंकड़ा था 196. 1989 में यह आंकड़ा 25 पर सिमटा था. कह सकते हैं कि आपातकाल के बाद हिंदी पट्टी में कांग्रेस के सामने पहली बार इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है.
सवाल है कि यह संकट क्यों खड़ा हुआ है. आज कांग्रेस के सामने आपातकाल जैसी कोई आसाधारण स्थिति नहीं थी. जनता ने दो बार लगातार कांग्रेस के पक्ष में नतीजे दिए थे. उसके पास काम करने का पर्याप्त मौका था. पर सरकार की जो छवि बनी वह एक भ्रष्टाचारी, दंभी, कॉर्पोरेट समर्थित और गरीब विरोधी की बनी. वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं, ‘राजनीतिक दलों का हाई और लो फेज आता है. कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में अपने हाई प्वाइंट को छू चुकी है, अब उसका लो फेज चल रहा है. इस स्थिति को राजनीतिक पार्टियां अपने गुड गवर्नेेेेंस के जरिए संभालती रहती हैं. पर यूपीए की सरकार गवर्नेंस के मोर्चे पर पूरी तरह से असफल रही है. कहीं पर राजनीतिक ताकत और कहीं पर कार्यकारी ताकत का फार्मूला एक कार्यकाल में तो सफलतापूर्वक चल गया, लेकिन इसे इतना लंबे समय तक खींचना संभव नहीं है. कांग्रेस इस गड़बड़ी को पहचान नहीं सकी.
[box]
विचित्र किंतु सत्य
दिल्ली में पहली बार खंडित जनादेश
दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस आसानी से बहुमत हासिल करने में कामयाब होते रहे हैं. लेकिन इस बार अपना पहला चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बाकियों के लिए ऐसा विध्वंसक रहा कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया. पहली बार दिल्ली में त्रिशंकु हालात बन गए. यही वजह है कि सरकार बनाने को लेकर यहां पहली बार इतनी अधिक माथा पच्ची चल रही है. 1993 में दिल्ली की पहली विधानसभा का गठन हुआ था. 1993 के पहले चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी. उसके बाद 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस ने तीन बार दिल्ली की सत्ता संभाली. अब दिल्ली पहली बार त्रिशंकु विधानसभा देख रही है.
[/box]
आज हालत यह है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है, पार्टी में नेतृत्व का कोई विकल्प बचा नहीं है. शीर्ष पर नेतृत्व का जो संकट है वह पूरी पार्टी से बड़ी कीमत वसूल रहा है.’ कांग्रेस की स्थिति आज उस सेना के जैसी हो गई है जिसका सेनापति युद्धभूमि से लापता हो गया है और सैनिक दिशाहीन होकर अफरा-तफरी में फंस गए हैं.
आपातकाल के बाद कांग्रेस हिंदी पट्टी से इसी तरह साफ हो गई थी, लेकिन तब उसके पास इंदिरा गांधी के रूप में मजूबत और करिश्माई नेतृत्व था. कांग्रेस के लिए संकट का दौर 1996 से 1998 के बीच भी रहा लेकिन तब सोनिया गांधी ने सफलतापूर्वक पार्टी को संभाला था. आज की स्थितियां थोड़ी जटिल हैं. आज सोनिया और राहुल दोनों ही शीर्ष पर आकर नेतृत्व देने के लिए अनिच्छुक दिख रहे हैं और वैकल्पिक नेतृत्व उन्होंने अब तक खड़ा नहीं किया है. इसकी वजह से जनता में भी कांग्रेस के प्रति किसी तरह का जोश नहीं पैदा हो पा रहा है. किदवई की मानें तो पार्टी के भीतर ढांचागत समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं. इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज तक जवाबदेही का तंत्र तक खड़ा नहीं कर पाए हैं. बिहार में पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई पर किसी नेता की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई, यही हाल उत्तर प्रदेश का रहा. लगभग सारे बड़े राज्य उनके हाथ से निकलते गए और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पार्टी अपनी गलतियों से कोई सीख लेते हुए सुधारवादी कदम उठा रही हो.
उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं. यहां 2012 के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के गहन प्रचार अभियान के बावजूद कांग्रेस 28 सीटों पर सिमट गई. इसके बाद राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि वे पूरे संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन लाएंगे, और वे खुद उत्तर प्रदेश आते रहेंगे. उन्होंने कहा था कि वे भागने वालों में से नहीं हंै. लेकिन उनका आचरण इसके बिल्कुल विपरीत दिखा. उत्तर प्रदेश के नाम पर वे इन डेढ़ सालों के दौरान यदाकदा अमेठी आते-जाते रहे. संगठन में बदलाव के नाम पर आज तक सिर्फ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर निर्मल खत्री की ताजपोशी कर दी और विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी प्रदीप माथुर को सौंप दी. इन दो प्रतीकात्मक बदलावों के अलावा और कुछ नहीं हुआ है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव इमरान खान बताते हैं, ‘सिर्फ खत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के अलावा और कुछ नहीं हुआ है. निर्मलजी आज अध्यक्ष बनने के डेढ़ साल बाद भी अपनी टीम का गठन नहीं कर पाए हैं. ऊपर से एक नई दुविधा और पैदा हो गई है. पूरे प्रदेश को 12 जोन में बांट कर सबके अलग-अलग जोनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं. यह व्यवस्था दिल्ली से थोपी गई है और दिल्ली को ही जवाबदेह है. उम्मीदवार चुनने से लेकर और तमाम फैसले का अधिकार इन जोनल कमेटियों को दे दिया गया है. अब प्रदेश कमेटी की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर ही एक दुविधा पैदा हो गई है.’
[box]
यूं होता तो क्या होता
यदि नंद कुमार पटेल जिंदा होते
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नंदकुमार पटेल यदि जीवित होते तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के आसार बढ़ सकते थे. माना जाता है कि पटेल होते तो पार्टी की गुटबाजी पर लगाम रहती. दूसरा, केंद्रीय राज्य मंत्री चरणदास महंत को प्रदेश कांग्रेस का सर्वेसर्वा नहीं बनाया जाता. महंत के पीसीसी अध्यक्ष बनने से पटेल के किए सारे प्रयोग फेल हो गए. पटेल सभी दिग्गज नेताओं को तो एक मंच पर लाए ही थे, खाली बैठे कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने पार्टी के काम में लगा दिया था. लेकिन उनके आकस्मिक निधन से पीसीसी में गुटबाजी फिर चरम पर पहुंच गई. वैसे भी महंत सर्वमान्य नेता नहीं हंै, ऐसे में महज छह माह में न तो वे कोई चमत्कार कर पाए, न ही उनकी ऐसी कोई क्षमता ही है.
[/box]
दिल्ली विधानसभा के नतीजों का एक और संदेश है. कांग्रेस के पास आज अपना कोई समर्पित वोटबैंक नहीं बचा है. शहरी झुग्गियों और मध्यवर्ग पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया है. इसी तरह की समस्याएं कांग्रेस के सामने हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्यों में आ रही हैं. आजादी के बाद से लेकर 90 के दशक के शुरुआती दिनों तक जो दलित, ब्राह्मण और मुसलमान एक साथ कांग्रेसी छाते के नीचे इकट्ठा हो जाता था उसने अब अपने नए-नए ठिकाने ढूंढ़ लिए हैं. सपा, बसपा, आप, भाजपा जैसे विकल्पों ने कांग्रेस को विकल्पहीन बना दिया है.
यह स्थितियां बताती हैं कि पार्टी में समस्या इकहरी नहीं बहुपरतीय है. न तो इंदिरा-राजीव जैसा नेतृत्व है, न समर्पित वोटबैंक बचा है और न संगठन है. ले देकर उनके पास एकमात्र उम्मीद है सत्ता विरोधी लहर. पर मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने कांग्रेस की उस उम्मीद को भी चोट पहुंचाई है.





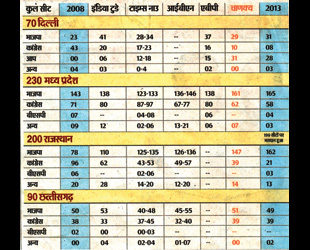
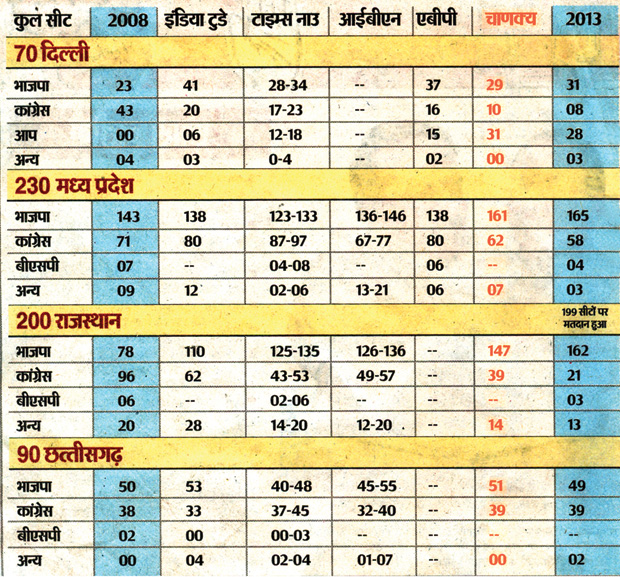






 2013 के आइने से 2014
2013 के आइने से 2014









 किसी ने सोचा नहीं था कि 15 साल तक दिल्ली पर राज करने वाली शीला दीक्षित का सियासी सितारा इस तरह डूबेगा. लोगों को यह तो जरूर लगता था कि कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा है, लेकिन साथ ही यह बात भी थी कि दीक्षित ने दिल्ली में काफी काम किए हैं और हो सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में उनकी वापसी हो जाए.
किसी ने सोचा नहीं था कि 15 साल तक दिल्ली पर राज करने वाली शीला दीक्षित का सियासी सितारा इस तरह डूबेगा. लोगों को यह तो जरूर लगता था कि कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा है, लेकिन साथ ही यह बात भी थी कि दीक्षित ने दिल्ली में काफी काम किए हैं और हो सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में उनकी वापसी हो जाए.
 प्रियंका गांधी आज कांग्रेस की जरूरत हैं. और मजबूरी भी. जरूरत वे कई सालों से थीं, खासकर उन सालों में जब राहुल गांधी हर फ्रंट पर असफलता की तहरीर लिख रहे थे. लेकिन राहुल के प्रति उनकी मां की आसक्ति, कांग्रेसियों की अंधभक्ति और पार्टी द्वारा एक कमजोर नेता को क्षितिज पर टांगने की लगातार आत्ममुग्ध कोशिशों के बीच अब कहीं कोई जंग लगी कील भी नहीं बची जिसपर टंगकर राजकुंवर गांधी चकमक-चकमक चमक सकें. तो अब 127 साल पुराने गर्व से फूली कांग्रेस इस कड़वे यथार्थ को स्वीकार कर प्रियंका को राहुल से आगे खड़ा करने की कोशिश कर सकती है. प्रियंका गांधी को आगे लाने की मजबूरी अगर पार्टी ने अभी भी नहीं समझी तो कांग्रेस सिर्फ 2014 के आम चुनावों की ही नहीं उसके बाद के कई सालों के लिए भी अपनी जमीन बंजर कर लेगी. जैसा कि गांधी परिवार पर लगातार लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, ‘पार्टी के अंदर इस तरह की बातें होना कि प्रियंका को 2019 में आगे लाएंगे, बेमानी है. अगर एक बार कांग्रेस पार्टी टूट गई, उसका बिखराव हो गया तो कोई भी गांधी उसे 2019 में नहीं बचा पाएगा.’
प्रियंका गांधी आज कांग्रेस की जरूरत हैं. और मजबूरी भी. जरूरत वे कई सालों से थीं, खासकर उन सालों में जब राहुल गांधी हर फ्रंट पर असफलता की तहरीर लिख रहे थे. लेकिन राहुल के प्रति उनकी मां की आसक्ति, कांग्रेसियों की अंधभक्ति और पार्टी द्वारा एक कमजोर नेता को क्षितिज पर टांगने की लगातार आत्ममुग्ध कोशिशों के बीच अब कहीं कोई जंग लगी कील भी नहीं बची जिसपर टंगकर राजकुंवर गांधी चकमक-चकमक चमक सकें. तो अब 127 साल पुराने गर्व से फूली कांग्रेस इस कड़वे यथार्थ को स्वीकार कर प्रियंका को राहुल से आगे खड़ा करने की कोशिश कर सकती है. प्रियंका गांधी को आगे लाने की मजबूरी अगर पार्टी ने अभी भी नहीं समझी तो कांग्रेस सिर्फ 2014 के आम चुनावों की ही नहीं उसके बाद के कई सालों के लिए भी अपनी जमीन बंजर कर लेगी. जैसा कि गांधी परिवार पर लगातार लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, ‘पार्टी के अंदर इस तरह की बातें होना कि प्रियंका को 2019 में आगे लाएंगे, बेमानी है. अगर एक बार कांग्रेस पार्टी टूट गई, उसका बिखराव हो गया तो कोई भी गांधी उसे 2019 में नहीं बचा पाएगा.’