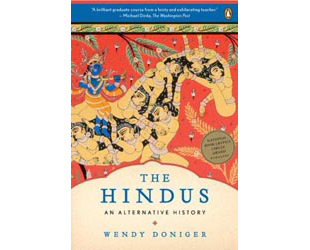कोई भारतीय सबसे पहले अमेरिका कब पहुंचा, इस सवाल का जवाब दो सदी से भी लंबी दूरी तय करता हुआ हमें 1790 तक पहुंचाता है. इसी साल अमेरिका के पूर्वी प्रांत मैसाच्यूसेट्स के तटीय कस्बे सेलेम में एक भारतीय दिखाई दिया था. यह जानकारी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर द्वारा संपादित और 1982 में प्रकाशित किताब फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका में मिलती है–इस संभावना के साथ कि भारतीय उपमहाद्वीप का वह यात्री किसी मालवाहक जहाज के साथ वहां पहुंचा होगा. सूचना के महासागर गूगल सर्च पर काफी वक्त बिताने के बाद भी उससे जुड़ी और कोई जानकारी नहीं मिलती.
लेकिन इसी गूगल सर्च पर सत्या नाडेला टाइप करें तो पल भर में ही जानकारी का महाद्वीप उभर आता है. सर्च इंजन तुरंत ही बताता है कि उसके पास इस नाम से जुड़े करीब 17 करोड़ खोज परिणाम हैं. भारत में पले-बढ़े नाडेला ने हाल ही में आईटी जगत की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कमान संभाली है. संयोग देखिए कि महीना भर पहले तक जब माइक्रोसॉफ्ट के अगले मुखिया के बारे में कयास लग रहे थे तो एक और भारतीय सुंदर पिचाई की भी बड़ी चर्चा हो रही थी. पिचाई उसी गूगल के शीर्ष प्रबंधन में शामिल हैं जिसका सर्च इंजन नाडेला से जुड़े 17 करोड़ खोज परिणाम देता है.
करीब दो सदियों के सिरे पर खड़े ये उदाहरण दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका में भारतीयों की यात्रा के ओर- छोर भी बनाते हैं. इनमें से एक छोर का रिश्ता महत्वहीनता और गुमनामी से जुड़ता है तो दूसरे का अहमियत और प्रसिद्धि से. नाडेला अमेरिका जा बसे भारतीयों की सफलता के सिलसिले की सबसे नई और बड़ी कड़ी हैं. इस सूची में एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, पेप्सी की कमान थाम रहीं इंद्रा नूयी, मास्टरकार्ड के मुखिया अजय बंगा, लुजियाना के गवर्नर पीयूष बाबी जिंदल और 2014 की मिस अमेरिका नीना दावुलूरी जैसे कई नाम मिलते हैं.
2010 की अमेरिकी जनगणना बताती है कि अमेरिका की करीब 30 करोड़ की आबादी में लगभग चार करोड़ अप्रवासी हैं. उनमें से करीब 28 लाख भारतीय मूल के हैं. यह संख्या कुल आबादी के एक फीसदी से भी कम है. लेकिन यह तथ्य तब चौंकाने लगता है जब पता चलता है कि इस छोटी-सी आबादी की उपलब्धियां इससे कई गुना ज्यादा हैं. चर्चित पत्रिका फोर्ब्स के एक हालिया लेख में जोसेफ रिशवाइन लिखते हैं कि आबादी का एक फीसदी से भी कम होने के बावजूद भारतीय अमेरिका के कुल इंजीनियरों का तीन फीसदी हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का वे सात फीसदी हैं तो डॉक्टरों का आठ फीसदी. यानी औसत अमेरिकी की बात करें तो उसके लिए किसी सड़क से गुजरता कोई आदमी भारतीय है इससे आठ गुना ज्यादा संभावना इस बात की है कि उसका डॉक्टर भारतीय हो.’
लेकिन जैसा कि हर सुखांत कथा में होता है, महत्वहीन से महत्वपूर्ण होने तक के इस सफर में भी मुश्किलों और संघर्ष के कई मोड़ हैं. और कुछ अहम सबक भी.
1790 के बाद अमेरिका में भारतीयों का जिक्र 1851 की एक घटना में मिलता है. उस साल चार जुलाई यानी अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेलेम में हुई परेड में छह भारतीयों ने भी हिस्सा लिया था. छोटी-छोटी बूंदों के रूप में वे आते गए और 19वीं सदी खत्म होते-होते अलग-अलग अनुमानों के मुताबिक अमेरिका में करीब 2000 भारतीय बस चुके थे. मुख्य रूप से कैलीफोर्निया जैसे पश्चिमी हिस्सों में रहने वाले इन लोगों में से ज्यादातर पंजाब से आए सिख थे और उन्हें खेती, कारखानों और रेल या सड़क से जुड़े निर्माण कार्यों में रोजगार मिला हुआ था. 20 वीं सदी के शुरुआती दशक में भारतीयों की यह संख्या और भी तेजी से बढ़ी. 1901 से लेकर 1911 तक के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि तब तक अमेरिका में कानूनी रूप से 6,250 भारतीयों को प्रवेश मिल चुका था. लेकिन गैरकानूनी रूप से रहने वाले भारतीयों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी. दरअसल अमेरिका के ही पड़ोस में स्थित कनाडा ब्रिटिश उपनिवेश था. वहां जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि भारत भी तब तक ब्रिटिश अधिकार में ही था. कनाडा आने के बाद अमेरिका में घुस जाना आसान था. इसलिए अमेरिका में भारतीयों की वास्तविक संख्या उनकी आधिकारिक संख्या से कहीं ज्यादा हो गई थी.
 यहीं से मुश्किल शुरू हुई. भारतीय ही नहीं बल्कि एशिया के दूसरे देशों जैसे चीन, कोरिया और जापान से भी बड़ी संख्या में लोग अमेरिका आने लगे थे. अपने काम में कुशल ये एशियाई ही अपनी-अपनी जड़ें छोड़कर सात समुंदर पार आए थे–सिर्फ इसलिए कि उनमें नए अवसर खोजने और उन्हें भुनाकर सफल होने की भूख थी. स्वाभाविक ही था कि वे कम पैसे में ज्यादा काम करने के लिए तैयार रहते थे. इसलिए काम देने वालों में उनकी पूछ भी बढ़ रही थी. यही वजह थी कि स्थानीय श्वेत समाज में धीरे-धीरे इनके खिलाफ असंतोष पनपने लगा. सामाजिक दबाव बढ़ा तो 1882 में आए चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट के साथ ऐसे कानूनों और अदालती फैसलों की शुरुआत हुई जो भारत सहित तमाम एशियाई देशों के लोगों को या तो अमेरिका आने से रोकते थे या पहले से वहां रह रहे लोगों को नागरिकता सहित दूसरे मूलभूत अधिकारों से वंचित करते थे.
यहीं से मुश्किल शुरू हुई. भारतीय ही नहीं बल्कि एशिया के दूसरे देशों जैसे चीन, कोरिया और जापान से भी बड़ी संख्या में लोग अमेरिका आने लगे थे. अपने काम में कुशल ये एशियाई ही अपनी-अपनी जड़ें छोड़कर सात समुंदर पार आए थे–सिर्फ इसलिए कि उनमें नए अवसर खोजने और उन्हें भुनाकर सफल होने की भूख थी. स्वाभाविक ही था कि वे कम पैसे में ज्यादा काम करने के लिए तैयार रहते थे. इसलिए काम देने वालों में उनकी पूछ भी बढ़ रही थी. यही वजह थी कि स्थानीय श्वेत समाज में धीरे-धीरे इनके खिलाफ असंतोष पनपने लगा. सामाजिक दबाव बढ़ा तो 1882 में आए चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट के साथ ऐसे कानूनों और अदालती फैसलों की शुरुआत हुई जो भारत सहित तमाम एशियाई देशों के लोगों को या तो अमेरिका आने से रोकते थे या पहले से वहां रह रहे लोगों को नागरिकता सहित दूसरे मूलभूत अधिकारों से वंचित करते थे.
एक तरफ कानून का कहर था तो दूसरी तरफ स्थानीय समाज की नफरत. अपने एक लेख में न्यूयॉर्क स्थित संगठन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह लिखते हैं, ‘शुरुआती भारतीयों में से ज्यादातर सिख थे. उनके सिर की पगड़ी की वजह से उन्हें अपमानजनक लहजे में रैगहेड्स कहा जाता था. उसी दौर में अमेरिका में एक एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग भी हुआ करती थी जो अमेरिका में हिंदुओं (तब भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोगों को हिंदू कहकर ही पुकारा जाता था) के खिलाफ दुष्प्रचार करती थी और मीडिया पर उनके खिलाफ लिखने का दबाव बनाती थी. 1907 में वाशिंगटन के बेलिंघम कस्बे में हुई एक घटना में करीब 500 लोगों की भीड़ ने वहां के बोर्डिंग हाउसों और कारखानों में घुसकर करीब 300 भारतीयों को नौकरी और कस्बा छोड़ने पर मजबूर कर दिया. पुलिस की भी उनके सामने एक न चली.’
फिर भी ये भारतीय अपने हक के लिए लड़ते रहे, सरकार पर नागरिकता के लिए दबाव बनाते रहे. लेकिन यह तभी संभव हो सकता था जब संसद में इसके लिए कानून लाया जाता. 1946 में यह संभव हुआ. राष्ट्रपति हैरी एस ट्रुमन ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और संसद ने ल्यूस-सैलर नामक बिल पर मुहर लगा दी. इसके बाद अमेरिका में रह रहे इन भारतीयों को नागरिकता का हक तो मिला ही, उन्हें कुछ और भी फायदे हुए. जैसे अब वे भारत जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को अमेरिका ला सकते थे. हर साल 100 लोग भारत से कानूनी रूप से अमेरिका आकर नागरिकता भी पा सकते थे. यह भारतीय अमेरिकियों की पहली विजय थी. इससे कुछ रास्ते खुले. इसके लिए दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले दिलीप सिंह सौंद 1957 में एक डेमोक्रेट के रूप में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पहले भारतीय सदस्य बने.
इसके बाद 1965 में बना इमिग्रेशन एेंड नेशनैलिटी एक्ट तो जैसे भारतीयों के लिए अवसरों की बाढ़ लेकर आया. इसके मुताबिक अमेरिका आने और नागरिकता प्राप्त करने के लिए हर देश का 20000 सालाना कोटा तय कर दिया गया. वैसे यह कानून बनाना उसकी मजबूरी बन गई थी. दरअसल वह अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलनों का दौर था. वहां और दुनिया भर में सवाल किए जा रहे थे कि फ्रीडम और लिबर्टी फॉर ऑल की बात करने वाले देश की सोच इतनी संकरी क्यों है कि वह अपने यहां रहने वाली एक बड़ी अश्वेत आबादी को उसका जायज हक नहीं दे रहा. अपने लेख में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया में इतिहास के अध्यापक विनय लाल लिखते हैं, ‘1965 से अमेरिका में भारतीयों के समकालीन इतिहास का सबसे नया दौर शुरू होता है.’ ये लोग शिक्षित थे, कुशल थे और अपनी योग्यता का अधिकतम इस्तेमाल करना चाहते थे. वे अमेरिका में भारतीय आबादी की दूसरी लहर जैसे थे. उनका लक्ष्य भी वही था जो उनसे पहले वाली पीढ़ी का था. यानी सफल होना. लेकिन वे इस मायने में अलग थे कि उनके पास नए ज्ञान की शक्ति थी. आइआइटी सहित दूसरे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों से निकली ये प्रतिभाएं अपने देश में उचित अवसरों की कमी और लालफीताशाही से त्रस्त होकर अमेरिका पहुंची थीं.
हालांकि मुश्किलें उनके लिए भी कम नहीं थीं. तब तक भले ही. रवींद्रनाथ टैगोर अपनी साहिित्यक और सीवी रमन अपनी वैज्ञानिक मेधा के लिए नोबेल जीत चुके थे, लेकिन अमेरिका में भारतीयों की छवि काफी कुछ 1927 में आए कैथरीन मायो के मदर इंडिया उपन्यास जनित ही थी–सांप-संपेरों, भालू-मदारियों और गंदगी से उफन रहे एक ऐसे देश के लोग जो अपना पेट तक ठीक से नहीं भर सकते. अपने एक लेख में चर्चित अमेरिकी-भारतीय उद्यमी कंवल रेखी कहते हैं, ‘कोई भारतीय किसी अमेरिकन कंपनी का मुखिया बनेगा यह सोचना 1967 में असंभव था जब मैं वहां पहुंचा था.’ फोर्ब्स में छपे एक लेख में स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता निशा बापट लिखती हैं, ‘ 50 या 60 के दशक के दौरान अमेरिका में जो चंद भारतीय मिलते थे वे कंपनी में निचले स्तरों पर काम करने वाले कुछ ऐसे इंजीनियर होते थे जो अमेरिका पढ़ने आए और वहीं रह गए. भारतीयों की आम छवि भिखारियों और संपेरों की थी. अमेरिका में शीर्ष पदों पर उनके होने की कल्पना तो बहुत दूर की कौड़ी ही थी.’
लेकिन 1965 के बाद जब धीरे-धीरे बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहां पहुंचने लगे और न सिर्फ अपने रंग-रूप बल्कि अपनी मेधा की वजह से भी वहां के आम छात्रों से अलग पहचाने जाने लगे तो यह छवि बदलने लगी. जैसा कि रेखी कहते हैं, ’70 के दशक के शुरुआती वर्षों तक अमेरिका थोड़ा शिकायती लहजे में ही सही पर मानने लग गए थे कि उनमें कुछ तो खास है. इन आरंभिक युवाओं में से कई डॉक्टरेट कर गए. सफलता की शुरुआत प्रोफेसर जैसे पदों के साथ हुई.’ धीरे-धीरे इन छात्रों को उद्योग जगत में अच्छी नौकरियां भी मिलती गईं.. भारतीयों को उनकी गणितीय कुशलता की वजह से अच्छे इंजीनियरों और प्रोग्रामरों के रूप में पहचाना जाने लगा. धीरे-धीरे भारत के मेडिकल स्कूलों और बिजनेस स्कूलों से निकली प्रतिभाएं भी वहां पहुंचने लगीं और डॉक्टर या वित्तीय प्रोफेशनल के तौर पर सफल होने लगीं. 1980 के दशक में भारतीय उद्यमी भी बन गए. रेखी कहते हैं, ‘ सिलिकॉन वैली जहां दुनिया भर की प्रतिभाएं इकट्ठा हो रही थीं, ऐसी सफलताओं का केंद्र बन गई. भारतीयों ने यहां कई असाधारण उपलब्धियां अर्जित कीं.’ फिर 1990 का दशक आया जिसे सिलिकॉन वैली में भारतीयों का स्वर्णकाल कहा जाता है. पेंटियम चिप के जनक कहे जाने वाले विनोद धाम, सन माइक्रोसिस्टम्स के सहसंस्थापक विनोद खोसला, गूगल के शुरुआती निवेशक और वर्तमान में इसके बोर्ड मेंबर केआर श्रीराम और हॉटमेल के सबीर भाटिया जैसे कई नामों की अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा हुई.
लेकिन तब भी अमेरिका में आम धारणा यह थी कि भारतीय बड़ी कंपनियों के सीईओ नहीं बन सकते. 21 वीं सदी के पहले दशक ने यह धारणा भी ढहा दी. 2004 में आरईसी राउरकेला से पढ़े सूर्या महापात्रा फॉर्च्यून 500 में आने वाली कंपनियों में से एक क्वेस्ट डॉयाग्नोस्टिक्स के सीईओ बने. 2006 में इंद्रा कृष्णमूर्ति नूयी ने पेप्सी की कमान संभाली. इस सूची में सिटीबैंक के विक्रम पंडित, काग्निजेंट के फ्रैंक डिसूजा, स्कैनडिस्क के संजय मेहरोत्रा जैसे कई नाम जुड़ते गए और सत्या नाडेला ने तो इस मोर्चे पर अब तक की सबसे बड़ी गूंज पैदा की है.
अमेरिका स्थित यूसी-बर्कले स्कूल ऑफ इनफॉर्मेशन के डीन एन्ना ली सक्सेनियन ने 1999 में एक अध्ययन किया था. पता चला कि 1980 से 1998 के बीच सिलिकॉन वैली में जो नई कंपनियां स्थापित हुई उनमें सात फीसदी भारत में जन्मे उद्यमियों ने शुरू की थीं. सक्सेनियन ने इसके आठ साल बाद यानी 2007 में ड्यूक यूनिवर्सिटी में शोध निदेशक प्रोफेसर विवेक बाधवा और स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर एफ डैनियल सिसिलियानो के साथ मिलकर एक अध्ययन किया. नतीजे चौंकाने वाले थे. पता चला कि सिलिकान वैली में चल रही कंपनियों में से 13.4 फीसदी भारतीयों की हैं और पूरे अमेरिका के लिए यह आंकड़ा 6.5 फीसदी है. अमेरिका में दूसरे सात अल्पसंख्यक समूहों को मिला दें तो भी भारतीय उनसे आगे हैं. बाहर से आए लोगों द्वारा अमेरिका में शुरू किए कुल उद्यमों से से 33.2 फीसदी हिस्सा भारतीयों का है. दिलचस्प यह भी है कि 2008 की मंदी और अमेरिका की जटिल आव्रजन नीति के चलते बीते कुछ समय के दौरान ऐसे उद्यमों और उद्यमियों का आंकड़ा गिरा है, लेकिन भारतीय तब भी धारा के विपरीत चलने में सफल रहे हैं. 2007 से भारतीयों द्वारा शुरू की गई कंपनियों का आंकड़ा 13.04 से बढ़कर 14 फीसदी हुआ है. यूएस सेंसस ब्यूरो के कुछ समय पहले के एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में करीब तीन लाख कंपनियां हैं जो भारतीय अमेरिकियों की हैं. इन कंपनियों में करीब साढ़े आठ लाख लोगों को रोजगार और उन्हें सालाना करीब 26 अरब डॉलर वेतन के रूप में मिलते हैं.
क्या है वजह
आखिर क्या वजह है कि अमेरिका में भारतीय वहां बसे चीनियों या रूसियों से इतना आगे हैं. कई जानकार मानते हैं कि उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उन्हें दूसरों की तुलना में बढ़त देती है. विवेक वाधवा कहते हैं, ‘भारतीयों को अपनी विरासत का फायदा मिलता है, वे अंग्रेजी बोलते हैं और एक लोकतांत्रिक समाज से आते हैं. अमेरिका की तरह भारतीय भी अपनी सरकार की आलोचना के लिए स्वतंत्र होते हैं. इसीलिए उनमें आजादख्याली का एक अहम गुण होता है.’ वे आगे जोड़ते हैं, ‘सांस्कृतिक रूप से अमेरिकी और भारतीय समान हैं और यही खासियत उन्हें दूसरे देशों के लोगों की तुलना में फायदा देती है. जब वे अमेरिका आते हैं तो तुरंत फिट हो जाते हैं.’ वाधवा कहते हैं, ‘चीन में आप सरकार की आलोचना की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि आपको अगले दिन उठा लिया जाए. आम चीनी अथॉरिटी से आतंकित रहता है. जो सत्ता के सख्त बंधन वाले देशों से आते हैं वे नियमों के परे जाने से डरते हैं. जबकि उद्यमी बनने के लिए आपको नियम तोड़ने का जोखिम उठाना होता है.’
एक और कारण यह भी है कि अमेरिका आने वाले भारतीय युवा एक तरह से प्रतिभाओं का सबसे ऊंचा स्तर होते हैं. सिलिकॉन वैली के अनुभवी पेशेवर और सिंफनी टेक्नॉलॉजी ग्रुप के संस्थापक रोमेश वाधवानी अपने एक लेख में कहते हैं, ‘भारत से अमेरिका आने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या पहले ही एक कठिन परीक्षा से गुजरकर अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी होती है. आईआईटी सहित कई दूसरे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों से यहां आए हम लोग डार्विन के श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता वाले सिद्धांत के तहत आगे बढ़े हैं.’ विवेक वाधवा इसकी वजह उस नेटवर्क को भी बताते हैं जो शुरुआत में वहां सफल होने वाले भारतीयों ने अगली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए बनाया. वे कहते हैं, ’30 साल पहले जब भारतीयों को सिलिकॉन वैली में शुरुआती सफलताएं मिलीं तो उन्होंने खास तौर पर इस मकसद से संस्थाएं बनाईं और सफल उद्यमियों की एक दूसरी पीढ़ी खड़ा होने में अहम योगदान दिया.’
एक अहम वजह यह भी है कि अपना धंधा जोड़ना भारतीय समाज में एक प्रतिष्ठा की बात समझी जाती है. यह एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति है. वाधवा कहते हैं, ‘इसके लिए भारत में सामाजिक प्रोत्साहन मिलता है.’ समाज की भूमिका यहीं सीमित नहीं होती. भारतीय समाज में अकादमिक उपलब्धि पर भी बहुत जोर होता है क्योंकि पारंपरिक रूप से वहां ज्ञान सबसे बड़ा गुण माना जाता रहा है. अमेरिका में होने वाली स्पेलिंग प्रतियोगिताओं में अगर भारतीय बच्चे चैंपियन हैं तो उन्हें दिन में कई घंटे पढ़ना पड़ता है और शब्द व उनकी उत्पत्ति का विज्ञान याद करना पड़ता है. इसमें दूसरी चीजों से कहीं ज्यादा बौद्धिक स्तर पर दूसरों से आगे आने का रोमांच होता है.
लेकिन साधारण से अति असाधारण बनने के लिए शिक्षा और संस्कृति ही काफी नहीं. प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा होनी भी जरूरी है. आपकी बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू स्वाभाविक रूप से औरों से ज्यादा होनी चाहिए. आपका दिमाग सहज ही औरों से ज्यादा परिष्कृत होना चाहिए. करीब एक दशक पहले प्रिंसटन युनिर्सिटी ने अपने एक सर्वे यानी न्यू इमिग्रेंट नामक सर्वे में पाया था कि अप्रवासी भारतीयों का औसत आईक्यू न सिर्फ अमेरिकियों से बल्कि बुद्धिमान कहे जाने वाले अश्केनाजी यहूदी समुदाय से भी ज्यादा होता है. हालांकि छोटे-से सैंपल साइज और इसकी पुष्टि करते किसी अध्ययन की गैरमौजूदगी में इस निष्कर्ष पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन भारतीयों की जो उपलब्धियां देखी जा रही हैं वे तो इसे वजन देती ही लगती हैं.
अपनी शिक्षा, सामाजिक संस्कृति और संभावित सहज प्रतिभा के बूते भारतीय अमेरिकी अमेरिका में एक आर्थिक ताकत बन चुके हैं. क्या वे राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसी ही सफलता हासिल कर पाएंगे? क्या गवर्नर जिंदल जैसे उदाहरण आगे और भी हो सकते हैं? जानकारों के मुताबिक यह इस पर निर्भर करेगा कि वे उन क्षेत्रों में कितनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा पाते हैं जिन्हें राजनीतिक करियर के लिहाज से अहम माना जाता है. रिशवाइन कहते हैं, ‘अमेरिका में राजनीतिक करियर के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र हैं लॉ और फायनैंस. यहां अभी भारतीयों का प्रभाव उतना नहीं है.’
लेकिन बाकी क्षेत्रों में उन्होंने जो प्रभाव पैदा किया है उसने बीती एक सदी के दौरान भारतीयों की आम छवि बिलकुल बदल दी है. रेखी कहते हैं, ‘आज अमेरिका में भारतीयों को एक आदर्श की तरह देखा जाता है जो जीवन के अच्छे पहलुओं को देखते हैं और परिवार को समय देते हैं. एक औसत अमेरिकी आज उन्हें क्लास में सबसे तेज बच्चे, यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छे प्रोफेसर और अस्पताल में सबसे बढ़िया डॉक्टर की तरह देखता है. ‘
अमेरिका में भारतीयों के करीब डेढ़ सदी लंबे सफर का एक अहम सबक यह भी है कि उदारता की तरफ बढ़ने वाले समाज की ताकत भी बढ़ती रहती है.






 प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मांग तथा इन पर पार्टी की प्रतिक्रियाएं दो अहम सवालों को जन्म देती हैं. पहला यह कि आखिर प्रियंका गांधी के राजनीति में आने की मांग समय-समय पर क्यों उठती रही है? और दूसरा यह कि इसके बावजूद प्रियंका को खुल कर राजनीति के मैदान में न उतारने की वजह क्या है?
प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मांग तथा इन पर पार्टी की प्रतिक्रियाएं दो अहम सवालों को जन्म देती हैं. पहला यह कि आखिर प्रियंका गांधी के राजनीति में आने की मांग समय-समय पर क्यों उठती रही है? और दूसरा यह कि इसके बावजूद प्रियंका को खुल कर राजनीति के मैदान में न उतारने की वजह क्या है?