[wzslider autoplay=”true” transition=”‘slide'” info=”true” lightbox=”true”]
सारा हैकान्सन सिर्फ दो साल की एक बच्ची है. सितंबर, 2013 में वह सारे स्वीडन में चर्चा का विषय बन गई. हुआ यह कि अगस्त, 2011 में, जब वह मात्र तीन महीने का नवजात शिशु थी, उसका नाम पुलिस के एक गोपनीय डाटाबैंक में दर्ज हो गया. डाटाबैंक के सभी पांच हजार नाम रोमा कहलाने वाले जातीय अल्पसंख्यकों के हैं. उन्होंने कुछ किया नहीं था. उनका रोमा होना ही काफी था. भारतीय मूल वाली लगभग 40 हजार जनसंख्या की यह बिरादरी पिछले 500 वर्षों से स्वीडन में रह रही है.
स्वीडिश दैनिक ‘दागेन न्यिहेतर’ ने ‘घुमंतू जन’ शीर्षक वाले इस डाटाबैंक का रहस्योद्घाटन किया था. पुलिस ने पहले तो इस डाटाबैंक के अस्तित्व से ही इंकार कर दिया. बाद में उसने कहा कि यह अपराधों की रोकथाम के विश्लेषण में काम आता है. उसमें संबद्ध व्यक्ति के 19वीं सदी तक के पूर्वजों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है. अखबार ने एक और डाटाबैंक खोज निकाला. उसमें 10 साल से कम के 106 बच्चों सहित 997 रोमा लोगों का विवरण दर्ज था. याद रहे कि नोबेल पुरस्कारों का देश स्वीडन संसार के सबसे खुशहाल, सुशासित और भ्रष्टाचार-मुक्त कल्याणकारी देशों में गिना जाता है.
15 साल की लेओनार्दा दिब्रानी नौ अक्टूबर, 2013 को, पूर्वी फ्रांस के लेवियेर में अपने स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रही थी. पुलिस ने स्कूल-बस रास्ते में ही रोक ली. लेओनार्दा को बलपूर्वक बस से उतार लिया गया और तुरंत ही उसे शेष परिवार के साथ कोसोवो भेज दिया गया. लेओनार्दा का रोमा का परिवार कोसोवो से ही आया था और पांच साल से फ्रांस में शरण लेने की कोशिशें कर रहा था. किस्सा यहीं खत्म हो जाता. लेकिन, हजारों छात्रों ने लेआनार्दा के निष्कासन के विरुद्ध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. मामला तूल पकड़ने लगा. मीडिया ने भी सरकारी निष्ठुरता को आड़े हाथों लिया. बात यहां तक पहुंची कि राष्ट्रपति फ्रोंस्वा ओलांद को, 20 अक्टूबर के दिन, टेलीविजन पर कहना पड़ा कि लेओनार्दा यदि चाहे तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ‘अकेले’ वापस आ सकती है. कोसोवो से लेओनार्दा का दो टूक उत्तर आया, ‘मैं अकेले फ्रांस वापस नहीं जाऊंगी, अपने परिवार को नहीं छोडूं़गी.’
सिर्फ 18 लाख जनसंख्या वाला मुस्लिम देश कोसोवो यूरोपीय संघ और पश्चिमी देशों के ‘नाटो’ सैन्य संगठन की सहायता से बना यूरोप का सबसे नया देश है. फरवरी, 2008 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा से पहले वह सर्बिया का, और 1990 वाले दशक में यूगोस्लाविया के विघटन से पहले सर्बिया यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था. 1999 में यूरोपीय संघ और नाटो की मदद से कोसोवो का कथित स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने पर वहां रह रहे एक लाख 20 हजार रोमा अल्पसंख्यकों में से ज्यादातर को भाग कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है.
कभी भारत से आए और पूर्वी यूरोप के देशों में सदियों से रहने वाले लाखों रोमा लोगों का जीना इन दिनों दूभर है. इन देशों की बहुमत जनसंख्या उन्हें ही अपने हर क्षोभ का कोपभाजन बनाती है. हर चोरी में, खासकर बच्चों के गायब होने में उन्हीं का हाथ देखा जाता है. नवंबर के शुरुआत में यूनान और आयरलैंड में पुलिस ने गोरे-चिट्टे रंग और सुनहले बालों वाले बच्चों को उनके घरवालों से इसलिए छीन लिया कि घरवाले रोमा थे. रोमा बच्चे आम तौर पर बहुत गोरे नहीं होते, इसलिए पू्र्वाग्रह-ग्रस्त पुलिस ने मान लिया कि ये गोरे बच्चे जरूर कहीं से चुराए गए हैं. लेकिन, डीएनए जांच ने दोनों मामलों में पुलिस को गलत ठहराया.
इस्तवान पिसोंत फुटबॉल खिलाड़ी था. उस की गणना हंगरी के सबसे होनहार फुटबॉल खिलाड़ियों में हुआ करती थी. 1980 वाले दशक में वह ‘होनवेद बुडापेस्ट’ क्लब के लिए खेला करता था. वह खेल-समीक्षकों से लेकर दर्शकों तक का दुलारा था. अपनी प्रसिद्धि को अपनी सिद्धि मान बैठा. 18 साल का होते ही एक टेलीविजन इंटरव्यू में कह बैठा कि उसके माता-पिता ‘रोमा’ हैं. इसके बाद तो वह फुटबॉल प्रेमियों की नजरों में ऐसा गिरा कि हीरो से जीरो बन गया. भद्दी फब्तियां कसी जानें लगीं, ‘साला बंजारा है…बंजारा…’ इस्तवान पिसोंत अपने देश के दर्शकों से दुखी होते हुए भी राष्ट्रीय ही नहीं, 31 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी खेल चुका है. कहता है, ‘हंगरी के कई नामी फुटबॉल खिलाड़ी रोमा हैं. पर, अपने अपमान और तिरस्कार के डर से वे कभी यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रोमा बंजारों की है.’ हंगरी की करीब एक करोड़ की जनसंख्या में छह लाख रोमा हैं. उनके नाच-गाने तो पसंद किए जाते हैं, पर आए दिन हमले होना, उनके घर-बार जला देना और पुलिस द्वारा उन्हें तंग करना भी आम बात है. वहां के दक्षिणपंथी अतिवादी 2007 के बाद से 10 रोमा लोगों की हत्या कर चुके हैं.
लोकतंत्र में रोमा संत्रस्त
दो दशक पूर्व पूर्वी यूरोप की कम्युनिस्ट सरकारों के पतन के बाद से लोकतंत्र बन गए वहां के हंगरी और रोमानिया से लेकर स्लोवाकिया और चेक गणराज्य तक डेढ़ दर्जन देशों में भारतीय पूर्वजों की संतान रोमा लोगों की हालत बद से बदतर होती गई है. अपने आप को लोकतंत्र और कानून के राज का आदर्श नमूना मानने वाले जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली या स्वीडन जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी रोमा लोगों के लिए वह सामाजिक मान्यता व समानता सपना ही है जो इस बीच समलैंगिकों तक को पूरे आदर-सम्मान के साथ मिलने लगी है.
मुख्य रूप से जर्मन-भाषी देशों में सिंती कहलाने वाले लोग भी रोमा बिरादरी की ही एक उपजाति हैं. पर, वे रोमा हैं या सिंती हैं, पूर्वी यूरोप में हैं या पश्चिमी यूरोप में, निपट गरीब ही हैं. अनपढ़ हैं. बदनाम कर दिए गए हैं कि भीख मांगने या चोरी-उठाईगीरी करने के सिवा कुछ नहीं जानते. उन्हें पास-पड़ोस में फटकने तक नहीं दिया जाता. उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है. न कोई घर-द्वार मिलता है और न नौकरी-धंधा. यह सब पहले भी था. लेकिन, जब से पू्र्वी यूरोप के भूतपूर्व समाजवादी देशों में ‘लोकतंत्र’ आया है, तब से उनका अपमान और तिरस्कार पराकाष्ठा पर है. नौबत यहां तक आ गई है कि पू्र्वी यूरोपीय देशों के हजारों रोमा अपने साथ नस्लवादी भेदभाव, अपनी गरीबी और मजबूरी से तंग आ कर पश्चिमी यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड या बेल्जियम जैसे देशों में शरण मांगने लगे हैं. पर, कोई देश उन्हें शरण नहीं देना चाहता. भारत जैसे देशों को गाहे-बगाहे अल्पसंख्यकों के साथ न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा का उपदेश देने वाले यूरोपीय देश, अपने सारे आदर्श भुला कर, रोमा लोगों को निकाल बाहर करने की ही जुगाड़ में रहते हैं. फ्रांस के पू्र्व राष्ट्रपति निकोला सार्कोजी ने तो वहां 2012 वाले चुनावों से पहले अवसरवादिता की हद ही कर दी. उन्होंने रोमानिया से आए हजारों रोमा शरणार्थियों को यह सोच कर बैरंग वापस भेज दिया कि इससे फ्रांसिसी जनता बाग-बाग हो जाएगी और चुनाव में जीत पक्की हो जाएगी. हालांकि वे चुनाव फिर भी हार गए. जर्मनी के कुछ राजनेता भी शोर मचा रहे हैं कि देश भिखमंगे व जेबकतरे रोमा शरणार्थियों से भरता जा रहा है.
जर्मनी का रोमा इतिहास
जर्मनी का इतिहास यहूदियों के ही नहीं, रोमा और सिंती जनों के खून से भी सना हुआ है. हिटलर की तानाशाही के समय यूरोप के 60 लाख यहूदियों के जातिसंहार के पाप का प्रायश्चित करते रहना जर्मनी में शाश्वत राजधर्म बन गया है. लेकिन, इस बात पर यथासंभव पर्दा ही डाला जाता रहा है कि हिटलर के आदेश पर, यहूदियों की ही तरह, यूरोप भर में पांच लाख रोमा और सिंती भी मौत के घाट उतार दिए गए थे. आम जर्मनों की नजर में रोमा और सिंती, आज भी, कहीं न टिकने वाले घुमंतू बंजारे ही हैं. उनके लिए ‘त्सिगोएनर’ (बंजारे) या ‘फ़ारन्डे फ़ोल्क’ (घुमंतू जाति) जैसे हिकारत भरे शब्द आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं.
‘त्सिगोएनर’ नाम से ही जर्मनी में पहली बार 1407 में हिल्डेसहाइम नगर के इतिहास में उनका उल्लेख मिलता है. शुरू में उन्हें तत्कालीन रजवाड़ों और सामंतों का संरक्षण भी मिला हुआ था, क्योंकि वे अच्छे हस्तशिल्पी, वाद्ययंत्र-निर्माता और आज्ञाकारी सैनिक हुआ करते थे. लेकिन 15वीं सदी का अंत आते-आते उनका व्यापक शोषण और दमन होने लगा. स्थानीय जर्मन हस्तशिल्पी उनसे जलने लगे. उन्हें गांवों-शहरों से दूर भागने के लिए विवश किया जाने लगा. ईसाई धर्माधिकारियों को भी यह पसंद नहीं था कि वे गैर-ईसाई देवी-देवताओं को पूजते थे. उनकी औरतें टोने-टोटके व भविष्यवाणियां करती थीं. लिंदाऊ और फ्राइबुर्ग के तत्कालीन शासकों ने तो यहां तक आदेश दे दिया कि जिसे अपनी जमीन-जायदाद पर कोई बंजारा दिखाई पड़ जाए, वह उसे मौत के घाट उतार सकता है. 1589 से तत्कालीन जर्मनी के कई प्रदेशों में पुलिस को यह अधिकार था कि वह बंजारों का माल-सामान छीन कर उन्हें खदेड़ बाहर कर सकती है. इस तरह उन्हें दर-दर भटकने और खानाबदोशों की तरह रहने पर मजबूर होना पड़ा.
वे बच्चे उठा ले जाते हैं
18वीं-19वीं सदी में यूरोप के जर्मन-भाषी क्षेत्रों में उन्हें एक जगह टिकाने-बसाने का विफल प्रयास भी हुआ. विफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि तत्कालीन ऑस्ट्रिया में, 1773 के बाद से, रोमा-सिंती बंजारों के बच्चों को उनसे छीन कर कोई रोजगार सिखाना और बाद में सेना में भर्ती किया जाने लगा. इससे होता यह कि बच्चे अपने माता-पिता के पारंपरिक हस्तशिल्पों से कट जाते और उन पर माता-पिता के संस्कारों की छाप भी नहीं पड़ती. चूंकि माता-पिता को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए बाल-शिविरों से वे अपने बच्चों को भगा ले जाते थे. प्रचारित कर दिया गया कि वे तो बच्चों का अपहरण करके उन्हें उठा ले जाते हैं. यह मान्यता एक रूढ़ि बन कर सारे यूरोप मंे आज भी जीवित है.
पूर्वी यूरोप के देशों में रोमा बंधुआ मजदूरों और गुलामों की तरह रखे व बेचे-खरीदे भी जाते थे. उनकी पहचान करने के लिए मवेशियों की तरह तपते लोहे से उन्हें दागा जाता था. साढ़े चार सौ वर्षों से चल रही इस दास प्रथा का अंत 1864 में रोमानिया और बुल्गारिया द्वारा उसे त्याग देने के साथ हुआ. दास प्रथा से मुक्त हुए रोमा जर्मनी जैसे पश्चिमी यूरोप के देशों में रहने-बसने की कोशिश करने लगे, पर हर जगह वे दुत्कारे ही जाते थे. जर्मनी में रह रहे रोमा या सिंती लोगों का 1899 से पंजीकरण शुरू कर दिया गया. इसी पंजीकरण के बल पर हिटलर के शासनकाल में उन्हें चुन-चुन कर पकड़ा गया, गोलियों से उड़ा दिया गया या फिर यहूदियों के साथ-साथ उन्हें भी यातना शिविरों की गैस-भट्ठियों में ठूंस कर मार डाला गया.
हिटलर की बलि चढ़े पांच लाख रोमा
हाल ही में प्रकाशित खोजपूर्ण पुस्तकों के अनुसार, हिटलर के शासनकाल में जर्मनी में करीब 30 हजार रोमा और सिंती रहते थे. उनमें से 90 प्रतिशत औरतों, बच्चों और मर्दों को यातना शिविरों में मौत के घाट उतार दिया गया. यही हाल जर्मनी से बाहर यूरोप के उन देशों के रोमा और सिंतियों का भी हुआ, जिन पर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हिटलर की सेना ने कब्जा कर लिया था. उनकी संख्या करीब पांच लाख आंकी जाती है.
अखिल जर्मन सिंती एवं रोमा केंद्रीय परिषद जर्मनी में रोमा व सिंती लोगों की मान्यता प्राप्त देशव्यापी प्रतिनिधि संस्था है. इसका काम है रोमा और सिंती संस्कृति का संरक्षण और प्रोत्साहन. इसके अध्यक्ष रोमानी रोजे के अपने परिवार के भी 13 सदस्य हिटलर के शासनकाल वाले आउश्वित्स और रावेंसब्रुइक यातना शिविरों में मौत के घाट उतार दिए गए थे. तब भी वे आज के जर्मनी में रोमा बिरादरी की रोजमर्रा जिंदगी को, सारी कमियों और विरोधाभासों के बावजूद कहीं बेहतर बताते हैं. तहलका के लिए एक विशेष बातचीत में वे कहते हैं, ‘जर्मनी में भी नस्लवाद और भेदभाव है. तब भी जर्मनी कानून के राज वाला देश है. यहां एक व्यापक जनाधार वाला नागरिक समाज है जो दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं अधिक मुखर है. जर्मनी में पहले से ही रह रहे और जर्मन नागरिकता प्राप्त करीब 70 हजार रोमा और सिंती हैं. यहां ऐसे भी रोमा हैं जिनके पास तुर्की या ग्रीस की, रोमानिया या बुल्गारिया की नागरिकता है. लेकिन, वे रोमा होने की अपनी पहचान छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें जर्मनी में भी अपने साथ भेदभाव होने और सामाजिक तिरस्कार का डर रहता है. पश्चिमी यूरोप के दूसरे देशों में, जैसे कि फ्रांस, इटली, हॉलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे आदि में भी यही स्थिति है. वहां भी भेदभाव और नस्लवाद का शिकार बनने से बचने के लिए रोमा लोगों को यथासंभव गुमनामी में ही जीवन बिताना पड़ता है.’ जर्मनी में रोमा-सिंती लोगों की कुल संख्या एक लाख 20 हजार आंकी जाती है. हालांकि रोजे यह भी मानते हैं कि रोमा अल्पसंख्यकों के साथ ‘जर्मनी में सरकारी स्तर पर भेदभाव अब भी होता है.’
यूरोप में रोमा आबादी
रोमा लोग वैसे तो इस बीच अमेरिका, ब्राज़ील और तुर्की में भी मिलते हैं, लेकिन उनका मुख्य निवासक्षेत्र यूरोप ही है. यूरोप के विभिन्न देशों में उनकी अनुमानित संख्या इस प्रकार हैःरोमानिया 24 00 000
बुल्गारिया 8 00 000
स्पेन 8 00 000
रूस 6 00 000
हंगरी 6 00 000
सर्बिया 5 00 000
तुर्की 5 00 000
स्लोवाकिया 4 50 000
फ्रांस 4 00 000
मेसेडोनिया 2 50 000
चेक गणराज्य 2 50 000
ग्रीस 2 20 000
यूक्रेन 2 00 000
ब्रिटेन 1 50 000
जर्मनी 1 40 000
इटली 1 00 000इसके अलावा अल्बानिया, बोस्निया, पुर्तगाल, पोलैंड, क्रोएशिया, स्वीडन, आयरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड आदि यूरोपीय देशों में भी रोमानी लोगों की काफी तादाद है |
भारत से पहुंचे थे यूरोप
जर्मनी के कोलोन शहर में रोमा बच्चों के लिए एक अलग स्कूल और किंडरगार्टन है. रोमा बिरादरी द्वारा संचालित इस विशेष स्कूल में पूर्वी यूरोप से आए रोमा शरणार्थियों के दो से 13 साल तक के 46 बच्चों को दो साल के भीतर किसी सामान्य जर्मन स्कूल में पढ़ने लायक बनाया जाता है. स्कूल का नाम है ‘अमारो खेर.’ रोमानी भाषा में इस नाम का अर्थ है ‘हमारा घर.’ साफ है कि राजस्थान जैसे राज्यों में प्रचलित ‘अमारो घर’ सदियों के समय और हजारों किलोमीटर की दूरी के बाद भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं.
भाग्य की मार और परिस्थितियों से हार कर सदियों से घुमंतू बंजारा जीवन बिताने वाले रोमा लोगों को लिखने-पढ़ने का न तो कभी ठीक से मौका मिला और न ही उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली. इसीलिए, उनके पास अपना कोई लिखित साहित्य, इतिहास या ऐसे दस्तावेज भी नहीं हैं जिनसे साफ पता चल सके कि वे कब, कहां से और कैसे यूरोप पहुंचे. वे जहां पहुंचे वहीं के बन गए. उन्होंने वहां प्रचलित धर्मों और नामों को तो अपना लिया पर अपने रीति-रिवाज, रहन-सहन, गीत-संगीत और पुरानी बोली-भाषा को यथासंभव संजोए रखा. उन्हीं के आधार पर भाषाविदों और इतिहासकारों का 18वीं सदी के बाद से यही मानना रहा है कि उनके पूर्वज कोई हजार-डेढ़ हजार साल पहले भारत के उन हिस्सों से चले थे जो आज राजस्थान, सिंध और पंजाब कहलाते हैं. समय के साथ वे तीन चरणों में पूरे यूरोप और अमेरिका तक फैल गए. पश्चिमी यूरोप में उनका फैलना 15वीं सदी में शुरू हुआ.
इन विद्वानों का यह भी कहना है कि आज की विभिन्न रोमा उपजातियों के बीच हालांकि कई प्रकार की बोलियां और भाषाएं मिलती हैं पर उनके मूल शब्द, बहुत-से संख्यावाचक और पारिवारिक संबंधसूचक शब्दों, शारीरिक अंगों और कार्यकलापों के नाम भारतीय उदगम के ही हैं. उनकी बोलियों-भाषाओं पर संस्कृत, हिंदी और पश्चिमोत्तर भारत की बोलियों की अमिट छाप है. भारत से वे कब और क्यों चले, इस बारे में नवीनतम आनुवंशिक अध्ययनों के आधार पर कहा जा रहा है कि उनके सबसे आरंभिक पूर्वज डोम जाति के थे. वे कोई डेढ़ हजार वर्ष पूर्व पांचवीं सदी में भारत से निकलना शुरू हुए. कई अलग-अलग रास्तों से और कई अलग-अलग झोंकों में वे पहले पश्चिम एशिया की तरफ बढ़े. कुछ तो पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व में ही रह गए और कुछ दक्षिणी भूमध्यसागर के तटवर्ती देशों में भी पहुंच गए. कहते हैं कि 11वीं सदी में इन भारतीयों का एक हिस्सा आज के रोमानिया, बुल्गारिया और भूतपूर्व यूगोस्लाविया वाले बाल्कन प्रायद्वीप पर पहुंच कर दो भागों में बंट गया. एक भाग दक्षिण-पूर्वी यूरोप की तरफ और दूसरा भाग मध्य यूरोप की तरफ बढ़ने लगा.
यह बात पश्चिमी इतिहासकारों के एक वर्ग के इस कथन का किसी हद तक समर्थन करती लगती है कि रोमा जनजातियों के पूर्वज अधिकतर ऐसे अनार्य (दलित) सैनिक भी रहे हो सकते हैं जिन्हें शायद महमूद गजनी से पहले के इस्लामी आक्रमणकारियों से तंग आ गए उस समय के भारतीय राजाओं को अपनी सेनाओं में भर्ती करना पड़ा था. इन इतिहासकारों के अनुसार, वे मूल रूप से डोम, लोहार, गुज्जर और टांडा जाति के थे; राजस्थान, पंजाब और सिंध जैसे भारत के पश्चिमी अंचलों में रहा करते थे और मुस्लिम आक्रमणकारियों का पीछा करते-करते ईरान के रास्ते से पश्चिम एशिया तक पहुंच गए. भारत से कट जाने और पश्चिम एशिया में पैर जमाए इस्लाम से लोहा लेने में असमर्थ होने के कारण हो सकता है कि वे उत्तर की ओर मुड़ कर रोमानिया जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों में पहुंचे हों. रोमानिया में आज भी 24 लाख, यानी पूरे यूरोप में सबसे अधिक रोमा रहते हैं.
इससे कुछ हट कर पश्चिमी इतिहासकारों के एक दूसरे वर्ग का मानना है कि रोमा लोगों के पूर्वज भारतीय राजाओं के सैनिक नहीं थे, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत के सामान्य निवासी थे. नवीं-दसवीं सदी में भारत पर जब मुस्लिम अरबों का आक्रमण बढ़ने लगा, तब वे इन निवासियों से गुलामी करवाने या उस समय के रोमन साम्राज्य के सैनिकों से लड़ने-भिड़ने के लिए उन्हें बंदी बना कर अपने साथ ले जाने लगे. उनका यह भी कहना है कि महमूद गजनी के 997 से 1030 के बीच भारत पर किए गए 17 आक्रमणों के दौरान तत्कालीन पश्चिमी भारत के लगभग पांच लाख निवासियों और बंजारों को बंदी बना कर भारत से दूर ले जाया गया और बाद में उन्हें गुलामों के तौर पर यूनान, रोमानिया, सर्बिया आदि बाल्कन देशों में बेच दिया गया. वहीं से कुछ तो गुलामों के तौर पर बिकते हुए और कुछ अपने बलबूते पर नए ठौर-ठिकानों की तलाश करते हुए यूरोप के दूसरे देशों में पहुंचे.
रोमा बिरादरी की सिंती जाति के बारे में कहा जाता है कि ‘सिंती’ नाम सिंधी से ही बना होना चाहिए, यानी उनके पूर्वज सिंध के रहे होंगे. वे स्वयं भी यही मानते हैं. पश्चिमी यूरोप के रोमा खुद को सिंती कहना ही पसंद करते हैं. रोमानी भाषा में ‘रोमा’ का अर्थ मनुष्य है. फ्रांस में उन्हें ‘मौनूष’ और स्पेन तथा पुर्तगाल में ‘काले’ भी कहा जाता है.
भारतवंशी होने की वैज्ञानिक पुष्टि
इसकी वैज्ञानिक पुष्टि भी हो चुकी है कि रोमा और सिंती के पूर्वज पश्चिमोत्तर भारत के रहने वाले भारतीय ही थे. 2012 में विज्ञान पत्रिका ‘करंट बायोलॉजी’ में प्रकाशित अपने एक शोधपत्र में नीदरलैंड में रोटरडाम के एरास्मस विश्वविद्यालय के मान्फ्रेड काइजर ने लिखा कि रोमा और सिंती बिरादरी के पू्र्वज करीब 1,500 साल पहले भारत में रहा करते थे. करीब 900 साल पूर्व, यानी 11वीं-12वीं सदी में, वे बाल्कन प्रायद्वीप (यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, भूतपूर्व यूगोस्लाविया) के रास्ते से यूरोप में फैलने लगे थे.
काइजर की टीम ने उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में रहने वाली रोमा बिरादरी की 13 उपजातियों से जुड़े 152 लोगों के जीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है. उनका कहना है कि भारत से चलने के बाद वाले आरंभिक चरण के उनके जीनोम (समग्र जोन) में पश्चिम एशिया, मध्य एशिया या कॉकेशिया के निवासियों के जीनों की मिलावट नहीं मिलती. यानी, शुरू-शुरू में वे एक ही समुदाय रहे और आपस में ही शादी-विवाह करते रहे. लेकिन, बाद में वे कई हिस्सों में बंट गए और अलग-अलग रास्तों पर चल पड़े. काइजर लिखते हैं, ‘रोमा लोग हालांकि आज भी बहुत कम ही स्थानीय लोगों से शादी-विवाह करते हैं, तब भी उनके जीनों में स्थानीय वैवाहिक संबंधों के आनुवंशिक निशान भी मिलते हैं.’ नए जीन अधिकतर हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया या स्लोवाकिया के मूल निवासियों से संबंध रखते हैं, जहां वे सबसे लंबे समय से और कहीं अधिक संख्या में बसे हुए हैं. पश्चिमी यूरोप के स्पेन, पुर्तगाल या जर्मनी जैसे देशों मंे रहने वाले रोमा लोगों के जीनोम में स्थानीय मूल निवासियों के जीनों की संख्या बहुत कम ही मिलती है. शायद इसलिए कि पश्चिमी यूरोप के निवासी रोमा जनों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए उनसे दूर ही रहते हैं.
बराबरी की लंबी लड़ाई
यूरोपीय देशों की सरकारों ही नहीं, अदालतों को भी रोमा लोगों को बराबरी का नागरिक मानने में काफी समय लगा है. स्वयं जर्मनी के सर्वोच्च न्यायालय ने 1956 में अपने एक फैसले में लिखा, ‘बंजारे अपराधवृत्ति वाले लोग हैं, विशेषकर चोरी और धोखाधड़ी करते हैं. दूसरों की वस्तुओं के प्रति आदारभाव का उनमें नैतिक अभाव है, क्योंकि वे आदिकालीन घटिया मनुष्यों की तरह सब कुछ बेझिझक हथियाने की फिराक में रहते हैं.’ यह फैसला 1963 तक वैध था. इसी कारण आज के लोकतांत्रिक जर्मनी को भी हिटलर के समय के सिंती-रोमा जातिसंहार को यहूदियों जैसा ही जातिसंहार मानने में काफी समय लगा.
अपने लिए मान्यता और नागरिक समानता पाने के उद्देश्य से ही 1970 में लंदन में रोमा बिरादरी का पहला विश्व सम्मेलन हुआ था. इसमें आए 25 देशों के रोमा प्रतिनिधियों ने अपनी बिरादरी का एक अलग झंडा और राष्ट्रगीत भी तय किया, हालांकि वे जिस किसी भी देश में रहते हैं, अपने आप को उसी देश का पुराना नागरिक मानते हैं. ऊपर नीले और नीचे हरे रंग की पट्टी के बीच में लाल रंग के अशोक-चक्र वाला रोमा झंडा भारत के प्रति उनके जीवंत लगाव के बारे में कोई संदेह नहीं रहने देता. इसी सम्मेलन में आठ अप्रैल, 1970 को यह भी तय हुआ कि दूसरे लोग उन्हें चाहे जिस हेय-सूचक नाम से पुकारें, वे खुद को हमेशा ‘रोमा’ ही कहेंगे और इसी नाम की मान्यता व अपने लिए समानता की मांग करेंगे. तब से आठ अप्रैल हर साल अंतरराष्ट्रीय रोमा दिवस के तौर पर मनाया जाता है. यूरोपीय संघ ने भी अब इस प्रथा को अपना लिया है.
यूरोप में रहने वाले रोमा लोगों की सही संख्या कोई नहीं जानता. अपने अपमान और तिरस्कार से बचने के लिए बहुत-से रोमा अब भी अपनी सही पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं. तब भी, यूरोपीय संघ ने भी औपचारिक तौर पर मान लिया है कि वे ही यूरोप का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक जातीय समुदाय हैं. संघ के सभी 28 देशों को मिला कर उनकी संख्या एक से सवा करोड़ तक हो सकती है. संघ ने 2005 से 2015 तक के समय को ‘रोमा दशक’ घोषित किया है और दो वर्ष पूर्व उनके शैक्षिक और सामाजिक उत्थान की एक रणनीति भी तैयार की है.
रोमानी भाषा में संस्कृत-हिंदी
रोमा खुद को भले ही एक ही बिरादरी मानते हों, उनके धर्म अनेक हैं. वे जहां भी हैं, वहीं के धर्म में रंग गए हैं. हिंदू तो शायद ही कोई खुद को मानता होगा. लेकिन, वे यूरोप की अपनी स्थानीय भाषाओं के शब्दों को लेते हुए ‘रोमानी’ या ‘रोमानेस’ नाम की जो साझी भाषा विकसित कर रहे हैं, उसके लगभग 800 सबसे आम शब्द संस्कृत और हिंदी के ही शुद्ध या अपभ्रंश रूप बताए जाते हैं. ‘रोमानी’ के बोलने वालों की संख्या 35 लाख से अधिक आंकी जाती है.
भाषा और भारत के नाम पर जर्मनी की केंद्रीय सिंती और रोमा परिषद के अध्यक्ष रोमानी रोजे बहुत भावुक हो जाते हैं. वे कहते हैं, ‘मैं 1984 में भारत गया था. वह मेरे लिए बहुत ही भावप्रवण यात्रा थी. अपनी जड़ों को जानने की यात्रा थी…मैं दिल्ली गया था, चंडीगढ़ गया था. वहां दुनिया भर के रोमा कलाकारों की मंडलियां आई थीं. रोमा भारत से जो कुछ कभी यूरोप ले गए थे, उसे एक बार फिर भारत लाए थे. वहां एक बड़े महोत्सव में उन्होंने अपनी रोमा संस्कृति को याद किया और प्रदर्शित भी किया.’ रोमानी भाषा का प्रसंग छिड़ने पर रोमानी रोजे ने बड़े गर्व से बताते हैं कि हजार साल बाद और हजारों किलोमीटर की दूरी के बावजूद उनकी भाषा संस्कृत और हिंदी से अब भी कितनी जुड़ी हुई है. उदाहरण के लिए, नाक को वे भी ‘नाक’, कान को ‘कान्त’, पिता या दादा के लिए ‘पापू’, दादी के लिए ‘मामी’, पानी के लिए ‘पानी’, बड़े लोगों के लिए ‘राई’ (राय साहब), मुंह के लिए ‘मुई’, दांत के लिए ‘दान्त’, जीभ के लिए ‘चीब’ या दिल के लिए ‘जी’ (जैसे, ‘जी करता है’ में ‘जी’ का अर्थ दिल है) कहते हैं. गिनती भी हिंदी से मिलती-जुलती है– एक, दुइ, द्रीन, स्तार, पांज, शोब, एस्ता, ओर्ता, एन्या, देस.
कत्थक बना फ्लामेंको
रोमानी रोजे के अनुसार, रोमा लोगों के नाच-गानों और संगीत में, उनकी गाथाओं और कलाओं में भारत अब भी बसा हुआ है. भारत का कत्थक नृत्य उन्हीं के माध्यम से स्पेन पहुंचा और अब वहां ‘फ्लामेंको’ के नाम से स्पेनी पहचान का प्रतीक बन गया है. लेकिन, उन्हें भारत की सरकार और जनता से यह शिकायत भी है कि मॉरीशस, फिजी या दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतवंशियों को तो बहुत सराहा-दुलारा जाता है, जबकि उनसे भी कहीं पहले यूरोप गए रोमा लोगों को भूल कर भी याद नहीं किया जाता. हिटलर के शासनकाल में हुए रोमा-जातिसंहार की याद में लंबे संघर्ष के बाद बर्लिन में बने स्मारक का 24 अक्टूबर, 2012 को लोकार्पण था. रोजे का कहना है कि इस समारोह में जर्मनी की चांसलर, जर्मन राष्ट्रपति तथा अमेरिका और फ्रांस सहित सभी प्रमुख देशों के राजदूत भी आए थे. उन्होंने भारतीय राजदूत (सुजाता सिंह, जो अब विदेश सचिव हैं) को भी अलग से आमंत्रित किया था. लेकिन वे नहीं आए. रोजे कहते हैं, ‘भारत और भारतीयों ने दक्षिण अफ्रीका को नस्लवाद से आजादी दिलाने में मदद दी, पर नस्लवाद के विरुद्ध हम रोमा लोगों की लड़ाई में कभी कोई मदद नहीं की.’
जर्मन रोमा बिरादरी के अध्यक्ष ने बताया कि भारत तो रोमा लोगों की उपेक्षा कर रहा है जबकि चीन उनमें दिलचस्पी ले रहा है. चीन ने उन्हें वहां के जातीय अल्पसंख्यकों की स्थिति दिखाने के लिए आमंत्रित किया. वे कहते हैं, ‘हम अल्पसंख्यक मामलों के चीनी मंत्री से भी मिले. बाद में चीनी मंत्री जब जर्मनी आए, तो हाइडेलबर्ग में हमारी केंद्रीय परिषद में भी आए.’ चीन की यह चाल भारत के लिए अलार्म जैसी होनी चाहिए. उसे सोचना चाहिए कि वह यूरोप के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की– जो कि सौभाग्य से भारतवंशी भी है– क्या इसी तरह उपेक्षा करता और चीन को उस पर डोरे डालते देखता रहेगा.
जर्मन केंद्रीय रोमा परिषद के पास 700 वर्गमीटर जगह के बराबर एक बड़ी प्रदर्शनी है. वह पूरे यूरोप सहित कई दूसरे देशों में भी दिखाई जा चुकी है. जहां भी गई, वहां के प्रधानमंत्री या विदेशमंत्री ने उसका उद्घाटन किया. परिषद के अध्यक्ष रोमानी रोजे की हार्दिक इच्छा है कि रोमा बिरादरी के जातिसंहार की कहानी कहती यह प्रदर्शनी एक बार उस देश में भी दिखाई जाए जहां से उनके पूर्वज आए थे. वे सवाल करते हैं, ‘यह प्रदर्शनी क्यों नहीं एक बार नई दिल्ली में भी दिखाई जा सकती? ‘रोमा बिरादरी का एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा भी है. रोजे कहते हैं, ‘ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भारत सरकार यह प्रदर्शनी लगाती और ऑर्केस्ट्रा को भी निमंत्रित करती? किसी विश्वविद्यालय में रोमा-जातिसंहार पर एक व्याख्यान होता?’
सरकार ही नहीं, भारत की गैरसरकारी संस्थाएं, सामाजिक संगठन या शिक्षा संस्थान भी उन्हें उनकी पुरानी जड़ों से जोड़ने के लिए आगे आ सकते हैं. प्रवासी भारतीयों की तरह रोमा भी भारत के अनौपचारिक दूत बन सकते हैं. उनकी बिरादरी संसार का एकमात्र ऐसा शांतिप्रिय समुदाय है जो यहूदियों, कुर्दों या (अरबी राष्ट्रवाद का हिस्सा होते हुए भी) फिलिस्तिनियों की तरह कोई अलग जनता या अलग राष्ट्र होने का दावा अथवा नया देश देने की मांग नहीं करता. जिसका न कोई नेता है और न कोई आंदोलन है. जो न पृथकतावादी है और न आतंकवादी. वह तो एक बहुत ही दलित और व्यथित बिरादरी है. शायद यही वजह है कि उसकी इस प्रार्थना को भी कोई नहीं सुनता कि वह जहां भी है, उसे वहीं का बन कर रहने दिया जाए. हां, जिप्सी या बंजारा नहीं, बस ‘रोमा’ (मनुष्य) कहा और यही समझा जाए.
अपने पूर्वजों के देश भारत की याद शायद हर रोमा के रोम-रोम में बसी हुई है. पर क्या भारत को भी कभी इन बिछड़े हुए भारतवंशियों की याद आएगी?








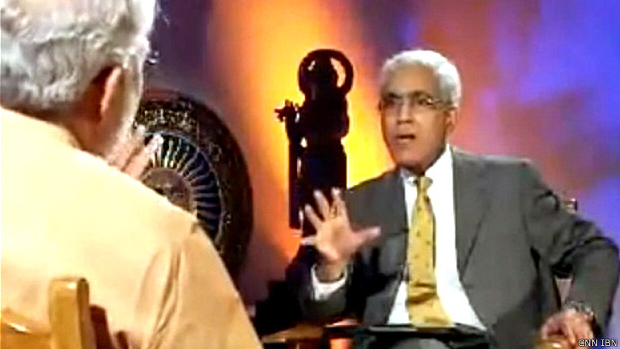
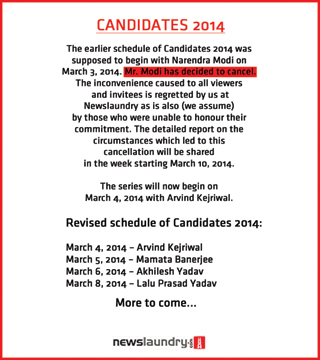

 नरेंद्र मोदी देश की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए किस कदर बेताब हैं इसकी जानकारी लगभग सभी को है. लेकिन मोदी के अलावा कोई और भी है जो उनके सर पर प्रधानमंत्री का ताज देखने के लिए उतना ही बेताब है. इसके लिए वह दिन-रात एक किए हुए है. यह व्यक्ति अपने ‘साहब’ के गांधीनगर से सात आरसीआर तक के रास्ते में मौजूद हर अड़चन, हर ठोकर को हटाने की जी-जान से कोशिश कर रहा है. मोदी के इस विश्वासपात्र का नाम है अमित अनिलचंद्र शाह. शाह, नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उनके लिए मोदी भगवान से कम नहीं हैं और वे भी शाह पर ही सबसे अधिक भरोसा करते हैं.
नरेंद्र मोदी देश की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए किस कदर बेताब हैं इसकी जानकारी लगभग सभी को है. लेकिन मोदी के अलावा कोई और भी है जो उनके सर पर प्रधानमंत्री का ताज देखने के लिए उतना ही बेताब है. इसके लिए वह दिन-रात एक किए हुए है. यह व्यक्ति अपने ‘साहब’ के गांधीनगर से सात आरसीआर तक के रास्ते में मौजूद हर अड़चन, हर ठोकर को हटाने की जी-जान से कोशिश कर रहा है. मोदी के इस विश्वासपात्र का नाम है अमित अनिलचंद्र शाह. शाह, नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उनके लिए मोदी भगवान से कम नहीं हैं और वे भी शाह पर ही सबसे अधिक भरोसा करते हैं.





 अमित शाह ने सालों से मरणासन्न पड़े संगठन को सक्रिय करने से अपने काम की शुरुआत की है. पार्टी नेता बताते हैं कि एक रणनीति बनाई गई है जिसके तहत लखनऊ से लेकर राज्य के हर बूथ तक पार्टी संगठन को सक्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है. पार्टी प्रवक्ता मनोज मिश्रा कहते हैं, ‘सबसे पहले अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम किया है. उन्होंने तेजी से जनसंपर्क किया है और सभी आठ क्षेत्रों में व्यक्तिगत दौरा किया है. पूरे राज्य में वैज्ञानिक तरीके से बूथ कमेटियां बनाई जा रही हैं.’ शाह के उत्तर प्रदेश में आने के बाद हुए बदलावों की चर्चा करते हुए वाजपेयी कहते हैं, ‘आज लगभग 80 प्रतिशत जगहों पर हमारी बूथ कमेटियां तैयार हो चुकी हैं. पहले ऐसा नहीं होता था. होता ये था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो फिर बूथ जाए भाड़ में मैं पार्टी के औपचारिक प्रत्याशी के खिलाफ काम करूंगा. इस बार ऐसा नहीं है. इस बार व्यक्ति नहीं पार्टी चुनाव लड़ रही है. संगठन के तंत्र से चुनाव लड़ा जा रहा है.’
अमित शाह ने सालों से मरणासन्न पड़े संगठन को सक्रिय करने से अपने काम की शुरुआत की है. पार्टी नेता बताते हैं कि एक रणनीति बनाई गई है जिसके तहत लखनऊ से लेकर राज्य के हर बूथ तक पार्टी संगठन को सक्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है. पार्टी प्रवक्ता मनोज मिश्रा कहते हैं, ‘सबसे पहले अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम किया है. उन्होंने तेजी से जनसंपर्क किया है और सभी आठ क्षेत्रों में व्यक्तिगत दौरा किया है. पूरे राज्य में वैज्ञानिक तरीके से बूथ कमेटियां बनाई जा रही हैं.’ शाह के उत्तर प्रदेश में आने के बाद हुए बदलावों की चर्चा करते हुए वाजपेयी कहते हैं, ‘आज लगभग 80 प्रतिशत जगहों पर हमारी बूथ कमेटियां तैयार हो चुकी हैं. पहले ऐसा नहीं होता था. होता ये था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो फिर बूथ जाए भाड़ में मैं पार्टी के औपचारिक प्रत्याशी के खिलाफ काम करूंगा. इस बार ऐसा नहीं है. इस बार व्यक्ति नहीं पार्टी चुनाव लड़ रही है. संगठन के तंत्र से चुनाव लड़ा जा रहा है.’