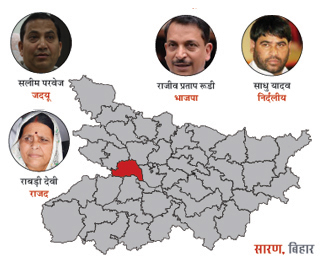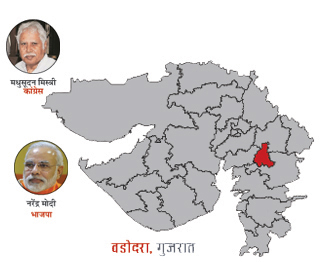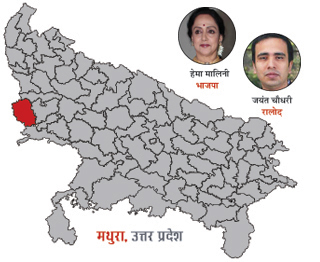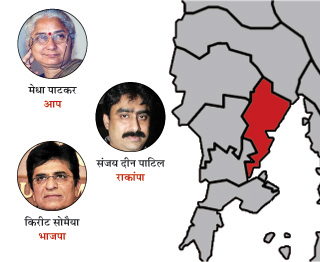वे मनुवादी हैं, यह एक ऐसा आरोप है जो बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता मायावती ने समय-समय पर तमाम राजनीतिक दलों से लेकर मीडिया तक पर लगाया है. उनके अनुसार दूसरी पार्टियों में दलित समाज के लोगों के लिए जगह नहीं है. मायावती मानती हैं कि बाकी पार्टियां सवर्णवादी हैं क्योंकि वे दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं देती, उन्हें टिकट नहीं देतीं.
इसका दूसरा मतलब यह है कि बसपा में तस्वीर ऐसी नहीं होगी. यानी जो पार्टी खुद को दलितों की पार्टी कहती है, जिसका उदय दलित आंदोलन से हुआ है, जिसका वोट बैंक दलित माने जाते हैं, जो दलितों की प्रतिनिधि पार्टी कही जाती है, उसमें वह नहीं होना चाहिए जिसका आरोप मायावती दूसरी पार्टियों पर लगाती हैं. लेकिन क्या ऐसा वास्तव में है?
हाल ही में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की. लखनऊ में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए मायावती ने कहा कि उन्होंने टिकट देने में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है और सभी वर्गों को टिकट के माध्यम से उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है. बसपा द्वारा बांटे गए इन 80 टिकटों में से 21 ब्राह्मण प्रत्याशियों के खाते में गई हैं तो आठ सीटों पर क्षत्रियों को टिकट दिया गया है. 19 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार बनाए गए तो 15 सीटों पर पार्टी ने पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार उतारे हैं. बाकी बची हुई 17 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं सो वहां से पार्टी ने अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट दिया है. इन 17 में से 10 जाटव, छह पासी और एक कश्यप समुदाय से हैं.
पार्टी द्वारा बांटे इन टिकटों को अगर बेहद ध्यान से देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है. पता चलता है कि पिछले लोकसभा चुनावों की तर्ज पर पार्टी ने इस बार भी दलितों को सिर्फ सुरक्षित सीट से टिकट दिया है. अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को इन सुरक्षित सीटों के अलावा किसी भी और सीट से टिकट नहीं दिया गया. सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा कोई और नहीं खड़ा हो सकता है, ऐसे में अगर दूसरी तरह से देखें तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया.
स्वाभाविक सवाल उठता है कि दलितों की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करने वाली पार्टी उसी दलित समाज के व्यक्ति को सुरक्षित सीट से बाहर टिकट क्यों नहीं देती. भाजपा हो या कांग्रेस या फिर कोई अन्य पार्टी, सुरक्षित सीटों पर तो सबको आरक्षित समुदाय का उम्मीदवार ही उतारना होता है. तो फिर दलितों की पार्टी कहे जाने वाली बसपा बाकियों से कहां अलग हुई? मायावती के मुताबिक दूसरे दल इसलिए मनुवादी हैं कि उनमें दलित समाज के लोगों के लिए जगह नहीं है या वे दलितों को टिकट नहीं देते, लेकिन उनकी पार्टी भी तो ऐसा करती दिख रही है.
तो क्या मायावती मनुवाद से लड़ते लड़ते खुद मनुवादी हो गई हैं ? उनके आलोचक कहते हैं कि आज बसपा की स्थिति ऐसी है कि उसमें दलितों को न टिकट मिल रहा है और न उन्हें पार्टी में कोई खास स्थान हासिल हो रहा है. कहा जा रहा है कि अगर सुरक्षित सीटों पर दलितों को ही टिकट देने की बाध्यता न होती तो शायद बसपा किसी दलित को टिकट देती ही नहीं.
मायावती की जीवनी ‘बहन जी’ के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस इस पर कहते हैं, ‘ ऐसा नहीं है कि यह कोई आज हो रहा है कि बसपा में दलितों को टिकट नहीं दिया जा रहा है. यह सब तो कांशीराम के जमाने से हो रहा है. बसपा में टिकट देने का एकमात्र आधार है कि व्यक्ति सीट जीत सकता है या नहीं. चूंकि सामान्य सीटों पर किसी दलित के जीतने की संभावना न के बराबर रहती है इसीलिए इन सीटों पर दलितो को टिकट नहीं मिलता. ’
बोस की बात को विस्तार देते हुए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शरत प्रधान कहते हैं, ‘बसपा का टिकट बांटने का तरीका बहुत सीधा है. ये सिर्फ दो चीजें देखते हैं. पहला जो टिकट चाह रहा है वह चुनाव जीत सकता है या नहीं और दूसरा, उसके पास पैसा कितना है. पहले पार्टी उनको टिकट देती है जो जीत सकता है. बाकी जिन सीटों पर पार्टी को लगता है कि वह जीत नहीं सकती वहां वह पैसा लेकर टिकट बेच देती है. पैसा दो और टिकट लो. ऐसे में पार्टी के पास दलितों को टिकट देने की कहां फुर्सत है ?’ बोस एक रोचक तथ्य की तरफ इशारा करते हुए आगे कहते हैं, ‘ बसपा में टिकट पाने के लिए आपको पार्टी का कार्यकर्ता बनने की जरूरत भी नहीं है. पार्टी किसी को भी टिकट दे देती है. बस आपका अपना एक आधार होना चाहिए. आप आधार लेकर आते हैं और फिर पार्टी उस क्षेत्र में अपना दलित वोट आपको ट्रांसफर कर देती है.’
हालांकि दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार दलितों को टिकट न देने के सवाल पर बसपा का बचाव करते हुए कहते हैं, ‘भारतीय समाज के जातिवादी होने का यह सबसे बेहतर प्रमाण है. सभी को पता है कि किसी सामान्य सीट से किसी दलित का जीत पाना लगभग असंभव है. क्या आपको लगता है कि अगर बसपा किसी दलित को गैरसुरक्षित सीट से खड़ा करती है तो सर्वण लोग उसे वोट देंगे? नहीं देंगे. यही कारण है कि बसपा चाहकर भी किसी दलित को टिकट नहीं दे पाती. जैसे ही कोई दलित खड़ा होता है दूसरी जातियां उसके खिलाफ लामबंद हो जाती हैं.’
जीत की संभावना न होने के कारण बसपा दलित व्यक्ति को सामान्य सीट से टिकट नहीं देती. तो उन सीटों पर पार्टी का हाल क्या है जो सुरक्षित कही जाती हैं? यूपी की सुरक्षित लोकसभा सीटों का वर्तमान और इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि पार्टी का इन सीटों पर प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है. उदाहरण के लिए 2009 के लोकसभा चुनाव में इन 17 सुरक्षित सीटों में से सपा के हिस्से में जहां नौ सीटें आईं वहीं बसपा को मात्र दो सीटें ही हासिल हुईं. बसपा सिर्फ लालगंज और मिश्रिख सुरक्षित सीट जीत पाने में ही सफल रही थी. इतिहास में भी उसकी स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही है. 1999 में भाजपा की सात के मुकाबले बसपा को पांच सीटें मिलीं. 2004 में सपा को आठ तो बसपा को पांच सीटें मिलीं.
और यह सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात नहीं है. बसपा का विधानसभा चुनावों में भी कमोबेश यही हाल रहा है. 1993 में दलितों के लिए आरक्षित कुल 88 विधानसभा सीटों में से जहां भाजपा को 33 सीटें मिली थीं वहीं बसपा को मात्र 23 सीटें हसिल हुईं. इतनी ही सीटें सपा को भी मिली थीं. सन 96 में भाजपा को 35 सीटें मिलीं तो बसपा को मात्र 20. 2002 में सपा को 36 सीटें मिलीं और बसपा को 24. हां, 2007 में पार्टी को 61 सीटें जरूर हासिल हुईं, लेकिन 2012 में जाकर उसकी हालत फिर खराब हो गई.
उत्तर प्रदेश की आबादी में 21 फीसदी दलित हैं. तो जिस पार्टी को दलितों की पार्टी कहा जाता है उसका सुरक्षित सीटों पर भी बेहद कमजोर प्रदर्शन किन संदेशों की तरफ इशारा करता है? बोस कहते हैं, ‘सुरक्षित सीटों पर चूंकि सारे दलों को दलितों को ही टिकट देना होता है. इस कारण से दलित मतों का विभाजन हो जाता है. ऐसी स्थिति में दलित प्रत्याशी का जीतना इस बात पर निर्भर करता है कि सवर्ण मतदाता किसको समर्थन देते हैं. जिसको सवर्णों का समर्थन मिल जाता है वह विजयी होता है. यही कारण है कि भाजपा और सपा इन सीटों पर अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन करते हैं.’
2009 में हुए लोकसभा चुनाव में देश की 84 आरक्षित लोकसभा सीटों में सबसे अधिक 30 कांग्रेस की झोली में गई थीं. दूसरे नंबर पर 12 सीटों के साथ भाजपा रही. वाम मोर्चा नौ सीटें जीतकर दलितों की तीसरी सबसे बड़ी पसंद बना. फिर मायावती की पार्टी बसपा का नंबर आया जिसे मात्र दो सीटें हासिल हुईं. .
विवेक कुमार सुरक्षित सीट के गणित को कुछ इस तरह बताते हैं, ‘यह सही है कि सुरक्षित सीटों पर बसपा अच्छा प्रदर्शन नहीं करती. आप देखेंगे कि पूरे देश में कांग्रेस और भाजपा इन सीटों पर कब्जा जमाती हैं. इसके पीछे जातिवाद मुख्य कारण है. होता यह है कि अगर सर्वण वोटर को दलित को वोट देने की मजबूरी हो जाए तो उस स्थिति में भी वह बसपा के दलित उम्मीदवार के बजाय कांग्रेस या भाजपा के दलित उम्मीदवार को वोट देना बेहतर समझता है.’
विवेक सुरक्षित सीटों पर भी सवाल खड़ा करते हैं. वे कहते हैं, ‘जिस परिसीमन के तहत सुरक्षित सीटों का निर्धारण हुआ वह भी गलत है. किसी भी सुरक्षित सीट पर दलित मतदाता 20-30 फीसदी से ज्यादा नहीं हैं. यही कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर ने इन सुरक्षित सीटों की यह कहकर आलोचना की थी कि इससे सवर्ण समाज के चमचे पैदा होंगे क्योंकि सवर्ण की मदद बिना दलित इन सीटों से जीत ही नहीं सकता. इस तरह से इसमें बसपा की कोई गलती नहीं है. उसकी कमजोरी नहीं है कि उसके दलित प्रत्याशी नहीं जीत पाते.’
दूसरी तरफ बोस दलितों को टिकट मिलने और बसपा में उनके प्रतिनिधित्व के प्रश्न को व्यापक रूप से देखने की बात करते हैं. वे कहते हैं, ‘टिकट छोड़िए यहां तो पार्टी का संगठन ही बेहद अजीबोगरीब है. जिस तरह से बाकी पार्टियों में है कि लोग संगठन से जुड़कर आगे बढ़ते हैं वैसा बसपा में नहीं है. आप अगर संगठन से जुड़ भी गए तो यह तय नहीं है कि पार्टी भविष्य में आपको टिकट दे या फिर संगठन में ही आप बहुत आगे जा पाएं. सब बहन जी की इच्छा पर ही निर्भर है. यही कारण है कि पार्टी संगठन में दलितों का प्रतिनिधित्व भी बेहद कम है.’
बसपा के संस्थापक सदस्य रहे रामाधीन अहिरवार पार्टी और दलित समाज के बीच के संबंधों पर बात करते हुए कहते हैं, ‘मायावती दलित समाज को मूर्ख समझती हैं. उन्हें पता है कि वे जिसे भी खड़ा कर देंगी उसे दलित समाज वोट दे देगा. यही कारण कि वे दलितों को न टिकट देती है, न पार्टी में उन्हें स्थान और न ही उन्हें आगे बढ़ने देती हैं. दलितों की पार्टी को चुनाव लड़ने वाला कोई दलित नहीं मिलता. वे जानती हैं कि ये लोग बेचारे अपनढ़ हैं. इनका कौन है? ये हमें छोड़कर के कहां जाएंगे. मायावती का चले तो वे सुरक्षित सीट पर भी दलितों को टिकट न दें.’
जानकारों की मानें तो यही कारण है कि दलित आंदोलन से निकली पार्टी के पास गिनने के लिए भी ढंग के दलित नेता नहीं हैं. पार्टी में दलित नेताओं के उभरने के लिए स्थान नहीं है. अपने अलावा कोई और दलित नेता मायावती को मंजूर नहीं है. ऐसे कई नेता हैं जो बसपा के संस्थापक सदस्य रहे, बड़े नेता रहे, लेकिन बाद में पार्टी से बाहर कर दिए गए. जैसे आरके चौधरी, रामसमुझ पासी, राजबहादुर, बरखूराम वर्मा आदि पार्टी में मायावती के अलावा किसी और दलित नेता का उभार न होने और दलितों की पार्टी में दलितों के लिए जगह न होने के सवाल पर बोस कहते हैं, ‘मायावती अपने अलावा किसी और नेता खासकर के दलित नेता को पार्टी में उभरते हुए नहीं देखना चाहतीं. पार्टी में जैसे ही कोई नेता उभरने की कोशिश करता है, वे उसे बाहर का रास्ता दिखा देती हैं. संगठन के स्तर पर भी दलितों का प्रतिनिधित्व बेहद सीमित है.’
यही कारण है कि पिछले कुछ समय में दलितों के बसपा से दूर जाने जैसी बातें भी सामने आती रही हैं. उदाहरण के लिए 2009 में दिल्ली स्थित सीएसडीएस द्वारा किए एक अध्ययन में सामने आया कि 2004 में बसपा के पास दलितों का वोट शेयर जो 65 फीसदी था वह 2009 में गिरकर 52 फीसदी पर आ गया.
दलितों के बसपा से दूर जाने के सवाल पर बोस कहते हैं, ‘जाटवों का वोट तो पहले से लेकर आज तक मायावती और बसपा के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है. लेकिन हां, 2012 के विधानसभा चुनाव में देखा गया कि दलितों में से गैर जाटव या कहें महादलितों का वोट बसपा से खिसकता हुआ दिखाई दिया. जबकी 2007 में पूरे दलित समाज ने बसपा को वोट किया था.’ बोस की बात का समर्थन करते हुए ‘द मेकिंग ऑफ दलित रिपब्लिक’ के लेखक और राजनीतिक विश्लेषक बद्रीनारायण कहते हैं, ‘जाटव तो नहीं, लेकिन बाकी दलित जरूर पार्टी से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं. बसपा के लिए यह चिंता का विषय जरूर होना चाहिए.’
2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हुए सीएसडीएस ने जाटव वोटों के बसपा से सपा की तरफ जाने की बात कही. उसके अध्ययन में दावा किया गया कि 1998 के बाद बसपा को इस बार सबसे कम जाटव मत मिले हैं. 2007 के बाद से बीएसपी के जाटव वोटों में 24 फीसदी की गिरावट आई है. दलितों में भी महादलित के मायावती से दूर जाने के सवाल पर शरत कहते हैं, ‘जिस जातिवाद के खिलाफ लड़ने की बात बसपा करती है वह खुद उसी जातिवाद से ग्रस्त है. यही कारण है कि पार्टी में जाटव और गैर जाटव के बीच में अलग संघर्ष चलता रहता है. मायावती भी पूरे दलित समाज के बजाय जाटवों की नेता बनती दिख रही हैं.’