नई लीक गढ़ती तकनीक
[wzslider autoplay=”true” transition=”‘slide'” info=”true” lightbox=”true”]
इंदौर के कारोबारी विनय वाधवानी ने कुछ समय पहले जब अचानक अपने पास मोबाइल फोन रखना बंद कर दिया तो उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को थोड़ा आश्चर्य हुआ. वे समझ नहीं पाए कि शरीर के किसी हिस्से की तरह जरूरी बन चुकी इस चीज को वाधवानी ने आखिर क्यों छोड़ दिया. लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं था कि यह फोन वाधवानी को मनोचिकित्सक यानी दिमागी बीमारियों के डॉक्टर का दरवाजा दिखा चुका है. दरअसल वाधवानी एक ऐसी परेशानी के शिकार हो चुके थे जिसका इससे पहले चिकित्सा विज्ञान ने नाम भी नहीं सुना था. उनको अपने मोबाइल फोन से डर लगने लगा था. फोन ने उनकी जिंदगी से निजता यानी प्राइवेसी को पूरी तरह खत्म कर दिया था. बेडरूम में, बाथरूम में, डाइनिंग टेबल पर, कार में…वह कभी भी और कहीं भी बज सकता था. हालत यह हो गई कि वाधवानी को वह फोन कम और टाइम बम ज्यादा लगने लगा. आखिरकार डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया.
वाधवानी को फोन के कभी भी और कहीं भी बजने से डर लगता था तो दिल्ली के अजय कोहली की तकलीफ इसके उलट थी. दिन में कई बार उन्हें लगता कि उनके मोबाइल फोन की घंटी बज रही है, लेकिन जब वे जेब से फोन निकालकर देखते या दूसरे कमरे में पड़े अपने फोन तक पहुंचते तो पता चलता कि किसी का फोन नहीं आ रहा है. बाद में डॉक्टर ने ही उन्हें बताया कि यह भी एक बीमारी है जिसे फैंटम रिंगिंग कहा जाता है.
हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की दिल्ली स्थित एक होटल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई. इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर की गई उनकी वे टिप्पणियां और भी महत्वपूर्ण हो गईं जो उन्होंने पिछले तीन-चार दिनों के दौरान की थीं और जिनकी वजह से वे देश-दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थीं. संयोग की बात है कि पहले भी जब वे या उनके पति थरूर सुर्खियों या विवादों में आए तो इसमें अक्सर ट्विटर पर की गई उनकी टिप्पणियों की ही भूमिका रही थी. इसके पहले बीते दिसंबर में जब सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अनवर ने बलात्कार का आरोप लगने के बाद खुदकुशी कर ली तो यह चर्चा भी खूब हुई कि यह कदम उन्होंने फेसबुक पर अपने बारे में चल रही तरह-तरह की खबरों के बाद उठाया. यानी वे सोशल मीडिया का शिकार हुए.
पिछली सदी के पूर्वार्ध में मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तकनीक इंसान पर भारी पड़ने लगी है. यह हाल तब था जब मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं के आम इंसान तक पहुंचने में कई दशक बाकी थे. आज आइंस्टाइन होते तो क्या कहते?
कहते हैं कि पहले तकनीक इंसान की उंगली पकड़कर चलती है और फिर इंसान तकनीक की उंगली पकड़कर चलने लगता है. धीरे-धीरे निर्भरता बहुत ज्यादा हो जाए तो यह चलना आंख बंद करके होने लगता है. चलते चलते जब कभी उंगली छूट जाए और आंख खुले तो अचानक ही अहसास होता है कि हम किस हद तक तकनीक पर निर्भर हो चुके हैं. बीते एक दशक के दौरान मानव व्यवहार पर जिन दो चीजों ने सबसे अधिक असर डाला है वे हैं मोबाइल फोन और इंटरनेट. कुछ समय पहले तक इन माध्यमों के बारे में कहा जाता था कि ये बस एक सीमित वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं- उस महानगरीय भारत की जिसके पास तकनीक की सुविधा और अंग्रेजी की समझ है- और इनके सरोकार उन्हीं सवालों तक सीमित हैं जिनका इनके जीवन से वास्ता है. लेकिन धीरे-धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी के साथ मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की घुसपैठ भारतीय समाज में कहीं ज्यादा गहरी हुई है. अपने एक आलेख में वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन कहते हैं, ‘छोटे-छोटे कस्बों और शहरों के लोग, घरों में काम करने वाली महिलाएं और दूर-दूर रहकर अपनी सृजनात्मकता में लीन कलाकार या कार्यकर्ता इस माध्यम से महानगरों से, और मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. देखा जाए तो यह एक मायने में औद्योगिक क्रांति के बाद की सबसे बड़ी क्रांति है जिसने पिछली सदी के बहुत सारे मानकों को पूरी तरह नहीं, तो बहुत दूर तक बदल डाला है.’ हमारे निजी से लेकर कामकाजी जीवन तक तकनीक से हुआ बदलाव हर तरफ दिखने लगा है. कभी-कभी तो इस हद तक कि उसके बिना जीवन की कल्पना मुश्किल हो जाती है. दिल्ली में बीकॉम की छात्रा विदुशी गुप्ता कहती हैं, ‘मोबाइल कहीं छूट जाए तो लगता है जैसे बाकी दुनिया से कट गए.’ नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम कर रहे सुशील कुमार कहते हैं, ‘कभी कभी कोई काम करने के बाद भाए नहीं तो लगता है कि कंट्रोल जेड कर दें.’ खूबसूरत कलम से उकेरा गया सुलेख अब बीते जमाने की बात हो चुका है. कलम के सिपाही अब कीबोर्ड के हो चुके हैं. पिछले दस साल के दौरान कंप्यूटर और मोबाइल के लगातार बढ़ते इस्तेमाल का एक नतीजा यह भी हुआ है कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, फैंटम रिंगिंग और इंटरनेट एडिक्शन जैसी पहले कभी न सुनी गईं बीमारियां हमारी जिंदगी में चली आई हैं.
दिल्ली में रहने वाली और पेशे से शिक्षिका कुसुम सिंह कहती हैं, ‘हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात पर अचरज करेंगी कि आखिर उनके दादा-दादी मोबाइल और इंटरनेट के बगैर कैसे रह लेते थे? आखिर हमें भी तो अपने बच्चों को यह समझाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हमारे बचपन में मोबाइल फोन और एसएमएस तो क्या कई बार तो बेसिक फोन भी नहीं हुआ करते थे.’ एक वक्त था जब घर पर बेसिक यानी लैंडलाइन फोन लगवाने के लिए सालों पहले वेटिंग लेनी पड़ती थी. गोरखपुर में रहने वाली सुमीता भारती कहती हैं, ‘उस खुशी को आज के युवा महसूस भी नहीं कर सकते. उनके लिए तो यह बात कल्पना से परे है कि पुराने जमाने में हम मीलों दूर अपने दोस्तों से मिलने बिना यह कन्फर्म किए चले जाते थे कि वह घर पर है भी अथवा नहीं.’
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की सात अरब आबादी में छह अरब से अधिक मोबाइल फोन हैं. अलग-अलग अनुमानों के मुताबिक हमारे देश में तकरीबन 90 करोड़ मोबाइल फोन हैं. इस उपकरण ने दूरियों को काफी हद तक नेस्तनाबूद कर दिया है. फिर मिलेंगे जैसे शब्दों का अहसास काफी कुछ बदल गया क्योंकि अब हम बिछड़ते ही नहीं. कभी संदेश भेजने और उसका जवाब मिलने की प्रक्रिया में कई दिन लग जाते थे. एसएमएस यानी शार्ट मैसेज सर्विस के जरिये मोबाइल ने इसे पल भर का खेल बना दिया. एसएमएस के असर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अकेले अमेरिका में पिछले वर्ष 20 खरब से ज्यादा मैसेज का आदान-प्रदान किया गया. एक औसत अमेरिकी युवा एक दिन में 50 से 100 एसएमएस भेजता है. व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशनों के चलते अब संदेश भेजने की सुविधा मुफ्त हो गई है तो यह आंकड़ा बढ़ेगा ही.
प्रियदर्शन कहते हैं, ‘आज एक मोबाइल सबकी जेब में है, एक नंबर सबकी मेमोरी में है और काम के लिए अपना घर छोड़ने वाले अमीर-गरीब सब आश्वस्त हैं कि उनके पास अपनी खोज-खबर देने का एक जरिया आ गया है. पहले आरा-छपरा से दिल्ली-मुंबई और सूरत काम करने निकला गरीब 6 दिन बाद पोस्टकार्ड भेजकर अपनी कुशल-क्षेम बताता था, अब वह ट्रेन पर बैठने से लेकर उतरने तक का हिसाब-किताब देता है. दस साल पहले तक दिल्ली की बसों में असुरक्षित-सा तना हुआ चेहरा लेकर बैठी दिखने वाली लड़कियां अब मोबाइल से चिपकी किसी और दुनिया में खोई दिखाई पड़ती हैं- आश्वस्त कि वे अकेली नहीं हैं और किसी संकट की घड़ी में अपनों को आवाज देने वाला एक यंत्र उनके हाथों में है.’ हमारी लोकतांत्रिक क्रांति ने वयस्क मताधिकार के जरिए जो राजनीतिक बराबरी सबको देने की कोशिश की उसे कहीं ज्यादा वास्तविक अर्थों में इसने संभव किया है.
लेकिन संवाद की इस सरलता ने हमें कुछ सुविधाएं दी हैं तो कुछ दुविधाएं भी पैदा की हैं. अब हम 24 घंटे दुनिया से जुड़े हुए हैं. लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे लगता है कि निरंतर जुड़ाव या कान्स्टेंट कनेक्टिविटी नाम की इस घटना ने हमारी निजता या जीवन के ठहराव का एक बड़ा हिस्सा हमसे छीन लिया है. मोबाइल के जरिये झट से पहुंच जाने वाले संदेश ने हमारा समय तो बहुत बचाया लेकिन ख्याल बुनने, उन्हें कागज पर उतारने और फिर पोस्ट करने वाली वह कड़ी खत्म कर दी जो इस कवायद को बहुत ही खास बनाती थी. पेशे से पत्रकार और जयपुर में रहने वाले कुशाल सिंह कहते हैं, ‘गांव से आने वाली मां की चिठ्ठी, किताब में छिपा महबूब का खत, या दोस्तों को लिखी शरारती चिठ्ठी….क्या एसएमएस कभी इनकी जगह ले पाएगा?’ और जैसे इतना ही काफी नहीं था, अब तो दुनिया के अलग-अलग कोनों से मोबाइल और एसएमएस पर ही तलाक देने की खबरें भी आने लगी हैं. बीते साल इंडोनेशिया के एक सरकारी अधिकारी ने अपनी दूसरी पत्नी को एसएमएस के जरिये तलाक दे डाला. एसएमएस ने और भी कई बदलाव किए हैं. एक वर्ग है जो मानता है कि इसने अंग्रेजी के परंपरागत व्याकरण की एक तरह से टांग तोड़ दी है. कई लोग हैं जो मानते हैं कि हर बार जब हम एसएमएस पर किसी शब्द का स्वरूप बिगाड़ते हैं तो हम दरअसल एक शब्द की हत्या कर रहे होते हैं. इतना ही नहीं, हमारी अभिव्यक्तियां भी नाइस, ऑसम, सैड जैसे शब्दों तक सिमटती जा रही हैं. शायद यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि एक समाज के रूप में हम अपनी भाषा खोते जा रहे हैं.
मोबाइल जब सुधर कर स्मार्टफोन हुआ तो जैसे यह अलादीन का चिराग ही हो गया. यह कुछ वैसा ही था जैसे इंटरनेट से लैस कंप्यूटर आपकी जेब में आ गया हो. नोकिया द्वारा 1996 में अपना पहला स्मार्ट फोन पेश किये जाने के बाद से अब तक इनकी संख्या बढ़कर एक अरब का आंकड़ा पार कर गई है. इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस समय देश में तकरीबन नौ करोड़ लोग अपने मोबाइल पर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और मार्च 2015 तक इनकी संख्या 16 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की वर्ष 2011 में आई रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त देश की 10 फीसदी आबादी यानी 12 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट पर सक्रिय थे जबकि इंटरनेट ऐंड मोबाइल ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश में कुल मिलाकर 14 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं. इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत चीन व अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है. चीन व अमेरिका में क्रमश: 52 करोड़ तथा 25 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. इंटरनेट पर सुरक्षा मुहैया कराने वाली कंपनी नॉर्टन द्वारा कुछ समय पहले कराए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले भारतीय सप्ताह में औसतन 58 घंटे का समय इंटरनेट पर देते हैं.
दरअसल मोबाइल हो या कंप्यूटर, अपने मूल उद्देश्यों का विस्तार करके ये मशीनें अब बहुआयामी उपकरणों यानी मल्टीटॉस्किंग डिवाइसेज में बदल गई हैं. इन उपकरणों ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है. ये कई काम एक साथ कर सकते हैं और वह भी बहुत जल्दी. अब ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से मिनटों में देश के किसी भी कोने में स्थित किसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. न छुट्टी की मुश्किल और न अपनी बारी का इंतजार करने की. और अगर अपनी बारी का इंतजार करने की नौबत आ ही जाए, जैसे कि किसी डॉक्टर के क्लीनिक में, तो भी कोई मुश्किल नहीं है. वहां भी आपका फोन या उसमें मौजूद इंटरनेट आपकी बोरियत को दूर कर सकता है. क्योंकि वह सिर्फ फोन नहीं बल्कि वीडियो गेम, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, ई बुक रीडर सब कुछ है. यानी अब ऊबने का कोई बहाना नहीं है. बीते साल मशहूर ब्रिटिश कंपनी ओटू ने एक सर्वे करवाया था. इसमें पता चला कि ब्रिटेन में स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे लोग रोज औसतन करीब दो घंटे मोबाइल के साथ बिता रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें सबसे ज्यादा समय (करीब 24 मिनट) वे इंटरनेट सर्फ करने में लगा रहे थे. इसके बाद सोशल नेटवर्क का नंबर था. फिर संगीत सुनने का और फिर गेम खेलने का. फोन और एसएमएस जैसी गतिविधियां, जो कभी फोन का बुनियादी उद्देश्य होती थीं, उनका नंबर इस सूची में पांचवें और छठें स्थान पर आया.
लेकिन ऊबने का अगर कोई बहाना नहीं है तो इसके चलते सब कुछ अच्छा ही हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है. इस दौर के बचपन में खेल की मौजूदगी घटती जा रही है. आज की पीढ़ी खेल के मैदानों को कंप्यूटर स्क्रीन के भीतर दाखिल कर चुकी है और हो सकता है कि अगली पीढ़ी के बच्चे बाजार हाट जैसी चीजों को भी केवल फिल्मों और किस्सों कहानियों में ही महसूस करने लगें. कम से कम तेजी से बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग कारोबार से तो यही संकेत मिलता है. एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में ऑनलाइन शॉपिंग कारोबार 10 खरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है. अमेजन, ईबे, फ्लिपकार्ट, ट्रेडस, जबॉन्ग, माइन्त्रा, मेकमाइट्रिप, यात्राडॉटकाम जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों की मदद से आज जूते, कपड़े, मोबाइल से लेकर बड़े-बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम और रेल या हवाई यात्रा के टिकट तक खरीदे जा सकते हैं.
इंटरनेट की इस सर्व और सहजसुलभता के अपने खतरे भी हैं. आप इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं तो ठगों ने भी इसके जरिये आपसे फायदा उठाने की तरकीबें ईजाद कर ली हैं. कहीं लोग किसी बड़ी कंपनी की लॉटरी के नाम पर ठगे जा रहे हैं तो कहीं किसी और तरीके से. इंटरनेट पर पोर्न सामग्री प्रचुरता से और महज एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है. बुरी बात यह है कि इस पर किसी तरह का फिल्टर भी नहीं है. कोई भी अपनी उम्र 18 साल से अधिक बताकर पोर्न की काली रहस्यमय दुनिया में दाखिल हो सकता है. यानी बच्चों और किशोरों के लिए इसके खतरे ज्यादा हैं. सिडनी विश्वविद्यालय के एक हालिया शोध ने इंटरनेट पोर्न के बढ़ते खतरे को उजागर किया है. शोध में शामिल 800 से ज्यादा लोगों में से 43 फीसदी ने माना कि उन्होंने 11 से 13 साल की उम्र के बीच पोर्न देखना शुरू किया था. कहने की जरूरत नहीं कि पोर्न तक उनकी आसान पहुंच इंटरनेट ने बनाई थी. शोध के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए सैन फ्रांसिस्को के मनोविज्ञानी माइकल हालवर्ड का कहना था, ‘ पोर्न एडिक्शन के शिकार लोगों में से ज्यादातर इससे बचे रहते अगर यह इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता.’ उन्होंने कहा कि सरल पहुंच वाला यह पोर्न लोगों में यौन कुंठा तथा यौन हिंसक व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है. जाहिर है अगर माइक्रोसॉफ्ट के प्रमोटर बिल गेट्स अपने बच्चों के कंप्यूटर पर चाइल्ड लॉक लगाकर रखते थे तो यह उनकी कितनी बड़ी मजबूरी थी.
इंटरनेट की बात हो तो सबसे पहले गूगल का नाम मन में कौंधता है. हर पल दुनिया में लाखों लोग इस पॉवरफुल सर्च इंजिन का इस्तेमाल अपने लिए जरूरी जानकारी जुटाने में करते रहते हैं. इसने हमारी स्मृति को बहुत तगड़ी क्षति पहुंचाई है. लोग अब कुछ भी याद नहीं रखना चाहते क्योंकि उनको पता है कि गूगल क्षण भर में उनको सारी जानकारी दे देगा. लेकिन स्मृति पर हमला तो सिर्फ एक पहलू है. प्रियदर्शन कहते हैं, ‘ज्ञान की यह सर्वसुलभता एक सीमा के बाद ज्ञान के लिए ही घातक हुई जा रही है. चूंकि पहले से कुछ भी जानना जरूरी नहीं रह गया है, इसलिए सोचना और विचार करना, उद्वेलित होना और प्रश्न खड़े करना भी छूट गया है. अब बने-बनाए प्रश्न हैं जिनके बने-बनाए उत्तर हैं. ज्ञान अब दुस्साहसी अन्वेषकों की सत्य-साधना से नहीं आता, वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे किसी बुद्ध की सात साल की प्रतीक्षा से नहीं आता, वह वैज्ञानिकों की प्रयोगधर्मी चेतना का नतीजा नहीं होता, वह एक पेशेवर उद्यम और सोचे-समझे निवेश का नतीजा होता है जिसके खोले हुए विश्वविद्यालयों, संस्थानों और केंद्रों में पूंजी को माकूल पड़ने वाला ज्ञान गढ़ा और बांटा जाता है- ऐसा ज्ञान नए टीवी, फ्रिज और कंप्यूटर बनाने के काम आता है, नया दिमाग और नया मनुष्य बनाने के काम नहीं.’
सोशल नेटवर्क
एक अरब सदस्यों का आंकड़ा पार कर चुकी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है. हालांकि इससे पहले ऑरकुट नामक वेबसाइट भी ऐसा प्रयास कर चुकी थी लेकिन उसे फेसबुक जैसी सफलता हासिल नहीं हो सकी थी. जैसे-जैसे सोशल नेटवर्क की लोकप्रियता बढ़ी, यह सवाल भी बढ़ता गया कि आखिर यह हमारे दिलोदिमाग पर क्या असर डालता है. तमाम अध्ययनों से यह बात साबित हो चुकी है कि सोशल नेटवर्क के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव हैं.
सकारात्मक असर की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग नए दोस्त और संपर्क बनाने में मदद कर रहा है. स्कूल के दिनों में बिछड़े दोस्तों को दसियों साल बाद खोज पाना सोशल नेटवर्किंग साइटों की वजह से ही संभव हुआ. इसने लोगों को आपसी बातचीत बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है. सोशल नेटवर्क लोगों की कारोबारी संभावनाओं को भी मजबूत बना रहा है. वहां अनेक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद हैं जो खास ब्रांडों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं. सोशल मार्केटिंग दरअसल भविष्य की मार्केटिंग है.
कई कंपनियों ने अब एक नया चलन भी शुरू किया है. वे कर्मचारियों को भर्ती करने से पहले चुपचाप उनके फेसबुक प्रोफाइल विजिट करती हैं. इससे उनको कर्मचारियों के सामाजिक दायरे, उनकी पसंद और काम को लेकर उनकी गंभीरता जैसी महत्वपूर्ण बातों का सही-सही अंदाजा मिल जाता है. वहीं तमाम ऐसे केस भी देखने को मिले हैं जहां पति-पत्नी एक की हरकतों पर नजर रखने के लिए फर्जी प्रोफाइल बनाकर एक दूसरे की मित्र सूची में दाखिल हो रहे हैं.
वर्ष 2011 में दुनिया ने सोशल नेटवर्क की असाधारण ताकत तब देखी जब वह समूचे अरब जगत में क्रांति का अग्रदूत बनकर सामने आया. हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में असाधारण सफलता पाने वाली आम आदमी पार्टी का आंदोलन जितना सड़क पर दिखता रहा, उतना ही फेसबुक और ट्विटर पर भी छाया रहा. प्रियदर्शन कहते हैं, ‘अब आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए डुग्गी नहीं पिटवानी पड़ती, मुनादी नहीं करवानी पड़ती, जगह-जगह छोटी-छोटी सभाएं नहीं करनी पड़तीं, आप फेसबुक पर एक पेज बनाते हैं और धीरे-धीरे लोग उस पेज को एक मंच में बदल डालते हैं. जेसिका के इंसाफ से लेकर अण्णा के आंदोलन तक जितनी लड़ाइयां सड़क पर लड़ी गईं, उससे कम फेसबुक या ऐसे दूसरे वर्चुअल, यानी आभासी माध्यमों पर नहीं. ‘
लेकिन इसी सोशल नेटवर्किंग के कुछ चिंताजनक पहलू भी हैं. फेसबुक से जुड़े अनेक शोधों से यह बात सामने आ चुकी है कि वहां मनवांछित संख्या में कमेंट और लाइक्स नहीं मिलने के चलते लोगों में अवसाद जैसी समस्याएं तक देखने को मिल रही हैं. बर्लिन के हंबोल्ट विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक फेसबुक आपसी ईर्ष्या और दुश्मनियों को भी बढ़ावा दे रहा है. तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें लोग अपने दोस्तों की प्रोफाइल पर उनके खूबसूरत साथियों, छुट्टियों और ऑफिस में सक्सेज की तस्वीरें देखते हैं और उनसे जलन महसूस करते हैं. कई बार यह जलन अपराध की वजह बन जाती है. शोधकर्ता हाना क्रास्नोवा के मुताबिक उनकी टीम यह देखकर चकित रह गई कि फेसबुक पर लोग अपने दोस्तों की अच्छी खुशनुमा तस्वीरें देखने के बाद खुश होने के बजाय अवसादग्रस्त हो जाते हैं और उनके अंदर ईर्ष्या की भावना जोर मारने लगती है.
कुछ समय पहले फिलीपींस के अल सल्वाडोर कस्बे में एक 13 वर्षीय किशोर की उसके दोस्त ने महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने फेसबुक पर उसकी महिला मित्र के साथ उसकी तस्वीर पर ऐसी टिप्पणी कर दी थी जो उसे नागवार गुजरी. इसी तरह कुछ समय पहले दिल्ली में 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ उसके फेसबुक मित्र तथा उसके भाई ने बलात्कार किया. मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले आरोपियों ने फेसबुक पर दोस्ती के बाद छात्रा को नए साल की पार्टी का निमंत्रण दिया और उसके साथ बलात्कार किया. ऐसी घटनाओं की सूची लगातार बढ़ती जा रही है.
महानगरीय जीवनशैली की गिरफ्त में फंसे लोगों के पास जहां असली रिश्तों को निभाने का वक्त कम से कमतर होता जा रहा है वहीं ऐसे आभासी रिश्ते उन्हें उस अपराधबोध से दूर ले जा रहे हैं जो उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं निभाने के कारण होती हैं. लोगों ने अपनी असली पहचान को इंटरनेट आईडी के पीछे छिपा लिया है. वहां आप अपनी पसंद से नकली नाम, उम्र, शक्ल और दोस्त तय कर सकते हैं. जाहिर है इस बात ने लोगों के आपस में सीधी मुलाकात करने की आदत पर असर डाला है. यहां तक कि एक छत के नीचे रहने वाले लोग भी आपस में उतनी बातचीत नहीं करते हैं जितनी कि वे फेसबुक पर दूसरों से करते हैं.
सोशल नेटवर्किंग हमारी कार्यक्षमता पर भी असर डाल रही है. सूचना तकनीक से जुड़े मसलों पर शोध करने वाली कंपनी न्यूक्लियस रिसर्च के मुताबिक ब्रिटेन में फेसबुक इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों की उत्पादकता में 1.5 फीसदी की कमी आई है. इस वजह से इन कंपनियों को औसतन 2.2 अरब पाउंड तक का सालाना नुकसान झेलना पड़ रहा है.
साइबर विशेषज्ञ तथा स्तंभकार पीयूष पांडे कहते हैं, ‘आभासी दुनिया और एकांत व निराशा परस्पर एकदूसरे पर निर्भर हैं. निराश व एकांतप्रिय लोगों को अधिक भाती है. साथ ही यह दुनिया लोगों को निराश और एकांतप्रिय भी बनाती है. रही बात सोशल मीडिया और स्मार्ट फोन की तो इनकी वजह से सूचनाओं का आधिक्य हो गया है. हमारे पास आज सूचनाएं तो भरपूर मात्रा में हैं लेकिन उनका विश्लेषण करने के लिए वक्त ही नहीं है. नतीजतन सूचनाएं आपस में टकरा रही हैं और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है.’
प्रियदर्शन कहते हैं, ‘निजी स्तर पर ज्ञान का जो सरलीकरण है वह सामाजिक स्तर पर संबंधों के सरलीकरण में बदल रहा है. फेसबुक के जरिए अब सब दोस्त हैं और एक जैसे दोस्त हैं. उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी जानी है, उन्हें अपनी यात्राओं के बारे में बताना है, उन्हें अपनी पार्टियों के फोटो दिखाने हैं. यह बेताबी, यह उत्कंठा इतनी ज्यादा है कि पार्टी चल रही होती है और कोई मोबाइलधारी उसका फोटो फेसबुक पर अपलोड कर रहा होता है. कहना मुश्किल है, एक-एक क्षण की यह रंगीन प्रस्तुति किसी आत्मीय साझेपन से उपजी है या एक अविचारित प्रदर्शनप्रियता की पैदाइश है.’
‘हमारी जिंदगी में एक स्थाई तनाव पैदा हो गया है जिसका हमें अहसास नहीं’
 पिछले एक दशक के दौरान इंसानी व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो सबसे बड़े तकनीकी बदलाव कौन से हैं और क्यों?
पिछले एक दशक के दौरान इंसानी व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो सबसे बड़े तकनीकी बदलाव कौन से हैं और क्यों?
पिछले कुछ समय के दौरान मानव व्यवहार पर सबसे अधिक जिन दो चीजों ने डाला है वे हैं इंटरनेट और मोबाइल फोन. इंटरनेट से दुनिया छोटी हो गई. आपको एक पल में पता चल जाता है कि दुनिया के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है. इससे सांस्कृतिक दूरियां कम हो रही हैं. आज आपकी तुलना केवल अपने आसपास के लोगों से नहीं है बल्कि दूरदराज स्थित लोगों से भी है. भारत के किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के मां-बाप अमेरिका के उसी उम्र के स्कूली बच्चों की उपलब्धियों पर नजर रखते हैं जबकि दोनों का एक दूसरे से कोई लेनादेना नहीं है तो यह एक तरह का अनावश्यक दबाव पैदा करता है. कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट ने एक तरफ जहां हमें सूचना संपन्न बनाया है वहीं इसकी वजह से सूचनाओं की जो बमबारी हो रही है उसमें सही और गलत का फर्क मिट गया है. मोबाइल से यह हुआ कि आपकी उपलब्धता बढ़ गई. अब आप 24 घंटे लोगों की पहुंच में हैं. इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं. फायदा यह है कि आप अपने चाहने वाले लोगों से हमेशा जुड़े रह सकते हैं. जबकि इसका नुकसान यह है कि अब आप एक तरह से 24 घंटे काम पर हैं. पहले आपके काम के घंटे सुबह 10 से शाम पांच बजे तक तय थे और आपका सार्वजनिक जीवन भी इससे बहुत अधिक नहीं था. लेकिन अब कोई भी आपको कभी भी फोन करके बुला सकता है. आपका बॉस आपको देर रात भी काम करने के लिए कह सकता है. इसने जीवन में एक स्थायी तनाव को जन्म दिया है जिसका हमें अहसास नहीं है. तो तकनीक ने हमारी निजता खत्म कर दी है.
इंटरनेट की बात सोशल नेटवर्किंग के बिना अधूरी है. इसने लोगों की जिंदगी कैसे बदली है?
सोशल नेटवर्किंग से एक बड़ा बदलाव यह आया कि दोस्ती के पैरामीटर्स (मानक) बदल गए. अब दोस्तियां आपकी वाल पोस्ट पर आई लाइक्स और कमेंट्स से तय होती हैं. हालांकि देखा जाए तो इसके भी अपने फायदे हैं, लेकिन उसके लिए हमें संतुलन कायम करना होगा. इसने कम उम्र नौजवानों की आउटडोर एक्टिविटीज पर असर डाला है. अब वे घर से बाहर निकलकर खेलने कूदने के बजाय फेसबुक पर व्यस्त नजर आते हैं.
क्या सोशल नेटवर्किंग हमें सामाजिक एकाकीपन की ओर ले जा रही है?
नहीं. मैं पूरी तरह तो ऐसा नहीं मानता, हां इसमें कुछ सच्चाई जरूर हो सकती है. अभी सोशल नेटवर्किंग के कारण सोशल आइसोलेशन की स्थिति आई नहीं है लेकिन वह दिन दूर नहीं जब ऐसी स्थिति आ जाएगी. हो सकता है कि फेसबुक पर आपके पांच हजार दोस्त हों जिनमें से कई आपकी पोस्ट लाइक करते हों, उस पर कमेंट करते हों लेकिन संभव है कि निजी जिंदगी में आपका एक भी ऐसा दोस्त न हो जिसके साथ आप अपने दिल की बात साझा कर सकें.
इससे कैसे बचा जा सकता है?
इसमें संतुलन की बहुत बड़ी भूमिका है. माता-पिता को अपने बच्चों को यह समझाना होगा कि वे फेसबुक करें, ट्विटर का इस्तेमाल करें सब कुछ करें, लेकिन एक निश्चित समय तक. इसका असर वे अपनी पर्सनल लाइफ मसलन दोस्तों से मिलने, शाम को खेलने आदि पर नहीं पड़ने दें.
इंटरनेट के अत्यधिक इस्तेमाल का सबसे बड़ा खतरा क्या है?
इंटरनेट का सबसे बड़ा खतरा है पोर्नोग्राफिक कंटेंट तक लोगों की आसान पहुंच. आज कोई भी कच्ची उम्र का बच्चा कंप्यूटर पर महज एक क्लिक करक पोर्न सामग्री तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है. यह लोगों के सेक्सुअल बिहैवियर पर असर डाल रहा है. पोर्नोग्राफिक कंटेंट सेक्स के असल स्वरूप से इतर उसका विकृत रूप बच्चों के दिमाग में बिठाते हैं. इससे उन बच्चों के सेक्सुअल कांसेप्ट खराब हो रहे हैं. जाहिर है इसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है. अगर हम बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ बदलते जीवन और घुसपैठ करती तकनीक के साथ तालमेल बिठाना सिखा दें तो मुझे लगता है कि इसके जरिये इस समस्या से निपटने में मदद मिलेगी.
क्या इंटरनेट पोर्नोग्राफी की लत भी लग सकती है?
देखिए एक जैसी विकृत चीजों से अगर आप रोज ब रोज रूबरू होंगे तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ना लाजिमी है. लगातार पोर्न सामग्री देखने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. यह किसी भी अन्य तरह के एडिक्शन की तरह ही होता है जिससे हमारा जीवन और हमारे निजी रिश्ते प्रभावित होते हैं.
क्या गूगल और इंटरनेट हमारी याद्दाश्त को प्रभावित कर रहे हैं?
नहीं अभी तक तो ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है जिससे यह पता लग सके कि इनकी वजह से हमारी सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ा है. लेकिन हां, इसकी वजह से हमने चीजों को थोड़ा आसानी से लेना जरूर शुरू किया है कि, अरे चलो गूगल है न तो दिमाग पर इतना अधिक जोर क्यों देना. इनकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन आसानी से मिल रही है इसलिए हम उन्हें याद रखने के लिए दिमाग पर जोर नहीं देते. ध्यान दीजिए कि कैसे बेस फोन के जमाने में हमें ढेर सारे दोस्तों के नंबर याद रहते थे लेकिन आज मोबाइल की फोनबुक मे भी उन्हें नाम से तलाश करना पड़ता है.
कोई खास केस जो आपको याद रह गया हो
मेरे पास ऐसे युवाओं के मामले आए हैं जो रोजाना चार से छह घंटे तक इंटरनेट पर पोर्न सामग्री देखते थे. घर पर पता चलने के बाद जब उनको रोका गया तो उन्होंने किसी न किसी बहाने बाहर साइबर कैफे पर जाकर इसे देखना शुरू कर दिया. इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग की लत के शिकार युवाओं के केस आए हैं जो हमेशा इसी चिंता में घुलते रहते थे कि उनकी वाल पर कहीं किसी ने कुछ लिखा तो नहीं, कोई कमेंट तो नहीं किया. उनका बाकी किसी काम में मन नहीं लगता था. मेरे पास ऐसी लड़कियों के केस आए हैं जिन्होंने विभिन्न वेबसाइट पर दी गई सलाह पर अमल करके डाइटिंग की शुरुआत कर दी. बाद में उनको हालत बिगड़ने पर डॉक्टरी दवा और मनोवैज्ञानिक सलाह लेनी पड़ी. ऐसी लत को पकड़ पाना भी आसान नहीं है बिल्कुल नशे की लत के शिकार की तरह आदतों को बारीकी से पकड़कर ही इसका पता चल पाता है.
दर्शन देते देवता…

हर्षित, मुदित नाच रही है देह, थिरक, फुदक रहा मन. वाणी गई कहीं खो, नैन गए फैल, पलकें हुई निर्निमेष. कैसे… कैसे बखान करें देवता के रूप का ! कैसे बखान करें उसकी लीलाओं का! सुधबुध खो गई है हमारी. कैसे आज देवता ने ली हम जैसो की सुध! कैसे देवता प्रकट हुए आज हमारे दर!
न कोई यज्ञ. न कोई तप. न कोई अनुष्ठान. न कोई आह्वान. न कोई करुण क्रंदन. न कोई याचना. न कोई विनती. फिर कैसे देवता हुए प्रकट!
मात्र दर्शन ही नहीं, बहुत कुछ दे रहे हैं देवता. दर्शन के साथ मुस्कुराहट, मुस्कुराहट के साथ अपनी उर की गर्माहट, उर की गर्माहट के साथ अपने करकमल की कोमल छुवन, करकमलों की कोमल छुवन के अतिरिक्त करकमलों का हार, करकमलों का हार ही नहीं अपने वचनों की लंबी माला, वचनों की लंबी माला ही नहीं, हमारे सभी कष्ट हरने का ठोस आश्वासन. वाकई बहुत कुछ दे रहे हैं. अरे वे दे कहां रहे, वे तो लुटा रहे हैं. इतना कुछ लुटाने के बाद भी और बहुत कुछ लुटाने की चाह रखते हैं. वे बहुत कुछ लुटाने के बाद भी कितने धनवान दिख रहे हैं.
आज ऐसा लग रहा है कि वे केवल एक को नहीं, सबको वर देने के मूड में है. और केवल एक वर ही क्यों! वे थोक में वर देने के मूड हैं. आज… आज वे किसी को निराश नहीं कर रहे. हाथ मिलाओे तो हाथ मिलाएंगे. गले लगाओ तो गले लगेंगे. सिर झुकाओ तो नत हो जाएंगे. पैर छुओ तो आशीर्वाद देंगे. भेंट करोगे तो भेंट देंगे. जो मांगो वह मिलेगा. ओहो, कितना विशाल नरम ह्नदय लेकर प्रकट हुए हैं, देवता!
कहां हम मात्र देवता की कामना करते थे पंरतु आज मात्र देवता ही नहीं प्रकट हुए, साथ उनके प्रकट हुई है यक्ष,गंधर्व की टोली भी. देवता अकेले नहीं आए हैं. क्या बहुत अधिक प्रतीक्षा कराने की परीक्षा का यह अतिरिक्त फल है! क्या उनके मन में कहीं किसी प्रकार का कोई खटका है! क्या उन्हें अपने भक्तों की नियत में खोट दिखा है! क्या वे किसी असुरक्षा भाव से घिरे हुए हैं? क्या उन्हें अपने पुजारियों की निष्ठा डगमगाती हुई दिखी! पुजारी पूजा न करे तो काहे का देवता! भक्त अगर सुमिरन न करे तो देवता का कैसा प्रताप! कैसी उसकी सत्ता! नहीं… नहीं… देवता को किसका डर! देवता को कैसा डर!
आज देवता स्वयं मझधार में हैं. देवता का देवत्व आज चुनाव की धार में है. उन्हें डर है कहीं उनका देवत्व इस धार में बह न जाए. हर पांच साल बाद ऐसी घड़ी आती है जब देवता बिन बुलाए ही प्रकट होते हैं. देवता जानता है कि लोकतंत्र के मंदिर में अगर उसे पुनः शोभायमान होना है तो उसे चुनाव का चक्रव्यूह भेदना होगा. देवता जानता है कि इसके लिए उसके कवच-कुंडल प्रर्याप्त नहीं. यह चक्रव्यूह तो भिदेगा वोटरूपी तीरों से. और वे तीर रखे हैं हम जैसे वंचितों के कमंडल में. वे एक-एक कमंडल का खंगालने निकले हैं इसलिए देवता दर्शन देने के लिए श्रम कर रहे हैं. देवता स्वयं दया का पात्र दिख रहा है. सुविधाभोगी देवता आज श्रमजीवी बन गया है. हाय! तनिक देखो तो!
कहीं थोक में देवताओं के दर्शन सुलभ हो रहे हैं या यूं कहें कि वे मनुष्यता ग्रहण करने लगे हैं, तो वहीं कहीं कोई मनुष्यता छोड़कर देवत्व पाने की ओर अग्रसर होना चाह रहा है.
लोकतंत्र में चुनाव की बेला भी क्या बेला है!
जो बली उसी की चली
[wzslider autoplay=”true” transition=”‘slide'” info=”true” lightbox=”true”]
सोमवार 24 मार्चः नीदरलैंड (हॉलैंड) की राजधानी हेग में जी-7 देशों का शिखर सम्मेलन. सप्ताह-भर पहले तक वह जी-8 कहलाता था. विश्व के सर्वप्रमुख औद्योगिक देशों की इस बिरादरी में 1998 से रूस भी बैठा करता था. इस बार उसे बाहर बिठा दिया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा यही चाहते थे. सम्मेलन से पहले डच प्रधानमंत्री मार्क रुटे के साथ वे पास ही में एम्सटर्डम का ‘राइक्स म्यूजियम’ देखने पहुंचे. वहां 17 वीं सदी के प्रसिद्ध डच चित्रकार रेम्ब्रांट (डच उच्चारण रेम्ब्रोंत) की कृति ‘रात्रिप्रहरी’(द नाइट वॉच) के सामने ठहर गए. 1642 की इस पेंटिंग में रेम्ब्रांट ने स्पेनी आधिपत्य के विरुद्ध डच जनसेना के कूच को दर्शाया है. तस्वीर को देखते ही, हो सकता है, ओबामा यूक्रेन के बारे में सोचने लगे हों.
दिसंबर के बाद से यूक्रेन में बहुत कुछ बदल गया है. जनविद्रोह के कारण राष्ट्रपति विक्तोर यानुकोविच को अपना पद खोना पड़ा. बदले में यूक्रेन को अपने दक्षिणी स्वायत्तशासी प्रदेश क्रीमिया से हाथ धोना पड़ा. रूस को जी-8 की सदस्यता खोनी पड़ी. अब उसे तरह-तरह के दंडात्मक प्रतिबंध भी झेलने होंगे. उधर, प्रतिबंध लगाने वाले सोच में पड़ गये हैं कि रूस के साथ तनातनी बढ़ने से उन्हें खुद भी क्या कुछ खोना पड़ सकता है. फिलहाल तो वे रूसी भालू को अपना बाहुबल दिखाने पर अड़े हैं.
हेग में डच प्रधानमंत्री के निवास पर हुई वार्ताएं केवल डेढ़ घंटे चलीं. राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, ‘क्रीमिया जब तक रूस की मुट्ठी में है, रूस को उसके ‘समावेशन की कीमत चुकानी होगी.’ ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन चाहते थे कि रूस को जी-8 से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए. सभी सात शिखर नेता एकमत थे कि यूक्रेन से नाता तोड़ने का क्रीमियाई जनमतसंग्रह और रूसी संघ में क्रीमिया का विलय अंतराराष्ट्रीय कानून का सरासर उल्लंघन है.
कानून और हकीकत
अंतरराष्ट्रीय कानून, आम सहमति पर आधारित कुछ ऐसे मानकों के ढांचे जैसा है, जो सरकारों और देशों के बीच टिकाऊ किस्म के व्यवस्थित संबंधों का नियमन करते हैं. पहले से चल रही ऐसी परिपाटियां, देशों और सरकारों के बीच के ऐसे संधि-समझौते और सभा-सम्मेलनों के आधार पर सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं-संगठनों के अंतरराष्ट्रीय महत्व के ऐसे निर्णय भी उसका स्रोत बन सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र से मेल खाते हैं. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय और महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव भी अंतरराष्ट्रीय कानून का रूप धारण कर सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय कानून किसी देश के संविधान या किसी दंडसंहिता के समान अनुच्छेद या धाराबद्ध नहीं है. केवल एक फ्रेम है, इसलिए उस में अस्पष्टता और मनपसंद अर्थ लगाने की गुंजाइश भी मिल ही जाती है.
अंतरराष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों संबंधी 24 अक्टूबर 1970 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव नंबर 2625(XXV) में कहा गया हैः ‘हर राज्यसत्ता का यह कर्तव्य है कि अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वह किसी दूसरे राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध ऐसी किसी धमकी या बलप्रयोग से परहेज करे या कोई ऐसा काम न करे, जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के विरुद्ध है. अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के निपटारे के लिए ऐसी धमकी या बलप्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र का उल्लंघन है और उसका कतई उपयोग नहीं होना चाहिये.’
लेकिन, सच्चाई यह है कि अमेरिका और उस के संगी-साथी अपने हितों के अनुसार बलप्रयोग से परहेज के इस नियम को हमेशा तोड़ते-मरोड़ते रहे हैं.
15 जुलाई 1974 के दिन भूमध्यसागरीय द्वीप-देश साइप्रस की सेना के एक हिस्से ने सत्ता हथिया ली. राष्ट्रपति आर्चबिशप मकारियोस को जान बचाने के लिए भागना पड़ा. साइप्रस के उत्तर-पूर्वी हिस्से में रहने वाले तुर्क समुदाय की रक्षा के नाम पर तुर्की ने पांच दिन बाद साइप्रस पर आक्रमण शुरू कर दिया. उसने एक महीने के भीतर साइप्रस के 40 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया और 13 फरवरी 1975 को उसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया. साइप्रस तब से विभाजित है. तुर्की 1952 से अमेरिका वाले नाटो सैन्य-संगठन का सदस्य है, इसलिए उसका कोई बाल बांका नहीं हुआ. तुर्क सेना कुर्द-विद्रोहियों का पीछा करते हुए कई बार इराक में भी दूर तक घुस चुकी है. क्या भारतीय सेना भी घुसपैठियों का पीछा करते हुए कथित ‘आजाद कश्मीर’ में घुसने की कभी हिम्मत कर सकती है?
मात्र 91 हजार की जनसंख्या वाले कैरेबियाई द्वीप-देश ग्रेनाडा में 1983 में सेना ने सत्ता पलट दी. यह कहते हुए कि वहां सोवियत संघ और क्यूबा के कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं और हमें अपने नागरिकों की रक्षा करनी है, अमेरिका ने 23 अक्टूबर 1983 को ग्रेनाडा पर बमबारी शुरू कर दी. उसने दो ही दिन में वहां कब्जा कर पुरानी सरकार को बहाल कर दिया. अमेरिकी वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुछ नहीं कर सकी. केवल महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर अमेरिकी आक्रमण की निंदा की.
सिलसिला यहीं नहीं रुकता. 1980 वाले दशक में पनामा के सत्ताधारी मानुएल नोरियेगा पर मादक द्रव्यों की तस्करी का आरोप लगाया गया. नोरियेगा को पकड़ने के लिए 20 दिसंबर 1989 को अमेरिकी वायुसेना ने आक्रमण शुरू कर दिया. 11 दिनों तक वैटिकन के पनामा स्थित दूतावास में छिपे रहने के बाद नोरियेगा ने तीन जनवरी 1990 को आत्मसमर्पण कर दिया. नोरियेगा पर अमेरिका में मुकदमा चला कर 10 जुलाई 1992 को उन्हें 40 साल के लिए जेल भेज दिया गया. नोरियेगा 10 साल तक सीआईए एजेंट भी रह चुके थे. 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अल कायदा के आतंकवादी हवाई हमलों के बाद अमेरिका ने जिन सच्चे-झूठे बहानों की आड़ लेकर अफगानिस्तान में तालिबान और इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता का सफाया किया, वह किन्हीं अन्य कारणों से उचित भले ही रहा हो, अंतरराष्ट्रीय कानून-सम्मत तो नहीं ही था.
आत्मनिर्णय का अधिकार
किसी देश का बंटवारा कैसे हो? कोई नया देश कैसे बने? या किसी देश का किसी दूसरे देश के साथ विलय कैसे हो? इस बारे में अंतरराष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों वाली संयुक्त राष्ट्र घोषण को सबसे अधिक तोड़ा-मरोड़ा गया है. इस घोषणा का कहना हैः हर जनता के लिए आत्मनिर्णय के एकसमान अधिकार के सिद्धांत का पालन करते हुए… ‘अपने स्वंतत्र निर्णय के बल पर किसी जनता द्वारा अपने लिए एक स्वतंत्र, सार्वभौम राज्यसत्ता की सथापना, किसी अन्य स्वतंत्र राज्यसत्ता के साथ संयोजन या एकीकरण या कोई अन्य राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करना, आत्मनिर्णय के उसके अधिकार को अमल में लाने के तरीके हो सकते हैं.’
जनता क्या चाहती है? उस का स्वतंत्र निर्णय क्या है? इसे जानने का सर्वोत्तम तरीका है जनमतसंग्रह द्वारा जनता की राय पूछना. संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में हुए इसी तरह के जनमतसंग्रहों के आधार पर 1991 में अफ्रीकी देश इरिट्रिया इथियोपिया से और 2011 में दक्षिणी सूडान शेष सूडान से अलग हो कर स्वतंत्र देश बन गया. जनमतसंग्रह के आधार पर ही अमेरिका से 3700 किलोमीटर दूर का हवाई द्वीपसमूह, 21 अगस्त 1959 के दिन से, अमेरिका का 50वां राज्य कहलाता है, जबकि स्पेनी भूमि पर स्थित ब्रिटिश उपनिवेश जिब्राल्टर, स्पेन के सारे प्रयासों को ठेंगा दिखाते हुए, अब भी ब्रिटिश बना हुआ है. भारत से कहा जाता है वह कश्मीर में जनमतसंग्रह क्यों नहीं करवाता. लेकिन, यही मांग तिब्बत के प्रसंग में चीन से, बास्कलैंड के प्रसंग में स्पेन से या कोर्सिका के प्रसंग में फ्रांस से नहीं की जाती.
घर लौटा क्रीमिया
यूक्रेन में 21 फरवरी को हुए आकस्मिक सत्तापलट के बाद उसके दक्षिणी स्वायत्तशासी प्रदेश क्रीमिया की स्थानीय संसद और सरकार ने 16 मार्च को जब वहां जनमतसंग्रह कराया, तो पश्चिमी देशों ने आसमान सिर पर उठा लिया. 23 लाख जनसंख्या वाले क्रीमिया की 60 प्रतिशत जनता रूसी, 24 प्रतिशत यूक्रेनी और 12 प्रतिशत तातार जाति वाली इस्लामधर्मी है. बताया गया कि 80 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया जिनमें से 97 प्रतिशत ने रूस के साथ विलय का समर्थन किया. एक सप्ताह के भीतर विलय की कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयीं. उल्लेखनीय है कि स्टालिन की मृत्यु के बाद 1953 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता बने निकिता ख्रुश्चेव ने, 1954 में, क्रीमिया प्रायद्वीप, जो 200 वर्षों से रूस का हिस्सा था, यूक्रेन को उपहार में दे दिया था. उस वर्ष रूस में यूक्रेन के विलय की 300वीं जयंती मनाई जा रही थी. ख्रुश्चेव स्वयं भी यूक्रेनी थे. शायद सोच रहे थे, क्रीमिया यूक्रेनी हो या रूसी, अंततः रहेगा तो सोवियत संघ में ही. उन्हें क्या पता कि एक दिन सोवियत संघ खुद ही नहीं रह जायेगा.
लेकिन, हर समय आत्मनिर्णय और जनमतसंग्रह की गुहार लगाने वाले पश्चिमी नेता क्रीमिया के जनमतसंग्रह पर बिफर गए. कहने लगे, यूक्रेनी संविधान अलगाव के लिए जनमतसंग्रह की अनुमति नहीं देता इसलिए जनमत संग्रह अवैध है. स्वयं अमेरिका भी ब्रिटेन की सहमति से नहीं, उसके प्रति विद्रोह के द्वारा स्वतंत्र हुआ था. पहली बात, संसार के हर देश का संविधान क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर ही लक्षित होता है. दूसरी बात, किएव में तीन महीनों से तोड़-फोड़ व आगजनी कर रहे प्रदर्शनकारियों ने 21 फ़रवरी की शाम जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के विदेश मंत्रियों की नाक के नीचे जिस तरह सत्ता हथिया ली, यूक्रेनी संविधान उसकी भी अनुमति नहीं देता. और तीसरी बात, स्लोवेनिया और क्रोएशिया भी 1991 में अपने यहां एकतरफा जनमतसंग्रह करवा कर भूतपूर्व युगोस्लाविया से अलग हो गए थे. उस समय यूक्रेन ही क्रोएशिया को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश था.
युगोस्लाविया का विघटन
युगोस्लाविया से अलग हुए दोनों नए देशों को मान्यता देने के लिए तत्पर जर्मनी ने युगोस्लाविया के अन्य गणतंत्रों को भी ऐसा ही करने के लिए उकसाया था. यहां तक कि स्लोवेनिया और क्रोएशिया को राजनयिक मान्यता टाल देने के 15 दिसंबर 1991 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रस्ताव की अवहेलना करते हुए, एक ही सप्ताह बाद, जर्मनी की जिद पर पहले स्लोवेनिया को और फिर क्रोएशिया को यूरोपीय संघ के उस समय के सभी 12 देशों ने मान्यता देदी. इससे युगोस्लाविया के बोस्निया और मेसेडोनिया जैसे वे गणराज्य भी अलग होने के लिए छपटाने लगे, जो तब तक शांत थे. युगोस्लाविया में भीषण गृहयुद्ध छिड़ गया. भारी मारकाट हुई. यहां तक कि युगोस्लाविया के सर्बिया गणराज्य का मुस्लिम बहुल प्रदेश कोसोवो भी, जर्मनी की अगुआई में सर्बिया पर बमबारी की बलिहारी से, 2008 में एक स्वतंत्र देश बनने में सफल हो गया. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार जर्मन विमानों ने किसी दूसरे देश पर बम बरसाए थे– वह भी इसलिए कि वह खंडित हो जाए. तब जर्मनी के चांसलर रहे गेरहार्ड श्रोएडर अब इस बमबारी पर पछताते हैं. यूक्रेन के संदर्भ में उन पुराने दिनों को याद करते हुए जर्मन नगर हैम्बर्ग में गत 9 मार्च को अपने एक भाषण में श्रोएडर ने पश्चिमी देशों की दोहरी नैतिकता की आलोचना की. उन्होंने कहा कि ‘चांसलर रहते हुए युगोस्लाविया युद्ध के समय मैंने स्वयं अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ा है… हमने नाटो के साथ मिल कर सर्बिया पर बमबारी करने के लिए अपने विमान भेजे. सुरक्षा परिषद के किसी प्रस्ताव के बिना एक सार्वभौम देश पर बमबारी की.’ इस स्वीकारोक्ति के लिए उनकी सरहाना करने के बदले जर्मनी में उन्हें ‘पूतिन का यार’ बता कर उन की खिल्ली उड़ाई जा रही है. यूरोपीय संसद के जर्मन सांसद उन का मुंह बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पास करवाना चाहते हैं.
पूर्व चांसलर श्रोएडर की ही तरह पिछले दशक में यूरोपीय आयोग में संघ के विस्तार संबंधी मामलों के आयुक्त रहे जर्मन राजनीतिज्ञ ग्युंटर फ़रहोएगन भी यूक्रेन के प्रति पश्चिम के अतिरंजित मोह से दुखी हैं. बीती 21 फ़रवरी को अत्यंत संदिग्ध परिस्थितियों में बनी यूक्रेन की अंतरिम सरकार को जर्मनी और यूरोपीय संघ ने जिस आनन-फ़ानन में मान्यता दे दी, उसकी आलोचना करते हुए एक रेडियो-इंटरव्यू में फ़रहोएगन ने कहा, ‘किएव में 21वीं सदी की ऐसी पहली सरकार बनी है, जिस में फासिस्ट बैठे हुए हैं… असंवैधानिक तरीकों से सत्ता में आई एक ऐसी सरकार को मान्यता देकर, उस के साथ सहयोग कर और उसे हर तरह की चीज़ें परोस कर यूरोपीय संघ स्थिति को और भी गंभीर बना रहा है. यह नहीं होना चाहिये था. विशेषकर जर्मनी को तो यह कभी नहीं करना चाहिये था.’
जब यानुकोविच भागे
जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के विदेशमंत्रियों के मध्यस्थता-प्रयासों से, 21 फरवरी के दिन, किएव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्तोर यानुकोविच और उनके विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच एक ऐसे समझैते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिस में प्रदर्शनकारियों की सारी मुख्य मांगें मान ली गई थीं. तब भी, किएव के मैदान-चौक पर रात-दिन धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों के सबसे उग्रवादी गुट ने समझौते को ठुकरा दिया और कहा कि अब वे राष्ट्रपति भवन और सरकारी मंत्रालयों पर कब्जा करेंगे. इससे राष्ट्रपति यानुकोविच को लगा कि अब जान खतरे में है, यहां से भाग निकलो. वे उसी शाम भूमिगत हो गए.
यानुकोविच के विरोधियों को जैसे ही भनक मिली कि किएव में सत्ता-शून्यता पैदा हो गई है, उन्होंने उसी रात अपनी एक अंतरिम सरकार बना कर सत्ता हथिया ली. समझौते पर हस्ताक्षर के केवल 10 घंटों के भीतर यह सब हो गया. यूरोपीय संघ वाले तीनों विदेशमंत्री तब तक किएव में ही थे. लेकिन, कुछ ही घंटे पहले के समझौते को उठा कर कूड़े पर फेंक देने की निन्दा करने के बदले तीनों देशों की सरकारों ने यह जानते हुए भी अंतरिम सरकार को मान्यता दे दी कि उस के कम से कम पांच मंत्री उग्र-दक्षिणपंथी और नव-नाजीवादी हैं. अंतरिम सरकार ने अपने पहले ही आदेश में रूसी भाषा को देश की दूसरी राजभाषा के पद से हटाते हुए यूक्रेनी को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया. स्वाभाविक था कि इससे क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के रूसी-भाषियों के बीच खलबली मच गई. वे सोचने लगे कि उनकी सुरक्षा इसी में है कि उनका भूभाग रूस का अंग बन जाए. क्रीमिया तो इस बीच रूस का अंग बन गया है, जबकि पूर्वी यूक्रेन में रूस के साथ विलय के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं.
नेकनीयती में संदेह
रूस यूक्रेन की अंतरिम सरकार को मान्यता देने से मना कर रहा है. उसका कहना है कि वह सत्ता-पलट द्वारा, न कि किसी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा, सत्ता में आई है. अंतरराष्ट्रीय कानून भी संवैधानिक प्रक्रिया को ही प्राथमिकता देता है. अंतरिम सरकार ने 25 मई 2014 को संसद और राष्ट्रपति के चुनाव करवाने की घोषणा की है. यदि इरादा सचमुच ईमानदारी भरा है, तो जरूरी नहीं था का यूरोपीय संघ और अमेरिका एक कामचलाऊ अंतरिम सरकार को तुरंत मान्यता देते. ईमानदारी पर संदेह इसलिए भी होता है, क्योंकि होग में जी-7 शिखर सम्मेलन से एक सप्ताह पहले, 15 मार्च के दिन, ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ ओर यूक्रेन की अंतरिम सरकार ने उस अशुभ ‘साझेदारी समझौते पर’हस्ताक्षर कर ही दिये, जिस पर यानुकोविच द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने के बाद यह सारा झमेला खड़ा हुआ था.
यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर करने का पुरस्कार एक अरब डॉलर से बढ़ा कर 15 अरब डॉलर कर दिया है. इतनी उदारता और जनादेश प्राप्त किसी वैध सरकार के साथ हस्ताक्षर करने से बचने की इस उतावली के पीछे कोई नेक इरादा होना संभव नहीं लगता. यूरोपीय संघ के मन में कहीं न कहीं यह शंका है कि है कि चुनावों के बाद की यूक्रेनी सरकार भी यानुकोविच की तरह ही हस्ताक्षर करने से मना कर सकती है, इसलिए बेहतर है कि कामचलाऊ सरकार के हस्ताक्षर द्वारा नई सरकार को पहले से ही बांध लिया जाए. यदि रूस को नीचा नहीं दिखाना है तो यह तोड़-मरोड़, यह तिकड़मबाजी भला किसलिए?
घृणा की पराकाष्ठा
यूक्रेन में 2005 वाली ‘नारंगी क्रांति’ की नेत्री, क्रांति के बाद कुछ महीनों की प्रधानमंत्री, उस दौरान बन गई डॉलर-करोड़पति और अब राष्ट्रपति बनने की आकंक्षी यूलिया तिमोशेंको ने तो रूस के प्रति घृणा की पराकाष्ठा ही कर दी. मार्च के शुरू में वे बर्लिन के सबसे बड़े व नामी अस्पताल शारिते में भर्ती थीं. क्रीमिया में जनमतसंग्रह के बाद 18 मार्च वाले जिस दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन ने रूस में क्रीमिया के विलय की संधि पर हस्ताक्षर किये, संभवतः उसी दिन तिमोशेंको ने यूक्रेन के एक सांसद नेस्तोर शुफ़्रिच से टेलीफोन पर बात की. इस बातचीत की रिकर्डिंग अब यूट्यूब पर तहलका मचा रही है. तिमोशेंको बड़े उत्तेजित स्वर में कहती हैं, ‘मैं खुद कलाश्निकोव (मशीनगन) उठा कर उस गंदे (पूतिन) के सिर में गोली मारने के लिए तैयार बैठी हूं…हद हो गई है… हमें हथियार उठा कर इन दुष्ट रूसियों और उनके नेताओं का काम तमाम कर देना चाहिये… काश! मैं वहां होती और खुद अगुआई कर सकती. वे क्रीमिया पाने के बदले… (लिखने के अयोग्य अपशब्द)… खा रहे होते….मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगी. मौका मिलते ही अपनी सारी जान-पहचान इस्तेमाल करते हुए सारी दुनिया को जगा दूंगी कि रूस जल कर खाक बन गया खेत भर रह जाए… कंबख्त! उन पर ऐटमबम पटक देना चाहिए.’
यूलिया तिमोशेंको ने इस टेलीफोन बातचीत की पुष्टि की है. उनकी सोच और शब्दों से पता चल जाना चाहिये कि यूक्रेन के नेताओं का दिमाग किस तरह दीवालिया हो गया है. इससे भी चिंताजनक बात यह है कि रात-दिन लोकतंत्र, स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय के अधिकार और मानवाधिकरों का ढिंढोरा पीटने वाले पश्चिम के लोकतंत्र खोखले आदर्शों वाले प्रचारतंत्र बनते जा रहे हैं. उनकी चली, तो 21 वीं सदी में भी भैंस उसी की होगी, जिस के पास लाठी होगी. क्योंकि उन्हीं की चलती है, इसलिए मिल-मिलाकर यही सबसे निर्णायक अंतरराष्ट्रीय कानून है.
‘आम आदमी पार्टी वाम का विकल्प नहीं बन सकती’

सर्वेक्षणों की मानें तो केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियां बुरी तरह हार रही हैं. हो सकता है आप इससे सहमत न हों, लेकिन पिछले एक दशक में वाममोर्चे की असफलता क्या रही?
सर्वेक्षणों ने पहले भी हमेशा से वामदलों को कम करके आंका है. इस बार भी ऐसा ही है. केरल में वाममोर्चा 2009 लोकसभा चुनावों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगा. बंगाल में यदि लोगों को स्वतंत्र होकर वोट देने का मौका मिला और विपक्षियों को दबाने के तृणमूल के प्रयास नाकाम रहे तो वहां भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पिछले तीन दशकों में वामदलों की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि वे पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा से बाहर अपना दायरा फैलाने में नाकाम रहे.
इस चुनाव में भी गठबंधन की ही सरकार बनने की प्रबल संभावना है. गठबंधन की राजनीति में वामदलों को आप किस तरफ पाते हैं?
यह तो निश्चित है कि जो भी सरकार आएगी वह गठबंधन की ही होगी. वाममोर्चा हमेशा गैर-कांग्रेसी और गैर-भाजपाई विकल्प के साथ खड़ा रहा है. लेकिन इसका वैकल्पिक नीतियों पर आधारित होना जरूरी है. लेकिन ऐसे विकल्प मौजूद ही नहीं हैं, इसलिए वाममोर्चा कुछ गैर-कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष ताकतों का सहयोग कर रहा है. चुनाव के बाद हमारी कोशिश होगी कि ऐसी सभी पार्टियों को एक साथ लाया जाए.
क्या यह संभव है कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए वामदल कांग्रेस का समर्थन करंे?
यह साफ है कि कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह हार रही है. ऐसी स्थिति में यह कांग्रेस को तय करना है कि वह भाजपा और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी वैकल्पिक गठबंधन को समर्थन दे.
क्या वामपंथी पार्टियों में एका संभव है? ऐसा लगता है कि इस एकीकरण की राह में छोटी-मोटी असहमतियां बाधा बन जाती हैं?
इस चुनाव में वामदल पहले से ज्यादा एकजुट होकर काम कर रहे हैं. कांग्रेस और भाजपा से लड़ाई हमारी साझी नीति का हिस्सा है. हमारे बीच ऐसा कोई बड़ा मतभेद नहीं है. वामदलों के बीच व्यापक एकता असम्भव बात नहीं है. ट्रेड यूनियनों से लेकर तमाम श्रमिक संगठनों के बीच एकता तो है ही.
इस बात के लिए वामदलों की आलोचना हो रही है कि उसकी असफलता ने आम आदमी आदमी पार्टी के लिए जगह खाली की है. वामदलों के मुकाबले आप ने जनता से सफलता पूर्वक संबंध स्थापित किया है. क्या आपको भी यह लगता है?
यह सिर्फ दिल्ली केंद्रित नजरिया है. यह सच है कि आप ने दिल्ली में व्यापक जनसमर्थन जुटाया है. लेकिन वामदल यहां पर हमेशा से ही कमजोर रहे हैं. पूरे देश की यदि बात करें तो इस चुनाव में आप का बहुत ही सीमित असर होगा. जहां वामदल मजबूत हंै वहां आप का कोई असर नहीं होगा. अस्तित्व में आने के एक साल बाद भी आप अपनी विचारधारा और नीतियों को स्पष्ट करने से बच रही है. फिलहाल तो वह सबको एक साथ खुश करने की कोशिश में लगी हुई है.
अपने हालिया घोषणापत्र में माकपा ने समलैंगिकों के आंदोलन का समर्थन किया है. लेकिन वाममोर्चा इस तरह के संघर्षों या महिला अधिकार आंदोलनों में अगुवा के रूप में नहीं दिखा है? क्या आपकी कामकाजी वर्ग की परिभाषा सीमित है?
हां, हमने स्वैछिक समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाने की मांग की है. महिला आंदोलनों और उनके संघर्षों को समर्थन देने में वाममोर्चा हमेशा आगे रहा है. पता नहीं यह आप कैसे कह रहे हैं. हमने हमेशा से नारीवादी आंदोलनों का साथ दिया है. असंगठित और घरेलू महिला श्रमिकों को बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र की ओर लाया जा रहा है. वाममोर्चे की कामकाजी वर्ग की परिभाषा कहीं ज्यादा विस्तृत है.
आज के मीडिया को आप कैसे देखते हैं?
मीडिया ही इस देश में पूंजीवादी विकास को दर्शाता है. एक समय था जब बड़े-बड़े मीडिया समूह हमारे पास आते थे और कहते थे कि ‘आप एफडीआई के खिलाफ लड़िए.’ जैसे ही एनडीए सरकार ने 26 प्रतिशत निवेश की अनुमति दी यहां दस्तखत करने वालों की लाइन लग गई. आज बड़ी पूंजी, मीडिया और बड़े विदेशी मीडिया घरानों ने आपस में हाथ मिला लिए हैं. हमने बहुत सी मांग रखी है कि मीडिया में क्रॉस-ओनरशिप (एक ही व्यक्ति या कंपनी का एक ही तरह के कई उपक्रमों में मालिकाना हक) नहीं होना चाहिए. इसके चलते हम पर कई मीडिया घराने हमलावर हैं. हमें लगता है कि मीडिया पर बाहरी नियंत्रण का समय आ गया है. बाहरी नियंत्रण का मतलब सरकारी नियंत्रण से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया का आत्मनियंत्रण असफल रहा है. ब्रिटेन में लेवेसन जांच के बाद इस मुद्दे पर बड़ी बहस चल रही है. सीपीएम या मार्क्सवादी नजरिये को छोड़िए, यह मुद्दा तो उदारवादियों को उठाना चाहिए.
नरेंद्र मोदी के उदय और हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई पर आपकी क्या राय है?
इस चुनाव में हिंदुत्ववादी संगठन जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी और भाजपा के माध्यम से हिंदुत्व का एजेंडा फिर से खड़ा कर दिया जाए. मीडिया यह बात समझने में पूरी तरह चूक गया है. मोदी के बनारस से चुनाव लड़ने का और दूसरा कोई अर्थ ही नहीं है. राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान विश्व हिन्दू परिषद वाले नारा लगाते थे, ‘अब की बारी अयोध्या, उसके बाद काशी और मथुरा.’ अब उन्होंने काशी चुना है. उनकी रैलियों की शुरुआत ‘हर-हर मोदी’ के नारों से हुई. यह उस शहर में हो रहा है जहां राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे. बनारस में इस ध्रुवीकरण के बाद भाजपा ने 2004 को छोड़ कर वहां का हर चुनाव जीता. गुजरात के विकास का मॉडल सिर्फ छलावा है. उनका असली एजेंडा तो हिंदुत्व है.
तो क्या वामपंथी पार्टियां अपने में परिवर्तन लाकर फिर से उठ खड़ी हो पाएंगी?
भारत उन कुछेक देशों में शामिल है जहां पर वामदलों का व्यापक जनाधार है. इसके अलावा वाम विचारधारा का यहां लोगों के ऊपर काफी असर भी है. मुझे उम्मीद है कि यह असर और भी बढ़ेगा. लेकिन मुझे इस परिवर्तन शब्द को लेकर आशंका है. इटली में वामदलों ने खुद में इतनी बार परिवर्तन कर दिए हैं कि आज उनमें और गैर-वामदलों में कोई फर्क ही नहीं दिखता.
महासमुंद का महासमर

छत्तीसगढ़ का महासमुंद लोकसभा क्षेत्र सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसके कई कारण हैं. पहला तो यह कि यहां से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी चुनाव लड़ रहे हैं. जोगी अपने राजनीतिक पैतरों के जाने जाते हैं. वहीं दूसरा और दिलचस्प कारण यह कि यहां से भाजपा प्रत्याशी चंदूलाल साहू के सामने उनके ही दस हमनाम यानि दस चंदूलाल साहू चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं. ओडिशा की सीमा तक फैले इस लोकसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या उड़िया मतदाताओं की भी है. उन्हें रिझाने के लिए उम्मीदवार दिन रात पसीना बहा रहे हैं. शिशुपाल पर्वत तक फैले इस लोकसभा क्षेत्र में जब हम पहुंचे समझ आया कि भले ही राष्ट्रीय स्तर पर यह मुकाबला सुर्खियों में न हो लेकिन यह अपने आप में काफी रोचक बन चुका है. राजधानी रायपुर से सरायपाली (महासमुंद लोकसभा का एक हिस्सा) जाते वक्त केवल अजीत जोगी के पक्ष में स्लोगन लिखे दिखाई पड़ते हैं, कहीं भी भाजपा प्रत्याशी या अन्य स्थानीय दल के नारे नजर नहीं आते.
42 डिग्री तापमान में खस्ताहाल और जर्जर राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर चलते हुए जब आप छत्तीसगढ़ से ओडिशा की तरफ जा रहे होते हैं तो इस बात का अंदाजा बिलकुल भी नहीं लगता सकते कि यह वो इलाका है, जहां से जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजे गए नेताओं का कद राष्ट्रीय स्तर का रहा है. इसी महासमुंद लोकसभा सीट से जीतकर छह बार विद्याचरण शुक्ल लोकसभा पहुंचे थे. 1970 से 1990 यानि तीन दशक तक यहां पर वीसी शुक्ल का एकछत्र साम्राज्य रहा. शुक्ल ने इंदिरा गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाला. 1972 में महासमुंद सीट से विधायक चुनकर आए पुरुषोत्तम लाल कौशिक आगे चलकर केंद्रीय मंत्री बने. रायपुर लोकसभा सीट से जनता पार्टी की टिकट पर जीतकर वे केंद्र सरकार में 1977 से 1980 तक कैबिनेट मंत्री रहे. 2004 में खुद अजीत जोगी यहां से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे. लेकिन महासमुंद जैसा था, आज भी वैसा ही है. सड़क के दोनों तरफ लगभग काटे जा चुके जंगल, “बारनवापारा” में आ रहे टाइगर प्रोजेक्ट के चलते विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए आवास और लगभग सूख चुकी जोंक व महानदी के किनारे बिकते हरे-हरे तरबूजों के अलावा रास्ते भर आपको कुछ विशेष दिखाई नहीं देगा. यहां के उड़ीसा से सटे बलौदा जैसे गांव जहां नक्सल समस्या से ग्रस्त हैं, वहीं भंवरपुर, अर्जुंदा, सांकरा, जोंक, तोरेसिंहा जैसे गांव आज भी विकास को तरस रहे हैं.
हमारे सफर का पहला पड़ाव छत्तीसगढ़ का सबसे आखिरी गांव बलौदा था, जिससे दस किलोमीटर की दूरी से ओडिशा की सीमा लग जाती है. लेकिन बलौदा पहुंचने के पहले रास्ते में कई गांव पड़ते हैं, जहां आम चुनाव की आहट सुनाई नहीं पड़ती. भाजपा प्रत्याशी चंदूलाल साहू के स्लोगन भी शायद इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि वे 2009 में भी यहां से जीत हासिल कर चुके हैं और उनकी चुनावी रणनीति बगैर किसी शोर शराबे के मतदाताओं को रिझाने की है. वैसे भी महासमुंद सीट पर साहू मतदाता भी बड़ी संख्या में है. जिनके मत 2009 में भाजपा के पक्ष में ही पड़े थे.
महासमुंद लोकसभा चुनाव में एक बात और सबसे ज्यादा आकर्षित करती है..वो है अजीत जोगी की जीवटता. जोगी का चुनाव प्रचार व्हील चेयर के सहारे है. इसी खस्ताहाल सड़क के रास्ते वे एक गांव से दूसरे गांव पहुंचकर मतदाताओं से बात कर रहे हैं. चार लोग उन्हें व्हील चेयर समेत गाड़ी से उतारते हैं और मंच तक पहुंचाते हैं. मंच पर मौजूद कार्यक्रम संचालक मतदाताओं को ये बताना नहीं भूलता कि जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री तो थे ही, साथ ही रायपुर कलेक्टर भी रह चुके हैं. जब जोगी कलेक्टर थे, तब रायपुर महासमुंद तक फैला हुआ था. जोगी लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर मुझे चुनकर लोकसभा में भेजो. अपनी चिरपरिचित हास्य से परिपूर्ण शैली में जोगी कहते हैं कि भाजपा ने नारा दिया है हर-हर मोदी. मैं नया नारा दे रहा हूं डर-डर मोदी-थर-थर मोदी.
क्यों छोड़े कोई आतंकवाद?
श्रीनगर का नवपुरा इलाका. मार्च, 2012 का एक दिन. दोपहर के तीन बज रहे थे. 70 वर्षीय वली मोहम्मद अपनी लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाली दुकान में काम करने के बाद खाना-खाने घर आए थे. अभी खाना परोसा ही जा रहा था कि दरवाजे पर किसी के ठकठकाने की आवाज आई. वली दरवाजा खोलने के लिए बाहर आए. दरवाजा खोला तो सामने 35-36 साल का एक नौजवान, एक महिला और तीन बच्चों के साथ, पीठ पर एक बड़ा-सा बैग लादे खड़ा था. महिला ने गोद में एक बच्ची को उठा रखा था. उनके दरवाजा खोलते ही सामने खड़े व्यक्ति ने झटके से बैग नीचे फेंका. महिला और बच्चों को पीछे छोड़कर वह उनसे लिपटते हुए फफक-फफककर रो पड़ा. वली हक्का-बक्का रह गए. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है? रोने की आवाज सुनकर उनकी बड़ी बहू के साथ ही आस-पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हो गए. रोते-रोते ही उस युवक ने कश्मीरी में कुछ कहा. जिसका मतलब था, ‘मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं सबकुछ छोड़कर अब आपके पास आ गया हूं.’ वली ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा. जवाब मिला, ‘जहांगीर.’ वली को लगा उन्होंने कुछ गलत सुना है. उन्होंने दोबारा पूछा. उसने फिर अपना नाम दोहराया. सुनते ही वली उसे गले लगाकर जोर-जोर से रोने लगे. रोते हुए ही आसपास जमा हो चुके लोगों की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, ‘मेरा जहांगीर आ गया. मेरा बेटा. सब कहते थे तू कभी नहीं आएगा लेकिन मैं जानता था तू एक दिन जरूर आएगा. अब मैं सुकून से मर सकूंगा.’
आसपास के लोगों ने वली मोहम्मद को संभाला. उन्हें सहारा देते हुए घर के अंदर ले गए. थोड़ा सामान्य होने के बाद वली ने साथ आई महिला और बच्चों के बारे में पूछा. जहांगीर ने बताया, ‘ यह आपकी बहू और पोते-पोतियां हैं.’ वली ने बच्चों को गले से लगा लिया. आंखों से आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे.
बीते कुछ महीनों में श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे इलाकों में ठीक इसी तरह के कई वाकये देखने और सुनने को मिले. हर बार पिता व बेटे के नाम बदल गए पर उनकी अनपेक्षित मुलाकातों में भावनात्मक तीव्रता का उफान एक जैसा ही रहा. ऐसा जैसे अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है. तो आखिर ऐसा क्या खास था इन मुलाकातों में? ये लोग कौन थे? आखिर क्यों इनकी वापसी की उम्मीद किसी को नहीं थी? और बाद में क्या हुआ? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हम एक बार फिर जहांगीर से बात शुरू करते हैं.
सन् 1990. मार्च की 20 तारीख. वली मोहम्मद के तीन बच्चों में से सबसे छोटा बेटा जहांगीर तब तकरीबन 14 साल का रहा होगा. उस दिन जहांगीर के दोस्त उस्मान के एक रिश्तेदार के घर शादी थी. उस्मान जहांगीर को लेकर शादी में शामिल होने गया था. शादी में उस्मान को दूल्हे के लिए माला लाने भेजा जाता है. वे दोनों स्कूटर से बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं. रास्ते में उस्मान जहांगीर को माला लेने से पहले एक और जगह चलने के लिए कहता है. यहां कुछ लोग उससे मिलना चाहते हैं. जहांगीर तैयार हो जाता है. श्रीनगर के उत्तरी इलाके में बने इस घर में उसकी मुलाकात यहां पहले से इकट्ठा करीब दर्जन भर लोगों से होती है. इस घटना के दो दिन बात सुबह जब वली सोकर उठते हैं तो उन्हें घर में कहीं जहांगीर दिखाई नहीं देता. उस दिन को याद करते हुए वे बताते हैं, ‘ मैंने सोचा कि वह कहीं बाहर दोस्तों के साथ घूमने चला गया होगा. शाम तक आ जाएगा. खैर शाम से रात और रात से सुबह हो गई लेकिन जहांगीर का कहीं कोई अता-पता नहीं चला.’ थक-हारकर उन्होंने पुलिस में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी. दिन, महीनों में तब्दील होते गए लेकिन जहांगीर की कोई खबर नहीं मिली.
करीब आठ महीने बाद वली के पास एक चिट्ठी आती है. इसकी इबारत पढ़कर उनके होश उड़ जाते हैं. चिट्ठी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद से आई थी. यह जहांगीर की थी. उसने लिखा था कि वह मुजफ्फराबाद से करीब सौ किलोमीटर दूर हिजबुल मुजाहिद्दीन (एचएम) के एक ट्रेनिंग कैंप में है. यहां उसके जैसे ढेर सारे लड़के हैं. उसका दोस्त उस्मान भी यहां है. उसने रफीक भाई की शादी के दिन कुछ लोगों से उसे मिलवाया था. उन्हीं के साथ वह यहां आया है. यहां उसे बंदूक चलाना और जेहाद करना सिखाया जा रहा है. वली बताते हैं, ‘चिट्ठी में लिखा था कि उसे अपने कश्मीर को भारत से आजाद कराना है. अब और गुलामी नहीं सहनी. यह काम सिर्फ हथियार से ही हो सकता है.’
जहांगीर के घर छोड़ने के ठीक बीस साल बाद एक और घटना हुई जहां उन्हें फिर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी. 2010 में जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक नीति बनाई थी. इसका मकसद था पूर्व आतंकवादियों का पुनर्वास करना. नीति में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के वे लोग जो नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार करके आतंकवादी प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गए हैं यदि अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो और वे आतंकी गतिविधियां छोड़कर वापस अपने घर आना चाहते हैं तो सरकार उन्हें आने की इजाजत देगी. इसके साथ ही उनका पुनर्वास भी किया जाएगा. इसके तहत यह नियम बनाया गया कि पूर्व आतंकवादी जो पाकिस्तान से वापस आना चाहते हैं उनके परिवार वालों को संबंधित जिले के एसपी के सामने उसके समर्पण का आवेदन देना होगा. उस आवेदन का खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां विश्लेषण करेंगी. उनसे हरी झंडी मिलने के बाद उस व्यक्ति की घर वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा. सरकार की इसी योजना के तहत 22 साल बाद जहांगीर अपने घर वापस आए हैं.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 855 लोग जिनमें आतंकवादी और उनके परिवार भी शामिल हैं, इस दौरान पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आ चुके हैं. इनमें 277 पुरुष, 140 औरतें और 438 बच्चे शामिल हैं. हालांकि सूत्रों की मानें तो आने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से काफी ज्यादा है. इनके मुताबिक पिछले कुछ सालों में कश्मीर में लगभग 1,500 से ज्यादा पूर्व आतंकवादी पाकिस्तान या पीओके से वापस अपने घर जम्मू कश्मीर आए हैं. लोगों के वहां से आने की शुरुआत योजना लागू होने से बहुत पहले हो गई थी. राज्य सरकार के मुताबिक पाकिस्तान में अभी-भी कश्मीरी मूल के तकरीबन तीन हजार पूर्व आतंकी मौजूद हैं. उनमें से लगभग एक तिहाई राज्य की पुनर्वास नीति के तहत घाटी में वापसी करना चाहते हैं.
जम्मू कश्मीर के लिए यह बिल्कुल नई परिघटना है. ऐसी जो राज्य के लिए बेहद आशावादी तस्वीर बनाती है. लेकिन तस्वीर का एक दूसरा और भयावह पहलू भी है. पूर्व आतंकवादी पुनर्वास की जिस आखिरी उम्मीद पर वापस आए हैं वह इस समय राज्य में उन्हें दूर-दूर तक पूरी होती दिखाई नहीं देती. इससे बड़ी विडंबना यह है कि आज की हालत में ज्यादातर पूर्व आतंकवादी अपने परिवार और राज्य में भी सबसे अवांछित व्यक्तियों में शामिल हो गए हैं. इसका नतीजा है कि वे अपने घर से दूर जिस त्रासदी से गुजर रहे थे, आज फिर उसी में आकर फंस गए हैं. आखिर इन लोगों की वापसी के साथ ये हालात क्यों बने? ये लोग किन-किन त्रासदियों के बीच जी रहे हैं? और इनका राज्य में भविष्य क्या है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर किन परिस्थितियों में जहांगीर और उनके जैसे हजारों लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी प्रशिक्षण लेने गए थे और वहां उनका मोहभंग कैसे हुआ.
युवकों के आतंकवादी बनने का सफर
26 साल पहले सन् 1987 में राज्य विधानसभा के चुनावों में कथित धांधली होने की बात को लेकर पूरे जम्मू-कश्मीर में एक अभूतपूर्व गुस्से की लहर थी. पूरे सूबे में युवा सड़क पर उतर आए. राज्य की एक बडी़ आबादी का मानना था कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट के प्रत्याशियों को फर्जीवाड़ा करके चुनाव हरवाया है.
1990 में सरहद पार गए और जून, 2012 में वापस आए पूर्व आतंकी एहसान उल हक कहते हैं, ’87 के चुनाव में धांधली ने सारा माहौल खराब कर दिया. युवाओं को लगा कि अब हथियार उठाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है.’
हिजबुल मुजाहिद्दीन (एचएम) के संस्थापक सदस्य एवं श्रीनगर और बड़गाम जिले के कमांडर रहे हनीफ हैदरी (55 वर्ष) उस समय एक लोहे के कारखाने में वेल्डिंग का काम करते थे. वे बताते हैं, ‘मैंने उस चुनाव में मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट का जमकर प्रचार किया. यह उन इस्लामिक पृथकतावादी दलों का गठबंधन था जो अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस को उखाड़ फेंकना चाहते थे. मैं उस चुनाव में सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह का चुनाव प्रभारी था. यूसुफ शाह की जीत पूरी तरह पक्की थी लेकिन नतीजे आने पर उसे हारा हुआ बताया गया. यह नतीजा उस चुनाव में हुई भयानक धांधली का सबसे बडा उदाहरण था.’ यही यूसुफ शाह आगे चलकर एक बड़ा आंतकवादी सैयद सलाउद्दीन बना. उस समय चुनाव के बाद सलाउद्दीन को उसके कई साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया. हैदरी को भी पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया था.
हैदरी के मुताबिक, ‘ चुनाव में हुई धांधली ने स्थापित कर दिया कि भारत सरकार खुद चुनावों में विश्वास नहीं करती. उससे न्याय मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं. हमें समझ में आ गया कि कश्मीर पर कब्जा करके बैठी भारत सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है. यह काम शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो सकता था क्योंकि इसका हश्र हम देख चुके थे. उसके बाद पूरे कश्मीर में यह नारा गूंजने लगा – हमें इलेक्शन और सलेक्शन नहीं चाहिए. हमें आजादी चाहिए. आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं.
हथियारों के दम पर भारत सरकार को कश्मीर से खदेड़ने और कश्मीर को आजाद कराने के उद्देश्य से युवा सरहद पार पीओके और पाकिस्तान में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित आतंक के ट्रेनिंग कैंपों में जाने लगे. 1988-89 तक आते-आते कश्मीर की आजादी को लेकर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ ) से जुड़े चरमपंथी पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग करके और वहां से हथियारों से लैस होकर वापस कश्मीर आ चुके थे. 30 जुलाई, 1988 को श्रीनगर के टेलीग्राफ ऑफिस को बम से उड़ाकर जेकेएलएफ के चरमपंथियों ने कश्मीर में आतंकवाद का दौर शुरू होने की औपचारिक घोषणा कर दी थी.
पू्र्व आंतकी सैफुल्ला फारुख उस दौर को याद करते हैं, ‘तब पूरे कश्मीर में दो नारे हर एक की जुबां पर छाए हुए थे. पहला यह कि हम क्या चाहते आजादी और दूसरा, पाकिस्तान जाएंगे, क्लाशनिकोव लाएंगे.’
जहांगीर श्रीनगर के अपने घर से पाकिस्तान के आतंकी प्रशिक्षण शिविर तक पहुंचने का अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, ‘ मैंने किसी को अपने घर में नहीं बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं. जाने वाली रात हम कुल 65 के करीब लोग थे. श्रीनगर से हम 20 लोग थे. बाकी जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों से थे. अधिकांश लड़के गांवों से थे. हम रात को निकले. कुपवाड़ा बॉर्डर से पाकिस्तान में हमें दाखिल होना था. पहाड़ और जंगलों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे. रास्ते में कई लड़कों की हिम्मत जवाब दे गई. कुछ इतना थक गए थे कि आगे जाने की स्थिति में नहीं रहे. वे वहीं रुक गए. पांच लड़के रास्ते में पहाड़ों पर चढ़ते हुए फिसल कर नीचे गिर कर मर गए. दो लड़के रास्ते में आर्मी स्नाइपर्स की गोलियों से मारे गए.’ जहांगीर याद करते हुए बताते हैं कि कैसे रास्ते में सात लोगों की मौत के बाद उनके गाइड ने सभी लड़कों से कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कहा था. इस तरह चार दिन के बाद ये लोग पीओके स्थित दूध निहार बॉर्डर पहुंचे और वहां से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर. इसके बाद जहांगीर व उनके साथियों को मुजफ्फराबाद ले जाया गया. मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद उन्हें एक ट्रक में चढ़ने को कहा गया.
जहांगीर बताते हैं, ‘हम सबके हाथ बांधकर आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई थी. मुझे याद है उसके बाद हमें एक-एक कर ट्रक के अंदर चढ़ा दिया गया. ट्रक में शायद बैठने के लिए कुछ नहीं था. हम सब खड़े थे. ट्रक स्टार्ट हुआ और चल पड़ा. हमें पता नहीं था कि हमें कहां ले जाया जा रहा है. रास्ते में कई लड़कों ने ट्रक में उल्टियां कर दी. अंदर हमारा दम घुट रहा था. लगभग आठ घंटे के लगातार चलने के बाद ट्रक एक जगह रुका. हमें एक-एक कर उतारा गया. हाथ और आंखें खोल दी गईं.’
इन लोगों को हिजबुल मुजाहिद्दीन के ट्रेनिंग कैंप में ले जाया गया. यह दीनी कैंप था. उस समय को याद करते हुए जहांगीर कहते हैं, ‘जब हमारी आंख खुली तो सामने आर्मी के मिलेट्री कैंपों की तरह एक बड़ा कैंप दिखाई दिया. हमें नहीं पता था कि हम इस वक्त कहां हैं. वहां पर 10 हजार के करीब कश्मीरी लड़के थे.’ वे बताते हैं कि कैंप का जीवन बहुत मुश्किल था. लेकिन वे इसके लिए तैयार थे क्योंकि उनके कश्मीर की आजादी का रास्ता यहीं से होकर निकलना था.
पीओके के इस कैंप में अगले तीन महीने तक जहांगीर और उनके साथियों की ट्रेनिंग हुई. इन्हें बम बनाने और चलाने से लेकर, एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाना, और गुरिल्ला यद्ध के तौर-तरीके आदि सिखाए गए. इसके बाद 25 लड़कों के एक समूह के साथ जहांगीर को आगे की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भेज दिया.
पाकिस्तान से मोहभंग और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन
जहांगीर पाकिस्तान-अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेने गए पहली पीढ़ी के युवकों में से नहीं थे. उनके इन कैंपों में पहुंचने के दो-तीन साल पहले से जम्मू कश्मीर के युवक वहां जाकर ट्रेनिंग ले रहे थे. इस समय तक हैदरी अफगानिस्तान में छह महीने का प्रशिक्षण पूरा कर मुजफ्फराबाद में रहने लगेे थे. यह 1989 की बात थी जब उन्हें एक नए आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) बनाने के बारे में बताया गया. तब तक जेकेएलएफ आतंकवादियों का सबसे प्रभावशाली संगठन था. इसका घोषित मकसद कश्मीर की आजादी. जमात ए इस्लामी से जुड़े हिजबुल मुजाहिदीन के उदय ने इस पूरी लड़ाई को अपेक्षाकृत धर्मनिरपेक्ष हथियारबंद सशस्त्र संघर्ष के बजाय इस्लामी और पाकिस्तान समर्थित बना डाला. कुछ महीनों बाद ही हैदरी इस संगठन में कमांडर बने और श्रीनगर आ गए.
जेकेएलएफ और एचएम के बीच पनप रहे अंतर का असर ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग पा रहे लड़ाकों पर भी पड़ा. पूर्व आतंकवादी बताते हैं कि कैंपों में पाकिस्तानी ट्रेनर एक सोची-समझी रणनीति के तहत श्रीनगर और कश्मीर की अन्य जगहों से आए लड़कों के बीच अलगाव पैदा करने का काम करते थे. दरअसल उनके लिए श्रीनगर से आए लड़कों को बरगला पाना आसान नहीं था. जबकि गांव के लड़कों को वे अपनी मर्जी से ढाल लेते थे. थोड़ा बहुत सोचने-समझने वाले लड़के आजादी के नाम पर चल रही इस लड़ाई के तौर तरीकों पर गाहेबगाहे सवाल उठाते रहते थे. जहांगीर बताते हैं, ‘पीओके के आम लोग भी कहते थे कि तुम लोग यहां आकर फंस गए हो. यहां कश्मीरियों को छोड़कर सभी को फायदा है. जेहाद के नाम पर फंड आ रहा है. धंधा चल रहा है. वे हमें सिखाते थे कि शिया काफिर हैं उन्हें मारना है. दरगाह और स्कूलों को खत्म करना है. मस्जिदों में बम फोड़कर लोगों में दहशत लाना है. मैं उनसे पूछा करता था कि मस्जिद में बम फेंकना कहां का जेहाद है. हम लोग तो यहां आजादी की लड़ाई लड़ने आए हैं.’ कई पूर्व आतंकवादी इस प्रचलित धारणा को भी गलत बताते हैं कि पीओके में पाकिस्तान का समर्थन है. उनके मुताबिक मीरपुर, रावलकोट, बाग-कोटली और पूंछ आदि में पाकिस्तान का भारी विरोध है.
इन्हीं दिनों एचएम ने खुले तौर पर जेकेएलएफ पर तंज कसने शुरू कर दिए. इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों संगठन एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति में आ गए. सन् 1990 से 1993 के बीच दोनों संगठनों ने एक-दूसरे के 200 से अधिक लोगों को मार दिया. जेकेएलएफ ने उस समय आरोप लगाया था कि एचएम आईसआई के साथ मिलकर उसके लोगों को मार रहा है. हैदरी बताते हैं, ‘ एचएम का गठन बहुत सोच-समझकर किया गया था. इसका एक बेहद समर्पित और मजबूत वैचारिक आधार था. यही कारण है कि संगठन आज भी जिंदा है और लड़ रहा है. इसके पीछे हमारा उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग करके एक इस्लामिक राज्य बनाना था. हमारी रणनीति व्यापक थी. हमने सोचा था कि भारत को हराने के बाद पाकिस्तान में हमारी बड़ी भूमिका हो जाएगी. हम पाकिस्तान को पूरी तरह से एक इस्लामिक राज्य बना देंगे.’
[box]
 ‘सैयद सलाउद्दीन तो सर्कस का शेर है, वह भी अधमरा’
‘सैयद सलाउद्दीन तो सर्कस का शेर है, वह भी अधमरा’
जो भी कश्मीरी लड़के पाकिस्तान में कश्मीर की आजादी की बात करते हैं वेे लोग उन्हें बॉर्डर पर भेजकर मरवा देते हैं. वे कश्मीर की आजादी के खिलाफ हैं. जहां तक सलाउद्दीन (हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख) की बात है तो देखिए कि उसके चारों बेटे यहां जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे हैं. चीफ कमांडर के बेटों को नौकरी मिल रही है, उनके पास पासपोर्ट है लेकिन जब आम कश्मीरी पासपोर्ट मांगता हैं तो सरकार कहती है नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा दूर का रिश्तेदार पहले आतंकवादी था. यह किस तरह का न्याय है. सलाउद्दीन तो बस वहां बैठकर आईएसआई के आदेश पर बयान देने का काम करता है. वह सर्कस के शेर जैसा है. जिसकी एक टांग टूटी हुई होती है. गले में पट्टा होता है. वह पहले से ही अधमरा होता है. उसे नचाने वाला आता है और जब आकर पीछे हंटर मारता है तो वह दहाड़ना शुरु कर देता है.
हनीफ हैदरी, हिजबुल मुजाहिद्दीन के संस्थापक सदस्य
[/box]
सैफुल्लाह बताते हैं, ‘ इन संगठनों के लोगों ने आपस में एक दूसरे के इतने लड़कों को मारा है जितने सेना के हाथों भी नहीं मारे गए.’
इसके बाद एचएम के नेताओं के बीच आपसी लड़ाई शुरू हो गई. वह अलग-अलग गुट में बंटने लगा. हर दिन दो लोग मिलकर नया संगठन खड़ा कर लेते थे. एक समय के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि पता नहीं चलता था कि कौन किसको मार रहा है. हैदरी कहते हैं, ‘ यह सबकुछ बेहद दुखद था. हम कश्मीर के लिए लड़ रहे थे. मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं. क्यों संगठन लगातार कमजोर हो रहा है. इसके पीछे के कारणों को जानने मैं पाकिस्तान स्थित ट्रेनिंग कैंपों में गया. वहां की स्थिति देखकर मैं हैरान रह गया. वहां जाकर मेरा पाकिस्तान और सशस्त्र संघर्ष से मोहभंग हो गया. मुझे पता चला कि इस सब बर्बादी के पीछे आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है. वही कश्मीर में गुटबाजी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे.’
ऐसा ही एक आतंकी ट्रेनिंग बेस कैंप जो मुजफ्फराबाद के पास था, में जब हैदरी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने कैंप को आतंकवाद की फैक्ट्री में बदल दिया है. यहां हजारों की संख्या में अलग-अलग देश और नस्ल के लोग अलग-अलग पार्टियों के कैंप में ट्रेनिंग ले रहे हैं. इन लोगों के लिए विचारधारा का कोई मतलब नहीं था.
‘ मैंने 11 अलग-अलग कैंपों में 11 अलग संगठनों के लोगों को पाया. जब मैं इन संगठनों के कमांडरों से मिला और उनसे पूछा कि इतने संगठन क्यों बने हुए हैं. सब एक साथ क्यों नहीं हैं. तो उन्होंने मुझसे कहा कि हर संगठन की अपनी अलग धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा है.’ हैदरी बताते हैं, ‘ इस तरह से वहाबियों के पास तहरीक उल मुजाहिद्दीन और लश्कर ए तैयबा था, शियाओं का हिजबुल मोहमिनीन तो सुन्नियों का हिजबुल मुजाहिद्दीन और हिज्ब ए इस्लामी था. इस तरह से तमाम ऐसे संगठन बने हुए थे. उस समय मैंने तय कर लिया कि मेरे जेहाद के दिन पूरे हो चुके हैं. मेरा आजादी की इस लड़ाई से मोहभंग हो चुका था. मैंने सब छोड़ दिया. ‘
हैदरी ही नहीं पाकिस्तान आए तमाम कश्मीरी नौजवानों का धीरे-धीरे पाकिस्तान की असलियत से सामना होने लगा. उन्हें समझ आने लगा कि उनको धोखा दिया जा रहा है. जिस देश को वे अपनी आजादी की लड़ाई में साथी मानकर चल रहे थे उसका इस समर्थन के पीछे अपना एजेंडा है. इनमें से ज्यादातर लड़के खुद को छला हुआ महसूस करने लगे. जल्दी ही इसकी प्रतिक्रिया भी यहां दिखाई देने लगी. हैदरी जानकारी देते हैं, ‘ मैंने वहां कश्मीरी लड़कों के लिए जम्मू और कश्मीर रिफ्यूजी वेल्फेयर एसोसिएशन शुरू की. दिन में मैं एक दुकान पर वेल्डिंग का काम करता और रात में पूर्व आंतकियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग करता. उनकी समस्याएं सुनता और यहां से कैसे निकल सकते हैं इस पर हम चर्चा करते.’ इन बैठकों में ही यह तय हुआ कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. फिर धीरे-धीरे पाकिस्तान के खिलाफ धरना-प्रदर्शन के आयोजन होने लगे. ये प्रदर्शन पाकिस्तान की कश्मीर में भूमिका और वहां रह रहे जम्मू कश्मीर के युवकों के साथ किए जा रहे बुरे सलूक के खिलाफ था.
पाकिस्तान ट्रेनिंग करने गए लोगों में से कई ऐसे थे जिन्होंने ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हथियार डाल दिए. उन्होंने कैंप, आतंक और आजादी की लड़ाई दोनों से मुंह मोड़ लिया. कई ऐसे थे जिनका बढ़ते समय के साथ आजादी की लड़ाई की जमीनी हकीकत से सामना होने पर मोहभंग हो गया. इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इस कथित आजादी की लड़ाई का संचालन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ में था. हाल ही में पीओके से वापस लौटे मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, ‘ मुझे वहां जाने के दो साल के भीतर ही समझ आ गया कि आईएसआई व पाकिस्तान का क्या एजेंडा है. मुझे पता चल गया कि इन लोगों को कश्मीर की आजादी से कोई मतलब नहीं है. भारत के खिलाफ लड़ाई में कश्मीर इनके लिए सिर्फ मोहरा भर है.’
वहीं कुछ समय के बाद ही वहां दूसरे आतंकी संगठनों के बीच भी आपसी लड़ाई शुरू हो गई. इन हालात में कुछ सालों के भीतर ही कई कश्मीरियों ने इस कथित आजादी की लड़ाई से किनारा कर लिया. 1995 तक पाकिस्तान और पीओके में ऐसे कश्मीरियों की संख्या काफी बढ़ गई जो लड़ाई छोड़कर बतौर शरणार्थी यहां रहने लगे थे. वे तभी से वापस अपने घर आना चाहते थे. लेकिन यह सोचकर उस दिशा में नहीं बढ़ पाते थे कि अगर वे ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आईएसआई और आतंकी संगठनों के लोग उन्हें मार डालेंगे और किसी तरह जान बचाकर भारत पहुंच गए तो भारत सरकार उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी.
इन लोगों द्वारा पाकिस्तान विरोध की शुरुआत होने के बाद उसका सबसे ज्यादा असर भारतीय हिस्से वाले कश्मीर में हुआ. यहां के युवाओं के सामने पाकिस्तान की असलियत खुल चुकी थी. लड़कों ने पीओके और पाकिस्तान जाना धीरे-धीरे बंद कर दिया. कश्मीर से जेहाद की ट्रेनिंग के लिए लड़के आने बंद हो गए. अब आलम यह हो गया कि 10-15 आतंकियों के समूह में कुल इक्का-दुक्का ही कश्मीरी होते थे. कश्मीरियों के मोहभंग को देखते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में पाकिस्तानी लड़कों को भेजना शुरू किया. लश्करे तैयबा जैसा संगठन जिसके पूरे कैडर में सभी पाकिस्तानी हैं, उसको आईएसआई ने कश्मीर में सक्रिय करना शुरू किया.

इस बीच अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले ने पाकिस्तान की हालत और खराब दी. अब उसे अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी निपटना था. अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का अलग दबाव था सो पाकिस्तान कश्मीर से दूर होता चला गया. हैदरी कहते हैं, ‘ हालत इतनी खराब हो गई कि पाकिस्तान में जेहाद के लिए चलने वाले कैंपों में राशन तक खत्म हो गया. जो अमीर पंजाबी कश्मीर में जेहाद के नाम पर पैसा और राशन भेजते थे उन्होंने अब तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था.’
पीओके में बने इन हालात का कश्मीर घाटी पर भी असर पड़ा. जानकार बताते हैं कि हिजबुल के समर्थन में आ रही गिरावट के कारण ही आज यह आलम है कि यहां एचएम पर लश्कर ए तैयबा भारी पड़ रहा है. हिजबुल को यहां कैडर नहीं मिल रहा है. सरकार इसे स्थानीय लोगों के आतंकवाद से मोहभंग होने के रूप में देखती है. आंकड़े बताते हैं कि आज घाटी में आतंक की घटनाएं पिछले 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर हैं. दो साल पहले के आंकड़े बताते हैं कि साल 2011 की तुलना में 2012 में आतंकी हिंसा में जहां 26 फीसदी की कमी आई वहीं हताहत होने वालों की संख्या में 48 फीसदी की गिरावट आई है.
इन पूर्व आतंकवादियों की पूरी व्यथा समझने के लिए हम एक बार फिर जहांगीर की कहानी पर वापस चलते हैं. अफगानिस्तान पहुंचे जहांगीर को भी कुछ महीनों के भीतर ही यह पता चल गया था कि वे यहां अलग तरह से गुलाम बनाए जा रहे हैं. यहीं एक ऐसी घटना हुई जिससे जहांगीर का कैंप के जीवन से मोहभंग हो गया. इसबारे में वे बताते हैं, ‘ कश्मीर में किन-किन जगहों को निशाना बनाना है इसको लेकर दो पाकिस्तानी कमांडर हम 25 लड़कों की क्लास ले रहे थे. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की सप्लाई लाइन को काटने के लिए सबसे पहले हमें पुलों को निशाना बनाना पड़ेगा. मैंने खड़े होकर कहा कि ऐसा करना गलत होगा. इससे भारतीय सेना को कोई दिक्कत नहीं होगी. उन्हें सप्लाई पहुंचाने के लिए पुल की जरूरत नहीं है. अगर उन्हें इसकी जरूरत पड़ती भी है तो वे चंद घंटों में ही अपनी जरूरत के लिए आपातकालीन पुल तैयार कर लेंगे. ऐसे में अगर हम पुल उड़ाते हैं तो इससे कश्मीर की आम जनता को परेशानी और नुकसान उठाना पड़ेगा. अधिकारियों ने कुछ लोगों की तरफ इशारा करके मुझे बाहर निकालने को कहा. उन्होंने मुझे एक पेड़ से बांध दिया. मुझे यकीन हो गया था कि ये लोग अगले कुछ समय में मेरा गला काट देंगे. मैं बुरी तरह डर गया था. तभी मेरे कुछ कश्मीरी दोस्त मुझसे मिलने आए और कहा कि अब तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है कि तुम खुद के पागल हो जाने का नाटक करो. अगले तीन दिनों तक मैं वहीं पेड़ से बंधा हुआ पाकिस्तान का राष्ट्रीय गीत और फिल्मी गाने गाता रहा. अमेरिका को गाली देता रहा. कमांडरों को पहले गाली देता फिर उनकी तारीफ करता.’
इसके बाद कमांडरों को भरोसा हो गया कि जहांगीर सच में पागल हो गए हैं. उनकी रस्सी खोल दी गई. फिर एक रात वे वहां से भाग निकले और कई महीनों तक मुजफ्फराबाद की एक मस्जिद में रहे. यहीं उनकी मुलाकात शफीक नाम के एक लड़के से हुई जिसने मुजफ्फराबाद ट्रेनिंग कैंप में उनके साथ ही ट्रेनिंग की थी. वह जेकेएलएफ से जुड़ा था. यह जानने के बाद कि जहांगीर संगठन में फिर वापस नहीं जाना चाहता शफीक उसे अपने घर ले गया. उसका घर पीओके के दक्षिण में स्थित कोटली जिले के सरसावां गांव में था. जहांगीर बताते हैं, ‘ शफीक अपने मां बाप का इकलौता लड़का था और वह जेहाद छोड़ना नहीं चाहता था. उसने अपने घरवालों से कहा कि वह जा रहा है लेकिन जहांगीर वहीं रहेगा. अगर उसे कुछ हो जाता है तो फिर जहांगीर को ही वे अपना बेटा मान लें.’ बकौल जहांगीर, ‘मैं वहां तीन साल रहा और इसी दौरान शफीक के मारे जाने की खबर भी हम लोगों को मिली. इसके बाद उन्होंने मुझे अपना बेटा ही मान लिया.’ शफीक के परिवार वालों ने ही उनकी शादी करवा दी. जहांगीर बताते हैं, ‘ वे लोग मुझे जान से ज्यादा प्यार करते थे लेकिन मुझे अपने घरवालों की बहुत याद आती थी. मैंने अपनी पत्नी को कह दिया था कि एक दिन मैं अपने घर वापस जाऊंगा.’
इन लोगों के घर वापसी के सपने के परवान चढ़ने की शुरुआत 2004 से मानी जा सकती है. तब भारत सरकार और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच लंबी बातचीत के बाद बॉर्डर पर स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगी थी. नियंत्रण रेखा के आर-पार बसों की आवाजाही शुरू हो गई. इसके बाद से पाकिस्तान में बैठे इन लोगों की घर वापस की छटपटाहट और बढ़ गई.
पुनर्वास की नीति और पाकिस्तान से वापसी
पाकिस्तान से वापस अपने घर का सफर इन लोगों के लिए बेहद डरावना, खर्चीला और परेशान करने वाला रहा. जम्मू-कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इनकी वापसी के लिए 2010 में जो नीति बनाई उसके तहत पूर्व आतंकवादियों के भारत में वापस आने के लिए चार रास्ते चिह्नित किए गए. ये थे- वाघा बॉर्डर, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (नई दिल्ली), उरी-मुजफ्फराबाद और पूंछ-रावलकोट. लेकिन सरकारी नीति की यह शर्त शुरुआत में ही पुनर्वास के इरादों पर बड़े सवाल खड़ा कर देती है. इससे जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जितने पूर्व आतंकी पाकिस्तान से वापस जम्मू कश्मीर आए हैं उनमें से मुश्किल से कोई ही इन रास्तों से वापस आया हो. वजह यह कि पाकिस्तान इन रास्तों के जरिए इन लोगों को सीमापार नहीं करने देता. यदि ये किसी तरह छुपते-छुपाते भारतीय सीमा में दाखिल हो भी जाते हैं तो भारतीय सेना इन्हें अंदर नहीं आने देती.

पूर्व आतंकी असलम खान अपना ऐसा ही एक अनुभव साझा करते हैं, ‘मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रात के अंधेरे में छुपते-छुपाते भारतीय सीमा पर पहुंचा था. मैंने बीएसएफ के जवानों को बताया कि मैं एक पूर्व आतंकवादी हूं और सरकारी नीति के तहत वापस आया हूं. लेकिन मेरी हालत उस समय खराब हो गई जब बीएसएफ के अधिकारी ने मुझे चुपचाप वापस पाकिस्तान चले जाने को कहा.’ असलम के मुताबिक जवानों ने उनसे कहा कि यदि वे वापस नहीं गए तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाएगी. उन्हें अपने परिवार सहित वापस लौटना पड़ा. वे बाद में नेपाल के रास्ते (सरकारी नीति में यह रास्ता अवैध है) जम्मू कश्मीर वापस आ पाए.
हालांकि, इक्का-दुक्का लोग ऐसे भी हैं जो किसी तरह से बचते-बचाते हुए सीमा पार करके वापस आने में सफल रहे हैं. हालांकि उनके लिए यह यात्रा कदम-कदम पर जानलेवा जोखिम से भरी रही. इन्हीं रास्तों से वापस आए सरफराज बताते हैं, ‘ हमारे पास नेपाल बॉर्डर से आने के लिए पैसा नहीं था. इस रास्ते से पहुंचाने के लिए एजेंट हमसे पांच लाख रुपये मांग रहे थे लेकिन मेरे पास पांच हजार रुपये तक नहीं थे. बॉर्डर क्रॉस करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था. हम अपने घर आने के लिए मुजफ्फराबाद से रात में निकले. रात भर लगातार चलते रहे. उसी में बारिश हो गई और हम पूरी तरह से भीग गए थे. लेकिन हम रुके नहीं चलते रहे. रास्ते में हमें कहीं कोई पाकिस्तानी सैनिक नहीं मिला और हम पाकिस्तानी सीमा पार कर आए. जब तक हम भारतीय सीमा में दाखिल हुए तब तक उजाला हो चुका था. हालांकि कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था. रात भर चल कर हम लोग थक चुके थे तो सामने एक खेत में लगी फसल की आड़ में बैठ गए. अभी वहां हमें बैठे कुछ मिनट ही हुए थे कि कहीं कोई हूटर बजा और देखते-देखते हमें भारतीय सैनिकों ने घेर लिया. हमसे उन्होंने अगले तीन घंटे तक पूछताछ की. उसके बाद हमें पुलिस को सौंप दिया गया.’ सरफराज की पत्नी जाहिदा 15 दिन के बाद जमानत पर रिहा हो गईं. लेकिन सरफराज पर पुलिस ने जनसुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाया था. वह छह महीने बाद जेल से बाहर आ पाए.
सरफराज की कहानी चंद अपवादों में से एक हैं. बाकी असलम जैसी कहानी लगभग हर उस व्यक्ति की है जिसने सरकार द्वारा तय किए गए या बॉर्डर के रास्तों से वापस आने की कोशिश की. जितने भी लोगों ने उन रास्तों से वापस आने की कोशिश की उन्हें वापस लौटा दिया गया. लेकिन ऐसा हुआ क्यों?
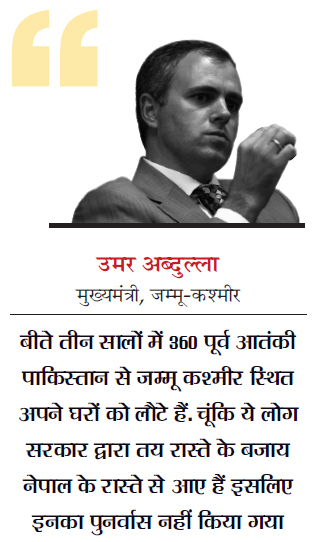 पूर्व आतंकी बशीर अहमद कहते हैं, ‘हमें भी नहीं पता. पाकिस्तान का तो समझ में आता है कि वह नहीं चाहेगा कि पूर्व आतंकवादी समर्पण करने के लिए भारत की सीमा में दाखिल हो क्योंकि इससे यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में आतंकवादी मौजूद है. उसने उन्हें पनाह दे रखी है. लेकिन भारत सरकार ने जब खुद ही हम लोगों की वापसी के लिए नीति बनाई है तो फिर वह क्यों चिह्नित रास्तों से हमें आने नहीं देती यह हमारी समझ के बाहर है.’
पूर्व आतंकी बशीर अहमद कहते हैं, ‘हमें भी नहीं पता. पाकिस्तान का तो समझ में आता है कि वह नहीं चाहेगा कि पूर्व आतंकवादी समर्पण करने के लिए भारत की सीमा में दाखिल हो क्योंकि इससे यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में आतंकवादी मौजूद है. उसने उन्हें पनाह दे रखी है. लेकिन भारत सरकार ने जब खुद ही हम लोगों की वापसी के लिए नीति बनाई है तो फिर वह क्यों चिह्नित रास्तों से हमें आने नहीं देती यह हमारी समझ के बाहर है.’
इस पूरे मामले में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग की भूमिका भी अजीबोगरीब है. जैसे ही लोगों को पता चला कि सरकार ने वापस जाने के लिए चार रास्ते चिह्नित किए हैं. इन लोगों ने पाकिस्तान स्थिति भारतीय उच्चायोग से संपर्क करना शुरू किया. इन्हें सूचना मिली थी कि वीजा, बाकी जरूरी दस्तावेज और भारत लौटने की अनुमति उन्हें वहीं से मिलेगी.
खैर, जहांगीर जैसे तमाम लोग उस समय हैरान रह गए जब इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने उनकी किसी तरह से मदद करने से इनकार कर दिया. पूर्व आतंकी एहसान कहते हैं, ‘उच्चायोग के अधिकारियों ने हमसे कहा कि हमें सरकार द्वारा चिह्नित चार रास्तों से घर जाने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए. यह संभव नहीं है. उच्चायोग के लोगों ने वापस जाने का एक चौंकाने वाला तरीका बताया. उन्होंने कहा आप लोग ऐसा करो नेपाल के रास्ते चले जाओ. जब आप अपने घर पहुंच जाएंगे तो हम कागजी कार्रवाई वहीं पूरी करा लेंगे. आपके पुनर्वास का काम उसके बाद शुरू हो जाएगा.’
भारतीय उच्चायोग द्वारा मदद से इनकार करने और नेपाल के रास्ते भारत जाने की सलाह देने के बाद ये लोग इस बात पर विचार करने लगे कि आखिर कैसे नेपाल के रास्ते से भारत जा सकते हैं.
जहांगीर बताते हैं कि उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उन्हें नेपाल के रास्ते भारत पहुंचाने के लिए तैयार हो गए. लेकिन इसके लिए घर के हर सदस्य के हिसाब से एक लाख रुपये का खर्च था. पांच लोगों के लिए उन्हें पांच लाख रुपये देने पड़े. नेपाल के रास्ते से अपने घर कश्मीर आए पूर्व आतंकी हमीद पठान बताते हैं, ‘ वहां एजेंट नेपाल जाने के लिए वीजा के लिए एप्लाई करवाते हैं. हमें यह कहना होता है कि हम अपने रिश्तेदार की शादी के लिए जा रहे हैं या इलाज कराने या घूमने. इसके बाद नेपाल जाने के टिकट के साथ ही वापस पाकिस्तान आने का भी टिकट कटाते हैं ताकि उन्हें लगे कि सामने वाला जा रहा है तो वापस भी आएगा. जहांगीर जानकारी देते हैं, ‘ ये सारे काम कराने वाले एजेंट कराची में हैं. कराची एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद वे नेपाल में अपने एजेंट का नंबर और संपर्क आदि दे देते हैं.’ काठमांडू पहुंचने के बाद वहां एक दूसरा एजेंट मिलता है जो इन लोगों को नेपाल सीमा पार करवाकर गोरखपुर लाता है. इन एजेंटों को पहले से यह निर्देश होता है कि पाकिस्तान से आ रहे इन लोगों के पासपोर्ट वह अपने कब्जे में लेकर तुरंत नष्ट कर दे जिससे यह सबूत मिट जाए कि वे पाकिस्तान से आ रहे हैं. इसके बाद ये लोग ट्रेन से जम्मू पहुंचते हैं. पूर्व आतंकवादी वापसी और पुनर्वास की नीति के तहत आए हैं इसलिए जम्मू आते ही सीधे अपने क्षेत्र के थाने में जाकर रिपोर्ट करते हैं.
एक नई त्रासदी की शुरुआत
अभी तक वापस आए पूर्व आतंकियों के मन में इस बात की जरा भी शंका नहीं थी कि कश्मीर में एक और त्रासदी उनका इंतजार कर रही है. यूसुफ अपनी आपबीती सुनाते कि हुए कहते हैं, ‘वापस आने के बाद पुलिस ने मुझ पर पाकिस्तान से ग्रेनेड लाने का झूठा केस दर्ज कर दिया. हमें कई दिनों तक बड़गाम थाने में बंद रहना पड़ा. आप ही बताइए कोई पत्नी और चार बच्चों के साथ ग्रेनेड लेकर आएगा? पत्नी को कहा कि वह दूसरे मुल्क की लड़की है. बॉर्डर क्रॉस करके भारत आई है. जबकि हम दोनों नेपाल वाले रास्ते से बच्चों के साथ आए थे. मुझ से कहा गया मैं नेपाल से अवैध तरीके से भारत आया हूं. पत्नी का केस पिछले पांच सालों से चल रहा है. मैं कहता हूं गलती मैंने की मुझे सजा दो. उस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो.’

फोटोः बृजेश सिंह
पुनर्वास योजना के तहत आए लगभग सभी पूर्व आतंकियों और उनके परिवार वालों के साथ कुछ इसी तरह का सलूक हुआ है. जहांगीर कहते हैं, ‘ मैं भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 11 दिनों तक श्रीनगर के एक पुलिस थाने में बंद रहा. उन्होंने हमारे पास मौजूद आखिरी 850 डॉलर भी अपने पास रख लिए. हमने उनसे कहा भी कि हम तो बीवी बच्चों के साथ आए हैं. हमारे पास कोई बंदूक भी नहीं फिर हमसे ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है.’ ये पूर्व आतंकवादी हर लिहाज से राज्य में सबसे आसान शिकार हैं. ऐसे लोगों को कानूनी मदद मुहैया करा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ताज हुसैन कहते हैं, ‘पुनर्वास तो दूर की बात है. सरकार इन्हें यहां शांति से रहने भी नहीं दे रही. अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने, पासपोर्ट कानून का उल्लंघन करने से लेकर इग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस (बिना वैध दस्तावेजों के आवाजाही), दुश्मन एजेंट अध्यादेश, पीएसए जैसे तमाम कानूनों के तहत इन पर केस दर्ज कर दिए जाते हैं.
ऐसा ही एक मामला किश्तवाड़ के मुजम्मिल खान का है. वे जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिद्दीन के ऑपरेशन कमांडर थे. वे बताते हैं, ‘ पुनर्वास की नीति बनने के बाद मैंने एके 47 और दो जिंदा मैग्जींस के साथ समर्पण किया था. आर्मी ने मुझे छोड़ दिया लेकिन पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया. मैं तीन साल जेल में रहा. वहां से बाहर निकला तो आज तक पुनर्वास की बाट जोह रहा हूं. अभी घर चलाने के लिए मजदूरी करता हूं. हमारा भी पंजाब और उत्तर-पूर्व के पूर्व आतंकवादियों की तर्ज पर पुनर्वास किया जाना चाहिए.’
ऐसे भी कई मामले हैं जहां पूर्व आतंकवादियों के मुताबिक सेना और पुलिस के लोग खुद उनसे कहते हैं कि वे किसी बड़े हथियार के साथ सरेंडर करें ताकि उनका जल्दी और अच्छे से पुनर्वास हो. लेकिन यहां सरेंडर करने के बाद उन पर तमाम तरह के केस लाद दिए जाते हैं. ऐसा ही कुछ अब्दुल गनी के साथ हुआ. गनी के मुताबिक वे जब से आए हैं तब से पुलिस उन्हें कुछ हथियार और गोला बारूद के साथ ‘आत्मसमर्पण’ के लिए कह रही है. वे कहते हैं, ‘ मैं जानता हूं वे लोग अपनी पदोन्नति और मेडल के लिए यह सब कराना चाहते हैं. लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए मैं हथियार कहां ले आऊं?’
वापस आए लोगों में तमाम लोग ऐसे हैं जो बाहर पुलिस और सरकार की उपेक्षा और उत्पीड़न के साथ ही घरवालों से अलग स्तर पर जूझ रहे हैं. साल 2010 में जब मंजूर अहमद बड़गाम जिले के नरबल स्थित अपने घर पहुंचे तो कुछ दिनों तक सबकुछ ठीक रहा. आस-पड़ोस वालों से लेकर दूर तक के सारे रिश्तेदार उनसे मिलने आए. सभी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. लेकिन एक महीने में सबकुछ बदल गया. भाइयों ने अपनी व्यवस्था कहीं और कर लेने की बात कहनी शुरू कर दी. बकौल मूंजूर, ‘उन्होंने दबे छुपे शब्दों में यह कहना शुरु कर दिया कि 20 साल तक तो तुम यहां थे नहीं. तुम्हारी वजह से पुलिस और एजेंसी वाले हमें पीटते थे. अब तुम आ गए हो तो अपनी और अपने परिवार की व्यवस्था देखो.’
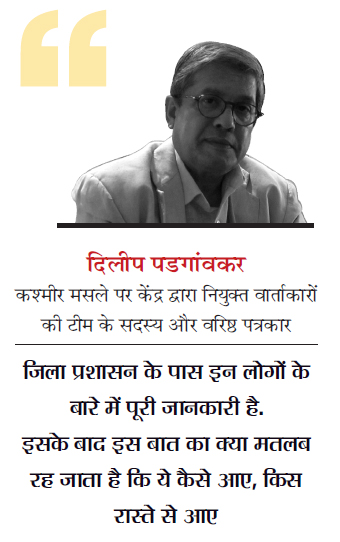 मंजूर, उनकी पत्नी और चार बच्चों को उनके भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया है. फिलहाल वे पूंछ जिले में एक किराए के मकान में रहते हैं. मंजूर के हिस्से की संपत्ति उनके भाइयों ने सालों पहले ही अपने नाम करा ली थी. पूर्व आतंकवादी सैफुल्ला बताते हैं, ‘ हमारी वापसी से सरकार खुश है या नाराज, यह तो पता नहीं लेकिन अधिकांश पूर्व आतंकवादियों के परिवार वाले, खासकर के उनके भाई वगैरह काफी नाराज हैं. दरअसल ये लोग इनके हिस्से की संपत्ति पहले ही अपने नाम करा चुके हैं. इन्हें विश्वास था कि पीओके गए लड़के कभी नहीं आएंगे. अब चूंकि इन लोगों की वापसी हो रही है तो इन्हें चिंता है कि कहीं वे संपत्ति में अपना हक ना मांगने लगे.’
मंजूर, उनकी पत्नी और चार बच्चों को उनके भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया है. फिलहाल वे पूंछ जिले में एक किराए के मकान में रहते हैं. मंजूर के हिस्से की संपत्ति उनके भाइयों ने सालों पहले ही अपने नाम करा ली थी. पूर्व आतंकवादी सैफुल्ला बताते हैं, ‘ हमारी वापसी से सरकार खुश है या नाराज, यह तो पता नहीं लेकिन अधिकांश पूर्व आतंकवादियों के परिवार वाले, खासकर के उनके भाई वगैरह काफी नाराज हैं. दरअसल ये लोग इनके हिस्से की संपत्ति पहले ही अपने नाम करा चुके हैं. इन्हें विश्वास था कि पीओके गए लड़के कभी नहीं आएंगे. अब चूंकि इन लोगों की वापसी हो रही है तो इन्हें चिंता है कि कहीं वे संपत्ति में अपना हक ना मांगने लगे.’
इस बात से सरकार इनकार नहीं करती कि उसने पूर्व आतंकियों की वापसी के लिए जो नीति बनाई उसमें इनके पुनर्वास का आश्वासन है. लेकिन पिछले चार सालों में किसी एक व्यक्ति का भी सरकार ने पुनर्वास नहीं किया. पिछले साल जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष महबूबा मुफ्ती के एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन को जानकारी दी थी कि बीते तीन सालों में 360 पूर्व आतंकी पाकिस्तान से अपने घर वापस जम्मू कश्मीर आए हैं और चूंकि सभी लोग सरकार द्वारा तय रास्ते के बजाय नेपाल के रास्ते से भारत आए हैं इसलिए इनमें से किसी का भी पुनर्वास नहीं किया गया. इन लोगों के प्रति राज्य सरकार का रुख आज तीन साल बाद भी बिल्कुल नहीं बदला है. तहलका ने इस मामले पर राज्य सरकार से कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन अभी तक हमें उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली. ऐसे मामलों में राज्य मानवाधिकार आयोग से भी कुछ उम्मीद की जा सकती है लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग का रवैया बेहद हास्यास्पद है. आयोग के सदस्य रफीक फिदा सफाई देते हैं, ‘हमें तो इस मसले पर कुछ पता ही नहीं. पूर्व आतंकवादियों में से किसी ने हम से संपर्क नहीं किया.’
पूर्व आतंकवादी बताते हैं कि उनके लिए सरकार द्वारा तयशुदा रास्तों से वापसी मुमकिन ही नहीं है. सरकार के इस रवैए को सारे पूर्व आतंकवादी धोखाधड़ी करार देते हैं. एहसान उल हक सवाल उठाते हैं, ‘सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है. इनसे पूछा जाना चाहिए कि हम लोग तय रूटों से आएं इसके लिए इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के साथ क्या इन्होंने इस संबंध में कोई बात की? अपने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को हमें वीजा और जरूरी कागजात मुहैया कराने के किए कहा? क्या बॉर्डर पर खड़ी सेना को इन्होंने कहा कि जो पूर्व आतंकी आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं उन्हें आने दो? स्थिति यह रही है कि जो लोग पाकिस्तानी एजेंसियों से किसी तरह छुपते-छुपाते बॉर्डर तक पहुंचे उन्हें सेना के लोग वापस नहीं जाने की स्थिति में गोली मारने की धमकी देते हैं. ऐसे में सरकार का यह कहना है कि ये लोग निर्धारित रुटों से नहीं आए एक बेहद अमानवीय और भद्दा मजाक है.’
यूसुफ कहते हैं, ‘इस बात का क्या मतलब कि हम किस रूट से आए. अरे आ तो गए हैं. हमारा पुनर्वास करो. जब तक मैं यहां नहीं आया था. सेना और सीआईडी के लोग मेरे अब्बू के पास रोज आते थे. उनसे कहते थे कि वे मुझे पाकिस्तान से वापस बुला लें. यहां सरकार मुझे नौकरी देगी. पैसा भी देगी. अब्बू ने मुझे उनके कहने के बाद ही वापस आने के लिए चिट्ठी लिखी. तभी मैं आया. लेकिन यहां आने के बाद वे लोग अपना वादा भूल गए. फौज तो कम से कम परेशान नहीं करती लेकिन सीआईडी वाले तो आए दिन तंग करते रहते हैं.’

फोटोः बृजेश सिंह
ये लोग 20-22 साल के बाद अपने घर वापस आए हैं. चूंकि इनमें से ज्यादातर लोग अपनी किशोरावस्था में ही सरहद पार चले गए थे ऐसी स्थिति में इनके पास जम्मू-कश्मीर का निवासी होने का कोई पहचान पत्र नहीं है. यानी एक तरह से जम्मू कश्मीर की नागरिकता का काम करने वाला ‘स्टेट सबजेक्ट’ नहीं हैं. राज्य में जिसके पास यह दस्तावेज होता है वही लोग जमीन जायदाद खरीद सकते है. इन्हीं लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा का अधिकार होता है.
सबसे ज्यादा दिक्कत इन लोगों की पत्नियों और बच्चों के साथ हैं. पूर्व आतंकियों में से लगभग सभी ने पीओके या पाकिस्तान की लड़कियों के साथ शादी की है. ऐसे में उनकी पत्नियों की पहचान का मामला अधर में लटका हुआ है. यहां आने के बाद का अपना अनुभव बताते हुए जहांगीर की पत्नी साजिया कहती हैं, ‘ मैं सिर्फ यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरे शौहर यहां आने चाहते थे. नहीं तो मेरा यहां मन एक सेकेंड भी नही लगता. न यहां की औरतों से हमारी सोच मिलती है, न जुबान, न रहन-सहन और न पहनावा. हम किसी से अपनी बात नहीं कर सकते.’
साजिया का अनुभव कोई अपवाद नहीं है. एक पूर्व आतंकी की पत्नी सबा परवीन कहती हैं, ‘ पहली दिक्कत तो यह है कि हमारी भाषा इन लोगों से बिलकुल अलग है. हमें कश्मीरी समझ में नहीं आती. ये लोग कश्मीरी भाषा में ही बात करते हैं. हम हिंदी, पंजाबी और उर्दू जानते हैं लेकिन इस भाषा में बात करने वाले बहुत कम लोग हैं यहां.’
इन महिलाओं के मन में इस बात की भी गहरी टीस है कि वे शायद कभी अपने घर वालों से नहीं मिल पाएंगी. साजिया कहती हैं, ‘ यहां इन लोगों के परिवार के सदस्य हमें पूरी तरह से नहीं अपना रहे हैं. ऐसे में अगर कल को इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी. यहां की लड़कियों का तो इस देश में मायका है. हमारा तो इनके अलावा कोई नहीं है और हम अपने घर भी नहीं जा सकते. शादी के बाद ही ये हमें छोड़कर चले आते तो तकलीफ नहीं होती. आज हमारे बच्चे हैं. ये उग्रवादी रहे हैं तो होंगे. इससे मेरा और मेरे बच्चों का क्या लेना देना.’ पूर्व आतंकी मतीन की पत्नी निशत फातिमा कहती हैं, ‘ सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए. हम तो बस अपने पति के कारण यहां आ गए. बस हमें हमारे घरवालों से मिलने जाने की इजाजत दे दें. जो बस उरी-मुजफ्फराबाद जाती है उससे हमें अपने घरवालो से भी मिलने जानें दें. हम पर रहम करें.’
हाल ही में यूसुफ की पत्नी शबीना के पिता का मुजफ्फराबाद में देहांत हो गया लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वे अपने पिता को देखने नहीं जा पाईं. युसूफ कहते हैं, ‘शबीना के अब्बू के इंतकाल पर मैंने हर जगह मिन्नतें कीं. मैंने कहा कि बस एक बार मेरी पत्नी को उसके पिता को देखने जाने दो लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी.’ सरकार को कोसते हुए युसूफ कहते हैं, ‘यह किस तरह का भेदभाव है. यासीन मलिक को आप पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट देते हैं. वह वहां जाकर शादी करता है. हाफीज सईद के साथ बैठक करता है. हमेशा आता-जाता है लेकिन हमारी पत्नियों को जाने की इजाजत नहीं है. जो लोग गन कल्चर को लेकर यहां आए उन्हें आप पासपोर्ट दे देते हो.’
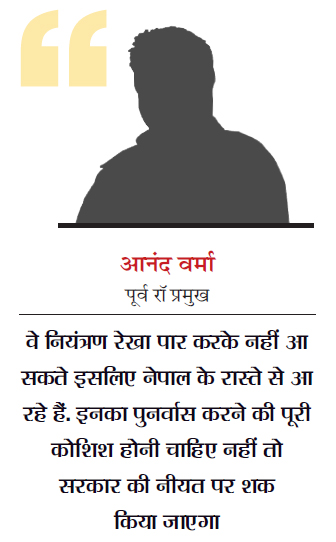 पूर्व आतंकवादियों की पत्नियों के साथ ही इनके बच्चों का जीवन भी यहां बेहद एकाकी और अलगाव से भरा है. पूर्व आतंकवादी जमील का 12 वर्षीय पुत्र इरफान कहता है, ‘ मेरे सभी दोस्त मुजफ्फराबाद में हैं. यहां के लड़कों की भाषा मुझे समझ नहीं आती.’ इन बच्चों की आगे की पढाई भी एक बड़ी दिक्कत है. बड़गाम के मंजूर अहमद कहते हैं, ‘ मेरा बड़ा बेटा वहां 10 वीं पास करके आया है लेकिन यहां आने के बाद उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है. पिछले दो सालों से मैं सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूं लेकिन स्कूल वाले हमारे बच्चों को एडमिशन देने से बिना कोई कारण बताए इंकार कर रहे हैं.’ यह अनुभव यहां लौटने वाले लगभग हर व्यक्ति का है. जहां तक प्रशासन की बात है तो वह इस समस्या को स्वीकार तो करता है लेकिन सीधा हल सुझाने की दिशा में कुछ करता नहीं दिखता. डीजीपी अशोक प्रसाद के अनुसार, ‘नागरिकता और आगे की पढ़ाई के लिए डिग्रियों की वैधता जटिल मामले हैं. उनके हल होने में थोडा समय लगेगा क्योंकि ये कानूनी और संवैधानिक मसला है. बाकी उनके जीवन को बेहतर बनाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं.’
पूर्व आतंकवादियों की पत्नियों के साथ ही इनके बच्चों का जीवन भी यहां बेहद एकाकी और अलगाव से भरा है. पूर्व आतंकवादी जमील का 12 वर्षीय पुत्र इरफान कहता है, ‘ मेरे सभी दोस्त मुजफ्फराबाद में हैं. यहां के लड़कों की भाषा मुझे समझ नहीं आती.’ इन बच्चों की आगे की पढाई भी एक बड़ी दिक्कत है. बड़गाम के मंजूर अहमद कहते हैं, ‘ मेरा बड़ा बेटा वहां 10 वीं पास करके आया है लेकिन यहां आने के बाद उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है. पिछले दो सालों से मैं सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूं लेकिन स्कूल वाले हमारे बच्चों को एडमिशन देने से बिना कोई कारण बताए इंकार कर रहे हैं.’ यह अनुभव यहां लौटने वाले लगभग हर व्यक्ति का है. जहां तक प्रशासन की बात है तो वह इस समस्या को स्वीकार तो करता है लेकिन सीधा हल सुझाने की दिशा में कुछ करता नहीं दिखता. डीजीपी अशोक प्रसाद के अनुसार, ‘नागरिकता और आगे की पढ़ाई के लिए डिग्रियों की वैधता जटिल मामले हैं. उनके हल होने में थोडा समय लगेगा क्योंकि ये कानूनी और संवैधानिक मसला है. बाकी उनके जीवन को बेहतर बनाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं.’
जब इन पूर्व आतंकवादियों का पुनर्वास नहीं हुआ तो इन्होंने राज्य में अपने स्तर पर रोजी-रोजगार करने की ठानी लेकिन इस मामले में भी इनके साथ मुसीबतें कम नहीं हैं. 2010 में पीओके से वापस आए फारुक अहमद शाह कहते हैं, ‘हमें कोई काम नहीं देता. जहां भी काम मांगने जाते हैं लोग हमारे मिलिटेंट बैकग्राउंड के कारण काम देने से इंकार कर देते हैं. एक तरफ रोजी रोटी का कोई इंतजाम है नहीं, वहीं हर दूसरे दिन पुलिस, सीआईडी पूछताछ के नाम पर बुलाती है. घंटों बैठाए रखती है. महीने में 20 दिन तो यही निकल जाते हैं. जब से आए हैं तभी से परेशान कर रहे हैं.’ पूर्व आतंकवादी अमजद अहमद कहते हैं, ‘यहां आने के बाद हमारे पास कोई रोजगार नहीं है. हम में से हर व्यक्ति पीओके में कोई ना कोई रोजगार कर रहा था लेकिन यहां हमारे सामने रोजी-रोटी का संकट है. 20-22 सालों में हमने जो भी कमाया था वह पूरा पैसा तो यहां आने में खर्च हो गया. अब यहां हमारे पास कोई रोजगार नहीं है.’ वापस आए ज्यादातर लोगों में से कोई दिहाड़ी मजदूरी कर अपना पेट पाल रहा है तो कोई ऑटो चलाकर या अन्य तरीकों से किसी तरह से दो जून की रोटी का इंतजाम अपने परिवार के लिए कर रहा है.
ये तमाम लोग आने के बाद किस तरह की अमानवीय स्थिति में जी रहे हैं, कितने प्रताड़ित हैं इसका पता उस समय चला जब हाल ही पाकिस्तान से वापस आए एक पूर्व आंतकी सैयद बशीर अहमद शाह ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. बशीर के 15 वर्षीय पुत्र फैजान कहते हैं, ‘अब्बू बहुत परेशान थे. पिछले साल ही हम लोग मुजफ्फराबाद से यहां आए थे. अम्मी यहां आने से रोक रहीं थीं लेकिन अब्बू नहीं माने. यहां आने के हफ्ते भर बाद ही अब्बू के बड़े भाई ने हमें घर से बाहर जाने के लिए कह दिया. हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. कुछ दिन के लिए हम अपने एक रिश्तेदार के पास चले गए. अब्बू के पास पैसे नहीं थे. वे घरों की रंगाई-पुताई का काम करने लगे. मजदूरी से जो पैसे मिलते थे उससे रोज का खर्च चलता था. दो महीने बाद उनसे वह दिहाड़ी मजदूरी भी छिन गई. घर खर्च के लिए लोगों से उन्होंने पैसे उधार लिए. वे लोग भी अपने पैसे मांगने लगे. आखिर में इन्हीं बातों का तनाव झेलते हुए उन्होंने एक दिन खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली.’
हाल ही में वापस आए मोहम्मद अशरफ वानी उर्फ जमील की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपनी बेटी की मजबूरी में शादी करनी पड़ी. जमील कहते हैं, मेरे पास यही विकल्प था कि अपनी बेटी को घर पर रखकर भूख से मार डालूं या कुछ करूं. मैंने उसकी शादी कर दी. मैं उसका गुनहगार हूं, वह 11 वीं में पढ़ती थी. मजबूरी में मैंने उसकी शादी की. न हमारे पास पहचान पत्र है, न राशन कार्ड. पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे हम. जमील बताते हैं उन्होंने ऑटो चलाकर अपना गुजारा करने की बात सोची थी लेकिन सरकार कहती है कि जब वे यहां तीन साल रह लेंगे तब उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा. इस समय उनके पास कोई रोजगार नहीं है और वे जैसे-तैसे गुजारा कर रहे हैं.
अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर ये लोग श्रीनगर में कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई परिवारों ने वापस पाकिस्तान जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है. हाल ही में सेना ने बारामुला से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाने का प्रयास करते हुए पांच परिवारों को गिरफ्तार किया था. पिछले दो महीने में तीन परिवारों के वापस जाने की भी खबरें आईं जिसमें दो परिवार उत्तरी कश्मीर के बंदीपुर जिले से थे और एक श्रीनगर से.
एहसान बताते हैं, ‘ अभी लगभग 25 हजार के करीब कश्मीरी लड़के पाकिस्तान में हैं. वे सभी वहां से आना चाहते हैं लेकिन हम उनसे कहते हैं, यहां आओगे तो भूखे मारे जाओगे. इसलिए वहीं रहो.’ जहांगीर झुंझलाते हुए कहते हैं, ‘आप से नहीं संभल रहा है तो हमें किसी तीसरे मुल्क में भेज दो. लोग सऊदी और कहां-कहां नौकरी करने जा रहे हैं लेकिन हम शहर से बाहर नहीं जा सकते. हम यहां कैद हो गए हैं. अगर मान लीजिए दिल्ली वगैरह में काम की तलाश में चले गए भी तो पुलिस पकड़ के कहेगी कि उसने एक बड़ा आतंकवादी पकड़ा है. लियाकत शाह का उदाहरण हमारे सामने है.’
[box]
 ‘पाकिस्तान में अब भी आतंकवादी शिविर चल रहे हैं’
‘पाकिस्तान में अब भी आतंकवादी शिविर चल रहे हैं’
पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग तो अभी-भी चल रही है. लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं है. जो लड़के कश्मीर से आए थे वे धीरे-धीरे सब हकीकत जान गए. इन लोगों को कहा गया था कि जेहाद में बरकत है. जेहाद में सबकुछ है. बड़े-बड़े वादे किए जाते थे कि कश्मीर आजाद होगा लेकिन हकीकत में पाकिस्तान और यहां की सेना को इससे कोई मतलब नहीं है. पाकिस्तान अपने स्वार्थ और मकसद के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहा है. ये खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं. जेहाद के लिए पहले जो ब्रेनवाश किया जाता था वह अब मुमकिन नहीं है. दूसरा यहां पर जेहादी गुटों के जो बड़े नेता हैं, उनके लड़के तो खुद जेहाद से बाहर हैं और वे यहां गरीब बच्चों को इस्तेमाल करते हैं. यहां जो कश्मीरी लड़के हैं वे भी देख रहे हैं कि भारतीय कश्मीर में स्थिति बेहतर हुई है. मुसलमान लड़के वहां से आईएएस बन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. उन्हें सरकारी नौकरियां मिल रही हैं. भारतीय कश्मीर में तो स्थिति बेहतर हो रही है. इसलिए अब ये लड़के पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंपों का रुख नहीं करते.
हफीज चाचड़, पाकिस्तान में बीबीसी के पूर्व संवाददाता
[/box]
इन पूर्व आतंकवादियों की राज्य में जो दुर्दशा है वह खुद ही कई खतरों को आमंत्रित कर सकती है. वरिष्ठ पत्रकार और जम्मू कश्मीर पर बने तीन सदस्यीय वार्ताकारों के समूह के सदस्य दिलीप पड़गांवकर इस बारे में इशारा करते हैं, ‘ यह एक दुखद सच है कि इन लोगों का पुनर्वास नहीं किया जा रहा. हम इन लोगों से मिले हैं. सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर वह इन लोगों का पुनर्वास नहीं करेंगे तो इसका फायदा आईएसआई और कश्मीर विरोधी ताकतें ही उठाएंगी.’ कुछ इसी तरह की बात हाल ही में पाकिस्तान से लौटे पूर्व आतंकवादी फारुक अहमद भी कहते हैं, ‘सरकार खुद चाहती है कि लोग मिलिटेंट बने. आज हमारे बच्चे तिल-तिल मर रहे हैं. अब ऐसे में कोई मुझे 10 लाख रुपये किसी गलत काम के लिए देगा तो क्या मैं नहीं लूंगा.’
एक तरफ पूर्व आतंकवादी वापस कश्मीर आने और अपने पुनर्वास को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो इधर एजेंसियां भी उनके ‘हृदय परिवर्तन’ की सच्चाई पर नजर बनाए हुए हैं. खुफिया विभाग के एक अधिकारी कहते हैं, ‘ हमें बिलकुल चौंकन्ना रहने की जरूरत है. सभी को पता है कि अफजल गुरु भी सरेंडर्ड मिलिटेंट ही था. डबल क्रॉस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.’ सरकार ने बेशक इन लोगों के लिए पुनर्वास की नीति बना दी हो लेकिन खुफिया विभाग का यह रवैया काफी हद तक इनके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है. खुफिया विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि पूर्व आतंकवादियों में से ज्यादातर ने पाकिस्तानी महिलाओं से शादी कर ली है. इनके बच्चे भी हैं. ऐसे में इनकी नागरिकता का दर्जा एक बड़ी समस्या है. पत्नी को वापस भेजा जा सकता है, लेकिन बच्चों का क्या करेंगे? सबसे बड़ा डर यह है कि आने वाले समय में ये बच्चे एक स्पष्ट नागरिकता के अभाव की स्थिति में कश्मीर विवाद की पहचान न बन जाएं. रॉ के पूर्व प्रमुख आनंद वर्मा कहते हैं, ‘इन लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए. कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे यहां के अमन चैन को कोई नुकसान पहुंचे. एजेंसियों को ध्यान रखना होगा कि इनके बीच ब्लैक शीप (संदिग्ध) ना आ जाएं. इन लोगों पर कुछ समय तक नजर रखने की जरूरत है.’
घाटी में पृथकतावादी भी इनकी वापसी को लेकर खुश नहीं है. सैयद अली शाह गिलानी कहते हैं, ‘ ये लोग लालच में आ गए. इन्हें यहां नहीं आना चाहिए था. पुर्नवास नीति के नाम पर भारत सरकार ने इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया जिसमें ये लोग फंस गए.’ जहां तक पूर्व आतंकवादियों की बात है तो वे खुद इन प्रथकतावादी संगठनों और उनके नेताओं की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं. जहांगीर कहते हैं, ‘आजादी की बात करने वाले ये लोग भारत और पाकिस्तान दोनों से पैसा लेते हैं. इनके बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे हैं. इन्होंने शहीदों की कब्रें बेच दीं. हम हुर्रियत के लोगों की कोठियों पर कब्जा करेंगे. इन्होंने ही हमें बंदूकें पकड़ाईं थी अब ये लोग आराम से नहीं बैठ सकते .’
चाहे राज्य सरकार हो, सुरक्षाबल, खुफिया एजेंसियां, प्रथकतावादी या अपना परिवार, हर किसी के लिए पाकिस्तान से आ रहे ये पूर्व आतंकवादी इस समय सबसे अवांछित व्यक्ति बन चुके हैं. ऐसा ही रहा तो मुमकिन है कि आने वाले समय ये भी राज्य की उन दर्जनों मानवीय त्रासदियों में शुमार हो जाएं जिनका जम्मू-कश्मीर के पास कोई स्थाई समाधान नहीं है.
जाति नहीं जाती कहीं
बक्सर लोकसभा सीट. ब्रह्मपुर ब्लॉक. एक मास्टर साहब मिलते हैं. चुनावी चर्चा चलने पर नंदपुर गांव के रहने वाले ये शिक्षक इत्मीनान से गणित बताने लगते हैं. कहते हैं, ‘देखिए हमारे क्षेत्र से इस बार बाबाजी यानी पंडित के नाम पर भाजपा ने अश्विनी चौबे को टिकट दे दिया है. अब वे भागलपुर इलाके के छी-छा वाले पंडितजी हैं तो कहां से हम लोग अपना तालमेल बिठा पाएंगे?’ मास्टर साहब आगे कहते हैं, ‘ठीक है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हवा-आंधी और ना जाने का-का है, लेकिन सांसद तो हमंे अपना ही चाहिए न. अपना माने हर तरह से अपना…!’ यह सब बताने के बाद मास्टर साहब चवन्निया हंसी दिखाते हैं और विदा ले लेतेे हैं.
औरंगाबाद जिले के ओबरा बाजार में अजय महतो से बात होती है. वे कहते हैं, ‘देखिए, बिहार में भाजपा लव-कुश यानि कुरमी-कोईरी गठजोड़ तोड़ने की तैयारी में है और उसके लिए राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी से उसका गठजोड़ भी हुआ है. हम कोईरी लोग यह गठजोड़ तोड़ भी देते, लेकिन काराकाट सीट यानी हमारे इलाके से चुनाव लड़ने राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के सर्वेसर्वा उपेंद्र कुशवाहा जी खुद आ गए हैं. अब उ गंगा पार के कुशवाहा हैं, अपना कोई कुशवाहा देते तो….! ’
बिहार में कई जगहों पर ऐसी ही बातें होती हैं. हर जगह अपने-अपने तरीके से लोग जाति की राजनीति का मुहावरा और गणित समझाते हैं. संकेत मिलता है कि बिहार इस बार के लोकसभा चुनाव में जाति के खोल में समाने की अकुलाहट में है. शायद यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के पहले अलग तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन टिकट तय होने के बाद से अनुमानों की दिशा दूसरी हो गई है. जो लोग कल तक यह आकलन कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के जरिये भाजपा राज्य में उफानी जीत की तरफ बढ़ रही है, वे अब ऐसा नहीं कह पा रहे हैं और जो कल तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के कुछ सीटों पर सिमट जाने का आकलन कर रहे थे, उनके सुर अब बदलते जा रहे हैं. वजह साफ है. बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव में उसने ही संभावनाओं को अपने पक्ष में किया है, जिसने जाति के साथ ही कुछ दूसरे समीकरण भी ध्यान में रखे हैं.
इस नजरिये से बिहार में सभी दलों ने अपने तरीके से पुरजोर मंथन किया. लेकिन कई दल उस मंथन की प्रक्रिया में ही ऐसे भटके कि टिकट बंटवारे का वक्त आते-आते दूसरी दिशा में चले गए. देखा गया कि पार्टियों को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा. पाला बदलकर दूसरे दलों में गए ऐसे नेताओं को तरजीह मिली जो सिर्फ जाति के आधार पर वोट जुगाड़ने की क्षमता रखते थे. ऐसे नेता रातों-रात टिकट पाने में भी सफल हुए.
बिहार में सभी दलों ने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया है उसे एक बार सरसरी तौर पर देखने पर सियासी गणित साफ-साफ दिखने लगता है.
बंटवारे का गणित
बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं. भाजपा 30 पर चुनाव लड़ रही है. शेष 10 सीटों में से सात उसकी सहयोगी पार्टी लोजपा के पास हैं और तीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के खाते में. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जदयू 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उसने दो सीट सीपीआई के लिए छोड़ी हैं. लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. 13 सीटें उसने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को दी हैं और एक सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में है.
अब इन पार्टियों के टिकट बंटवारे में जाति के समीकरण देखते हैं. भाजपा ने राजपूत जाति के सात, ब्राह्मण जाति के तीन, यादव जाति के चार, भूमिहार जाति के तीन, कायस्थ जाति के एक, अनुसूचित जाति के तीन, कुशवाहा जाति के एक, वैश्य समुदाय के तीन, अतिपिछड़ा समूह के तीन और मुस्लिम समुदाय के एक उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. भाजपा के नये-नवेले सहयोगी बने रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा के लिए सात सीटें रखी हैं, लेकिन उनमें से तीन सीटें अपने परिवार के खाते में ही डाल दी हैं. एक और पासवान को भी रामविलास ने तरजीह दी है. शेष तीन सीटों पर उन्होंने एक राजपूत, एक भूमिहार और एक मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है. जदयू की बात करें तो उसने छह टिकट यादव समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को दिए हैं तो छह कुशवाहा समुदाय को. इसके अलावा पार्टी ने पांच मुस्लिम , पांच महादलित, एक दलित, चार भूमिहार, दो ब्राहमण, दो राजपूत, एक कायस्थ, दो वैश्य, एक कुरमी और तीन अतिपिछड़ा समुदायों के प्रतिनिधियों को मैदान में उतारा है.
राजद ने 27 सीटों पर जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें नौ यादव समुदाय से हैं और छह मुस्लिम, तीन राजपूत, एक ब्राहमण, एक कायस्थ और दो कुशवाहा समुदाय से. इसके अलावा उसके तीन उम्मीदवार अतिपिछड़ा समूह से और दो अनुसूचित जाति से आते हैं. भाजपा के नए साथी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के खाते में तीन सीट आई हैं जिनमें दो पर कुशवाहा उम्मीदवार उतारे गए हैं जबकि एक पर भूमिहार प्रत्याशी है. जदयू ने जो दो सीट सीपीआई को दी हैं उनमें एक पर भूमिहार और एक पर यादव प्रत्याशी है. 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने पांच सीटों पर दलित-महादलितों को मैदान में उतारा है. बाकी में एक राजपूत, दो यादव, एक भूमिहार, एक ब्राहमण, एक कुरमी और एक मुस्लिम समुदाय का प्रत्याशी मैदान में हैं.
बंटवारे के निहितार्थ
बिहार में विभिन्न दलों द्वारा जाति व समूह को साधने के फेरे में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, उसने चुनावों और नतीजों से पहले ही काफी कुछ कह दिया है. लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ सालों में लगातार सवर्णों से माफी मांग रहे थे. माना जा रहा था कि अपनी पार्टी में तीन-तीन राजपूत सांसद होने की वजह से वे राजपूतों को ज्यादा तरजीह देकर एक नये किस्म का समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे. लेकिन जब टिकट बंटवारे पर फैसला करने का समय आया तो उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा अपने पुराने समीकरण माई पर ही किया. यानी मुस्लिम और यादव समुदाय के उम्मीदवारों को ही ज्यादा तरजीह दी. आश्चर्य यह रहा कि लालू प्रसाद ने लव-कुश समीकरण में एक समूह यानी कुशवाहा को तो टिकट दिया, लेकिन नीतीश कुमार जिस कुरमी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उससे उन्होंने एक भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा. राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं, ‘अगर लालू सोच रहे हैं कि मुसलमान अब भी पूरी तरह उनके साथ है तो ऐसा नहीं है. मुसलमान अब देखते हैं कि लालू या नीतीश में जिसके उम्मीदवार जीत की स्थिति में होंगे, वे उनके साथ ही जाएंगे.’
राजद जैसा ही हाल भाजपा का भी रहा. पार्टी लगातार अतिपिछड़ों और महादलितों में सेंधमारी की कोशिश कर रही थी. नरेंद्र मोदी अतिपिछड़े समुदाय से आते हैं, यह शोर भी मचाया जा रहा था. लेकिन टिकट बंटवारे में तरजीह मिली सवर्णों को.
इन सबके बीच नीतीश कुमार ने बहुत ही चतुराई से टिकट का बंटवारा किया है. जानकार मानते हैं कि उन्होंने सभी जातियों व समूहों को साधने की कोशिश की है. भाजपा जहां उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठजोड़ करके नीतीश कुमार के लव-कुश समीकरण को तोड़ने का अभियान चलाने में लगी रही, वहीं नीतीश ने अधिक से अधिक कुशवाहा प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर चुनाव के पहले ही भाजपा के अरमानों व उम्मीदों पर एक तरीके से पानी फेरने का काम किया है. जानकारों का यह भी मानना है कि अपने समुदाय यानी कुरमी समुदाय से सिर्फ एक उम्मीदवार को टिकट देकर नीतीश यह संदेश देने में भी सफल रहे हैं कि वे अपनी जाति के एकमात्र नेता हैं और टिकट दें या न दंे, उनकी जाति पूरी तरह से उनके साथ है.
बिहार में टिकट बंटवारे के बाद जो स्थितियां बनी हैं उन्हें देखकर माना जा रहा है कि द्वंद्व और दुविधा का सबसे ज्यादा शिकार भाजपा हुई है. एक तरफ तो वह नरेंद्र मोदी को अतिपिछड़े समूह का बताकर अतिपिछड़े समूह को अपने पक्ष में करने का अभियान चलाती रही, लेकिन टिकट बंटवारे में उस समूह का उस तरह से ख्याल नहीं रख सकी. इतना ही नहीं, भाजपा ने सबसे ज्यादा दांव सवर्णों पर और उनमें भी राजपूतों पर लगाया है जबकि बिहार की जमीनी हकीकत यह भी है कि सवर्ण समूह के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा या तो पलायित कर बाहर रहता है या रहता भी है तो जल्दी वोट देने नहीं आता.
राजद नेता प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि 1989 में भाजपा ने पूरे देश में 50 प्रतिशत ब्राह्मणों को ही उम्मीदवार बनाया था और ऐसी ही नीतियों की वजह से लालू और मुलायम जैसे नेताओं का आसानी और तेजी से उभार हुआ था. वे कहते हैं कि फिर से भाजपा उसी राह पर है–यानी राजनीति तो वह अतिपिछड़ों की करती रही, लेकिन टिकट बंटवारे में वह हिस्सेदारी नहीं दे सकी. हालांकि रालोसपा के रामबिहारी सिंह जैसे नेता कहते हैं कि किसी समूह की राजनीति करना और उसी समूह के नेता को अधिक से अधिक टिकट देना, दो बातें हैं. वे कहते हैं, ‘बिहार में तो भाजपा के दो तीन बड़े नेता ही पिछड़े समूह से आते हैं, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है!’
जानकारों के मुताबिक भाजपा को लग रहा है कि इस बार मुसलमानों का वोट लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच बंटेगा जिससे उसे फायदा होगा. एक ओर तो कांग्रेस के साथ होने और खुद की भी धर्मनिरपेक्ष छवि होने की वजह से लालू प्रसाद के खाते में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जाएगा. दूसरी ओर चूंकि नीतीश कुमार की छवि नरेंद्र मोदी का खुलकर विरोध करनेवाले नेता की बनी है, इसलिए मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग नीतीश के पक्ष में बात करता है.
हालांकि जानकार यह भी मानते हैं कि भाजपा को चिंता भी होनी चाहिए. उनके मुताबिक पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक और संसदीय क्षेत्र के हिसाब से प्रत्याशी मैदान में उतार तो दिए हैं, लेकिन कई जगहों पर सिर्फ जाति का ही काॅकटेल तैयार करने की कोशिश की है. उसमें यह ध्यान नहीं रखा कि क्या जाति के नाम पर आयातित प्रत्याशी भी चल जाएंगे या फिर स्थानीय प्रत्याशियों को उतारने का अपना महत्व होता है.
आंकड़ों से आत्मविश्वास!
[wzslider autoplay=”true” transition=”‘slide'” info=”true” lightbox=”true”]
पिछले दिनों सोशल नेटवर्किंग साइटों पर राजनीतिक चुटकलों की श्रंखला में एक और चुटकुला आया. इसका लब्बोलुआब यह था कि भाजपा में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगनेवालों के बीच मारामारी मची है. आम आदमी पार्टी (आप) की टिकट उम्मीदवार वापस कर रहे हैं. और कांग्रेस में तो जैसे टिकटों की सेल लगी है लेकिन कोई लेनेवाला नहीं. यह चुटकुला कुछ सच्ची घटनाओं से उपजा था, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो देश में बाकी आम जनता की नजर से यह बिल्कुल सटीक था. छत्तीसगढ़ की बात इसलिए कि यहां भाजपा और आप के लिए टिकट चाहने वालों की संख्या में कमी नहीं थी तो कांग्रेस के लिए भी यही हाल था. सबसे हैरानी की बात है कि इस समय जब तकरीबन सभी हिंदीभाषी राज्यों में कांग्रेस का मनोबल टूटा हुआ लग रहा है वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इतनी उत्साहित है कि वह अभी से राज्य की आधे से ज्यादा सीटें अपनी झोली में मानकर चल रही है.
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राज्य की कम से कम छह सीटों पर उसकी जीत पक्की है. पार्टी के पास इस दावे के पीछे अपने तर्क भी हैं. कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उसकी स्थिति उन सीटों पर मजबूत है जहां विधानसभा चुनाव में उसके भाजपा से ज्यादा विधायक चुन कर आए हैं या फिर पार्टी के कुल मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है. इन सीटों में बस्तर, कांकेर, सरगुजा, कोरबा और बिलासपुर शामिल हैं. पार्टी महासमुंद सीट पर भी जीत तय मान रही है. इसका एक मात्र कारण यहां से पार्टी के उम्मीदवार अजीत जोगी का कुशल चुनाव प्रबंधन है. अब यह कांग्रेस का मुगालता है या सचमुच ही पार्टी इन छह सीटों पर जीत रही है, यह समझने के लिए इन छह सीटों का मिजाज समझना जरूरी है.
प्रदेश में सबसे पहले बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होना है. कांग्रेस इस सीट को लेकर अत्यधिक उत्साहित है. दरअसल 2013 के अंत में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की स्थिति डावांडोल हो गई है. बस्तर लोकसभा सीट के तहत आने वाली आठ विधानसभा सीटों में से पांच सीटों – कोंडागांव, बस्तर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा और कोंटा में कांग्रेस का कब्जा है. जबकि केवल तीन सीटें, नारायणपुर, जगदलपुर और बीजापुर में भाजपा जीत पाई है. इतना ही नहीं बस्तर लोकसभा के तहत आने वाली आठों विधानसभा सीटों के कुल वोट जोड़ें तो कांग्रेस को करीब नौ हजार मतों की बढ़त भी मिली है. यही दो बातें कांग्रेस का उत्साह बढ़ा रही हैं. लेकिन जरूरत से ज्यादा उत्साहित कांग्रेस इस तथ्य की अनदेखी कर रही है कि बस्तर सीट पर उसे केवल भाजपा से ही नहीं, बल्कि ‘आप’ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) से भी चुनौती मिल रही है. ‘आप’ ने इस सीट से सोनी सोरी को मैदान में उतारा है. वहीं सीपीआई की विमला सोरी भी मैदान में हैं. विमला रिश्ते में सोनी सोरी की बहन लगती हैं. ये दोनों उम्मीदवार भाजपा के किले में कम, कांग्रेस के गढ़ में ज्यादा सेंध लगाएंगे. कांग्रेस ने यहां से झीरम घाटी नक्सल हमले में मारे गए महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक कर्मा पर भरोसा जताया है.
दूसरे चरण यानि 17 अप्रैल को महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट पर मतदान होना है. इन दोनों सीटों को लेकर भी कांग्रेस में गजब का आत्मविश्वास है. महासमुंद में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के बगावती तेवर में आने के बाद भी कांग्रेस यहां से निश्चिंत है. इस सीट से पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को उम्मीदवार बनाया है. लेकिन 2009 में इसी सीट से कांग्रेस की टिकट में चुनाव लड़कर हार चुके मोतीलाल साहू ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी है. साहू कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे. वहीं दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की बेटी प्रतिभा पांडे भी महासमुंद से टिकट की दावेदारी कर रही थीं. उनके समर्थक भी पूरी तरह पार्टी के साथ नहीं िदख रहे हैं.
कांकेर लोकसभा सीट की बात करें तो 2009 में यहां से भाजपा उम्मीदवार सोहन पोटाई चुनाव जीते थे. नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को मदद करने के आरोपों का सामना कर रहे पोटाई को बैकफुट पर करते हुए भाजपा ने यहां से विक्रम उसेंडी को टिकट दिया है. उसेंडी पूर्व वन मंत्री तो हैं ही साथ ही अंतागढ़ सीट से विधायक भी हैं. कांग्रेस ने यहां से जोगी समर्थक फूलोदेवी नेताम को टिकट दिया है. कांकेर सीट को लेकर कांग्रेस की निश्चिंतता का कारण हाल के विधानसभा चुनाव में उसे मिला जनसमर्थन है. इस लोकसभा सीट के तहत आने वाली 8 में से 6 विधानसभा सीटों को जीतकर कांग्रेस ने भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश की है. कांग्रेस को कांकेर लोकसभा क्षेत्र की आठ विधानसभा सीटों में उसे 87 हजार वोट की बढ़त भी मिली है. यही कारण है कि उसे ये सीट आसान नजर आ रही है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल कहते हैं, ‘ हम सभी सीटों पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की जीत साफ दिखाई दे रही है. विधानसभा के जनादेश में जिन सीटों पर जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था, लोकसभा चुनाव में उसका फायदा तो मिलेगा ही.’
2009 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 11 सीटों में से केवल कोरबा (सामान्य सीट) ही कांग्रेस के खाते में गई थी. पार्टी ने इस सीट से एक बार फिर वर्तमान सांसद चरणदास महंत को प्रत्याशी बनाया है. कांग्रेस इस सीट को लेकर आश्वस्त दिख रही है. वैसे 2013 के विधानसभा चुनाव में कोरबा लोकसभा के तहत आने वाली आठ विधानसभा सीटों में से कांग्रेस-भाजपा दोनों को चार-चार सीटें मिली थीं लेकिन कांग्रेस कोरबा लोकसभा क्षेत्र में करीब 86 हजार वोट की बढ़त हासिल करने में कामयाब रही. इसके साथ ही पाली-तानीखार नाम की एक विधानसभा सीट पर भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई थी. यहां से जीत का सेहरा कांग्रेस के रामदयाल उइके के सिर बंधा था. वहीं दूसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आमद दर्ज करवाई थी. इन समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस के नेता कोरबा को भले ही पूरी तरह सुरक्षित सीट ना मान रहे हों लेकिन उन्हें लगता है कि इस सीट पर कम मशक्कत में ही फतह हासिल की जा सकती है. हालांकि कांग्रेस के अंदरखाने बात ये भी है कि बगैर अजीत जोगी की मदद के महंत के लिए कोरबा सीट निकालना मुश्किल है. दरअसल कोरबा में मरवाही और पाली तालाखार विधानसभा सीट पर जोगी गुट का कब्जा है. मरवाही से जोगी के पुत्र अमित जोगी और पाली तानाखार से कट्टर जोगी समर्थक रामदयाल उइके विधायक हैं. इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जबर्दस्त तरीके से बढ़त हासिल की थी. यही कारण है कि महंत इन दिनों जोगी के बंगले के चक्कर काटते देखे जा सकते हैं. हाल ही में महंत से जब इन मुलाकातों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, ‘ जोगी मेरे बड़े भाई हैं. इसलिए मैं उनसे मिलते रहता हूं. इन मुलाकातों में केवल पारिवारिक बातें हुई हैं, राजनीतिक बातें नहीं.’
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट सरगुजा भी कांग्रेस को जीती हुई ही प्रतीत हो रही है. सरगुजा की आठ विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने सात सीटों पर फतह हासिल की है. भाजपा केवल प्रतापपुर सीट ही जीत पाई. यहां से रामसेवक पैकरा विधायक चुनकर आए. वे इस समय प्रदेश के गृहमंत्री हैं. सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में प्रतापपुर को छोड़कर बाकी सातों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का परचम लहराया. यदि सरगुजा लोकसभा में आने वाली सभी आठ विधानसभा इलाकों के मतों को जोड़ दें तो यहां कांग्रेस को पांच लाख पचहत्तर हजार से ज्यादा वोट मिले हैं. जबकि भाजपा को चार लाख अड़सठ हजार वोट मिले. इस तरह आठ विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को करीब एक लाख वोट से अधिक की बढ़त मिली है. पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में ही रहा है. कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक रामदेव राम को अपना उम्मीदवार बनाया है. जबकि पिछली बार निर्वाचित मुरारी लाल सिंह के निधन के कारण भाजपा ने नए उम्मीदवार के रूप में कमलभान सिंह को उतारा है. सरगुजा इलाके में गोंड़ समाज के आदिवासियों की आबादी अधिक है. लेकिन इसे कांग्रेस का अति आत्मविश्वास ही कहेंगे कि कांग्रेस ने गोंड बहुल इस सीट पर उरांव समुदाय के रामदेव राम को मैदान में उतारा. छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का कहना है, ‘सरगुजा सीट पर कांग्रेस आलाकमान की भी निगाह है. आखिर हमने यहां की आठ विधानसभा सीटों में से सात पर फतह हासिल की है.’
सामान्य सीट बिलासपुर को लेकर भी कांग्रेस को काफी उम्मीद है. पार्टी ने यहां से करुणा शुक्ला को मैदान में उतारा है. करुणा पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की भतीजी हैं. वे 32 साल भाजपा में रहने के बाद हाल ही में पार्टी में शामिल हुई हैं. ब्राह्मण और साहू बहुल सीट बिलासपुर में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को लग रहा है कि वह मैदान मार लेगी. हालांकि इसका दूसरा कारण ये भी है कि विधानसभा चुनाव में यहां से दिलचस्प तस्वीर उभरकर सामने आई है. भले ही बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की आठ विधानसभा सीटों में से पांच भाजपा के खाते में गई और कांग्रेस को तीन सीटों पर संतोष करना पड़ा. लेकिन आठ विधानसभा क्षेत्रों में मिले कुल वोट का हिसाब देखें तो कांग्रेस को करीब नौ हजार से अधिक वोट की बढ़त मिली है. 2009 में बिलासपुर सीट से भाजपा के दिलीप सिंह जूदेव जीते थे. कार्यकाल पूरा करने के पहले उनके निधन के बाद भाजपा ने इस सीट से नए चेहरे लखन साहू पर दांव खेला है. अब नई पार्टी में आई करुणा शुक्ला कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाती हैं ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन इतना जरूर है कि बिलासपुर में जब कांग्रेस ने लोकसभा टिकट के लिए उनकी उम्मीदवारी पर गंभीर चर्चा शुरू की थी तब ही कुछ बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी. इस नुकसान की भरपायी पार्टी कैसे करेगी इसका जवाब उसके पास नहीं है.
बहरहाल 2009 में केवल एक सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार आंकड़ों के गणित पर भरोसा करते हुए राज्य की आधी से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है. लेकिन आम लोगों से लेकर खास लोग तक जानते हैं कि राजनीति ‘कला’ का विषय है न कि गणित का.
विरासत विहीन?

किसी अवश्यंभावी युद्ध के लिए आमने-सामने खड़ी दो सेनाओं में से किसी एक सेना के कुछ बड़े सिपाही अगर ऐन मौके पर लड़ने से इंकार कर दें, और कुछ प्रतिपक्षी बेड़े में शामिल होने लगें तो यह स्थिति उस सेना के गिरते मनोबल को साफ तौर पर दर्शाती है. सामान्य बुद्धि व्यवहार से लेकर आदर्शवाद तक का तकाजा कहता है कि ऐसी स्थिति में उस सेना के सेनापति को सामने आकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहिए और खुद पहल करते हुए विपक्षी दल पर पहला वार करना चाहिए. लेकिन अगर वह सेनापति ऐसा करने के बजाय पहले ही लड़ाई के मैदान में उतरने से इंकार कर चुका हो और उसकी जगह पर सेना की अगुआई करने के लिए भी कोई लड़ाका सामने न आए तो ऐसी स्थिति में उस सेना की हार अवश्यंभावी हो जाती है. इस सबके बीच एक अहम सवाल यह भी पैदा होता है कि इतिहास में उस सेनापति को किस तरह याद रखा जाएगा?
देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के मौजूदा हालातों पर यह काल्पनिक कहानी और इसके पात्र पूरी तरह फिट बैठते नजर आते हैं. आगामी चुनावों के लिए यह पार्टी मैदान में उतर चुकी है. तयशुदा हार को देखते हुए उसके कई प्रमुख नेता चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके हैं, और कुछ दलबदलू बन कर विपक्षी जहाज में चढ़ गए हैं. सेनापति की भूमिका वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मोर्चा संभालने के बजाय पहले ही चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके हैं और पार्टी उनके बगैर बिना किसी घोषित नाम की अगुआई के चुनाव मैदान में खड़ी है. इन परिस्थियों को देखते हुए बहुत से राजनीतिक पंडित पार्टी की हार को तय मान रहे हैं. यदि हार-जीत के सवाल को अलग भी रख दिया जाए तब भी ऊपर वाली कहानी की भांति यहां भी वैसा ही अहम सवाल पैदा होता है – इतिहास उन मनमोहन सिंह को किस तरह याद रखेगा जिनके द्वारा पार्टी की अगुआई से हाथ खींचने के बाद उनकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा शख्स सामने ही नहीं आया?
इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने के लिए मनमोहन सिंह के दशक भर लंबे कार्यकाल का लेखा-जोखा खंगालने के साथ ही उन घटनाओं, परिस्थितियों तथा परिणामों का आकलन करना जरूरी है जो कुछ लोगों के लिए उनके व्यक्तित्व को विरासत-विहीन बताने का आधार तैयार करती हैं.
2004 में यूपीए की पहली पारी की कमान संभालने से पहले मनमोहन सिंह को राजनीतिक मायनों मे लो-प्रोफाइल से भी नीचे की जमात का व्यक्ति माना जाता था. इसकी बहुत बड़ी वजह उनका 24 कैरेट ब्यूरोक्रेट वाला कलेवर और गैर-राजनीतिक प्रवृत्ति का होना था. लेकिन देश की कमान संभालने के बाद इस शर्मीले सरदार का पूरा व्यक्तित्व अनिवार्य रूप से राजनीतिक परिधि में आ गया. यहीं से उनको पास और फेल की कसौटी पर तौलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई.
इससे पहले मनमोहन सिंह राजीव गांधी की सरकार में योजना आयोग का दफ्तर संभालने से लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर और देश के वित्तमंत्री रह चुके थे. 1991 में वित्तमंत्री बनने के बाद उन्होंने ही देश में आर्थिक सुधारों के दरवाजे खोले थे. इस सबके बावजूद शायद ही किसी को भी इस बात का भान रहा होगा कि वे कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं. 2004 में अनुकूल परिस्थियों के बावजूद विदेशी मूल के मुद्दे पर जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इंकार कर दिया था तो तब भी अटकलों का पेंडुलम शुरुआती दौर में प्रणव मुखर्जी और अर्जुन सिंह जैसे बड़े नामों की तरफ ही झुका था. लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह पर मुहर लगा दी और वे प्रधानमंत्री बन गए. तभी से उन पर सोनिया गांधी की कृपा से सात रेसकोर्स रोड पहुंचने वाले शख्स का तमगा भी चस्पा कर दिया गया. वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, ‘गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद सोनिया गांधी का उन्हें प्रधानमंत्री बनाना इस बात की तरफ साफ इशारा था कि वे दस जनपथ के द्वारा ही गवर्न किए जाएंगे.’
सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान बहुत सारी घटनाओं ने इस धारणा को धार देना शुरू किया. बाद में यह धारणा तब और भी बलवती हो गई जब मनरेगा और आरटीआई जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां मनमोहन सरकार के बजाय सोनिया गांधी के खाते में जाती दिखीं. यहां तक कि 2009 के चुनाव में उतरते वक्त भी पार्टी ने इनका श्रेय सोनिया गांधी को ही दिया. इस मामले में सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि इस सब पर प्रधानमंत्री ने कभी कोई आपत्ति तक नहीं की. कई जानकारों के मुताबिक यह एक तरह से मनमोहन सिंह की हाईकमान के प्रति अगाध आस्था का परिचायक थी. इसके बाद बहुत से और भी मौके आए जब मनमोहन सिंह पूरी तरह दस जनपथ के रंग में रंगे मिले. धीरे-धीरे लोगों के मन में उनके रोबोट प्रधानमंत्री होने की धारणा इस कदर घर कर गई कि अखबारों में छपने वाले कार्टूनों से लेकर सोशल मीडिया तक में यह साफ दिखने लगा. कार्टूनों के जरिए जहां सांकेतिक तौर पर उन्हें सोनिया गांधी के इशारे पर चलने वाला प्रधानमंत्री बताया गया, वहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस बारे में खुलकर कमेंटबाजी होने लगी. मौजूदा राजनीतिक जमात में सबसे सीनियर और प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें अब तक का सबसे कमजोर और लाचार प्रधानमंत्री तक करार दिया. अपने दस साल के कार्यकाल की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियां और सराहना बटोरने वाले मनमोहन सिंह अपने दूसरे कार्यकाल में वहां भी गरियाये जाने लगे. पश्चिमी मीडिया के निशाने पर आए प्रधानमंत्री को पहले टाइम पत्रिका ने ‘अंडरअचीवर’ की संज्ञा दी और फिर इंडिपेंडेंट ने भी उनकी आलोचना में लेख छापा. अमरीका के जाने-माने अखबार ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने तो उनकी काबिलियत पर सवाल उठाते हुए यहां तक लिख दिया कि, ‘मनमोहन सिंह के सर पर इतिहास में एक विफल नेता के तौर पर याद किये जाने का खतरा है.’
जानकारों की मानें तो देश से लेकर दुनिया भर में हो रही इस आलोचना के पीछे बेशक बहुत सारे दूसरे कारण भी माने जा सकते हैं लेकिन बारीकी से देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण उनका दस जनपथ के इशारे पर चलने वाली इमेज में बंधा होना ही था. अपनी सरकार की उपलब्धियों का सारा श्रेय सोनिया गांधी के सुपुर्द करने से लेकर राहुल गांधी के लिए किसी भी वक्त कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहने जैसे वक्तव्य देकर मनमोहन सिंह ने कई मौकों पर इस बात को चरितार्थ भी किया है. जेएनयू में प्रोफेसर पुष्पेश पंत कहते हैं, ‘दागी जन प्रतिनिधियो के संबंध में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राहुल गांधी की नाराजगी के बाद तुरंत वापस लेने की घटना से भी इस बात को बहुत हद तक समझा जा सकता है कि दस जनपथ के प्रति वे किस कदर आस्थावान हैं.’
हालांकि इस सबके बावजूद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ मौकों पर इस धारणा को तोड़ने का प्रयास भी किया. परमाणु करार के मुद्दे पर लेफ्ट पार्टियों द्वारा सरकार गिराने की धमकी के बावजूद टस से मस न होने के उनके फैसले को इस नजरिए से बेहद अहम कहा जा सकता है. जानकारों का मानना है कि पूरे कार्यकाल में एकमात्र इस मौके पर ही ऐसा हुआ जब मनमोहन सिंह दस जनपथ के खोल से बाहर निकल कर काम करते दिखे. गौरतलब है कि परमाणु करार के मुद्दे पर मनमोहन सिंह अपनी शांत छवि के विपरीत एक ऐसे जिद्दी सरदार के रूप में तब्दील हो गए थे जिसने अपनी कुर्सी दांव पर लगी होने के बावजूद इस करार को लेकर गजब की प्रतिबद्धता दिखाई. इस करार पर उनके दस्तखत करते ही बाहर से समर्थन दे रही वाम पार्टियों ने सरकार को तलाक देकर उसके सामने शक्ति परीक्षण की चुनौती रख दी थी. हालांकि तब समाजवादी पार्टी ने उसे जरूरी आक्सीजन मुहैया करा दी लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना भी हुई जिसने मनमोहन के इस फैसले को अपनी कालिख से धुंधला कर दिया. परमाणु करार के मुद्दे पर जिस वक्त संसद में शक्ति परीक्षण हो रहा था, उसी वक्त कुछ सांसदों ने लोक सभा में नोटों की गड्डियां लहरा दीं. इन सांसदों का आरोप था कि परमाणु करार पर समर्थन जुटाने के लिए उन्हें रिश्वत दी गई थी. इस घटना ने भारतीय लोकतंत्र के मुंह पर जोरदार तमाचा तो मारा ही साथ ही मनमोहन सरकार पर भी संदेह की सुइयां टिका दीं. जानकारों की मानें तो यह मामला सिर्फ नोट लहराने या सरकार बचाने भर का नहीं था. चूंकि उस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मनमोहन सिंह बैठे थे इस लिए कई लोग इस घटना के लिए उन्हें भी कम से कम नैतिक रूप से दोषी मानते हैं.
प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह पर इसके अलावा दूसरी संवैधानिक संस्थाओं का मानमर्दन करने के आरोप भी लगे. ऐसे में एक नजर उन घटनाओं की तरफ डालना जरूरी है जिनके जरिए ऐसी संवैधानिक संस्थाओं पर पड़ी चोटों के निशान ढूंढे जा सकते हैं.
सबसे पहले सीएजी को लेकर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के रवैये का जिक्र करते हैं. कोल आवंटन को लेकर हुई तमाम गड़बड़ियों के संदर्भ में मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि इस बेहद सम्मानित संवैधानिक संस्था पर तब जम कर बरछे, भाले बरसाए गए जब उसने 2012 में अपनी रिपोर्ट में इन गड़बड़ियों को उजागर किया. सीएजी ने 2006 से 2010 के बीच हुए कोयला ब्लाक आवंटन में हुई अनियमितताओं के चलते देश को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात उजागर की थी. इस दौरान एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री खुद ही कोयला मंत्रालय का काम संभाल रहे थे. लेकिन इस पर कोई जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने सीएजी पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए. उसकी रिपोर्ट को विवादास्पद बताते हुए मनमोहन सिंह का कहना था कि इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति (पीएसी) के सामने आने पर चुनौती दी जाएगी. जानकारों की मानंे तो यह कृत्य पूरी तरह से एक संवैधानिक संस्था के अधिकारों को चुनौती देने की संज्ञा में आता है. तब प्रधानमंत्री द्वारा सीएजी पर सवाल उठाने की घटना से हैरानी जताने वालों में एक दौर में राज्यसभा में उनके साथी रहे और राजीव गांधी सरकार के दौरान सीएजी रहे टीएन चतुर्वेदी भी शामिल थे. उनका कहना था कि, ‘सीएजी की रिपोर्ट को पीएसी में चुनौती देने की बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किस आधार पर कही जा सकती है जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि पीएसी सरकार की नहीं बल्कि संसद की होती है, और इसके कामकाज का निर्धारण सरकार का मुखिया नहीं कर सकता.’

यहां पर एक और घटना का जिक्र किया जाना बेहद प्रासंगिक है. दरअसल 1952 में पहली बार संसद में सीएजी को लेकर कुछ सांसदों ने नाराजगी का भाव दिखाया था. लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि, ‘संसद में सीएजी की आलोचना करना उसके संवैधानिक अधिकार को चुनौती देना है.’ जानकारों की नजर में नेहरू के इस वक्तव्य में संवैधानिक संस्था के रूप में सीएजी के प्रति उनके सम्मान और आस्था का भाव तो था ही साथ ही एक अहम संदेश यह भी था कि भविष्य में संसद को सीएजी की आलोचना से बचना चाहिए. लेकिन इस घटना के छह दशक बाद जब उन्हीं की पार्टी की सरकार ने सीएजी की भूमिका पर संसद में सवाल उठाए तो मनमोहन सिंह ने इन आवाजों को और भी ऊंचा सुर दे दिया.
मनमोहन सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने का एक और पड़ाव था केंद्रीय चुनाव आयोग. दरअसल इसी साल – 2012 में – उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे. इस दौरान दो केंद्रीय मंत्रियों सलमान खुर्शीद और बेनी प्रसाद वर्मा को चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए धर लिया. एक चुनावी रैली में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने मुस्लिम आरक्षण का लॉलीपाप निकालते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में नौ प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना और खुर्शीद से जवाब तलब किया. लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने चुनाव आयोग को उन्हें सूली पर लटका देने की चुनौती दे डाली. इसके बाद व्यथित चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की जिसके बाद चौतरफा दबाव को देते हुए खुर्शीद को औपचारिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी.
इसी तरह की एक और गुस्ताखी इसके ठीक दो दिन बाद केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने भी की. उन्होंने भी मुस्लिम आरक्षण का वही लालीपाप निकाल कर मुस्लिम वोट साधने की जुगत भिड़ाई. चुनाव आयोग को अपने खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती देने के बाद उन्होंने बाद में अफसोस जताने की औपचारिकता भी निभाई, इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का कहना था, ‘नेताओं द्वारा माफी मांग लिए जाने की सूरत में आयोग उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता लेकिन संबंधित दलों को ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके.’ लेकिन इस मामले में कुरैशी की राय से सरकार का कितना इत्तफाक रहा, यह इससे समझा जा सकता है कि बेनी प्रसाद वर्मा और सलमान खुर्शीद न तो मंत्रिमंडल से हटाए गए और न ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कोई डांट पिलाई.
संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप की मानें तो ऐसा नहीं है कि सलमान खुर्शीद या बेनी प्रसाद वर्मा को चुनाव के कायदे पता नहीं थे. इसके बावजूद अगर वे आयोग से टकराए तो इसके छिपे अर्थों को समझना जरूरी हो जाता है. वे कहते हैं, ‘ऐसे समय में जब देश की ज्यादातर संवैधानिक संस्थाओं की साख घटती जा रही है, चुनाव आयोग पर इस तरह के हमले होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.’
चुनाव आयोग की साख गिराने के बाद मनमोहन सरकार पर सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का मान गिराने का आरोप भी लगा. बताया जाता है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति में उनकी सरकार ने कानूनी पहलुओं की पूरी तरह अनदेखी की और पामोलिन तेल आयात घोटाले में शामिल होने के आरोप वाले पीजे थॉमस को इस पद पर बिठा दिया. लोकसभा में विपक्ष की नेता होने के नाते सीवीसी की चयन समिति की सदस्य रहीं सुषमा स्वराज ने समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाया भी था. लेकिन सरकार ने इस बात की अनदेखी कर दी. बाद में मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा और उसने थॉमस की नियुक्ति को अवैध करार दिया था. इस मामले में महत्वपूर्ण यह था कि भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करने वाली सीवीसी की कमान मनमोहन सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देने की कोशिश की थी जिस पर खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे.
बेशक इस मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकना पड़ा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रति मनमोहन सरकार का रवैया हमेशा ‘यस मी लार्ड’ वाला ही रहा हो. दरअसल मनमोहन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कई सदस्यों ने कई मौकों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से न्यायपालिका को अपने दायरे में रहने की गैर-जरूरी सलाह दी है. इस सबकी शुरुआत तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने टू-जी मामले में जांच की निगरानी समेत कई दूसरे मामलों को भी अपने हाथों में लेना शुरू किया. सरकार और अदालत का टकराव उन स्थितियों में ज्यादा दिखा जब चुनावी लाभ कमाने की मंशा से शुरू की गई सरकारी योजनाओं को अदालत ने सेंसर करना शुरू किया. अध्यादेश रूपी ब्रह्मास्त्र की आड़ में कई मौकों पर मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का काम भी करने लगी. हाल ही में दागी जन प्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद जिस तेजी से सरकार ने इस बाबत अध्यादेश लाने का उपक्रम किया था वह भी सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसके दुराग्रह को साफ दर्शाता है.
मनमोहन सरकार के कार्यकाल में सरकार और सेना के बीच टकराव की घटना भी हुई. पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की जन्म तिथि को लेकर शुरू हुए विवाद ने प्रधानंमत्री मनमोहन सिंह और उनकी सरकार पर किसी खास व्यक्ति को सेनाध्यक्ष बनाने के लिए मुहिम चलाने का ऐसा आरोप लगाया जिसने एक संस्थान के रूप में सेना की प्रतिष्ठा पर जबरदस्त चोट पहुंचाने का काम किया. इस प्रकरण में आरोप लगा कि सिख अधिकारी विक्रमजीत सिंह को सेना प्रमुख बनाने की चाह में सरकार ने जनरल वीके सिंह के खिलाफ काम किया. यानी इस मामले में भी यूपीए की सरकार साफ तौर पर सेना जैसी सम्मानित संस्था के खिलाफ टकराव मोल लेती दिखी.
कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएजी से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सेना तक के मामले में शायद ही कोई ऐसी संवैधानिक संस्था होगी जिसके प्रति मनमोहन सिंह ने प्रेम और अनुराग की मिसाल छोड़ी हो. यूपीए सरकार ने हरसंभव हाथ आए मौकों पर इन संवैधानिक संस्थाओं की साख को धता बताने का काम बेरोकटोक और मनमर्जी से किया. एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि यह सब कुछ उन मनमोहन सिंह की सरपरस्ती में हुआ जिन्हें सौम्य, विनम्र और भलेमानस की संज्ञा दी जाती रही है.
हांलांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा समय-समय पर मनमोहन सरकार के इन फैसलों को क्लीन चिट दी जाती रही है. लेकिन बावजूद इसके यह सवाल तो उठता ही है कि अगर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा किए गए ये कृत्य कहीं से भी गलत नहीं हैं तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी उनके इन कामों को आधार बना कर आगे बढने का साहस नहीं कर पाई ? सवाल तो यह भी है कि क्या वाकई में मनमोहन सिंह की ऐसी कोई विरासत है भी कि जिस पर इतराया जा सकता है.
जानकारों की मानें तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मनमोहन सिंह के दस साला कार्यकाल में महंगाई का सूचकांक जिस रफ्तार से ऊंचाई को छूकर निकला है उससे भी उनकी विरासत संभालने से काग्रेस पार्टी हिचक रही है. यह भी एक विसंगति ही कही जानी चाहिए कि एक कुशल अर्थशास्त्री की संज्ञा प्राप्त मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर तक पहुंचा.
इस पूरी कथा में लोकपाल बिल का जिक्र करना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा. अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद फजीहत झेल चुकी सरकार ने लोकपाल बिल को जब अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मंजूरी दी तो उसने इसे अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भुनाना चाहा. लेकिन उसकी इस कोशिश को तब जोरदार झटका लगा जब पहले प्रख्यात अधिवक्ता फाली नरीमन ने लोकपाल चयन के लिए बनी कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और फिर न्यायमूर्ति केटी थॉमस ने भी खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उन्हें संदेह है. यह घटना संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बनाने की कवायद में मनमोहन सरकार की एक और कोशिश की तरफ साफ इशारा करती है. इस तरह देखा जाए तो कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह की सरकार के दस बरस तमाम संवैधानिक संस्थाओं की खिलाफत करने में समर्पित रहे हैं.
इस दौरान बहुत से मौके ऐसे भी आए जब खुद प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी लड़खड़ाते देखा गया. कुछ घटनाओं की पड़ताल करने पर यह बात और भी आश्चर्यजनक ढंग से सामने आती है कि अधिकतर मौकों पर ऐसा करने वाले खुद प्रधानमंत्री ही थे. इस बात का सबसे सटीक उदाहरण उनके उस वक्तव्य में देखा जा सकता है जब वे बार-बार राहुल के नेतृत्व में काम करने और उनके लिए किसी भी वक्त कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहने की बात करते हैं. इसके अलावा दागी सांसदों के चुनाव लड़ने संबंधी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की ‘ना’ के बाद मनमोहन सरकार द्वारा पहले अध्यादेश लाने का फैसला करना और फिर राहुल गांधी के इंकार के बाद इससे पलट जाना भी प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विपरीत जाता है. कई कांग्रेसी भी अनौपचारिक बातचीत में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनके मंत्रिमंडल तक में उन्हें गंभीरता से लेने वाले गिने-चुने ही हैं. इसके अलावा बहुत सी दूसरी घटनाएं और भी हैं जो दिखाती हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की साख पर आंच आई है. हाल ही में तेलंगाना विधेयक को संसद में पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के वक्त कुछ सांसदों द्वारा जिस तरह हो हल्ला मचाया गया उससे भी इस बात को समझा जा सकता है.
एक सबसे अहम उदाहरण का जिक्र किए बगैर यह प्रसंग अधूरा कहा जा सकता है. दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के फौरन बाद ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) नाम की एक समिति बनाई थी. सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली इस समिति को एक प्रकार से सरकार से ऊपर का दर्जा प्राप्त था. कुछ समय पहले तहलका से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता यशवंत सिन्हा का कहना था कि, ‘मनमोहन सिंह के पास जिम्मेदारी तो है लेकिन ताकत नहीं है, जबकि जिन सोनिया गांधी के पास ताकत है उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है.’ यशवंत सिन्हा की बातों से निकले मर्म को देश के संदर्भ में निकाला जाए तो एक सवाल खड़ा होता है कि देश को जिस नेतृत्व की इस वक्त सबसे अधिक जरूरत है, क्या मनमोहन सिंह उस खांचे के लिए अनफिट हैं ?
इसके अलावा आगामी चुनावों में मनमोहन सिंह की गौण हो चुकी भूमिका को सिन्हा के कथन के संदर्भ में देखा जाए तो कहीं यही वह वजह तो नहीं कि पार्टी उन्हें विरासत विहीन नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुकी है. इन दोनों सवालों का बेहतर जवाब यदि कोई दे सकता है तो निस्संदेह वह खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही होंगे. लेकिन वे ‘हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी..’ वाला शेर सुना कर बहुत पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका जवाब क्या होगा. इसके अलावा एक और तथ्य यह है कि अपने दस साला कार्यकाल में वे सिर्फ तीन बार ही औपचारिक रूप से मीडिया के सामने आए हैं. इस पर भी उनकी बातों का लब्बोलुआब यही रहा है कि उनका मूल्यांकन इतिहास करेगा. ऐसे में अगर इतिहास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कामों का मूल्यांकन कर भी दे और उन्हें सौ बटा सौ नंबर भी दे दे तब भी क्या वे कभी इस सवाल का सामना कर पाएंगे कि उनकी शख्सियत एक विरासत विहीन नेतृत्वकर्ता की नहीं थी.








