
16 मई को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के साथ-साथ देश भर में भाजपा की भारी जीत की धूम मचने लगी थी. कांग्रेस व वामपंथी दलों समेत कई क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी करारी हार के चलते चिंता में डूबे जा रहे थे. उधर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जद यू के नेताओं की टकटकी लोकसभा चुनाव परिणाम के समानांतर ही एक दूसरे नतीजे पर भी लगी हुई थी. दरअसल वह बिहार में पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों का भी दिन था. लोकसभा में जदयू की 20 सीटों का दो तक सिमट जाना ही नीतीश और उनकी पार्टी को निराशा की गर्त में भेजने के लिए काफी था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के परिणाम तो जले पर नमक छिड़कने जैसे हो गए. जदयू पांच सीटों में से सिर्फ एक पर जीत सकी. लोकसभा चुनाव में बदतर प्रदर्शन को लेकर जदयू का कोई नेता बोलने की स्थिति में नहीं था. भाजपा से अलगाव के बाद और लोकसभा चुनाव करीब आने के पहले दिल्ली में मोदी और बिहार के लिए नीतीश ही सबसे फिट हैं, का जो मिथ गढ़ा या रचा गया था वह इस आंधी में भरभराकर बिखर गया.
रही-सही कसर अपनों ने पूरी कर दी. कल तक नीतीश के करिश्मे और चमत्कार के सहारे ही मोदी से लड़कर जंग जीतने का दम भरने वाले जदयू नेताओं के बयान पलटने लगे. जदयू के एक धाकड़ विधायक ज्ञानू सिंह ने कहा, ‘नीतीश कुमार में आत्मबल की कमी है. उनका यही रवैया रहा तो अगले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की लुटिया डूबेगी.’ चुनाव में चुप्पी साधे रहनेवाले ज्ञानू सिंह आगे बोले, ‘पांच-पांच टिकट कुशवाहा, यादव और मुसलमानों को देने की क्या जरूरत थी? ज्यादा से ज्यादा बाहर से आये दलबदलुओं को टिकट देने की क्या जरूरत थी?’
ज्ञानू सिंह का यह कहना सिर्फ हार से उपजी पीड़ा भर नहीं थी बल्कि वे सीधे-सीधे नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ और रणनीति को चुनौती दे रहे थे. शाम तक अंदरखाने में यह बात तैरने लगी कि ज्ञानू सिंह ने नये अध्याय की शुरुआत कर दी है, अब इस अध्याय को बढ़ाने का सिलसिला कल से जारी होगा. जदयू से हाल में निकाले गए शिवानंद तिवारी जैसे नेता नसीहत देने लगे कि नीतीश को अब इस्तीफा दे देना चाहिए. नैतिकता के आधार पर नीतीश से इस्तीफा मांगनेवाले और लोग भी सामने आए. हवा में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की वह बात भी तैरने लगी जो उन्होंने कुछ दिनों पहले कही थी. मोदी ने कहा था कि जदयू के 50 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं.
16 मई को जब यह सब हो रहा था और तमाम बातें एक-दूसरे से टकरा रही थीं तो नीतीश कुमार मौन साधे हुए थे. जदयू के नेता उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन उनमें से कइयों को बैरंग लौटना पड़ रहा था. शाम होते-होते बातें होने लगीं कि नीतीश फिर कोई चौंकानेवाला फैसला लेंगे. अगले दिन 17 को वह समय भी आ गया जब शाम को अचानक खबर फैली कि नीतीश ने राजभवन को अपना इस्तीफा भेज दिया है. लेकिन साथ ही यह भी सामने आया कि उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की है. नीतीश कुमार ने संक्षिप्त प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि वे हार की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे रहे हैं. यह भी कि यह कदम सोच समझकर और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेने के बाद उठाया गया है. नीतीश कुमार अपनी ओर से अगर यह नहीं भी बताते तो भी सबको यह बात समझ में आ जाती कि उन्होंने यह फैसला सोच समझकर ही लिया होगा. सोचने समझने के लिए ही वे चुनाव परिणाम वाले दिन कोई प्रतिक्रिया देने, टिप्पणी करने या बयान देने से बचे होंगे. लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने का रास्ता क्यों चुना. क्या वाकई नैतिक आधार पर ही या मजबूरी में एक आखिरी दांव खेलकर वे एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं?
नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं. जानकारों के मुताबिक ऐसा फैसला करनेवाले नेता के तौर पर उन्हें माना जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा से अलग होने के जदयू के फैसले में सबसे अहम भूमिका उनकी ही थी. तब भी नीतीश कुमार जानते थे कि भाजपा से अलग होने और कांग्रेस का साथ नहीं मिलने के बाद उनकी स्थिति कमजोर होगी. इसके बावजूद उन्होंने तब यह फैसला लिया था. लेकिन 17 मई को नीतीश कुमार ने जिस तरह से अचानक इस्तीफे का ऐलान किया तो इसे लेकर तमाम तरह की बातें की जाने लगीं. मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की तो यह माना गया कि यह एक तीर से कई शिकार करने की चाल भी है.
नीतीश के सामने अगर सिर्फ लोकसभा में बुरी तरह से हार जाने का मामला होता तो शायद वे इस रास्ते को नहीं अपनाते. लेकिन वे कई तरफ से घिर रहे थे. विधानसभा उपचुनावों में भी बुरी तरह से हार जाना, हार के बाद तुरंत पार्टी नेताओं का विरोध में बयान आने लगना, विधानसभा में भी संख्या बल के लिहाज में रिस्क जोन में पहुंच जाना उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी करता दिख रहा था. बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. एक सीट खाली है. नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में फिलहाल 113 सीटें है. कांग्रेस के चार, भाकपा के एक और छह निर्दलीय विधायकों के सहारे उनकी सरकार चल रही है. कुल मिलाकर बहुमत बनाए और सरकार चलाए रखने के लिए उन्हें 122 सीटें चाहिए. वैसे तो नीतीश कुमार के पास 124 सीटें हैं. बहुमत से दो ज्यादा. लेकिन मुश्किल यह है कि अब उनका बुरा समय है तो निर्दलीय सरकार को बचाए रखने की कीमत तो वसूलने की कोशिश करेंगे ही. उधर, कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर पर अब तक के सबसे बुरे दौर में आ चुकी पार्टी है, किसी भी समय नीतीश से दामन छुड़ा सकती है. लोकसभा चुनाव तक तो कांग्रेस लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, दोनों को एक साथ साधती रही. दिल्ली की सत्ता के लिए उसने लालू का साथ लिया और बिहार में नीतीश की सरकार को भी समर्थन देकर बचाए रखा. बिहार में विधानसभा चुनाव भी अगले ही साल होनेवाला है, इसलिए जानकारों के मुताबिक कांग्रेस को तय करना होगा कि वह लालू और नीतीश में से किसका साथ लेगी या देगी. प्रदेश में 40 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में करीब 34 सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा से राजद ही लड़ाई में रहा. यानी राजद की स्थिति ठीक रही. इसलिए संभव है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीतीश की बजाय लालू के साथ ही जाए. उधर, सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति में भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का भविष्य अब कांग्रेस के ही आजू-बाजू जाकर सिमट गया है, भले ही कांग्रेस बुरे दौर में आ गई पार्टी हो.
जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार जानते हैं कि भाजपा या दूसरे दलों के खेल की बात तो बाद में आती है, अब उनके लिए अपने ही दल के नेताओं की बगावत झेलना या उनका खेल समझना इतना आसान नहीं होगा. इसलिए उन्होंने आखिरी दांव के तौर पर यह चाल चली और विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की. विश्लेषक कह रहे हैं कि ऐसा करके नीतीश कुमार ने शहादत भी दी और विकल्प भी अपने पाले में बचाए रखा. उन्होंने यही सोचकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की ताकि फिर उनके दल के नेता उनमें विश्वास जताएं और तब वे अपनी पार्टी के नेताओं को हिदायत दे सकें कि यदि उनके साथ, उनके नेतृत्व में चलना है तो फिर विधानसभा चुनाव तक उनके कहे अनुसार चलना होगा. नीतीश कुमार के लिए अब यह जरूरी हो गया था कि वे अपने विधायकों को एक साथ बिठाकर निकट भविष्य में बगावत के उभरनेवाले स्वर को अभी से ही दबाने की कोशिश करें. वरना खतरा जदयू विधायकों के ही विद्रोह से नेता के बदलने से लेकर उनके भाजपा के संग मिलकर नयी सरकार बना लेने तक का था. उनका यह दांव काम करता भी लग रहा है. खबर लिखे जाने तक कई विधायक और मंत्री इस फैसले के विरोध में मुख्यमंत्री निवास के बाहर जमा भी हो गए थे. एक ने तो नीतीश द्वारा इस्तीफा वापस न लिए जाने पर आत्मदाह की धमकी भी दे डाली.
नीतीश के सामने मुश्किलें और भी मोर्चों पर हैं. पिछले कई महीने से मंत्रिपरिषद की 12 सीटें खाली हैं. इतने विभागों का काम नीतीश अपने पास ही रखे हुए हैं और उन विभागों को आईएएस अधिकारी संचालित करते हैं. इससे जदयू नेताओं में नाराजगी पहले से ही है. नीतीश पर दबाव होगा कि वे मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द करें. उन्हें मजबूरी में यह विस्तार करना होगा. लेकिन इसकी अपनी मुश्किलें हैं. जदयू के विधायक पहले से उम्मीद लगाए बैठे हैं. निर्दलीय समर्थन देने के एवज में मलाईदार विभाग मांगेंगे. सौदेबाजी करेंगे. एक की सुनें तो दूसरा नाराज.
नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद हार के कारणों की समीक्षा की बजाय इतने सारे सवालों से पहले निपटना था. उनकी पार्टी अलग-थलग पड़ चुकी है. वे खुद भी अलग-थलग पड़ चुके हैं. ऐसे में नीतीश के सामने यही एक मजबूत वैकल्पिक रास्ता था कि वे इस्तीफा देकर एक साथ कई मसले सुलझा लें. यानी राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता के रास्ते चर्चा में आ जाएं. अपने दल का अंतर्कलह शांत कर लें. बागी-विरोधी नेताओं को साधकर फिर से अपनी पार्टी पर मजबूत पकड़ बना लें ताकि अगले साल होनेवाले विधानसभा चुनाव को भी अपनी रणनीति के साथ लड़ सकें.
नीतीश के इस्तीफे की वजह नैतिक रही या यह एक आखिरी दांव की तरह रहा, इसे तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक नीतीश खुद के पत्ते खुद ही न खोल दें. अगर वे फिर से पार्टी नेताओं के दबाव की दुहाई देकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो माना जाएगा कि यह नाखून कटाकर शहीद होने जैसा था. हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने साफ कर दिया है कि विधायक दल के नेता का चुनाव होगा. लेकिन नीतीश के इस्तीफे का एक मतलब यह भी है कि वे चाहते हैं कि भाजपा आनन-फानन में कोई खेल करे ताकि वे अभी से ही जनता की अदालत में चले जाएं और सबको समझाएं कि आप तय कीजिए कि बिहार में कौन चाहिए! लेकिन भाजपा भी अभी इस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती. पार्टी विधायक दल के नेता नंदकिशोर यादव कहते हैं, ‘नीतीश कुमार ने अपने दल के अंदर के विद्रोह को दबाने की कोशिश में इस्तीफा दिया है. इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है.’ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय कहते हैं, ‘यह इस्तीफा एक नाटक है. नीतीश कुमार अपने काम के आधार पर ही लोकसभा चुनाव में वोट मांग रहे थे, लोगों ने उनके काम को नकार दिया, वोट नहीं दिया तो उन्हें मुकम्मल इस्तीफा देना चाहिए था. आगे क्या होगा, आगे की बात है.’



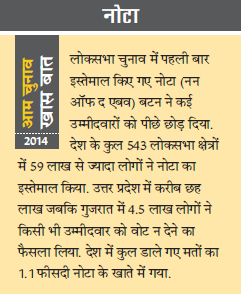 आप के अंदरूनी लोगों से बातचीत में जो बात सामने आती है उसके मुताबिक आज भले ही लोग इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने को गलत बता रहे हों लेकिन जब यह फैसला लिया गया था उस समय इतने ही लोग इसके पक्ष में भी थे. एक आकलन यह था कि जनता में आप को लेकर एक सकारात्मक माहौल है, अगले लोकसभा चुनाव पांच साल बाद होंगे तो क्यों न इस सकारात्मक माहौल का फायदा उठा लिया जाए. एक राजनीतिक दल के लिहाज से ऐसा सोचना गलत भी नहीं था.
आप के अंदरूनी लोगों से बातचीत में जो बात सामने आती है उसके मुताबिक आज भले ही लोग इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने को गलत बता रहे हों लेकिन जब यह फैसला लिया गया था उस समय इतने ही लोग इसके पक्ष में भी थे. एक आकलन यह था कि जनता में आप को लेकर एक सकारात्मक माहौल है, अगले लोकसभा चुनाव पांच साल बाद होंगे तो क्यों न इस सकारात्मक माहौल का फायदा उठा लिया जाए. एक राजनीतिक दल के लिहाज से ऐसा सोचना गलत भी नहीं था. इस लोकसभा चुनाव के लिए यह रिकॉर्ड ही कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आधे दर्जन राज्यों की सभी सीटें जीती हैं. इसमें भी विशेष बात है कि राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और गोवा की इन सभी सीटों पर उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला था, यानी चुनाव में यहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया. इन राज्यों में यदि गुजरात को छोड़ दें तो भाजपा की जीत से फिलहाल कांग्रेस से जुड़े कोई दीर्घकालिक नतीजे नहीं निकाले जा सकते. लेकिन इसके साथ देश में दो राज्य ऐसे भी हैं जहां कहने के लिए तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ नहीं हुआ लेकिन बीते एक दशक में वह ऐसी हालत में पहुंच चुकी है जहां से उसकी वापसी दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही है. हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की. इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को क्रमश: दो और एक सीट मिली है.
इस लोकसभा चुनाव के लिए यह रिकॉर्ड ही कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आधे दर्जन राज्यों की सभी सीटें जीती हैं. इसमें भी विशेष बात है कि राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और गोवा की इन सभी सीटों पर उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला था, यानी चुनाव में यहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया. इन राज्यों में यदि गुजरात को छोड़ दें तो भाजपा की जीत से फिलहाल कांग्रेस से जुड़े कोई दीर्घकालिक नतीजे नहीं निकाले जा सकते. लेकिन इसके साथ देश में दो राज्य ऐसे भी हैं जहां कहने के लिए तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ नहीं हुआ लेकिन बीते एक दशक में वह ऐसी हालत में पहुंच चुकी है जहां से उसकी वापसी दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही है. हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की. इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को क्रमश: दो और एक सीट मिली है.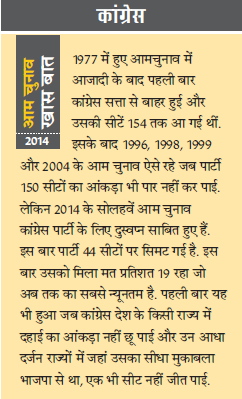 नेतृत्व का अभाव
नेतृत्व का अभाव
 लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तराखंड के राजनीतिक आकाश में अस्थिरता के बादल मंडराने लगे हैं. प्रदेश की पांचों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार का भविष्य कितना सुरक्षित होगा, इसको लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. जीत से लबरेज भाजपाइयों की मानें तो पार्टी को मिली शानदार जीत हरीश रावत सरकार की उल्टी गिनती का आधार तैयार कर चुकी है. सियासी हलकों में इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि तमाम गुटों में बंटे कांग्रेसी विधायक कहीं सरकार को झटका तो नहीं देने वाले हैं? इसके अलावा सरकार में शामिल निर्दलीय और बसपा विधायकों के रुख पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं. इस सबके बीच लोकसभा चुनावों से ऐन पहले भाजपा में शामिल होने वाले आध्यात्मिक गुरु और पूर्व कांग्रेसी सतपाल महाराज ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए हरीश रावत से इस्तीफे की मांग तक कर दी है. उनका कहना था, ‘हरीश रावत ने लोक सभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की कीमत पर ही विजय बहुगुणा से सीट हथियाई थी लिहाजा उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.’ हालांकि जानकारों की एक बड़ी जमात सतपाल की इस मांग को उनके सीएम बनने की छटपटाहट का नतीजा मान रही है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि हरीश रावत सरकार पर खतरे की जो चर्चाएं चल रही हैं यदि वे निकट भविष्य में हकीकत में तब्दील होती हैं तो इसमें महाराज की भूमिका बहुत निर्णायक हो सकती है.
लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तराखंड के राजनीतिक आकाश में अस्थिरता के बादल मंडराने लगे हैं. प्रदेश की पांचों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार का भविष्य कितना सुरक्षित होगा, इसको लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. जीत से लबरेज भाजपाइयों की मानें तो पार्टी को मिली शानदार जीत हरीश रावत सरकार की उल्टी गिनती का आधार तैयार कर चुकी है. सियासी हलकों में इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि तमाम गुटों में बंटे कांग्रेसी विधायक कहीं सरकार को झटका तो नहीं देने वाले हैं? इसके अलावा सरकार में शामिल निर्दलीय और बसपा विधायकों के रुख पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं. इस सबके बीच लोकसभा चुनावों से ऐन पहले भाजपा में शामिल होने वाले आध्यात्मिक गुरु और पूर्व कांग्रेसी सतपाल महाराज ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए हरीश रावत से इस्तीफे की मांग तक कर दी है. उनका कहना था, ‘हरीश रावत ने लोक सभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की कीमत पर ही विजय बहुगुणा से सीट हथियाई थी लिहाजा उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.’ हालांकि जानकारों की एक बड़ी जमात सतपाल की इस मांग को उनके सीएम बनने की छटपटाहट का नतीजा मान रही है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि हरीश रावत सरकार पर खतरे की जो चर्चाएं चल रही हैं यदि वे निकट भविष्य में हकीकत में तब्दील होती हैं तो इसमें महाराज की भूमिका बहुत निर्णायक हो सकती है.
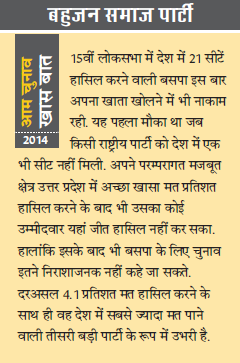 लेकिन विधायकों के सत्ता की तरफ झुकाव के इन दो उदाहरणों के बीच राजीव नयन बहुगुणा एक और बात भी कहते हैं, ‘राजनीतिक कौशल के मोर्चे पर सतपाल महाराज के मुकाबले हरीश रावत ज्यादा सक्षम नेता माने जाते हैं, और बहुत संभव है कि महाराज की पत्नी को छोड़ उनके खेमे के बाकी विधायकों को वे आसानी से अपने पाले में खींच लेंगे.’ वे सवालिया अंदाज में कहते हैं, ‘दशक भर तक सर-पैर पटकने के बाद सीएम की कुर्सी पाने वाले हरीश रावत क्या इतनी आसानी से हथियार डाल देंगें?’
लेकिन विधायकों के सत्ता की तरफ झुकाव के इन दो उदाहरणों के बीच राजीव नयन बहुगुणा एक और बात भी कहते हैं, ‘राजनीतिक कौशल के मोर्चे पर सतपाल महाराज के मुकाबले हरीश रावत ज्यादा सक्षम नेता माने जाते हैं, और बहुत संभव है कि महाराज की पत्नी को छोड़ उनके खेमे के बाकी विधायकों को वे आसानी से अपने पाले में खींच लेंगे.’ वे सवालिया अंदाज में कहते हैं, ‘दशक भर तक सर-पैर पटकने के बाद सीएम की कुर्सी पाने वाले हरीश रावत क्या इतनी आसानी से हथियार डाल देंगें?’
 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी और भाजपा/एनडीए कई रिकॉर्ड बनाते हुए जीत गए हैं. हालांकि मोदी की इस जीत के पीछे कई कारक और कारण हैं. लेकिन इस जीत में मोदी की सुनियोजित तरीके से गढ़ी हुई ‘लार्जर दैन लाइफ’ छवि और उसकी जबरदस्त मार्केटिंग की बड़ी भूमिका है. इसे अनदेखा करना मुश्किल है कि गुजरात दंगों और फर्जी मुठभेड़ों से लेकर एक महिला की जासूसी करवाने और चहेते कॉरपोरेट समूहों को लाभ पहुंचाने जैसे विवादों और आरोपों से घिरे रहने के बावजूद कॉरपोरेट मीडिया-पीआर-विज्ञापन कॉम्प्लेक्स ने मोदी की एक ‘सख्त, प्रभावी और सफल प्रशासक और विकासपुरुष’ की छवि निर्मित करने और फिर उसे मतदाताओं को सफलतापूर्वक बेचने में कामयाबी हासिल की है.
2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी और भाजपा/एनडीए कई रिकॉर्ड बनाते हुए जीत गए हैं. हालांकि मोदी की इस जीत के पीछे कई कारक और कारण हैं. लेकिन इस जीत में मोदी की सुनियोजित तरीके से गढ़ी हुई ‘लार्जर दैन लाइफ’ छवि और उसकी जबरदस्त मार्केटिंग की बड़ी भूमिका है. इसे अनदेखा करना मुश्किल है कि गुजरात दंगों और फर्जी मुठभेड़ों से लेकर एक महिला की जासूसी करवाने और चहेते कॉरपोरेट समूहों को लाभ पहुंचाने जैसे विवादों और आरोपों से घिरे रहने के बावजूद कॉरपोरेट मीडिया-पीआर-विज्ञापन कॉम्प्लेक्स ने मोदी की एक ‘सख्त, प्रभावी और सफल प्रशासक और विकासपुरुष’ की छवि निर्मित करने और फिर उसे मतदाताओं को सफलतापूर्वक बेचने में कामयाबी हासिल की है.

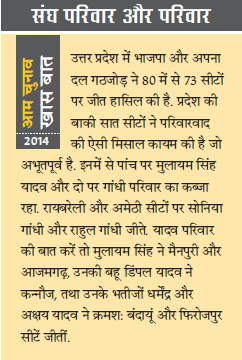 लेकिन एक बार जब यह संतुलन टूटता है तो चीजें जैसे बिखर जाती हैं. 2008 की वैश्विक मंदी का असर 2009 के भारत पर पड़ता है और हम पाते हैं कि अचानक औद्योगिक वृद्धि दर नीचे जा चुकी है, शेयर बाजार गोते खा रहा है, कंपनियां नई परियोजनाएं बंद कर रही हैं और नौजवानों की बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है. अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री इस मोड़ पर बेबस है. इसी दौर में सरकार के द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून के मार्फत अचानक कई पुरानी फाइलें खुलनी शुरू होती हैं और टू जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदानों के आवंटन जैसे मामले मनमोहन सरकार की ईमानदारी का मुंह चिढ़ाने लगते हैं. कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारी में हुई गड़बड़ी और आदर्श घोटाले जैसे मूलतः राज्य केंद्रित मुद्दे भी अंततः मनमोहन सरकार की अलोकप्रियता में इजाफा करते हैं. इसी समय आर्थिक मंदी से बिलबिलाया उद्योग जगत अपने लिए तरह-तरह की राहतें मांग रहा है और न मिलने पर सरकार पर नीतियों की अपाहिजता का आरोप लगा रहा है. और यही दौर है जब लोकतंत्र के दूसरे प्रहरियों में एक हमारी न्यायपालिका के दबाव में कई मामलों की जांच शुरू हो रही है और मनमोहन सरकार के मंत्री और अफसर जेल के पीछे दिखाई पड़ रहे हैं. इस ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में सिर्फ महंगाई दर बढ़ रही है और जो मध्यवर्ग इसी दौरान पहले छोटी और फिर बड़ी गाड़ियां खरीदता रहा, वह पेट्रोल से प्याज तक के दाम बढ़ने पर नाराज है.
लेकिन एक बार जब यह संतुलन टूटता है तो चीजें जैसे बिखर जाती हैं. 2008 की वैश्विक मंदी का असर 2009 के भारत पर पड़ता है और हम पाते हैं कि अचानक औद्योगिक वृद्धि दर नीचे जा चुकी है, शेयर बाजार गोते खा रहा है, कंपनियां नई परियोजनाएं बंद कर रही हैं और नौजवानों की बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है. अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री इस मोड़ पर बेबस है. इसी दौर में सरकार के द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून के मार्फत अचानक कई पुरानी फाइलें खुलनी शुरू होती हैं और टू जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदानों के आवंटन जैसे मामले मनमोहन सरकार की ईमानदारी का मुंह चिढ़ाने लगते हैं. कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारी में हुई गड़बड़ी और आदर्श घोटाले जैसे मूलतः राज्य केंद्रित मुद्दे भी अंततः मनमोहन सरकार की अलोकप्रियता में इजाफा करते हैं. इसी समय आर्थिक मंदी से बिलबिलाया उद्योग जगत अपने लिए तरह-तरह की राहतें मांग रहा है और न मिलने पर सरकार पर नीतियों की अपाहिजता का आरोप लगा रहा है. और यही दौर है जब लोकतंत्र के दूसरे प्रहरियों में एक हमारी न्यायपालिका के दबाव में कई मामलों की जांच शुरू हो रही है और मनमोहन सरकार के मंत्री और अफसर जेल के पीछे दिखाई पड़ रहे हैं. इस ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में सिर्फ महंगाई दर बढ़ रही है और जो मध्यवर्ग इसी दौरान पहले छोटी और फिर बड़ी गाड़ियां खरीदता रहा, वह पेट्रोल से प्याज तक के दाम बढ़ने पर नाराज है.
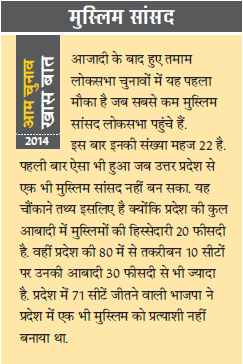 बसपा के लिए तो लोकसभा चुनाव एक भयानक स्वप्न ही बन गए हैं. मायावती के अति आत्मविश्वास को चुनाव नतीजों ने बुरी तरह झकझोर दिया है. पार्टी के लिए यह हार इसलिए भी खतरनाक संकेत है क्योंकि पार्टी की यह लगातार दूसरी बड़ी हार है. बसपा के लिए विधानसभा की पराजय का अवसाद अभी खत्म भी नहीं हो पाया था कि यह नई और भीषण पराजय सामने आ गई है. इस हार ने लगातार अकेली पड़ती जा रही मायावती को और अकेला बना दिया है. इससे मायावती की कथित सोशल इंजीनियरिंग की तो भद्द पिटी ही है. मायावती का भरोसेमंद वोट बैंक भी बिखरता हुआ दिखाई देने लगा है. हालांकि चुनाव के अंतिम दौर में मायावती को इस बात का अंदेशा हो गया था और इसीलिए उन दिनों वे लगातार लखनऊ मंे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने वोटरों को सचेत करने की कोशिश करने में लगी थीं. मगर न उनकी अपील से दलित मुस्लिम गठजोड़ कायम रह सका और न ही उनका खुद का अपना वोट बैंक. मायावती अब इस सबके लिए भले ही भाजपा और उनके नेताओं के ‘शैतानी भरे हथकंडों’ को दोषी ठहराएं, भले ही दलितों के हिंदू होने पर यह कह कर सवाल उठाएं कि दलितों ने तो बाबा साहब के नेतृत्व में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और भले ही यह कह कर सफाई दें कि उनका वोट बैंक जस का तस है, लेकिन यह तय है कि मायावती के लिए आगे की राह बहुत आसान नहीं रह गई है. दलित मतदाताओं के बीच तो विश्वास का संकट कायम है. मुस्लिम मतदाताओं के लिए वे खुद कह रही हैं कि वे पहले गलती करते हैं फिर पछताते हैं और ऐसी ही कुछ धारणा अपर कास्ट के बारे में भी उनकी है कि वे भी वोट देते वक्त बहक जाते है. इसलिए अगले विधानसभा चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा होने जा रहे हैं. मायावती किस तरह की तैयारी करके अपनी आगे की राह बनाती हंै, यही बात उनका भविष्य तय करेगी.
बसपा के लिए तो लोकसभा चुनाव एक भयानक स्वप्न ही बन गए हैं. मायावती के अति आत्मविश्वास को चुनाव नतीजों ने बुरी तरह झकझोर दिया है. पार्टी के लिए यह हार इसलिए भी खतरनाक संकेत है क्योंकि पार्टी की यह लगातार दूसरी बड़ी हार है. बसपा के लिए विधानसभा की पराजय का अवसाद अभी खत्म भी नहीं हो पाया था कि यह नई और भीषण पराजय सामने आ गई है. इस हार ने लगातार अकेली पड़ती जा रही मायावती को और अकेला बना दिया है. इससे मायावती की कथित सोशल इंजीनियरिंग की तो भद्द पिटी ही है. मायावती का भरोसेमंद वोट बैंक भी बिखरता हुआ दिखाई देने लगा है. हालांकि चुनाव के अंतिम दौर में मायावती को इस बात का अंदेशा हो गया था और इसीलिए उन दिनों वे लगातार लखनऊ मंे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने वोटरों को सचेत करने की कोशिश करने में लगी थीं. मगर न उनकी अपील से दलित मुस्लिम गठजोड़ कायम रह सका और न ही उनका खुद का अपना वोट बैंक. मायावती अब इस सबके लिए भले ही भाजपा और उनके नेताओं के ‘शैतानी भरे हथकंडों’ को दोषी ठहराएं, भले ही दलितों के हिंदू होने पर यह कह कर सवाल उठाएं कि दलितों ने तो बाबा साहब के नेतृत्व में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और भले ही यह कह कर सफाई दें कि उनका वोट बैंक जस का तस है, लेकिन यह तय है कि मायावती के लिए आगे की राह बहुत आसान नहीं रह गई है. दलित मतदाताओं के बीच तो विश्वास का संकट कायम है. मुस्लिम मतदाताओं के लिए वे खुद कह रही हैं कि वे पहले गलती करते हैं फिर पछताते हैं और ऐसी ही कुछ धारणा अपर कास्ट के बारे में भी उनकी है कि वे भी वोट देते वक्त बहक जाते है. इसलिए अगले विधानसभा चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा होने जा रहे हैं. मायावती किस तरह की तैयारी करके अपनी आगे की राह बनाती हंै, यही बात उनका भविष्य तय करेगी.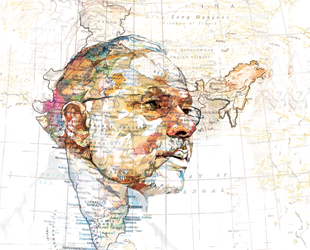


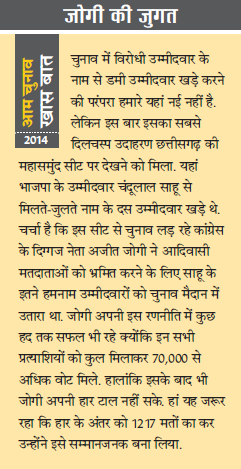 यह जरूर था कि मोदी का प्रधानमंत्री के लिए नाम उछलने पर संघ नेतृत्व अपने गुजरात अनुभव के कारण सशंकित था. लेकिन बाद में चौतरफा बने माहौल और कैडरों के दबाव में उसे मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार करना पड़ा. इसके बाद से चुनाव अभियान के आखिरी दिन तक संघ के स्वंयसेवक मोदी को पीएम बनाने के लिए देश भर में प्रचार करते रहे. संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं, ‘संघ के हमारे स्वंयसेवकों ने गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से मोदी जी के लिए वोट मांगा है. संघ जितना सक्रिय इस चुनाव में था उतना कभी नहीं रहा. इस बात को मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं.’
यह जरूर था कि मोदी का प्रधानमंत्री के लिए नाम उछलने पर संघ नेतृत्व अपने गुजरात अनुभव के कारण सशंकित था. लेकिन बाद में चौतरफा बने माहौल और कैडरों के दबाव में उसे मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार करना पड़ा. इसके बाद से चुनाव अभियान के आखिरी दिन तक संघ के स्वंयसेवक मोदी को पीएम बनाने के लिए देश भर में प्रचार करते रहे. संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं, ‘संघ के हमारे स्वंयसेवकों ने गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से मोदी जी के लिए वोट मांगा है. संघ जितना सक्रिय इस चुनाव में था उतना कभी नहीं रहा. इस बात को मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं.’





