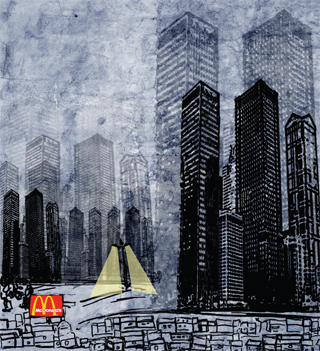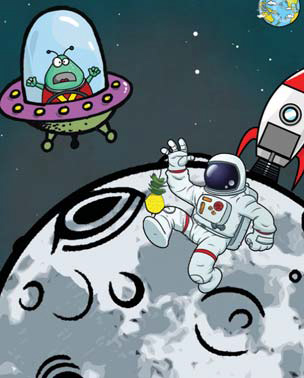मेरा बचपन मेरठ में गुजरा. मेरे पिता कवि थे और एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे. सिनेमा ही हमारे मनोरंजन का इकलौता साधन था. बचपन की देखी फिल्में याद करूं तो मुझे ‘परदे के पीछे’ याद आती है. उसमें विनोद मेहरा और नंदा थे. लेकिन फिल्मों में असली रुचि ‘शोले’ से जगी. तब हम पांचवीं-छठी कक्षा में पढ़ते थे. उसके बाद तो अमिताभ बच्चन के ऐसे दीवाने हुए कि उनकी ‘अमर अकबर एंथनी’, ‘नसीब’, ‘सुहाग’, हर फिल्म देखी. ऐसी फिल्में ही हम देखते थे. इन फिल्मों ने ही असर डालना शुरू किया. श्याम बेनेगल की एक-दो फिल्में भी देखी थीं. कॉलेज में आते-आते ‘उत्सव’ और ‘कलयुग’ आ गई थीं. उस दौर की फिल्म ‘विजेता’ याद है. ज्यादातर फिल्में दोस्तों के साथ देखीं. फिल्मों में इंटरेस्ट था, लेकिन मैं इतना सीरियस दर्शक नहीं था. सच कहूं तो बहुत बाद में म्यूजिक डायरेक्टर बन जाने के बाद भी फिल्मों और डायरेक्शन का खयाल नहीं आया था.
मेरे पिता जी ने मुंबई आकर फिल्मों के लिए कुछ गाने भी लिखे. उनकी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल से दोस्ती थी. मेरे पिता जी का नाम राम भारद्वाज हुआ. वे शौकिया तौर पर गाने लिखते थे. वे छुट्टी लेकर मुंबई आते. बाद में उन्होंने बिजनेस में आने की भी कोशिश की. फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में उतरे, लेकिन नाकाम रहे. उस वजह से घर कर्ज में आ गया. मेरा तो तब संगीत का भी इरादा नहीं था. मैं क्रिकेट खेलता था और उसी में आगे बढ़ना चाहता था. तब मैं स्कूल की टीम में खेलता था और उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी भी गया था. दिल्ली आने पर एक दोस्त की वजह से संगीत में दिलचस्पी हुई. मेरी दिलचस्पी थी संगीत में, लेकिन संगीतकार बनने के बारे में नहीं सोचा था. यह इंटरेस्ट बाद में इतना सीरियस हो गया कि क्रिकेट छूट गया.
उन दिनों गजलों का दौर था. हम सभी गजल गाते थे. एक दोस्त पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के जानकार थे. उनके साथ रहने से पश्चिमी संगीत का ज्ञान बढ़ा. मैंने ‘पेन म्यूजिक’ रिकॉर्डिंग कंपनी ज्वाइन कर ली. उसी जॉब में ट्रांसफर लेकर मुंबई आ गया. एक-डेढ़ साल यहां स्ट्रगल किया. तभी दिल्ली में गुलजार साहब से मुलाकात हुई. दरअसल मैं लंबे अरसे से उनसे मिलना चाहता था. उसके लिए युक्ति की थी. उन्होंने हौसला बढ़ाया और पीठ पर हाथ रखा. गुलजार भाई की वजह से ही मैं कुछ बन पाया. वे मेरे पिता की तरह हैं. उन्हीं के साथ ‘चड्डी पहन के फूल खिला है’ गीत की रिकॉर्डिंग की. उसके बाद ‘माचिस’ का ऑफर मिला और मैं फिल्मों के लिए संगीत बनाने लगा.
अवसर कब आपके सामने आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. आपको हमेशा अपनी क्रिएटिविटी की बंदूक लोड करके रखनी होगी
सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था. लोग मेरे काम को पसंद भी कर रहे थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में स्पॉट ब्वॉय से लेकर प्रोड्यूसर तक के मन में डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश रहती है. मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदुस्तान में फिल्म और क्रिकेट दो ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में हर किसी को लगता है कि उससे बेहतर कोई नहीं जानता. सचिन को ऐसा शॉट खेलना चाहिए और डायरेक्टर को ऐसे शॉट लेना चाहिए. हर एक के पास अपनी एक कहानी रहती है. रही मेरी बात तो संगीतकार के तौर पर जगह बनाने के बाद मैं फिल्मों की स्क्रिप्ट पर निर्देशकों से बातें करने लगा था. स्क्रिप्ट समझने के बाद ही आप बेहतर संगीत दे सकते हैं. स्क्रिप्ट सेशन में निर्देशकों से ज्यादा सवाल करने लगा था. उन बैठकों से मुझे लगा कि जिस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, उससे बेहतर मैं कर सकता हूं. इसी दरम्यान संगीत निर्देशन के लिए फिल्मों का मिलना कम हो गया तो लगा कि इस रफ्तार से तो दो साल के बाद मेरे लिए काम ही नहीं रहेगा. मेरा काम और एटीट्यूड भी आड़े आ रहा था. उन्ही दिनों संयोग से मुंबई में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ. तब यह देश के विभिन्न शहरों में हुआ करता था. गुलजार साहब की वजह से मैं फेस्टिवल देखने गया. वे अपने साथ ले जाते थे. उस फेस्टिवल में किस्लोवस्की की फिल्म ‘रैड’, ‘ब्लू’ और ‘व्हाइट’ देखी. उसे देखने के बाद झटका लगा. एहसास हुआ कि फिल्में तो ऐसी ही होनी चाहिए. अगले साल त्रिवेंद्रम में किस्लोवस्की की ‘डे के लॉग’ देखी. उसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया. मुझे लगा कि सिनेमा इतनी बड़ी मानवीय अभिव्यक्ति है. उससे पहले सिनेमा मेरे लिए सिर्फ मनोरंजन था. सिनेमा का वास्तविक असर उस फिल्म को देखने के बाद ही हुआ. उसके बाद मैंने फिल्म फेस्टिवल मिस नहीं किए. फेस्टिवल की फिल्में देख-देख कर फिल्मों के बारे में जाना और समझा. फिल्म फेस्टिवल ही मेरा फिल्म स्कूल रहा.
उससे पहले जो सिनेमा देखा था, उसे और उसके असर को भूला (अनलर्न) तो नहीं जा सकता. हमारे अवचेतन में सारे अनुभव जमा हो जाते हैं, लेकिन सही में सिनेमा की शक्ति, अभिव्यक्ति और मीडियम की समझ फेस्टिवल की फिल्मों के बाद ही आई. बहुत बड़ा कंट्रास्ट था. उन फिल्मों ने हिला कर रख दिया कि फिल्में इस तरह से भी असर कर सकती हैं. हमारी कमर्शियल फिल्में मुख्य रूप से मनोरंजन होती हैं. विषय और प्रभाव के स्तर पर वे सतह पर ही रहती हैं. जबकि अच्छी फिल्में तो सीने में कुछ जोड़ देती हैं. सत्यजित राय की फिल्में देखीं. उनकी ‘चारुलता’ कई बार देखी. इतने बड़े फिल्मकार को लोगों ने बदनाम कर दिया कि वे केवल गरीबी बेचते हैं. हिंदुस्तान में अगर गरीबी है तो क्यों नहीं दिखायी जाए? हमें गरीबी पर शर्म नहीं आती, उन पर बनी फिल्मों पर आती है. उन्होंने 40-50 साल पहले जैसी फिल्में बनाईं, वैसी फिल्में आज भी फिल्ममेकर नहीं बना पा रहे हैं. उनकी ‘चारुलता’ की छवियां ‘देवदास’ की ऐश्वर्या राय में दिखती हैं.

इन सब फिल्मकारों के असर और अपने भीतर की बेचैनी में मैंने निर्देशन पर किताबें पढ़नी शुरू कर दीं. खासकर ‘आर्ट ऑफ रोमांटिक राइटिंग’ का बहुत असर हुआ. उन दिनों जीटीवी के लोग ‘गुब्बारे’ के संगीत के लिए मेरे पास आए. मैंने एक शर्त रखी कि मैं आपका म्यूजिक कर दूंगा लेकिन आप मुझे एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए दो. एक तरह से उन्हें ब्लैकमेल किया और मुझे दो शॉर्ट फिल्में मिल गईं. उन फिल्मों को करने के बाद लगा कि मैं कितना खराब लेखक हूं. सबसे पहले मुझे लिखना सीखना होगा.
उत्तराखंड का मेरा एक दोस्त प्रेम कहानियों की एक सीरीज कर रहा था. मैंने उसे दो और कहानियों के बीच अपनी कहानी रख कर दे दी. उसे कहानी पसंद आई तो फिर स्क्रीनप्ले और संवाद मैंने ही लिखे. फिर भी लगा कि लेखन पर पढ़ना जरूरी है. बहुत पढ़ने के बाद नए विषय की खोज में निकला. अब्बास टायरवाला के पास एक थ्रिलर कहानी थी ‘मेहमान’. मैं मनोज बाजपेयी से मिला. वह मेरा दोस्त था. उसे बड़ी रेगुलर टाइप की कहानी लगी. उस वक्त मेरे पास हिंदुस्तान-पाकिस्तान के दो सैनिकों की एक कहानी थी. उन्होंने कहा कि इस पर काम करते हैं. वे फिल्म के लिए राजी हो गए. इसी बीच रॉबिन भट्ट ने मुझे अजय देवगन से मिलवा दिया. उन्हें कहानी पसंद आ गई और वे फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए. फिल्म के गाने रिकॉर्ड हो गए, एक्टर साइन हो गए और लोकेशंस देखी जाने लगीं. मगर इस बीच उनकी ‘राजू चाचा’ फ्लॉप हो गई. एक महीने बाद मेरी फिल्म की शूटिंग थी, लेकिन वह ठप हो गई. उस फिल्म की स्क्रिप्ट और गानों पर मैंने एक साल से अधिक समय तक काम किया था.
हमारे यहां एक अजीब-सा सिस्टम है जिसमें सबके लिए जगह है. ‘इश्किया’ भी हिट होती है और ‘वो आती जवानी रात में’ भी चलती है
उसके बाद मैंने हर डायरेक्टर को कहानी सुनाई. एक्टर कहानी सुनने के नाम पर भाग जाते थे और प्रोड्यूसर मेरी कहानी समझ नहीं पाते थे. मुंबई में ज्यादातर प्रोड्यूसर को नाम समझ में आता है, काम समझ में नहीं आता है. एक साल की कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैं चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी गया. वहां ‘मकड़ी’ की स्क्रिप्ट जमा की. वह उन्हें पसंद आ गई. वह स्क्रिप्ट मजबूरी में मैंने स्वयं लिखी थी. तब मेरे दोस्त अब्बास टायरवाला व्यस्त थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी लेखक को दूं.
‘मकड़ी’ के साथ दूसरे किस्म का हादसा हुआ. फिल्म बन जाने के बाद सोसायटी ने फिल्म रिजेक्ट कर दी. कहा, बहुत ही खराब फिल्म है. मैंने गुलजार साहब और दोस्तों को दिखाई. सभी को फिल्म अच्छी लगी. मैंने फिल्म को स्वयं रिलीज करने का फैसला किया. दोस्तों से पैसे उधार लेकर चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी के पैसे वापस किए. उन दिनों मल्टीप्लेक्स शुरू हो रहे थे. मेरी फिल्म डेढ़ घंटे की थी. ऐसी फिल्म के लिए कोई स्लॉट नहीं था. उसे बेचने और रिलीज करने में नानी याद आ गई. लेकिन ‘मकड़ी’ रिलीज होने के बाद कल्ट फिल्म बन गई और मेरा सफर शुरू हुआ.
यूं तो ‘मकड़ी’ और ‘मकबूल’ भी जैसी मैं चाहता था, वैसी ही बनीं लेकिन उनके बाद अड़चनें कम हो गईं. ‘मकड़ी’ के बारे में ज्यादातर लोग मानते हैं कि वह बच्चों की फिल्म है. ‘मकड़ी’ में मुझे 12 लाख का नुकसान हुआ था. ‘मकबूल’ के साथ मामला अलग हुआ. उसे बनाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे. एक्टर भी तैयार नहीं हो रहे थे. मैंने तब एनएफडीसी भी संपर्क किया तो उन्हें फिल्म का बजट ज्यादा लगा. मैंने बैंक लोन की कोशिश की तो वह अटका रहा. तभी संयोग से बॉबी बेदी से मुलाकात हो गई. बॉबी बेदी उस फिल्म के निर्माण के लिए तैयार हो गए. उन्होंने कहा कि फिल्म का बजट ज्यादा है, लाभ हुआ तभी तुम्हें पैसे दूंगा. इस तरह मैंने फ्री में ही काम किया. इस फिल्म से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ, लेकिन फिल्म पसंद आई और मुझे पांव टिकाने की जगह मिल गई. डायरेक्टर के तौर पर मुझे स्वीकार कर लिया गया. उस फिल्म की वजह से मुझे आमिर खान ने बुलाया. हालांकि वह फिल्म नहीं बन पाई. उसके बाद ‘ओमकारा’ में मेरे साथ सारे एक्टर काम करना चाहते थे.
अब तक मेरी समझ में आ गया था कि यह माध्यम निर्देशक का ही है. निर्देशक गलत भी बोल रहा हो तो सभी को बात माननी पड़ेगी. साथ ही यह भी लगा कि फिल्म मेकिंग से बड़ा कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं है. यह सारे फाईन आर्ट्स का समागम है. इसमें संगीत, कविता, नाटक, सब कुछ है. फिल्ममेकर होने पर सर्जक की फीलिंग आ जाती है. हां, कभी-कभी तानाशाह भी बनना पड़ता है, लेकिन कभी-कभी बच्चे की तरह सुनना भी पड़ता है. निर्देशक को हर तरह की सलाह और विचार के लिए खुला रहना होता है. आप अपने फैसलों पर दृढ़ रहें, लेकिन अहंकार और डिक्टेटरशिप आ गई तो आपके हाथ से कमान छूट भी सकती है.
लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था. मुझे भी जल्दी अवसर नहीं मिला. लंबा संघर्ष करना पड़ा. एक बात गुलजार साहब ने समझाई थी कि अवसर टारगेट की तरह होते हैं. वह कब आपके सामने आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. आपको हमेशा अपनी क्रिएटिविटी की बंदूक लोड करके रखनी होगी. अगर आप यह सोचते हैं कि अवसर आएगा तो गन साफ करके, गोली भरकर, फिर फायर करेंगे तो टारगेट निकल जाएगा. इसलिए हमेशा तैयार रहना होगा और धैर्य भी बनाए रखना होगा.
संघर्ष लंबा तो था लेकिन मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बाहर से आने वाले लोगों के जितने विरोधी हैं, उससे ज्यादा समर्थक हैं. मैं अपनी ही फिल्मों की बात करूं तो अब मेरी ऐसी कमाल की जगह बन गई है कि मुझे हिट या फ्लॉप की चिंता नहीं रहती. अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है. सच तो बाहर आ ही जाता है. यह नैचुरल प्रोसेस है. यह सभी के साथ होगा, इसलिए बगैर घबराए ईमानदारी से अपनी सोच पर काम करने की जरूरत है. अगर सभी लोग सड़क पर चल रहे हों और आप निकल कर कच्चे रास्ते पर आ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि उल्लू का पट्ठा है. वे आपको खींच कर सड़क पर लाने की कोशिश करेंगे. उन्हें डर रहेगा कि कच्चे रास्ते से ही कहीं यह आगे न निकल जाए. वे चाहेंगे कि हम उनकी चाल में आ जाएं. लेकिन मेरे लिए तो अपना चुना कच्चा रास्ता ही ज्यादा अच्छा है.
लेकिन इस कच्चे का अर्थ डार्क फिल्म नहीं था. यह संयोग से ही हुआ कि मेरी फिल्में डार्क होती हैं. बस लोगों को पसंद आ गईं फिल्में. मुझे मानव मस्तिष्क में चल रही खुराफातें आकर्षित करती हैं. इंसानी दिमाग की अंधेरी तरफ जबरदस्त ड्रामा रहता है. हमलोग सिनेमा में उसे दिखाने से बचते हैं. हम लोग डील ही नहीं कर पाते. मुझे लगता है कि इस पर काम करना चाहिए. अगर ‘मैकबेथ’ और ‘ओथेलो’ चार सौ साल से लोकप्रिय है तो उसकी अपील का असर समझ सकते हैं. सच कहूं तो मैं तो कॉमेडी फिल्म बनाने की पूरी तैयारी कर चुका था. ‘मिस्टर मेहता और मिसेज सिंह’ की स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन वह फिल्म नहीं बन सकी.
अब भी मैं देश-विदेश की फिल्में देखता रहता हूं. मुझे व्यक्तिगत तौर पर स्कॉरसीज, कपोला, वांग कार वाई और किस्लोवस्की की फिल्में पसंद हैं.
राजकुमार हिरानी की ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ देख कर बहुत जोश आया और प्रेरणा मिली. ‘लगान’ या ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ बना पाना बहुत मुश्किल है जिसमें मुख्यधारा में भी रहें और अपने सेंस भी ना छोड़ें. आप पूरी डिग्निटी के साथ एक बड़ी फिल्म बना दें, यह बड़ा मुश्किल काम है. दर्शकों में जहां एक्सपोजर है, जहां अच्छी पढ़ाई-लिखाई है, उनकी समझ अलग है. जहां रोटी-पानी के लिए ही दिक्कत है, उनको फिर आप उस तरह से सिनेमा कैसे दिखा सकते हैं? हमारे यहां ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ भी हिट होती है, ‘इश्किया’ भी हिट होती है. ‘वो आती जवानी रात में’, वो भी चलती है अपने लेवल पर. हमारे यहां दर्शकों के तीन-चार प्रकार हैं. एक अजीब-सा सिस्टम है जिसमें सबके लिए जगह है. आप जिस तरह के लोगों से आयडेंटीफाई करते हैं, अगर उन्हीं से आप प्रशंसा चाहते हैं तो फिर आपको उन्हीं के लिए फिल्म बनानी चाहिए.
लेकिन मेरे खयाल से अब भी हिंदी सिनेमा में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है. हम अभी भी जीरो हैं. आप्रवासी भारतीयों की संख्या ज्यादा है. वे फिल्में देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करते हें. किसी भी फिल्म का बिजनेस 75 और 100 करोड़ हो जाता है, लेकिन क्वालिटी जीरो रहती है. मेरे खयाल से ‘बैंडिट क्वीन’ के बाद कोई भी हिंदी फिल्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं बनी है. मीरा नायर की फिल्में अच्छी होती हैं. अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारा कमर्शियल सिनेमा ‘लाफिंग स्टॉक’ ही है. माना जाता है कि हम केवल हंसते-नाचते और गाते रहते हैं. धारणा ऐसी बन गई है कि हमारी फिल्मों को गंभीरता से नहीं लिया जाता. अजीब बात तो यह है कि टोरंटो फेस्टिवल में ‘कभी अलविदा ना कहना’ चुन ली जाती है और ‘ओमकारा’ रिजेक्ट हो जाती है. मैं यह नहीं कहता कि एक ही प्रकार का सिनेमा बने. हर कोई ‘ओमकारा’ बनाने लगेगा तो माहौल रूखा हो जाएगा. लेकिन ऐसा चुनाव मेरी समझ में नहीं आता और मैं कनफ्यूज्ड हो जाता हूं.
इस पर यह और कि मुंबई में जान-पहचान के लोग केवल फिल्मों की ही बातें करते हैं. बचने के लिए मैं अक्सर मुंबई से बाहर निकल जाता हूं. आम आदमी की तरह रहने और जीने की कोशिश करता हूं. टिकट की कतार में लग जाता हूं, किसी रेस्तरां में बैठ जाता हूं. बाहर निकलो तो दुनिया के आम लोगों से मेलजोल होता है और अपनी भी खबर लगती है. पता चलता है कि अभी क्या और कैसे हो रहा है. वैसे तो सूचना के इतने माध्यम आ गए हैं, लेकिन दुनिया से सीधे जुड़ने का अब भी कोई विकल्प नहीं है.
इन दिनों एक बहुत अच्छा परिवर्तन यह आया है कि मल्टीप्लेक्स के आने की वजह से छोटी और गंभीर फिल्में भी हिट हो रही हैं. मुझे लगता है कि राज कपूर के समय में श्याम बेनेगल और सत्यजीत रे की फिल्मों के दर्शक बिल्कुल नहीं थे. अब 25 प्रतिशत दर्शक वैसे हैं. उस वक्त विश्व सिनेमा का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था. यूरोपियन फिल्में आती नहीं थीं. फेस्टिवल में खास प्रतिशत में ही लोग देखते थे. करोड़ों की आबादी में चार हजार लोग ही ढंग की विदेशी फिल्में देख पाते थे. अब एक्सपोजर के बाद दर्शक और फिल्ममेकर दोनों बदले हैं. पहले शायद मजबूरी में राज कपूर को व्यावसायिक फिल्में बनानी पड़ती होंगी. हमें नहीं पता. हो सकता है कि राज कपूर यूरोप में जाकर देखते हों तो उनको लगता हो कि यार मैं ऐसी फिल्में बना पाता, पर मेरे देश में दर्शक ही नहीं हैं यह देखने के लिए. आज वे होते तो बहुत खुश होते.
अजय ब्रह्मात्मज से बातचीत पर आधारित.
मुलत: 100 साल का सिनेमा(15 मई 2012) में प्रकाशित





 1996 की कक्षा के तीन विद्यार्थी जब 2021 में अपने रजत जयंती पुनर्मिलन समारोह में मिलेंगे तो तब तक इतिहास एक क्रम व्यवस्थित कर चुका होगा. उनकी उपलब्धियां भी एक परिप्रेक्ष्य में रखी जा चुकी होंगी. अभी जो महत्वपूर्ण लग रहा है तब वह सिर्फ प्रासंगिक लग रहा होगा. 1996 में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. 1961-62 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि कौशल में इतनी विविधता और उपलब्धियों में इतनी असाधारणता रखने वाले तीन खिलाड़ियों ने एक ही सत्र में शुरुआत की हो. तब मंसूर अली खान पटौदी, फारुख इंजीनियर और रापल्ली प्रसन्ना कुछ हफ्तों के अंतराल पर ही भारतीय क्रिकेट टीम में आए थे.
1996 की कक्षा के तीन विद्यार्थी जब 2021 में अपने रजत जयंती पुनर्मिलन समारोह में मिलेंगे तो तब तक इतिहास एक क्रम व्यवस्थित कर चुका होगा. उनकी उपलब्धियां भी एक परिप्रेक्ष्य में रखी जा चुकी होंगी. अभी जो महत्वपूर्ण लग रहा है तब वह सिर्फ प्रासंगिक लग रहा होगा. 1996 में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. 1961-62 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि कौशल में इतनी विविधता और उपलब्धियों में इतनी असाधारणता रखने वाले तीन खिलाड़ियों ने एक ही सत्र में शुरुआत की हो. तब मंसूर अली खान पटौदी, फारुख इंजीनियर और रापल्ली प्रसन्ना कुछ हफ्तों के अंतराल पर ही भारतीय क्रिकेट टीम में आए थे.