
सिक्के खनकते हैं, लेकिन जब उनकी कीमत बढ़कर उन्हें नोटों में बदल देती है तब वे आवाज नहीं करते. करते भी हों, उन्हें आवाज करनी तो नहीं चाहिए.
अमिताभ बेशकीमती हैं. वे अपनी लोकप्रिय विनम्र शैली में इसे कहेंगे कि वे कुछ नहीं हैं और उन्हें बेशकीमती बना दिया गया है. मगर किसी खामखयाली में मत रहिए. वे हमेशा इतने विनम्र नहीं रहते. वे भूलते नहीं और न ही माफ करते हैं. चटपटी खबरों की तलाश में रहने वाले मुंबई मिरर के एक पत्रकार ने एक हड़बड़ी वाली दोपहर में जब ऐश्वर्या को टीबी होने की खबर लिखी तो उसे इसका अंदाजा नहीं था. किसी गलतफहमी में वह अमिताभ के गुस्से को भूल गया होगा या उन्हें बूढ़ा मानकर बेफिक्र रहा होगा.
मगर यह 1996 नहीं है, जब उदास और हारे हुए से एक इंटरव्यू के बीच में एक पत्रकार ने अमिताभ से अचानक पूछा कि वे कितना काम और करेंगे. उनका उत्तर था, ‘दो साल और. मैं बूढ़ा हो रहा हूं और हमेशा इस गति से काम नहीं कर सकता.’
तब वे 54 साल के थे और उन्हें लग रहा था कि अपनी निरंतर कम होती क्षमताओं के साथ वे ज्यादा दिन तक लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे.
इस बात को चौदह साल बीत चुके हैं और आज भी उन्हें बूढ़ा कहना, बुढ़ापे को असीम ऊर्जा, रफ्तार और अटूट इच्छा-शक्ति का पर्याय बनाने जैसा है. यह अदम्य उत्साह शायद इलाहाबाद में बीते बचपन की उन गर्मियों से निकला है, जब वे दोपहर की लू में साइकिल पर घर लौटते थे और सुराही का ठंडा पानी, एक टेबल फैन या खस की चटाई ही सबसे आरामदेह चीजें हुआ करती थीं. आज ‘प्रतीक्षा’ में अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए जब वे अपने मैक पर टाइप कर रहे होते हैं तब उन्हें जुबान पर डाक टिकट फिराकर उसे चिट्ठी पर चिपकाने वाले दिन भी उसी शिद्दत से याद आते हैं.
‘आप परिवार के पुरुषों के बारे में कुछ कहेंगे तो मैं सहन भी कर लूंगा, लेकिन अपने परिवार की औरतों के बारे में एक शब्द भी नहीं ‘
यही बात है जो उन्हें उस विशालता से अलग करती है जो हमारे महानायकों को हमसे कई हाथ ऊंचे सिंहासन पर बिठा देती है और हम उन्हें बिलकुुल सामने से कभी नहीं देख पाते. वे हमारे पिताओं और बच्चों दोनों को अपने दोस्त-से लगते हैं. हम जादुई सचिन या प्रतिभावान शाहरुख से चाहकर भी वह स्नेहिल पारिवारिक रिश्ता नहीं जोड़ पाते, जो अमिताभ से अपने आप जुड़ जाता है. लेकिन क्या इस रिश्ते का भ्रम जान-बूझकर रचा गया है और हम एक बड़े खेल का बेवकूफ-सा हिस्सा भर हैं?
कुछ लोगों का मानना है कि वे हमेशा से इतने अपने नहीं लगते थे और अपनी सबसे नई पारी में उन्होंने यह नया व्यक्तित्व जान-बूझकर रचा है. मतलब यह कि बहुत सारी असफलताओं के बाद दिखा उनका यह सार्वजनिक चेहरा भी शहंशाह या ऑरो की तरह एक किरदार है, जिसे वे पूरी लगन के साथ निभा रहे हैं.
जो भी हो, हम सब उस अपनेपन को नहीं खोना चाहते. इसलिए हमें वह रास्ता खोजना था जिससे हम उनके मन की कुछ और तहों तक पहुंच सकें. अमिताभ ने कहीं लिखा है कि उनका लिखना, उनके अस्तित्व को अर्थ देता है. सो हमने भी उनके ब्लॉग पर लिखे हुए की उंगली थामी और उसमें छिपे अर्थों के जरिए उन्हें एक व्यक्ति के रूप में जानने की कोशिश की.
अमिताभ को जानना सिर्फ उन्हें जानना नहीं है. वे हमारे पूरे दौर की परिभाषा से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं. उन्हें जानना चूर-चूर होकर बिखर जाने के बाद फिर से पहाड़ पर चढ़ने के ख्वाब को देखने जैसा है. उन्हें जानना एक चोटिल अभिनेता के लिए एक धार्मिक देश की असंख्य दुआओं को महसूस करना है और इस तरह घोर मसाला फिल्मों के प्रति एक रूढ़िवादी समाज की रोचक आस्थाओं को जानना है. उन्हें जानना भारत की राजनीति के उलझे काले रहस्यों को जानना भी है. उन्हें जानना भारत की संकल्पना के उस जिद्दी स्वप्न को देखने जैसा भी है जो तमाम विषमताओं के बावज़ूद अपनी राह पर बढ़ते रहने का हौसला देता है. उन्हें जानना उस मध्यवर्गीय भारत को जानने जैसा है जो एक लॉटरी के टिकट या एक घंटे के टीवी शो के माध्यम से अपनी तकदीर बदल देना चाहता है.
उनके काम को छोड़ दिया जाए तो वे किसी रिटायर्ड कस्बाई अध्यापक की तरह ही लगते हैं. ब्लॉग पर आम बातों के बीच में वे अचानक दार्शनिक हो जाते हैं, गुस्से में बहुत डांटते हैं और कभी-कभी बहुत दुलारते भी हैं. इस उम्र में उन्हें अपने पिता बहुत याद आने लगे हैं और अपनी सीमाओं में वे हम सबके लिए बहुत फिक्रमंद हैं. कम से कम ऐसा कहते तो हैं ही.

घर-परिवार
पारिवारिक सदस्य के रूप में यदि अमिताभ की तुलना किसी फिल्मी चरित्र से करनी हो तो नब्बे के दशक की सुपरहिट फिल्मों में आलोकनाथ और अनुपम खेर द्वारा निभाए गए किरदार याद आते हैं. वे एक समृद्ध परिवार के मुखिया हैं. ऐसा परिवार जिसके पास पांच पद्म सम्मान हैं. वे किसी सामान्य भारतीय से ज्यादा आस्तिक हैं. ‘मोहब्बतें’ के सख्त पिता के उलट वे प्यार के बीच में नहीं खड़े होते. उनका सबसे पहले नजर में आने वाला गुण विनम्रता है (कभी-कभी गुस्सा भी), विनम्रता इतनी ज्यादा कि कभी-कभी बनावटी भी लगती है. वे उत्सवप्रिय हैं. वे अपनी समधिन का जन्मदिन मनाने पूरे परिवार के साथ डिनर पर जाते हैं. वे अपने बच्चों के दोस्त और आदर्श हैं. वे अपनी बहू को बेटी जैसा मानते हैं और इस तरह बेटे जैसा भी, क्योंकि भारत में बेटियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का यह राजदूत बार-बार स्त्री-पुरुष समानता के पक्ष में खड़ा होता है (मुंबई मिरर और दूसरे अखबारों की उन खबरों के बावजूद जिनमें बार-बार कहा जाता है कि अमिताभ पोता पाने के लिए बेताब हैं). बहुत-से पुरुषों की तरह वे मानते हैं कि अपनी पत्नी में वे मां का अक्स भी तलाशते और पाते रहते हैं.
वे अपने पुराने दोस्त राजीव गांधी का उतना ही कम जिक्र करते हैं जितना अपने भाई अजिताभ का
उन फिल्मी किरदारों से समानताएं यहीं खत्म नहीं होतीं. यदि आप परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ गलत कहते हैं तो अमिताभ दुर्भेद्य सुरक्षा-कवच की तरह सामने आ खड़े होते हैं. उन्हें इतना गुस्सा आता है कि अकसर वे फिर से पारंपरिक भारतीय मर्द का चोला पहन लेते हैं और कहते हैं, ‘आप परिवार के पुरुषों के बारे में कुछ कहेंगे तो मैं सहन भी कर लूंगा, लेकिन अपने परिवार की औरतों के बारे में एक शब्द भी नहीं.’
परिवार की दो औरतों, जया और श्वेता के बारे में आम तौर पर कोई उल्टा-सीधा नहीं कहता, लेकिन उनकी विश्व-सुंदरी को (वे स्नेह और क्रोध, दोनों के अतिरेक में ये ही शब्द इस्तेमाल करते हैं- ‘मेरी विश्व सुंदरी’) अफवाहों से बचाकर रखना इतना आसान नहीं. कभी उन्हें मांगलिक बताया जाता है और यह भी कि उनकी ग्रह-दशा शांत करवाने के लिए पूरा बच्चन परिवार मंदिरों में घूम रहा है और कभी यह कहा जाता है कि उन्हें पेट की टीबी है और इस कारण वे गर्भवती नहीं हो पा रहीं.
वे बार-बार सफाई देते हैं, क्रोध में दहाड़ते हैं और कभी-कभी अंधविश्वास के पैरोकार बड़े अखबारों के दफ्तरों में जाकर उनके पचासों संपादकों को समझाते भी हैं कि उन्होंने ऐश्वर्या की शादी कभी किसी पेड़ से नहीं करवाई. लेकिन कोई फायदा नहीं होता. वह बहू, कान्स में उन्हें जिसके नाम से जाना जाता है, हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री है और उसे मसाला खबरों की खुराक बनना ही पड़ता है.
परिवार के सदस्यों में अभिषेक और ऐश्वर्या के नाम उनके ब्लॉग पर सबसे ज्यादा दिखते हैं. हां, पिता हरिवंशराय बच्चन से थोड़ा कम. मां का जिक्र सबसे कम होता है. यह बात और है कि आजकल उनकी आस्थाएं मां के सिख धर्म की ओर मुड़ने लगी हैं. मां को कम याद करने की बात इस फिल्मी संदर्भ में मजेदार है कि अपनी जवानी में उन्होंने हिन्दी फिल्मों को ऐसे कई हीरो दिए हैं जो अपनी मां को बहुत प्यार करते थे और पिता के बारे में कम जानते थे. मगर यह याद इतनी कम भी नहीं क्योंकि उदयपुर के भीड़ भरे बाजारों से गुजरते हुए अचानक मां का आईसीयू में जिंदगी और मौत से चला संघर्ष आंखों के आगे घूम जाना इतना अनायास भी नहीं हो सकता.
सिख धर्म की ओर झुकाव होने, गले में गुरु नानक देव जी के लॉकेट पहनने और सच्चे बादशाह से ऊर्जा पाने की बात 1984 में सिख-विरोधी दंगे भड़काने के ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के आरोपों को धीमे जहर की तरह खत्म करती है. वैसे अमिताभ कहते हैं कि वे आम खूबियों वाले आम आदमी हैं और उनकी बातों के गहरे अर्थ न तलाशे जाएं.
उन्हें आंगन बहुत प्यारा है और उसमें नीम का पेड़ भी हो तो उन्हें उसमें खो जाने से रोकना और भी मुश्किल हो जाता है. जया का जिक्र वे दिल्ली के अपने घर ‘सोपान’, आंगन और नीम से बस थोड़ा ही ज्यादा करते होंगे.
सच्चाई, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और प्रतिभा के सम्मान की बातें वे बार-बार करते हैं, मगर बॉलीवुड में बढ़ते वंशवाद की कभी नहीं करते. शायद उन्हें इकतीसवें दिन की अपनी पोस्ट पर अभिषेक का वह कमेंट याद आ जाता होगाे जिसमें उन्होंने लिखा था, ‘मैं आपसे प्यार करता हूं. वैसा होने के लिए जो आप हैं- दुनिया के सबसे अच्छे पिता..’
कभी-कभी अच्छा पिता होने के लिए बाकी बातों को भूल जाना पड़ता है. और आप हैं कि हर बात में नुक्स तलाशते हैं.
मीडिया
1997 के पहले अंक में आउटलुक की आवरण कथा थी. पिछले वर्ष के खलनायक. उसमें अमिताभ बच्चन छठे स्थान पर थे. ये वे साल थे जब उनकी कंपनी एबीसीएल उन्हें कर्ज में डुबाकर डूब गई थी. उस कर्ज में एक बड़ा हिस्सा दूरदर्शन का भी था और देश के हर चौराहे पर कहा जा रहा था कि अमिताभ का सुनहरा दौर अब खत्म हो गया है. मीडिया शत्रुघ्न सिन्हा के उन बयानों को गर्व से छाप रहा था जिनमें कहा गया था कि वे सिर्फ कट-आउट में ही अच्छे लगते हैं, असल में नहीं. हर दौर में उन्होंने गलत कहानियां और निर्देशक ज्यादा चुने हैं और यह वे तब भी कर रहे थे और असफल हो रहे थे. अपने करियर को उठाने के लिए उन्हें गोविंदा की फूहड़ कॉमेडी का सहारा लेना पड़ रहा था. नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक वे दुनिया के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा अपनी फिल्मों से ज्यादा स्तरीय थे. अमिताभ हताश दिखते थे और टीवी पर साजिद खान उन्हें राष्ट्रीय मजाक बनाकर मशहूर होने की कोशिश में लगे हुए थे. इस हाल से बाहर आने के लिए वे मिरिंडा का विज्ञापन करते थे तो देश भर को वे अपने गरिमामयी शिखर से गिरते हुए नजर आते थे. अखबार और पत्रिकाएं ईश्वर के अंदाज में यह घोषणा कर रहे थे कि अमिताभ नाम का सितारा मिस वर्ल्ड के तंबुओं की तरह टूटकर गिर गया है. मिस इंडिया करवाने वाला अखबार मिस वर्ल्ड के आयोजन के उनके इरादों को देखकर कुछ अधिक भारतीय हो गया था और उन्हें संस्कृति के पाठ पढ़ाने लगा था. उन्हीं दिनों में एक बार बहुत धीमे स्वर में उन्होंने कहा था, ‘मुझे उम्मीद है कि अगले दस साल में भारतीय कुछ अधिक उदार हो जाएंगे.’ लेकिन वे कभी उदार नहीं हुए बल्कि हमेशा या तो सनकी भक्त रहे या कटु आलोचक.
पिता ही हैं जिनके लिखे ‘सिलसिला’ और ‘बागबान’ के होली वाले गीत होली के दिन सड़कों पर सुनकर अमिताभ का सीना चौड़ा हो जाता है
क्या विडंबना थी कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में सबसे लंबे समय तक परदे पर लोगों के सपनों को सच करता और उनकी लड़ाइयां लड़ता यह महानायक मुंबई के एक अखबार के सर्वे में तीसरे स्थान पर था, जिसका सवाल था कि आप किस मशहूर शख्सियत से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं.
उन्होंने यह दौर बार-बार देखा है और अपने ब्लॉग के माध्यम से मीडिया पर उनके बार-बार बरसने को यदि आप बिलकुल गैरजरूरी मानते हैं तो क्या आपको अस्सी के दशक का ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ का वह पहला पन्ना याद नहीं जो अमिताभ के बारे में था और जिसका शीर्षक था- देश का गद्दार.
एक समय में उन पर आरोप था कि वे इंदिरा गांधी के नजदीकी हैं और आपातकाल में प्रेस पर सेंसरशिप के लिए वे ही उत्तरदायी थे. पहले मीडिया ने उन पर घोषित प्रतिबंध लगाया और बाद में उन्होंने मीडिया पर. मीडिया से अमिताभ का रिश्ता इसी पंक्ति के इर्द-गिर्द घूमता रहा है. सब सेलिब्रिटियों की तरह मीडिया उनकी जिंदगी के भी बिलकुल अंदर तक बेरोकटोक घुसना चाहता है और जब वे अपने बेटे की शादी में बिना बुलाए घुस आए पत्रकारों पर थोड़े सख्त हो जाते हैं तो वह फिर से उनका पूरा बायकॉट कर देता है. इस रिश्ते में बीच का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वे ब्लॉग लिखते हैं, जो कई मायनों में उनकी व्यक्तिगत न्यूज एजेंसी की तरह भी है.
उनकी और भी शिकायतें हैं. उन फोटोग्राफरों से जो उन्हें तब मुस्कुराकर फोटो खिंचवाने को कहते हैं जब वे किसी अस्पताल में मौत से जूझते बेसहारा बच्चों से मिल रहे होते हैं. उन पत्रकारों से जो हर इंटरव्यू में वही सवाल पूछते हैं और उनकी आधी शक्ति उनका अलग-अलग तरह से जवाब देने में खर्च हो जाती है.
मगर क्या उन एक जैसे सवालों के लिए अमिताभ ही कहीं न कहीं उत्तरदायी नहीं हैं? बहुत-से सवालों को वे व्यक्तिगत सवालों की लिस्ट में डाल देते हैं और कुछ पर उनकी प्रतिक्रिया इतनी ‘पोलिटिकली करेक्ट’ होती है कि इंटरव्यू को नीरस बनने से बचाने के लिए उसे काटना पड़ता है. अब सिर्फ एक जैसे कुछ सवाल ही सुरक्षित बचते हैं, मसलन इस फिल्म में आपका क्या रोल है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं. आप कितने भी वाकपटु हों, उनसे ऐसे किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर राय नहीं ले सकते जिस पर किसी के नाराज हो जाने का खतरा हो.
अमिताभ जब देर रात में पोस्ट लिखते हैं तो उस पर आधी प्रतिक्रियाएं तो यही होती हैं कि उन्हें जल्दी सोना चाहिए
गलती चाहे किसी की भी रही हो, उनका ब्लॉग मीडिया को कोसने का एक मंच बन गया है. उनका साक्षात्कार लेने वाले पत्रकार उनका कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आसानी से अपने अखबार में नहीं छाप सकते, क्योंकि उसे अकसर अमिताभ अपने ब्लॉग पर छाप चुके होते हैं (कभी-कभी अखबार से पहले ही) और वे नहीं चाहते कि उनकी एक भी पंक्ति से कोई छेड़छाड़ की जाए. नतीजा होता है, एक जैसे सपाट उत्तरों की एक लिस्ट, जिससे आप किसी भी मुद्दे पर उनका स्टैंड नहीं जान सकते.
वे अपनी प्राइवेसी के बारे में बहुत सतर्क रहते हैं, लेकिन इस चक्कर में वे कई बार उन पत्रकारों की प्राइवेसी का सम्मान करना भूल जाते हैं जिनकी ईमेल आईडी और एसएमएस वे अपने ब्लॉग पर जनता के सामने रख देते हैं. ये वे संदेश और संवाद होते हैं जो यह समझकर लिखे गए होते हैं कि इन्हें वे अपने तक ही सीमित रखेंगे. दूसरों की निजता का हनन करने वाली इस हंसी में कभी-कभी अहंकारी अट्टहास दिखता है, जो उनके जायज गुस्से के बावजूद उतना ही नाजायज है.

दोस्त और कुछ कम अच्छे दोस्त
अमिताभ के नजदीकी मित्रों की संख्या ज्यादा नहीं है और यदि है भी तो वे उनके बारे में उतनी ही कम बातें करते हैं. दोस्ती के दिनों में भी अमर सिंह को वे अमर सिंह जी लिखते थे, जो सुनने में दोस्ती का संबोधन तो नहीं लगता. पुराने दोस्त राजीव गांधी का वे उतना ही कम जिक्र करते हैं जितना अपने भाई अजिताभ का. छुट्टी के दिन उन्हें परिवार के साथ फिल्म देखना और फिर शाम को कहीं बाहर खाने पर जाना पसंद है. परिवार के लोग व्यस्त हों (और ऐसा तो अक्सर होता होगा) तो वे अकेले रहना पसंद करते हैं. उनकी जिंदगी में ऐसा कोई वीरू नहीं दिखाई पड़ता जिसके लिए जान देने को भी तैयार हुआ जा सके. चाहे-अनचाहे उनके इर्द-गिर्द ऐसा आभामंडल बन गया है जो उन्हें जय की तरह मुंहफट और बेपरवाह नहीं होने देता और दुर्भाग्यवश, वीरू जैसा कोई दोस्त आपके पास होने के लिए यही पहली शर्त है.
फिल्मी दुनिया की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखें तो पहले दर्जे के अधिकांश सक्रिय लोग उम्र में उनसे काफी छोटे हैं और बीच में आया सम्मान का परदा उन्हें अनौपचारिक नहीं होने देता. यह गांव के सबसे बूढ़े बचे व्यक्ति के अकेलेपन जैसा है, जो अपने दोस्तों को एक-एक कर जाते हुए देख चुका है. इस फिल्मफेयर में व्हीलचेयर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लेने आए शशि कपूर को देखने के बाद से वे उन्हें कई बार याद कर चुके हैं. शशि ही थे जिन्होंने ‘शेक्सपीयरवाला’ की शूटिंग के दौरान उन्हें अंतिम-संस्कार की भीड़ में एक्स्ट्रा बनकर खड़े देखा था और खींचकर यह कहते हुए बाहर ले आए थे कि तुम्हें बहुत बड़े काम करने हैं.
[box]
मैं स्टूडियो की ओर भागता हूं. यथार्थ की ओर. अपनी राह की ओर. संघर्ष करने, तलाशने, बाधाएं झेलने और घायल होने, उन लोगों का भेदभाव झेलने जो अपने इलाकों में मुझे नहीं देखना चाहते, जो मुझे शिकायतों और विवादों से चिढ़ाते हैं, मेरे काम, मेरे बर्ताव, मेरे दृष्टिकोण की बुराई करते हैं. जो मेरे हर काम को अविश्वास से देखते हैं, मेरी ईमानदारी, मेरी हर दोस्ती, मेरे लिखे और बोले हर शब्द को चुनौती देते हैं…
जब कैमरा शुरू होता है और निर्देशक ‘एक्शन’ बोलता है, कहीं किसी विचार या भावना के लिए जगह नहीं होती, जगह होती है सिर्फ मेरे शरीर के लिए, मेरे किरदार के लिए, मेरी आवाज और मेरे भावों के लिए. उस स्पेस में न कोई आ सका है, न आ पाएगा. वह मेरी अपनी दुनिया है, जिसमें मेरी आस्था है और जिसे मैं पाना चाहता हूं. वहां कोई भेदभाव नहीं है, न नफरत, न गुस्सा, न राजनीति, न सामाजिक और नैतिक बंधन. वहां सिर्फ वह किरदार है जिसे मैं कैमरे के खूबसूरत लेंस के लिए जीता हूं और जो मुझे मेरी मधुशाला में ले जाता है… (ब्लॉग से)
[/box]
उनके सबसे नए फिल्मी दोस्त शायद रामगोपाल वर्मा हैं और दोनों एक-दूसरे को ‘सरकार’ कहकर पुकारते हैं.
कुछ कम अच्छे दोस्तों की फेहरिस्त थोड़ी लंबी है. उसमें सलीम खान भी हैं, जो आम आदमी की अभागी याददाश्त के कारण ‘शोले’ और ‘दीवार’ के लेखक के रूप में कम और सलमान के पिता के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं. जब भी अमिताभ की आलोचना होती है, उनके बयान सबसे पहले आते हैं. अमिताभ की नाराजगी का बड़ा कारण वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमिताभ पैसे लेकर यूपी सरकार के लिए विज्ञापन कर रहे हैं. पुराने साथी कलाकार और पड़ोसी शत्रुघ्न सिन्हा भी साल में एक बार तो उनके विरुद्ध बोल ही देते हैं. शत्रुघ्न ही थे जिन्होंने अभिषेक की शादी की शगुन की मिठाई लौटा दी थी और आईफा पुरस्कारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, ‘सब किसी का बेटा है या किसी की बहू या किसी की बीवी.’ मगर उसकी प्रतिक्रिया में जब अमिताभ आपा खोते हैं तो उसकी चपेट में उनकी पत्नी पूनम, शोले के सांभा मैकमोहन, रवीना टंडन और राष्ट्रीय पुरस्कार तक आ जाते हैं. यह उनके गुस्से का खास शालीन स्टाइल है.
कभी दोस्त रहे खालिद मोहम्मद जब भूतनाथ की कुछ अधिक व्यक्तिगत होती समीक्षा में यह लिखते हैं कि अमिताभ ऐक्टिंग भूल गए हैं तो अमिताभ भी किसी तार्किक आधार पर उन्हें गलत नहीं ठहराते. वे खालिद को वह महंगी शराब याद दिलाते हैं जो उन्हें अमिताभ की डाइनिंग टेबल पर ही नसीब हुआ करती थी.
आप उनकी मुलाकातों और मुस्कुराहटों से उनके नए दोस्तों का अनुमान लगाएंगे तो शायद नरेंद्र मोदी का नाम भी लेंगे, मगर अमिताभ कहते हैं कि वे अपने काम और रुतबे के सिलसिले में इतने लोगों से मिलते हैं कि तब तो सीएनएन आईबीएन के राजदीप सरदेसाई, एनडीटीवी के प्रणय रॉय, इंफोसिस के नारायणमूर्ति से भी उनकी दोस्ती की चर्चा होनी चाहिए और लेबर पार्टी से लेकर डीएमके, भाजपा, कांग्रेस और बाल ठाकरे से भी. हां, याद आया, जिस विवाद में ‘ठाकरे’ जुड़ जाए उसमें वे चुप्पी साध लेते हैं. तब वे वैसी तल्ख प्रतिक्रियाएं नहीं देते जैसी खालिद मोहम्मद या शत्रुघ्न सिन्हा को देते हैं. यह शायद मुंबई में रहने का नया नियम है, जिसे ‘सरकार’ तोड़ना नहीं चाहते.
पिता
अमिताभ अपने पिता के पिता के पुनर्जन्म जैसे हैं. ऐसा उनके पिता कहते थे. हरिवंशराय बच्चन भी ऐश्वर्या की तरह, जितना अमिताभ को सिर ऊंचा करने के कारण देते हैं, उतना ही लोग उन्हें अमिताभ को परेशानी देने वाले माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं.
मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता
शत्रु मेरा बन गया है छलरहित व्यवहार मेरा.
ये पंक्तियां अमिताभ अकसर अपने आप को निष्कपट बताने के लिए ब्लॉग पर लिखते हैं, लेकिन उसी तरह लोग उनके पिता की पंक्तियां लिखते हैं- मैं हूं उनके साथ, जो सीधी रखते अपनी रीढ़, और उन्हें याद दिलाते हैं कि वे तटस्थ दिखने की बजाय सच का रास्ता चुनें और अपने पिता की राह पर चलें. गुस्से में अमिताभ कहते हैं कि कोई ऐसा कॉपीराइट होना चाहिए जिससे कोई भी उनके पिता की पंक्तियों को यूं ही मनचाहे संदर्भ में इस्तेमाल न कर सके. वे ब्लॉग पर अपने पिता की विरासत को बार-बार महान और संग्रहणीय भी कहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि उसे और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उनका नाम काम आ सके. हिंदी के किसी और लेखक के पास अपने प्रचार-प्रसार के लिए इतना सफल बेटा नहीं है.
जया के शब्दों में अमिताभ भोले-भाले स्कूली लड़के की तरह हैं जो होमवर्क समय पर और अच्छी तरह पूरा करने के अलावा और कुछ नहीं जानता. वह स्कूली लड़का अपने पिता के सर्वाधिक निकट है और उसे वे दिन अच्छी तरह याद हैं जब आर्थिक तंगी के बीच कैंब्रिज में अपनी थीसिस पूरी करके लौटे उनके पिता बच्चों के लिए उपहार के रूप में उस थीसिस के रफ ड्राफ्ट लेकर आए थे (वैसे यह अलग बहस का विषय है कि आज भी आर्थिक तंगी में कितने प्रतिशत भारतीय कैंब्रिज पढ़ने जा सकते हैं). अमिताभ ने उस उपहार को आज भी संभालकर रखा है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपनी मां और पिता के कमरे आज भी उसी स्थिति में रखे हैं जिसमें वे उन्हें छोड़ गए थे.
यदि आपको लगता है कि ‘सात हिंदुस्तानी’ उनकी पहली फिल्म थी तो मैं आपको टोकना चाहूंगा. उनकी आंखों ने चमक, प्रसिद्धि और तालियों की जिस दुनिया में पहली बार अपने आपको पाया वह उन कवि सम्मेलनों की थी जिनमें वे अपने पिता की उंगली पकड़कर जाते थे और फिर मंत्रमुग्ध-से उन्हें हजारों की भीड़ के सामने मधुशाला गाते हुए देखते थे. वही फिल्म है जिसकी रील सब मुश्किल घड़ियों में आंखें बंद करते ही उनके सामने घूमने लगती है और उन्हें पिता की एक और बात याद आती है- मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा.
पिता ही हैं जिनके लिखे ‘सिलसिला’ और ‘बागबान’ के होली वाले गीत होली के दिन सड़कों पर सुनकर अमिताभ का सीना चौड़ा हो जाता है. शायद पिता की दी हुई शक्ति ही है कि आप अमिताभ को कितना भी तोड़ें, वे दुगुनी हिम्मत के साथ हर बार फिर से जुड़कर खड़े हो जाते हैं. नैनीताल के शेरवुड कॉलेज के दिनों में अपने अध्यापकों के लाख रोकने के बावजूद वे हर बार बॉक्सिंग रिंग में कूदते थे. चूंकि अपने लंबे कद के कारण हमेशा वे अपनी सामर्थ्य से अधिक भारवर्ग में होते थे और इसलिए हारते भी थे, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा. इसी तरह वे तब भी लड़ना नहीं छोड़ते जब सवा अरब लोगों की आंखें उनकी निजी जिंदगी को और उम्मीदें उनके प्रयोगों को अपने बोझ तले कुचल डालना चाहती हैं. आज भी पिता की कविताएं पढ़ने से उनकी बेचैन रातें कुछ आसान हो जाती हैं, कुछ मुश्किल फैसले उतने मुश्किल नहीं रह जाते, जीवन उतना रंगीन और मृत्यु उतनी भयावह नहीं लगती.
 सरकार और उनके दीवाने
सरकार और उनके दीवाने
अमिताभ की छवि ऐसी है कि कोई भी उत्तरभारतीय मध्यवर्गीय परिवार उन्हें अपने घर के बुजुर्ग जैसा मान सकता है. बीस साल पहले तक वह उन्हें अपने लिए लड़ने वाला जवान बेटा मानता था. आप कस्बों और गांवों की ओर बढ़ेंगे तो वह छवि कई मिथक अपने साथ जोड़ती जाएगी. मसलन अपने बचपन में हम सबके लिए वही दुनिया के सबसे लंबे आदमी थे. मेरे पिता के लिए वे ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अदभुत सफलता को अपने सिर नहीं चढ़ने दिया और सब संस्कार बचाकर रखे. यह सब सितारों के साथ होता है, इसीलिए ‘अमिताभ बच्चन’ एक व्यक्ति न होकर एक संस्कृति हो गए हैं. अमिताभ शराब-सिगरेट नहीं पीते, मांस नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते वाली यह छवि पौराणिक नायकों जैसी है और अमिताभ खुद महसूस करते हैं कि कई बार वह उन पर अतिरिक्त बोझ डाल देती है.
लेकिन आप उनका ब्लॉग पढ़ेंगे तो लगेगा कि यह बोझ थोड़ा तो जान-बूझकर भी डाला गया है. जब आप उन्हें घर के बाहर जमा भीड़ के लिए हाथ हिलाते देखेंगे तो उनके चेहरे पर उपलब्धि का भाव होगा, कुछ-कुछ ‘सरकार’ जैसा. उन्हें किसी भी दूसरे सितारे से थोड़ा ज्यादा अपने प्रशंसकों को अपना बनाए रखने का खयाल है. ब्लॉग के पाठक उनकी एक्सटेंडेड फैमिली हैं और कभी-कभी वे उनमें से कुछ को जन्मदिन की बधाई भी दे देते हैं और कुछ के लिए उनके किसी अपने की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं. अब अमिताभ बच्चन एक बार भी ऐसा कर दें तो हजार लोग इस उम्मीद में महीनों उनके ब्लॉग पर अपनी टिप्पणियां देते रहेंगे कि उनका नंबर भी आएगा. वैसे उन टिप्पणियों को पढ़ना भी एक रोचक अनुभव है और तब आप जान पाते हैं कि उस दीवानगी की हदें कितनी दूर तक हैं.
जैसे बनारस में जन्मी एक बंगाली लड़की तीन साल की उम्र से उनकी दीवानी है. और बहुत-से प्रशंसकों की तरह वह दावा करती है कि उसने उनकी सभी फिल्में कम से कम पच्चीस बार देखी हैं. उसे एक लड़के से सिर्फ इसलिए प्यार हुआ क्योंकि वह हर बात में अमिताभ के डायलॉग बोलता था और शादी के बाद वे जब भी घूमने जाते थे, रास्ते भर ‘सिलसिला’ के गाने गुनगुनाते थे. एक जनाब दावा करते हैं कि अमिताभ उन्हें अकसर सपने में दिखते हैं – घर के सदस्य की तरह – और उन्होंने चार साल पहले खरीदी एक किताब अब तक इसलिए नहीं खोली कि उसे उस पर अमिताभ के साइन चाहिए. अखबार के समस्या-समाधान वाले कॉलम की तरह लोग अपनी घरेलू समस्याएं तक लिखते हैं और अमिताभ से मार्गदर्शन मांगते हैं, जैसे वे जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा. अमिताभ जब देर रात में पोस्ट लिखते हैं तो उस पर आधी प्रतिक्रियाएं तो यही होती हैं कि उन्हें जल्दी सोना चाहिए और अपनी सेहत का खयाल रखना चाहिए. कुछ उनके लिए लंबी कविताएं लिखते है तो कुछ उन्हें तीस साल पहले की कोई मुलाकात याद दिलाने की भी कोशिश करते हैं, जब भीड़ में अमिताभ ने हाथ मिलाने के बाद उनका नाम भी पूछा था.
लेकिन यह अपनापन इतना अनायास नहीं है. मुंबई की बारिश में वे कुछ लड़कियों को अपनी कार में लिफ्ट देते हैं, बारिश इतनी है कि उनके घर में भी पानी घुस आया है जिसे बाल्टियों से निकालना पड़ रहा है, सड़क पर मिलने वाले भूखे लोगों और अनाथ बच्चों से उनकी सहानुभूति है और कभी-कभी वे उन्हें खाना या कपड़े भी दे देते हैं, औरतों के अधिकारों के वे प्रबल समर्थक हैं, एक नौकर की पत्नी के बीमार होने पर वे उसकी आर्थिक मदद करते हैं और हर सुख-दुख में साथ रहे घर के नौकर ही बेटे की शादी में उनके लिए सर्वाधिक अपने और महत्वपूर्ण मेहमान हैं, उस दिन अमिताभ उन्हें कुर्सी पर बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसते हैं.
अब ऐसा इंसान किसे अपना नहीं लगेगा? आप उनके काम के भी प्रशंसक हों तब तो इतने दीवाने हो ही जाएंगे. अमिताभ को गुस्सा आता है कि मीडिया उनका यह पहलू कभी नहीं दिखाता. लेकिन एक बात और गौर करने लायक है कि ये सब चीजें तो कम या ज्यादा, हम सभी करते हैं. फिर अमिताभ इन्हें बार-बार खूबियों की तरह क्यों लिखते हैं? वह भी तब जब वे उस मुकाम पर हैं जहां अपनी अच्छाइयां अपने आप बताना न तो जरूरी है और न ही ठीक.
(सिनेमा, 15 अक्टूबर 2010 में प्रकाशित)

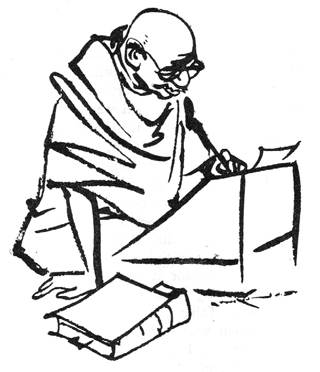
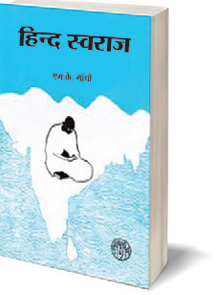 इस किताब में गांधी इन सारे रूपों में दिखाई देते हैं- अपनी स्थापनाओं के प्रति आग्रही भी, आक्रामक भी. वे हर मुद्दे पर बहस में उतरते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, ललकारते भी हैं. वे उन सारी मान्यताओं की धज्जियां उड़ा देते हैं जो आज की सभ्यता की ध्वजा उठाए फिरती हैं. उन्हें इसका पूरा अंदाजा है कि औद्योगिक सभ्यता की तड़क-भड़क इतनी सम्मोहक है और उसकी पहुंच इतनी व्यापक है कि उस पर हमला करते हुए किसी संकोच से काम नहीं चलेगा. लेकिन वे जो लिखते हैं, वह उनकी गहरी समझ में से विकसित हुआ है: ‘लंदन में रहने वाले हर एक नामी अराजकतावादी हिंदुस्तानी के संपर्क में मैं आया. उनकी शूर-वीरता का असर मेरे मन में पड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि उनके जोश ने उल्टी राह पकड़ ली है. मुझे लगा कि हिंसा हिंदुस्तान के दुखों का इलाज नहीं है, और उसकी संस्कृति को देखते हुए आत्मरक्षा के लिए कोई अलग व ऊंचे प्रकार का शस्त्र काम में लाना चाहिए.’
इस किताब में गांधी इन सारे रूपों में दिखाई देते हैं- अपनी स्थापनाओं के प्रति आग्रही भी, आक्रामक भी. वे हर मुद्दे पर बहस में उतरते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, ललकारते भी हैं. वे उन सारी मान्यताओं की धज्जियां उड़ा देते हैं जो आज की सभ्यता की ध्वजा उठाए फिरती हैं. उन्हें इसका पूरा अंदाजा है कि औद्योगिक सभ्यता की तड़क-भड़क इतनी सम्मोहक है और उसकी पहुंच इतनी व्यापक है कि उस पर हमला करते हुए किसी संकोच से काम नहीं चलेगा. लेकिन वे जो लिखते हैं, वह उनकी गहरी समझ में से विकसित हुआ है: ‘लंदन में रहने वाले हर एक नामी अराजकतावादी हिंदुस्तानी के संपर्क में मैं आया. उनकी शूर-वीरता का असर मेरे मन में पड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि उनके जोश ने उल्टी राह पकड़ ली है. मुझे लगा कि हिंसा हिंदुस्तान के दुखों का इलाज नहीं है, और उसकी संस्कृति को देखते हुए आत्मरक्षा के लिए कोई अलग व ऊंचे प्रकार का शस्त्र काम में लाना चाहिए.’

 इस दौर में ज्यादातर लोगों को चार तरह के घरों में जाना बुरा लगता है. एक वे जिनमें जूते बाहर उतार अंदर जाना पड़े. दूसरे वे जहां पैर छूने को परंपरा/संस्कृति की सर्वोत्तम कसौटी माना जाए. तीसरे वे जहां 40 पार का मनुष्य दूसरे 40 पार के मनुष्य को सामने देखते ही चेहरे की झुर्रियों में चिंता भर सिर्फ ‘तबीयत’ से जुड़े सवाल-जवाब करता मिले, ‘कैसी तबीयत है आपकी?’,‘तबीयत ठीक नहीं लग रही, आराम करिए आप’. और फिर चौथे वे घर जहां लोग चेहरे पर, कपड़ों पर और बातों में रुपये-पैसे चिपकाए घूमते-बैठते मिलें. आपका फेसबुक इन चारों तरह के घरों से अलग है. यहां न भेद है, न वेद है. यह यत्र तत्र सर्वत्र है.
इस दौर में ज्यादातर लोगों को चार तरह के घरों में जाना बुरा लगता है. एक वे जिनमें जूते बाहर उतार अंदर जाना पड़े. दूसरे वे जहां पैर छूने को परंपरा/संस्कृति की सर्वोत्तम कसौटी माना जाए. तीसरे वे जहां 40 पार का मनुष्य दूसरे 40 पार के मनुष्य को सामने देखते ही चेहरे की झुर्रियों में चिंता भर सिर्फ ‘तबीयत’ से जुड़े सवाल-जवाब करता मिले, ‘कैसी तबीयत है आपकी?’,‘तबीयत ठीक नहीं लग रही, आराम करिए आप’. और फिर चौथे वे घर जहां लोग चेहरे पर, कपड़ों पर और बातों में रुपये-पैसे चिपकाए घूमते-बैठते मिलें. आपका फेसबुक इन चारों तरह के घरों से अलग है. यहां न भेद है, न वेद है. यह यत्र तत्र सर्वत्र है.


 संगीत, कविता और सिनेमा से गहरा जुड़ाव होने के नाते मुझे जिज्ञासा होती है कि क्या मैं भगत सिंह को इतिहास के पन्नों से कुछ देर के लिए उधार लेकर उनके व्यक्तित्व को एक अलग रोशनी में देख सकता हूं.
संगीत, कविता और सिनेमा से गहरा जुड़ाव होने के नाते मुझे जिज्ञासा होती है कि क्या मैं भगत सिंह को इतिहास के पन्नों से कुछ देर के लिए उधार लेकर उनके व्यक्तित्व को एक अलग रोशनी में देख सकता हूं.
