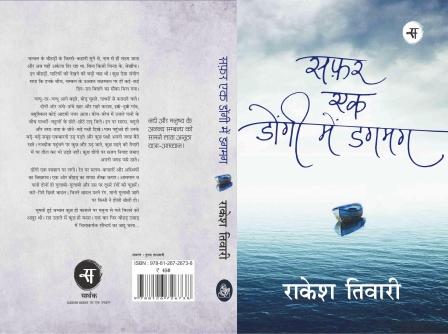पांच साल या हो सकता है कि दो साल में ही, पूरा सीन बदल जाएगा. और बदलेगा इतनी तेजी से और इतना ज्यादा कि शक्लोसूरत पहचान में नहीं आएगी. मेरा अनुमान है कि दो साल के बाद इस देश में कुछ करोड़ लोग पत्रकारिता कर रहे होंगे और 80 फीसदी से ज्यादा पत्रकारों के पास करने के लिए कुछ और काम होगा या कोई काम नहीं होगा. मैं पत्रकारों की नौकरियां जाने की ही बात कर रहा हूं.
अमेरिकी स्कॉलर एन. कूपर ने आज से कुछ साल पहले कहा था, ‘सवाल यह नहीं है कि पत्रकार कौन है. सवाल यह है कि पत्रकारिता कौन कर रहा है.’ क्या वह आदमी पत्रकार माना जाएगा, जिसने राडिया टेप कांड के बारे में, मेनस्ट्रीम कहे जाने वाले मीडिया में, पहली लाइन लिखे या बोले जाने से पहले टेप को यूट्यूब पर डाल दिया था और एक पत्रिका में पहली बार राडिया टेप के बारे में रिपोर्ट होने से पहले लाखों लोगों को पता था कि राडिया टेप कांड हो चुका है और वे इस बारे में कमेंट और जवाबी कमेंट पढ़कर अपना नजरिया भी बना चुके थे. वे किसी के बताने के पहले जान चुके थे कि इस देश में कॉरपोरेट पब्लिक रिलेशन का तंत्र
इतना ताकतवर हो चुका है कि वह केंद्रीय मंत्रिमडल में कौन होगा और कौन नहीं और कौन-सा मंत्री किस विभाग में होगा, आदि तय कर रहा है.
और अगर वह शख्स पत्रकारिता कर रहा था, जिसने राडिया टेप को यूट्यूब में डाला, तो यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि भारत भी करोड़ों पत्रकारों के युग में प्रवेश कर चुका है. पूरी दुनिया में और खासकर पश्चिमी दुनिया में मास मीडिया के क्षेत्र में जो चल रहा है, उसने अब भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया है. जो लोग इस बदलाव को नोटिस नहीं करना चाहते, वे किसी एक दिन जगेंगे, तो उन्हें लगेगा का सब कुछ बदल चुका है.
हालांकि इंटरनेट के जरिए भी, हम तक ज्यादातर समाचार परंपरागत टीवी चैनलों और अखबारों के पोर्टल के जरिए ही पहुंच रहे हैं, फिर भी आज एक आदमी जिसके पास ढाई-तीन हजार रुपये का स्मार्टफोन है और 10 रुपये का इंटरनेट पैक है, वह अपनी किसी सूचना या समाचार को टेक्स्ट, फोटो या वीडियाे के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की ताकत रखता है. हालांकि यह बात सिद्धांत रूप में ही सच है और ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह संभव है. अब देश दुनिया की कई सूचनाएं हम तक इसी तरह पहुंचने लगी हैं.
परंपरागत पत्रकारों के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है. इंटरनेट की वजह से लोग पहले से ही तमाम माध्यमों से खबर लेने में सक्षम हो चुके हैं. ऐसे में करोड़ों पत्रकारों के युग में उनके लिए विश्वसनीय होने और सबसे अलग होने की चुनौती भयंकर शक्ल ले चुकी है. एक दुर्घटना या किसी नेताजी के एक भाषण का जो वीडियो हर किसी के पास है या प्रधानमंत्री का एक ट्वीट जो सबके पास है, उसके बारे में कोई पत्रकार अलग से ऐसा क्या बताएगा, जिसे जानने देखने के लिए एक ग्राहक अखबार खरीदे या टीवी देखे? किसी रैली में सैकड़ों की भीड़ को लाखों की भीड़ बताने के दौर का भी अंत हो चुका है. ऐसा कोई पत्रकार अपनी साख खोने के जोखिम के साथ ही कर सकता है. वर्तमान समय में अगर पत्रकारिता पेशे की इज्जत निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है और पिछले दस साल में जिस भी फिल्म में पत्रकार आया है, वह विलेन या मसखरे की शक्ल में आया है, तो इसकी दर्जनों वजहों में से यह भी एक है कि समाचारों के ग्राहक अब कई माध्यमों के बीच अपना सच चुनने की स्थिति में आ गए हैं.
उपभोक्ताओं के लिए न्यूज कंज्यूम करने का प्लेटफॉर्म लगातार बदल रहा है. मिसाल के तौर पर मेरे अपार्टमेंट में जो न्यूजपेपर एजेंट सारे फ्लैट्स में अखबार देता है, उसने मुझे कुछ दिलचस्प जानकारियां दीं. उसकी दी कई जानकारियों में यह सूचना इस लेख के लिए महत्वपूर्ण है कि 2200 फ्लैट वाले इस अपार्टमेंट में जिन फ्लैट्स में रहने वाले सारे लोग 25 साल से कम उम्र के हैं, वहां कोई अखबार नहीं जाता. जाहिर है, 25 साल से कम उम्र के लोग देश दुनिया की सूचनाओं और समाचारों से अनजान नहीं हैं. शायद वे पुरानी पीढ़ी से ज्यादा अवेयर है, फर्क सिर्फ यह है कि उन लोगों ने सूचनाएं लेने का तरीका बदल लिया है. इन लोगों के लिए सूचनाओं का माध्यम वेब हो चुका है. पूरी दुनिया के साथ भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है.
एक और बदलाव यह है कि सूचनाओं और समाचार का प्राथमिक स्रोत सोशल मीडिया बनता जा रहा है. फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे माध्यम अब बड़ी संख्या में लोगों के लिए वह जरिया बन चुके हैं, जहां उन्हें देश, दुनिया या पड़ोस में होने वाली हलचल की पहली जानकारी मिलती है. ऐसे लोग कई बार न्यूज वेबसाइट पर जाते होंगे और इस बारे में कोई स्टडी नहीं है कि कितने लोग सोशल मीडिया में कोई सूचना पाने के बाद ऐसा नहीं करते. लेकिन सूचना के पहले स्रोत के रूप में सोशल मीडिया का स्थापित होना स्थापित तथ्य बनता जा रहा है. इसके महत्व का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और अब तो कंपनियां भी कई बार अपनी घोषणाएं सबसे पहले सोशल मीडिया पर डाल रही हैं.
एक समय था जब केंद्र सरकार की खबरें मीडिया को देने वाली संस्था प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी पत्रकारों को प्रेस रिलीज जारी करता था. यह रिलीज छपे हुए कागज पर पत्रकारों को मिलती थी. प्रेस रिलीज पाना पत्रकारों का विशेषाधिकार था. इसके बाद वे इस सूचना को अगले दिन अखबारों के जरिए पाठकों को पहुंचाते थे. लेकिन अब अरसा हो चुका है जब पीआईबी पत्रकारों को प्रेस रिलीज जारी करता था. अब प्रेस रिलीज पीआईबी की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं और जिस समय ये रिलीज पत्रकारों को मिलती है, उसी समय दुनिया के हर उस व्यक्ति के पास यह होती है, जिसके पास इंटरनेट है और जिसकी प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो की रिलीज में दिलचस्पी है. कई कंपनियां भी प्रेस रिलीज अपनी साइट पर अपलोड करने लगी हैं. सूचनाओं के सीमित और नियंत्रित प्रवाह के अभ्यस्त पत्रकारों के लिए यह नई और कुछ के लिए तो यह विषम परिस्थिति है.
टीवी पर समाचार अब भी देखा जा रहा है. लेकिन समाचार के परंपरागत अर्थों में देखें तो टीवी का समाचार समाचार नहीं है. वह दरअसल मनोरंजन है और टीवी सीरियल से यह सिर्फ इस मायने में अलग है कि इसमें तात्कालिक सूचनाएं हैं. टीवी समाचारों को लेकर न्यूजरूम की सोच से लेकर उसे पैकेज करने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी शक्ल एंटरटेनमेंट की हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा समय तक टीवी से चिपके रहें. हालांकि इस शक्ल में भी टीवी का समाचार कब तक जिंदा रह पाएगा, इसे लेकर पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता. मनोरंजन के क्षेत्र में टीवी समाचारों का बाकी के मनोरंजन, खेल और फिल्म तथा कार्टून चैनलों के साथ कड़ा मुकाबला है. जिन लोगों ने समाचार के पहले स्रोत के तौर पर वेब को स्वीकार कर लिया है, उनके लिए टीवी समाचारों का समाचार के तौर पर महत्व खत्म हो चुका है. दिल बहलाने के लिए वे बेशक टीवी चैनल देखते हैं.
एक और बड़ा बदलाव जो आते-आते रह गया है और कभी भी आ सकता है, वह है वेब पर न्यूज देखने के लिए ब्रॉडबैंड का फ्री होना. यानी, अब जब आप कुछ खास वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां सर्फिंग करने पर आपका ब्रॉडबैंड खर्च नहीं होगा. ऐसी साइट्स में न्यूज साइट्स भी हो सकती हैं. ‘नेट न्यूट्रलिटी’ के नाम पर भारत के बड़े समाचारपत्र और टीवी समूहों की सामूहिक लॉबिंग की वजह से हालांकि यह होना टल गया है लेकिन परंपरागत मीडिया कॉरपोरेशन इसे कब तक रोक पाएंगे, यह देखना होगा.
देश के ज्यादातर न्यूज चैनल लंबे समय तक फ्री टू एयर रहे और कई न्यूज चैनल अब भी फ्री टू एयर हैं. इन्हें दिखाने के लिए केबल ऑपरेटर या डीटीएच प्लेटफॉर्म कोई फीस नहीं लेते. बल्कि न्यूज चैनल इस बात के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं कि उन्हें दिखाया जाए. इतना खर्च करके एक न्यूज चैनल खुद को फ्री टू एयर बना देता है और दिखाए जाने के लिए केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म को करोड़ो रुपये की फीस भी देता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये चैनल विज्ञापन से कमाई करके उसकी भरपाई करने के मॉडल पर चलते हैं. इसी तरह अखबार भी अपने प्रोडक्शन कॉस्ट के चौथाई से भी कम कीमत पर इसलिए बेचे जाते हैं क्योंकि उनके लिए कमाई का मुख्य स्रोत सर्कुलेशन रेवेन्यू नहीं, बल्कि एड रेवेन्यू है.
टीवी और प्रिंट में जिस तरह फ्री या कम कीमत पर माल बेचने का चलन है, वह वेब पर न हो, इसका कोई कारण नहीं है. ये साइट अपनी कमाई और बाकी खर्च की भरपाई विज्ञापनों से करेंगे. अब कल्पना कीजिए कि फेसबुक जैसी सोशल साइट पर सर्फिंग करने से अगर ब्रॉडबैंड का खर्च न आए और अगर फेसबुक न्यूज देना शुरू कर दे तो? यानी फेसबुक, किसी खबर का लिंक न देकर सीधे सीधे खबर दे और फेसबुक देखने का ब्रॉडबैंड खर्चा जीरो हो तो क्या पत्रकारों की दुनिया वैसी ही रह जाएगी, जैसी अभी है?
मुझे नहीं लगता इसकी वजह यह है कि अपने भारी भरकम यूजर बेस के साथ फेसबुक, न्यूज स्पेस का बड़ा हिस्सा घेर लेगा. वह समाचारों के लिए किसी एक या दो समाचार संकलनकर्ता से समझौता करेगा जिनके साथ वह विज्ञापन रेवेन्यू साझा करेगा या जिनसे वह खबरें खरीद लेगा. इस तरह किसी एक बाजार में दर्जनों चैनलों और अखबारों की जगह एक या दो न्यूज विक्रेता रह जाएंगे, जिनका माल फेसबुक बेचेगा. न्यूज कंज्यूम करने वालों के लिए इसका मतलब यह होगा कि समाचार जानने का उनका खर्च शून्य हो जाएगा बदले में वे विज्ञापन देखेंगे और माल खरीदेंगे. फ्री टू एयर न्यूज चैनलों और लगभग कौड़ियों के मोल मिल रहे अखबारों के जरिए उसके साथ यही हो रहा है. फर्क सिर्फ यह है कि ऐसा ही वेब पर भी हो जाएगा. साथ ही फेसबुक अपने यूजर के सर्फिंग बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उसे प्राथमिकता के आधार पर वैसी खबरें देगा, जिनमें उनकी या उनके दोस्तों की दिलचस्पी है.
पत्रकारों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में चैनल और अखबार बंद होंगे. पत्रकारिता तो फिर भी होती रहेगी. करोड़ों लोग पत्रकारिता कर रहे होंगे. सूचनाओं और समाचारों का प्रवाह पहले से कई गुना बढ़ चुका
होगा. लेकिन पत्रकार के पेशे का आकार बेहद छोटा हो चुका होगा.
पत्रकार महोदय, क्या आप यह सब होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं?
(लेखक इंडिया टुडे के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं और अब भारतीय पत्रकारिता के सामाजिक चरित्र पर जेएनयू में शोधरत हैं)