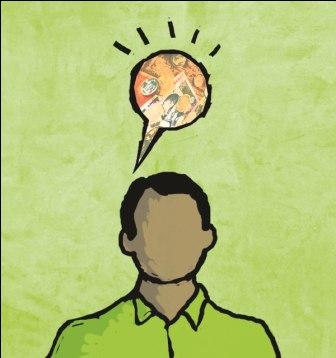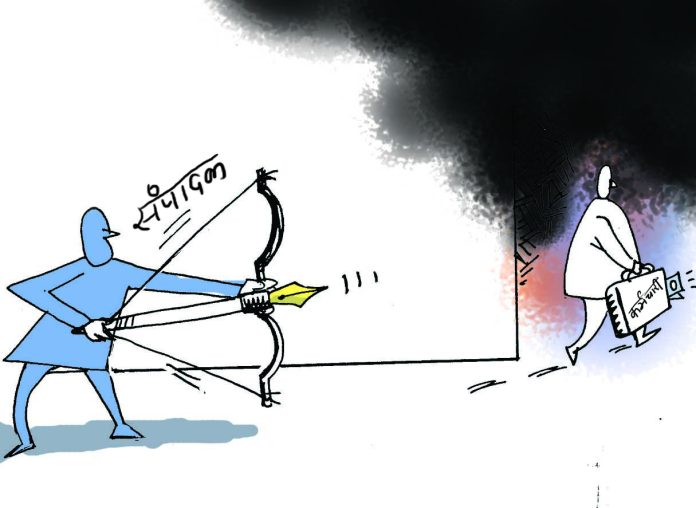इसी वर्ष एक जून को के पत्रकार जगेंद्र को जिस तरह एक मंत्री के आदेश पर जिंदा जला दिया गया, वह दिल दहला देने वाला था. जगेंद्र एक स्वतंत्र पत्रकार थे और उनकी हत्या के आरोपी की मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री हैं. इससे भी जरूरी परिचय ये है कि वे क्षेत्र के खनन माफिया हैं, जिनके खिलाफ जगेंद्र ने लिखने की जुर्रत की थी. परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा. जगेंद्र को जलाकर मार डालने की यह घटना नेताओं, माफियाओं के खिलाफ खड़े पत्रकारों पर दमन की ताजा बर्बर मिसाल है.
इसी वर्ष एक जून को के पत्रकार जगेंद्र को जिस तरह एक मंत्री के आदेश पर जिंदा जला दिया गया, वह दिल दहला देने वाला था. जगेंद्र एक स्वतंत्र पत्रकार थे और उनकी हत्या के आरोपी की मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री हैं. इससे भी जरूरी परिचय ये है कि वे क्षेत्र के खनन माफिया हैं, जिनके खिलाफ जगेंद्र ने लिखने की जुर्रत की थी. परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा. जगेंद्र को जलाकर मार डालने की यह घटना नेताओं, माफियाओं के खिलाफ खड़े पत्रकारों पर दमन की ताजा बर्बर मिसाल है.
2009 में जब पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में छत्रधर महतो के संगठन ने आताताई सरकार को वहां से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था, उसी संदर्भ में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने खुलेआम धमकी दी थी कि छत्रधर महतो और उनके पक्ष में लिखने-बोलने वालों पर भी यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून) लगाया जाएगा. यह धमकी सीधे-सीधे मानवाधिकार कर्मियों के साथ पत्रकारों को भी थी. 2010 की फरवरी में जब यूपी एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया तो उनके सवाल थे-
‘लालगढ़ की घटना के लिए मुख्य तौर पर आप किसे जिम्मेदार मानती हैं?’
‘आपने लालगढ़ पर ही क्यों लिखा, कोई दूसरा विषय नहीं था?’
मुझे तुरंत चिदंबरम की धमकी याद आई थी. इसके अलावा कुछ और सवाल थे-
‘घूरपुर के किन-किन गांवों में गई हैं?’(इलाहाबाद का यह क्षेत्र यमुना के किनारे है और खनन माफियाओं के खिलाफ पारंपरिक बालू मजदूरों और उनके आंदोलनों के लिए जाना जाता है, जिस पर मैंने लेख लिखा और इनका पक्ष भी लिया)
‘एआईकेएमएस से आपका क्या रिश्ता है?’ (ये बालू मजदूरों का संगठन है)
‘दस्तक (पत्रिका, जिसे मैं अन्य लोगों के सहयोग से निकालती हूं) का सर्कुलेशन कहां-कहां हैं?’
‘बलिया और फर्रूखाबाद (जहां मैं गंगा एक्सप्रेस वे और इसके खिलाफ होने वाले आंदोलनों के बारे में जानने और लिखने के लिए गई थी) में किस-किस को जानती हैं?’
‘महिला मुद्दे तो ठीक हैं, लेकिन आप दलितों और मुसलमानों के मुद्दों पर क्यों लिखती हैं?’
ध्यान दें, ये सारे सवाल मेरे पत्रकारिता जीवन से जुड़े सवाल हैं, न कि मेरे माओवादी होने या न होने से. गिरफ्तारी के तुरंत पहले मैंने आपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ एक पुस्तिका भी निकाली थी, जिसका शीर्षक था ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट : आदिवासियों को उजाड़ने की साजिश, समस्या कौन, माओवादी या भारतीय राज्य.’ यह शीर्षक दरअसल हिमांशु कुमार के एक लेख का है. इस पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम के दौरान ही मैं निशाने पर आ गई थी और मुझे मेरे फोन रिकॉर्ड होने के संकेत मिलने लगे थे. गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछे उससे जाहिर है कि उन्हें समस्या मेरे माओवादी होने की नहीं थी, बल्कि पत्रकार होने से थी. ऐसी पत्रकार जिसके लेख उनके लिए असुविधाजनक स्थितियां खड़ी कर रहे थे.
मेरी गिरफ्तारी के बाद एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में बरखा दत्त ने तत्कालीन मंत्री मणिशंकर अय्यर से सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश की एक पत्रकार सीमा आजाद को यह आरोप लगाकर जेल में डाला गया है कि उसके पास से माओवादी साहित्य मिला है, न कि कोई हथियार. हम पत्रकार साक्षात्कार के लिए या लेख लिखने के लिए माओवादियों या अलगाववादियों से मिलते भी हैं और उनका साहित्य भी पढ़ते हैं. इस तरह तो हम सभी खतरे में हैं? जवाब में मणिशंकर अय्यर ने जो कहा वह महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, ‘गैरकानूनी साहित्य रखना हथियार रखने से भी बड़ा अपराध है. हमें ये अंतर समझना होगा कि हथियार उतना खतरनाक नहीं है, जितना कि विचार.’ मणिशंकर अय्यर का यह वक्तव्य स्पष्ट कर देता है कि सरकारें और उनके बनाए कानून लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कैसे सोचते और काम करते हैं. इस तरह इनके निशाने पर पत्रकारों का एक समूह हमेशा ही रहेगा, जो उनसे विरोधी विचार रखता है.
वास्तव में पत्रकार जब कुछ लिख रहा होता है तो वह किसी न किसी विचार को ही फैला रहा होता है. जब यह विचार सरकारों के विचार से मेल खाता है तो उस पत्रकार को पुरस्कारों और दूसरी बहुत-सी सुविधाओं से नवाजा जाता है और जब ये विचार सरकारों के विरोध में होती हैं तो उन्हें धमकी मिलती है, धक्के खाने पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है, कई बार तो जान से हाथ भी धोना पड़ता है. पिछले 25-30 सालों से सरकारों की आर्थिक नीतियां जितनी आक्रामक होती जा रही हैं, पत्रकार इनका दो तरीकों से शिकार हो रहे हैं. पहला ऐसे कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने मालिक के गुलाम बनाए जा रहे हैं, उनकी छंटनी, बेगारी कराने और तमाम सुविधाओं को छीने जाने की तलवार ज्यादा धारदार होती जा रही है. दूसरी ओर वे सरकारों का सीधा शिकार भी हो रहे है. यानी निशाने पर सिर्फ जनद्रोही नीतियों की मुखालफत करने वाले सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि सच कहने वाला पत्रकार भी हैं.
व्यापमं मामले में अन्य लोगों के अतिरिक्त इस पर खोजी रिपोर्टिंग करने गए दो पत्रकारों की रहस्यमय मौत का मामला अभी ताजा ही है. इसके पहले भी पत्रकारों के दमन का सिलसिला है. कुछ सालों का ही उदाहरण देख लें तो 2014 के सितंबर महीने में गुवाहाटी से एक टीवी पत्रकार जैकलांग ब्रह्मा को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के कुछ ही दिन पहले उन्होंने ‘डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ असम’ के एक धड़े के कमांडर का साक्षात्कार लिया था. पुलिस का आरोप है कि जैकलांग इसी संगठन से जुड़ाव रखते हैं.
2002 में कश्मीर टाइम्स के पत्रकार इफ्तिखार गिलानी को आईएसआई का एजेंट बताकर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से ऐसे दस्तावेज होने का हौव्वा बनाया गया, जो वास्तव में भारतीय कानून की नजर में भी गैरकानूनी नहीं थे.
2008 की जनवरी में रायपुर के एक पत्रकार प्रफुल्ल झा को गिरफ्तार कर कहा गया कि वे माओवादियों के शहरी नेटवर्क को खड़ा करने में सहयोगी थे. इस मामले में वे 7 साल सजा काटने के बाद इसी साल की शुरुआत में बाहर आए हैं. उन्हें सजा दिलाकर संतुष्ट होने के बाद पुलिस ने बयान दिया कि प्रफुल्ल माओवादी नहीं हैं, उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया था ताकि इससे दूसरों को सबक मिल सके.
2008 के ही मार्च महीने में तमिलनाडु के पत्रकार जयप्रकाश सित्ताम्पलम को गिरफ्तार किया गया. वे संडे टाइम्स से जुड़े तमिलनाडु के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं. उन पर लिट्टे से संबंध रखने का आरोप लगाकर राज्य की सरकार ने न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि 20 साल की सजा भी सुनाई. इस सजा की आलोचना तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी की.
2008 में ही देहरादून के पत्रकार प्रशांत राही को गिरफ्तार कर लिया गया. वे सालों तक ‘स्टेट्समैन’ से जुड़े रहे और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस समय वे पत्रकार से ‘एक्टिविस्ट’ की भूमिका में आ चुके थे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि पत्रकार के तौर पर वे समाज परिवर्तन का जमीनी काम नहीं कर पा रहे हैं. सरकारों के लिए यह ‘नीम चढ़े करेले’ जैसा था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर तमाम फर्जी आरोपों से नवाज दिया.
उत्तराखंड के ही पत्रकार हेम चंद्र पांडेय को तो गिरफ्तार करने की बजाय सीधे मार डाला गया. मारे जाने के समय हेम माओवादी पार्टी के नेता आजाद के साथ थे. दोनों को पकड़कर ठंडे दिमाग से मारा गया और इसे मुठभेड़ का नाम दिया गया. सरकारी निजाम इसकी जांच कराने को भी तैयार नहीं हुआ. हेम को भी पहले माओवादी ही बताया गया, जब लोगों ने उसे पहचाना तब सरकार ने माना कि वो दिल्ली का एक उभरता हुआ पत्रकार था. गौरतलब है कि हेम चंद्र के लिखे और छपे लेखों में एक लेख का शीर्षक था ‘पत्रकारिता का पेशा हुआ जोखिम भरा’. इस जोखिम को समझते हुए भी उसने माओवादी नेता आजाद से मिलने की हिम्मत की और सरकारी गोली का शिकार हुआ.
इनके अलावा भी ऐसे न जाने कितने पत्रकार होंगे जिन्हें अनाम रहते हुए ही कुचल दिया गया. जरूरी नहीं कि उन्हें जेलों में ठूंसकर या उनकी हत्या कर ही कुचला गया हो, बल्कि इस बात का खौफ दिखाकर भी न जाने कितने साहसी और समाजोपयोगी पत्रकारों को आकार लेने के पहले ही खत्म कर दिया गया होगा. इनकी जगह जिन पत्रकारों का जन्म हुआ, उनसे कौन-से समाज को लाभ मिल रहा है, ये आसानी से समझा जा सकता है. यह पूरी एक व्यवस्था है जो ऐसे पत्रकारों को जन्म देती है, जिनका मकसद पत्रकारिता से सिर्फ कमाई करना ही नहीं, बल्कि ‘पैसे बनाना’ है. पत्रकारिता के पेशे में आए ज्यादातर नौजवान आदर्शवादी ही होते हैं. सच लिखना, सच लिखकर नेताओं की पोल खोलना, समाज में परिवर्तन लाना आदि ज्यादातर नवागंतुक पत्रकारों का सपना होता है लेकिन इनमें से ज्यादातर के आदर्शों का हरण हो जाता है और उनकी पत्रकारिता का क्षरण. इनमें से कई तो पत्रकार से दलाल की भूमिका में आ जाते हैं, खबरों की दलाली शुरू कर देते हैं. मैंने अपने इर्द-गिर्द भी ऐसे पत्रकारों को बनते देखा है.
अपनी पत्रकारिता की शुरुआत मैंने देहरादून से की थी. जिस समय मैं वहां के एक अखबार से जुड़ी, तीन लोग और जुड़े. हम सब एक जैसी स्थिति वाले लोग ही थे. हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, रिपोर्टिंग के लिए टेम्पो से ही जाया करते थे. मेरे साथ दो लड़के जो क्राइम रिपोर्टर थे. उनमें से एक ने एक-दो महीने के भीतर ही अपने पैसे से बाइक खरीद ली, जबकि हमारी तनख्वाह इतनी थी ही नहीं. कुछ दिन बाद जब हम सबमें अच्छी दोस्ती हो गई तो उसने मुझे इसका राज बताया कि ये गाड़ी उसने पुलिस वालों की मदद से खरीदी है जिनकी खबरें वह उनके अनुसार ही लिखा करता है. जब मैंने आश्चर्य जताया और इसे गलत बताया तो उसने कहा कि तुम ऐसे ही रह जाओगी. कुछ दिन बाद मेरी साइकिल चोरी हो गई, मैंने उसे ये बात बताई तो उसने कहा कि तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया. मैंने कहा कि अरे इतने दिन बीत गए अब उसे पुलिस भी नहीं खोज सकेगी. उसने हंसते हुए कहा, ‘अरे तुम्हारी वाली नहीं मिलेगी तो, दूसरी दिला दूंगा पुलिस वालों से.’ मैंने मना कर दिया पर उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं उस वक्त आश्चर्य में पड़ जाती थी. उस वक्त मैं इतनी समझदार भी नहीं थी कि इन बातों का सही विश्लेषण कर पाती, पर इस रास्ते की ओर मेरा आकर्षण कभी नहीं बना. मुझे मेरी मेहनत से लिखे लेखों को छपा हुआ देखना ही अच्छा लगता था. प्रशांत राही उस वक्त देहरादून में स्टेट्समैन में पत्रकार थे. उनसे भी मेरी जान-पहचान थी. वे भी मुझे लेखों के विषय पढ़ने और लिखने के लिए सुझाया करते थे. उस वक्त देहरादून का मुख्य डाकघर ही उनका ऑफिस हुआ करता था, जहां से वे अपनी खबरें लिखकर अखबार को भेजा करते थे. वे पत्रकारों के घुमंतू और ‘जगलर’ घेरे से दूर रहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कम ही जाते थे. जब मेरी उनसे दोस्ती हो गई तो वे मुझे भी इनसे दूर रहने को कहते थे. इस कारण ज्यादातर पत्रकार प्रशांत को पसंद नहीं करते थे, उन्हें घमंडी कहते थे. मैं क्योंकि इस क्षेत्र में नई थी, इसलिए मुझे तो इनका घेरा आकर्षित करता था लेकिन जब उनकी चर्चा का स्तर देखती थी, तो प्रशांत राही की हिदायत सही भी लगती थी. मैं इन दोनों के बीच झूलती रही. अब जबकि मैं दूर खड़ी होकर अपने पत्रकारी जीवन की इस शुरुआत को देखती हूं तो लगता है कि प्रशांत की बात सही थी, लेकिन उनके बीच रहकर मुझे जो अनुभव मिला वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है. शायद हर नया पत्रकार इसी उधेड़बुन से गुजरता होगा और अपना रास्ता चुनता होगा कि उसे कैसा पत्रकार बनना है. सच को सामने लाने के खतरे उठाने वाला, सुरक्षित रहते हुए सिर्फ नौकरी करने वाला या पत्रकारिता से पैसे बनाने वाला.
किताबों में पत्रकारों को तटस्थ रहना सिखाया जाता है. वास्तव में उन्हें तटस्थता के नाम पर समाज से कटे रहना सिखाया जाता है लेकिन जमीन पर ‘तटस्थता’ जैसी कोई स्थिति होती नहीं है. जब पूरा समाज पक्षों में बंटा हो तो पत्रकार कैसे तटस्थ हो सकता है. उसे सही या गलत कोई पक्ष चुनना ही होता है, तभी न केवल वह अच्छा और बौद्घिक पत्रकार बन सकता है बल्कि सिर्फ तभी वह सही रिपोर्टिंग भी कर सकता है. वास्तव में ‘तटस्थता’ भी अपने आप में एक पक्ष है, जो इस संदर्भ में ज्यादातर नकारात्मक होती है. पत्रकारिता में प्रगतिशीलता तटस्थता का दूसरा पक्ष है.
इससे ही जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सच लिखने वाले नेताओं, माफियाओं, नौकरशाहों की पोल खोलने वाले पत्रकारों का दायरा इतने दमन के बीच भी अपने काम में मुस्तैदी से लगा है. ऐसे पत्रकारों की एक खेप हर साल आती है. वास्तव में यह देखना महत्वपूर्ण है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों के चलते सच लिखना उतना मुश्किल भी नहीं है और सच लिखने वाले बहुत से पत्रकार आज बेहद सफल भी है. उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है. सरकारों को उनसे कोई खास शिकायत भी नहीं होती है. थोड़ी असुविधा भले ही हो सकती है. उसे समस्या तभी लगती है, जब पत्रकार सच लिखने के साथ-साथ सरकार विरोधी आंदोलनों की आवाज बनने लगता है. जब उसके लिखे द्वारा आंदोलन की खबरें फैलने लगती हैं, तब उसका काम सरकार विरोधी मान लिया जाता है और उसकी सजा दी जाती है, जो जेल से लेकर मौत तक हो सकती है. ऊपर जितने पत्रकारों का जिक्र है उनसे सरकारों को यही खतरा था. यह खतरा सिर्फ भारत की सरकार को ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों को है.
‘कमेटी फॉर प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट’ के मुताबिक सन 2014 में पूरी दुनिया में कुल 221 पत्रकारों को जेल भेजा गया. 2013 में 211 और 2012 में 232 पत्रकारों को. इनमें से ज्यादातर सरकार की अलोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ और आंदोलनों के पक्ष में लिखने वाले पत्रकार हैं. यानी खतरा ऐसे पत्रकारों से ही है जो आंदोलन का बीज बोते हैं या उसका परागण करते हैं. देश में आजादी की लड़ाई के समय में भी इस तरह के पत्रकार मौजूद थे जिन्होंने इसका दंश झेला. आज भी इस खतरे को उठाते हुए बहुत से पत्रकार इस जमात में शामिल हो रहे है और इसे मजबूत कर रहे हैं. वर्ना पत्रकारिता की जो स्थिति है उसे देखते हुए उसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहे जाने पर ही कई सवाल खड़े होते हैं. जैसे- वो कैसा लोकतंत्र है जिसके लिए मीडिया जगत खंभा बना हुआ है? वास्तव में वो कौन हैं जो इस खंभे की नींव हैं- मीडिया के कॉरपोरेट घराने या पत्रकार? पत्रकारों को इस लोकतंत्र के लिए खंभा बने रहना आवश्यक है या इसे कंधा देना? आखिर में- इस खंभे का बने रहना जरूरी है या इसका ढह जाना, ताकि नए सिरे से इसकी बुनियाद रखी जा सके? पत्रकारों को इन सभी सवालों पर सोच कर अपनी पत्रकारिता की दिशा और अपना भविष्य चुनना है.
(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)