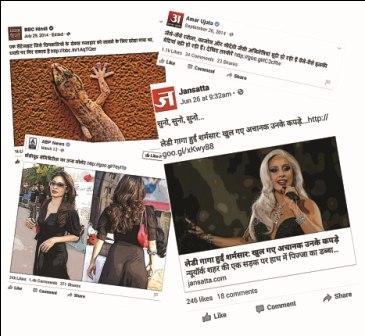बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि प्रसारण पत्रकारिता के इतिहास के सबसे बड़े क्षण ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया था. 1967 में डेविड फ्रॉस्ट अपने शो ‘फ्रॉस्ट प्रोग्राम’ में एमिल सवुंद्रा से सवाल-जवाब कर रहे थे. सवुंद्रा श्रीलंकाई काले बाजार के एक व्यापारी थे जिन पर उस वक्त एक बड़े मोटर इंश्योरेंस घोटाले का आरोप था. सवुंद्रा इस घोटाले को लेकर खबरों में थे और इस प्रोग्राम में ये सोचकर आए थे कि उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ अपना पक्ष जनता के सामने रखने का मौका मिलेगा. पर हुआ इसके उलट. फ्रॉस्ट के आक्रामक सवालों के सामने सवुंद्रा टिक नहीं पाए. इंटरव्यू शुरू हुए दस ही मिनट हुए थे कि फ्रॉस्ट के सवालों में उलझे सवुंद्रा ये कह गए कि उनकी किसी के भी प्रति कोई कानूनी या नैतिक जिम्मेदारी नहीं है. जहां सवुंद्रा को इस बात के लिए दर्शकों का गुस्सा झेलना पड़ा वहीं फ्रॉस्ट की इस पर की गई गुस्से भरी प्रतिक्रियाओं को दर्शकों की तालियां मिलीं. जनता को न केवल ये लगा कि फ्रॉस्ट इस मामले के पारखी हैं बल्कि सवुंद्रा के जवाबों पर फ्रॉस्ट की गुस्से भरी प्रतिक्रियाओं से उन्हें लगा कि फ्रॉस्ट उनमें से ही एक हैं. इस कार्यक्रम के कुछ महीनों बाद सवुंद्रा को अपराधी घोषित कर जेल भेज दिया गया और फ्रॉस्ट अपने टीवी पत्रकारिता के कॅरिअर में सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे.
जब टीवी पत्रकारिता में हुई इस ऐतिहासिक घटना ने लोगों को प्रभावित किया, तब मीडिया और बाहरी दुनिया में टेलीविजन पर होने वाले बर्ताव और अदालती मुकदमे जैसी पूछताछ से उपजी गलतफहमियों से शो के निर्माताओं ने शो के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी. और इसी तरह पहली बार ‘ट्रायल बाय टेलीविजन’ शब्द चलन में आया.
उस समय फ्रॉस्ट को निजी सवाल पूछने के कारण, एक कठिन साक्षात्कारकर्ता का जो तमगा मिला था, आज दशकों बाद टीवी पर रोज होने वाली बहसों को देखते हुए हम उसकी जटिलताएं समझ सकते हैं. मीडिया के ऐसे व्यवहार पर चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है जब हाल ही में पत्रकार अविरूक सेन की किताब ‘आरुषि’ सामने आई. ये किताब देश की सबसे बड़ी ‘मर्डर मिस्ट्री’ कहे गए आरुषि तलवार हत्याकांड पर बात करती है.
2008 में 14 साल की आरुषि की संदिग्ध मौत ने देशभर का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. इसके पीछे कौन था, ये आज तक एक पहेली बना हुआ है. बहुत-सी बातें किसी जासूसी उपन्यास के रहस्य की तरह आज भी अबूझ हैं, जैसे कि क्यों बस एक दीवार के फासले पर सोए आरुषि के माता-पिता को उसकी हत्या का पता नहीं चला, घर के नौकर हेमराज की हत्या कैसे और किसने की और कैसे उसकी लाश छत पर पहुंच गई?
ये हत्याकांड सुर्खियों में ही था जब तलवार दंपति पर ही उंगलियां उठने लगीं. फिर जल्द ही नई बहसों का जन्म हुआ और विशेषज्ञों, जिनमें नामी लेखिका शोभा डे भी शामिल थीं, ने तलवार दंपति के खिलाफ स्पष्ट निर्णय दे दिया. कुछ ने आरुषि को उच्छृंखल कहा तो कुछ का ये भी कहना था कि ये ‘ऑनर किलिंग’ का मामला है. ये भी कहा गया कि तलवार दंपति दिल्ली के एक विशिष्ट ‘वाइफ स्वैपिंग क्लब’ के सदस्य थे. एक चैनल ने तो सभी हदें पार कर दीं, बाल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने एक एमएमएस क्लिपिंग दिखाई जिसमें एक किशोर लड़की कैमरे के सामने अपने कपड़े उतार रही थी. चैनल का दावा था कि ये बच्ची आरुषि है.

जहां एक तरफ ये ‘कामुक सुर्खियां’ खबर बना रही थीं, जांच एजेंसियों की बताई कहानियां भी कुछ ऐसी ही थीं. ऐसा लग रहा था कि अपने ‘अनाम सूत्रों’ से प्राप्त ‘एक्सक्लूसिव’ खबरों को चलाने वाले चैनल इन जांच एजेंसियों के प्रवक्ता के रूप में ही ये बात कह रहे थे. इस तरह मीडिया ने घोषित किया कि आरुषि के माता-पिता ‘दोषी’ हैं और नवंबर 2013 में अदालत ने भी उन्हें दोषी करार दिया.
हालांकि तलवार दंपत्ति के दोषी या निर्दोष होने पर कोई टिप्पणी करना अनजाने में ही पूर्वाग्रहों के हिसाब से चलना होगा, पर मीडिया द्वारा जनता में फैलाई गई राय से प्रभावित होकर अदालत के फैसला सुनाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता. पत्रकार और ‘आरुषि’ किताब के लेखक अविरूक सेन ‘तहलका’ को बताते हैं, ‘जब तक ‘मुंबई मिरर’ ने 2012 में मुझे इस केस के ट्रायल के बारे में लिखने की जिम्मेदारी नहीं दी थी, मेरी इस मामले के बारे में कोई राय नहीं थी, सिवाय इसके कि उसके माता-पिता ने ही ये अपराध किया होगा क्योंकि पूरा मीडिया यही कह रहा था. इस बात ने जनता और मामले के प्रमुख लोगों को भी प्रभावित किया ही होगा और चाहें ये जांच एजेंसियां हों या अदालत, वे भी तो इसी जनता में ही आते हैं. ऐसे में हम इस केस में मीडिया के प्रभाव को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते.’
मार्च 2015 में, दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड पर आधारित लेस्ली उडविन की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया’ज डॉटर’ ने देशभर में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर बैन लगाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कहने वाली एक याचिका की सुनवाई में कहा था, ‘मीडिया ट्रायल जजों को प्रभावित करने का माद्दा रखते हैं. इससे अप्रत्यक्ष रूप से एक दबाव बनता है जिससे आरोपी/अपराधी की सजा का निर्णय प्रभावित होता है.’
याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि किसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने से मीडिया द्वारा विचाराधीन मामलों में झूठी रिपोर्ट आने की संभावना बढ़ जाएगी और कोर्ट ने ये माना भी कि कैसे पहले ये अलिखित कोड था कि विचाराधीन मामलों के बारे में रिपोर्ट नहीं की जाएगी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं माना जाता.
इसी तरह 17वें विधि आयोग में अपनी 200वीं रिपोर्ट में मीडिया ट्रायल और खबरों की अधिकता के भविष्य को देखते हुए केंद्र से ये सिफारिश की थी कि किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी के गिरफ्तार होने से लेकर फैसला आ जाने तक किसी भी तरह की रिपोर्टिंग करने से मीडिया पर रोक होनी चाहिए, ताकि आरोपी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी भी मीडिया माध्यम को किसी आपराधिक मामले के बारे में कोई भी प्रकाशन या प्रसारण को निर्देशित करने का अधिकार हाईकोर्ट को होना चाहिए. साथ ही मीडिया द्वारा ऐसे किसी मामले के प्रयोग को नियंत्रित करने का अधिकार भी हाईकोर्ट को होना चाहिए. आयोग ने कहा, ‘आजकल टेलीविजन और केबल के बढ़ते व्यापक प्रसार में समाचार प्रकाशन का स्वरूप बदल गया है और ऐसे कई प्रकाशन संदिग्धों, आरोपियों, गवाहों यहां तक कि जजों यानी पूरे न्याय तंत्र को भी प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकते हैं.’
जहां एक ओर तलवार दंपति के मामले को भारतीय प्रेस काउंसिल ने मीडिया द्वारा लोगों पर नकारात्मक प्रभाव बनाने के रूप में देखा, वहीं एसएआर गिलानी के विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले और खुर्शीद अनवर पर यौन उत्पीड़न के आरोप, दो ऐसी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ रहे जिन्होंने मीडिया के प्रति विश्वास को ‘ब्रेक’ यानी तोड़कर रख दिया. 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर पांच आतंकियों द्वारा किए गए हमले के दूसरे ही दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दावा किया कि उन्होंने इस हमले में शामिल कई संदिग्धों को ढूंढ लिया है. इस मामले में उन्होंने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें चार कश्मीरी शामिल थे- दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसएआर गिलानी, शौकत हुसैन गुरु और मोहम्मद अफजल गुरु व अफज़ल की पत्नी अफ्जान.
उनकी गिरफ्तारी से पहले ही मीडिया में उनके अपराध के विवरण के साथ उनके कुबूलनामे की खबरें आ चुकी थीं. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ ने लिखा था कि ‘आतंकवादियों’ ने पाकिस्तान के नंबर पर फोन कॉल करने से पहले गिलानी को कॉल किया था, वहीं ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की हेडलाइन में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को आतंकी योजनाओं का सरगना कहा गया था. जहां ऐसी खबरों ने पहले ही संदिग्धों के खिलाफ एक राय कायम कर दी थी, जी न्यूज के डॉक्यू ड्रामा ‘13 दिसंबर’, जिसमें संसद हमले के पूरे घटनाक्रम का नाट्य रूपांतरण किया गया था, को सरकार की सहमति और समर्थन के बाद प्रसारित किया गया जिसने इन संदिग्धों को आतंकवादी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
जब हाईकोर्ट को गिलानी पर लगे इन आरोपों को साबित करने वाला कोई तथ्य नहीं मिला तो उन्होंने गिलानी और अफ्जान को बरी कर दिया, मगर तब तक बरी हो चुके इन लोगों के लिए अपनी सामान्य जिंदगी में लौटना नामुमकिन हो चुका था. क्या कोर्ट के इन्हें बेगुनाह मानने के बाद लोगों की इनके बारे में राय बदल सकती थी? क्या मीडिया संस्थान अपनी कहानियां वापस ले सकते थे? क्या वो तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के लिए गिलानी से माफी मांग सकते थे? अफजल इस मामले में बदकिस्मत रहे कि अपनी बेगुनाही साबित कर बरी हो पाने के लिए उन्हें पर्याप्त सुबूत नहीं मिले, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि उन्हें ‘सामूहिक अंतःकरण की संतुष्टि’ के लिए मरना ही होगा. अफजल के खिलाफ मीडिया द्वारा हुईं चूकों ने जिस सामूहिक विवेक को जन्म दिया वो दिखाता है कि कैसे प्रेस किसी व्यक्ति के जीने-मरने को प्रभावित कर सकता है.
2013 में इसी तरह का एक और निंदा अभियान टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर तब चला जब ‘इंस्टिट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी’ नाम के एक एनजीओ के कार्यकारी निदेशक खुर्शीद अनवर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे. जबकि इन आरोपों की सच्चाई पर ही संदेह था. सोशल मीडिया और इंडिया टीवी पर लगातार इस मुद्दे पर हो रही बहस ने खुर्शीद अनवर को अपनी जिंदगी खत्म कर देने जैसा गंभीर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया. मीडिया ने आरोपों के आधार पर ही उन्हें बलात्कारी घोषित कर दिया. इंडिया टीवी ने तो अभियान ही शुरू कर दिया था, जिसमें बार-बार ‘औरतों पर अन्याय को बढ़ावा देने वाले आदमी को सजा मिलनी चाहिए’ जैसी बातें पूरी उत्तेजना के साथ कही जा रही थीं, इसके बाद ही खुर्शीद ने अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी.
अनवर के शुभचिंतकों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों आदि ने मीडिया द्वारा एफआईआर से पहले ही अनवर को बलात्कारी घोषित कर देने की घोर निंदा की. एक फोरम ‘जस्टिस फॉर खुर्शीद अनवर’ की सदस्य अंकिता चंद्रनाथ बताती हैं, ‘रजत शर्मा द्वारा इंडिया टीवी पर अनवर द्वारा किए गए कथित बलात्कार की रिपोर्ट निर्भया कांड के ठीक एक साल बाद पेश की गई थी. मीडिया को दिसंबर तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी जब कथित बलात्कार का मामला सितंबर की शुरुआत का था? इंडिया टीवी की रिपोर्ट पूरी तरह से एकपक्षीय थी. यहां तक कि उस लड़की का अनवर के खिलाफ बयान हद दर्जे तक संपादित था, साथ ही चैनल आक्रामक रूप से उसे ‘दूसरी निर्भया’ के नाम से प्रसारित कर रहा था.’ 2008 में हुए मुंबई हमले की बात करें तो उस समय ऐसी खबरें भी आई थीं कि सेना की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आतंक फैलाने वालों के आका देखकर आतंकियों को निर्देश दे रहे थे. इसी तरह पिछले दिनों गुरदासपुर में हुई आतंकी वारदात के समय खुफिया विभागों को समाचार चैनलों से सीधा प्रसारण न करने की अपील करनी पड़ी थी. ऐसे में मीडिया संस्थानों को इस बात पर भी सोचने और ध्यान देने की जरूरत है कि उनकी सीमाएं किस हद तक हैं और कहीं इससे किसी व्यक्ति विशेष या फिर राष्ट्र का हित तो नहीं प्रभावित हो रहा है.
विश्वस्त सूत्रों के हवाले से
दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, ‘अकेले रिपोर्टर को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता. सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता इसके खतरों के बावजूद खबरें इकठ्ठा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है. और जहां संवाददाताओं की अपराध की वास्तविक स्थिति तक सीधी पहुंच नहीं है, तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है, वहां उन्हें अधिकारियों द्वारा उनके हितों के अनुरूप चुने गए तथ्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है. तथ्यों की इस चयनात्मक प्रस्तुति से कई बार बड़े नाटकीय निष्कर्ष निकलते हैं. एक टीवी न्यूजरूम के अंदर जो कहानियां हेडलाइन बनती हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं. अगर एक चैनल किसी घटना पर संतुलित रिपोर्ट दिखाता है और दूसरा चैनल उसी खबर को सनसनीखेज तरीके से दिखाता है तो दर्शकों का ध्यान उस सनसनीखेज रिपोर्ट पर ही जाएगा, जिससे टीआरपी भी बढ़ती है और साथ ही विज्ञापनों से आने वाला धन भी. कॉरपोरेट घरानों द्वारा चलाए जा रहे इस क्षेत्र में कई बार रिपोर्टरों को अनाम स्रोतों के नाम पर ऐसी कहानियां गढ़ने को कहा जाता है, जिससे चैनल की टीआरपी बढ़ाई जा सके. यहां पर इन अनाम सूत्रों पर भी सवाल उठता है, जिन्हें अमूमन ‘उच्च पदस्थ’ बताया जाता है. सरकारी महकमों के सूत्र सामान्यतया अपना नाम बताने से बचते हैं, ऐसे में कहानियां गढ़ने में और आसानी हो जाती है.
वर्तमान में मीडिया के किसी हत्या, बलात्कार की रिपोर्टिंग में लांघी गई नैतिकता की सीमाओं के एवज में चैनल सिर्फ चुप्पी साध लेता है.
[box]
जहां निभाई महत्वपूर्ण भूमिका
भारतीय मीडिया संस्थान केवल सनसनीखेज खबरें देते हैं ये कहना भी सही नहीं होगा. चार ऐसे मामले जहां न्याय की लड़ाई में पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
- जेसिकालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी को बरी करने के विरोध में एक अनाम एसएमएस विभिन्न मीडिया संस्थानों में पहुंचा और मीडिया के ढेरों लोग इंडिया गेट पर कैंडल लाइट मार्च के रूप अपना विरोध दर्ज कराने पहुंच गए. 1999 में दिल्ली के एक रेस्तरां-बार में हरियाणा के एक सांसद के बेटे मनु शर्मा ने 200 लोगों के सामने जेसिकालाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने देर रात शराब परोसने से मना कर दिया था. इस हाई प्रोफाइल मामले में मीडिया द्वारा बनाए गए दबाव के फलस्वरूप अदालत ने उसके सांसद पिता के प्रभाव को नजरअंदाज करके सजा सुनाई थी.
- नीतीश कटारा की उस समय हत्या कर दी गई जब उनके भारती यादव से प्रेम संबंध के बारे में भारती के घरवालों को पता चला. 2002 में हुआ यह मामला ऑनर किलिंग का था. उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटों विशाल और विकास यादव ने नीतीश की हत्या की क्योंकि वे अलग जाति के थे. विकास यादव इस मामले में अपने पिता के प्रभाव के कारण साफ बचकर निकल गए होते अगर एनडीटीवी चैनल उसके इकबाल-ए-जुर्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने नहीं लाया होता.
- एस. मंजूनाथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में ग्रेड ‘ए’ के अधिकारी थे . 2005 में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मंजूनाथ ने दो पेट्रोल पंपों को मिलावटी पेट्रोल बेचने के संदेह के चलते सील कर दिया था. मंजूनाथ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वे महीने भर पहले ही खुले एक पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण करने से पहुंच गए थे. इस केस में पेट्रोल पंप के मालिक पवन कुमार मित्तल सहित छह लोगों को दोषी घोषित किया गया. मंजूनाथ को मिले इसे न्याय का श्रेय उन कार्यकर्ताओं और मंजूनाथ षणमुगम ट्रस्ट को जाता है जिन्होंने इतने लंबे समय तक इस केस को जिंदा रखा.
- संजीव नंदा को 1999 के हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई पर 2 साल बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया. नशे में धुत संजीव ने तीन पुलिसकर्मियों सहित छह लोगों को बीएमडब्ल्यू कार से कुचल दिया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. यदि मीडिया का दबाव न होता तो अपने दादा एसएम नंदा (पूर्व नेवी प्रमुख) के रसूख के चलते संजीव को बरी कर दिया गया होता.
निकिता लांबा
[/box]
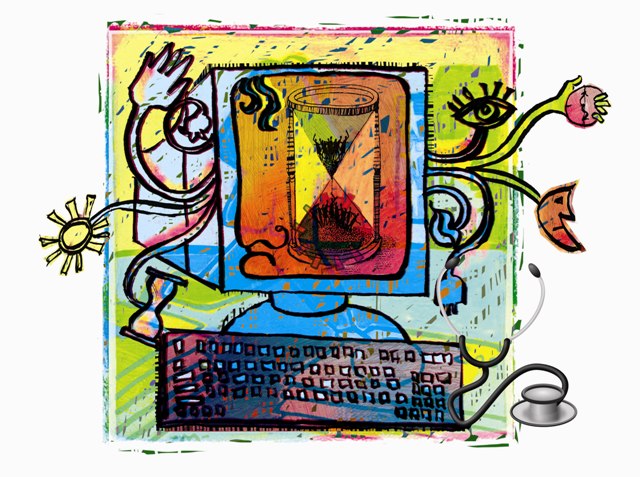 अनिश्चित दिनचर्या और खाने-पीने का कोई सही समय न हो पाने की वजह से पत्रकारों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. कुछ साल पहले मीडिया स्टडीज ग्रुप की ओर से देश में कार्यरत मीडियाकर्मियों की कार्यस्थिति और जीवन-स्तर का अंदाजा लगाने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण किया गया. 13 जुलाई, 2008 से 13 जून, 2009 तक चले इस सर्वेक्षण के दौरान 150 मीडियाकर्मियों ने अपनी राय दी थी. आम तौर पर मीडियाकर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही कम सर्वे किए जाते हैं. यह अपनी तरह का अनूठा सर्वे था, जो मीडियाकर्मियों की बुरी हालत की झलक दिखाता है. इसे नजीर के तौर पर देखें तो आज कई सालों बाद मीडिया में लोगों के काम करने की स्थितियां कमोबेश वैसी ही हैं जैसी सर्वे होने के समय थीं.
अनिश्चित दिनचर्या और खाने-पीने का कोई सही समय न हो पाने की वजह से पत्रकारों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. कुछ साल पहले मीडिया स्टडीज ग्रुप की ओर से देश में कार्यरत मीडियाकर्मियों की कार्यस्थिति और जीवन-स्तर का अंदाजा लगाने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण किया गया. 13 जुलाई, 2008 से 13 जून, 2009 तक चले इस सर्वेक्षण के दौरान 150 मीडियाकर्मियों ने अपनी राय दी थी. आम तौर पर मीडियाकर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही कम सर्वे किए जाते हैं. यह अपनी तरह का अनूठा सर्वे था, जो मीडियाकर्मियों की बुरी हालत की झलक दिखाता है. इसे नजीर के तौर पर देखें तो आज कई सालों बाद मीडिया में लोगों के काम करने की स्थितियां कमोबेश वैसी ही हैं जैसी सर्वे होने के समय थीं.