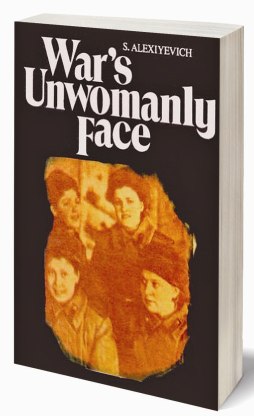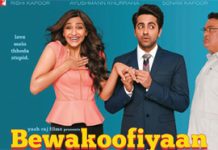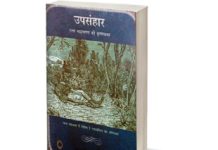इस साल साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बेलारूस की खोजी पत्रकार और नॉन फिक्शन (गैर काल्पनिक) लेखिका स्वेतलाना एलेक्सीविच की सबसे चर्चित किताब ‘वॉयसेज फ्रॉम चर्नोबिल’ के बारे में पढ़ते हुए मेरा ध्यान सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी के साहित्यिक दस्तावेजीकरण की तरफ गया. यह किताब वर्ष 1986 में यूक्रेन के चर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुए भयानक विस्फोट के दुष्परिणामों पर आधारित है. अपनी रिपोर्टिंग के दौरान स्वेतलाना ने दुनिया की सबसे वीभत्स औद्योगिक आपदाओं में से एक के तौर पर पहचाने जाने वाली ‘चर्नोबिल आपदा’ के पीिड़तों का कई सालों तक साक्षात्कार लिया. बारम्बार… तब तक लोगों से दोबारा-तिबारा मिलती रहीं, जब तक लोग घटना से जुड़ी अपनी सबसे ईमानदार ‘भावनात्मक याद’ उन्हें बता न दें. जाहिर है पीिड़तों की यादों के जरिये चर्नोबिल विभीषिका की कहानी का करुणामयी दस्तावेजीकरण करके उसे किताब की शक्ल देने का काम उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना और उन्हें प्रसिद्धि दिलाई. स्वेतलाना का जन्म यूक्रेन में हुआ था पर उन्होंने अपना सारा जीवन यूक्रेन से सटे बेलारूस और उसके पड़ोसी स्लाविक क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करते हुए बिताया. स्थानीय रूसी भाषा में रिपोर्ताज और किताबें लिखीं और हाशिये पर खड़े आम लोगों की जिंदगियां इतिहास में दर्ज करती रहीं.
स्वेतलाना को अभी-अभी मिले साहित्य के नोबेल पुरस्कार और ‘वॉयसेज फ्रॉम चर्नोबिल’ के साथ-साथ ‘वॉर्स अनवूमेनली फेस’ जैसी उनकी महत्वपूर्ण नॉन-फिक्शन (सत्य घटनाओं पर आधारित/ गैर काल्पनिक) किताबों ने एक तरफ जहां एक पत्रकार के तौर पर मुझे प्रेरित किया, वहीं मेरे जेहन में भोपाल गैस त्रासदी से लेकर हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य तक से जुड़े कई सवाल भी पैदा किए. लेकिन इन सवालों पर आने से पहले इस साल के साहित्य नोबेल पुरस्कार के वैश्विक महत्व में झांकना जरूरी है.
आठ अक्टूबर की दोपहर घोषित हुआ साहित्य का नोबेल पुरस्कार मेरे लिए प्रोत्साहन और उम्मीद से भरी एक चिट्ठी की तरह था. शायद यह मेरे साथ हर पत्रकार के लिए गर्व का क्षण था. नोबेल पुरस्कार के इतिहास में पहली बार एक सक्रिय खोजी पत्रकार को नॉन-फिक्शन लेखन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है. यहां यह दोहराना भी जरूरी है कि उपन्यासों, कविताओं और कहानियों जैसी विधाओं से पहचाने जाने वाले वैश्विक साहित्यिक संसार में नॉन फिक्शन विधा को दोयम दर्जे का समझा जाता रहा है. इस भेदभाव के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि ‘कल्पना की उड़ान’ भरकर ‘कला’ को ऊंचाइयों तक ले जाने की जो आजादी काल्पनिक उपन्यासों-कविताओं और कहानियों के पास है, वह सिर्फ सत्य घटनाओं पर आधारित नॉन-फिक्शन के पास कहां? इतना ही नहीं, हर रोज आपदाओं के बीच बदल रही दुनिया का दस्तावेजीकरण करने वाली रिपोर्ताज (लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग) की महत्वपूर्ण विधा को भी हिकारत की नजर से देखकर हमेशा खारिज ही किया गया है. ऐसे में स्वेतलाना को नोबेल मिलने की खबर आने के बाद जब कुछ लोगों से सोशल मीडिया पर नोबेल पुरस्कार समिति को ‘शेम शेम’ कहते हुए उनके गिरते हुए स्तर को कोसा तो मुझे बिलकुल भी हैरानी नहीं हुई. एक सज्जन ने तो पुरस्कार समिति से ही सवाल किया कि क्या वे यह भूल गए थे कि स्वेतलाना सिर्फ एक ‘पत्रकार’ हैं?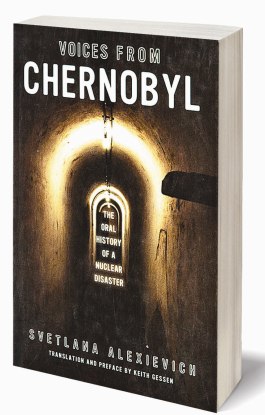
स्वेतलाना को यह पुरस्कार मिलना कई कारणों से महत्वपूर्ण है. एक रिपोर्टर होने के नाते स्वेतलाना के काम और उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है. इस बात का गर्व भी है कि हमारे ही बीच के एक साथी रिपोर्टर ने अपनी गहरी संवेदना, लगन और लेखन शैली पर सालों लगातार काम करने के बाद विश्व के लिए कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए. अपने एक इंटरव्यू में स्वेतलाना ने कहा, ‘अगर मैं 19वीं सदी में पैदा हुई होती तो जरूर उपन्यास लिखती, लेकिन युद्ध, महामारी, अकाल, अत्याचार जैसी अनगिनत आपदाओं से भरी 20वीं सदी के इतिहास को बताने के लिए फिक्शन कमजोर माध्यम है, इसलिए मैंने हजारों साक्षात्कारों के बाद सामने आने वाली लोगों की भावनात्मक यादों के आधार पर लिखे गए रिपोर्ताज का रास्ता चुना.’ उनकी किताबों को नोबेल पुरस्कार समिति ने ‘सोवियत रूस का भावनात्मक इतिहास’ कहकर संबोधित किया है.
इस पुरस्कार को साहित्यिक सामंतों के दंभ को तोड़ने वाली घटना के तौर पर भी देखा जा सकता है. शायद अपनी आराम कुर्सियों पर बैठकर कल्पना की उड़ाने भरते हुए अंग्रेजी में लिखने-पढ़ने वाले एक बड़े वर्ग के लिए यह सच पचा पाना बहुत मुश्किल होगा कि एक छोटे से गांव में गरीब ग्रामीण प्राथमिक शिक्षक के घर जन्मी एक लड़की को अपनी स्थानीय भाषा में लिखने के लिए नोबेल कैसे मिल गया? और उसने लिखा भी तो क्या! छोटे ग्रामीण अखबारों से लेकर पत्रिकाओं तक में लिखा, हाशिये पर ढकेल दी गईं आम औरतों और बच्चों की जबान बनीं.
स्वेतलाना को मिला यह पुरस्कार एक ओर जहां रिपोर्ताज के महत्व को दोबारा स्थापित करता है, वहीं भारतीय पत्रकारिता के सामने कई सवालों के सिरे भी छोड़ जाता है. सवाल ये कि हिंदी पत्रकारिता और लेखन में लंबे रिपोर्ताज पर आधारित जमीनी किताबों की क्या स्थिति है? फणीश्वर नाथ रेणु की ‘ऋणजल धनजल’ और फिर अनिल यादव की ‘वह भी कोई देस है महाराज’ जैसी गिनती की कुछ किताबों के नाम ही याद आते हैं, जबकि हमारे देश में आपदाओं और महामारियों के साथ-साथ समाज की हर परत में गहरा टकराव है, जिसकी वजह से भारत विदेशी पत्रकारों और लेखकों को हमेशा आकर्षित करता रहा है. यह हमारे लिए आत्मविश्लेषण का प्रश्न है कि क्यों आंतरिक संघर्षों और अनगिनत टकरावों के बारूद पर बैठे इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर सबसे अच्छा काम विदेशी लेखकों का है?
उदाहरण के लिए भोपाल गैस त्रासदी पर प्रकाशित हुई सबसे प्रसिद्ध किताब ‘फाइव पास्ट मिडनाइट इन भोपाल’ फ्रांसीसी लेखकों डॉमिनिक लैपियर और जेवियर मोरो ने लिखी, फिर पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित कैथरीन बू की किताब ‘बिहाइंड द ब्यूटीफुल फॉरएवर्स’ को भारतीय गरीबी पर सबसे मजबूत किताब के तौर पर देखा जाता है. भारत में जो थोड़ी बहुत रिपोर्ताज प्रकाशित होती हैं, वे सिर्फ अंग्रेजी में काम करने वाले मीडिया संस्थान ही करते हैं. स्थानीय भाषा में लिखने वाले हिंदी पत्रकारों को लंबी रिपोर्ताज लिखने के लिए प्रोत्साहित और प्रकाशित करना न सिर्फ लेखन के लोकतांत्रिकरण के लिए, बल्कि विषय के साथ न्याय करने के लिए भी जरूरी है. लेकिन हिंदी के अखबार महत्वपूर्ण विषयों पर लंबी रिपोर्ताज प्रकाशित करने के लिए आम तौर पर दो पन्ने की जगह भी नहीं देते. सामंती सोच, औपनिवेशिक असर के साथ हिंदी में संसाधनों की कमी भी इसके लिए जिम्मेदार है. कारण कई हो सकते हैं पर हिंदी साहित्यकारों के साथ ही हिंदी पत्रकार भी कभी अपने समय का ईमानदार दस्तावेजीकरण न करने पाने की जवाबदेही से इनकार नहीं कर पाएगी.