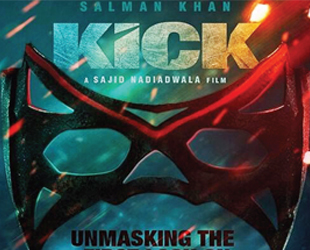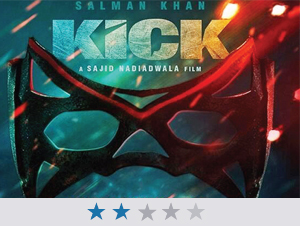आज से तकरीबन 130 साल पहले हिंदी के नामी साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ‘अंधेर नगरी’ नाम का एक नाटक लिखा था. व्यंगात्मक और रोचक प्रहसनों की भरमार वाले इस नाटक में एक आदमी अपनी बकरी के मरने की फरियाद लेकर राजदरबार में पहुंचता है और राजा से न्याय की गुहार लगाता है. उस व्यक्ति को मुआवजा दिलाने के बजाय राजा, बकरी की मौत के जिम्मेदार अपराधी का पता लगाने के लिए हास्यापद खोज का ऐसा सिलसिला शुरू करता है जो कल्लू बनिया नाम के दुकानदार से लेकर एक कारीगर, चूनेवाले, और गड़रिये से होते-होते अंतत: नगर के कोतवाल पर आकर थमता है. राजा कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है. पर इस बीच घटनाक्रम कुछ ऐसा घूमता है कि आखिर में राजा खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है. इसके साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है और बकरी की मौत पर न्याय मांगने आया फरियादी खाली हाथ रह जाता है.
उस दौर की अव्यवस्थित और अराजक प्रशासनिक व्यवस्था पर चोट करने वाले इस नाटक को लिखे आज एक सदी से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है. इस नाटक की भाषा में ही कहा जाए तो तब ‘एक टके’ में गली-नुक्कड़ों में आसानी से मिल जानेवाला सामान आज डॉलर और पाउंड की कीमत पर बड़े-बड़े शॉपिंग कांप्लेक्सों में मिलता है. लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के मोर्चे पर तुलना की जाए तो ‘अंधेर नगरी’ वाला वह ‘चौपट राज’ आज भी उसी तरह कायम है. प्रशासन की तमाम इकाइयों में तब से ही घुस चुके अव्यवस्था के ये विषबीज अब सूचना का अधिकार (आरटीआई) नाम के उस कानून की अवधारणा पर चोट कर रहे हैं जिसे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से साल 2005 में बड़े जोर-शोर से लागू किया गया था. देश-भर के अलग-अलग हिस्सों में इस कानून के तहत सूचना मांगने के ऐसे बहुत से मामले हैं जो भारतेंदु के उस नाटक को अक्षरश: चरितार्थ करते नजर आते हैं. यानी, सूचना चाहनेवाला फरियादी संबंधित विभाग में आवेदन लगाता है. इस पर सूचना देने के बजाय उस विभाग का सूचना अधिकारी आवेदन को एक विभाग से दूसरे, तीसरे और चौथे विभाग को सौंप देता है. तय सीमा से कहीं ज्यादा समय तक चलनेवाली इस आंखमिचौली के बाद भी जब सूचना नहीं मिलती है तो सूचना आयोग ‘राजा की फांसी’ की तरह सूचना अधिकारी पर जुर्माना ठोक देता है. इस तरह यह असली नाटक भी खत्म हो जाता है और यहां भी आवेदन करनेवाला फरियादी हाथ मलता रह जाता है.
‘सूचना अधिकार अधिनियम 2005’ के लागू होने से अब तक लगभग नौ साल की इस समयावधि में इसके प्रावधानों के तहत सूचना मांगे जाने पर सूचना न देने, आनाकानी करने, बहाना बनाने और आवेदनों को खारिज कर देने के ऐसे बहुत से मामले देश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आ चुके हैं. ये मामले साफ तौर पर बताते हैं कि आरटीआई के तहत आवेदन करने पर पहली बार में ही सूचना हासिल करना किसी महाभारत लड़ने से कम नहीं है. इसके अलावा इन मामलों से यह भी पता चलता है कि किसी आवेदन को अलग-अलग विभागों की सैर पर भेज देने में खर्च होने वाले अतिरिक्त पैसे और समय की बर्बादी के चलते कई बार हासिल होने वाली सूचना सही होने के बावजूद भी रद्दी के अलावा किसी काम की नहीं रह जाती.
बात पिछले साल जून के महीने की है. उत्तराखंड के केदारनाथ समेत कई अन्य हिस्सों में आपदा ने भयंकर विनाशलीला मचाई थी. आपदा से हुए जानमाल के भारी भरकम नुकसान के लिए तब प्रदेश की सरकार को बहुत हद तक जिम्मेदार बताया जा रहा था. सरकार पर आरोप था कि आपदा से निपटने को लेकर उसकी तैयारियां पर्याप्त नहीं थीं. इन आरोपों की पड़ताल करने के लिए तहलका ने आठ जुलाई, 2013 को उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई आवेदन लगाया. इसमें चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले तीन सालों में की गई बैठकों का ब्यौरा मांगा गया. आमतौर पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली बैठकों का कार्यवृत्त तैयार किए जाने की जिम्मेदारी सीधे-सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की होती है. इस लिहाज से देखा जाय तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय को अपने स्तर से यह सूचना प्रदान करनी थी. लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस आवेदन पर सूचना देने के बजाय इसे प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग तथा पर्यटन विभाग को सौंप दिया. इन दोनों विभागों ने कुछ जानकारियां देने के साथ अन्य जानकारियों के लिए आवेदन को आपदा एवं न्यूनीकरण अनुभाग, धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग, चार धाम विकास प्राधिकरण तथा कुछ अन्य विभागों की तरफ सरका दिया. तकरीबन तीन महीने के बाद अलग-अलग विभागों से तहलका को जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार का रवैया बेहद रस्मी था. आलम यह था कि 2011 में हुई बैठक के दौरान लिए गए बहुत से निर्णय दो साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर सके थे. आपदा को लेकर सरकार के राहत कार्यक्रमों की पोल खोलने के लिहाज यह एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी. लेकिन सूचना मिलने में हुई देरी के कारण इसका औचित्य लगभग समाप्त हो चुका था.
इसी तरह का एक और मामला मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय का भी है. तहलका ने पांच जुलाई, 2013 को मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय से राज्य के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हुई भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या तथा उनको लेकर लोकायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी. कायदे के मुताबिक मुख्य सचिव कार्यालय को इस आवेदन के जवाब में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी अपने स्तर से देनी चाहिए थी. लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय ने यह आवेदन मध्यप्रदेश के लोकायुक्त कार्यालय को सौंप दिया.
इसके बाद इस आवेदन के साथ जो कुछ हुआ वह भी बेहद हैरान करनेवाला है. लोकायुक्त कार्यालय ने इस पर कोई सूचना देने के बजाय इस आवेदन को यह कहकर अमान्य करार दिया कि इसमें क्यों, कैसे, और कितने जैसे प्रश्नावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है. कार्यालय का साफ कहना था कि प्रश्नवाचक भाव वाले आवेदनों का जवाब आरटीआई के तहत नहीं दिया जा सकता.
कई बार अधिकारी आवेदन को सिर्फ इसलिए अन्य विभागों को भेज देते हैं ताकि सूचना छिपाई जा सके. वे सूचना न देने के जुर्म से भी बच जाते हैं और आवेदक को सही सूचना भी नहीं मिलती
जिस ‘कितने’ शब्द पर आयोग के लोक सूचना अधिकारी को आपत्ति थी जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं. तहलका ने अपने सवाल में पूछा था कि, ‘जनवरी 2010 से अब तक लोकायुक्त के पास दर्ज हुई शिकायतों में जांच के बाद लोकायुक्त ने ‘कितने’ मामलों में आरोपितों को दोषी माना? तथा इन मामलों में से जन प्रतिनिधियों (राज्य के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं विधायकों आदि) की संख्या ‘कितनी’ है?