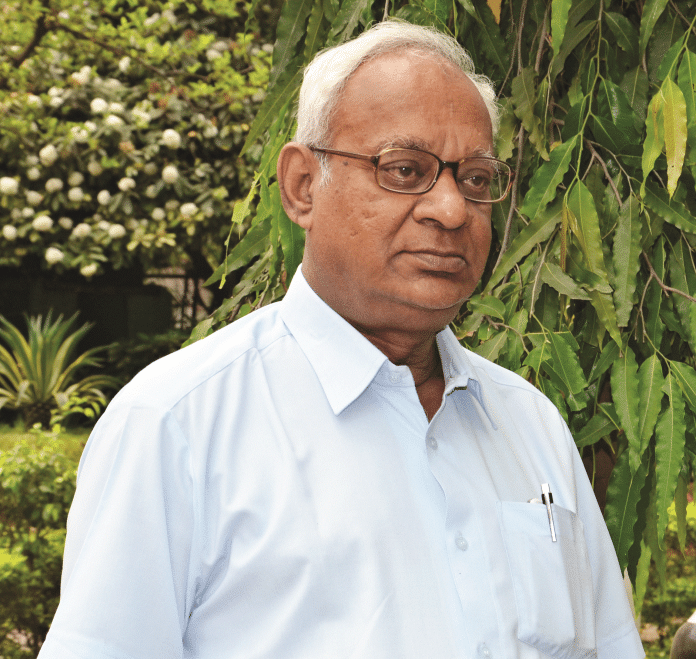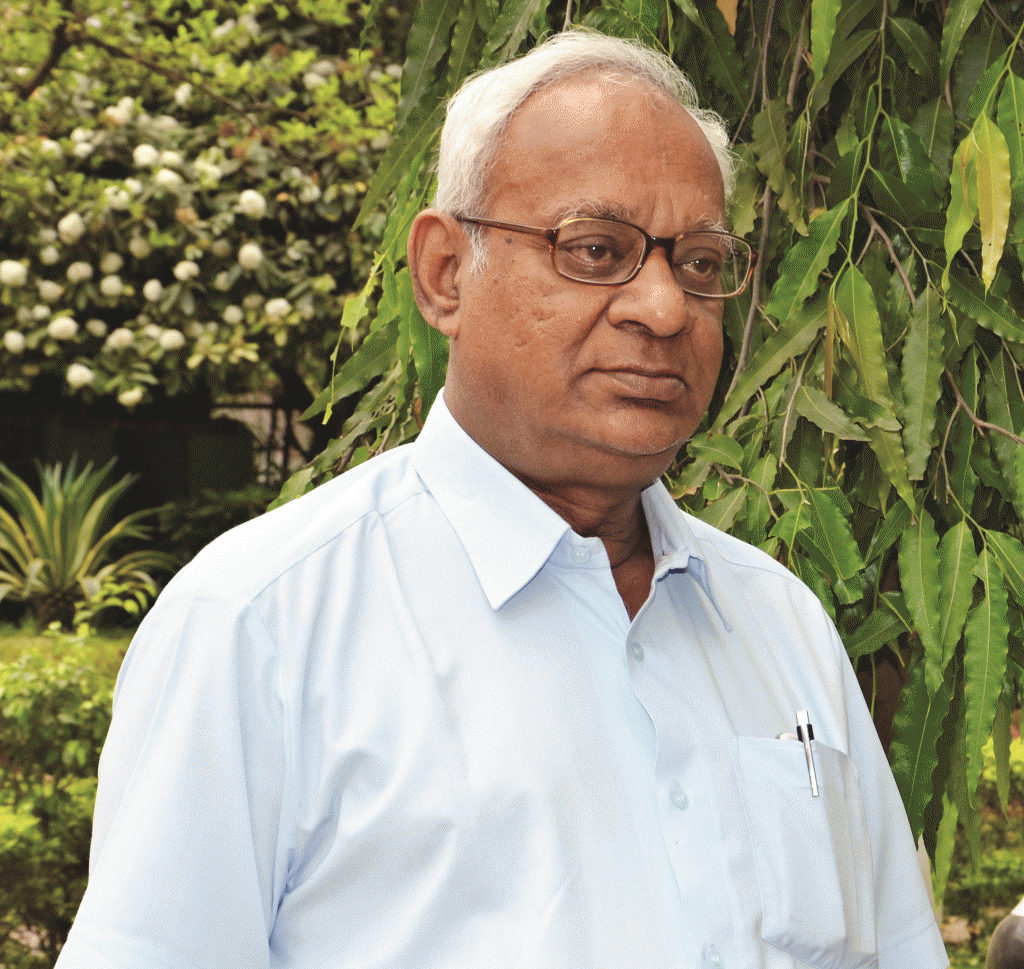 किसी कैदी को फांसी देने के समय वहां उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किलों से भरा रहा होगा? अपने अनुभव साझा करें.
किसी कैदी को फांसी देने के समय वहां उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किलों से भरा रहा होगा? अपने अनुभव साझा करें.
मैंने जब यह रिपोर्टिंग की थी तब मेरी उम्र महज 25 साल की थी. पत्रकारिता के मेरे शुरुआती दिन थे. तब सचमुच यह पता नहीं था कि फांसी की रिपोर्टिंग करना कोई दुर्लभ काम है. देशबंधु, जहां मैं काम करता था, अखबार में रिपोर्टिंग प्रकाशित होने के बाद जब देश भर से प्रतिक्रियाएं आईं और कई पत्र-पत्रिकाओं ने उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया तब अहसास हुआ कि हमने कोई महत्वपूर्ण व नायाब रिपोर्टिंग की है.
अखबार के संपादक ने आपको कॅरियर की शुरुआत में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी?
इस रिपोर्टिंग का प्रस्ताव मैं और मेरे एक सहयोगी सुनील ने जब अपने संपादक ललित सुरजन को दिया तो उन्होंने हमारा उत्साहवर्द्घन किया और सहर्ष अपनी सहमति दी थी. मेरे वरिष्ठ स्व. राजनारायण मिश्र ने फांसी देखने व रिपोर्टिंग की अनुमति दिलाने में मदद की थी. तब रिपोर्टरों की कोई बीट नहीं होती थी. इससे रिपोर्टर किसी विषय या क्षेत्र में बंधा न होकर हर विषय और विधा की रिपोर्टिंग कर सकता था. इतना ही नहीं, प्रूफ पढ़ने से लेकर पेज जमाने तक का काम रिपोर्टर को ही करना पड़ता था. अक्सर रिपोर्टर ही इवेंट या विषय चुनता था जिसे संपादक के साथ चर्चा कर अंतिम रूप दिया जाता था. संपादक से रिपोर्ट का प्लान बनाने से लेकर काॅपी को अंतिम रूप देने तक जीवंत संवाद बना रहता था. हमारे संपादक ललित सुरजन के अनुभव का लाभ मुझे लंबे समय तक कई मौकों पर मिलता रहा.
इस रिपोर्टिंग से पहले आपने क्या तैयारी की थी?
यह वाकई बहुत मुश्किल मामला था. इससे पहले कभी फांसी की सजा दिए जाने की रिपोर्टिंग का कोई उदाहरण मेरे सामने नहीं था. यह घटना भी जीवन की आम घटनाओं से बिल्कुल अलग थी. अतः इस रिपोर्टिंग पर जाने से पहले कोई तैयारी करना संभव नहीं था. बस, मन में उठते सवालों और जिज्ञासाओं को विस्तार देते हुए उनके जवाब ढूंढ़ने का मानस बना हुआ था. टेपरिकॉर्डर, कैमरा आदि साथ रखने की अनुमति नहीं थी. डायरी भी साथ नहीं थी. केवल सारी घटना को आंखों व कानों के जरिए दिमाग में उतारने की तैयारी भर थी. फांसी की सजा दिए जाने के कुछ दिन पहले जेल अधीक्षक जीके अग्रवाल ने जब यह जानकारी मुझे दी तब से ही इस घटना की रिपोर्टिंग करने का मानस बन गया था. यह जानते हुए भी कि फांसी की सजा दिए जाने के दौरान किसी पत्रकार की उपस्थिति बिना विशेष अनुमति के संभव नहीं होगी. राष्ट्रपति द्वारा मर्सी पिटीशन खारिज होने की सूचना मिलने के साथ ही फांसी की सजा दिए जाने की तारीख तय हो जाती है और जेल में इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हंै. इन तैयारियों से मैं तीन-चार दिनों से रूबरू होता रहा और जब फांसी की सजा दिए जाने के दिन से इसे देखने की अनुमति मिली तो वह रोमांचक क्षण था. इस प्रक्रिया को आप रिपोर्टिंग की मेरी तैयारी कह सकते हैं.
फांसी की रिपोर्टिंग तो क्राइम रिपोर्टिंग है. क्या उसके बाद भी आपने क्राइम रिपोर्टिंग की?
मैं क्राइम रिपोर्टर कभी नहीं रहा, न इसमें मेरी कोई दिलचस्पी रही. यह तो एक विशेष घटना थी जिसकी नवीनता ने रिपोर्टिंग के लिए आकर्षित किया था. विकास पत्रकारिता मेरा विषय था और बस्तर में आदिवासियों के विकास की विसंगति पर मेरी रिपोर्ट को 1980 में स्टेट्समैन का रूरल रिपोर्टिंग अवार्ड मिला था. बाद में चुनाव व राजनीति मेरा विषय हो गया और पिछले दो दशक से इसी विषय पर मैं काम कर रहा हूं. लोगों को यह अचरज होगा कि राजनीतिक विश्लेषण के बीच ‘आंखों देखी फांसी’ कहां से आ गई. यह मेरी रिपोर्टिंग का अपवाद भी है और विशिष्ट प्रसंग भी.
हर पत्रकार की यह लालसा होती है कि वह कोई ऐसी रिपोर्ट लिखे जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेे. उस समय यह बहुत बड़ी खबर रही होगी. क्या आज की तरह उस समय भी ब्रेकिंग न्यूज जैसी लालसा पत्रकारों के मन में रहती थी?
1978 में जब मैंने यह रिपोर्टिंग की थी तब ब्रेकिंग न्यूज की पत्रकारिता नहीं होती थी. तब नाम कमाना, कॅरियर बनाना पत्रकारों की सोच नहीं होती थी. हां, कुछ अलग, कुछ बेहतर, कुछ नया करने की ललक जरूर होती थी, जो मुझमें भी थी और उसी के चलते फांसी जैसी दुर्लभ रिपोर्टिंग संभव हो सकी.
बैजू की फांसी के समय आपकी मनःस्थिति कैसी थी?
मेरी मनःस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण बैजू की मनःस्थिति थी जिसे पढ़ने-समझने की कोशिश मैं कर रहा था. बैजू एक अनपढ़ ग्रामीण था जो अपने मनोभावों को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ था. अतः संवाद से परे दाढ़ी में छिपे उसके चेहरे, उसकी आंखों और उसकी भाव-भंगिमाओं से ही उसकी मनःस्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था. मेरी मनःस्थिति का तो मुझे खयाल ही नहीं था, मैं तो पूरी तरह बैजू में खोया हुआ था.
बैजू कीे फांसी के लगभग 36 साल बाद किताब की जरूरत महसूस क्यों हुई?
जरूरत कुछ नहीं थी. फांसी की रिपोर्टिंग की चर्चा लंबे समय तक होती रही. कुछ मित्रों ने सलाह दी कि इसे पुस्तक का रूप दिया जाना चाहिए क्योंकि यह दुर्लभ प्रसंग है. काफी समय तक मैं ऊहापोह में रहा कि वाकई ऐसा करना चाहिए और हां, तो कैसे? इसी उधेड़बुन में फांसी की सजा से संबंधित प्रकाशनों से गुजरता गया. अधिकांश सामग्री फांसी की सजा को कायम रखने या समाप्त करने के पक्ष में थी, जिससे मैं बचना चाहता था. मैं फांसी की सजा दिए जाने की घटना तक अपने आपको सीमित रखना चाहता था ताकि पुस्तक रिपोर्टिंग पर ही केंद्रित हो पाए. इसे मैं फांसी की सजा पर व्यापक अध्ययन या शोध प्रबंध नहीं बनाना चाहता था. एक पत्रकार के रूप में अपनी रिपोर्टिंग को केंद्र में रखकर फांसी की सजा से संबंधित तथ्यों को मैंने पुस्तक के रूप में शामिल किया ताकि फांसी की सजा को पाठक समग्रता में जान सकें. धीरे-धीरे पुस्तक का स्वरूप उभरने लगा लेकिन दैनंदिन जद्दोजहद में वक्त नहीं मिल पा रहा था. इसलिये इसे तैयार करने में बरसों का वक्त लग गया. मेरा आलस्य भी इस देरी की एक वजह रही.
किताब की भूमिका में आपने लिखा है कि लिखते समय बार-बार काट-छांट करनी पड़ी और बहुत बदलाव भी, जो आपके स्वभाव के विपरीत था. आपसे जानना चाहूंगा.
इस रिपोर्टिंग पर किताब लिखने का खयाल कभी नहीं रहा. जैसा मैंने पहले कहा था कि रिपोर्टिंग करने के पहले मुझे अहसास ही नहीं था कि फांसी की रिपोर्टिंग कोई दुर्लभ रिपोर्टिंग है. लिहाजा न तो घटना से संबंधित कोई नोट्स लिया गया था और न कोई अन्य होमवर्क. फांसी की सजा पाए कैदी बैजू द्वारा बताई गई बातों की तस्दीक करने या उसके गांव जाकर उसके परिवार से मिलने का भी काम नहीं किया जा सकता था. मेरी पूरी एकाग्रता फांसी की सजा दिए जाने की रिपोर्टिंग तक सीमित थी और रिपोर्टिंग के बाद यह चैप्टर समाप्त हो गया था. अब जब इस रिपोर्टिंग को पुस्तक का स्वरूप देेने की पहल हुई तब संकट यह था कि घटना से संबंधित संदर्भ व जानकारियां भी देनी थीं और विषय से बाहर के विस्तार से भी बचना था. कोशिश पूरी थी कि पुस्तक फांसी की रिपोर्टिंग पर ही केंद्रित हो. वैसे भी जब कोई पुस्तक टुकड़ों-टुकड़ाें में व लंबे अंतराल में लिखी जाए तब उसे अंतिम रूप देने में ऐसा होना स्वाभाविक है.