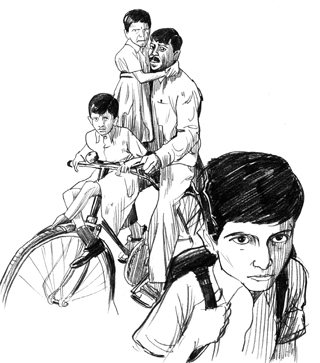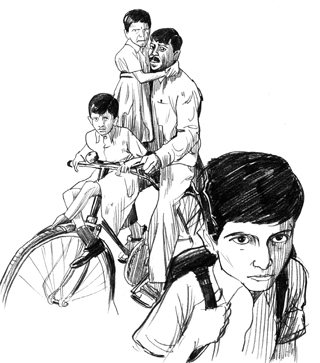 वीएस नायपाल ने हमारे अंग्रेजी मीडिया पर कहा था कि वे भारत की ही स्थितियों पर ऐसे बोलते-लिखते हैं जैसे किसी दूसरे देश की रिपोर्टिंग कर रहे हों. वस्तुत: यह यहां के प्रभावशाली पूरे बौद्धिक वर्ग के बारे में सच है. विश्वविद्यालयों में समाज अध्ययन (विज्ञान) विषय की सामग्री इसका प्रमाण है.
वीएस नायपाल ने हमारे अंग्रेजी मीडिया पर कहा था कि वे भारत की ही स्थितियों पर ऐसे बोलते-लिखते हैं जैसे किसी दूसरे देश की रिपोर्टिंग कर रहे हों. वस्तुत: यह यहां के प्रभावशाली पूरे बौद्धिक वर्ग के बारे में सच है. विश्वविद्यालयों में समाज अध्ययन (विज्ञान) विषय की सामग्री इसका प्रमाण है.
स्कूलों के लिए लिखी पाठ्य-पुस्तकों में भी वही झलक है. राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास जैसे विषयों की पुस्तकें मानो बाहरी लोगों द्वारा लिखी प्रतीत होती हैं. यद्यपि लेखक, प्रकाशन संस्थान आदि सब यहीं के हैं किंतु उसकी सामग्री इतनी दूरी, तटस्थता और अजनबियत से लिखी है कि जैसे किसी विदेशी ने उसे लिखा हो. पाठों में दिए गए उदाहरण विदेशी नामों और प्रसंगों से अटे होते हैं.
जैसे एक स्कूली पाठ्य-पुस्तक में मनुष्य का रहन-सहन समझाने के लिए बस्तियों के चित्रों में यूरोपीय गांव, नगरों के चित्र दिए गए हैं. अन्य वर्णन भी ऐसे हैं मानो जीवन केवल उच्चवर्गीय, महानगरीय ही होता है. घर में कार होना, खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना, टूरिज्म का आनंद लेना, टिन-बंद शीतल पेय का सेवन आदि ऐसे प्रस्तुत है मानो यह तो हर घर की सामान्य बात हो. इनकी उपलब्धता सब पाठकों, बच्चों के लिए सहज, रोजमर्रा की बात मान कर चली गई है. जबकि वह पुस्तक किन्हीं विशेष मंहगे विद्यालय के बच्चों के लिए नहीं, पूरे देश के सामान्य विद्यालयों के लिए लिखी गई है.
हमारी परजीविता इतनी सामान्य बन गई है कि कई लेखकों, प्रकाशकों को चिंता भी नहीं कि जो वे लिख-परोस रहे हैं, उसका कोई स्पष्ट अर्थ या सार्थकता बच्चों, शिक्षकों के लिए बनती भी है या नहीं. चैप्टर बन गए, पन्ने भर गए, तस्वीरें डल गईं, अशुद्धियां जैसे-तैसे देख ली गईं और हो गया. अब और क्या चाहिए! दिए गए पाठों में संगति और अंतर्विरोध तक देखने वाला कोई नहीं होता. जैसे, एक पुस्तक की प्रस्तुति में एक ओर तो पूरा महानगरीय वातावरण छाया हुआ है क्योंकि गांव के उदाहरण, प्रसंग, अनुभूतियां उसमें नदारद हैं. दूसरी ओर उसी पुस्तक के एक अभ्यास में बच्चे से कहा गया है, ‘अपने बगीचे से पानी छिड़कने वाला डब्बा ले आएं’. मूल पंक्ति है, ‘यू कैन टेक द स्प्रिंक्लिंग केन फ्रॉम योर गार्डेन.’ लेखक मान कर चल रहा है कि गार्डन तो है ही हर बच्चे के बंगले में!! मानो सभी बच्चे लोदी इस्टेट या बंजारा हिल्स पर रहते हों. ऐसे पाठ किस दृष्टि से लिखे गए?
अनेक पाठ्य-पुस्तकों में, चाहे इतिहास हो या भूगोल, राजनीति या अर्थशास्त्र, सभी कुछ अमेरिका या यूरोप से ही आरंभ होता है. विचार, विवरण, उदाहरण, महापुरुष, चित्र सब कुछ. विवरण भारत पहुंचता भी है तो ‘फार-ईस्ट’ (या अब ‘साउथ एशिया’) वाली विदेशी, औपनिवेशिक दृष्टि से! एक पुस्तक में लद्दाख और मध्य-एशिया के बारे में परिचयात्मक विवरण है. मात्र चार पंक्तियों में भी यह बात प्रमुखता से लिखी गई है, फिर अभ्यास-पाठ में भी दुहराई है कि वहां के लोग बौद्ध या मुसलमान हैं. किंतु उसी पुस्तक में उत्तरी अमेरिका के बारे में दिए बहुत बड़े अंश में भी यह कहीं नहीं मिलता कि वहां के लोग ईसाई हैं. क्यों? क्योंकि पाठ ही अमेरिकी-ईसाई दृष्टि से लिखा गया है, जो अपने लिए तो जानता ही है कि वह ईसाई है. उसे क्या लिखना! यह तो दूर फार-ईस्ट के देशों के बारे में ही जानने लायक बात है कि वहां के लोग मुस्लिम या बौद्ध हैं, ईसाई नहीं. भारतीय लेखकों में ऐसी दृष्टि जाने-अनजाने एक विदेशी दृष्टि के सिवा और क्या है!
इसीलिए यहां समाज विज्ञान पुस्तकों/ पत्रिकाओं का विवरण भारत के बारे में लिखते हुए भी जिन स्थितियों, समस्याओं की, अच्छी या बुरी जो भी चर्चा करता है वह प्राय: आॅक्सफोर्ड, कैंब्रिज, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालयों के प्रकाशनों या फिर उधर की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में महत्व पाई चीजों तक ही घूमता है. भारत के संबंध में भी कोलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, कास्ट, दलित, वीमेन, जेंडर, रेन फॉरेस्ट, गुजरात, ह्यूमन राइट्स, सेक्युलरिज्म, मायनॉरिटीज, मल्टीकल्चरिज्म, अरुंधंती राय, गे राइट्स, एनवायरमेंट आदि विषय-बिंदु ही पढ़ने-पढ़ाने के लायक माने जाते हैं. अर्थात यहां के बारे में जो पश्चिमी मीडिया या विमर्श का दुराग्रह है. मानो उन चीजों के अतिरिक्त भारतीय छात्रों, लोगों के लिए और विषय महत्वपूर्ण, शिक्षणीय या विचारणीय नहीं हो सकते.
इस प्रकार, यहां समाज अध्ययन की अधिकांश पाठ्य-पुस्तकें अपने ही देश की चिंताओं, मान्यताओं, प्राथमिकताओं, तथा यहां के चित्त और मानस के प्रति निर्विकार दिखती हैं. इसीलिए उनमें भारतीय चिंतन, अध्ययन और जीवन को कोई स्थान नहीं मिलता या फिर नगण्य स्थान मिलता है, वह भी उस आलोचनात्मक दृष्टि से जैसे पश्चिमी-ईसाई विमर्श उसे देखता है. इसीलिए रामायण के बारे में भी अमेरिकी, यूरोपीय लेखकों के लिखे पाठ हमारे सिलेबस में हैं! दिल्ली विश्वविद्यालय, इतिहास विभाग के ‘मेनी रामायण्स’ विवाद में यह उजागर हुआ.
एक स्कूली पाठ्य-पुस्तक में किसी अभ्यास में एक शब्द-पहेली (क्रासवर्ड्स पजल) दी गई है. हिंदी में प्रस्तुत उस पुस्तक में वहां सीधे लिख दिया गया है कि वह पहेली और इसके उत्तर अंग्रेजी में हैं. लेखक-प्रकाशक को परवाह नहीं कि जो लाखों बच्चे हिंदी या बंगला में पढ़ रहे हैं, वे उस अभ्यास का क्या करेंगे? ऐसे उदाहरण केवल लापरवाही ही नहीं, अपराध भी हैं क्योंकि हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी शब्द-पहेलियां मजे से बनती हैं. पत्र-पत्रिकाओं में नियमित ऐसी पहेलियां रहती हैं यानी उन्हें बनाना कोई बड़ा कार्य नहीं है. लेकिन उस हिंदी पाठ्य-पुस्तक के पाठ के लिए हिंदी की शब्द-पहेली नहीं बनवाई गई, जिसे पूरे वर्ष लाखों बच्चों के लिए उपयोग में आना हो! जबकि समय और साधन की कमी नहीं थी. तब यह किस कारण है?
यह वही चीज है जिसे मोहनदास गांधी ने भी समझा था, जिसे नायपाल ने भिन्न रूप में कहा है कि हमारा उच्च-आंग्ल-बौद्धिक वर्ग संपूर्ण देश और देशवासियों की चिंता नहीं करता. वह ‘हार्ड-हर्टेड इंटेलीजेंसिया’ है जो मात्र अपने स्वार्थ में मगन है. वह अपनी स्वार्थ पूर्ति को ही राष्ट्रीय कर्म भी मान लेता है और उसी को देश पर थोप देता है. यह वर्ग किसी ऐसे परिवार प्रमुख की तरह आचरण कर रहा है जो अपने काम-धाम, खर्च-वर्च, घूमना-फिरना, आदि यह भूल कर करता हो कि उसके घर में पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता-पिता भी हैं जो उस पर आश्रित हैं. वह अपने रोजगारदाता तथा सरकार से उनकी आवश्यकता पूर्ति के नाम पर भी अतिरिक्त वेतन और सुविधाएं लेता है. किंतु उस जिम्मेदारी को भूल कर केवल व्यक्तिगत सुख-सुविधा के हिसाब से व्यवहार करता है. उसकी पूरी दृष्टि पश्चिमी-भोगवादी, व्यक्तिवादी और दासवत है. वह जाने-अनजाने हर उस बात की चिंता करता है जो सेमेटिक-पश्चिमी दृष्टि की चिंता है. चाहे भारत हो या विश्व के बारे में जैसे, पर्यावरण. विलासितापूर्ण, मात्र भोग-आधारित, असंयमित, अप्राकृतिक जीवन-पद्धति से उसे कोई परेशानी नहीं होती जो भयावह कचरे, प्रदूषण, प्राकृतिक असंतुलन और तरह-तरह की अपरिमित हानियों की जड़ में है. किंतु यदि लोग देश में दातून प्रयोग करते हैं, नदियों पर दाह-संस्कार करते हैं तो इसे पर्यावरण को नष्ट करने वाला कारक बताया जाता है. अनियंत्रित शहरीकरण, यूज एंड थ्रो वाली मर्मांतक प्रदूषणकारी उपभोग-पद्धति, अनष्टनीय औद्योगिक कचरा, गंदगी का ढेर, शहरों का सीवर नदियों में डालना आदि रोकने की उसे चिंता नहीं, क्योंकि अमेरीकियों को उसकी चिंता नहीं है. बेतहाशा जंगल काटकर धनाढ्य वर्गों और कंपनियों के लिए नित नए फर्नीचर बनाने, वायुयान, पेट्रोलियम वाहनों की अंधाधुंध वृद्धि रोकने की उसे चिंता नहीं, जो पर्यावरण को सबसे अधिक नष्ट कर रही हैं.
अर्थात जो सब पश्चिमी-उपभोगवादी जीवन-पद्धति की आवश्यकताएं हैं, उन्हें हमारे बुद्धिजीवी भी स्वभाविक मानते हैं. इसीलिए जब वे वायु, नदी, वन की रक्षा भी करना चाहते हैं तो उसी पश्चिमी-सेमेटिक उपभोगवादी, प्रकृति-विरोधी, साम्राज्यवादी दृष्टि से. भारत की स्वस्थ, सामंजस्यपूर्ण धर्म-परंपरा से नहीं जो अपनी सहज दृष्टि से प्रकृति-पूजक और चरित्र से ही नदी, पहाड़, पेड़, जीव-जंतुओं का आदर करने वाली है. पर्यावरण तो एक उदाहरण भर है. वस्तुत: अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास जैसे तमाम विषयों में सभी जगह उसी पश्चिमी सेमेटिक दृष्टि से लिखी चीजों का बोलबाला है. हमारा अकादमिक, शैक्षिक विमर्श उसी अंदाज से होता है. इसीलिए यहां इसी देश के क्लासिक शिक्षा दर्शन, धर्म-परंपरा को आधार मान कर कही गई सुविचारित बातों को भी लांछित किया जाता है. विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ, श्रीअरविंद, अज्ञेय,जैसे बड़े से बड़े मनीषी के विचारों को भी सांप्रदायिक या बेकार कह कर किनारे कर दिया गया है. ऐसी आत्म-विरोधी दृष्टि हमें कहां ले जाएगी? अब तक इसका क्या परिणाम हुआ है?
एक परिणाम तो सामने है: देश में मौलिक चिंतन की संभावना कम से कमतर हो गई है. सभी विषयों में स्थिति यह है कि विदेशी भाषाओं के पुराने, नए चिंतन का पहले अंग्रेजी में अनुचिंतन होता है. फिर उस का घटिया अंग्रेजी में अनुलेखन होता है. तब उस का जैसा-तैसा अनुवाद भारतीय भाषाओं में आता है. इसी तीसरे दर्जे की बौद्धिक सामग्री पर हमारी संपूर्ण व्यवस्था पल रही है. उसी से हमारे कर्णधार, शिक्षाविद्, पत्रकार, प्रशासक आदि बन रहे हैं. उनमें दर्शन, साहित्य आदि किसी विषय में मौलिक चिंतन से लेकर सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने की क्षमता ही कहां से पैदा होगी?
खुला मंच
31 अक्टूबर 2008