
नरेंद्र मोदी को मिला प्रचंड जनादेश क्या मनमोहन सरकार के प्रति लोगों के गुस्से का परिणाम है? भाजपा भले इसे मोदी लहर बताती रही और दूसरे कांग्रेस विरोधी लहर- लेकिन यह सबने माना कि लहर थी. इस लिहाज से देखें तो भारतीय जनता ने हाल ही में व्यक्त की गई मनमोहन सिंह की यह अपेक्षा पूरी नहीं की है कि इतिहास उनके साथ शायद बहुत सख्त नहीं होगा. वैसे इस जनादेश से ठीक पहले मनमोहन सिंह के मातहत काम करने वाले दो लोगों संजय बारू और पीसी पारख की दो किताबों, ‘द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ और ‘ क्रूसेडर ऑर कॉन्सपिरेटर’ ने भी मनमोहन सिंह के प्रति कोई सदाशयता नहीं दिखाई. हालांकि कहा जा सकता है कि यह इतिहास नहीं, वर्तमान है जिसमें अपनी तरह की हड़बड़ाहट होती है, लेकिन फिर भी यह वर्तमान कुछ इशारे तो करता ही है.
लेकिन मनमोहन सिंह को यह उम्मीद क्यों करनी चाहिए कि इतिहास उनके साथ सदाशय होगा? समय वैसे ही मनमोहन सिंह के साथ उदार रहा है. एक अरब की आबादी के हिंदुस्तान के जिस नेतृत्व का सपना लिए कई नेता तिरोहित हो गए, जिसके लिए लोग राजनीति की गलियों में बरसों खाक छानते रहते हैं, जिसके लिए तरह-तरह के राजनीतिक गठजोड़ करने पड़ते हैं, वह 10 साल पहले उन्हें बिल्कुल थाली में सजा कर दे दिया गया. मई 2004 में जब यूपीए बहुमत के बेहद करीब था, जब लेफ्ट फ्रंट उनके साथ आ गया था और जब तमाम दलों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के समर्थन की चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंप दी थी, तभी सोनिया गांधी ने अचानक मनमोहन सिंह को 10 जनपथ के सामने खड़े अपने समर्थकों, वफादारों और चापलूसों के हुजूम के बीच ला खड़ा किया और उनके जज्बाती विरोध के बावजूद मनमोहन के नाम पर मुहर लगवा ली.
जाहिर है, यह त्याग और प्राप्ति, दोनों इतने बड़े थे जो भरोसे और वफादारी के बहुत गहरे संबंध के बिना संभव नहीं होते. इसलिए यह स्वभाविक था कि मनमोहन सोनिया गांधी के प्रति वफादार बने रहें और सोनिया भी मनमोहन में वह भरोसा बनाए रखें जिससे सरकार चलती रहे. इसमें संदेह नहीं कि 10 साल के दौरान आए छिटपुट मौकों को छोड़कर सोनिया और मनमोहन दोनों ने इस रिश्ते की मर्यादा निभाई. मनमोहन कभी सोनिया की सीधी अवज्ञा करते नहीं दिखे तो सोनिया ने कभी मनमोहन पर अविश्वास की तलवार नहीं लटकाई. बीच के दौर में जब कांग्रेस के भीतर किसी को उप प्रधानमंत्री बनाने की एक नकली बहस खड़ी की गई तो सोनिया ने स्पष्ट कहा कि मनमोहन सरकार के इकलौते नेता हैं. इसी तरह 2009 में जब कुछ जोशीले कांग्रेसी राहुल गांधी को आगे लाने की मांग कर रहे थे तब भी सोनिया गांधी ने कांग्रेस का घोषणापत्र जारी करते हुए साफ किया कि मनमोहन सिंह ही अगली सरकार के प्रधानमंत्री होंगे.
लेकिन ये दस साल मनमोहन-सोनिया के रिश्तों के दस साल भर नहीं हैं, इक्कीसवीं सदी में बनी पहली केंद्रीय सरकार के भी दस साल हैं. इस कसौटी पर देखें तो मनमोहन सिंह का पूरा कार्यकाल दो तरह के अंतरविरोधों को साधते हुए बीतता दिखाई पड़ता है. उनके एक तरफ कांग्रेस की जीन में शामिल वह ढुलमुल समग्रतावादी विरासत है जिसमें एक हल्का समाजवादी रुझान विद्यमान रहता है तो दूसरी तरफ उनकी अपनी विचारधारा है जो मूलतः बाजार और उदारीकरण के रास्तों में बहुत गहरी आस्था से पैदा हुई है. इसलिए एक तरफ वे उद्योगों का भरोसा जीत रहे हैं, नव उदारवादी मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कानून भी पास कर रहे हैं. मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार इस सरकार की उजली उपलब्धियां हैं. शिक्षा का अधिकार, भोजन की गारंटी, आवास का अधिकार आदि इसके अगले कदम हैं. दूसरी तरफ इसी दौर में विकास दर करीब 10 फीसदी के पार जा रही है जो आजाद भारत में कभी नहीं दिखी. इस दौर में उद्योग-धंधे भी फूल-फल रहे हैं. कांग्रेस के अपने इस अंतर्विरोध के साथ वाम मोर्चे का प्रतिरोध भी शामिल है जो मनमोहन सरकार को कई मोर्चों पर बेलगाम नहीं होने देता.
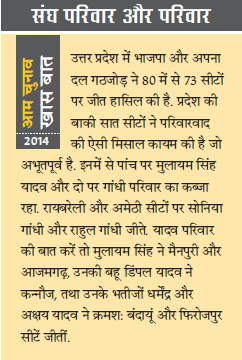 लेकिन एक बार जब यह संतुलन टूटता है तो चीजें जैसे बिखर जाती हैं. 2008 की वैश्विक मंदी का असर 2009 के भारत पर पड़ता है और हम पाते हैं कि अचानक औद्योगिक वृद्धि दर नीचे जा चुकी है, शेयर बाजार गोते खा रहा है, कंपनियां नई परियोजनाएं बंद कर रही हैं और नौजवानों की बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है. अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री इस मोड़ पर बेबस है. इसी दौर में सरकार के द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून के मार्फत अचानक कई पुरानी फाइलें खुलनी शुरू होती हैं और टू जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदानों के आवंटन जैसे मामले मनमोहन सरकार की ईमानदारी का मुंह चिढ़ाने लगते हैं. कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारी में हुई गड़बड़ी और आदर्श घोटाले जैसे मूलतः राज्य केंद्रित मुद्दे भी अंततः मनमोहन सरकार की अलोकप्रियता में इजाफा करते हैं. इसी समय आर्थिक मंदी से बिलबिलाया उद्योग जगत अपने लिए तरह-तरह की राहतें मांग रहा है और न मिलने पर सरकार पर नीतियों की अपाहिजता का आरोप लगा रहा है. और यही दौर है जब लोकतंत्र के दूसरे प्रहरियों में एक हमारी न्यायपालिका के दबाव में कई मामलों की जांच शुरू हो रही है और मनमोहन सरकार के मंत्री और अफसर जेल के पीछे दिखाई पड़ रहे हैं. इस ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में सिर्फ महंगाई दर बढ़ रही है और जो मध्यवर्ग इसी दौरान पहले छोटी और फिर बड़ी गाड़ियां खरीदता रहा, वह पेट्रोल से प्याज तक के दाम बढ़ने पर नाराज है.
लेकिन एक बार जब यह संतुलन टूटता है तो चीजें जैसे बिखर जाती हैं. 2008 की वैश्विक मंदी का असर 2009 के भारत पर पड़ता है और हम पाते हैं कि अचानक औद्योगिक वृद्धि दर नीचे जा चुकी है, शेयर बाजार गोते खा रहा है, कंपनियां नई परियोजनाएं बंद कर रही हैं और नौजवानों की बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है. अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री इस मोड़ पर बेबस है. इसी दौर में सरकार के द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून के मार्फत अचानक कई पुरानी फाइलें खुलनी शुरू होती हैं और टू जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदानों के आवंटन जैसे मामले मनमोहन सरकार की ईमानदारी का मुंह चिढ़ाने लगते हैं. कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारी में हुई गड़बड़ी और आदर्श घोटाले जैसे मूलतः राज्य केंद्रित मुद्दे भी अंततः मनमोहन सरकार की अलोकप्रियता में इजाफा करते हैं. इसी समय आर्थिक मंदी से बिलबिलाया उद्योग जगत अपने लिए तरह-तरह की राहतें मांग रहा है और न मिलने पर सरकार पर नीतियों की अपाहिजता का आरोप लगा रहा है. और यही दौर है जब लोकतंत्र के दूसरे प्रहरियों में एक हमारी न्यायपालिका के दबाव में कई मामलों की जांच शुरू हो रही है और मनमोहन सरकार के मंत्री और अफसर जेल के पीछे दिखाई पड़ रहे हैं. इस ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में सिर्फ महंगाई दर बढ़ रही है और जो मध्यवर्ग इसी दौरान पहले छोटी और फिर बड़ी गाड़ियां खरीदता रहा, वह पेट्रोल से प्याज तक के दाम बढ़ने पर नाराज है.
वाकई यह एक बुरा समय था जिसके बीच अण्णा हजारे और उनके साथियों ने जनलोकपाल के लिए आंदोलन शुरू किया और मनमोहन सिंह के विरुद्ध एक देशव्यापी लहर पैदा की. लेकिन निजी संकल्पों के पहाड़ों से निकला प्रतिरोध का यह झरना चाहे जितना भी सुंदर और वेगवान रहा हो, उससे बिजली पैदा कर सकने लायक संगठन-व्यवस्था टीम अण्णा और बाद में उसकी राजनीतिक उत्तराधिकारी आम आदमी पार्टी में नहीं थी. मूलतः एक विचारहीनता के बीच चले इस जज्बाती आंदोलन का भाजपा या संघ परिवार की विचारधारा से कोई विरोध भी नहीं था. इसलिए पहले संघ परिवार ने परदे में रह कर इस आंदोलन का समर्थन किया और जब यह लहर बिल्कुल देशव्यापी हो गई तो इसकी पीठ पर नरेंद्र मोदी को बिठा दिया- बताते हुए कि उनके पास एक चमकता-दमकता गुजरात है और बाकी भारत को भी वे ऐसा ही चमकता-दमकता बना देंगे.
सवाल है, मनमोहन सिंह इन सबके मूकदर्शक क्यों बने रहे? वे इन स्थितियों को संभाल क्यों नहीं पाए? जवाब है- क्योंकि मनमोहन सिंह मूलतः एक प्रशासक रहे जिन्हें सरकारी फाइलों को पढ़ना तो आता था, माहौल को पढ़ना और बदलना उनके बूते में नहीं था. सोनिया गांधी को दरअसल ऐसा ही आदमी चाहिए था जो उनकी या कांग्रेस की योजनाओं को मूर्त रूप दे सके. जब तक यह काम होता रहा, सरकार ठीक से चलती रही, लेकिन जहां दूरंदेशी के मोड़ आए, वहां मनमोहन बुरी तरह फिसलते दिखे. सोनिया गांधी और मनमोहन के बीच पहली बड़ी दरार ऐटमी करार के वक्त दिखाई पड़ती है जब लेफ्ट के विरोध के बीच यूपीए एक तरह से इस करार से पीछे हटने का मन बना चुका था, लेकिन मनमोहन ने इसे बिल्कुल निजी जिद का मसला बना लिया. वाम के अलग होने, समाजवादी पार्टी के समर्थन देने और संसद में नोट उछाले जाने की शर्मनाक कहानी इसी के बाद शुरू होती है जिसके कुछ दाग सीधे-सीधे मनमोहन सिंह तक भी पहुंचते हैं.
दरअसल पहले दौर में मनमोहन सिंह की कामयाबी या स्वीकृति एक ऐसे व्यक्ति को बाजार की तरफ से मिली स्वीकृति थी जो बिल्कुल पश्चिम की पढ़ाई किताबों के हिसाब से सोचता और चलता था. मनमोहन सिंह जैसा ही कोई प्रधानमंत्री हो सकता था जो 2005 में ऑक्सफोर्ड जाकर बोल आए कि भारत को इंग्लैंड ने ही आधुनिकता और नए जमाने की तालीम दी और 2008 में अमेरिका जाकर जॉर्ज बुश को बता आए कि भारतीय उससे कितना प्यार करते हैं. ऐसा ही प्रधानमंत्री शर्म अल शेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा साझा वक्तव्य जारी कर सकता था जिसके बचाव में कांग्रेस तक नहीं आई.
बहरहाल, मनमोहन सिंह की इन विफलताओं या सीमाओं के बावजूद 10 साल की यूपीए सरकार ऐसी निकम्मी या बेमानी सरकार नहीं थी जो बताई जा रही है. इन दस सालों की औसत विकास दर 8.5 फीसदी के आसपास रही जो शायद पहले कभी नहीं रही. इन्हीं वर्षों में सूचना, रोजगार, रोटी और शिक्षा के हक के साथ दूसरे मानवाधिकारों पर ढेर सारे फैसले हुए जिनकी वजह से सरकार भी पारदर्शी हुई और जनता भी अधिकारसंपन्न. बेशक, इस दौर में महंगाई बढ़ी, लेकिन साथ-साथ कमाई भी बढ़ी.
सवाल है, फिर मनमोहन विफल कहां रहे? उस हिंदुस्तान को समझने में जिसे पहले अटल-आडवाणी भी नहीं समझ पाए थे. 2004 में फील गुड और शाइनिंग इंडिया के नारों के बावजूद अगर एनडीए हारा तो इसलिए कि उसने उस गरीब हिंदुस्तान की परवाह नहीं की जो सबसे ज्यादा वोट देता है. मनमोहन सिंह आंकड़े पेश करते हैं- और शायद वे ठीक भी हों- कि उनके दौर में गरीबी बड़े पैमाने पर कम हुई है, लेकिन ज्यादा बड़ी सच्चाई यह है कि इस दौर में गरीबों के साथ छल भी बहुत हुए. उनकी जमीन छीनी गई, उनके स्कूल-अस्पताल छीने गए, शिक्षा और सेहत का बजट वैसे नहीं बढ़ा जैसे बढ़ना चाहिए था. इस दौर में बड़े हुए नक्सलवाद को मनमोहन देश का सबसे बड़ा खतरा भर बताते रहे, यह नहीं समझ पाए कि यह नक्सल गलियारा वैसे-वैसे बड़ा हो रहा है जैसे-जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सरहदें बड़ी हो रही हैं.
लेकिन मनमोहन को सिर्फ इसकी सजा नहीं मिली. उन्हें उस कॉरपोरेट इंडिया का एजेंडा आगे न बढ़ा पाने की भी सजा मिली जिसने एक दौर में उन पर बहुत भरोसा किया. यह कारपोरेट इंडिया आज नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है. वही मनमोहन सिंह का मूल्यांकन कर और करवा रहा है. विकास के नए मिथक इसी कारपोरेट इंडिया में गढ़े जा रहे हैं- शायद यह हिंदुस्तान के गरीबों पर नए सिरे से भारी गुजरे.
बहरहाल, मनमोहन संतोष कर सकते हैं कि इत्तिफाक ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी, उसे उन्होंने पूरा किया. वे नेहरू और इंदिरा के बाद सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे. वे राजनीति के एक ऐसे दौर में प्रधानमंत्री रहे जब क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाएं और ग्लोबल हसरतें साथ-साथ चल भी रही थीं और टकरा भी रही थीं- वे एक तरह से मंडल-कमंडल के बाद की भूमंडलीकृत राजनीति के पहले प्रधानमंत्री रहे. वे जब तक दोनों के बीच संतुलन साध पाए, तब तक चले, जब यह संतुलन बिगड़ा तो गिर पड़े. अब नया दौर राष्ट्रवादी सपनों और ग्लोबल हसरतों की जुगलबंदी का है. इस जुगलबंदी का हश्र वह वास्तविक परिप्रेक्ष्य देगा जिसमें हम मनमोहन सिंह का कायदे से मूल्यांकन कर सकेंगे. तब तक मनमोहन सिंह को यह उम्मीद करने का हक है कि इतिहास उनके साथ नरमी बरतेगा.





