
आपकी कहानियों की तरह इस उपन्यास में भी त्रासद विडम्बनाओं, विद्रूपताओं पर हंसने की प्रवृत्ति स्पष्ट तौर पर दिखती है. बार-बार ये प्रवृत्ति कहां से आती है? क्या आप इसे सायास अपनी शैली के बतौर लाते हैं?
मैं और बहुत से लोग इस तरह सोचते हैं कि बहुत गंभीर बात को अगर आप बिल्कुल गंभीर मुद्रा में कहेंगे तो शायद वो अपना असर कम कर देती है. मैं कोशिश करता हूं कि बहुत गंभीर मुद्दों को भी जीवन के छोटे-छोटे अनुभवों से हल्के-फुल्के ढंग से पेश किया जाए लेकिन इसमें खतरा भी है कि कहीं आप प्रवाह में न बह जाएं. इसमें संतुलन रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा न हो कि आपका हलका-फुलका लहजा आपकी गंभीरता पर भारी पड़ जाए या आपकी गंभीरता जीवन के रस पर भारी पड़ जाए. किसी भी दुख को अगर आप एकदम दुखी मुद्रा में, दुखी स्वर से चुनौती देंगे तो शायद आप उससे जीत नहीं पाएंगे. उसको पराजित करने का तरीका यह भी होता है कि आप उसकी औकात कम कर दें.
असल जिंदगी में आप बेहद कम बोलने वाले, चुनिंदा दोस्त बनाने वाले, देर में खुलने वाले आदमी के बतौर जाने जाते हैं. जबकि आपके पात्र बेहद शरारती, हंसोड़ और बतरस से भरे हुए दिखाई देते हैं तो इस विरोधाभास की तह में क्या है?
मैं सोचता हूं कि किसी भी आदमी के अंदर सिर्फ एक मिजाज का आदमी नहीं होता है. हो सकता है कि सरसरी तौर पर देखने पर वो एक ही रंगवाला लगे लेकिन उसके अंदर विभिन्न रंग, विभिन्न धाराएं और विभिन्न छवियां होती हैं. अब ये अलग बात है कि हम अपने सामाजिक जीवन में अपने लिए एक तरह की मुद्रा तय कर लेते हैं. लेकिन असल में जैसे जिंदगी, यथार्थ और इंसान तरह-तरह के रंगों से निर्मित होता है वैसे ही पात्र भी होते हैं. इसलिए आप देखेंगे कि मेरी रचनाओं में पात्र में जहां हास्य ज्यादा बढ़ने लगता है, खिलंदड़पन बढ़ता जा रहा होता है ठीक उसी वक्त आपको मिलेगा कि वह सीधे कविता के धरातल पर चला जाता है या विडम्बना के तनाव को दर्ज करने लगता है. और अपनी बात करूं तो ऐसा कतई नहीं है कि मैं हंसोड़ नहीं हूं बस इतना जरूर है कि मैं अपने करतब और अपने बारे में खुद बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता.
इस उपन्यास में जगह-जगह पात्र खुद आकर अपना पक्ष रखते हैं. इस युक्ति के प्रयोग के पीछे क्या वजह थी?
इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे लगता है और आज ये मान्य धारणा है कि किसी भी चीज का सिर्फ एक ही पाठ नहीं होता. आप उसको एक नजरिए से देख रहे हैं कोई दूसरा दूसरे नजरिए से देख सकता है और ये यथार्थ को गड़बड़ नहीं करते हैं बल्कि किसी चीज के एक से ज्यादा पाठ यथार्थ को स्पष्ट करने में मदद ही पहुंचाते हैं, और उसे विस्तार भी देते हैं. इसके अलावा उपन्यास को स्फीति- शब्दों की फिजूलखर्ची से बचाने के लिए भी मुझे ऐसा करना पड़ा. जैसे अगर मैं ऐसा न करता तो किसी एक चीज के अलग-अलग डायमेंशन्स को दिखाने के लिए अलग अध्याय रचने पड़ते.
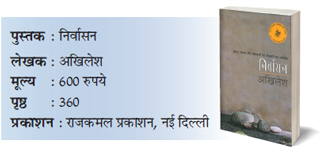 इस उपन्यास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है चाचा जिसका इस तथाकथित विकास से मोहभंग हो चुका है और वो आत्मनिर्वासन चुनता है, क्या आप मानते हैं कि जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं वहां हर संवेदनशील या रियलाइजेशन रखने वाले व्यक्ति की नियति चाचा बन जाना ही है?
इस उपन्यास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है चाचा जिसका इस तथाकथित विकास से मोहभंग हो चुका है और वो आत्मनिर्वासन चुनता है, क्या आप मानते हैं कि जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं वहां हर संवेदनशील या रियलाइजेशन रखने वाले व्यक्ति की नियति चाचा बन जाना ही है?
चाचा बनना हर व्यक्ति की नियति नहीं है. उत्तर पूंजीवाद की दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, सबको इसका फायदा लेना है. इस अंधी दौड़ का नकार चाचा का अपना चयन है. उसके मुताबिक वह इसे बदल नहीं सकता लेकिन वह ये अहसास कराना चाहता है कि इस धरती पर कोई एक ऐसा भी है जो इसके अधिपत्य को स्वीकार नहीं करता. ये व्यवस्था से मुक्ति का रास्ता नहीं है. इस चरित्र के जरिए प्रतिरोध की चेतना दिखलाना मेरा उतना मकसद नहीं था जितना उस पीड़ा को दिखाना था जो आधुनिकता, विकास द्वारा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को अकेला, निहत्था कर दिए जाने से पैदा होती है. अकेले किया गया कोई प्रतिरोध बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकता. चूंकि इस व्यवस्था और आधुनिकता-पूंजीवाद का प्रतिरोध करने के लिए हमारे समाज में व्यापक रूप से कोई एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही है ऐसे में जो इसे नकारता है उसकी नियति हो सकती है कि वो चाचा जैसा हो जाए.
आधुनिकता और विकास को लेकर जो सवाल उपन्यास में उठाए गए हैं, गांधी ने भी उन सवालों को अपने ढंग से उठाया था तो क्या उपन्यास को रचते समय गांधी कहीं जेहन में थे?
निश्चित रूप से गांधी मेरे दिमाग में थे और इसीलिए एक अध्याय का शीर्षक बतर्ज हिन्द स्वराज है. वो पुस्तक भी एक तरह से इसी आधुनिकता की आलोचना थी. इसीलिए उस अध्याय का फॉर्मेट भी हिन्द स्वराज की तरह ही रखा गया है. इस अध्याय में विचार के स्तर पर, दर्शन के स्तर पर और सौन्दर्य चेतना के स्तर पर आधुनिकता को समस्याग्रस्त करने की कोशिश मैंने की है.
आप हमेशा कहते रहे हैं कि आप अपनी राजनीतिक चेतना या अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रचना नहीं करता. फिर इस अध्याय में जब पात्रों के बीच आधुनिकता, विकास और समाज जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर बहस हो रही है क्या तब भी आपकी अपनी सोच रचना में नहीं आई?
मैं अपने विचार चरित्रों पर नहीं लादता. ऐसा भी नहीं है कि लेखक के विचार रचना में आते नहीं हैं. लेकिन उन विचारों को चरित्र और यथार्थ नियंत्रित करते हैं. बुरा तब होता है जब चरित्र और यथार्थ को विचार अपने हिसाब से नियंत्रित करने लगे. ऐसा नहीं है कि विचार कोई रचना विरोधी चीज होती है लेकिन अगर विचार यथार्थ से बाहर तैरता दिखाई देगा या उसकी संवेदना को डैमेज करेगा तो मैं उसे एक रचना विरोधी कार्रवाई मानता हूं.
उपन्यास में एक जगह बिना नाम लिए पासिंग रेफरेंस के तौर पर नरेन्द्र मोदी का जिक्र आया है जबकि कई प्रसंगों में बहुत से नेताओं का बकायदा नाम आया है तो मोदी से गुरेज की क्या वजह थी?
मैं मोदी पर लिखने के लिए रचना नहीं कर रहा था. मुझे पुनरुत्थानवाद, आधुनिकता और विकास का जो स्वीकृत मॉडल है उसकी गहराई में जाकर उसे देखने और प्रकट करने का प्रयास करना था. दूसरे जो नाम यहां आए हैं वो लेखक की तरफ से एक वर्णन की शक्ल में आते हैं, जबकि मोदी वाली बात एक पात्र के कथन में आई है और वहां वही वाक्य रचना मेरे हिसाब से ठीक है. अगर मुझे मोदी को लेकर संकोच होता तो मैं वो बात ही न कहता. दरअसल मैं लाउड मुहावरे में बात नहीं करना चाहता.
इस उपन्यास में बीसवी सदी की कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है, कुछ आंकड़े भी हैं. इन सब पर लिखने के लिए कैसी तैयारी करनी पड़ी?
इस उपन्यास के लिए मैंने थोड़ा बहुत शोध किया है. अध्ययन भी. इसके अलावा सुल्तानपुर जनपद के गजेटियर के पन्ने भी पलटे हैं.
निर्वासन में आपने जाति, एवं स्त्री संबंधी प्रश्नों को भी सूक्ष्मता से उठाया है, अगर हिंदी के समकालीन परिदृश्य की बात करें तो इसमें अस्मिता के विमर्शों का हासिल क्या रहा?
हासिल क्या रहा इस पर कुछ कहने के बजाए ये कहना चाहूंगा कि मेरे विचार से मुक्ति की कोई लड़ाई अकेले नहीं हो सकती. दलित या स्त्री की मुक्ति के स्वप्न के पीछे अगर पूरे समाज की मुक्ति का स्वप्न नहीं होगा, तो आपकी मुक्ति की लड़ाई इकहरी होगी और देर-सबेर उसे असफल हो जाना है. साहित्य में जब विमर्श आते हैं तो चुनौती ये होती है कि विचार आपकी संवेदना, अनुभव और यथार्थ का हिस्सा बनकर सामने आएं. अस्मितावादी विमर्श के मामले में भी यही चीज महत्वपूर्ण है. जहां विचार आपमें इनबिल्ट होता है और आपकी संवेदना तथा भावबोध के साथ घुला हुआ आता है वहां तो अच्छी रचना होती है, लेकिन अगर आपकी प्रतिज्ञा रचनात्मकता और संवेदना न होकर अपने अस्मितावाद की नारेबाजी है तो रचना बेहतर नहीं होगी.
निर्वासन में बेशुमार किस्से आते हैं, इमरजेंसी के किस्से, गोसाईगंज के बसने के किस्से, चाचा भतीजे के किस्से… ये आपने खुद गढ़े हैं या लोक से उधार लिए हैं या हकीकत हैं और इन्हें कहानी में ढालना कितना मुश्किल होता है?
ऐसा नहीं है कि किस्से और कहानी का निर्धारण दो स्वतंत्र चीजे हैं. कई बार कहानी के निर्धारण की प्रक्रिया में किस्से उपजते हैं. जिन किस्सों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें प्राय: मेरी गढ़ंत है, लेकिन यह इसीलिए संभव हो सके हैं क्योंकि लोक में ऐसे किस्सों की समृद्ध परंपरा है. किस्सों के मामले में मैंने यह एहतियात जरूर बरती है कि वे हकीकत लगें. दरअसल आप कह सकते हैं कि इन किस्सों में आधी हकीकत आधा फसाना है.
निर्वासन के साथ-साथ एक और चीज जिससे इस उपन्यास के पात्र जूझते नजर आते हैं वो है नॉस्टेल्जिया. आप इसकी उपस्थिति उपन्यास में किस तरह देखते हैं?
नॉस्टेल्जिया और स्मृति में फर्क है. ये उपन्यास नॉस्टेल्जिया में फंसता नहीं है बल्कि उसका विखण्डन करता है. स्मृति यथार्थ की नाभि होती है और वह वर्तमान की व्याख्या में मददगार होती है. जबकि नॉस्टेल्जिया में अतीत का मोह होता है. आप देखेंगे कि उपन्यास के दो प्रमुख पात्र सूर्यकांत और गौरी अपने अतीत को लेकर ‘क्रिटिकल’ हैं साथ ही उसको लेकर विक्षोभ से भरे हुए हैं. सूर्यकांत जब न सिर्फ घर के लोगों द्वारा दिए गए सामानों का थैला ट्रेन से बाहर फेंक देता है तो वह एक तरह से नॉस्टेल्जिया से मोहभंग और उससे उबरने का प्रयास है.




