
सन 1964 में हम लोग भी दिल्ली आ गए थे और सप्ताह में चार-पांच शामें हमारी साथ ही गुजरती थीं. ज्यादातर कॉफी हाउस में तो कभी एक-दूसरे के घर में. कमलेश्वर जी और राकेश जी करोल बाग के डब्ल्यू के एक ही मकान में ऊपर नीचे रहते थे और हम शक्तिनगर में. जहां तक याद है सन 64 की न्यू ईयर ईव हमारे घर मनाने की योजना बनी. हंसी-मजाक और दुनिया जहान की बातों के बीच इस पर भी चर्चा हुई कि नए साल में क्या-क्या करना है. साढ़े ग्यारह बजे के करीब कमलेश्वर जी ने जेब से कुछ कागज निकाले और बोले, ‘तुम लोग तो जो करोगे सो करोगे पर मैंने तो आज से ही नए साल की शुरुआत कर दी… लो, सुनो मेरी कहानी.’ और उन्होंने अपनी नई कहानी पढ़ना शुरू कर दिया. शीर्षक था ‘तलाश’. रात का वह माहौल… मोमबत्ती की रोशनी में कमलेश्वर जी का कहानी पढ़ना (इस कला में तो माहिर थे वे). कुछ ऐसा समां बंधा कि हम लोग मंत्र-मुग्ध से कहानी सुनते रहे. बारह बजे उन्होंने सारी बत्तियां जलाईं और कहानी हमारे सामने पटकते हुए बोले, ‘लो मैंने तो नए साल का झंडा गाड़ दिया… अब दिखाओ इसके टक्कर की कहानी लिखकर. ‘कहानी सचमुच अच्छी थी (बाद में इस पर ‘फिर भी’ नाम की फिल्म भी बनी… कहानी का शुद्ध बलात्कार). कुछ देर उसी पर बात होती रही और मैं यही सोचती रही कि दुनिया भर के प्रपंचों के बीच बिना किसी तामझाम के कैसे लिख लेते हैं कमलेश्वर जी कहानियां? अपनी कई छोटी-मोटी खुराफातों के बावजूद उस समय कमलेश्वर जी कमलेश्वर जी थे… वे कमलेश्वर जी जिनके प्रति मेरे मन में सम्मान था, लगाव था, अपनत्व था और जिनसे मैं गहरे से जुड़ी हुई भी थी.
वे जितने अच्छे कथाकार थे उससे कहीं ज्यादा अच्छे किस्सागो थे. विट और ह्यूमर उनकी बातों में इस तरह गुंथे रहते कि सुनने वाले लहालोट हो जाएं और सुनाने की अदा… आज तक मैंने किस्सा सुनाने की ऐसी अदाकारी किसी में नहीं देखी. किस्सों की कोई कमी न थी उनके पास. शैतानी में लिपटे वे किस्से जो केवल हंसने-हंसाने के लिए होते थे. जिनको लेकर किस्से गढ़े जाते थे वह भी हंसता था. सुनने वाले भी हंसते थे और सुनाने वाले की हंसी तो सुनाने के ढंग में ही लिपटी रहती थी. अपने विरोधियों की लानत-मलामत करने वाले किस्से उनकी अनुपस्थिति में ही सुनाए जाते थे. जिन पर केवल सुनने वाले ही हंसते थे. कुछ नॉनवेज किस्म के किस्से, जिन्हें सुनाने से पहले वे मुझ से अनुरोध करते थे कि मैं वहां से हट जाऊं. मेरे न हटने पर क्षमा-याचना सहित वे सुना ही डालते थे. झूठ में लिपटे कुछ किस्से उन्होंने अपने को लेकर भी गढ़ रखे थे… लेकिन यहां बात हंसने-हंसाने की नहीं बल्कि एक अनकहे दंभ की होती थी… इन्हें बार-बार दोहरा कर, लिखकर वे खुद भी इनकी सच्चाई पर विश्वास करने लगते थे.
जैसे-जैसे कमलेश्वर जी का कमलेश्वरपन (जिससे मुझे लगाव था) खत्म होता जा रहा था, झूठ में लिपटे ऐसे किस्सों की संख्या बढ़ती जा रही थी. मैं सोचती कि क्या कमलेश्वर जी मित्रों को या पढ़ने-सुनने वालों को बेवकूफ समझते हैं… अरे वे सब भी तो इसी साहित्यिक दुनिया में रहते हैं… और सब कुछ जानते-समझते देखते हैं… उनके सामने कैसे इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं. शुरू में शायद थोड़ा कम पर धीरे-धीरे झूठ उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गया था. खैर ये सब बाद की बातें- अभी तो मैं लौटती हूं सन 64 पर.
राकेश जी और कमलेश्वर जी के जबरदस्त आग्रह और राजेंद्र की अकुलाहट भरी बेचैनी के चलते हम दिल्ली आए थे. राजेंद्र से तो इन लोगों की अंतरंगता थी ही दिल्ली आकर मेरी मित्रता भी कब अंतरंगता में बदल गई, इसका एहसास ही नहीं हुआ. साहित्यिक बातों के साथ-साथ, बिना किसी हिचक के हम लोग निजी बातें भी शेयर करते पर मैंने एक बात नोटिस की कि मैं जब उन दिनों अपने दुख, अपनी यातना की बातें कमलेश्वर जी के आगे उड़ेलती तो वे केवल सुनते ही नहीं मुझे बहुत सांत्वना भी देते… दुलराते भी थे… पर अपने निजी जीवन की कोई बात कभी होठों पर नहीं लाते. कई बार मेरा मन हुआ कि उनसे दीपा की बात पूछूं पर यही सोचकर चुप रह जाती कि जो प्रसंग समाप्त हुआ, उसे कुरेदकर क्यों व्यर्थ ही उनके घाव को हरा करूं? पर देर-सबेर उन बातों की जानकारी तो मिलनी ही थी सो मिली और मैं हैरान. दीपा दिल्ली में ही एक अलग मकान में रहती थी और कमलेश्वर जी के साथ उसके संबंध बदस्तूर चालू थे. इतना ही नहीं, दीपा से उनका एक बेटा भी था यानी उनके दो घर थे. बेटी मानू के साथ गायत्री का एक घर और बेटे (जिसका नाम मुझे नहीं मालूम) के साथ दीपा का दूसरा घर. दोनों को चलाने की जिम्मेदारी कमलेश्वर जी पर. यह तो गनीमत थी कि ओमप्रकाश जी ‘नई कहानियां’ पत्रिका दिल्ली ले आए थे और उसकी संपादकी इन्हें सौंप दी थी. इस संपादकी से कुछ आर्थिक जुगाड़ तो हो ही गया था… फिर भी दो घर चलाने के कारण आर्थिक संकट बराबर बना रहता था. इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए जैसी हेराफेरी वे करते… जैसी तिकड़मबाजियां करते… क्या कहूं उन सबके लिए? एक छोटा-सा उदाहरण जरूर दूंगी.
उन्होंने एक उपन्यास की पांडुलिपि एक प्रकाशक को दी और उससे अग्रिम रॉयल्टी ले ली. फिर उपन्यास का शीर्षक बदलकर (हो सकता है शुरू की कुछ पंक्तियां भी बदल दी हों) वही पांडुलिपि दूसरे प्रकाशक को भी दे दी और उससे भी अग्रिम रॉयल्टी झटक ली. छपने के बाद बात खुली… हंगामा हुआ. मैं नहीं जानती उन्होंने इसे कैसे सुलटाया… उनके लिए तो इतना ही काफी था कि उन्हें रुपये मिल चुके थे. मेरे लिए ऐसी बातें अक्षम्य अपराध की कोटि में आती थीं पर आश्चर्य कि कमलेश्वर जी को लेकर मुझे क्रोध नहीं आया. बल्कि मैं ऐसी बातों को उनके अभाव और परिस्थितिजन्य मजबूरियों के साथ जोड़कर दरकिनार भी कर देती थी. यह भी सुना कि दीपा अपने नाम के आगे कमलेश्वर लिखती थी. घर के बाहर भी उसने दीपा कमलेश्वर के नाम की नेमप्लेट लगा रखी थी. लड़-झगड़कर कमलेश्वर जी ने उसे मजबूर किया कि वह उनका नाम हटाए और कभी, कहीं भी अपने नाम के साथ उनके नाम का प्रयोग न करे. वे संबंध रखने में तो विश्वास रखते थे पर उन संबंधों के बारे में लोग जानें, यह उन्हें गवारा न था. कैसा था यह संबंध? इलाहाबाद का वह भावनात्मक लगाव क्या अब केवल शरीर तक आकर सिमट गया था? वैसे तो वे दीपा को छोड़ भी सकते थे पर बेटे से शायद उन्हें बहुत लगाव था. राकेश जी ने एक बार मुझे बताया था कि वैसे तो कमलेश्वर अपनी निजी जिंदगी की बात कभी नहीं करता… बस एक बार उसने अपने पर्स से अपने बेटे की फोटो मुझे दिखाई थी.
सन 65 में श्रीमती शीला संधू ने राजकमल प्रकाशन का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर ओमप्रकाश जी को वहां से हटा दिया. ओमप्रकाश जी के लिए यह झटका था ही, राकेश जी के लिए भी कम झटका नहीं था. नई कहानियां पत्रिका राजकमल से ही निकलती थी सो राजकमल के साथ पत्रिका भी शीला जी के पास चली गई और राकेश जी और कमलेश्वर जी को भी उसकी संपादकी छोड़नी पड़ी. कमलेश्वर जी का यह आर्थिक आधार भी जाता रहा… अब क्या करें? यों छुटपुट काम तो कुछ न कुछ करते ही रहते थे पर जरूरत थी एक ठोस आधार की. तभी कलकत्ता में एक विशाल कथा समारोह आयोजित करने की योजना बनी. आयोजक पत्र-व्यवहार द्वारा इन लोगों से भी सलाह-सुझाव मांगते रहते थे. ये आयोजकों को तो सुझाव देते ही थे… अपनी योजना भी बनाते रहते थे. साहित्य की राजनीति का मैं तो क, ख, ग भी नहीं जानती थी…न उस दिशा में मेरी कोई रुचि थी पर इनकी बातें सुनती तो थी ही. इनकी प्रत्यक्ष-परोक्ष बातों को सुनकर इतना समझ गई कि कथा समारोह में शिरकत करने का इनका मुख्य उद्देश्य था पुरानी पीढ़ी को ध्वस्त करके अपनी पीढ़ी को जमाना… पीढ़ी तो क्या अपनी तिकड़ी को जमाना. राकेश जी सन 62 में सारिका की संपादकी छोड़कर आ गए थे. कलकत्ता में बहुत आग्रह करने पर भी राजेंद्र ने उसे स्वीकार नहीं किया सो अभी चंद्रगुप्त विद्यालंकार उसके संपादक थे. सुना था कि प्रबंधक उनसे बहुत संतुष्ट नहीं थे. समारोह में जाने का मुख्य उद्देश्य तो था पुरानी पीढ़ी को ध्वस्त करना लेकिन अप्रत्यक्ष उद्देश्य था कमलेश्वर जी के लिए सारिका की संपादकी हथियाना. पर इसका सारा दारोमदार तो कमलेश्वर जी पर ही था.
समारोह हुआ और हर सेशन में राकेश जी और कमलेश्वर जी ने वो धुआंधार भाषण दिए कि नई कहानी का झंडा तो गाड़ा ही अपने नाम के परचम भी लहरा दिए. चारों तरफ इन दोनों के हल्ले थे. इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों ही बहुत अच्छे वक्ता थे. राजेंद्र ने तो इस कला को साधा ‘हंस’ निकलने के बाद.
कहने का मतलब यह है कि एक उद्देश्य तो इन्होंने पूरा कर लिया और दूसरे की एक पुख्ता पृष्ठभूमि तैयार कर ली. साहित्य और साहित्यकारों में विशेष रुचि रखने वाली श्रीमती रमा जैन भी इस समारोह में दिख जाती थीं और अनुमान है कि कमलेश्वर जी अपने भाषणों के कारण उनकी नजरों में भी अटके ही होंगे. एक दिन जब रमा जैन ने आयोजन में शिरकत करने वाले कथाकारों को अपने घर पर दावत दी तो कमलेश्वर जी शायद संवाद बनाने के इरादे से उनके इर्द-गिर्द ही घूम-टहल रहे थे. बैठे चाहे हम दूसरी तरफ थे पर नजर तो हम लोगों की भी कमलेश्वर जी पर ही टिकी थी और एक बार जब मेहमान होकर भी मेजबान की तरह वह एक प्लेट लेकर रमा जी को कुछ सर्व करने पहुंचे तो लगा कि हो गई कमलेश्वर जी की नौकरी पक्की. कुछ समय बाद वे सारिका के संपादक नियुक्त हो गए.
कथा समारोह से लौटे तो लग रहा था जैसे किला फतह करके लौटे हों. कहने को चाहे नई कहानी का नाम हो पर असल में तिकड़ी का बल्कि कहूं कि ये दोनों अपने नाम का झंडा गाड़ कर आए थे. आश्चर्य तो मुझे इस बात का होना चाहिए कि उस समय एक से एक अच्छे कथाकार जैसे अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा आदि सक्रिय थे और उन्होंने कई अच्छी कहानियां हिंदी को दीं उसके बावजूद यह इनका कौशल ही था कि जहां-तहां नई कहानी के साथ नाम इन्हीं तीनों के लिए जाते. बाकी कथाकार अपनी कहानियां लिखते रहते पर ये भाषण दे-दे कर कॉलम और लेख लिखकर अपनी रचनाओं से कहीं अधिक अपने नाम का डंका बजवाते रहते. लिखना तो एक कला है ही पर अपने लिखे की खूब धूम मचवाना उससे भी बड़ी कला है जिसे साध रखा था राकेश जी ने और कमलेश्वर जी को तो उनके पीछे चलना ही था. सारिका में जाने के बाद राकेश जी का साया तो उन पर से हटा पर इस कला को उन्होंने नहीं छोड़ा बल्कि समय के साथ साथ इजाफा ही करते रहे. हंस निकालने के बाद राजेंद्र ने भी इसे ज्यों का त्यों अपनाया. इन तीनों का एक ही लक्ष्य था जैसे भी हो साहित्य के क्षेत्र में हमेशा चर्चा के केंद्र में बने रहना.
सन 66 में कमलेश्वर जी सारिका की संपादकी संभालने बंबई चले गए. इसमें कोई संदेह नहीं कि कमलेश्वर जी का व्यक्तित्व ही बहुआयामी नहीं था, वे बहुआयामी प्रतिभा के भी धनी थे. सो सारिका ने फिर से अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली. उसमें प्रतिष्ठित लेखक तो छपते ही थे, नए लेखकों को प्रकाश में लाने का उनका प्रयास भी बराबर जारी रहा. उन्होंने टीवी में ‘परिक्रमा’ नाम से एक सीरियल शुरू किया. इसमें वे निम्नवर्ग के लोगों जैसे भाजी बेचने वाले, ठेले वाले, धोबी, घर में काम करने वाली बाई का इंटरव्यू लेते, इंटरव्यू क्या उनसे बातचीत करते थे. उनकी विशेषता थी कि कैमरे के सामने आते ही लोगों की घबराहट को वे अपने आत्मीय व्यवहार से केवल दूर ही नहीं कर देते थे बल्कि उन्हें इतना सहज बना देते थे कि फिर वे बिना किसी संकोच-झिझक के अपना संघर्ष, अपनी समस्याएं, अपनी कठिनाइयां कमलेश्वर जी के सामने खोलते चलते थे. कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि उनकी पहचान ही इसके साथ जुड़ गई. इस कला में सचमुच माहिर थे कमलेश्वर जी. उनकी आवाज, बात करने का उनका अंदाज सामने वाले को अपने साथ जोड़ लेने की उनकी क्षमता सब बेजोड़ थी.
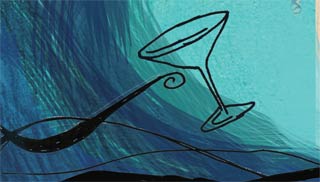
कमलेश्वर जी के बंबई जाने के कुछ समय बाद हम लोग भी उनके पास बंबई गए थे. वार्डन रोड में इन्हें सारिका की ओर से एक अच्छा फ्लैट मिला हुआ था. हम जब तक रहे बहुत खातिर की हम लोगों की. भाभी बड़े प्रेम से हम लोगों के लिए खाना बनातीं और तब मैंने महसूस किया कि मेहमाननवाजी भी एक बड़ी विशेषता है कमलेश्वर जी की. भाभी के चेहरे पर भी मैंने पहली बार ऐसी चमक देखी. पैरों के नीचे आर्थिक सुरक्षा की ठोस जमीन, कमलेश्वर जी का बेटी मानू के प्रति गहरा लगाव और शायद दीपा-दंश से मुक्ति. कमलेश्वर जी के भी सबसे अच्छे दिन थे ये, अपनी प्रतिभा और बलबूते से पाई यह नौकरी, मासिक पत्रिका के संपादक का रुतबा, जिसके चलते प्रशंसकों और चहेतों की भीड़ तो अगल-बगल में जुटी ही रहती थी. निरंतर फैलता यश और शायद एक अनकहा सा कारण राकेश जी के वर्चस्व के साये का हटना. इस संदर्भ में एक घटना का उल्लेख करूंगी.
‘नई कहानियां’ पत्रिका की संपादकी कमलेश्वर जी को राकेश जी के कहने पर ही मिली थी. ओमप्रकाश जी से राकेश जी के संबंध मात्र प्रकाशक, लेखक के ही नहीं, बल्कि कहीं अधिक घनिष्ठ थे. इसीलिए जब ‘नई कहानियां’ दिल्ली आई तो उनके कहने से ही उसकी संपादकी कमलेश्वर जी को मिली और सौजन्य-संपादक वे खुद बने. पत्रिका के कवर पर इन दोनों के नाम इसी तरह जाते थे. एक दिन राकेश जी के हाथ की लिखी छोटी-छोटी पर्चियां लेकर कमलेश्वर जी हमारे शक्तिनगर वाले फ्लैट में आए, बेहद दुखी और त्रस्त. उन पर्चियों को हमारे सामने फैलाते हुए बोले, ‘ऊपर नीचे ही तो रहते हैं- मुझे बुलाकर पूछ सकता था- बता सकता था पर नहीं, ये पर्चियां भेज-कर बॉसगीरी झाड़ता रहता है. एक तरफ तो मित्रता और एक तरफ ये व्यवहार. मैं क्या समझता नहीं.’ खैर उस समय तो इस बात को नजर -अंदाज करने की सलाह देकर उन्हें शांत किया पर बाद में मैं इस पर जरूर सोचने लगी. कलकत्ता के कथा समारोह से लौटकर एक बात जो मैंने जानी समझी वह यह कि अपने वर्चस्व और अपनी श्रेष्ठता को लेकर राकेश जी हमेशा बहुत सजग, बहुत चौकस रहते थे. बंबई आकर कमलेश्वर जी इन बातों से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे और राकेश जी के लिए उनके मन में पहले जैसा सम्मान, लगाव और अपनत्व बरकरार था.




