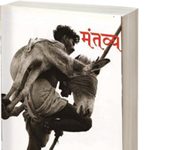दूरदर्शन के एक प्रसारण में कैफ़ी आजमी से पूछा गया- आपकी पहचान नज़्मों के लिए रही है, ग़ज़लें आपने बहुत कम कही हैं. लेकिन इन दिनों आप फिर से ग़ज़लें कहने लगे हैं. इसकी क्या वजह है? कैफ़ी ने जवाब दिया, ‘मैंने वापस ग़ज़लें कहना उसी वजह से शुरू किया जिस वजह से ग़ालिब मुसव्विरी सीखना चाहते थे. मैं ग़ज़ल इसलिए कहता हूं ताकि मैं ग़ज़ल यानी बेगम अख़्तर से नज़दीक हो जाऊं.’ कैफ़ी आज़मी का ये जुमला बेगम अख़्तर की शख़्सियत के बारे में बहुत कुछ कह जाता है. वो सचमुच हमारे मुल्क, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ग़ज़ल का दूसरा नाम हैं. किसी भी महफिल में जब ग़ज़ल का ज़िक्र छिड़ता है, तो बात बेगम अख़्तर से ही शुरू होती है और उन्हीं पर आकर ख़त्म होती है. बेगम अख़्तर ने ग़ज़ल गायिकी को और ग़ज़ल गायिकी ने बेगम अख़्तर को बेपनाह शोहरत अता की. कोठे से उतरी ठेठ दरबारी शैली की ग़ज़ल गायिकी को आवाम के बीच रचा-बसा देने का करिश्मा वही कर सकती थीं.
दूरदर्शन के एक प्रसारण में कैफ़ी आजमी से पूछा गया- आपकी पहचान नज़्मों के लिए रही है, ग़ज़लें आपने बहुत कम कही हैं. लेकिन इन दिनों आप फिर से ग़ज़लें कहने लगे हैं. इसकी क्या वजह है? कैफ़ी ने जवाब दिया, ‘मैंने वापस ग़ज़लें कहना उसी वजह से शुरू किया जिस वजह से ग़ालिब मुसव्विरी सीखना चाहते थे. मैं ग़ज़ल इसलिए कहता हूं ताकि मैं ग़ज़ल यानी बेगम अख़्तर से नज़दीक हो जाऊं.’ कैफ़ी आज़मी का ये जुमला बेगम अख़्तर की शख़्सियत के बारे में बहुत कुछ कह जाता है. वो सचमुच हमारे मुल्क, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ग़ज़ल का दूसरा नाम हैं. किसी भी महफिल में जब ग़ज़ल का ज़िक्र छिड़ता है, तो बात बेगम अख़्तर से ही शुरू होती है और उन्हीं पर आकर ख़त्म होती है. बेगम अख़्तर ने ग़ज़ल गायिकी को और ग़ज़ल गायिकी ने बेगम अख़्तर को बेपनाह शोहरत अता की. कोठे से उतरी ठेठ दरबारी शैली की ग़ज़ल गायिकी को आवाम के बीच रचा-बसा देने का करिश्मा वही कर सकती थीं.
ग़ज़ल उनकी गायिकी का सबसे दिलकश अंदाज़ ठहरा, लेकिन उनकी ज़ंबील में ग़ज़ल के अलावा ठुमरी, चैती, दादरा, ख़याल आदि विधाओं के भी बेशुमार नगीने हैं. उपशास्त्रीय गायन का सम्मोहन बेगम अख़्तर के यहां अपने शबाब पर दिखता है. जो कुछ भी उन्होंने गाया, यूं लगा कि वो बेगम के लिए ही बना है और बेगम भी उसी के लिए ही बनी हैं. उनके अनन्य प्रशंसक यतीन्द्र मिश्र उनकी गायिकी को विश्लेषित करते हुए लिखते हैं, ‘उनकी शास्त्रीय संगीत की परंपरा पटियाला घराने के उस्ताद अता मोहम्मद ख़ान और किराना घराने के दिग्गज उस्ताद अब्दुल वाहिद ख़ान से संबद्ध रही है. वे जहां पटियाला घराने की गंभीर गायकी में अपने उस्ताद से ग़ज़ल, ठुमरी और दादरा सीखने में व्यस्त रहीं, ठीक उसी समय उन्हें किराना घराने के ख़याल की बारीकियों को सीखने का अवसर मिला. बेग़म अख़्तर की पूरी संगीत यात्रा, इन्हीं दो घरानों के बीच किसी नाजुक बिन्दु पर संतुलित मिलती है’. यतीन्द्र के मुताबिक उनके लिए संगीत सिरजना सिर्फ़ राग, ताल और धुनों पर ही आधारित काम नहीं था, बल्कि वे गीत के शब्दों और बोलों की सटीक अर्थ-व्याप्ति के लिए भावों को बहुत गौर से बरतने में तल्लीन दिखाई पड़ती हैं.
बिब्बी से अख़्तरी, अख़्तरी से अख़्तरीबाई फैज़ाबादी और अख़्तरीबाई फैज़ाबादी से बेगम अख़्तर बनने के सफ़र में ग़म और गायिकी दोनों उनके हमसफ़र बने रहे
बेगम अख़्तर की गायिकी के इस वैभव के नज़दीक जाने के लिए उनके जीवन के नज़दीक जाना जरूरी है. अंतिम दिनों में एक उद्घोषिका ने रेडियो पर उनको बेग़म अख़्तर कह कर संबोधित कर दिया, तो बेगम ने उससे कहा, ‘बेटी पूरी ज़िंदगी तो ग़मों के बीच ही गुज़री है, मैं बेग़म कहां हूं?’ बिब्बी से अख़्तरी, अख़्तरी से अख़्तरीबाई फैज़ाबादी और अख़्तरीबाई फैज़ाबादी से बेगम अख़्तर बनने के सफ़र में ग़म और गायिकी दोनों उनके हमसफ़र बने रहे. जन्म फैज़ाबाद के करीब भदरसा कस्बे में जुड़वा बहन के साथ 7 अक्टूबर 1914 को हुआ. नाम मिला बिब्बी उर्फ अख़्तरी. उनकी मां मुश्तरीबाई अपने ज़माने की मशहूर गानेवाली थीं, जबकि वालिद सैयद असग़र हुसैन सिविल जज थे, जिन्होंने मुश्तरी को किसी महफिल में सुना था और फिर दूसरी बीवी के तौर पर अपने घर ले आए थे. अख़्तरी अभी तीन साल की भी नहीं हुईं थीं कि उनकी जुड़वा बहन अनवरी का इंतक़ाल हो गया और इसके थोड़े ही वक्त बाद उनके वालिद ने उनकी मां मुश्तरी को छोड़ दिया. मां पर पड़ी दुखों की इस दोहरी मार को अख़्तरी ने भी बहुत छोटी उम्र में ही न केवल महसूस किया, बल्कि उनके साथ-साथ भोगा भी. अख़्तरी की मां उनके सबसे नज़दीक थीं. उनकी पूरी शख़्सियत पर मां की अटूट छाप दिखाई देती है. मां ने तमाम मुसीबतों और मुफ्लिसी के बीच जिस तरह अख़्तरी की तरबियत की, वो भी अपने आप में एक मिसाल है. आकाशवाणी के लिए बेगम अख़्तर के जीवन पर ‘कुछ नक़्श तेरी याद के’ जैसा चर्चित धारावाहिक लिखने वाले पत्रकार अटल तिवारी मुश्तरी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं- ‘मुश्तरी ने जिस तरह का अविश्वसनीय संघर्ष अपनी बेटी का मुस्तकबिल संवारने के लिए किया, वो उन्हंे किसी प्रेरणाप्रद नायिका की तरह सामने लाता है. उस वक़्त के समाज में बेटी को अकेले पालना, उसे कोठे की रिवायत से निकालने के लिए अलग-अलग शहरों में ले जाकर बड़े-बड़े उस्तादों से तालीम दिलवाना, बेटी की तालीम के लिए अपना सब कुछ बेच देना वगैरह इस बात की बानगी है कि मुश्तरी में किस दर्जे की दूरदर्शिता, प्रगतिशीलता और विद्रोह था.’
बचपन की पढ़ाई-लिखाई में अख़्तरी का ज्यादा मन नहीं लगा, अलबत्ता फैज़ाबाद के मिशन स्कूल में वो टीचर की चोटी काट देने जैसे कारनामों से ज़्यादा जानी जाती रहीं. लेकिन मां से नज़दीकी की वजह से गायिकी की तरफ बचपन से ही उनका संजीदा रुज्हान रहा. इसे देखते हुए मां ने मशहूर सारंगी वादक इमदाद अली खां से अख़्तरी को सिखाने को कहा. अख़्तरी ने अभी सीखना शुरू ही किया था कि फैज़ाबाद में उनका घर जला दिया गया. पतियों द्वारा छोड़ी जा चुकी तवायफों के ऊपर इस तरह के ख़तरे उन दिनों आम थे. फैज़ाबाद से दाना-पानी उठने के बाद मां-बेटी ने बिहार के गया का रुख किया. गया पहुंचने के बाद मुश्तरी ने बेटी की संगीत शिक्षा की तरफ और संजीदगी से ध्यान दिया. गहने, बर्तन बेच-बेचकर उन्होंने बेटी को पहले सख़ावत हुसैन और फिर पटियाला घराने के उस्ताद अता मोहम्मद से तालीम दिलवाई. मां के अलावा अख़्तरी की गायिकी पर बुनियादी असरात अता मोहम्मद के ही दिखते हैं. सीखा भी अख़्तरी ने सबसे ज़्यादा उन्हीं से.
अख़्तरी की पूरी शख़्सियत पर मां की अटूट छाप दिखाई देती है. मां ने तमाम मुसीबतों और मुफ्लिसी के बीच जिस तरह अख़्तरी की तरबियत की, वो भी अपने आपमें एक मिसाल है
1924 में अख़्तरी मां के साथ कोलकाता चली आईं, जो उस वक्त गीत, संगीत और नाटक का गढ़ था, फिल्म इंडस्ट्री भी वहीं थी. अता मोहम्मद से उनकी तालीम लंबे वक्त तक जारी रही. इसके बाद उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खां और अंत में झंडे खां से सीखा. इस दरमियान अख़्तरी कोलकाता की छोटी-मोटी निजी नशिस्तों में जाने लगी थीं. लेकिन कोलकाता में उनकी गायिकी ने पहले-पहल धूम सिर्फ बीस साल की उम्र में 1934 में मचाई, जब भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की मौजूदगी में उन्होंने बिहार भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए एक आयोजन में स्थानापन्न कलाकार के बतौर गाते हुए सैंकड़ों दर्शकों पर जादू कर दिया था. इस जलसे की तब के कलकत्ता में बड़ी चर्चा हुई और इसी के बाद अख़्तरी अख़्तरीबाई फैज़ाबादी बन गईं. लेकिन गाने वाली बाइयों के साथ होनेवाला व्यवहार उन्हें हमेशा सालता रहा. इस सिलसिले में उनका क़ौल मशहूर है, ‘इस समाज को क्या कहा जाए, जहां मर्द अच्छा गाता है, तो उस्ताद या पंडित कहलाता है और औरत अच्छा गाती है तो बाई कहलाती है.’
1934 में ही मेगाफोन कंपनी के मालिक जेएन घोष ने उन्हें छह ग़ज़लें रिकॉर्ड करने का प्रस्ताव दिया, जिसे अख़्तरी ने कुबूल कर लिया. रिकॉर्ड की गई उनकी पहली ग़ज़ल थी, वो असीरे दामे बला हूं. मेगाफोन द्वारा जारी किया गया ये रिकॉर्ड चल निकला और अख़्तरी ने पहली बार शोहरत का स्वाद महसूस किया. इसके बाद उनके ठुमरी, दादरा, चैती और ख़याल गायिकी के भी कई रिकॉर्ड्स निकले और कामयाब रहे. जिसके चलते 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, कोलकाता ने भी उन्हें रिकॉर्ड किया. इस बीच वो बतौर अभिनेत्री फिल्म और थिएटर में भी काम करना शुरू कर चुकी थीं. लैला मजनूं (1934) और नई दुल्हन (1934) उनके मशहूर नाटक थे. साथ ही नल दमयंती (1933), एक दिन का बादशाह (1933), मुमताज़ बेगम (1934), अमीना (1934), रूपकुमारी (1934), जवानी का नशा (1935), नसीब का चक्कर (1936) जैसी फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम करने के बाद उनकी शोहरत अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी और इसका सीधा फ़ायदा उनकी व्यावसायिक गायिकी की साख को हुआ था. मेगाफोन कंपनी अब उनके रिकॉर्ड्स का बाकायदा विज्ञापन जारी करती थी, जिस पर उनका परिचय लिखा होता था- ‘अख़्तरीबाई फैज़ाबादी फिल्म स्टार’. इस दौरान एक फिल्म कंपनी बिना उनका बकाया चुकाए बंद हो गई, तो उन्होंने उस पर मुकदमा करने की भी ठान ली. इसी सिलसिले में 1937 में लखनऊ के बैरिस्टर इश्तियाक़ अहमद सिद्दीक़ी से उनकी पहली मुलाक़ात हुई थी. इतना ही नहीं अब उन्हें हिंदुस्तान के प्रमुख दरबारों से ख़ुसूसी न्यौता भी मिलने लगा था. निज़ाम हैदराबाद ने उनके लिए सौ रुपये प्रतिमाह का वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर दिया था, तो नवाब रामपुर ने उन्हें अपने दरबार में अहम पदवी से नवाजा था. अख़्तरी अब आधा वक्त रामपुर में और आधा लखनऊ में गुज़ारने लगी थीं.
1924 में अख़्तरी कोलकाता आईं, जो उस वक्त गीत, संगीत और नाटक का गढ़ था. कोलकाता में उनकी गायिकी ने पहले-पहल धूम सिर्फ बीस साल की उम्र में मचाई
1938 में अख़्तरी ने लखनऊ में अपना ख़ुद का घर बनवाया, वो भी हज़रतगंज जैसे इलाके के पास. ये कदम उनके रुतबे का पता देता है, क्योंकि उस वक्त तक लखनऊ की ज़्यादातर गानेवालियां चौक या दूसरे इलाक़ों की गलियों में रहती आईं थी. हज़रतगंज के आसपास उनका क़याम कभी नहीं रहा था. अख़्तरी ने ये दस्तूर बदला, क्योंकि शहर के ज़्यादातर रईस हज़रतगंज के आसपास ही रहते थे. व्यावसायिक तौर पर ये जगह उनके लिए ज़्यादा मुफ़ीद थी. फिल्म अभिनेत्री होने के बावजूद उनकी ज़्यादा मज़बूत पहचान गायिका की ही थी. रामपुर दरबार से जुड़ जाने के बाद भी लखनऊ में वो महफ़िलों का हिस्सा लगातार बनी रहीं. मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी बेगम की गायिकी के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें कहती हैं, ‘पहली बात तो ये है कि वो जिस मिट्टी की थीं यानी लखनऊ-फैज़ाबाद उसके संगीत की तमाम विधाओं को उन्होंने इस ख़ूबी के साथ गाया कि वो सभी पूरी दुनिया में पहुंच गईं. ठुमरी, दादरा, चैती, होरी, कजरी, मर्सिया, ग़ज़ल सब कुछ. उन्होंने अपने आपको कभी किसी एक विधा (जैसे ग़ज़ल) में महदूद नहीं किया. ये काम उनके चाहनेवालों ने किया. दूसरी बात कि उन्होंने कठिन चीज़ें भी जिस सहजता से गा दी हैं, वो बताता है कि उनकी अपनी आवाज़ पर कितनी पकड़ थी, कितनी समझ थी, कितना परिचय था. ये लंबे रियाज़ के बाद आता है. इसी का नतीजा है कि बेगम जब गाती हैं, तो बेहद कठिन चीज़ को भी बेहद आसानी से निभा ले जाती हैं और साधारण से साधारण श्रोता को भी मंत्रमुग्ध कर देती हैं.’
1940 के आस पास उनका फ़िल्मों से जी उचाट होने लगा था. क्योंकि उनके उस्ताद अता मोहम्मद को उनका फिल्मों में काम करना गायिकी के साथ अन्याय लगता था. वे इसके ख़िलाफ़ थे. नवाब रामपुर भी उनके फ़िल्मों में काम करने के पक्ष में नहीं थे. इसलिए महबूब खान की फिल्म रोटी (1942) के बाद उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया. अब वो पूरा ध्यान अपनी गायिकी पर देने लगीं. उम्र अब तीस के करीब पहुंच रही थी, इसलिए लड़कपन की शोख़ी भी अब संजीदगी में बदल रही थी. ज़िंदगी एक दूसरे तरह का स्थायित्व चाह रही थी. नवाब रामपुर ने उनसे शादी करने की ख्वाहिश भी जताई, लेकिन अख़्तरी ने ख़ुद को नाचीज़ कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया. उन्होंने अपने लिए लखनऊ के बैरिस्टर अब्बासी को चुना, जिनसे उनकी पुरानी आश्नाई थी. दोनों एक-दूसरे के क़ायल भी थे. मगर अख़्तरी के गाने-बजाने का पेशा अब्बासी और उनके बीच दीवार बना हुआ था. फिर एक दिन अख़्तरी ने फैसला किया कि वो गाना छोड़कर अब्बासी का हाथ थामेंगी. हुआ भी ऐसा ही. 1945 में अख़्तरी बाई फैज़ाबादी बेगम अख़्तर बन गईं और गायिकी से उनका रिश्ता टूट गया.
फिल्म अभिनेत्री होने के बावजूद अख्तरी की ज़्यादा मज़बूत पहचान गायिका की ही थी. रामपुर दरबार से जुड़ने के बाद भी लखनऊ में वो महफ़िलों का हिस्सा लगातार बनी रहीं
बेगम दुनिया में गाने के लिए ही आईं थीं. उनकी मां ने उनको ढाला भी ऐसे ही था. बेगम के हज़ारों चाहनेवालों को उनके गाना छोड़ने का रंज था. इस बात से सबसे ज़्यादा दुखी उनकी मां मुश्तरी ही थीं. उन्होंने अपना पूरा जीवन अख़्तरी के लिए वक़्फ कर दिया था. मुसीबतें उठा-उठाकर उनको तालीम दिलवाई थी. यहां तक कि अख़्तरी जब स्टार बन गईं थीं, तब भी मुश्तरी उनके एक-एक कदम का हिसाब रखतीं थीं और उनको गाहे-बगाहे सलाह भी देती रहती थीं. बेगम ने गाना छोड़ा, तो उनकी मां पूरा-पूरा दिन उनके रिकॉर्ड सुनती रहतीं और रोती रहतीं. खुद बेगम अख़्तर की हालत गाने के बिना बेहाल थी. अब वो अकेलेपन और अवसाद में घिर गईं थीं, जिसने धीरे-धीरे कई बीमारियों को दावत दे दी थी. तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हुई, तो डाक्टरों ने उनके पति अब्बासी से कहा कि अब इन्हें गाने की इजाज़त दे दी जाए, तभी तबीयत संभल सकती है. आख़िरकार शौहर ने हारकर बेगम को वापस गाने के लिए कहा. इसके बाद बेगम ने चार साल के तवील अंतराल के बाद 1949 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए रिकॉर्डिंग की.
[ilink url=”http://tehelkahindi.com/continued-part-of-begum-akhtar/” style=”tick”]जारी…[/ilink]