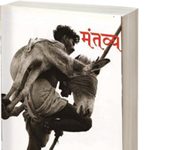उत्तर प्रदेश व बिहार में सालों से प्रचलित और फिल्म दबंग के ‘मुन्नी बदनाम हुई…’ के बाद चर्चा में आए गीत ‘लौंडा बदनाम हुआ, नसीबन तेरे लिए…’ का मूल लेखक कौन है यह किसी को नहीं पता. लेकिन इस क्षेत्र में लगभग सभी यह जरूर जानते हैं कि इसे गा-गाकर लोकमानस में रचाने-बसाने का काम ताराबानो फैजाबादी ने किया है. ताराबानो ने अपनी दिलकश अदाओं के साथ प्रस्तुति देते हुए इसे लोकप्रिय तो बनाया लेकिन अनजाने में ही इससे ‘लौंडों’ को बदनाम होने की रवायत शुरू हो गई.
‘लौंडा’ यानी हल्के-फुल्के अंदाज में समझें तो इसका अर्थ है, लड़का. एक इलाके विशेष के अंदाज में मानें तो वे लड़के जो स्त्रियों की वेशभूषा धारण कर नाचने-गाने का काम करते हैं उन्हें ‘लौंडा’ कहा जाता है और इस विधा को लौंडा नाच. पहली नजर में इस विधा में बदनामी की अपार संभावनाएं दिखती हैं. सो ऐसा हुआ भी. प्रकाश झा ने अपनी चर्चित व राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म ‘दामुल’ में ‘हमरी चढ़ल बा जवनिया गवना ले जा राजा जी…’ गीत के साथ लौंडा नाच का इस्तेमाल किया तो मशहूर फिल्म ‘नदिया के पार’ में ‘जोगीजी धीरे-धीरे, नदी के तीरे-तीरे…’ होली गीत में लौंडा नाच मजेदार अंदाज में सामने आया था. वहीं अनुराग कश्यप को भी ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के लिए भी लौंडा नाच की जरूरत महसूस हुई. इन सबके बाद राजनीति की बात करें तो लालू प्रसाद का लौंडा नाच प्रेम हर बिहारी जानता है. आरंभ से ही लालू अपने राजनीतिक आयोजनों में लौंडा नाच करवाते रहे हैं. पिछले साल उनकी परिवर्तन रैली के बाद भी पटना की सड़कों पर लौंडा नाच का जलवा बिखरा था. यानी लौंडा नाच का उपयोग सबने अपनी-अपनी सहूलियत से किया लेकिन गांव-गिरांव, लोकगायन, सिनेमा में धूम मचाने के बाद लौंडा नाच की विधा और उसके कलाकार गति-दुर्गति को प्राप्त करते रहे और चला-चली की बेला में आ गए.
तो आखिर क्या है इस विशिष्ट कला विधा से जुड़े कलाकारों की पीड़ा? वे लोक कलाकार से नचनिया के रास्ते लौंडा कब से कहलाने लगे और लौंडा कहलाए तो उन्हें बदनामी का पर्याय क्यों बनाया गया. फिर जब बदनाम हुए तो एक पीढ़ीगत परंपरा गति से दुर्गति को प्राप्त क्यों करने लगी? सबसे पहले हम ये सवाल हसन इमाम के सामने रखते हैं. हसन इमाम रंगकर्मी हैं और लोक-कलाओं के गहरे अध्येता भी. दलित लोक कला में प्रतिरोध उनकी चर्चित किताब रही है और हालिया दिनों में उन्होंने एक शोध ‘बिहार के लोक कलाकार-प्रजातांत्रिक अधिकारों के सांस्कृतिक प्रवक्ता’ शीर्षक से किया है. वे कहते हैं, ‘नाम होने, बदनाम होने की बात तो बाद की है लेकिन प्लीज, आप लोक कलाकारों व नर्तकों को लौंडा शब्द से संबोधित न करें. यह नाम ही सामंतमिजाजी समाज की देन है. किसी भी किस्म का नाच प्रतिरोध का प्रतीक है. चूंकि दलित-दमित जाति के लोक कलाकारों ने ही इस नाच को परवान चढ़ाया है. इस नाच को सामाजिक स्वीकृति न मिले और यह गौरव का विषय न बने तो सामंतों ने उपहास उड़ाने के लिए इसे लौंडा नाच कहा था. लौंडा नाच जैसी कोई कला फॉर्म नहीं होती और न ही इसकी चर्चा कहीं मिलती है.’ हसन इमाम आगे कुछ बताने के बजाय सवाल पूछते हैं, ‘गांव के नाटकों में लड़के ही लड़की बन अभिनय, नाच, गान सब करते रहे हैं. सबको लौंडा कहते हैं आप? मनोहर श्याम जोशी महिला की भूमिका ही निभाते थे, उन्हें लौंडा कहेंगे? हबीब तनवीर के नाटक में, रतन थियेम के नाटक में लड़के ही लड़की बनकर आते रहे हैं. उन्हें लौंडा कहते हैं? और आप बिरजू महाराज या कथक के दूसरे मशहूर कलाकारों को लौंडा कहेंगे? वे भी तो नाचते ही हैं, स्त्री जैसा बनकर?’ हसन कहते हैं, ‘आप गौर कीजिए कि कब से लौंडा शब्द चलन में आया और कब से वे बदनामी के पर्याय बने. बिहार के मशहूर लोक कलाकार भिखारी ठाकुर दलितों, दमितों, उपेक्षितों के बीच बड़े कलाकार माने जाते थे, सम्मान पाते थे और सामंतों-संभ्रांतों के बीच लौंडा कहे जाते थे.’ ऐसे ही सवालों के साथ हम वरिष्ठ नाटककार हृषिकेश सुलभ से भी बातचीत करते हैं. सुलभ कहते हैं, ‘पुरुषों द्वारा नर्तकी बनकर नाचने की परंपरा कोई आज की नहीं है. दक्षिण के मंदिरों में इसकी समृद्ध परंपरा रही है और पुरी के मंदिर में तो ‘गोटीपुआ’ नामक एक नाच परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जिसमें कम उम्र के बच्चे नाचते हैं. हरम में लौंडों के रखने का वर्णन भी मिलता है.’
लोककलाओं के अध्येता बताते हैं कि इस परंपरा में बिगड़ाव सामंतवादी युग में आया क्योंकि सामंतवाद अपनी विकृत मानसिकता को लोक कलाओं पर थोपता रहा है. स्त्री के लिए वर्जनाओं के दौर में पुरुष कलाकार ही नचनिया बनकर नाचते थे लेकिन सामंतों ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया. नाच दल निम्नवर्गीय लोग चलाते थे. दो-चार माह की व्यस्तता के बाद उनके पास काम नहीं होता था. ऐसे में सामंतों ने ‘लौंडों’ को अपने यहां काम पर रखना शुरू किया. काम भी लेतेे, नचवाते भी थे और यौन उत्पीड़न भी करतेे. बिहार में कई सामंत हुए हैं जिन्होंने ‘लौंडों’ को अपने यहां रखा और उनकी कारगुजारियों से ‘लौंडा’ बनने वाले लड़के बदनाम होते गए. सुलभ याद करते हैं कि एक लौंडे को उन्होंने अपने साथियों की मदद से आरा के एक प्रोफेसर साहब के यहां से निकलवाया था. प्रोफेसर उसका यौन उत्पीड़न करते थे. बकौल सुलभ, ‘लौंडा नाच को विकृत कर उसे खत्म करने में सामंत मिजाजियों की भूमिका सबसे ज्यादा रही है. अब तो यह विधा चलाचली की बेला में ही आ चुकी है. क्योंकि उनकी जगह बांग्लादेश, नेपाल की लड़कियां गांव में भी नाच करने जाने लगी हैं.’
सुलभ की यह बात बिल्कुल सही है. अब यह नाच विधा हाशिये पर सिसकियां ले रही है लेकिन एक जमाना था जब इसकी धूम थी और हर इलाके में मशहूर पुरुष नचनिए हुआ करते थे. वे बजाप्ता एक दल चलाते थे. उनके दल का नाम दूर-दूर तक होता था. इस परंपरा और विधा के परवान चढ़ने के पीछे एक वजह और दिखती है. इसे समझने के लिए थोड़ा गहराई से परिस्थितियों पर गौर करना होगा. नाच मनोरंजन की एक महत्वपूर्ण विधा सदियों से, पीढ़ियों से रही है लेकिन उसका दायरा हमेशा अलग किस्म का रहा. जब नामचीन तवायफों का दौर था और उनकी धूम देश भर में थी तो वे राजा-महाराजाओं के महलों तक सीमित रहती थीं. जिस राजा-महाराजा के पास सामर्थ्य होता था वह उन्हें अपने यहां बुलाता था. नचवाता-गवाता था. तवायफों के बाद बाईजी युग का अवतरण हुआ तो उन पर जमींदारों और धनाढ्यों का कब्जा हुआ. ये पैसे और रसूखदार लोग थे. शादी-ब्याह, खास आयोजन में बाईजी को अपने यहां बुलाने लगे और नचवाने-गवाने लगे, उन पर पैसे उड़ाने लगे और उनकी कलाई पकड़ने लगे, सार्वजनिक तौर पर उनके हाथ-गाल को छूने लगे. नाच मनोरंजन की एक महत्वपूर्ण विधा होने के बावजूद एक दायरे में जकड़ी रही. एक बड़ा वर्ग, हाशिए और वंचितों का समूह इसके आसपास फटक भी नहीं सका. वह इससे वंचित रहा तो खुद ही इसके विकल्प में, प्रतिरोध में एक शैली विकसित की. पुरुष ही स्त्री की तरह बनने लगा. वंचितों के यहां नाचने लगा. राह चलते भी नाचने लगा. जो लोग इस महत्वपूर्ण मनोरंजन विधा से सदियों से वंचित थे वे जनाना बने पुरुष को ही देखकर सीटियां बजाने लगे. उसका हाथ पकड़ने लगे. यहां उस पर भी पैसा उड़ाया जाने लगा. देखते ही देखते इस नाच विधा ने लोकप्रियता के पैमाने में बाईजी आदि को काफी पीछे छोड़ दिया. वंचित समुदाय ने खुद लौंडा बनकर सिर्फ मनोरंजन की एक महत्वपूर्ण विधा नाच का सामान्यीकरण कर इस पर सदियों से वर्चस्व जमाए बैठे सामंतों, जमींदारों और राजे-रजवाड़ों को चुनौती ही नहीं दी बल्कि इस परंपरा में नायक भी खड़े करने लगे.
[box]
तमाशे से आगे…
अरसे बाद एक बार फिर ‘लौंडा’ अपनी बदनामी के साथ रंगकर्म के जरिए जलवा बिखेरने की अकुलाहट में है. जलवा बिखेरने भी लगा है. कभी मनोरंजन के लिए सबसे सुलभ और लोकप्रिय रहे ‘लौंडों’ को बदनामी के पर्याय से निकालकर, गांव की गलियों में गुम हो जाने के बाद शहरी संभ्रांतों के बीच उन्हें लाने के लिए कई सूत्रधार उभर रहे हैं. बिहार के नालंदा जिले के दोसुत गांव में जन्मे कुमार उदय सिंह लौंडा नाच को नए फॉर्मेट में लेकर दुनिया के दूसरे मुल्कों तक पहुंच चुके हैं तो ‘झूलन लौंडे का डीएनए’ नाम से बने नाटक में बिहार के कलाकार लौंडों की असल जिंदगी के श्याम व शुक्ल पक्ष को सामने ला रहे हैं. लौंडा नाच और लौंडों की जिंदगी पर चल रहे नए प्रयोग में ही एक अहम सूत्रधार बनकर उभरे हैं बिहार के सुपौल के रहने वाले रंगकर्मी पंकज पवन (बाएं) . पंकज पवन इन दिनों अपने नाटक शो ‘लौंडा बदनाम हुआ…’ के जरिए चर्चा में हैं और आमजन, बौद्धिकों से लेकर संभ्रांतों के बीच जोरदार दस्तक दे रहे हैं. लेकिन पंकज लौंडे को उस तरह बदनाम नहीं करवा रहे जैसा पहले से होता रहा था. वे लौंडा बनकर नाचने वाले समूह की पीड़ा लेकर सामने आ रहे हैं. खुद स्त्री वेश धारण कर लौंडा बनकर मंच पर आ रहे हैं, पुरुषों के नजरिए का आकलन कर रहे हैं. लोगों को यह बता रहे हैं कि जनाब आप एक लड़के के लड़की जैसा बन जाने पर फब्तियां कसने और छेड़ने को इतने आतुर हो जा रहे हैं तो सच में किसी लड़की या महिला को देखने के बाद आप जरूर कुंठित होते होंगे और एक क्रूर-घृणित इतिहास रचने को बेचैन भी हो जाते होंगे.
बात पिछले साल की है. पंकज पवन ने ‘लौंडा बदनाम हुआ’ का शो इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया था. देखने वाले टिकट लेकर पहुंचे. अधिकतर संभ्रांत थे. ‘लहरिया लूट ए राजा, मुंहवा पर डाली के चदरिया, लहरिया लूट ए राजा…’ गीत से नाटक की शुरुआत हुई थी. शो के आखिरी में किसी ने पंकज पवन से कहा, ‘आप हिल रहे थे तो मजा आ रहा था.’ पंकज की त्वरित प्रतिक्रिया थी, ‘मैं लड़का हूं, आप जानते हैं, फिर भी मेरे हिलने-हिलाने पर इतने डूब गए. बाकी नाटक में कुछ नहीं दिखा.’ पटना में भी इसी शो को लेकर आए थे पंकज. तब एक बुजुर्ग अपनी पोती के साथ नाटक देखने पहुंचे. वहां भी ‘लहरिया लूट ए राजा…’ से ही नाटक की शुरुआत हुई थी… वह बुजुर्ग नाटक का बहिष्कार करते हुए अपनी पोती के साथ सभागार से निकल गए लेकिन नाटक के बाद पंकज से मिलकर बोले, ‘मुझे नहीं पता था कि आरंभ में कुछ देर तक के लटके-झटके के बाद लौंडा बनकर इतनी गंभीरता से समाज को आइना दिखाएंगे और क्रूर सच्चाइयों को सामने लाएंगे.’ पंकज लौंडों की पीड़ा को सामने लाकर लोगों का दिल जीत रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है. वे कहते हैं, ‘मेरे सामने ‘लौंडा बदनाम हुआ’ नाटक को लेकर कई तरह की चुनौतियां थीं. मैंने आज तक, अब तक आमने-सामने से लौंडा नाच कभी नहीं देखा. जो देखा वह यू-ट्यूब और कुछ सिनेमा में देखा.’ पंकज नाटक के लिए बेगुसराय के अपने एक मित्र को प्रेरणास्त्रोत बताते हुए कहते हैं, ‘मेरा वह मित्र स्त्रैण स्वभाव का था. पुरुष होते हुए भी स्त्री की तरह रहना चाहता था लेकिन सभ्य समाज में यह संभव नहीं था. वह अपनी आकांक्षा के साथ एक दिन सदा-सदा के लिए अपना गांव छोड़कर चला गया.’ यहीं से पंकज के मन में बिहार की लोकप्रिय शैली लौंडा नाच का ख्याल आया. उन्होंने झटपट इसकी स्क्रिप्ट लिख ली. फिर इसके लिए अभिनेता की तलाश शुरू की. लेकिन यह खोज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई. पंकज बताते हैं, ‘मैंने जितने कलाकारों से यह नाटक करने को कहा सभी मुकर गए. लगभग सभी का कहना था कि वे लौंडा बनकर अपने कैरियर को दांव पर नहीं लगाएंगे.’ आखिरकार पंकज ने खुद मंच पर उतरने का फैसला किया और तब से वे ‘लौंडा बदनाम हुआ’ का शो कर रहे हैं.
पंकज पवन के पास जिद है, जुनून है. संभव है वे ‘लौंडा बदनाम हुआ…’ को आगे भी करते रहें. लेकिन असल में जिन लोककलाकारों को लौंडा की परिधि में लाया गया, उनके सामने सिर्फ बदनाम होने, पुरुष होकर स्त्री की तरह रंग-रूप धरकर नाचने में आनेवाली मुश्किलों से उपजी पीड़ा भर नहीं है. वे पीड़ा के अथाह समंदर में गोता लगाते-लगाते इस लोकप्रिय और समृद्ध परंपरा से ही तौबा करते जा रहे हैं.
[/box]

इस नाच परंपरा से इतर एक सवाल यह भी हो सकता है कि ‘लौंडा’ शब्द कब से चलन में आया? यह भले ही मालूम न हो लेकिन यह तो साफ दिखता है कि जो जिंदगी भर स्त्री वेष धारण कर एक कला विधा को स्थापित करने, जनता के संघर्ष को आवाज देने, लोगों का मनोरंजन करने में अपनी ऊर्जा लगाते रहे और आखिरी में उनके हिस्से फकत गुमनामी नसीब हुई. हृषिकेश सुलभ बिहार के गोपालगंज जिला के रहनेवाले रसूल का किस्सा बताते हैं. वह कहते हैं, रसूल नाचते तो थे ही लेकिन वे देश की आजादी की लड़ाई में भी अपनी भूमिका नाच के जरिए निभा रहे थे. गांधी के मरने पर रसूल ने एक गीत रचा, उस पर नाचे, प्रतिरोध किया. गीत के बोल थे, ‘के मारल हो, हमरा गांधी के तीन गो गोली , धकाधक…!’ सुलभ कहते हैं, कौन जानता है रसूल को. क्या उन्हें महज लौंडा कहकर उपेक्षित या खारिज किया जा सकता है? सुलभ रसूल की बात करते हैं. भोजपुरी लोककलाओं के अध्येता बीएन तिवारी उर्फ भाईजी भोजपुरिया चाईं ओझा के बारे में बताते हैं. भाईजी भोजपुरिया कहते हैं, ‘चाईं ओझा लोक मानस में गहरे रचे-बसे लोक कलाकार रहे हैं. वे ब्राह्मण जाति से थे. 12 साल की उम्र में ही नाच से मोह हुआ. नाच के प्रति दीवानगी बढ़ी तो इलाके के दलितों को लेकर नाच करने लगे. उनके नाच दल का नाम दूर-दूर तक हुआ. वे राज्य में और राज्य के बाहर मशहूर होते रहे लेकिन उन्हें अपने समाज, गांव से बहिष्कृत कर दिया गया. उन्हें बदनामी का ऐसा पर्याय माना गया कि आज भी उनका नाम उस इलाके के ब्राह्मण समाज के लोग खुलकर नहीं लेना चाहते.’ चाईं ओझा के बारे में यह ख्यात है कि वे स्त्री वेष धारण कर नाचने में इतने उस्ताद थे कि अनजान लोग बिना बताए यह नहीं जान सकते थे कि यह कोई पुरुष नाच रहा है. लेकिन आज चाईं ओझा और उनके नाम पर सम्मान का भाव कहीं नहीं दिखता. यहां तक कि उनकी पहचान को सदा-सदा के लिए दफन कर दिए जाने का अभियान आज भी एक वर्ग चला रहा है.
यदि हम लोक मानस के इतिहास में कैद रसूल, चाईं ओझा को छोड़ वर्तमान की ही बात करें तो रामअंगेया राम को भला कितने लोग जानते होंगे. रामअंगेया भिखारी ठाकुर के साथ नाचा करते थे, अभिनय करते थे. अब उनकी उम्र 105 साल की हो गई है. अब भी एक दल चलाते हैं. आरा के पास गांव में रहते हैं. भिखारी ठाकुर का नाटक करते हैं. खुद मुख्य अभिनेता बनकर उतरते हैं मंच पर. उनका मन नाचने को हमेशा बेताब रहता है. चट मरद, फट मेहरारू बनकर मंच पर उतरने में उस्ताद हैं वे. रामअंगेया भारत में इतनी उम्र में सिर्फ जिंदा ही नहीं सक्रिय कलाकारों में संभवतः अपने तरीके के इकलौते कलाकार होंगे लेकिन उनको देश और राज्य क्या उनका अपना इलाका ही ठीक से नहीं जानता. भाईजी भोजपुरिया रामअंगेया के बारे में बात करते हुए अपनी एक ही टिप्पणी में इस विधा और इन कलाकारों के हाशिये पर जाने की वजह स्पष्ट करते हैं, ‘ जो संभ्रांत और सामंतमिजाजी हैं, वे आज भी वही कहते हैं- कौन रामअंगेया, अच्छा लौंडा रामअंगेया…! इस जमाने में लौंडा का ठप्पा लगे होने की वजह से जब रामअंगेया जैसा महान अभिनेता, नर्तक और कलाकार उपेक्षित है तो दूसरों की क्या स्थिति होगी, समझ सकते हैं और यह भी महसूस सकते हैं कि लौंडों को बदनाम कौन करता रहा है…! ‘