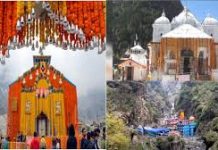सरकारों का रुख
अरुंधती राय नर्मदा बांध पर अपने चर्चित लेख ‘द ग्रेटर कॉमन गुड’ की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू द्वारा हीराकुंड बांध के शिलान्यास के मौके पर दिए गए भाषण की उन लाइनों से करती हैं जिसमें उन्होंने कहा था, ‘अगर आपको कष्ट उठाना पड़ता है तो आपको देशहित में ऐसा करना चाहिए.’ बड़ी परियोजनाओं के संदर्भ में इसी ‘व्यापक जनहित’ की छाप अब भी सरकारों की सोच पर हावी है. अब तो एक कदम आगे बढ़कर सरकारें नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलनों पर यह आरोप लगाती हैं कि ये विकास के रास्ते में रोड़े अटका रही हैं. इसकी ताजा मिसाल इस साल गर्मियों में ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर बढ़ाए जाने के विरोध में जल सत्याग्रह कर रहे किसानों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिया वह बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘यह आंदोलन विकास और जनविरोधी है, इससे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान हो रहा है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है.’ नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पिछले तीस सालों में इसी सोच को चुनौती दी है. रहमत कहते हैं, ‘सरकारों का रवैया सिर्फ नर्मदा बचाओ आंदोलन के मामले में ही निरंकुश नहीं हुआ है बल्कि पिछले कुछ सालों से हमारे लोकतंत्र के सामने चुनौतियां गंभीर हुई हैं. भूमि अधिग्रहण का ही मसला ले लें, जिस तरह से किसानों के हितों के खिलाफ और व्यापक विरोध के बावजूद सरकार इसे किसी भी कीमत पर पास करना चाहती था, वह चिंता का विषय था. इस मामले में सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए ये अलग बात है. एक तरफ तो सरकारें ‘इनवेस्टर मीट’ का आयोजन करके उद्योगपतियों को मुफ्त जमीन और सारी सुविधाएं देने की घोषणा कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बांध प्रभावित और जल सत्याग्रह कर रहे लोगों की बात तक कोई सुनने को तैयार नहीं है.’
शंकर तड़वले कहते हैं, ‘मामला एकतरफा हो गया है. अब तो सरकारें जन आंदोलनों की बात भी सुनने को राजी नहीं हैं और आंदोलन करने वालों को एक तरह से विकास विरोधी, शत्रु और यहां तक कि नक्सली के तौर पर देखने लगी है.’ इसकी वजह बताते हुए वे कहते हैं, ‘देश में एक वर्ग है जो संगठित होकर संसाधनों को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता है, ताकि अपने फायदे के लिए वे इनका दोहन कर सकें.’
शरदचंद्र बेहार का मानना है कि सरकार और प्रशासन में यह सोच हावी है कि पूरे देश के विकास के लिए कुछ लोगों का बलिदान करना पड़े तो यह जायज है. राजनेताओं में जन आंदोलनों को लेकर एक सोच यह भी रहती है कि इस तरह के आंदोलनों की कोई वैधता नहीं होती है, जनता के असली प्रतिनिधि तो हम हैं. अपने अनुभवों को साझा करते हुए वह बताते हैं, ‘जब मैं प्रशासन में था तो कुछ राजनेताओं द्वारा मुझसे कहा जाता था कि जनता क्या चाहती है इसके बारे में ठीक तरह से सामाजिक आंदोलन के लोग जानेंगे या हम?’
राजनीति बनाम गैर-राजनीति की बहस
जन आंदोलनों के राजनीतिक या गैर-राजनीतिक होने के सवाल पर बहस पुरानी है. इसे लेकर कई तरह की राय रही है. कुछ लोगों का मानना है कि वे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनका राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं है, वहीं एक खेमा यह मानता है कि भले ही वे चुनावी राजनीति में शामिल न हों लेकिन उनके मुद्दे राजनीतिक हैं. एक तीसरा पक्ष भी है जो चुनावी राजनीति में शामिल होने की वकालत करता है. आम आदमी पार्टी के परिदृश्य पर उभरने के बाद यह सवाल फिर सामने आया था. नर्मदा बचाओ आंदोलन सहित देश के कई आंदोलनों से जुड़े लोग ‘आप’ में शामिल हुए और चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी. आंदोलन से जुड़े रहे आलोक अग्रवाल इस समय ‘आप’ की मध्य प्रदेश इकाई में संयोजक की भूमिका में हैं.
रहमत कहते हैं, ‘राजनीति व चुनावी राजनीति को लेकर हमारे समाज में हमेशा से ही भ्रम रहा है. शुरू में मुख्यधारा की राजनीति से जुड़े लोग यह आरोप लगाते थे कि हम आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं. उन्हें सफाई देनी पड़ती थी कि हम उन लोगों की तरह पार्टीगत राजनीति नहीं करते हैं, इससे भ्रम फैला. 1995-96 से सामाजिक आंदोलनों में यह चर्चा होनी शुरू हुई कि अगर हमें अपने मुद्दों को सही अंजाम तक पहुंचाना है तो चुनावी राजनीति में शामिल होना पड़ेगा लेकिन साथ में इस पर भी चर्चा होती थी कि चुनावी राजनीति के अपने नियम हैं, जहां मुद्दों की जगह जाति, समुदाय, पैसा और माफिया हावी हैं. इस दिशा में ये सब व्यवहारिक रुकावटें हैं. बाद में अन्ना आंदोलन और ‘आप’ के गठन को देखकर लगा था कि साफ-सुथरे तरीके से चुनावी राजनीति में सफल हुआ जा सकता है, इसीलिए पिछले लोकसभा चुनाव में आंदोलन से जुड़े लोगों ने चुनाव लड़ा था.’
शरदचंद्र बेहार कहते हैं, ‘राज्य समाज का एक हिस्सा है और राजनीति उसका एक पहलू मात्र है. हालांकि समकालीन बातचीत और विमर्श में राजनीति को समाज से अलग करके देखा जाता है. ‘सामाजिक’ शब्द का इस्तेमाल कर एक तरह से यह भ्रम पैदा किया जाता है मानो जन आंदोलन जिन मुद्दों को उठाते हैं वे गैर-राजनीतिक हों, दूसरी तरफ आंदोलन के लोगों के ‘आप’ से जुड़ने के बाद सरकारों को लगा अगर वे आंदोलन की मांगों को मान लेंगे तो इसका फायदा ‘आप’ को मिल सकता है. इसलिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि चुनावी राजनीति से जुड़ने के बाद आंदोलन की नैतिक ताकत कमजोर हो गई है. हमें यह समझना होगा कि एनबीए. सामाजिक आंदोलन नहीं बल्कि नॉन-इलेक्ट्रोरल (गैर निर्वाचित) राजनीति है. इस फर्क को समझना जरूरी है.’ अब्दुल जब्बार कहते हैं, ‘जन आंदोलनों के चुनावी राजनीति में अपना प्रतिनिधि खड़ा करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन हमारी आदत मैगी खाने की हो गई है जबकि ऐसे आंदोलनों के लिए तैयारी और धैर्य की जरूरत है.’
आप से जुड़ाव और उसके बाद
13 जनवरी 2014 को मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थीं. इसे इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है. उस समय उन्होंने कहा था कि उनके लिए चुनावी राजनीति में आने का फैसला काफी मुश्किल भरा था. पिछले लोकसभा चुनाव में मेधा पाटकर और आंदोलन के दूसरे प्रमुख नेता आलोक अग्रवाल ने चुनाव भी लड़ा था. हालांकि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव प्रकरण के बाद मेधा पाटकर ने यह कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि पार्टी तमाशा बनकर रह गई है. उस समय अरविंद केजरीवाल को भेजे गए अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा था, ‘वैकल्पिक राजनीति की अपेक्षाओं की तुलना में प्राप्त हुई थोड़ी उपलब्धियां हमारे कुछ सीमित उद्देश्यों को ही पूरा करने वाली हैं.’
इन सबके बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ‘आप’ से जुड़ने का फैसला सही था या गलत? जवाब इस घटना में ढूंढा जा सकता है. इस साल अप्रैल और मई में मध्य प्रदेश के घोघलगांव में जल सत्याग्रह को लेकर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया बदली हुई नजर आई, जबकि 2012 में इसी घोघलगांव के जल सत्याग्रह के बाद राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई थी. तब जलस्तर कम करने और जमीन के बदले जमीन देने जैसी मांगों को मान लिया गया था. वहीं इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन को विकास विरोधी बताया. भाजपा अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने भी इसे कुछ लोगों की नौटंकी करार दिया था. वहीं केंद्र सरकार ऐसा जता रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो. आंदोलन से जुड़े रहे कई लोग इसे चुनावी राजनीति से जुड़ जाने के बाद आंदोलन की नैतिक ताकत का कम होना मानते हैं. वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता योगेश दीवान कहते हैं, ‘आप’ में कार्यकर्ताओं के शामिल होने से आंदोलन को धक्का लगा क्योंकि वहां लोग वैकल्पिक राजनीति के नाम पर चले तो गए थे लेकिन असलियत में वहां कोई वैकल्पिक ढांचा था ही नहीं और न ही ऐसा माहौल था कि इस बारे में बात भी की जा सके.’
डूब प्रभावित गांव भीलखेड़ा (बड़वानी) से नर्मदा बचाओ आंदोलन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कैलाश अवास्या खरगोन-बड़वानी सीट से ‘आप’ के टिकट पर पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं. वे कहते हैं, ‘हम लोग ‘आप’ से इसी मंशा के साथ जुड़े थे कि साफ-सुथरी राजनीति होगी और इससे बदलाव आ सकता है, लेकिन बाद में वहां जाकर अनुभव हुआ कि हमें अभी जन आंदोलन और दबाव समूह के रूप में ही काम करना चाहिए.’ वे बताते हैं, ‘उन्होंने अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन अभी जो कुछ वहां चल रहा है उससे वे असहमत हैं.’ देवराम कनेरा कहते हैं, ‘हम ‘आप’ के साथ काफी मंथन के बाद जुड़े थे, लेकिन पार्टी से जो उम्मीद थी वह सही साबित नहीं हुई. नर्मदा घाटी में आंदोलन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा.’ उनका कहना है, ‘अगर हम राजनीति के साथ जुड़कर आंदोलन करेंगे तो हमारी बात पहले की तरह नहीं सुनी जाएगी और इसे वोट की राजनीति के नजरिये से देखा जाएगा.’ महादेव भगवान दास का कहना है, ‘आप’ से जुड़ने का कोई नुकसान हुआ हो ऐसा डूब क्षेत्र में तो नहीं दिखाई देता है, अब भी सब संगठन के साथ जुड़े हैं.’
आंदोलन का भविष्य
बीते 28 जुलाई को दिल्ली के कॉन्सटीट्यूशन क्लब में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें आंदोलन के तीस साल पूरे होने पर इसके संघर्ष, चुनौतियों और भविष्य पर चर्चा की गई. सम्मेलन में तय किया गया कि बांध में पानी का स्तर कम करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा पूरी नर्मदा घाटी में पदयात्रा की जाएगी. 6 अगस्त को खालघाट (धार) से यह पदयात्रा शुरू होकर 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के बड़वानी स्थित राजघाट पहुंची. आंदोलन से जुड़े लोगों ने यहां अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया है. इस बीच एक छह सदस्यीय स्वतंत्र टीम द्वारा परियोजना से प्रभावित गांवों के मई में किए गए दौरे की रिपोर्ट भी आ गई है. ‘डिस्ट्रॉयिंग अ सिविलाइजेशन’ नाम की इस रिपोर्ट के अनुसार अब भी हजारों परिवार सही मुआवजा और पुनर्वास से वंचित हैं, कई प्रभावितों को तो डूब क्षेत्र में शामिल ही नहीं किया गया है और अगर भविष्य में बांध की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाई जाती है तो इससे और ज्यादा परिवार डूब क्षेत्र में आ जाएंगे.
तीस साल के लंबे संघर्ष के बाद हम देखें तो ‘कोई नहीं हटेगा बांध नहीं बनेगा’ के नारे के साथ आंदोलन शुरू हुआ था लेकिन तमाम संघर्ष और कुर्बानियों के बीच बांध के निर्माण को रोका नहीं जा सका और इस बीच लड़ाई की मांगों का दायरा भी धीरे-धीरे कम होता गया. बड़े बांध के खिलाफ शुरू हुआ यह संघर्ष बाद में बांधों की ऊंचाई के खिलाफ, फिर बेहतर पुनर्वास के लिए और अब पुनर्वास में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सिमटता जा रहा है. इन सब को लेकर शरदचंद्र बेहार कहते हैं, ‘या तो हम गलत मांग कर रहे हैं या फिर सरकार जनता के लिए है ही नहीं. ऐसे में अब आंदोलनों के सामने बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि कैसे सरकारों को जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए.’ वे दार्शनिक प्लेटो को कोट करते हुए कहते हैं, ‘लोकतंत्र के नाम पर जब तक थोड़े लोगों का राज होगा तब तक असली लोकतंत्र नहीं आ पाएगा. इसलिए सारे आंदोलनों को मिलकर अपनी पहचान और मुद्दों को कायम रखते हुए सच्चे लोकतांत्रिकरण के लिए संघर्ष शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की सरकारें जब तक चलती रहेंगी तब तक नर्मदा बचाओ आंदोलन और इस तरह के दूसरे संघर्षों की बातें अनसुनी की जाती रहेंगी और उनके पास अपने संघर्ष की मांगों को सीमित करने का विकल्प ही बचेगा.’
तीस साल आंदोलन की पगडंडी पर चलते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़े बांधों और उससे जुड़े विकास के मॉडल पर सवाल और बहस खड़ा करने में कामयाब रहा है. इसने विस्थापितों के सवाल को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया और अंत में इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि किस तरह से तमाम रुकावटों के बीच नर्मदा घाटी के लोग हिम्मत और प्रतिबद्धता के साथ अहिंसात्मक तरीके से न केवल संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का काम भी किया है.
आंदोलन के महत्वपूर्ण पड़ाव
1985 : महाराष्ट्र में ‘नर्मदा धारणग्रस्थ समिति’, मध्य प्रदेश में ‘नर्मदा घाटी नव निर्माण समिति’ और गुजरात में ‘नर्मदा असरग्रस्त संघर्ष समिति’ की ओर से सरदार सरोवर बांध परियोजना का विरोध शुरू हुआ. इन तीनों संगठनों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया. इस तरह से ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ का गठन हुआ.
28 अगस्त 1989 : मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति बनी जिसमें यह कहा गया कि विस्थापितों को कम से कम 5 एकड़ संचित और उपजाऊ जमीन और पुनर्वास स्थल पर आवश्यक संसाधनों सहित आवास के लिए जमीन प्रदान की जाएगी.
28 सितंबर 1989 : हरसूद में आयोजित संकल्प मेले में पूरे देश से लगभग 50,000 लोगों ने एकजुट होकर इस बांध का विरोध किया.
09 अगस्त 1991 : सुप्रीम कोर्ट ने बीडी शर्मा बनाम भारत सरकार मामले में आदेश दिया कि सरकार द्वारा छह महीने के अंदर विस्थापित लोगों का अनिवार्य रूप से पुनर्वास किया जाए.
18 जून 1992 : विश्व बैंक के एक स्वतंत्र समीक्षा संस्था ‘मॉरिस कमेटी’ की रिपोर्ट जारी. रिपोर्ट में बैंक को सरदार सरोवर परियोजना से अलग होने की अनुशंसा की गई.
26 जून 1992 : 16 देशों की 42 संस्थाओं द्वारा समर्थित नर्मदा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पैनल ने अपनी रिपार्ट जारी की.
20 जुलाई 1994 : पांच सदस्यों वाली एक स्वतंत्र समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी. इसी साल कानूनी विवादों के चलते बांध बनाने का काम रोक दिया गया.
1999 : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बांध का काम फिर से शुरू हुआ.
07 जनवरी 2002 : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्वास और पुनर्सुधार के लिए पीड़ितों को नकद राशि देने की योजना की शुरुआत हुई.
14 अप्रैल 2003 : सुप्रीम कोर्ट ने बांध की ऊंचाई 95 मीटर से 100 मीटर बढ़ाने का आदेश दिया.
16 जून 2005 : मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष पुनर्वास अनुदान में बदलाव कर उसे विशेष पुनर्वास पैकेज में बदल दिया, जिसमें रकम के बदले जमीन देने की बात की गई. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुनर्वास और विस्थापन की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थीं.
2006 : बांध के काम को और बढ़ाने के लिए आवेदन दिया गया, जिस पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने भूख हड़ताल की पर काम जारी रहा. साथ ही पुनर्वास और विस्थापन परियोजना असफल हो गई.
23 फरवरी 2009 : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जस्टिस झा कमीशन को निर्देश दिया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना पुनर्वास और पुनर्सुधार में हो रहे घपले की जांच करे.
24 जून 2010 : सरदार सरोवर बांध की समीक्षा करने वाले जस्टिस शाह आयोग की रिपोर्ट भोपाल में जारी. इसमें पूर्ण पुनर्वास और पर्यावरण सुरक्षा की सिफारिश की गई.
12 दिसंबर 2014 : नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील.
(स्रोत : नर्मदा: 30 ईयर्स ऑफ रेजिलेंस)
[box]
जीवनशाला : संघर्ष और निर्माण साथ-साथ
नर्मदा बचाओ आंदोलन और इससे जुड़े लोगों ने परियोजना के विरोध के साथ कई रचनात्मक काम भी किए हैं, जिसमें बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की स्थिति में सुधार जैसे काम शामिल हैं. आंदोलन द्वारा संचालित ‘नर्मदा नवनिर्माण अभियान’ ट्रस्ट दूरदराज के डूब क्षेत्रों में जीवनशाला चलाता है. आंदोलन के दौरान पता चला कि इन इलाकों में स्कूल नहीं हैं और अगर हैं भी तो ठीक से चलते नहीं. आंदोलन से जुड़ीं परवीन जहांगीर बताती हैं, ‘शुरू में सरकार पर इन इलाकों में स्कूल खोलने के लिए दबाव बनाया गया. लगातार आवेदन दिए गए लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही. तब आंदोलनकारियों और समुदाय ने खुद पहल करते हुए जीवनशाला स्कूल खोला. 1991 में पहली जीवनशाला शुरू हुई जो कि महाराष्ट्र के चिमलखेड़ी और नीमगांव में थी. यहां वर्तमान में नौ जीवनशालाएं चल रही हैं, जिसमें 7 महाराष्ट्र और 2 मध्य प्रदेश में हैं. यहां कुल 910 बच्चे पढ़ते हैं. महाराष्ट्र की जीवनशालाओं में 780 और मध्य प्रदेश में 130 बच्चे हैं. वर्तमान में कुल 40 शिक्षक हैं. इसके अलावा हर जीवनशाला में एक मौसी (खाना बनाने के लिए) और एक कमाथी (सहायक) होते हैं. ये शालाएं आवासीय होती हैं. यहां 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है. मध्य प्रदेश की जीवनशालाओं में पहली से 5वीं तक शिक्षा दी जाती है, वहीं महाराष्ट्र में पहले यह चौथी तक था, अब उसे 5वीं कक्षा तक किया गया है. 2012-13 से महाराष्ट्र की जीवनशालाओं को राज्य सरकार से मान्यता भी मिल गई है.’ परवीन बताती हैं, ‘सभी जीवनशालाओं को सर्व शिक्षा अभियान के तहत किताबों के अलावा कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है और इसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है.’
जीवनशालाएं महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम की सोच पर आधारित हैं, जिसमें जीवन कौशल और पढ़ाई साथ-साथ होती है. यहां सामुदायिक जीवन निर्वाह, आत्मनिर्भरता, सहयोग, आदिवासी संस्कृति, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है. पढ़ाई की शुरुआत मातृभाषा में होती है फिर दूसरी भाषाएं सिखाई जाती हैं. किताबों का अनुवाद भी स्थानीय बोलियों में किया गया है. इन किताबों में अन्य बातों के अलावा स्थानीय समाज-संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी गई है. परवीन बताती हैं, ‘यहां से दो लड़के एथलीट भी बने हैं जिन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर कई पदक जीते हैं. इसी तरह से महाराष्ट्र में खेलों को बढ़ावा देने वाली क्रिया प्रबोधनी परीक्षा में जीवनशाला के बच्चे भी बैठे थे. नंदूरबार जिले से इस परीक्षा में केवल दो बच्चों का चयन हुआ, ये दोनों ही बच्चे जीवनशाला से हैं.’
जीवनशालाएं लोगों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत चंदे और समुदाय के सहयोग से चलती हैं. समुदाय जो भी उगाता है, उसमें से थोड़ा हिस्सा बच्चों को देता है. समुदाय को जीवनशाला से जोड़ा भी गया है. समुदाय से लोगों को देख-रेख कमेटी में चुना जाता है जो कि निगरानी का काम करते हैं. जीवनशालाओं के अलावा महाराष्ट्र के धड़गांव में एक छात्रवास भी चलाया जा रहा है, जहां वर्तमान में 23 बच्चे रहकर 5वीं के बाद दूसरे स्कूलों में आगे की पढ़ाई कर रहे हैं. परवीन जहांगीर बताती हैं, ‘जीवनशाला से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दूरदराज के आदिवासी बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिले.’
[/box]
[ilink url=”http://tehelkahindi.com/medha-patkars-take-on-narmada-bachao-andolan/” style=”tick”]मेधा पाटकर का साक्षात्कार [/ilink]