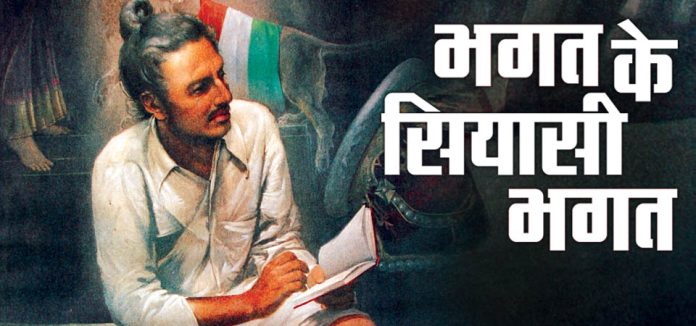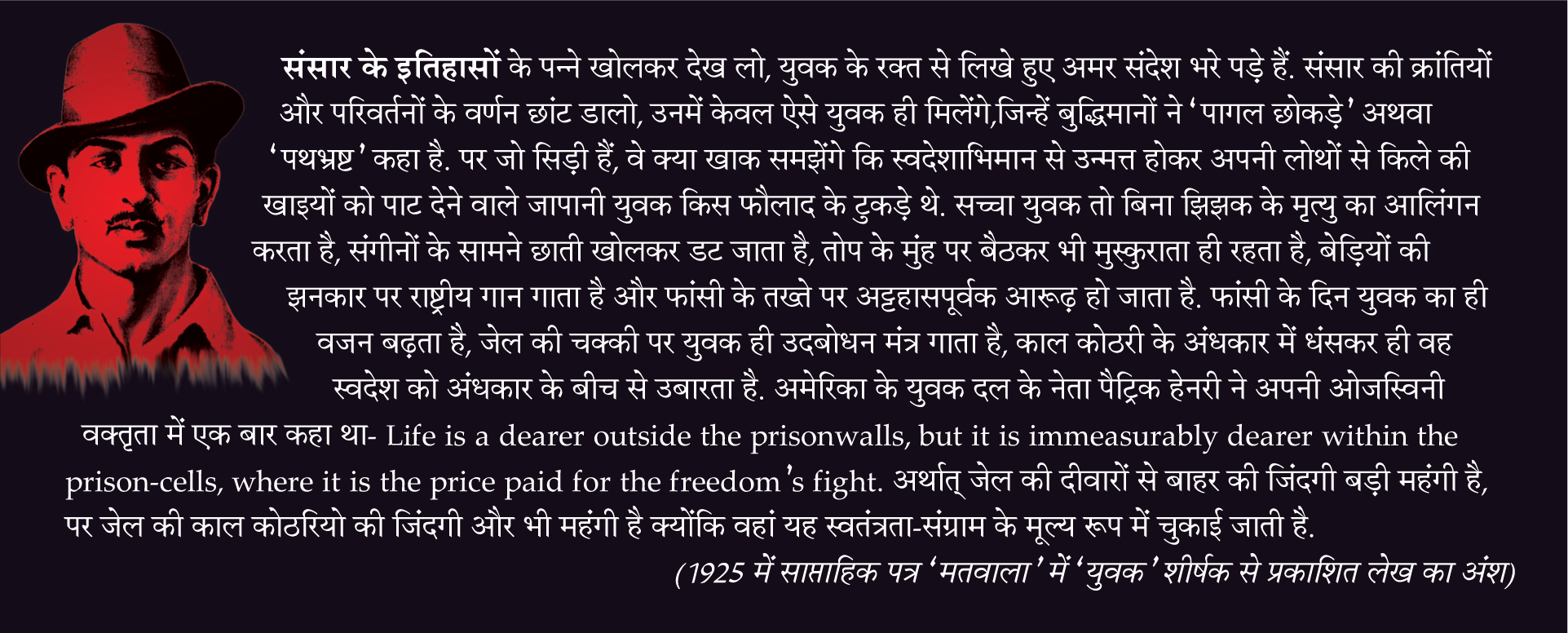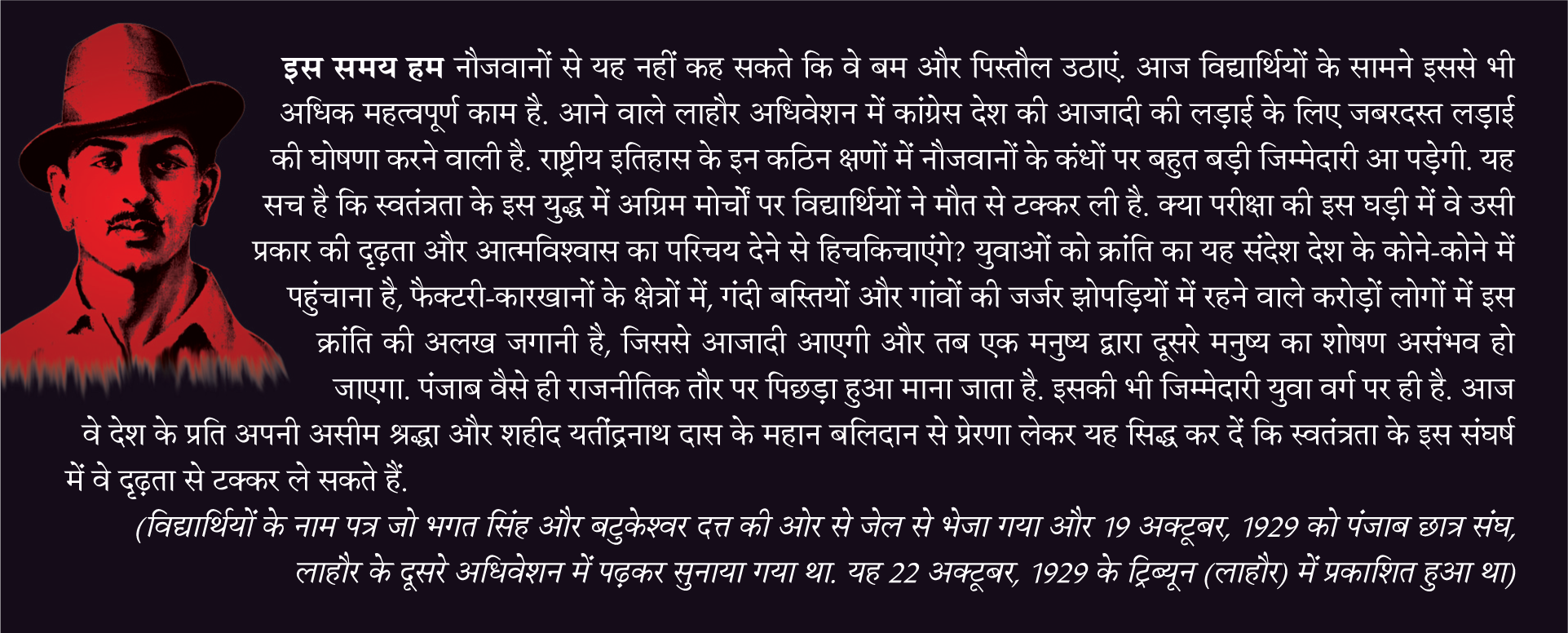‘मां, मुझे कोई शंका नहीं है कि मेरा मुल्क एक दिन आजाद हो जाएगा, पर मुझे डर है कि गोरे साहब जिन कुर्सियों को छोड़कर जाएंगे, उन पर भूरे साहबों का कब्जा हो जाएगा.’ आजादी के तमाम नायकों में से एक शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह ने अपनी मां को लिखी चिट्ठी में यह बात कही थी. उन्हीं भगत सिंह ने शहीद होने से पहले अपनी जेल डायरी में लिखा था, ‘सरकार जेलों और राजमहलों, या कंगाली और शान-शौकत के बीच किसी समझौते के रूप में नहीं होती. यह इसलिए गठित नहीं की जाती कि जरूरतमंद से उसकी दमड़ी भी लूट ली जाए और खस्ताहालों की दुर्दशा और बढ़ा दी जाए.’ उसी डायरी में वे एक जगह लिखते हैं, ‘शासक के लिए यही उचित है कि उसके शासन में कोई भी आदमी ठंड और भूख से पीड़ित न रहे. आदमी के पास जब जीने के मामूली साधन भी नहीं रहते, तो वह अपने नैतिक स्तर को बनाए नहीं रख सकता.’ किसी के भूखे न रहने का सपना देखने वाला यह शहीद देश के शासक वर्ग के लिए सबसे लोकलुभावन हीरो है, जबकि इस देश के सरकारी आंकड़ों में इस वक्त करीब 30 करोड़ लोग भूखे सोते हैं. सवाल उठता है कि भगत सिंह तो सबके हैं लेकिन उनके विचार किसके हैं.
‘जब तक कोई निचला वर्ग है, मैं उसमें ही हूं. जब तक कोई अपराधी तत्व है, मैं उसमें ही हूं. जब तक कोई जेल में कैद है, मैं आजाद नहीं हूं.’ भगत सिंह की जेल डायरी में दर्ज ऐसी तमाम पंक्तियां उनके क्रांतिकारी सपनों का आईना हैं, जिन पर वक्त के साथ उपेक्षाओं की धूल भरी मोटी चादर बिछा दी गई है. भगत सिंह के नाम का नारा लगाने वाले ज्यादातर राजनीतिज्ञ इन सपनों के बारे में शायद ही कोई बात करते हों. अगर भगत सिंह हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं तो भूख से मर रहे लोगों, कर्ज से आत्महत्या करते किसानों और जेलों में सड़ रही लाखों जिंदगियों में क्या भगत सिंह जीवित नहीं हैं, जैसा कि उक्त पंक्तियों में दर्ज है? फिर हमारी सियासत इस बात पर क्यों उलझ गई कि कन्हैया कुमार नामक युवक में भगत सिंह है कि नहीं? भगत सिंह के दस्तावेज गवाह हैं कि उनका सपना मजदूर, किसान, वंचित, दलित और हर उस व्यक्ति के लिए लड़ना रहा जो पीड़ित है. क्या देश की कुर्सी पर ‘भूरे साहबों के कब्जे’ को लेकर भगत सिंह का डर सच साबित हुआ? अगर यह सच न होता तो भगत सिंह की राजनीतिक विरासत और उनके सपनों के हिंदुस्तान पर बहस होती, न कि इस बात पर कि भगत सिंह ‘भारत माता की जय’ बोलकर फांसी पर चढ़ने वाले ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ थे, या भगवा रंग की पगड़ी पहनने वाले सरदार? क्या भगत सिंह का सम्मान करने का अर्थ यह नहीं है कि उनके लिखे को स्वीकारते हुए उन्हें नास्तिकता, तर्कवाद और वैज्ञानिकता का झंडा बुलंद करने वाला क्रांतिकारी माना जाए और जब तक एक भी व्यक्ति शोषित है, तब तक व्यवस्था बदलने का सतत प्रयास होता रहे?
शहीद भगत सिंह इस देश की राजनीति के लिए अचानक महत्वपूर्ण हो उठे हैं. हर राजनीतिक दल उन्हें अपना साबित करने के लिए बेकरार है. सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक सियासतदानों को उनकी याद आ गई. इतिहास के पन्ने जिन लोगों को वैचारिक या राजनीतिक तौर पर भगत सिंह के खिलाफ खड़ा करते हैं, वे लोग अब उनकी विरासत के सबसे बड़े झंडाबरदार बनकर खड़े हैं. जिन लोगों ने उनके समय में उनसे दूरी बनाकर रखी, सबसे पहला दावा आज उन्हीं का है. वैचारिक निकटता या अंगीकार के चलते कोई भगत सिंह को अपना कहे तो भी गनीमत है, लेकिन भगत सिंह के सपनों की हत्या करने वाले लोग भी अगर भगत सिंह को अपना कहें तो यह भगत सिंह समेत पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का अपमान है जो आजादी के साथ समता, बंधुता और मानव मुक्ति के उद्देश्यों के साथ लड़ा गया.
[symple_box color=”red” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

अमृतसर में 11-12-13 अप्रैल को राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई और साथ ही युवकों की भी कॉन्फ्रेंस हुई. दो-तीन सवालों पर इसमें बड़ा झगड़ा और बहस हुई. उनमें से एक सवाल धर्म का भी था. प्रांतीय कॉन्फ्रेंस की विषय समिति में भी मौलाना जफर अली साहब के पांच-सात बार खुदा-खुदा करने पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस मंच पर आकर खुदा-खुदा न कहें. आप धर्म के मिशनरी हैं तो मैं धर्महीनता का प्रचारक हूं.
यदि किसी का धर्म बाहर लोगों की सुख-शांति में कोई विघ्न डालता हो तो किसी को भी उसके विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत हो सकती है? लेकिन सवाल तो यह है कि अब तक का अनुभव क्या बताता है? पिछले आंदोलन में भी धर्म का यही सवाल उठा और सभी को पूरी आजादी दे दी गई. यहां तक कि कांग्रेस के मंच से भी आयतें और मंत्र पढ़े जाने लगे. उन दिनों धर्म में पीछे रहने वाला कोई भी आदमी अच्छा नहीं समझा जाता था. फलस्वरूप संकीर्णता बढ़ने लगी. जो दुष्परिणाम हुआ, वह किससे छिपा है? अब राष्ट्रवादी या स्वतंत्रता प्रेमी लोग धर्म की असलियत समझ गए हैं और वही उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझते हैं.
बात यह है कि क्या धर्म घर में रखते हुए भी, लोगों के दिलों में भेदभाव नहीं बढ़ता? क्या उसका देश के पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक पहुंचने में कोई असर नहीं पड़ता? इस समय पूर्ण स्वतंत्रता के उपासक सज्जन धर्म को दिमागी गुलामी का नाम देते हैं. वे यह भी कहते हैं कि बच्चे से यह कहना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य कुछ भी नहीं, मिट्टी का पुतला है, बच्चे को हमेशा के लिए कमजोर बनाना है. उसके दिल की ताकत और उसके आत्मविश्वास की भावना को ही नष्ट कर देना है. लेकिन इस बात पर बहस न भी करें और सीधे अपने सामने रखे दो प्रश्नों पर ही विचार करें तो हमें नजर आता है कि धर्म हमारे रास्ते में एक रोड़ा है. मसलन हम चाहते हैं कि सभी लोग एक-से हों. उनमें पूंजीपतियों के ऊंच-नीच की छूत-अछूत का कोई विभाजन न रहे. लेकिन सनातन धर्म इस भेदभाव के पक्ष में है. बीसवीं सदी में भी पंडित, मौलवी जी जैसे लोग भंगी के लड़के के हार पहनाने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं और अछूतों को जनेऊ तक देने की इनकारी है. यदि इस धर्म के विरुद्ध कुछ न कहने की कसम ले लें तो चुप कर घर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो धर्म का विरोध करना होगा.
(1928 में ‘किरती’ में छपे भगत सिंह के लेख ‘धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम’ से)[/symple_box]
आजादी के नायकों में से दो विभूतियों को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है एक गांधी और दूसरे भगत सिंह. गांधी के साथ वामपंथ और दक्षिणपंथ की घोर असहमतियां रही हैं, जो अब भी बरकरार हैं, लेकिन भगत सिंह की सभी खुले स्वर में प्रशंसा करते हैं और सभी उन्हें अपना साबित करने की कोशिश करते हैं. वामपंथी भगत सिंह को वामपंथी कहकर उनके सपनों के भारत की बात करते हैं, जबकि संघ परिवार उन्हें कट्टर राष्ट्रवादी और देश के लिए प्राणों की बलि देने वाला देशभक्त बताकर उनका महिमामंडन करता है. लेकिन भगत सिंह को लेकर मची इस छीना-झपटी में असली भगत सिंह कहां हैं? देश को लेकर उनके क्या विचार थे? वे कैसा भारत चाहते थे? वे कैसी राजनीति चाहते थे? आज के राजनीतिक दलों और उनके विचारों का भगत सिंह से कितना साम्य है? आज भगत सिंह होते तो मौजूदा राजनीति में किस तरह से हस्तक्षेप करते? इन सारे सवालों का जवाब उन लेखों और दस्तावेजों में मिल सकता है जो उन्होंने खुद लिखे हैं या जो उनसे संबंधित हैं.
राजनीतिक दलों के बीच भगत सिंह को अपनाने की इस कदर होड़ क्यों मची है, इसके जवाब में पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और इतिहासकार राजीव लोचन कहते हैं, ‘जीते-जी जिस भगत सिंह की राजनीतिक दलों ने अवहेलना की, उसे अब सब अपना कहने पर आमादा हैं. भगत सिंह जब अंग्रेज सरकार के हाथ लगे तो अखबारों ने रिपोर्ट में लिखा कि ‘समाजवादी क्रांतिकारी’ गिरफ्तार हुआ है. पर भारत के वामपंथी आम तौर पर भगत सिंह के मसले पर चुप रहना पसंद करते रहे. आखिर भगत सिंह वामपंथी पार्टी के सदस्य जो नहीं थे. वामपंथियों की तुलना में, कम से कम आज, भारत में कांग्रेस और भाजपा में होड़ लगी है कि किसी तरह भगत सिंह को अपना लें. जिहाद के जाल में फंसे पाकिस्तान में भी कुछ लोग भगत सिंह की याद को ताजा करने में लगे हैं. आखिर भगत सिंह की कर्म भूमि भी तो वह जमीन थी जो आज पाकिस्तान है.’
इन्हीं सवालों को लेकर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष गाताडे कहते हैं, ‘अपने सीमित राजनीतिक जीवन में भगत सिंह ने जो भविष्यवाणी की थी, आज खुलकर उसे सामने देख रहे हैं. आजादी के बाद कुछ चीजों को लेकर भले ही भ्रम रहा हो, लेकिन अब चाहे सांप्रदायिकता के मसले को देखें, जाति के मसले को देखें या काले अंग्रेज-भूरे अंग्रेज की उनकी जो समझदारी थी, मेरे ख्याल से वो खुलकर सामने आ रहा है. एक तो उनकी भविष्यवाणी सामने आ रही है. इसके अलावा मुझे लगता है कि जो भी संकट दिख रहा है, एक तरफ तो सांप्रदायिक ताकतें हैं, दूसरी तरफ विकल्प के तौर पर जो शक्तियां हैं वे भी संकट में हैं. वामपंथी पार्टियां और आंदोलन खुद संकट में है. ऐसे समय में समाज अपने नायकों को याद करता है. बढ़े हुए संकट के दौर में भगत सिंह लोगों को अपने करीब लगने लगे हैं.’
भगत सिंह को लेकर महत्वपूर्ण शोधकार्य करने वाले प्रो. चमन लाल कहते हैं, ‘कट्टरपंथी राष्ट्रवाद के अभियान का यह चरम है कि भगत सिंह के बारे में ज्ञात तथ्यों को भी झुठलाया जा रहा है. शशि थरूर ने कन्हैया कुमार की तुलना भगत सिंह से की तो प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह झूठ बोलकर भगत सिंह के प्रति शिष्टाचार की सारी हदें पार कर दीं कि ‘भगत सिंह भारत माता की जय बोलकर फांसी पर चढ़े थे.’ सारी दुनिया अब तक यही जानती है कि 23 मार्च, 1931 को फांसी के दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ‘इंकलाब जिंदाबाद’ और ‘साम्राज्यवाद का नाश हो’ के नारे लगाए थे. उन्होंने ‘सरफरोशी की तमन्ना’ गाना भी गाया था और चेहरे पर काला कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया था. अब फर्जी राष्ट्रवादी, जिनकी पार्टी और पूर्वजों का राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता संघर्ष में कोई भूमिका नहीं रही है, इतिहास को गोएबल्स की स्टाइल में उलट-पलट रहे हैं, जैसा कि हिटलर के समय किया गया था.’
इतिहासकार राजीव लोचन कहते हैं, ‘कई सालों तक गांधी जी भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों को गौण और असंगत बताते रहे. स्वतंत्रता के बाद के काल में देश अपनी ही समस्याओं में कुछ इस तरह उलझ गया कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को भूल ही गया. बस वे ही याद रहे जिनकी याद सरकार को रही. स्वतंत्रता के उत्साह में देश तेजी से प्रगति भी कर रहा था. ऐसे माहौल में भगत सिंह की याद कम ही लोगों को आई. पर इसके बाद के समय में भी राजनीतिक दलों ने भगत सिंह को अपने से दूर ही रखा. सरकार द्वारा कभी-कभी भगत सिंह के नाम की दुहाई जरूर दी जाती रही पर उनके विचारों को समझने या लोगों तक पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की गई. भगत सिंह को याद करना महज 26 जनवरी और 15 अगस्त को फिल्म ‘शहीद’ के गाने सुनने तक ही रह गया. जैसे-जैसे निजी रेडियो और टीवी स्टेशनों का जाल देश पर फैला, यह थोड़ी-सी याद भी खत्म कर दी गई. इसके बाद 1997 में भगत सिंह की याद आई कम्युनिस्टों को , देश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर. कम्युनिस्टों को लगा कि देश की आजादी में उनके योगदान को नकारा जा रहा है.’
वे आगे कहते हैं, ‘इतिहासकार प्रोफेसर बिपन चंद्र 1990 के शुरुआती दशक में भगत सिंह को क्रांतिकारी के रूप में लोगों के सामने ले आए. इसके बाद कम्युनिस्टों ने भगत सिंह को अपना बताते हुए इक्के-दुक्के बयान दिए, भगत सिंह केे कुछ पर्चों के नए संस्करण छापे गए. फिर शांति छा गई. दस साल बाद, नई शताब्दी में दक्षिणपंथियों ने भगत सिंह पर अपना हक जताया. किसी ने उनको पगड़ी पहना दी. हालांकि अभी तक भगत सिंह की सबसे ज्यादा दिखने वाली तस्वीर में वे टोपी पहने दिखाए जाते रहे थे. किसी ने उन पर गेरुआ वस्त्र डाल दिए, तो किसी ने उन्हें भारत की सभ्यता का संरक्षक बना डाला.’
[symple_box color=”red” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
 भारत वर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है. एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं. अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है. यदि इस बात का अभी यकीन न हो तो लाहौर के ताजा दंगे ही देख लें. किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों, हिंदुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है. यह मार-काट इसलिए नहीं की गई कि फलां आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फलां आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है. जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है.
भारत वर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है. एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं. अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है. यदि इस बात का अभी यकीन न हो तो लाहौर के ताजा दंगे ही देख लें. किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों, हिंदुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है. यह मार-काट इसलिए नहीं की गई कि फलां आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फलां आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है. जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है.
ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है. इन ‘धर्मों’ ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है. और अभी पता नहीं कि इस तरह के धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे. इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है. और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं. इतना रक्तपात होने पर इन ‘धर्मजनों’ पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने आ जाता है.
यहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है. इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली. वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था और जो ‘समान राष्ट्रीयता’ और ‘स्वराज्य-स्वराज्य’ के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छिपाए चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं. जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे बहुत ही कम हैं. और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे.
दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, अखबार वाले हैं. पत्रकारिता का व्यवसाय, किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था. आज बहुत ही गंदा हो गया है. यह लोग एक-दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे-मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटौव्वल करवाते हैं. एक-दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं. ऐसे लेखक बहुत कम हैं जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो.
अखबारों का असली कर्त्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल-मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई-झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है.
(जून, 1928 में ‘किरती’ में छपे भगत सिंह के लेख ‘सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज’ का अंश)
[/symple_box]
भगत सिंह समेत दूसरे क्रांतिकारियों पर महत्वपूर्ण किताबें लिखने वाले सुधीर विद्यार्थी कहते हैं, ‘शहीद भगत सिंह पर दावेदारी कोई नई बात नहीं है. यह काफी समय से जारी है. खास तौर से जब भगत सिंह की जन्म शताब्दी आई. इस वर्ष उनके सिर पर पगड़ी पहनाने का प्रयास हुआ. ये सब इसलिए ताकि भगत सिंह को जाति और धर्म के खांचे में धकेल दिया जाए ताकि उनका जो पैनापन है, जो विचार उनके पास हैं, पूरे क्रांतिकारी आंदोलन में उनकी जो छवि उभरती है उसे खत्म किया जा सके.’ भगत सिंह की प्रतीकात्मक पहचान और विचारधारा से छेड़छाड़ पर चिंता जताते हुए विद्यार्थी कहते हैं, ‘जिस व्यक्ति ने खुद कहा हो कि अभी तो मैंने केवल बाल कटवाए हैं, मैं धर्मनिरपेक्ष होने और दिखने के लिए अपने शरीर से सिखी का एक-एक नक्श मिटा देना चाहता हूं, आप उसके सिर पर फिर पगड़ी रख रहे हैं. आप यही तो बताना चाह रहे हैं कि भगत सिंह इसलिए बहादुर थे कि सिख थे. तब कहना पड़ेगा कि राम प्रसाद बिस्मिल इसलिए बहादुर थे कि ब्राह्मण थे, रोशन सिंह इसलिए बहादुर थे कि ठाकुर थे, अशफाक उल्ला इसलिए बहादुर थे कि पठान थे. आप कितना भी प्रयास कर लें भगत सिंह के सिर पर पगड़ी रखने का, लेकिन 23 साल का वह युवा क्रांतिकारी इतना बड़ा हो गया है कि उस पर कोई पगड़ी अब फिट नहीं हो सकती.’
भगत सिंह को लेकर आजकल ज्यादा शोर इसलिए सुनाई दे रहा है कि भगत सिंह को अपनाने की होड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल हो गया है. संघ पर यह भी आरोप लगता है कि उसके प्रयासों से भगत सिंह को पगड़ी पहनाकर उन्हें धार्मिक दिखाने की कोशिश की गई. सुभाष गाताडे कहते हैं, ‘आरएसएस इस मामले में दिलचस्प है. जिस गांधी की हत्या में उनका या उनकी विचारधारा का हाथ था, जब उन पर दावा कर सकती है, तो और क्या कहा जाए. आंबेडकर जिनके विचारों से उनकी ताउम्र दुश्मनी रही, आंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, आरएसएस उनको भी क्लेम करता है. आरएसएस को इसमें सलाहियत हासिल है. बस एक ही व्यक्ति बचते हैैं वो हैं नेहरू, क्योंकि उनकी जगह वह सरदार पटेल को अपनाता है. दूसरा, क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर आम जनमानस में जो एक छवि है कि वे पिस्तौल और बम वाले लोग थे, बड़े बहादुर थे, उसके साथ जोड़कर खुद को पेश करते हैं. वे भगत सिंह की टोपी वाली इमेज नहीं दिखाते हैं, उनको सरदार टाइप दिखाते हैं. पगड़ी पहनाकर. आरएसएस और भाजपा आंबेडकर व भगत सिंह को चुनिंदा ढंग से अपनाते हैं. इसमें प्रगतिशील लोगों की कमजोरी है कि आरएसएस नायकों को अपनाने की कोशिश कर पा रहा है.’
इतिहासकार राजीव लोचन कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहते हैं, ‘जब भगत सिंह सक्रिय थे, उस समय राजनीतिक दल उनसे बिल्कुल परे हट कर रहते थे. भगत सिंह का जो सीधा संवाद होता था, वो गांधी के साथ होता था. बाकी हमारे जितने नेतागण थे, भगत सिंह की जब मौत हुई तो फट से पल्ला झाड़ा और उसके बाद उन्हें कभी याद नहीं किया. 1980 के बाद भगत सिंह की याद सबको आनी शुरू हुई, जब नेताओं की एनिवर्सरीज आनी शुरू हुईं. अगर आपको याद हो तो 80 और 90 के दशक में रेडियो और टीवी पर जो गाने भगत सिंह को लेकर हुआ करते थे, वे गाने बजने बंद हो गए. उस वक्त कुछ टीवी वालों ने चर्चा में मुझसे कहा था कि अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता, इसलिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. एनिवर्सरीज नजदीक आईं तो लोगों को भगत सिंह की याद आई. एक तो याद आई हमारे कम्युनिस्ट साथियों को जो कि उस वक्त भगत सिंह का पूरी तरह विरोध करते थे. अभी तो कहने भी लगे हैं कि भगत सिंह हमारे हैं, लेकिन उस वक्त सख्त खिलाफ थे. ये बेचारे इसलिए भी याद करने लगे क्योंकि 60 साल से जूते पड़ रहे थे कि तुम तो गद्दार हो, 1942 में अंग्रेजों का साथ दिया. तो उनको अचानक समझ में आया कि भगत सिंह को इस्तेमाल करके हम भी अपने को राष्ट्रवादी साबित कर सकते हैं. कम्युनिस्ट इस्तेमाल करने लगे तो जो बाकी लोग थे वे भी भगत सिंह पर टूट पड़े और भगत सिंह को सर आंखों पर उठाया. इस पूरे माहौल में बीजेपी एक पार्टी थी जो कि पीछे रही क्योंकि बीजेपी का भगत सिंह के साथ कोई भी संबंध नहीं है. अब बीजेपी ने उनको याद करना शुरू किया और बीजेपी ने जिस तरह याद किया वो हमें दिख ही रहा है.’
भगत सिंह पर असली दावेदारी किसकी है, इस सवाल पर प्रो. चमन लाल कहते हैं, ‘भगत सिंह भारत के कामगार, मजदूर, किसान, दलित और निचले वर्ग के साथ थे. 1929 से 1931 के दौरान जब भगत सिंह के केस का ट्रायल चल रहा था, उस वक्त सभी अखबार वामपंथी और ‘समाजवादी क्रांतिकारी’ लिख रहे थे. 24 जनवरी, 1930 को वे कोर्ट में ‘लाल स्कार्फ’ पहनकर पहुंचे थे और जज से अंतरराष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए सोवियत यूनियन को शुभकामना भेजने का अनुरोध किया था.’
वे आगे कहते हैं, ‘एक वक्त पर भगत सिंह, चंद्रशेखर और उनके साथियों ने ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाया था, लेकिन सितंबर, 1928 में अपने संगठन के नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के बाद ‘इंकलाब जिंदाबाद’ व ‘साम्राज्यवाद का नाश हो’ के नारे को अपनाया. 2 फरवरी, 1931 को लिखे उनके ‘युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पत्र’ में स्पष्ट रूप से ‘समाजवादी सिद्धांत’ को भारतीय स्वतंत्रता का रास्ता बताया है. कोई भी व्यक्ति जिसने ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़े हैं, वह भगत सिंह के मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित ‘समाजवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी’ होने से इनकार नहीं कर सकता.’
बिपन चंद्र लिखते हैं, ‘वे मार्क्सवादी हो चले थे और इस बात में विश्वास करने लगे थे कि व्यापक जनांदोलन से ही क्रांति लाई जा सकती है. दूसरे शब्दों में जनता ही जनता के लिए क्रांति कर सकती है. अदालत में और अदालत के बाहर भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने जो बयान दिए, उनका सार यह है कि क्रांति का अर्थ है क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में समाज के शोषित, दलित व गरीब तबकों के जनांदोलन का विकास. भगत सिंह एक जागरूक, धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी होने के नाते राष्ट्र और राष्ट्रीय आंदोलन के सम्मुख मौजूद सांप्रदायिकता के खतरे को पहचानते थे. अपने साथियों, श्रोताओं से वे बराबर कहा करते थे कि सांप्रदायिकता उतनी ही खतरनाक है जितना उपनिवेशवाद. नौजवान भारत सभा के छह नियम, जिन्हें भगत सिंह ने तैयार करवाए थे, में से दो इस तरह थे- ‘ऐसी किसी भी संस्था, संगठन या पार्टी से किसी तरह का संपर्क न रखना जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो’ और ‘धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानते हुए जनता के बीच एक-दूसरे के प्रति सहनशीलता की भावना पैदा करना और इस पर दृढ़ता से काम करना.’
लेखक अशोक कुमार पांडेय कहते हैं, ‘भगत सिंह ने ‘वंदे मातरम’ या ‘भारत माता की जय’ की जगह ‘इंकलाब जिंदाबाद’ और ‘साम्राज्यवाद मुर्दाबाद’ का नारा दिया. जाहिर है वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं थे कि यह एक विदेशी हुकूमत थी. वे साम्राज्यवाद के खिलाफ थे और इसके विकल्प के रूप में समाजवाद के समर्थक. भगत सिंह निश्चित तौर पर भारत की आधिकारिक कम्युनिस्ट पार्टियों का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अपने विचारों में वे वैज्ञानिक समाजवाद के बेहद करीब थे. आजाद हिंदुस्तान को लेकर उनके स्वप्न एक शोषण विहीन और समानता आधारित समाज के थे जिसमें सत्ता का संचालन कामगार वर्ग के हाथ में हो. वह लड़ाई उपनिवेशवाद की मुक्ति तक तो पहुंची लेकिन उसके आगे जाकर वंचित जनों के हाथ में सत्ता देकर एक समतावादी समाज की स्थापना अब भी एक स्वप्न ही है.’
भगत सिंह और उनके साथियों के उद्देश्यों को लेकर इतिहासकार बिपन चंद्र लिखते हैं, ‘भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने पहली बार क्रांतिकारियों के समक्ष एक क्रांतिकारी दर्शन रखा. उन्हें बताया कि क्रांति का लक्ष्य क्या होना चाहिए. 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के घोषणापत्र में कहा गया कि हमारा उद्देश्य उन तमाम व्यवस्थाओं का उन्मूलन करना है, जिनके तहत एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है. क्रांतिकारी लक्ष्य प्राप्त करने में दर्शन या विचारधारा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने लाहौर कोर्ट के सामने कहा था, ‘क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है.’
भगत सिंह आज कितने प्रासंगिक हैं, इस सवाल पर लेखक अशोक कुमार पांडेय कहते हैं, ‘हमने जो आर्थिक व्यवस्था चुनी वह समतावादी होने की जगह लगातार विषमता बढ़ाने वाली साबित हुई और आज आजादी के सात दशकों बाद भी हम अपनी जनता के बड़े हिस्से को जरूरी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा पा रहे. सामाजिक ताना-बाना भी बुरी तरह उलझा और ध्वस्त हुआ है. एक अपेक्षाकृत बराबरी वाला संविधान अपनाने के बावजूद समाज के भीतर जातीय, धार्मिक और इलाकाई भेदभाव लगातार बढ़ता गया है. दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हुई हैं और धर्म का स्पेस राजनीति में घटने की जगह भयावह रूप से विस्तारित होता चला जा रहा है. कश्मीर और उत्तर-पूर्व में जिस तरह उत्पीिड़त राष्ट्रीयताओं का प्रतिरोध और दमन देखा जा रहा है वह देश के रूप में हमारी परिकल्पना को ही प्रश्नांकित कर रहा है. ऐसे में भगत सिंह को याद करना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की क्रांतिकारी तथा जनपक्षधर धारा को याद करना है.’
[ilink url=”https://tehelkahindi.com/opinion-of-bhagat-singh-s-nephew-on-ongoing-debate-on-bhagat-singh/” style=”tick”]जानें भगत सिंह के भतीजे प्रो. जगमोहन सिंह के विचार[/ilink]
सबके अपने-अपने पक्ष हैं और सब पार्टियां और विचारक अपने तरीके से भगत को पेश करते हैं. राजीव लोचन कहते हैं, ‘पार्टियां ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि युवा वर्ग भगत सिंह से बहुत प्रभावित होता है. पंजाब में आप देखेंगे कि भिंडरावाले और भगत सिंह के पोस्टर एक साथ लगे. दोनों एक साथ लोगों का दिल जीतते हैं. युवाओं को लगता है बम और पिस्तौल लेकर सारी समस्या का हल खोज सकते हैं. बाकी लोग तो बेवकूफ की माफिक चर्चाएं कर रहे हैं, सॉल्यूशन तो बंदूक में है. उसे भगत सिंह भी अच्छा लग जाता है, भिंडरावाले भी अच्छा लग जाता है. भाजपा को लग रहा है कि अगर भगत सिंह उसके हो गए तो उसकी बल्ले-बल्ले. लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा. भगत सिंह के सब दस्तावेज मौजूद हैं. उन्हें इंटरनेट पर भी कोई भी देख सकता है. जब आप कहते हैं कि भगत सिंह भारत माता की जय बोलता था, तब लोगों को इसकी हकीकत आसानी से पता चल सकती है. भाजपा के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि वह पहले अपना रवैया बदले, फिर भगत सिंह का नारा लगाए.’
राजीव लोचन आगे कहते हैं, ‘भगत सिंह पूरी तरह वामपंथी थे. उस समय के लोगों का भी मानना था कि वे वामपंथी हैं. असेंबली में बम फेंकने के बाद अगले दिन की खबर में यह नहीं था कि भगत सिंह ने बम फोड़ा, अखबारों ने लिखा था सोशलिस्टों ने बम फोड़ा.’
भगत सिंह के सहयोगी रहे कॉमरेड शिव वर्मा ने ‘शहीद भगत सिंह की चुनी हुईं कृतियां’ शीर्षक से एक किताब संपादित की, जो 1987 में कानपुर से छपी. इसकी भूमिका में वे लिखते हैं, ‘आम जनता यह बात नहीं जानती कि भगत सिंह वास्तव में थे क्या. वह इतना ही जानती है कि वे एक बहादुर इंसान थे जिन्होंने सांडर्स को मारकर लाला जी की हत्या का बदला लिया और सेंट्रल असेंबली में बम फेंका. यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह एक उच्च कोटि के बुद्धिजीवी भी थे. इस कारण से स्वार्थी व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी आंदोलन और खासकर भगत सिंह के वैचारिक पक्ष को विकृत करना आसान हो जाता है.’
भगत सिंह और उनके साथियों को करीब से जानने वाले शिव वर्मा आगे लिखते हैं, ‘एक बुद्धिजीवी के रूप में भगत सिंह हम सबसे बहुत ऊंचे थे. जिस समय जल्लाद ने उनको जीवन के अधिकार से वंचित किया, वे मुश्किल से 23 साल के थे. इतनी कम आयु में उन्होंने बड़े अधिकार के साथ कई विषयों पर लिखा. राजनीति, ईश्वर, धर्म, भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, प्रेम, सौंदर्य, आत्महत्या, फौरी समस्याओं और कई दूसरे विषयों पर उन्होंने विचार व्यक्त किए थे. क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का, उसके वैचारिक संघर्ष और विकास का गहरा अध्ययन-मनन उन्होंने किया था और उससे समुचित निष्कर्ष निकाले थे. इसलिए अगर हमें भगत सिंह को ठीक तरह से समझना है तो हमें उनकी इस पृष्ठभूमि की भी कुछ जानकारी होनी चाहिए.’
यह सच है कि राजनीतिक दावेदारी के शोर में भगत सिंह के सपनों की कोई चर्चा नहीं है. भगत सिंह के लेखों और पत्रों से गुजरते हुए आप पाएंगे कि भगत सिंह गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित के पक्ष में साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और शोषण के विरुद्ध युद्ध की बार-बार घोषणा कर रहे थे. लाहौर षड्यंत्र केस के तीन अभियुक्तों को फांसी हुई तो इन अभियुक्तों ने मांग की कि उन्हें युद्धबंदी माना जाए और फांसी न देकर गोली से उड़ा दिया जाए. उस समय युद्धबंदियों को गोली से उड़ाया जाता था. लाहौर षड्यंत्र केस के साथियों का साथ देते हुए भगत सिंह और उनके दोनों साथियों ने भी अंग्रेज सरकार से यही मांग रखते हुए पत्र लिखा. उस पत्र में लिखा गया, ‘हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शक्तिशाली लोगों ने मेहनत-मजदूरी करने वाले भारतीयों और जनसाधारण के प्राकृतिक साधनों पर अपने स्वार्थसाधन के लिए अधिकार जमा रखा है. इस प्रकार से स्वार्थ साधने वाले चाहे अंग्रेज पूंजीपति हों, चाहे हिंदुस्तानी, उन्होंने आपस में मिलकर लूट जारी कर रखी हो या युद्ध, भारतीय पूंजी के द्वारा ही गरीब का खून चूसा जा रहा हो, इन बातों से अवस्था में कोई अंतर नहीं आता.’
भगत सिंह का नारा लगाकर उन पर दावा ठोंकने वाली सियासत ने इन प्रश्नों पर कब विचार किया है, जो भगत सिंह के लिए मौत के पहले के प्रश्न थे कि ‘मुट्ठी भर शक्तिशाली लोगों ने मेहनत-मजदूरी करने वाले भारतीयों और जनसाधारण के प्राकृतिक साधनों पर अपने स्वार्थसाधन के लिए अधिकार जमा रखा है.’
निचली अदालत में भगत सिंह से पूछा गया था कि क्रांति से उनका क्या मतलब है, इसके जवाब में भगत सिंह ने कहा था, ‘क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयां अनिवार्य नहीं हैं. और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है. वो बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है. क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन… मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं. दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने-दाने के लिए तरस जाते हैं… यह भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की ओर लिए जा रहा है. यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती. स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठकर रंगरेलियां मना रहा है…’ भगत सिंह ने जिन सवालों को ताल ठोंककर अंग्रेज सरकार के सामने उठाया था, वही सवाल अब भारतीय संसद में तीन लाख से अधिक किसानों की आत्महत्या के बाद भी नहीं उठते. क्या भगत सिंह का ‘व्यवस्था पर भूरे साहबों’ द्वारा कब्जा कर लेने से जुड़ा शक सही नहीं हो गया है?
[symple_box color=”red” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
‘सरकार में बैठे लोग हर सूबे से चार भगत सिंह ढूंढें और फांसी चढ़ा दें’
जिस दिन गांधी जी ने यह कहा कि भगवान उनका मार्गदर्शन करता है, संसार को चलाने के लिए वर्णाश्रम एक श्रेष्ठ व्यवस्था है और जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, उसी दिन हम इस निर्णय पर पहुंच गए थे कि गांधीवाद और ब्राह्मणवाद में कोई फर्क नहीं है. हमने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि देश का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक कांग्रेस पार्टी जो इस दर्शन और सिद्धांत पर चलती है, समाप्त न हो जाए. लेकिन अब यह तथ्य कम से कम कुछ लोग मानने लगे हैं, उनके पास ज्ञान और साहस आ गया है कि वे गांधीवाद के पतन के लिए प्रयास कर सकें. यह हमारे उद्देश्य की महान सफलता है. यदि भगत सिंह को फांसी न दी गई होती तो इतने लोकप्रिय ढंग इस विजय के आधार न होते. बल्कि हम तो यह बात कहने का जोखिम उठाते हैं कि यदि भगत सिंह को फांसी न हुई होती तो गांधीवाद को और जमीन मिली होती.
भगत सिंह बीमार पड़कर नहीं मरे, जैसा आम तौर पर लोगों के साथ होता है. उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को वास्तविक समानता और शांति का मार्ग दिखाने के महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया. भगत सिंह एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां सामान्यतया कोई नहीं पहुंच पाया. हमें उनकी शहादत पर हृदय से गर्व है. साथ ही साथ हम सरकार में बैठे लोगों से यह प्रार्थना करते हैं कि वे हर सूबे में चार भगत सिंह जैसे सच्चे आदमी ढूंढें और फांसी पर चढ़ा दें.
(भगत सिंह की फांसी के बाद रामास्वामी पेरियार द्वारा अपने अखबार ‘कुडई आरसु’ में लिखे संपादकीय का अंश)[/symple_box]
भगत सिंह के पास सिर्फ स्वप्न नहीं थे. उनकी निगाह में हिंसा एक ‘विवशता का हथियार’ भर थी. बाकी पूरी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका स्पष्ट दर्शन बार-बार वे पेश करते रहे. लेकिन उन्होंने शहादत इसलिए दी कि उनकी शहादत ‘युवाओं को मदहोश करेगी और वे आजादी और क्रांति के लिए पागल हो उठेंगे.’ वे ‘बम और पिस्तौल का रास्ता’ अपनाकर खून बहाने की जगह युवाओं को सलाह देते हैं कि ‘करोड़ों लोगों को जागरूक करना’ हमारा कर्तव्य है. वे अदालत में स्वीकार करते हैं कि ‘हम मानव जीवन को अकथनीय पवित्रता प्रदान करते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बजाय हम मानव-सेवा में हंसते-हंसते अपने प्राण विसर्जित कर देंगे.’ इंसानियत के बचाव और शोषण के विरुद्ध उनके बलिदान की चर्चाएं करने की जगह सिर्फ उनकी विरासत पर कब्जे की कोशिश क्या भगत सिंह को दोबारा फांसी देने के समान नहीं है?
भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में पृष्ठ 24 पर एक स्पेनी शिक्षक फ्रांसिस्को फेरेर, जिन्हें षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी, की वसीयत लिखी. इसमें कहा गया है, ‘मैं अपने दोस्तों से यह भी कहना चाहूंगा कि वे मेरे बारे में कम से कम चर्चा करेंगे या बिल्कुल ही चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदमी की तारीफ होने लगती है तो उसे इंसान के बजाय देवप्रतिमा-सा बना दिया जाता है और यह मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत बुरी बात है. सिर्फ कर्मों पर ही गौर करना चाहिए, उन्हीं की तारीफ या निंदा होनी चाहिए, चाहे वे किसी के द्वारा किए गए हों. अगर लोगों को इनसे सार्वजनिक हित के लिए प्रेरणा मिलती दिखाई दे तो वे इनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सामान्य हित के लिए हानिकारक लगें तो वे इनकी निंदा भी कर सकते हैं, ताकि फिर इनकी पुनरावृत्ति न हो सके… मरे हुए के लिए खर्च किए जाने वाले समय का बेहतर इस्तेमाल उन लोगों की जीवन दशाओं को सुधारने में किया जा सकता है जिनमें से बहुतेरों को इसकी भारी आवश्यकता है.’ क्या भगत सिंह के नाम पर नारा लगाकर शोर मचाने वाले सत्ताधारी उनकी इस विरासत पर अमल करेंगे?
[symple_box color=”red” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा! उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे! कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा! ये सवाल बीसवीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनते ही शर्म आती है… हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं जबकि पूर्णतया भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इंकलाब की आवाज उठा रहा है. उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी. आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटा कर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है. हम सदा ही आत्मा-परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा? वे वेद-शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं? हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता. अंग्रेजी शासन हमें अंग्रजों के समान नहीं समझता. लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है?
30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा! उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे! कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा! ये सवाल बीसवीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनते ही शर्म आती है… हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं जबकि पूर्णतया भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इंकलाब की आवाज उठा रहा है. उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी. आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटा कर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है. हम सदा ही आत्मा-परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा? वे वेद-शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं? हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता. अंग्रेजी शासन हमें अंग्रजों के समान नहीं समझता. लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है?
जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो? जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए?
जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया-बीता समझोगे तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों-जैसा व्यवहार किया जाएगा. फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्यर्थ होगा.
समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का हक है अथवा नहीं? तथा क्या उन्हें वेद-शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है? बड़े-बड़े समाज-सुधारक तमतमा गए, लेकिन लालाजी ने सबको सहमत कर दिया तथा यह दो बातें स्वीकृत कर हिंदू धर्म की लाज रख ली. वरना जरा सोचो, कितनी शर्म की बात होती. कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है. हमारी रसोई में निःसंग फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है.
(1928 में ‘किरती’ में ‘अछूत का सवाल’ शीर्षक से छपे भगत सिंह के लेख का अंश)[/symple_box]