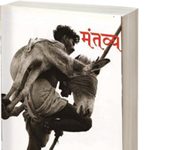पांच राज्यों के चुनावी नतीजों की धूल अब बैठ चुकी है. अब यह देखने का समय है कि इन चुनावों ने हमारे लोकतंत्र के रक्तचाप पर क्या असर डाला है. उत्तर प्रदेश में यह लगातार दूसरी बार है जब वोटरों ने किसी एक दल को साफ बहुमत दिया है. 2007 के पहले बीते बीस सालों में ऐसा नहीं हुआ था. पंजाब में 40 साल में पहली बार है जब किसी दल या गठबंधन को लगातार दूसरी बार विधानसभा में बहुमत मिला हो. उत्तराखंड में किसी को बहुमत नहीं मिला और सिर्फ एक सीट के अंतर से सबसे आगे निकलने वाली कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी.
यूपी-पंजाब को देखते हुए एक बात कही जा रही है कि भारतीय मतदाता अब स्थिर सरकारें चाहता है, इसलिए उसने दलों को स्पष्ट बहुमत दिया है. लेकिन क्या स्पष्ट बहुमत कोई ऐसी चीज है जिससे लोकतंत्र या राजकाज के बेहतर होने की गारंटी मिलती हो? मायावती से पहले आखिरी बार उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की जिस सरकार को बहुमत हासिल हुआ था उसके रहते और उसकी भागीदारी से बाबरी मस्जिद गिरी. गुजरात में दंगों के बावजूद नरेंद्र मोदी को विराट बहुमत मिला और अब तो वे खुद को गुजरात का गौरव बताते हैं. 2004 में अपने सहयोगियों पर कहीं ज्यादा निर्भर यूपीए सरकार कहीं ज्यादा जिम्मेदार नजर आती रही, लेकिन 2009 की मजबूत हैसियत ने उसे आज की तारीख में ज्यादा गैरजिम्मेदार बनाया है.
वोटर को अपने इलाके के दल और नेता चाहिए. राहुल गांधी जनता की निगाह में बाहरी थे जिसके मुकाबले अखिलेश बिल्कुल लोकल थे
मतलब यह कि स्पष्ट बहुमत वह चीज नहीं है जिस पर लोकतंत्र को बहुत खुश होना चाहिए. बेशक, इसकी वजह से विधानसभाओं में दिखने वाली घोड़ा मंडी बंद हो जाती है, कई बार सरकारें बेजा दबाव झेलने से भी बच जाती हैं, लेकिन अक्सर बड़ा बहुमत सत्ताओं को निरंकुश बनाता है और ताकतवर तबकों के बहुसंख्यकवाद को मजबूत करता है. जब कांशीराम कहा करते थे कि उन्हें मजबूत नहीं मजबूर सरकारें चाहिए तो वे दरअसल यही बताया करते थे कि मजबूत सरकारें कमजोर लोगों और तबकों की नहीं सुनतीं. यूपी में मजबूर सरकारों के सहारे ही वह दलित राजनीति परवान चढ़ पाई जिसने इस राज्य को आजादी के बाद पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया. विडंबना बस यही है कि मायावती खुद को मिले स्पष्ट बहुमत को दीर्घावधिक जनादेश में नहीं बदल सकीं. भरोसा करना चाहिए कि अखिलेश यादव मायावती का हश्र याद रखेंगे.
बहरहाल, अब दूसरे मुद्दे पर लौटें. यह सच है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में राहुल गांधी नहीं चले, जबकि उनकी मदद के लिए सोनिया भी आईं और प्रियंका भी. लेकिन सारा दम लगा लेने के बावजूद कांग्रेस 30 सीटों तक भी नहीं पहुंच सकी. नेहरू-गांधी परिवार के विरोधी मानते हैं कि जनता ने राहुल गांधी के नाटक को नकार दिया है. लेकिन क्या यह राहुल गांधी या वंशवाद की हार है? बेशक, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलीं जितनी उसे उम्मीद थी, लेकिन कायदे से राज्य में उसके वोट भी बढ़े हैं और सीटें भी. इसलिए यह नतीजा जल्दबाजी भरा लगता है कि वे यूपी में अंतिम तौर पर खत्म हो गए हैं या खारिज कर दिए गए हैं. आखिर 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को यहीं से 22 सीटें मिली थीं.
दूसरी बात यह कि नेहरू-गांधी परिवारवाद की भले हार हुई हो, उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में परिवारवाद ही जीता है. मुलायम सिंह यादव की जगह अखिलेश यादव ले रहे हैं और प्रकाश सिंह बादल की जीत का सेहरा सुखबीर सिंह बादल के सिर बांधा जा रहा है. जाहिर है, पार्टियों में वह आंतरिक लोकतंत्र नहीं है जिसमें परिवार के बाहर किसी नेता के उदय की गुंजाइश बने.
सवाल है, इन चुनावों का क्या कोई सकारात्मक पहलू है? एक तो यह कि जनता ने इन चुनावों में, जहां-जहां क्षेत्रीय विकल्प दिखे, उन्हें तरजीह दी. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बाद ही बीजेपी-कांग्रेस को जगह मिली है. पंजाब में अकाली-बीजेपी गठजोड़ का जो बहुमत है वह अकालियों के बूते आया है, बीजेपी की सीटें भी घटी हैं और उनके वोट भी. उत्तराखंड में चूंकि ऐसा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए लड़ाई कांग्रेस-बीजेपी के बीच बनी रही. गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दी, लेकिन अपनी राष्ट्रीय छवि से अलग उसने वहां एक उदार चेहरा पेश किया और चर्च का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की. मणिपुर में कांग्रेस के दबदबे को चुनौती देने की स्थिति नहीं थी, लेकिन वहां भी तृणमूल कांग्रेस ने अपनी लक्ष्य की जा सकने लायक मौजूदगी दर्ज करा दीं.
इसका एक मतलब साफ है कि वोटर को अपने इलाके के दल और नेता चाहिए. यूपी में राहुल गांधी के पिटने की एक वजह यह भी रही कि वे जनता की निगाह में बाहरी आदमी थे जिसके मुकाबले अखिलेश बिल्कुल लोकल थे. इस लिहाज से ये चुनाव भारतीय राष्ट्र राज्य के संघीय ढांचे की अवधारणा को कुछ और ताकत देते हैं. दिल्ली की निर्भरता राज्यों पर बढ़ी है- लखनऊ, पटना, भोपाल, या कोलकाता में अब वह अपने फैसले आसानी से थोप नहीं सकती. बेशक, यह स्थिति इन चुनावों से पहले भी थी- आखिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से पहले बीएसपी की ही सरकार थी. फिर भी इन चुनावों से यह प्रक्रिया मजबूत हुई है और कांग्रेस और बीजेपी जैसे दलों पर यह दबाव है कि वे अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं में कुछ स्थानीय हसरतों के लिए भी गुंजाइश बनाएं. दरअसल इन चुनावों में सबसे बुरा हाल बीजेपी का हुआ है. उसकी सीटें भी कम हुई हैं, वोट भी, और जहां उसे कामयाबी मिली है – गोवा में- वहां स्थानीय स्तर पर खुद को बदलने की कोशिश की वजह से ही मिली है.
बहरहाल, यह चुनाव चर्चा कुछ सरलीकरणों का सच समझे बिना पूरी नहीं होगी. एक सरलीकरण तो यह था कि इस बार बहुत बड़ी तादाद में वोटर निकले. जबकि चुनाव शास्त्र के जानकार योगेंद्र यादव बताते हैं कि जो नई मतदाता सूचियां हैं वे पहले से कहीं बेहतर और सटीक हैं जिनमें बरसों से चले आ रहे, या अलग-अलग जगहों पर दुहराए जा रहे नाम हटाए जा चुके हैं. इसलिए वोटरों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन यह बढ़ोतरी उतनी बड़ी नहीं है जितनी प्रतिशत के लिहाज से दिखती है.
दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात चुनाव आयोग की वह भूमिका है जिसकी इन दिनों कुछ ज्यादा तारीफ हो रही है. बेशक, चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से कई गड़बड़ियां रुकी हैं, लेकिन इसके कुछ अवांतर प्रभाव भी रहे. जो चुनाव भारत में लोकतंत्र के त्योहार की तरह हुआ करते थे, वे बहुत तकनीकी किस्म की औपचारिकता में बदलते जा रहे हैं. हमारे यहां चुनावी राजनीति का एक देशज रंग रहा जिसमें आम लोगों को चुनाव होने की जानकारी चुनाव आयोग की अधिसूचनाओं से नहीं, दीवारों पर लिखे लाल नारों से होती थी. पार्टियों के वादों की सूचना उनके घोषणापत्रों से नहीं, नेताओं के भाषणों से मिलती थी और चुनावी हवा की थाह घरों और सड़कों पर लगे झंडों से लगती थी. लेकिन अब घरों पर झंडे नहीं लग सकते, दीवारों पर नारे नहीं लिखे जा सकते और नेता मनचाहे वादे नहीं कर सकते. सतह पर दिख रहा है कि इससे चुनाव साफ-सुथरे हुए हैं, लेकिन सच यह है कि इसकी वजह से जो खर्च खुलकर होता था वह अब छिपकर होने लगा है और उसमें काले पैसे की भूमिका और बढ़ गई है. इन चुनावों में यूपी से पंजाब तक जितने बड़े पैमाने पर रुपये और शराब बंटने की खबर आई, उससे अंदाजा मिलता है कि यह चुनावी साफ-सुथरापन कैसा था. दूसरी बात यह कि सड़क और मैदान पर प्रचार की कमी ने मीडिया पर नेताओं और पार्टियों की निर्भरता बढ़ाई और जानकार बताते हैं कि इन चुनावों में पेड न्यूज का खेल शर्मनाक ढंग से खेला गया.
बेशक, चुनाव आयोग को अपना काम करना चाहिए और नेता कायदे तोड़ें तो उन्हें रोकना भी चाहिए. लेकिन अंततः चुनाव आयोग एक प्रशासनिक संस्था ही है, राजनीतिक प्रक्रियाओं के नियमन और निर्धारण में उसकी भूमिका एक हद से आगे नहीं हो सकती. चुनाव अंततः समाज में और लोगों के बीच लड़े जाने हैं. लोग अपने ढंग से फैसले करते हैं और उन्होंने किया है. यूपी में पूरी तरह सरकार बदल डाली, पंजाब में अकालियों को दुबारा मौका दिया और उत्तराखंड में कांग्रेस को सांत्वना पुरस्कार देकर छोड़ दिया कि वह मिल-मिलाकर सरकार बना ले. यह भी स्पष्ट है कि लोग मीडिया के असर में नहीं आए. मीडिया में राहुल गांधी की हवा चल रही थी जो जनता के बीच निकल गई. ज्यादातर एग्जिट पोल इन नतीजों का अनुमान लगाने में नाकाम रहे.
जो लोग इन चुनावों को 2014 की लोकसभा का सेमीफाइनल बता रहे हैं, वे कुछ ज्यादा हड़बड़ी में हैं. इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं, अगले साल पहले कर्नाटक में और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले चार और राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में. हालांकि तब भी उन नतीजों को लोकसभा चुनावों का पूर्वाभास मानने की भूल खतरनाक होगी. हम याद कर सकते हैं कि 2003 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत ने ही बीजेपी को यह गुमान दिया कि अगर वह जल्दी चुनाव कराए तो 2004 में केंद्र में लौट सकती है. लेकिन नतीजों ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया.
दरअसल इन चुनावों ने यही बताया है कि सारे तनावों-दबावों के बीच, पैसे और बाहुबल जैसी बीमारियों के बावजूद और जातिगत-सांप्रदायिक मधुमेह के रहते हुए भी हमारे लोकतंत्र के बुनियादी अवयव ठीक से काम कर रहे हैं, उसका रक्तचाप दुरुस्त है और उसकी सेहत अच्छी है.