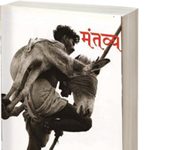हिंदी साहित्य जगत में किसी किताब का एक बेस्ट सेलर हो जाना एक चर्चा लायक घटना है. शायद यही वजह थी कि मई, 2013 में सारा हिंदी साहित्य जगत अचानक चौंक गया. लोगों को पता चला कि हिंदी की एक युवा लेखिका का एक कहानी संग्रह ‘बेस्ट सेलर’ हो गया है. यह खबर लोगों के बीच तब पहुंची जब प्रकाशन गृह वाणी प्रकाशन ने इसके उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक आयोजन किया. वहां वाणी प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अरुण माहेश्वरी ने गर्व के साथ बताया कि दो महीने के भीतर कहानी संग्रह की 1,000 प्रतियां बिकने के बाद इसे बेस्ट सेलर घोषित किया गया है. यानी 50 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली हिंदी में किसी पुस्तक की महज 1,000 प्रतियों का बिकना उसे बेस्ट सेलर का दर्जा दिलाने के लिए पर्याप्त है!
इसकी तुलना में अगर हम अंग्रेजी साहित्य पर नजर डालें तो हिंदी किताबों की बिक्री सागर में एक बूंद के समान नजर आती है. चेतन भगत के पिछले उपन्यास ‘रिवॉल्युशन 2020’ को 10 लाख प्रतियों के साथ बाजार में उतारा गया था और पहले ही दिन इसकी बिक्री लाखों में हुई. अब तक आ चुके उनके पांच उपन्यासों की बिक्री 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं अमीष त्रिपाठी की शिवा ट्राइलॉजी (द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागाज और द ओथ ऑफ वायुपुत्राज) की तकरीबन 20 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं और इससे 50 करोड़ रुपये से अधिक की खुदरा आय हो चुकी है.
अब हम हिंदी में बेस्ट सेलर वाली घटना पर वापस लौटते हैं. दरअसल इस घटना से हिंदी साहित्य जगत की कई गुत्थियों को समझा जा सकता है. इसी से यह भी समझा सकता है कि लेखन,पठन और प्रकाशन के खेल में प्रकाशक सारे नियम तय करने वाले कैसे बन बैठे हैं. सबसे पहले लेखक की बात करते हैं. पिछले साल जिन लेखिका की किताब बेस्ट सेलर घोषित की गई थी उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी आजीविका के लिए पूर्ण रूप से साहित्य लेखन पर निर्भर नहीं हैं. यदि ऐसा किसी बेस्ट सेलर की लेखिका के लिए कहा जा सकता है तो बाकी साहित्यकारों के लिए यह मानने में कोई मुश्किल नहीं है कि केवल लेखन के जरिये अपनी आजीविका चलाना उनके लिए लगभग असंभव है. वैसे यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि हिंदी के सभी स्थापित लेखक अपनी आजीविका के लिए नौकरी या व्यवसाय पर निर्भर हैं.
उधर दूसरी तरफ पाठकों की यह आम शिकायत है कि हिंदी में उत्कृष्ट और पठनीय सामग्री कम मिलती है जबकि अंग्रेजी में शोधपरक और तथ्यात्मक रचनाओं की भरमार है. हिंदी में फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबों के निम्न स्तर तथा हिंदी व अंग्रेजी किताबों की तुलना के बारे में कवि एवं दखल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार पांडेय कहते हैं, ‘चूंकि प्रकाशक पैसे नहीं देते इसलिए हिंदी के अधिकतर लेखक पार्ट टाइम लेखक हैं. नौकरी या व्यापार से बचे हुए समय में लिखने वाले. उनके पास अंग्रेजी के लेखकों की तरह शोध करने, घुमक्कड़ी करने या मूड के हिसाब से लिखने का वक्त भी नहीं और सुविधा भी नहीं.’ अशोक ने कुछ समय पहले ही अपने कुछ साथियों के साथ प्रकाशनगृह शुरू किया है.
पाठकों कमी बस एक बहाना है
यह एक बड़ा सवाल है कि तकरीबन आधा अरब लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी जिसमें देश के सर्वाधिक प्रसार वाले अखबार प्रकाशित होते हैं, उसमें किताबों की बिक्री की दशा इतनी शोचनीय क्यों है? अगर पढ़ने वाले इतने ही कम होते तो हिंदी में इतने सारे अखबार हर साल प्रसार संख्या का नया रिकॉर्ड नहीं बना रहे होते. पिछले दिनों तहलका समेत हिंदी की प्रमुख राजनीतिक और विमर्श पत्रिकाओं ने साहित्य-संस्कृति पर केंद्रित जो विशेषांक निकाले उन्हें पाठकों ने खूब पढ़ा और सराहा. इसी तरह हिंदी में साहित्य और विचार पर आधारित अनेक मासिक पत्रिकाएं निकलती हैं जिनकी अच्छी-खासी प्रसार संख्या है. ऐसे में किसी को भी इस बात पर आश्चर्य हो सकता है कि क्या ये पाठक साहित्यिक किताबों में रुचि नहीं रखते? दरअसल किताबें की बिक्री का सीधा संबंध उनकी कीमतों से जुड़ता है. यदि आप एक ही किताब, जो अलग-अलग प्रकाशनगृह ने छापी है को ही देख लें तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्यजगत में कीमतों का कोई नियम नहीं है. एक प्रकाशनगृह अगर 150 पृष्ठ की किताब को 70 रुपये में बेच रहा है तो दूसरा उसी को 200 रुपये में और तीसरा 500 रुपये में भी बेच सकता है. हिंदी के प्रतिष्ठित कवि विष्णु खरे ने कुछ अरसा पहले अपने एक आलेख में हिंदी प्रकाशन जगत पर जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा था कि वे अपनी पुस्तकों का दाम लागत से कम से कम छह गुना अधिक रखते हैं और इस तरह वे केवल संस्थागत खरीद के ही लायक रह जाती हैं. इसी आलेख में खरे यह सुझाव भी देते हैं कि पुस्तकों के मूल्य निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें लेखक, प्रकाशक और सरकार सभी के प्रतिनिधि शामिल हों. ऐसा करने से इसमें कुछ हद तक पारदर्शिता लाई जा सकती है.
आधिकारिक तौर पर इस बात को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है लेकिन हिंदी प्रकाशन जगत की एक बड़ी सच्चाई यह है कि पाठक बड़े प्रकाशकों की सोच की जद से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं. हिंदी के एक बड़े कहानीकार नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं, ‘ हमारे लेखन का मकसद है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. लेकिन हमारी तमाम शिकायतों पर प्रकाशकों का एक ही जवाब है कि हिंदी में साहित्य के पाठक नहीं हैं.’ प्रकाशकों के संबंध में इन कहानीकार की बात बिल्कुल सही प्रतीत होती है. औपचारिक-अनौपचारिक हर तरह की चर्चा में तमाम बड़े प्रकाशक पाठकों की कमी को हिंदी प्रकाशन उद्योग के लिए एक खतरे की तरह बताते हैं. यदि इस बात में सच्चाई है तो पिछले सालों दर्जनों प्रकाशन गृहों को बंद हो जाना चाहिए था? लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उल्टे बीते एक दशक में कई प्रकाशन गृह न सिर्फ स्थापित हुए बल्कि छपने वाली किताबों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. इस उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रकाशक किताबों के प्रकाशन के वक्त पुस्तकालयों और सरकारी खरीद को ही ध्यान में रखते हैं. यही वजह है कि उनकी किताबों के दाम बहुत ज्यादा होते हैं. प्रकाशन जगत के एक और स्याह पहलू को उजागर करते हुए अशोक कहते हैं, ‘कुछ बड़े लेखक जो सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज होते हैं वे बड़े प्रकाशकों के साथ होते हैं. वे सारे इंतजामात में मदद करते हैं. पाठकों की कमी का रोना दरअसल लेखकों को उनकी हद में रखने और रॉयल्टी आदि से बचने के लिए किया जाता है. इससे प्रकाशक बहुत बड़ा और लेखक बहुत छोटा बनता चला गया है.’ अशोक अपनी बात आगे बढ़ाते हुए हिंदी में बेस्ट सेलर की असलियत बताते हुए एक और बात उजागर करते हैं, ‘ हिंदी में बेस्ट सेलर जैसा कुछ नहीं होता, इसे प्रकाशक गढ़ता है. पिछले दिनों एक युवा लेखिका की बेहद औसत किताब को जबरदस्ती चर्चा में लाया गया. बेस्टसेलर घोषित किया गया. बाद में पता चला कि वह हिंदी के दो बड़े प्रकाशक भाइयों की प्रतिद्वंद्विता का फल था.’
हिंदी साहित्य जगत में कई छोटे प्रकाशक भी हैं. ये अपनी आमदनी के लिए सर्वथा अलग तरीका अपनाते हैं. ऐसा तरीका जिसे अनैतिकता की बहस से बाहर जाकर देखें तो यह अपने आप में काफी दिलचस्प है. दरअसल हिंदी पट्टी में साहित्यकार कहलाने की चाहत रखने वाले कुछ स्तरहीन लेखकों की बड़ी जमात मौजूद है. ये किसी भी कीमत पर किताब छपवाने के लिए व्याकुल रहते हैं. इनका फायदा ऐसे प्रकाशक उठाते हैं. वे लेखकों से प्रकाशन मूल्य से अधिक पैसे लेकर सौ-दो सौ प्रतियां छाप देते हैं. यहां किताब छपने से पहले ही प्रकाशक को अपने हिस्से का मुनाफा हासिल हो जाता है. खैर पाठकों को तो ऐसे ‘ साहित्यकारों ‘ से कुछ लेनादेना ही नहीं होता. फेसबुक और ब्लॉग जैसे त्वरित माध्यमों के आने के बाद ऐसे लेखकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. नतीजतन छोटे प्रकाशक भी उसी अनुपात में बढ़े हैं. हाल ही में दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इसकी एक मजेदार बानगी देखने को मिली. एक प्रकाशक ने बाकायदा लेखकों से अपील की कि वह उचित दर पर पुस्तकें छापने का उनका सपना पूरा कर सकता है. उस प्रकाशक ने न केवल किताब छापने बल्कि सभा, गोष्ठी करवाने तथा पुस्तक की समीक्षा करवाने जैसी मार्केटिंग रणनीतियां अपनाने का भी आश्वासन दिया.
रॉयल्टी का गणित
हिंदी लेखकों को मिलने वाली रॉयल्टी एक ऐसा मुद्दा है जिसको सुलझाने से यदि शुरुआत की जाए तो पाठकों और साहित्यकारों की कई शिकायतें दूर हो सकती हैं. लेखकों को उनकी हर बिकने वाली किताब पर मुनाफे का एक हिस्सा, वार्षिक आधार पर दिया जाता है. यही रॉयल्टी होती है. आमतौर पर हार्डबाउंड पुस्तकों के मूल्य का 10 से 15 फीसदी जबकि पेपरबैक पर तकरीबन 7.5 फीसदी रॉयल्टी देने का चलन है. लेकिन यह गणित कागज पर जितना आकर्षक दिखता है वास्तव में उतना है नहीं. क्योंकि लेखकों को मिलने वाली रॉयल्टी का किताबों की बिक्री से सीधा संबंध है और किताबों की बिक्री के आंकड़े प्रकाशन समूह के पास रहते हैं. ऐसे में ज्यादातर साहित्यकारों को अपनी कृतियों पर नाममात्र रॉयल्टी ही मिल पाती है. वरिष्ठ साहित्यकार मधु कांकरिया बताती हैं कि उनके चार उपन्यास और एक कहानी संग्रह राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हो चुके हैं जिनके लिए उन्हें एक साल में तकरीबन 8,000 रुपये की रॉयल्टी मिलती है. इसके अलावा वाणी प्रकाशन, किताबघर और ज्ञानपीठ से प्रकाशित किताबों के लिए कांकरिया को क्रमश: 6,000 और तीन-तीन हजार रुपये रॉयल्टी के रूप में मिले हैं. वहीं जब उनकी किताब ‘सेज पर संस्कृति’ त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय के बीए के पाठ्यक्रम में शामिल की गई तो राजकमल प्रकाशन ने उसका विद्यार्थी संस्करण प्रकाशित किया. इस नए संस्करण के बारे में काफी लिखत-पढ़त के बाद उनको 500 रुपये की रॉयल्टी दी गई जो ऊपर लिखी गई 8,000 रुपये की राशि में शामिल है.
रॉयल्टी के इस खेल को स्पष्ट करते हुए कांकरिया बताती हैं, ‘ प्रकाशकों का पूरा जोर नई किताबें छापने पर होता है क्योंकि उन किताबों की सरकारी खरीद और पुस्तकालयों में आपूर्ति आदि की संभावना रहती है. ऐसे में पुरानी किताबों की बिक्री अगर होती भी है तो उसके आंकड़े प्राय: सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं. इसका असर लेखक को मिलने वाली रॉयल्टी पर पड़ता है.’
एक सीधा गणित है कि यदि किताबें ज्यादा से ज्यादा बिकें तो लेखकों को रॉयल्टी के जरिए ज्यादा आमदनी होगी वहीं प्रकाशकों को भी फायदा होगा. लेकिन इसके लिए किताबों को पाठकों के बजट के भीतर लाना होगा. यानी उनकी कीमतों में कमी करनी होगी. किताबें सस्ती करने के खिलाफ प्रकाशक चाहे जो भी तर्क दें लेकिन यह इतना मुश्किल भी नहीं है. इस समय प्रकाशक सीधे वितरकों को अपनी किताबें बेचने के लिए 20 से 30 फीसदी तक की छूट दे देते हैं. अगर यह छूट पाठकों तक पहुंचे तो क्या किताबों की बिक्री में जबरदस्त इजाफा नहीं होगा?
हिंदी के प्रकाशक और लेखक किताबों की मार्केटिंग को भी तवज्जो नहीं देते जबकि यह किताबों की बिक्री के लिए खासी अहम है. कुछ अरसा पहले अमीष त्रिपाठी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि कोई भी लेखक अगर यह सोचता है कि अच्छी किताब खुद लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो वह गलत है. बगैर मार्केटिंग के ऐसा संभव नहीं है. भारतीय इतिहास में सबसे तेज बिक्री वाली किताबें लिखकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके अमीष ने खुद जब अपनी पहली किताब लिखी थी तो उसे बाजार में उतारने के पहले उसके कुछ चैप्टर उन्होंने प्रतिष्ठित बुक स्टोर पर रखवाए थे. ये चैप्टर वहां से खरीदारी करने वाले हर ग्राहक को मुफ्त दिए जाते थे. आश्चर्य नहीं कि बाजार में आने के पहले ही उनकी किताब की भारी मांग तैयार हो चुकी थी. शायद यही वजह है कि चेतन भगत और अमीष त्रिपाठी समेत आज देश के बेस्टसेलर लेखकों में से ज्यादातर आईआईएम के पासआउट हैं.
क्या आज की परिस्थितियों के देखते हुए यह माना जाए हिंदी साहित्य जगत अपने असली बेस्टेसेलर की खोज का कोई उपाय नहीं है और इसका निर्णय हमेशा की तरह प्रकाशक ही करते रहेंगे? युवा साहित्यकार सत्यनारायण पटेल इसका एक सटीक समाधान देते हैं, ‘ हमारे यहां लेखकों को किताबें छपवाकर अनुगृहीत होने का भाव त्यागना चाहिए. यदि उन्हें प्रकाशकों की जरूरत है तो प्रकाशकों के लिए भी वे जरूरी हैं. इस संबंध में जितनी बराबरी आएगी, उतनी अच्छी किताबें छपेंगी, उतने ज्यादा पाठक बढ़ेंगे.’