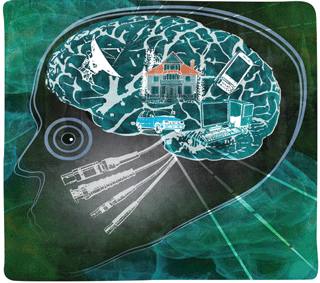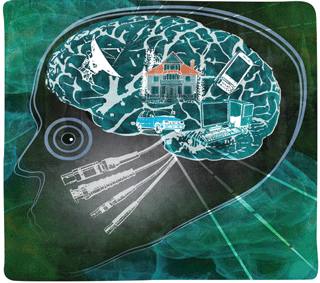 कुछ समय हुआ द संडे टाइम्स में एंड्रयू सूलिवान की टिप्पणी पढ़ी थी, द वे वी थिंक नाउ (हम आज जैसा सोचते हैं). इस विचारपरक टिप्पणी में ‘निकोलस कार’ के एक लेख का हवाला था. श्री कार टेक्नॉलाजी से जुड़े प्रसंगों, पहलुओं और विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञ हैं.
कुछ समय हुआ द संडे टाइम्स में एंड्रयू सूलिवान की टिप्पणी पढ़ी थी, द वे वी थिंक नाउ (हम आज जैसा सोचते हैं). इस विचारपरक टिप्पणी में ‘निकोलस कार’ के एक लेख का हवाला था. श्री कार टेक्नॉलाजी से जुड़े प्रसंगों, पहलुओं और विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञ हैं.
इसे पढ़ते हुए गांधीजी याद आये. याद आयी उनकी पुस्तिका ‘हिंद स्वराज’ जिसे लिखे, 100 वर्ष हो रहे हैं. ‘हिंद स्वराज’ के मौलिक विचार, तब आघात की तरह लोगों को लगे. हर विचार, चिंतन या कृति, देश, काल और परिस्थितियों के सापेक्ष होती है. लेकिन उन दिनों ही मनुष्य और मशीन के रिश्ते पर गहराई से सोचने की बात, गांधीजी ने की. आज सूचना क्रांति के इस दौर में तकनीकी विशेषज्ञ भी इन सवालों पर नए सिरे से सोच-विचार रहे हैं. सच है कि तकनीक ने जीवन को सुखद बनाया है, दुनिया समृद्ध हुई है, पर अनेक नये सवाल भी जन्मे हैं.
निकोलस कार ने दार्शनिक नीत्से का एक प्रसंग बताया है. अपने एक मित्र को नीत्से ने लिखा, हमारे लिखने का यंत्र भी, हमारे विचार गढ़ने-सोचने की प्रक्रिया में हिस्सेदार होता हैं. नीत्से पहले हाथ से लिखते थे फिर वे टाइपराइटर पर काम करने लगे. निकोलस को लगा, अगर एक टाइपराइटर का यह असर हो सकता है, तो आज गूगल का क्या असर होगा? ईमेल, ब्लॉग, गूगल पर उपलब्ध सामग्रियों के अथाह सागर में गोते लगाना, ब्राउजिंग करना, हमारे सोचने-समझने और काम के तरीके पर असर डालते हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सब मिलकर मस्तिष्क पर बंबार्डमेंट कर रहे हैं.
एंड्रयू यह सवाल उठाते हैं कि क्या इस रास्ते चिंतन-मनन संभव है? क्या इससे हमारे लिखने-पढ़ने की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा? इस क्रम में हम क्या अनमोल चीज खो रहे हैं? गहराई और शांति से सोचने-विचारने की क्षमता! चिंतन शांत परिवेश में ही संभव है, एंड्रयू ऐसा मानते हैं. वे कहते हैं कि तेज इन्फार्मेशन हाइवे जैसी चीजें मनुष्य को स्थिरचित्त नहीं रहने देंगी. ऐसे माहौल में अंदर की शांत और खामोश आवाज शायद न निकले. निकोलस कार अपने लेख में एक सज्जन ब्रूस फ्रीडमैन का जिक्र करते हैं जो मेडिसिन के क्षेत्र में लगातार ब्लाग बनाते हैं, सूचनाएं दर्ज करते हैं.
तेज इन्फार्मेशन हाइवे जैसी चीजें मनुष्य को स्थिरचित्त नहीं रहने देंगी. ऐसे माहौल में अंदर की शांत और खामोश आवाज शायद निकलना ही बंद हो जाए
वे कहते हैं कि इंटरनेट ने उनकी मानसिक आदतों को बदल दिया है, ‘मैंने पढ़ने की पूरी क्षमता खो दी है. मेरा मस्तिष्क वेब पर या छपा हुआ लंबा लेख ग्रहण नहीं कर पाता है.’ कहने का आशय है, पढ़ने की आदत घटना. पहले पुस्तकों को पढ़कर लोग बहस-चिंतन करते थे. उसमें उठाये गये सवालों पर सोचते-विचारते थे, अब वह चिंतन की प्रक्रिया छीज रही है.
टेलीविजन के सामाजिक असर पर भी लगातार अध्ययन हुए हैं. लगातार मोबाइल या टीवी से चिपके रहने के कारण, समाज या परिवार में संवादहीनता का माहौल बना है. ऐसा आकलन है कि तकनीकों के कारण आज समाज में अधिक सूचनासंपन्न नागरिक हैं, भौगोलिक दूरियां मिटी हैं, पर सार्वजिनक सवालों पर सामाजिक सरोकार घटे हैं.
यह सही है कि हमारे दौर के संकट भरे सवालों पर आज गंभीर विचार नहीं हो रहा. कुछ ही दिनों पहले लेस्टर आर ब्राउन की चर्चित पुस्तक आयी ‘ईको-इकोनॉमी: बिल्डिंग एन इकोनॉमी फार द अर्थ’. इस पुस्तक का मूल संदेश है कि हमने ऐसी अर्थव्यवस्था बना ली है, जो इस आर्थिक प्रगति की गति को नहीं बनाये रख सकती है. इससे तेजी से प्राकृतिक संपदा का क्षय हो रहा है. गंभीर पर्यावरण संकट के सवाल खड़े हो रहे हैं. और इसका असर होगा, आर्थिक प्रगति में उतार और संकट.
ब्राउन की इस चेतावनी की अनदेखी का परिणाम सामने है. द आॅब्जर्वर (10 अगस्त 2008) के साइंस संपादक की रिपोर्ट है कि पांच वर्षों में ही उत्तरी ध्रुव बर्फमुक्त क्षेत्र बन जायेगा. पहले अनुमान था कि 60 वर्ष में ऐसा होगा. शायद आज की दुनिया के लिए इससे गंभीर मुद्दा दूसरा नहीं होगा. अगर उत्तरी ध्रुव पांच वर्षों में बर्फविहीन हो जाता है, तो इस दुनिया का क्या होगा?
खाद्यान्न संकट, पेट्रोलियम संकट, पर्यावरण संकट जैसे सवाल अलग हैं. पूरी दुनिया में इन सवालों को लेकर बेचैनी न होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या सूचना क्रांति के इस दौर में मनुष्य व्यक्तिवादी हो गया है? मशीनों से जुड़कर उसने खुद एक नयी दुनिया बना ली है, जो आत्मसीमित, आत्मकेंद्रित, आत्ममुग्ध और आत्मलीन है. और इस निजी दुनिया में सिमटा मनुष्य गंभीर सार्वजनिक सवालों को तरजीह नहीं देता या इनके प्रति तटस्थ बन जाता है. जानना रोचक होगा कि ऐसी स्थिति के लिए मनुष्य और मशीन के रिश्ते कहां तक जिम्मेवार हैं?
हरिवंश जी प्रभात खबर के प्रधान संपादक हैंं